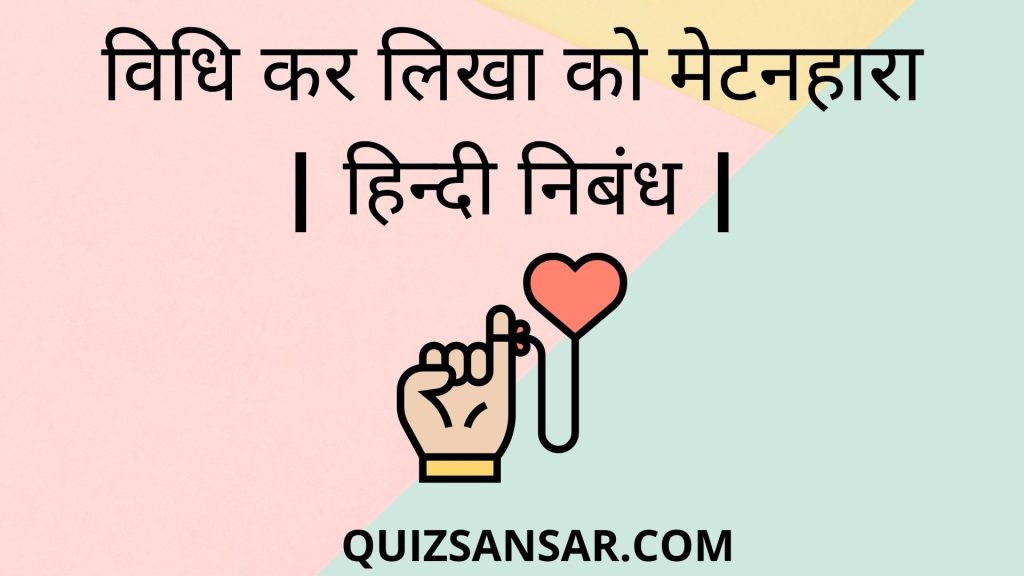पुरस्कार एवं सम्मान | PURASKAR EVAM SAMMAN |
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का पुरस्कार एवं सम्मान | PURASKAR EVAM SAMMAN | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
राष्ट्रीय पुरस्कार
भारत रत्न
- कला, साहित्य, विज्ञान, खेल तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के साथ जनसेवा के लिए यह देश का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कारों को बन्द कर दिया गया था, किन्तु 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू किया।
- यह अलंकरण काँस्य निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह 216 इंच लम्बा, 17 इंच चौड़ा तथा इंच मोटा होता है। इस अलंकरण के मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति अंकित होती है, जिसके नीचे भारत रत्न शब्द खुदे होते हैं। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिह्न और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है।
- सचिन तेन्दुलकर एवं सी एन राव को वर्ष 2014 के भारत रत्न पुरस्कार के लिए घोषित गया है।
- वर्ष 2016 के लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी और महामना मदनमोहन मालवीय (मरणोपरान्त) को दिया गया था।
- वर्ष 2019 में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को तथा नानाजी देशमुख (मरणोपरान्त) व भूपेन हजारिका (मरणोपरान्त) को दिया गया।
पद्म पुरस्कार
- भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी।
- ये पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के होते हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री |
वीरता पुरस्कार
परमवीर चक्र
वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी।
महावीर चक्र
देश का यह द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रु के दमन में अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित किया हो।
वीर चक्र
शौर्य एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार उसे प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रुओं का सामना अदम्य साहस के साथ करके उसे पीछे धकेला हो अथवा मौत के घाट उतार दिया हो।
अशोक चक्र
यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शान्तिकालीन शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी शौर्य प्रदर्शन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले बहादुर कर्मी को प्रदान किया जाता है।
कीर्ति चक्र
शौर्य का यह पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है, जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हो।
शौर्य चक्र
युद्ध की परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार
प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित | किया जाता है। इसके अन्तर्गत भारत अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड, संजय चोपड़ा अवार्ड गैधानी अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं।
साहित्य पुरस्कार
अकादमी पुरस्कार
साहित्य अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी, उत्कृष्ट साहित्य के लिए तथा अन्य दो कला व संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देती है।
इकबाल सम्मान
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त यह सम्मान उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है।
कबीर सम्मान
सर्वाधिक सम्मानित यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषा में सामाजिक उत्कृष्ट कविता लेखन के लिए दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार
यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रायोजित होता है। यह सांस्कृतिक संस्था वर्ष 1949 में शान्ति प्रसाद जैन द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 2017 का 53वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार हिन्दी लेखक ‘कृष्णा सोबती’ को दिया गया।
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2019 प्रसिद्ध मलयालम कवि ‘अक्कितम अच्युतन नम्बूदरी’ को प्रदान किया गया।
फिल्म एवं कला-संगीत पुरस्कार
दादासाहेब फाल्के पुरस्कार
सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1969 से दिया जा रहा है।
तुलसी सम्मान
राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोककला के विकास में योगदान के लिए यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
कालिदास सम्मान
रूपंकर कलाओं व रंगकर्म के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
लता मंगेशकर सम्मान
सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा उत्कृष्ट फिल्मों तथा उनसे सम्बद्ध कलाकारों को प्रदान किया जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार
- नोबेल पुरस्कार का प्रारम्भ वर्ष 1901 मे डाइनामाइट के आविष्कारक तथा प्रमुख उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुरूप किया गया।
- 1886 ई. में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में अपने उद्योगो की वार्षिक आय पुरस्कारों के लिए दान कर दी।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को दिए जाते हैं।
अर्न्तराष्ट्रीय मलाला अवार्ड
मलाला दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल इनवॉय फॉर ग्लोबल एजुकेशन्स यूथ करेज अवार्ड फॉर एजुकेशन’ प्रदान किया गया। प्रथम मलाला अवार्ड मेरठ (उत्तर प्रदेश, भारत) की जरिया सुल्ताना को मिला।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
राष्ट्रीय पुरस्कार कौन-कौन से हैं ?
भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है ?
फिल्म से संबंद्धित कौन-कौन से पुरस्कार होतें हैं ?
दादासाहेब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है ?
- Biomass – Importance of biomass, classification of energy production , pyrolysis and gasification
- Are events like ‘ Beauty Contests ‘ an insult to womenhood ?
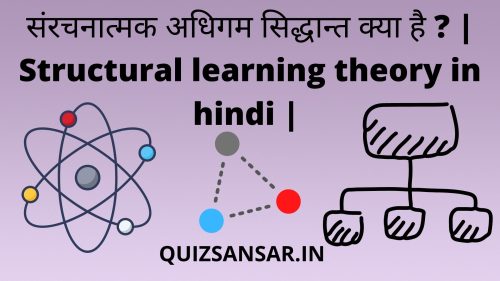
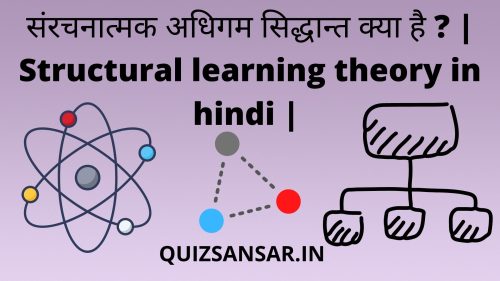
जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत | Structural learning theory in Hindi | JERO BRUNAR KA SANRACHNATMAK ADHIGAM SIDDHANT |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का जेरोमब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत | Structural learning theory in hindi | JERO BRUNAR KA SANRACHNATMAK ADHIGAM SIDDHANT | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
ब्रूनर के सिद्धांत के अन्यनाम
- संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत |
- निर्मित्तवाद |
जेरोमब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत
इस सिद्धांत के प्रवर्तक ब्रुनर को कहा जाता है | संरचनात्मकता शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुयी है। इसलिए जोरोमब्रुनर का सिद्धान्त आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है |
“ यदि बालक को कंप्यूटर का ज्ञान करवाना है तो बालक को कंप्यूटर के समस्त उपकरणों के निर्माण प्रक्रिया को बताते हुए अधिगम करवाना चाहिए। संरचनात्मक शब्द का तात्पर्य अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना है। “
संरचनात्मक अधिगम का शैक्षिक महत्व
- स्व केन्द्रित क्रिया |
- स्वयं ज्ञान का सृजन |
- नवीन ज्ञान सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर |
- पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल |
- सक्रियता व तत्परता पर बल |
- अर्थपूर्ण अधिगम व अन्वेषणात्मक अधिगम पर बल |
- ज्ञान की जाँच पर पर्याप्तता की जाँच |
- बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करता है।
- आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना |
- शिक्षक की भूमिका – निर्देशक / पथ प्रदर्शक / सरलीकृत अथवा सुविधाप्रदान |
- शिक्षक बालको के संवाद कर सकता है।
- पाठ्यपुस्तक की सहायता नहीं ली जाती |
- चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करना |
- तरीका – आगमनात्मक विधी |
- समूह बनाना – विषय सम्बन्धी समस्या देना |
- समाचार पर चर्चा |
- पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की अन्तः क्रिया |
- समस्या समाधान व निष्कर्ष |
निर्मित्तवाद के मुख्य प्रकार
इसके मुख्य तीन प्रकार हैं |
- संज्ञानात्मक निर्मित्तवाद |
- सामाजिक निर्मित्तवाद |
- त्रिज्यीय निर्मित्तवाद |
संज्ञानात्मक निर्मित्तवाद
जीन पियाजे के अनुसार –
“ बालक व वातावरण के बीच अन्तः क्रिया ज्ञान का निर्माण करती है | ”
सामाजिक निर्मित्तवाद
वाइगोत्सकी के अनुसार –
“ सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, भाषा के द्वारा ज्ञान का निर्माण | ”
त्रिज्यीय निर्मित्तवाद
जेरोम ब्रूनर के अनुसार –
“ ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है जो की बालक को विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाता है | ”
Note – ज्ञान व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही रूपों में दिया जाता है |
ब्रूनर के अनुसार संरचनात्मक अधिगम की अवस्थाएं
ब्रूनर के अनुसार संरचनात्मक अधिगम की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं |
- क्रियात्मक अवस्था |
- प्रतिबिम्बात्मक अवस्था |
- सांकेतिक अवस्था |
क्रियात्मक अवस्था
इसे विधिनिर्माण आधारित अधिगम की अवस्था भी कहतें हैं यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों के बालकों की होती है |इसे अन्य समाज शाश्त्रियों के अनुसार शैशवावस्था भी कहते हैं ?
प्रतिबिम्बात्मक अवस्था
इसे प्रतिमान आधारित अधिगम की अवस्था भी कहतें हैं यह अवस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बालको की होती है | इसे balyavastha भी कहते है इसमें ये पूर्व balyavastha ०३-०६ वर्ष एवं उत्तर बाल्यावस्था ०६-12 वर्ष की मानी जाती है |
सांकेतिक अवस्था
इसे चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था भी कहतें हैं यह अवस्था 12 वर्ष के बाद शुरू होती है |यह किशोरा अवस्था से शुरू होती है
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- माखन लाल चतुर्वेदी | हिन्दी निबंध | MAKHAN LAL CHATURVEDI |
- बाबू गुलाब राय | हिन्दी निबंध | BABU GULAB ROY |
- निर्देशन क्या है ? | directing in hindi | NIRDESHAN KYA HAI |
- Environmental pollution Essay
- what is voucher in accounting / Tally
संरचनात्मक अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है ?
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करना |
तरीका – आगनात्मक विधी |
समूह बनाना – विषय सम्बन्धी समस्या देना |
समाचार पर चर्चा |
पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की अन्तः क्रिया |
समस्या समाधान व निष्कर्ष |
जेरोमब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत क्या है ?
“यदि बालक को कंप्यूटर का ज्ञान करवाना है तो बालक को कंप्यूटर के समस्त उपकरणों के निर्माण प्रक्रिया को बताते हुए अधिगम करवाना चाहिए। संरचनात्मक शब्द का तात्पर्य अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना है।“


भाषा विकास क्या है ? | language development in hindi | BHASHA VIKAS KYA HAI |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का भाषा विकास क्या है ? | Language Development In Hindi | BHASHA VIKAS KYA HAI | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
भाषा विकास क्या है ?
- भाषा व विचार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं |
- भाषा मानसिक विकास को भी सुनिश्चित करती है |
- सोचने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |
श्रीमति हरलॉक के अनुसार –
“भाषा अन्य व्यक्तियों के विचारों का आदान – प्रदान व सूचना सम्प्रेषण की योग्यता है |”
बालक का प्रथम 6 वर्षों में भाषा विकास
जन्म से लेकर 12 माह –
भाषा भाव का विकास तेजी से होता है।
प्रथम माह –
- शिशु जीवन का आरम्भ – क्रन्दन (प्रथम भाषा) |
- भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं।
दूसरा माह –
“OOO” (मुंह का shape) बनाना, बिना ध्वनि के स्वर निकालना |
3 से 8 माह –
बबलाना (निरर्थक ध्वनियाँ)
9 माह –
ध्वनि का लगातार दोहराव | जैसे – दा दा दा , मा मा मा |
12 माह –
बालक माँ मे अच्छा क्रियाकलाप व सहयोग | जैसे –
- माँ – बेटा कप उठा दो |
- बेटा – ता ता ता |
एक शब्दीय वाक्य बोलना | जैसे –
- पानी – पानी पीना है।
- दुध – दूध पीना है |
Note – एक वर्ष का बालक सबसे पहले संख्या सीखता है |
1 से 2 वर्ष –
- 1 ½ वर्ष – दो शब्दीय वाक्य का प्रयोग |
- जैसे – दूध पानी , पानी पानी |
- 2 वर्ष – क्रियाएँ सीख जाता है |
2 से 3 वर्ष –
- 3 से 4 शब्दों का वाक्य बनाना |
- 20 से 60 प्रतिशत वाक्य अधूरे होते है।
- 2 ½ वर्ष का बालक विशेषण फिर क्रिया विशेषण सीख जाता है |
- लय का अधिक प्रयोग करता है |
3 से 4 वर्ष –
- घर वालों के साथ-साथ बाहर वालों की भी भाषा समझ आना |
- शुरू में वाक्य छोटे (6-8 शब्दों के) बाद बढ़ने लगते हैं |
- सर्वनाम का भी प्रयोग | जैसे – हम, हमारी, तुम्हारी आदि |
4 से 6 वर्ष –
- उच्चारण में परिपक्वता |
- 10-11 शब्दों में अपने वाक्य बोलना |
- भाषा – विकास शब्द भण्डार में वृद्धि |
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
भाषा विकास क्या है ?
जन्म से लेकर 12 माह तक होने वाला विकास|
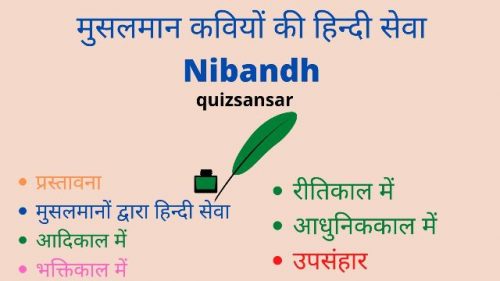
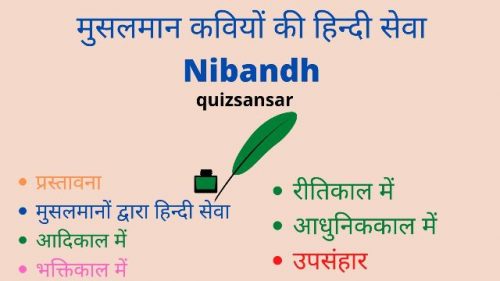
मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा nibandh
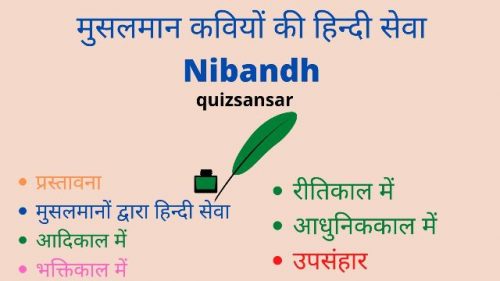
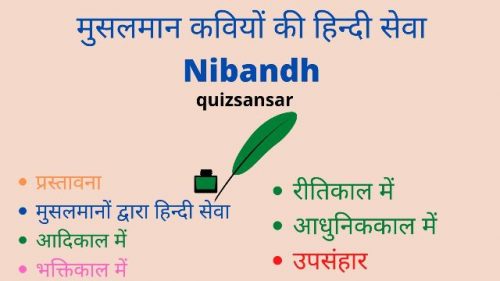
namaskar dosto आज हम आपके लिए एक नया निबंध लेकर आए हैं – मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा Nibandh , musalman kaviyo ki sewa | उम्मीद करते हैं की आपको यह पसंद आएगा |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- मुसलमानों द्वारा हिन्दी सेवा
- आदिकाल में
- भक्तिकाल में
- रीतिकाल में
- आधुनिककाल में
- उपसंहार
प्रस्तावना
राजनैतिक क्षेत्र में हिन्दू और मुसलमानों के कुछ भी सम्बन्ध रहे हों, परन्तु साहित्यिक क्षेत्र में मुसलमानों ने हिन्दी की अमूल्य सेवा की, वे हिन्दुओं के अधिक निकट आये।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए, धार्मिक मुसलमान कवियों की हिन्दी सेवा क्षेत्र में यद्यपि वे एकेश्वरवाद को मानते थे। उनका मूलमन्त्र था—
‘ला इला इल अल्लाह’
अर्थात् अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा अल्लाह नहीं। इतना होते हुए भी, वे भारतीय कृष्ण-भक्ति परम्परा से बड़े प्रभावित हुए।
पुरुषों ने ही नहीं मुसलमान स्त्रियों ने भी कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया।
यद्यपि उस समय का शासन-सूत्र मुसलमानों के ही हाथों में था, पारस्परिक कटुता दोनों ओर से हृदय में समाई हुई थी, फिर भी मुसलमानों में भी कुछ महापुरुष ऐसे थे, जो कृष्ण-भक्ति में और भक्तिकाव्य के प्रणयन में हिन्दुओं से कम नहीं थे।
इन्हीं मुसलमान भक्त कवियों की प्रशंसा में एक दिन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मुख से निम्न पंक्ति सहज ही में फूट निकली थीं –
“इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये।”
मुसलमानों द्वारा हिन्दी सेवा आदिकाल में
हिन्दी साहित्य के आदिकाल से ही मुसलमान कवियों ने अपनी अमूल्य साहित्यिक कृतियों से हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की खड़ी बोली हिन्दी के आदि कवि खुसरो अब से लगभग 700 वर्ष पहले सम्वत् 1300 के लगभग विद्यमान थे।
वे बलबन के पुत्र मुहम्मद के आश्रित कवि थे। इन्होंने अपनी पहेलियों और मुकरियों द्वारा जनता का खूब मनोरंजन किया।
अरबी, फारसी के साथ-साथ इन्हें संस्कृत का भी पर्याप्त ज्ञान था। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने काव्य रचना की थी। ये बड़े विनोदी स्वभाव के थे, इनका सांसारिक वैभव भी बढ़ा-चढ़ा था।
खुसरो की लोकप्रियता का एक विशेष कारण यह था कि उन्होंने जन-साधारण की बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा उसमें हास्य का पुट भी पर्याप्त मात्रा में रखा।
उदाहरण-स्वरूप कुछ रचनायें उद्धृत की जा रही हैं, जिनमें यह बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी-
(हास्य) खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाय,
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाय,
और फिर “ला पानी पिला।”
(मुकरी) वह आए तब शादी होय, उस बिन दूजा और न कोय।
मीठे लागें वाके बोल, क्यों सखि साजन? ना सखि ढोल ।।
(पहेली) एक थाल मोती से भरा सब के सिर पर औंधा धरा ।
भक्तिकाल में
भक्तिकाल में चार धारायें प्रवाहित हुईं दो निर्गुण के अन्तर्गत तथा दो सगुण के अन्तर्गत निर्गुण पंथ की दोनों धाराओं में मुसलमान कवियों ने अमूल्य योगदान दिया।
ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर मुसलमान थे, इसमें संदेह नहीं। नीमा नीरू के पालन-पोषण ने उनके मन में इस्लामी संस्कार पूर्णरूपेण से जमा दिए।
अपढ़ होते हुए भी, अपने अनुभवों के आधार पर कबीर ने हिन्दी साहित्य की जो सेवा की वह अमूल्य है। कबीर के हमें तीन स्वरूप प्राप्त होते हैं— कवि, ज्ञानी तथा समाज सुधारक । वे एक सच्चे समाज-सुधारक थे।
उन्होंने ज्ञान की गहन गुत्थियों को अपने विचित्र प्रतीकों और रूपकों द्वारा जनता को समझाने का प्रयत्न किया। आत्मा और माया के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कराने वाला वैचित्र्य देखिये-
जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तत् कथ्यों गियानी ||
काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी ।
तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥
इसी प्रकार, “नैया बिच नदिया डूबी जाये” आदि उलटवासियों द्वारा गम्भीर तथ्यों को समझाने की चेष्टा की है। जिस रहस्यवाद की आज के कवि छीछालेदर कर रहे हैं उसी ज्ञानात्मक रहस्यवाद के वे जन्मदाता थे।
आध्यात्मिक प्रेम और विरह की जैसी तीव्र अनुभूति हमें कबीर की रचनाओं में मिलती है, वैसी अधिकांश हिन्दी के कवियों में प्राप्त नहीं होती।
कबीर के पश्चात् प्रेमाश्रयी शाखा के प्रधान कवि मलिक मुहम्मद जायसी का नाम आता है। ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की कोटि में आते हैं।
जायसी ने अपने पद्मावत काव्य से जिन दोहों और चौपाइयों का मार्ग प्रशस्त किया था आगे चलकर तुलसी ने उन्हीं का अनुकरण किया।
जायसी का पद्मावत उनकी कीर्ति का अक्षय स्तम्भ है। इसमें लौकिक और अलौकिक प्रेम का सामंजस्य उपस्थित किया गया है –
तनु चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनि चीन्हा ।
गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत् को निरगुन पावा।
नागमीत यह दुनिया धन्या, बाँचा सोई न एहि चित बन्था ।
राघव दूत सोई सैतानू माया अलाउद्दीन सुल्तानू ॥
प्रेममार्गी शाखा तो एक प्रकार से मुसलमान कवियों की ही थी।
कुतबन शेरशाह के पिता हुसैनशाह के दरबारी कवि थे। इनका मृगावती नामक काव्य अत्यन्त प्रसिद्ध है, इस पुस्तक में चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है।
प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा वर्णन है, जो साधक के लिए बड़ी उपदेश-प्रद है। इस काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता है।
मंझन कवि ने मधुमालती की रचना की, तो उस्मान ने चित्रावली की।
इसके अतिरिक्त, शेख नवी, कासिमशाह, नूरमुहम्मद तथा फाजिलशाह आदि कवियों ने भी सुन्दर प्रेम गाथायें लिखीं।
अकबर के सेनापति बैरमखाँ के पुत्र अब्दुर्रहीम खानखाना ने भी अपने नीतिपूर्ण दोहों से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की। बरवै छन्द के तो जन्मदाता ही वे थे।
बरवै नायिका भेद और मदनाष्टक उनकी सुन्दर रचनायें हैं। बरवै का प्रारम्भिक छन्द देखिए-
प्रेम प्रीत को बिरवा चल्यौ लगाइ।
सींचन की सुधि लीजिओ कहुँ मुरझि न जाइ।
बिहारी के दोहे तो रसिकों के हृदय में घाव करते थे, परन्तु रहीम के दोहे सबको समान रूप से बाँधते रहे हैं, चाहे वे रसिक हों या नीतिज्ञ ।
रहिमन यों सुख होत है बढ़त देखि निज गोत।
ज्यों बड़री अंखियाँ निरखि आँखिन को सुख होत ।।
रहिमन अँसुवा नयन रि, जिय दुःख प्रकट करेई ।
जाहि निकारो गेह ते, भेद कहि देई ॥
राम-भक्ति शाखा में यद्यपि कोई गुसलमान कवि नहीं हुआ परन्तु कृष्ण-भक्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि ताज नामक मुसलमान महिला भी कह उठी –
नन्द के कुमार कुरबान तेरी सूरत पै।
हाँ तो मुगलानी, हिन्दुवानी है रहौंगी मैं ।।
ताज की तरह शेख नाम की रंगरेजिन भी हिन्दी की भक्त कवियित्री थी जिसके प्रेम में फँसकर आलम कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गये थे।
आलम की गणना हिन्दी के प्रसिद्ध मुसलमान कवियों में की जाती है।
यह प्रसिद्ध दोहा आलम का ही है-
कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन ।
शेख ने इनका उत्तरार्द्ध यो पूरा किया
‘कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन।’
इस पर मुग्ध होकर आलम ने शेख से विवाह कर लिया।
विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उज्ज्वल स्वरूप हमें रसखान की रचनाओं में प्राप्त होता है। पठान होते हुए भी इनका मन कृष्ण भक्ति में रमा हुआ था।
परिष्कृत भाषा और भाव सौन्दर्य की दृष्टि से रसखान का स्थान हिन्दी के गिने-चुने कवियों में है। सूरदास की छोड़कर रसखान की तुलना में कोई भी भक्त कवि नहीं ठहरता।
आज भी उनके सवैये और कवित्त बड़े प्रेम से कहे और सुने जाते हैं –
रसखान कबहुँ इन आँखिन सौं ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ।
कोटिक हूँ कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारौ।
मानुस हों तो वही रसखानि बसों बज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
भक्तिकाल के इन कवियों के अतिरिक्त कादिर और मुबारक आदि कवियों ने भी कृष्ण की वन्दना के स्वरों में अपने स्वर मिलाये, जिसका गुंजन आज भी कभी-कभी इधर-उधर सुनाई पड़ जाता है।
रीतिकाल में
हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में भी मुसलमानों ने योगदान दिया। वैसे तो रहीम ने भी रीति ग्रन्थ लिखा है। पठान सुल्तान ने बिहारी की सतसई की तरह कुण्डलियाँ लिखी थीं।
रीतिकाल में सैयद रसलीन प्रसिद्ध कवि हुए। ये सम्वत्1974 के आस-पास विद्यमान थे। इनकी अंग दर्पण नाम की पुस्तक प्रसिद्ध है।
आज भी निम्नलिखित दोहा जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अधिकांश लोग बिहारी का समझते हैं-
अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार |
जियतुं, मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार ।।
आगरे में सम्वत्1997 में नजीर अकबरावादी हुए, जिन्होंने सर्वसाधारण की भाषा में बड़ी मधुर रचनायें कीं। इन्होंने हिन्दी में उर्दू शब्दों का प्रयोग किया। एक उदाहरण देखिए-
यारो सुनो ये दधि लुटैया का बालपन।
और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ।।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन।
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन॥
आधुनिक काल में
पद्य के अतिरिक्त गद्य का हिन्दी साहित्य क्षेत्र भी मुसलमान साहित्यकारों का ऋणी है। गद्य में खड़ी बोली का श्रीगणेश भी खुसरो ने किया था।
गद्य में इंशाअल्ला खाँ ने ‘रानी केतकी की कहानी’ में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि इसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली की पुट नहीं है, आधुनिक काल में मुसलमान हिन्दी से दूर भागने लगे, इसका मुख्य कारण था, अंग्रेजों द्वारा पारस्परिक द्वेष और भेद-भावना का विष वमन करना उनकी नीति सफल हुई, मुसलमान हिन्दी और हिन्दुओं से दूर हो गए।
फिर भी मुन्शी अजमेरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, अध्यापक जहूरबख्श, मीर अहमद बिलग्रामी आदि लेखकों ने हिन्दी में अच्छा गद्य लिखा है।
उपसंहार
अब भारतवर्ष स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र भारत में सरकार हिन्दी और उर्दू की समान उन्नति के लिये प्रयत्नशील है। आज उर्दू के बहुत से विद्वान् हिन्दी में लिखने का प्रयास कर रहे हैं।
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। अतः सभी भारतीय नागरिक राष्ट्र भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं।
अगर इस post से सम्बंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं |
इन्हें भी देखें
- हिन्दी साहित्य में उपन्यासों का उद्भव और विकास
- हिन्दी साहित्य में कहानी का उद्भव एवं विकास पर निबंध
- RNA kya hai ye कितने प्रकार के होते हैं
- समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका
- हिन्दी काव्य/कविता में प्रकृति चित्रण | कवियों की दृष्टि में प्रकृति


RNA kya hai ye कितने प्रकार के होते हैं


सभी पाठकों को नमस्कार आज हम आपके लिए नई post RNA Kya Hai Ye कितने प्रकार के होते हैं लेकर आए हैं उम्मीद है आपको यह post पसंद आएगी|
RNA क्या है
RNA अधिक अणुभार वाली पालीन्युलियोटाइड से मिलकर बना है |
यह DNA से भिन्न होता है, क्योंकी इसमें डीओक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर युरेसिल होता है |
rna ki khoj kisne ki ?
आरएनए की खोज सेवेरो ओकोआ, रॉबर्ट हॉली और कार्ल वोसे ने की थी।
RNA के प्रकार
प्रत्येक कोशिका में RNA निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं-
संदेशवाहक RNA (m-RNA)
इनका निर्माणकेन्द्रक में उपस्थित DNA पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है |
ये कोशिका की कुल RNA का 3-5% होते हैं और इनका आणविक-भार 500,000 से 2,000,000 होता है |
केन्द्रक में DNA साँचे पर इनका निर्माण होता है | सन 1961 में फ्रैंसिस जैकब तथा जैक्यू मोनाड ने इन्हें संदेशवाहक RNA अणुओं का नाम दिया |
m-RNA कार्य
संदेशवाहक RNA अणु केन्द्रक से बाहर कोशिकाद्रव्य में आ जाता है | यहाँ यह केन्द्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनता है |
राइबोसोमल RNA (r-RNA)
ये RNA के संरचनात्मक अणु होते हैं | यह कोशिका की कुल RNA का 80% होता है |
rRNA केन्द्रक में DNA से उत्पन्न होता है | तीनों प्रकार के RNA में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है |
प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग rRNA का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है |
r-RNA कार्य
rRNA राइबोसोम्स की रचना में भाग लेते हैं | यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है |
स्थानान्तरण RNA(t-RNA or s-RNA)
यह कोशिका की कुल RNA का 15-18% होता है | यह कोशिकाद्रव्य में पाया जाता है |
ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं; अतः इन्हें विलेय RNA अणु भी कहते हैं | इनका निर्माण केन्द्रक में DNA के सांचे पर होता है |
t-RNA or s-RNA कार्य
ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है |
t-RNA की संरचना
वलन के कारण इनके अणुओं में द्वितीयक तथा तृतीयक स्तरों की संरचना होती है |
इसके फलस्वरूप साइटोसाल में इन अणुओं की तृतीयक स्तर की त्रिविम आकृति अत्यधिक कुण्डली “एल(L)” जैसी होती है | राबर्ट होले ने सन 1964 में tRNA की संरचना का क्लोवर लीफ माडल प्रस्तुत किया |
इस माडल के अनुसार tRNA के प्रत्येक अणु की द्विविम आकृति मटर कुल के एक पौधे तिपतिया चारा की पत्ती जैसी होती है |
ये चारों भुजाएं सभी tRNA अणुओं में एक सी होती हैं | तीन भुजाओं के सिरे लूप सदृश पाँचवी भुजा भी प्रायः होती है जिसे लम्प कहतें हैं | परन्तु यह सामान नहीं होती |
tRNA की चार भुजाएं निम्न हैं-
अंगीकार भुजा
इस भुजा को एमिनो अम्ल भुजा भी कहतें हैं, इस भुजा के छोर पर लूप नहीं होता, बल्की द्विकुण्डलिनी का एक सूत्र 5’ सिरे वाला तथा दूसरा 3’ सिरे वाला होता है | 3’ सिरे वाले सूत्र के छोर पर साइटोसीन- साइटोसीन-एडीनीन (CCA) समाक्षरों वाले राइबोन्युक्लिओटाइड्स का अनुक्रम होता है |
20 में से किसी एक विशेष प्रकार का एमीनो अम्ल अणु, अपने कार्बोक्सिल समूह (-COOH) द्वारा, साइटोसीन- साइटोसीन-ऐडेनीन (CCA) की ऐडीनोसीन के 2’ या 3’ नम्बर के हाइड्राक्सिल समूह (-OH) से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है |
यह ATP की सहायता से बनने वाला एक उच्च-ऊर्जा एस्टर बंध होता है जिसका उत्प्रेरण एक मैग्नीशियमयुक्त (Mg2+) ऐमीनोऐसिल-tRNA सिन्थेटेज नामक एंजाइम करता है |
प्रत्येक प्रकार के एमीनो अम्ल को निर्दिष्ट tRNA से जोड़ने के लिए पृथक सिन्थेटेज एंजाइम होता है |
अतः 20 प्रकार के एमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के मिलते-जुलते सिन्थेटेज एन्जाइम्स होते हैं | निर्दिष्ट एमिनो अम्ल से जुड़े tRNA को ऐमीनोऐसिलेटेड tRNA कहतें हैं |
एन्टीकोडॉन भुजा
एन्टीकोडॉन भुजा के छोर में लूप होता है | लूप के छोर पर तीन समाक्षरों का अनुक्रम होता है जी mRNA अणु के उसी त्रिगुण कोड का सम्पूरक होता है जिसमे कि AA भुजा से जुड़े एमिनो अम्ल की संकेत सूचना होती है |
इसलिए, इस त्रिगुणी समाक्षर अनुक्रम को ऐंटीकोडॉन कहतें हैं |
DHU भुजा
DHU भुजा एक एंजाइम से जुड़ती है अर्थात यह एंजाइम स्थल है |
T C भुजा
यह भुजा tRNA अणु को राइबोसोम से जुडती है |
kaisi lagi आपको हमारी यह post RNA के प्रकार उम्मीद करते हैं आपको यह post पसंद आई होगी |
यह भी पढ़ें – DNA का द्विगुणन , डीएनए का द्विगुणन का महत्व AND WORK OF DNA
अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर दें |
यह भी पढ़ें
- समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका
- हिन्दी काव्य/कविता में प्रकृति चित्रण | कवियों की दृष्टि में प्रकृति
- जल के गुण , प्रकार एवं संरचना
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन परिचय , रचनाएँ एवं lekhan शैली
- महाकवि बिहारी का जीवन परिचय
- Branches of science and its meaning
- ONE LINER CURRENT AFFAIRS
- 60 FAMOUS WRITERS AND THEIR BOOKS { प्रसिद्ध लेखक व उनकी पुस्तकें }
- one liner current affairs
- Computer ( कंप्यूटर )
Rna कितने प्रकार के होते हैं ?
राइबोसोमल RNA (r-RNA)
स्थानान्तरण RNA(t-RNA or s-RNA)
संदेशवाहक RNA (m-RNA)
RNA Full form
t rna ka full form
r rna ka full form
m rna ka full form
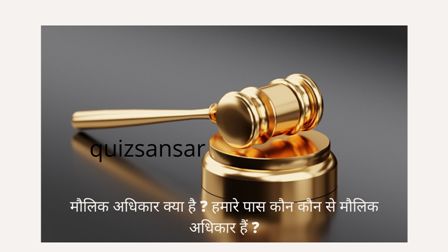
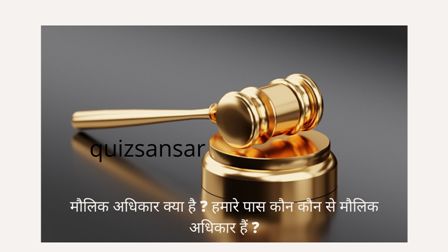
मौलिक अधिकार क्या है ? हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ?
नमस्कार दोस्तों कैसे है आप लोग आज हम फिर से आपके लिए नयी post लेकर आए हैं जिसका नाम है ” मौलिक अधिकार क्या है ? हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ? ” उम्मीद करते हैं की आपको हमारी post पसंद आएगी |
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार ( Fundamental Rights Of Indian Citizens )
मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। संविधान में दर्शाए गए छह मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रारंभ में, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44 वें संवैधानिक संशोधन 1978 में “संपत्ति के अधिकार” को हटा दिया गया। प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से नीचे दिए गए हैं।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद – 14 से 18तक )


कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान रूप से संरक्षण (अनुच्छेद 14)
धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
अस्पृश्यता का उन्मूलन और इस प्रथा का निषेध (अनुच्छेद 17)
सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर पदवी की समाप्ति (अनुच्छेद 18)
भारत के संविधान द्वारा दी गई समानता के अधिकार का अपवाद है कि किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 19 से 22तक )


स्वतंत्रता संबंधित छह अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19)
(i) भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार
(ii) हथियारों के बिना और शांति से सभा करने का अधिकार,
(iii) संगठन या संघ बनाने का अधिकार
(iv) पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार,
(v) देश के किसी भी हिस्से में निवास का अधिकार,
(vi) कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार या संचालित करने का अधिकार,
अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21): कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा।
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A): यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है।
कुछ मामलों के गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22): गिरफ्तारी के आधार के बारे में बिना बताए, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद- 23 & 24)


मानव के अवैध व्यापार और जबरन मजदूरी कराने का निषेध (अनुच्छेद 23) देह व्यापार और भीख मंगवाने और इस प्रकार के अन्य जबरन काम कराने का निषेध हैं।
कारखानों में बाल मजदुर पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24) 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें – महत्त्वपूर्ण दिवस एवं दिनांक ( importent dates and days )
4. धर्म स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 25 से 28तक )


मान्यता और पेशा चयन, धर्म चयन और इसके प्रचार की स्वतंत्रता(अनुच्छेद 25)
धार्मिक कर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)-राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थानों के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
शिक्षण संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)


अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29) जहां एक धार्मिक समुदाय अल्पमत में है, संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है।
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30) – ऐसे समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और राज्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए ऐसे शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. बीआर अंबेडकर ने “संविधान की आत्मा” कहा है।


मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, न्यायपालिका को अधिकार जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक आदेश या निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:
(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus): यह आधिकारिक या एक निजी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखा है। बाद में अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि अदालत को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया है।
(ii) परमादेश(Mandamus): इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश। यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे व्यक्ति ने करने से मना कर दिया है।
(iii) निषेध(Prohibition): यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं जाने के लिए जारी की जाती है। यह कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान जारी किया जाता है।
(iv) सर्टिओररी: यह रिट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश या फैसले को रद्द करने के लिए अदालतों या ट्रिब्यूनलों के खिलाफ भी जारी की जाती है। आदेश होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है।
(v) क्वो वारंटो(Quo warranty): यह एक कार्यवाही है जहां अदालत दावे की वैधता की जांच करती है। इसमें, एक उच्च न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को हटा सकता है यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त कर लिया है।
यह भी पढ़ें –
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
मौलिक अधिकार क्या है ? हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ?
कैसी लगी आपको हमारी ” मौलिक अधिकार क्या है ? हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ? ” post अगर इस post से सम्बंधित कोई भी सुझाव हों तो हमें जरुर दें |
Disclaimer:
quizsansar.com केवल शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाई गयी है | हम सिर्फ Internet पर पहले से उपलब्ध Link और Material provide करते है| यदि किसी भी तरह यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है तो Please हमे Mail करे- alok@quizsansar.com
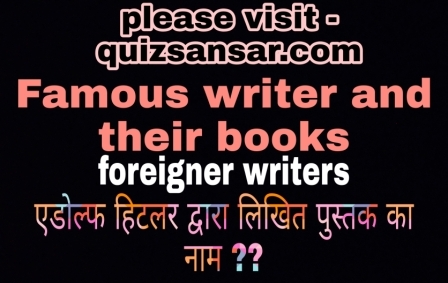
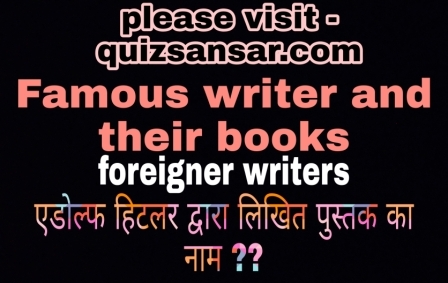
famous books and their authors
Welcome friends in https://quizsansar.com/ today we are here with the new post famous books and their authors . In this post you will get the famous book name and the name of their Author . these books are very Importent for one day exam . you can participate in the quiz in this website https://quizsansar.in/ .
64 famous foreigner writer and their books
here below you will get famous books and their authors and some very Importent foreigner writers and their books name . this is very importent for all oneday exam spacially UPSC . wystories.com
here you will find many answer.
- who is the Author of this book ?
- what is the name of book written by ?
- how a book is write?
famous books and their writer
famous books and their authors
| Writer | Their Books |
|---|---|
| पी.वी.नरसिंह राव | द.इंसाइडर |
| श्रीदत्त रामफल | इन्सेपेरेबल ह्यूमैनिटी |
| डा.सादिक हुसैन | तारीख-ए-मुजाहिद्दीन |
| स्टेनले कल्पागे | मिशन टू इंडिया |
| अरुणा शौरी | इंडियन कंट्रोवार्सीज : एसोज ऑन रिलीजन |
| मैडोना | सेक्स |
| ब्रिया लैपिंग्स | एंड ऑफ़ एम्पायर |
| मिखाइल गोर्वाचोव | पीस हिज नो आल्टरनेटिव |
| डेरेक वाल्कट | एनदर लाइफ |
| तस्लीमा नसरीन | लज्जा,फोरेशी प्रेमिका |
| गीता मेहता | ए रिवर सूत्र |
| वेद मेहता | द स्टोलेन लाइट |
| मदर टरेसा | डाउन द मेमोरी लेन |
| जगमोहन | माई फ्रोजेन टर्बुलेंस इन कश्मीर |
| एम.एफ.हुसैन | संसद उपनिसद |
| टी.एन.शेषन | डीजेनेरेशन ऑफ़ इंडिया |
| यु.आर.अन्नतमूर्ती | संस्कार |
| डा.सीताकांत महापात्र | बियोंड द वार |
| सलमान रूश्दी | सैटेनिक वर्सेज , फ्यूरी |
| सोनिया गांधी | राजीव |
| आंग सान सू की | फ्रीडम फ्रॉम फीयर |
| लाल कृष्ण आडवाणी | माई कंट्री माई लाइफ |
| कपिल देव | स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट |
| टॉम आल्टर | द लांगेस्ट रेस |
| रोमिला थापर | सोमनाथ : द मेनी वायस ऑफ़ ए हिस्ट्री |
| मनोहर जोशी | स्पीकर्स डायरी |
| अनीता देसाई | फास्टिंग , फीस्टिंग |
| टाइगर वुड्स | हाऊ आई प्ले गोल्फ |
| एपीजे अब्दुल कलाम | इग्नाइटेड माइंडस |
| मारग्रेट थैचर | द पाथ टू पॉवर |
| एम.एस.स्वामीनाथन | टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड |
| एच.जी.वेल्स | द इनभिजिबुल मैंन, द टाइम मशीन |
| लेसी फासवर्थ | इंडिया गेट |
| अटल बिहारी बाजपेयी | राजनीति की रपटीली राहें, संसद के तीन दशक |
| अरुंधती राय | द गॉड ऑफ़ स्माल थिंग |
| डेरेक वाल्कट | इन ए ग्रीन नाईट , ओमेरास |
| एम.जे.अकबर | इंडिया द सीज विदिन |
| तारिक अली | कैन पाकिस्तान सर्वाइव |
| शशि अहलुवालिया | नेताजी एंड गांधी |
| डोमिनिक लैपियर | द सिटी ऑफ़ जॉय |
| विक्रम सेठ | सूटेबल बॉय, गोल्डेन गेट |
| एन.एस.सक्सेना | इंडिया टुवर्ड्स एनार्की |
| थॉमस कोनोली | शिनडलर्स लिस्ट |
| नवीन चावला | मदर टरेसा |
| डा.हरिवंश राय बच्चन | दश द्वार से सोपान तक |
| वी.पी.मलिक | कारगिल : फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री |
| जनरल के सुंदरजी | ब्लाइंड मेन ऑफ़ हिन्दुस्तान |
| पी.सी.अलेक्जेंडर | द पेरिल्स ऑफ़ डेमोक्रेसी |
| के.गोविन्दन कुट्टी | शेषन : ए इंटीमेंट स्टोरी |
| मेनका गांधी | हेड्स एंड टेल्स |
| नेल्सन मंडेला | लॉन्ग वाक टू फ्रीडम |
| बोरिस येल्तसिन | अगेंट्स द ग्रेन |
| खालिद मोहम्मद | टू बी और नॉट टू बी |
| हिलेरी रॉथम क्लिंटन | लिविंग हिस्ट्री |
| तुषार गांधी | लेट्स किल गांधी |
| खुशवंत सिंह | बुरियल एट सी |
| झुम्पा लाहिड़ी | द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ़ मेलोडीज |
| व्लादिमीर पुतिन | फर्स्ट पर्सन |
| अमित चौधरी | ए न्यू वर्ल्ड |
| वी.एस.नायपाल | हाफ ए लाइफ |
| सतीश गुजराल | ए ब्रुश विद लाइफ |
| मेघनाद देसाई | रीडिस्कवरी ऑफ़ इंडिया |
| बेनजीर भुट्टो | डॉटर ऑफ़ द ईस्ट |
| स्टीफन हाकिंग | द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ़ टाइम |
famous books and their authors
34 foreigner writer and their books
| Wriiter | Their books |
|---|---|
| एडम स्मिथ | वेल्थ ऑफ़ नेशंस |
| अलबर्ट आइन्स्टीन | द वर्ल्ड एज आई सी इट |
| आर्थर हेले | एयरपोर्ट |
| सैमुअल हर्ष | प्राइस ऑफ़ पावर |
| दांते | डिवाइन कॉमेडी |
| होमर | ओडीसी, इलियड |
| हेनरी मिलर | ट्रोपिक ऑफ़ कैंसर |
| न्यूटन | प्रिन्सीपिया |
| जॉन मिल्टन | पैराडाइज लास्ट |
| प्लेटो | रिपब्लिक |
| गुन्नार मिर्डल | अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा |
| जॉर्ज आर्बिल | फार्म हाउस, एनीमल पार्क |
| शेक्सपियर | कॉमेडी ऑफ़ एरर्स, एज यु लाइक इट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो |
| जेड.ए.भुट्टो | ग्रेट ट्रेजडी |
| जार्ज बर्नार्ड शा | मैंन एंड सुपर मैंन, एपिल कार्ट, आर्म्स एंड द मैंन, सीजर एंड क्लीयोपेट्रो |
| हेराल्ड जे. लाश्की | डाईलेमा ऑफ़ आवर टाइम, ग्रामर ऑफ़ पोलिटिक्स |
| मैक्सिकम गोर्की | मदर |
| माओ-त्से-तुंग | ऑन कंट्राडिक्सन |
| एडोल्फ हिटलर | मीन केम्फ़ |
| ए.एल.बाशम | द वंडर दैट वाज इंडिया |
| अरस्तू | पॉलिटिक्स |
| डायना मोस्की | द लाइफ ऑफ़ कंट्रास्ट |
| ई.एम.फोस्टर | ए पैसेज टू इंडिया |
| लियो टाल्सटाय | वार एंड पीस |
| हेराल्ड माइकमिलन | राइजिंग द स्ट्राम |
| कैथरीन मेयो | मदर इंडिया |
| जे.एम.बेरी | हिन्दू सिविलाईजेसन |
| रूसो | द सोशल कांट्रैक्ट |
| मैकियाबेली | द प्रिंस, ऑन द आर्ट ऑफ़ वार |
| चार्ल्स डार्विन | डिसेंट ऑफ़ मैंन |
| चार्ल्स डिकिंग | ए टेल टू सिटीज , पिकनिक पेपर्स , ओलिवर ट्विस्ट,डेविड कापरफील्ड |
| एडवर्ड थामसन | फेयरवेल टू इंडिया |
| जे.के.गालब्रेथ | द चाइना पैसेज , द नेचर ऑफ़ मास पावर्टी एम्बेसडर्स जनरल , दि ट्राम्फ |
| विंसेट चर्चिल | गैदरिंग स्टोर्म्स , हिस्ट्री ऑफ़ द सेकेण्ड वर्ल्ड वार |
| एच.डब्लू. लागफेलो | साम ऑफ़ लाइफ |
अगर आपको हाम्मारी यह post famous books and their authors पसंद आई हों तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा कारण ना भूलें |
read these 6 post also .
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000


- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon


- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300


- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi


- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi

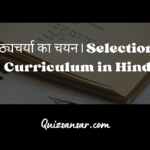
- पाठ्यचर्या चयन में प्रमुख समस्याएँ | Main Problems in Curriculum Selection in Hindi


- ज्ञान की प्रकृति एंव उद्देश्य | Nature of Knowledge in Hindi

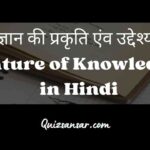
- ज्ञान के स्रोत | Sources of Knowledge in Hindi


- ज्ञान का वर्गीकरण | Classification of Knowledge in Hindi


- ज्ञान से सम्बन्धित विश्वास | Beliefs Related to Knowledge in Hindi