

विकासवादी सुखवाद के समबन्ध में स्पेन्सर का योगदान
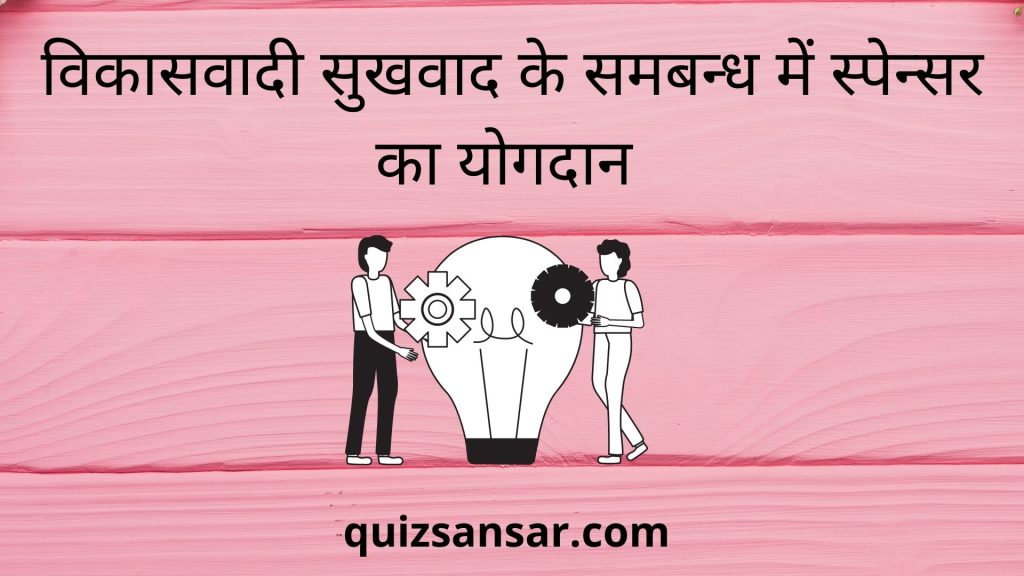
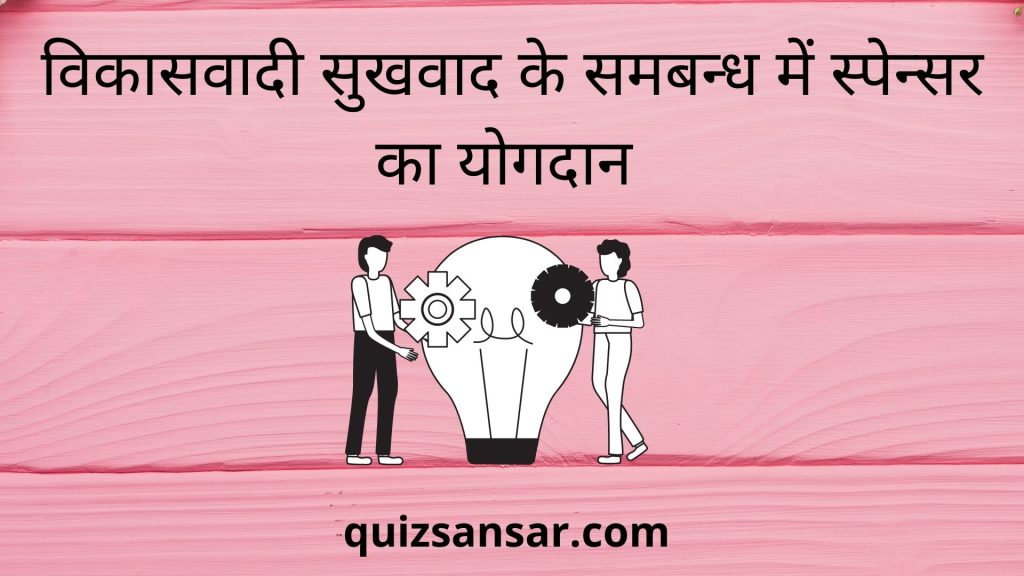
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है विकासवादी सुखवाद के समबन्ध में स्पेन्सर का योगदान उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
हरवर्ट स्पेन्सर, लेजली, स्टीफन, अलेक्जेण्डर ने जिस सुखवाद को माना है उसे विकासवादी सुखवाद कहा जाता है। क्योंकि इन लोगों में नैतिक नियमों को जीव के विकास के नियमों के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया है।
आधुनिक सुखवादियों में स्पेन्सर का नाम विकासवादी सुखवादियों में प्रमुख है, जिन्होंने डार्विन के विकासवाद के आधार पर ही अपने विकासवादी सुखवाद की स्थापना की है। स्पेन्सर ने विकासवाद के आधार पर ही सभी सामाजिक और नैतिक नियमों को समझने का प्रयास किया है।
इन्होंने जिस नैतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वह विकासवादी सुखवाद है। स्पेन्सर के सिद्धान्त को विकासवादी सुखवाद इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने विकासवाद तथा सुखवाद दोनों को आधार मानकर मनुष्य के आचरण, व्यवहार तथा नैतिक नियमों की व्याख्या की है।
अतः स्पष्ट है स्पेन्सर ने डाविन से विकासवादी सिद्धान्त को लिया तथा सुखवादियों से सुखवाद के सिद्धान्त को लेकर विकासवादी सुखवाद का सिद्धान्त नीतिशास्त्र में लागू किया।
Table of Contents
विकासवाद और स्पेन्सर
स्पेन्सर ने डार्विन के विकासवादी सिद्धान्त को ही स्वीकार करते हुये ‘विकास’ की परिभाषा की और बताया कि असंगठन से संगठन की ओर, सरल से जटिल की ओर, तथा एकता से अनेकता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का नाम ही विकास है। डार्विन ने जहाँ इस सिद्धान्त को जीवों के विकास तक सीमित रखा वहाँ स्पेन्सर ने इसे विचारों के विकास में भी प्रयुक्त किया।
सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आदि विचारों का विकास इसी प्रक्रिया से हुआ। सारांश यह है कि नैतिक नियमों को स्पेन्सर ने, जैविक नियमों में प्राप्त किया है। नीतिशास्त्र का मूल आधार जैविक नियम है। नैतिक नियमों की व्याख्या विकासवादी दृष्टि से की गई है। स्पेन्सर की दृष्टि में नैतिकता का विकास पशुओं के नैतिकता-हीन जीवन से हुआ है।
विकासवादी सुखवाद के सिद्धात
स्पेन्सर के विकासवादी सुखवाद के निम्नलिखित सिद्धान्त है –
- स्पेन्सर ने विकासवादी धारणा के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों को शुभ-अशुभ, सत् -असत् सिद्ध करने का प्रयास किया है।
- जहाँ एक ओर स्पेन्सर विकासवाद के आधार पर मान-व्यवहार को शुभ-अशुभ सिद्ध करते हैं वहीं दूसरी ओर सुखवाद के आधार पर भी मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए उसका सिद्धान्त विकासवादी सुखवाद कहलाता है। सुखवादियों की तरह उन्होंने भी सुख को परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार सुखद जीवन शुभ और दुखद जीवन अशुभ होता है। अर्थात् पूर्ण रूप से शुभ या सत् व्यवहार वह होता है जो दुःख विहीन सुख प्रदान करता है। यहाँ भी स्पेन्सर समायोजन को ही महत्त्व देते हैं।
- सन्निकट लक्ष्य जीवन की लम्बाई-चौड़ाई हैस्पेन्सर जीवन का परम लक्ष्य सुख को मानते हैं। इस अर्थ में उनका सुखवादियों से पूर्ण मतैक्य है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, परन्तु सन्निकट तथा तात्कालिक लक्ष्य जीवन की लम्बाई और चौड़ाई है। जीवन की लम्बाई से उनका मतलब है दीर्घ और स्थायी जीवन दार्घ और स्थायी जीवन तभी सम्भव है जब मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो । स्पेन्सर शारीरिक स्वस्थताको महत्त्व देते हैं।
- स्पेन्सर के आत्मरक्षण जाति-रक्षण के सिद्धान्त से ही नैतिकता का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वार्थ और परार्थ भी जुड़ा हुआ है। अन्य सुखवादी दार्शनिकों की तरह स्पेन्सर भी स्वार्थ और परार्थ की चर्चा करते हैं परन्तु कुछ सुखवादियों जैसे हाब्स तथा बेन्थम की तरह स्पेन्सर यह नहीं मानते कि मनुष्य स्वभावतः पूर्णतया स्वार्थी होता है। स्पेन्सर के अनुसार मनुष्य में स्वार्थ प्रवृत्ति के साथ परार्थ-प्रवृत्ति भी होती है। उन्होंने विकासवादी धारणा के आधार पर यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को देखकर यही पता चलता है कि वह अपने हित को देखते हुए समाज के हित का भी ध्यान रखता है। स्पेन्सर की दृष्टि में स्वार्थ की प्रवृत्ति निन्दनीय नहीं है। इसका अपना महत्त्व और स्थान है, क्योंकि इसी के कारण मनुष्य अपनी रक्षा और विकास कर सका है।
- नैतिक चेतना की उत्पत्ति के लिए स्पेन्सर बेन्थम की तरह बाह्य दबाव को मानते हैं। इनकी दृष्टि में मनुष्य में नैतिकता की भावना बाहरी दबाव के कारण उत्पन्न होती है। ये बाह्य दबाव हैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इनके कारण ही नैतिक बाध्यता और कर्त्तव्य बोध की उत्पत्ति होती है। इन तीनों बाह्य कारकों के अतिरिक्त स्पेन्सर ने मिल के समान एक आन्तरिक दबाव को भी स्वीकार किया है। इस आन्तरिक दबाव को स्पेन्सर ‘नैतिक नियंत्रण’ कहते हैं। मिल के शब्दों में यही आन्तरिक आदेश है। यही नैतिक बाध्यता और कर्त्तव्य-भावना है। इसी से सत् कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और असत् कर्म करने से यही मना करता है परन्तु स्पेन्सर का विचार है कि नैतिक चेतना का यह रूप स्थायी नहीं कहा जा सकता। इसके विषय में उनका कहना है कि कर्त्तव्य बोध या नैतिक बाध्यता स्थायी नहीं है। जितनी शीघ्रता से नैतिकीकरण में विकास और वृद्धि होती है, उतनी ही शीघ्रता से उसमें कमी होगी। प्रारम्भ में तो नैतिक बाध्यता का बोध होता है, परन्तु अन्त में वह विलीन हो जाता है। इस प्रकार कर्म बिना बाध्यता के ही होने लगता है।
नैतिक चेतना के विकास की धारणा से स्पेन्सर नैतिकता के विकास की एक ऐसी स्थिति की ओर संकेत करते हैं जिसमें व्यक्तियों का पारस्परिक संघर्ष और विरोध समाप्त हो जाएगा। पूर्ण समायोजन की स्थिति में नैतिक नियम अनावश्यक हो जाएँगे। व्यक्ति समाज के हित में ही अपना हित समझता है।
यह अवस्था निरपेक्ष नैतिकता की अवस्था है। निरपेक्ष-नैतिकता का अर्थ है, वह नैतिकता जो किसी देश, काल तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। नैतिक नियम स्वयं में अनिवार्य और स्वाभाविक होते हैं। उन नियमों का पालन व्यक्ति सहजता तथा स्वाभाविक रूप में करता है।
इसका विरोधी मत सापेक्ष नैतिकता है, जिसका अर्थ यह है कि नैतिकता, देश, काल तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसमें देश, काल तथा परिस्थितियों की बाध्यता रहती है। व्यक्ति बाध्य होकर नैतिक नियमों का पालन करता है। स्पेन्सर विकास की प्रक्रिया में निरपेक्ष नैतिकता की बात करते हैं।
स्पेन्सर ने विकासवादी सिद्धान्त के आधार पर न्याय की भी व्याख्या की है। न्याय का महत्त्व मानव-जीवन तक ही नहीं सीमित है। यह तो सामूहिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी प्राणियों के जीवन में महत्त्वपूर्ण है। स्पेन्सर न्याय के सूत्र की चर्चा इस प्रकार करते हैं योग्यतम की विजय हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भले बुरे कर्मों के सुखप्रद अथवा दुःखप्रद फल प्राप्त होना चाहिये।
स्पेन्सर के अनुसार न्याय के दो नियम हैं –
- समाज में जो सदस्य जितना ही असहाय हो उसे दूसरों का उतना ही सहयोग तथा संरक्षण मिलना चाहिए। इस नियम से प्राणियों के अस्तित्त्व और विकास में सहायता मिलती है।
- समाज के सदस्यों को जो लाभ मिले वह उनकी योग्यता की माप उसके अस्तित्त्व की दशाओं को बनाए रखने की योग्यता से होनी चाहिए। यदि प्रथम नियम तोड़ा जाता है तो असहाय लोगों का अस्तित्त्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा नियम सभी प्राणियों पर लागू होता है- प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का सुखद, दुःखद परिणाम मिलना चाहिए।
व्यक्ति को न्याय की दृष्टि से कार्य करने की स्वतन्त्रता तो आवश्यक है, साथ ही विकास का समान अवसर भी उसे मिलना चाहिए। स्पेन्सर की दृष्टि में व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य को सम्पादित करने की स्वतन्त्रता है, जिससे किसी दूसरे की स्वतन्त्रता में बाधा न उत्पन्न हो ।
न्याय का यह ऐसा सिद्धान्त है जिससे मनुष्य की स्वतन्त्रता को समान रूप से महत्त्व दिया गया है। इसी नियम के अनुसार आचरण करना मनुष्य का कर्त्तव्य है। समानता के विषय में स्पेन्सर की धारणा है कि समाज में न्याय का अस्तित्त्व बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले, परन्तु यह समानता व्यक्ति की क्षमता और योग्यता के अनुसार ही हो।
इसी में न्याय है। इस सम्बन्ध में स्पेन्सर साम्यवादी विचारधारा से सहमत नहीं है। समानता के न्याय के साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार सुविधा और अवसर मिलना चाहिए।
स्पेन्सर के अनुसार यदि साम्यवादियों का यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय तो इससे ‘योग्यतम की विजय के सिद्धान्त का उल्लंघन हो जाता है। इस सिद्धान्त को तोड़ने से सम्पूर्ण मानव जाति की हानि होगी। समानता का न्याय इस अर्थ में है कि सभी को कर्मों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और प्रत्येक कर्त्ता को अपने किए गए कर्मों की भलाई-बुराई प्राप्त होनी चाहिए।
स्पेन्सर का योगदान
नीतिशास्त्र के क्षेत्र में स्पेन्सर का योगदान स्वीकार करने योग्य है, इसमें सन्देह नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान की अन्य शाखाओं में ज्ञान के नियमों के उद्भव और विकास को जानना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में भी उसके नियमों का उद्भव और विकास ज्ञात करना आवश्यक और उपयोगी है।
इस प्रकार के ज्ञान से नैतिकता का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। स्पेन्सर की बहुत बड़ी देन व्यक्ति और समाज के बीच उचित समायोजन का सिद्धान्त है। मनुष्य का सामाजिक जीवन तभी सफल कहा जा सकता है जब शुभ कर्म किये जायें।
स्पेन्सर ने शुभ कर्मों के आधार पर ही उचित समायोजन को स्थापित करने पर बल दिया है। विकास अग्रसर होने का घोतक है, और स्पेन्सर ने विकास की इसी अग्रगति की संभावना को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष नैतिकता की घोषणा की है। नैतिकता का यह स्तर स्वर्गिक राज्य के अवतरण की घोषणा है, वर्तमान समय में यह काल्पनिक और स्वप्निल प्रतीत तो अवश्य होता है, परन्तु इसकी कल्पना ही सुखद है। यदि समाज इस ओर अग्रसर हो तो कल्पना ही साकार रूप ले सकती है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
विकासवादी सुखवाद में स्पेन्सर का योगदान क्या था ?
नीतिशास्त्र के क्षेत्र में स्पेन्सर का योगदान स्वीकार करने योग्य है, इसमें सन्देह नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान की अन्य शाखाओं में ज्ञान के नियमों के उद्भव और विकास को जानना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में भी उसके नियमों का उद्भव और विकास ज्ञात करना आवश्यक और उपयोगी है।
विकासवादी सुखवाद के सिद्धात क्या हैं ?
स्पेन्सर ने विकासवादी धारणा के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों को शुभ-अशुभ, सत् -असत् सिद्ध करने का प्रयास किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय आयोजित होने वाले खेल | International organized sports |
- खेल जगत | एथलेटिक्स | मैराथन |
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms
