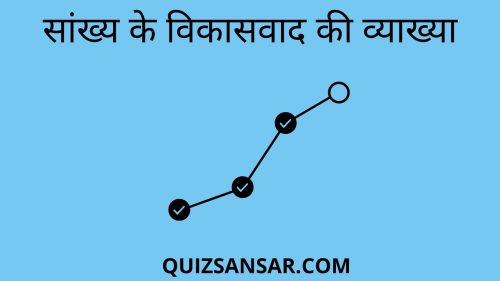
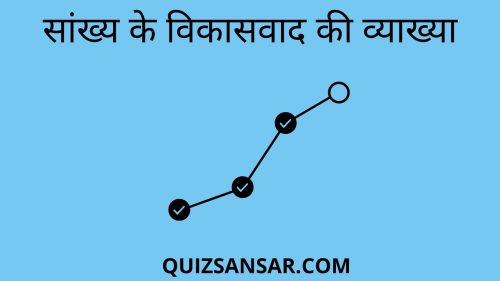
सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
विकास की प्रक्रिया-प्रकृति-पुरुष संबंध
संसार की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया से निष्पादित होती है अर्थात् जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है तभी संसार की उत्पत्ति होती है प्रकृति और पुरुष का संयोग दो भौतिक द्रव्यों जैसा साधारण संयोग नहीं है। यह एक प्रकार का विलक्षण संयोग है। प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव वैसा ही पड़ता है जैसे विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर जब तक दोनों का किसी तरह सम्बन्ध नहीं होता, जब तक संसार की सृष्टि नहीं हो सकती, किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति और पुरुष तो एक-दूसरे से भिन्न और विरुद्ध धर्म के हैं। तब फिर उनका पारस्परिक सहयोग कैसे सम्भव है? सांख्य इसके उत्तर में कहता है जैसे एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों मिलकर परस्पर सहयोग के साथ जंगल पार कर सकते हैं, उसी प्रकार जड़ प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष में दोनों परस्पर मिलकर एक-दूसरे की सहायता से अपना कार्य सम्पादित कर सकते प्रकृति दर्शनार्थ पुरुष की अपेक्षा रखती है और पुरुष कैवल्यार्थ प्रकृति की सहायता लेता है।
सृष्टि के पूर्व सभी गुण साम्यावस्था में रहते हैं। प्रकृति और पुरुष का सानिध्य होने पर इस मायावस्था में विकार उत्पन्न होता है। इस अवस्था को गुण-क्षोम कहते स्वभावतः क्रियात्मक है परिवर्तनशील होता है और तक उसके कारण और गुणों में भी स्पन्दन होने सर्वप्रथम रजोगुण जो लगता है और इसी प्रकार क्रमश: तीनों गुणों का पृथवकरण और संयोजन होता है और न्यूनाधिक अनुपातों में उनके संयोगों के फलस्वरूप नाना प्रकार के संसारिक विषय उत्पन्न होते हैं।
महत् अथवा बुद्धि = महर्षि कपिल के अनुसार सांख्य में विकास की प्रथम कृति महत् या ‘बुद्धि’ का प्रादुर्भाव है। यह प्रकृति का प्रथम विकार है, बाह्य जगत् की दृष्टि से यह विराट बीज स्वरूप है अतएव महत् कहलाता है। आन्तरिक दृष्टि से यह वह बुद्धि है तो जीवों में विद्यमान रहती है। बुद्धि का विशेष कार्य निश्चय और अवधारण है। उसके द्वारा हो ज्ञाता-ज्ञेय का भेद और किसी विषय का निर्णय निश्चित होता है। सत्वगुण के अधिक्य से बुद्धि का उदय होता है। उसका स्वाभाविक धर्म स्वयं को तथा वस्तुओं को प्रकाशित करना है। तत्त्व की अधिक वृद्धि होने से बुद्धि में सत्त्वगुण की अधिकता होती है और इसी प्रकार तक की वृद्धि की सहायता से पुरुष अपना और प्रकृति का भेद समझकर अपने यथार्थ स्वरूप की विवेचना कर सकता है। बुद्धि आत्मा से भिन्न है क्योंकि पुरुष या आत्मा समस्त भौतिक द्रव्यों और गुणों से परे है। इन्द्रियों और मन का व्यापार बुद्धि के लिए है और बुद्धि का व्यापार आत्मा के लिए है।
अहंकार
प्रकृति का दूसरा विकार ‘अहंकार’ है। अहंकार महत् से उत्पन्न होता है। कपिल ने कहा है‘अभिमानोहेकार’ अभिमान ही अहंकार है। अहंकार के कारण ही पुरुष अपने को कर्त्ता, कामी और स्वामी समझने लगता है। अहंकार ही समस्त व्यवहारों का मूल है। इन्द्रियों द्वारा सर्वप्रथम विषयों का प्रत्यक्ष होता है फिर वह विषयों पर विचार करके उनका स्वरूप निर्धारित करता है। उन विषयों में हमारा, मेरा और मेरे लिए का अहंकार जाग्रत हो सकता है।
‘अहंकार’ तीन प्रकार के माने गये हैं –
वैकारिक अथवा सात्त्विक
इसमें सत्वगुण प्रधान होता है। सार्वभौम रूप से यह मनस, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न करता है।
भूतादि या तामस
इसमें तमस गुण प्रधान होता है। विश्वरूप में यह पञ्च तन्मात्राओं की उत्पत्ति करता है।
तैजस अथवा राजस्
इसमें राजस गुण प्रधान होता है। विश्व रूप में यह सात्त्विक और तामस गुणों के लिए शक्ति प्रदान करता है।
अहंकार से सृष्टि या उपरोक्त क्रम सांख्यकारिका में दिया गया है, परन्तु विज्ञानभिक्षु ने सांख्य में दिया गया है। परन्तु विज्ञानभिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य में मन को ही एकमात्र ऐसी इन्द्रिय माना है जो कि सत्वगुण प्रधान है और सात्विक अहंकार होता है। शेष दस इन्द्रियाँ राजस अहंकार का और मंच तन्मात्र तामस अहंकार का परिणाम है।
मन
मन का सहयोग ज्ञान और कर्म दोनों में आवश्यक है। यह आभ्यान्तकि इन्द्रिय है और यही अन्य इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर प्रेरित करता है। सूक्ष्म होते हुए भी यह सावयव है और भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो सकता है। ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ बाह्य कारण हैं। प्राण की क्रिया अन्तःकरण है। प्राण की क्रिया अन्तःकरण से प्रवर्तित होती है। अन्तःकरण को बाह्य इन्द्रियाँ प्रभावित करती हैं। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्रहीत प्रत्यक्ष निर्विकल्प होता है। मन उसका स्वरूप निर्धारित करके उसे सविकल्प प्रत्यक्ष के रूप में परिणित करता है। अहंकार प्रत्यक्ष विषयों पर स्वत्व जमाता है। वह उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल विषयों में राग तथा प्रतिकूल विषयों से द्वेष रखता है। बुद्धि इन विषयों का ग्रहण या त्याग करने का निश्चय करती है। तीन अन्तःकरण और दस बाह्य करण मिलकर त्रयोदशकरण कहलाते हैं। बाह्य इन्द्रियाँ वर्तमान विषयों से ही सम्बन्ध रखती हैं जबकि आभ्यन्तरिक इन्द्रियाँ भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कालों के विषयों से सम्बन्ध रखती हैं।
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ
नेत्र, श्रवण, घ्राण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनसे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श का ज्ञान होता है। ये अहंकार के परिणाम हैं और पुरुष के निमित्त उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण एक-दूसरे को दबाने की चेष्टा करता है। जिस वस्तु में जो गुण प्रबल रहता है वैसा ही उस वस्तु का स्वभाव बन जाता है। इन्हीं गुणों के कारण ही संसार की समस्त वस्तुओं को इष्ट, अनिष्ट तथा तटस्थ इन तीन वर्गों में बाँटा जाता है। ये तीन गुण निरंतर परिवर्तनशील है। ये एक क्षण भी अविकृत नहीं रह सकते क्योंकि विकार उसका स्वभाव है।
सरूप और विरूप परिणाम
गुणों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं-सरूप और विरूप। प्रलयावस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खिंचकर स्वयं अपने में परिणत हो जाता है। इस प्रकार सत्व, सत्व में, रज-रज में और तम, तम में परिणत हो जाता है। यह परिणामस्वरूप परिणाम कहलाता है। पृथक्-पृथक् रहने के कारण इस अवस्था में गुण कोई काम नहीं करता। सृष्टि के पूर्व भी यही साम्यावस्था रहती है। दूसरे शब्दों में, वे अस्फुटित रूप से ऐसे अव्यक्त पिंडरूप में रहते हैं जिसमें न रूपान्तर है, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गन्ध और न कोई विषय होता है। यही साम्यावस्था सांख्य की ‘प्रकृति’ है। दूसरे प्रकार के परिणाम तब उत्पन्न होता है जब गुणों में से एक प्रबल हो उठता है और शेष दो उसके अधीन हो जाते हैं। इस स्थिति में ही विषयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का परिणाम विरूप परिणाम कहलाता है। इसी से सृष्टि का प्रारम्भ होता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
- सुखवाद क्या है?
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
अहंकार क्या है ?
प्रकृति का दूसरा विकार ‘अहंकार’ है। अहंकार महत् से उत्पन्न होता है। कपिल ने कहा है‘अभिमानोहेकार’ अभिमान ही अहंकार है।
सरूप और विरूप के क्या परिणाम हैं ?
गुणों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं-सरूप और विरूप। प्रलयावस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खिंचकर स्वयं अपने में परिणत हो जाता है। इस प्रकार सत्व, सत्व में, रज-रज में और तम, तम में परिणत हो जाता है। यह परिणामस्वरूप परिणाम कहलाता है। पृथक्-पृथक् रहने के कारण इस अवस्था में गुण कोई काम नहीं करता। सृष्टि के पूर्व भी यही साम्यावस्था रहती है। दूसरे शब्दों में, वे अस्फुटित रूप से ऐसे अव्यक्त पिंडरूप में रहते हैं जिसमें न रूपान्तर है, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गन्ध और न कोई विषय होता है। यही साम्यावस्था सांख्य की ‘प्रकृति’ है। दूसरे प्रकार के परिणाम तब उत्पन्न होता है जब गुणों में से एक प्रबल हो उठता है और शेष दो उसके अधीन हो जाते हैं। इस स्थिति में ही विषयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का परिणाम विरूप परिणाम कहलाता है। इसी से सृष्टि का प्रारम्भ होता है।

I was eagerly searching for detail knowledge on SAANKHYA YOG…..Finally i got through this website/article….An excellent explanation…Thanks a lot…!