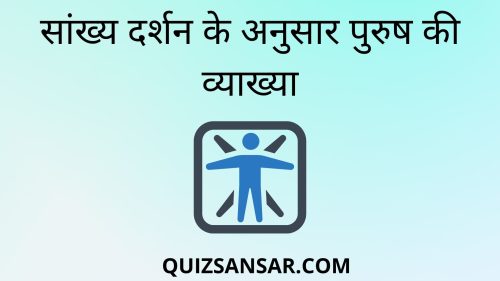
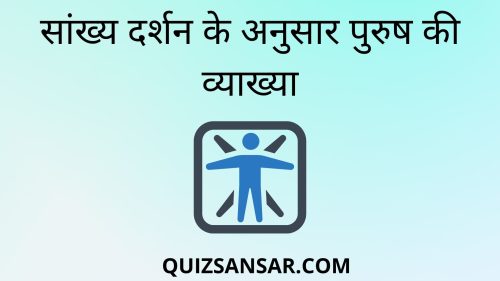
सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
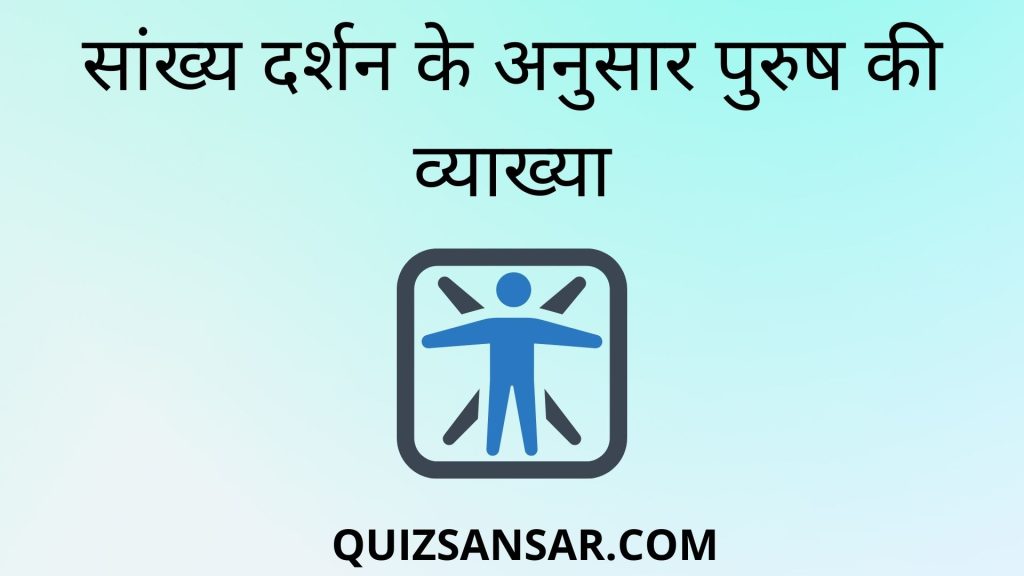
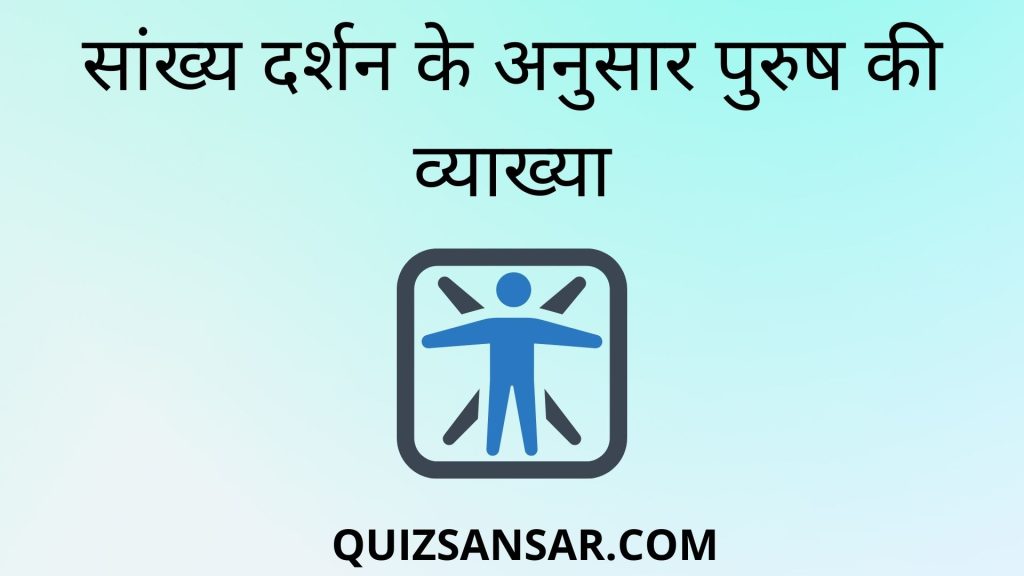
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
पुरुष (आत्मा) का अस्तित्त्व
पुरुष या आत्मा-स्वरूप-सांख्य दर्शन का एक तत्त्व तो प्रकृति है, दूसरा तत्त्व पुरुष या आत्मा है। ‘मैं’ ‘मेरा’ यह सभी व्यक्तियों का सहज स्वाभाविक अनुभव है जिसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्त्व अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए सांख्य कहता है कि आत्मा (पुरुष) का अस्तित्त्व स्वयंसिद्ध (स्वतः प्रकाश) है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया जा सकता।
जहाँ तक आत्मा के अस्तित्त्व में सभी सम्प्रदायों में मतैक्य है वही आत्मा के स्वरूप में नाना मत मतान्तर है। जहाँ तक सांख्य का प्रश्न है सांख्य के अनुसार आत्मा (पुरुष) शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। यह सांसारिक विषय नहीं है। मस्तिष्क, स्नायुमंडल या अनुभव-समूह को आत्मा समझना भूल है। आत्मा वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में रहता है वह कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं, किन्तु स्वतः चैतन्य स्वरूप नहीं। चैतन्य इसका गुण नहीं स्वभाव है। सांख्य वेदान्त की तरह आत्मा को आनन्दस्वरूप नहीं मानता। आनन्द और चैतन्य दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं अतएव उन्हें एक ही पदार्थ का तत्त्व मानना उचित नहीं। पुरुष या आत्मा केवल द्रष्टा है जो प्रकृति से परे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उनका ज्ञान प्रकाश सर्वदा बना रहता है, जबकि ज्ञान विषय बदलते रहते हैं, किन्तु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता है वह नहीं बदलता। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। वह निष्क्रिय और अविकारी होता है। वह स्वयं नित्य और अविकारी होता है। वह स्वयं नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सभी विषयों से असंपृक्त और राग-द्वेष से रहित है। जितने कर्म या परिणाम हैं जितने सुख या दुःख हैं, वे सभी प्रकृति और उसके विकारों के धर्म हैं। जब अज्ञान के कारण पुरुष अपने को शरीर या इन्द्रिय समझ बैठता है तो उसे आभास होता है कि वह धर्म या परिवर्तन के प्रवाह में पड़कर नाना प्रकार के दुःखों, क्लेशों के दलदल में फँस गया है।
सांख्यकारिका में पुरुष के अस्तित्त्व को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ दी गई हैं –
संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्या अधिष्ठानात्,
पुरुषोंस्तिभोक्तृ भावत् कैवल्यार्थ प्रवृतेश्च ।
संघात परार्थत्वात्
सभी संघात अर्थात अवयवीय पदार्थ किसी अन्य के लिये होते हैं अचेतन तत्त्व इनका उपभोग नहीं कर सकता। अतः यह सब पदार्थ आत्मा अथवा पुरुष के लिये हैं। शरीर, इन्द्रियाँ मानस तथा बुद्धि यह सभी पुरुष के लिये साधन मात्र हैं। त्रिगुण प्रकृति सूक्ष्म शरीर सभी से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है। विकास प्रयोजनमय है। यह प्रयोजन पुरुष का कार्य ही है। पुरुष के कार्य साधन के लिये ही प्रकृति जगत् के रूप में अभिव्यक्त होती है।
त्रिगुणादि विपर्ययात्
सभी पदार्थ तीनों गुणों से निर्मित हैं, अत: पुरुष का भी होना आवश्यक है जो कि इन तीनों गुणों का साक्षी है और स्वयं इनसे परे है, तीनों गुणों से बने पदार्थ निस्तैगुण को उपस्थिति सिद्ध करते हैं जो कि उनसे परे है।
अधिष्ठानात्
समस्त अनुभवों का समन्वय करने के लिए एक अनुभवातीत समन्वयात्मक शुद्ध चेतना होनी चाहिए। सभी ज्ञान पर निर्भर है। पुरुष सभी व्यावहारिक ज्ञान का अधिष्ठाता है। सभी प्रकार की स्वीकृति एवं निषेध में उसका होना आवश्यक है।
भोक्तृभावात्
अचेतन प्रकृति अपनी कृतियों का उपभोग नहीं कर सकती। उसका उपभोग करने के लिए एक चेतन तत्त्व की आवश्यकता है। प्रकृति भोग्या है, अतः उसे एक भोक्ता की आवश्यकता पड़ती है। संसार के समस्त पदार्थ सुख दुःख अथवा उदासीनता उत्पन्न करते हैं, परन्तु सुख-दुःख और उदासीनता का अनुभव करने के लिए एक चेतन तत्त्व की आवश्यकता है। अतः पुरुष का होना अनिवार्य है।
केवल्यार्थ प्रवृते
शिष्ट पुरुषों की युक्ति के लिए प्रकृति होती है और यह दिखाई भी पड़ता है कि यह युक्ति त्रिगुण होने से सुख-दुःखात्मक प्रकृत्यादि पदार्थों की नहीं हो सकती। इसलिए मुमुक्षुजनों की प्रवृत्ति के उद्देश्य रूप मुक्ति का आधार त्रिगुणातीत चेतन पुरुष को मानना आवश्यक है।
इस प्रकार सांख्य ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं। अद्वैत वेदान्त के विरुद्ध और जैन तथा मीमांसा के समान सांख्य भी पुरुष को अनेक मानता है। तत्त्व रूप में वे सब एक ही हैं, परन्तु उनकी संख्या अनेक हैं। उनका तत्त्व चैतन्य है। यह सभी आत्माओं में समान रूप से है। इस अनेकात्मवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका में निम्नलिखित श्लोक मिलता है।
जन्ममरणकरणानाम् प्रतिनियमात् युगपत्प्रवृतेश्च
पुरुष बहुत्वं सिद्धंगण्यविपर्धयाच्चैव |
(1,2,3) जन्म, मरण, करणानां प्रतिनियमात् प्रत्येक पुरुष का जन्म मरण तथा करण अर्थात् इन्द्रियों का कार्य व्यापार भिन्न-भिन्न रूप से नियमित है। एक उत्पन्न होता है तो दूसरा मरता है। एक अन्या है तो दूसरा आँख वाला है। एक के अंधे या बहरे होने से सभी व्यक्ति अंधे या बहरे नहीं हो जाते यह भेद तभी सम्भव है जबकि पुरुष अनेक हैं। यदि एक ही पुरुष होता तो एक के मरने से सभी मर जाते एक के अन्ये या बहरे होने से सभी अन्धे या बहरे हो जाते, परन्तु ऐसा अनुभव में नहीं होता। अतः सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है।
अयुगपत्प्रवृतेश्च
सभी व्यक्तियों में समान प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। प्रत्येक व्यक्ति में पृथक्-पृथक् प्रवृत्ति दिखाई देती है। किसी में एक समय प्रवृत्ति है तो दूसरे में उसी समय निवृत्ति है। जब एक उपर्युक्त किसी समय सोया रहता है तो दूसरा उसी समय काम करता रहता है। जब एक रोता है तो दूसरा हँसता रहता है। इस प्रकार जीवों में एक ही समय प्रवृत्ति न दिखाई देने से यह सूचित होता है कि पुरुष अनेक है। यदि एक ही पुरुष या आत्मा होती तो जीवों में एक ही समय में एक ही प्रकार की निवृत्ति अथवा प्रवृत्ति दिखाई पड़ती।
त्रैगुण्यविनर्ययात्
संसार के सभी जीवों में तीनों गुण भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलते हैं। वैसे प्रत्येक वस्तु में सत्व, रजस और तमस में तीनों ही गुण उपस्थित है, परन्तु फिर भी कोई व्यक्ति सात्त्विक है, कोई राजसिक तथा कोई तामसिक जो सात्विक है उसमें शान्ति, प्रकाश तथा सुख प्रधान है। जो राजसिक है उसमें दुःख, अशान्ति तथा क्रोध प्रधान है तथा जो तामसिक है उसमें मोह तथा अज्ञान प्रधान है। यदि एक ही पुरुष होता तो सभी सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होते, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। अतः पुरुष अनेक हैं।
स्त्री, पुरुष जहाँ एक तरफ पशु-पक्षियों से ऊपर की श्रेणी में हैं वहीं दूसरी तरफ देवताओं से नीचे की श्रेणी में हैं। यदि पशु, पक्षी, मनुष्य देवता सभी में एक ही आत्मा का निवास होता तो ये विभिन्नताएँ नहीं होतीं। इन बातों से सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। ये आत्मा या पुरुष नित्य द्रष्टा या ज्ञाता स्वरूप रहते हैं। प्रकृति एक है पुरुष अनेक प्रकृति विषयों का जड़ आधार है, पुरुष उनका चेतन द्रष्टा है। प्रकृति प्रमेय है पुरुष प्रमाता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
पुरुष (आत्मा) का अस्तित्त्व क्या है ?
पुरुष या आत्मा-स्वरूप-सांख्य दर्शन का एक तत्त्व तो प्रकृति है, दूसरा तत्त्व पुरुष या आत्मा है। ‘मैं’ ‘मेरा’ यह सभी व्यक्तियों का सहज स्वाभाविक अनुभव है जिसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्त्व अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए सांख्य कहता है कि आत्मा (पुरुष) का अस्तित्त्व स्वयंसिद्ध (स्वतः प्रकाश) है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया जा सकता।
त्रिगुणादि विपर्ययात् क्या है ?
सभी पदार्थ तीनों गुणों से निर्मित हैं, अत: पुरुष का भी होना आवश्यक है जो कि इन तीनों गुणों का साक्षी है और स्वयं इनसे परे है, तीनों गुणों से बने पदार्थ निस्तैगुण को उपस्थिति सिद्ध करते हैं जो कि उनसे परे है।

Very useful and informative
Very good experience 👍
thank you❣