

रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | ramdhari singh dinkar biography


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व
रूपरेखा
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- काव्यगत विशेषताएं
- भाषा
- शैली
- रस, छंद, तथा अलंकार
“अपनी वाणी के बाणों से अग्नि वर्षा करने वाले दिनकर उन महाकवियों में हैं जो प्राचीन भारत के गौरवमय अतीत पर मुग्ध हो उठते हैं और वर्तमान के शोषण, उत्पीड़न, पतन और वैषम्य के प्रति जिनका हृदय हाहाकार करते हुए हुँकार कर विद्रोह कर उठता है। निःसन्देह दिनकर जी का काव्य दलित मानवता और सिसकती हुई करुणा का काव्य है। आधुनिक युग की नई गीता के रूप में इनका ‘कुरुक्षेत्र’ महाकाव्य हैं।“
जीवन वृत्त
‘दिनकर’ का जन्म बिहार प्रान्त में, मुंगेर जिले के सिमिरिया घाट नामक गाँव में सन् 1907 ई० में हुआ था। 1932 ई० में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बी० ए० ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की।
जीवन के क्षेत्र में पदार्पण करने पर ये सब-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुये । कुछ दिनों तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और कुछ समय प्रोफेसर भी रहे।
केन्द्रीय राज्य परिषद् के ये मनोनीत सदस्य भी रह चुके थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे।
‘दिनकर’ जी को काव्य-रचना से बाल्यकाल से ही अगाध अनुराग था। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने ‘प्राण भंग’: नामक काव्य की रचना की थी, जो 1921 ई० में प्रकाशित हुई थी।
जीवन पर्यन्त दिनकर जी निरन्तर साहित्य सेवा में संलग्न रहे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिहार के सभापति भी रह चुके हैं।
जवान बेटे की मृत्यु ने इनके ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खण्डित कर दिया और पिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 24 अप्रैल 1974 को यह साहित्य सूर्य सदैव के लिये अस्त हो गया।
रचनायें / रामधारी सिंह दिनकर के निबंध
दिनकर जी ने पद्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में अनेकों ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें प्रमुख कवि के रूप में ही हैं
- काव्य– रेणुका, रसवन्ती, द्वन्द्व गीत, हुँकार, धूप-छाँह, सावधेनी, एकायन, इतिहास के आँसू, धूप और धुआँ आदि ।
- खण्डकाव्य- कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ।
- आलोचना- ‘मिट्टी की ओर।’
- इतिहास- ‘संस्कृति के चार अध्याय’।
- गद्य संग्रह- ‘मिट्टी की ओर’ ‘अर्धनारीश्वर’ ‘रेती के फूल’।
- बाल साहित्य- चित्तौड़ का साका, मिर्च का मजा।
रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं
रेणुका, रसवन्ती, द्वन्द्व गीत, हुँकार, धूप-छाँह, सावधेनी, एकायन, इतिहास के आँसू, धूप और धुआँ आदि ।
दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन, गाँधी जी की विचारधारा तथा बढ़ती हुई समाज की विषमताओं, अत्याचारों ने मिलकर दिनकर जी की आत्मा को प्रभावित किया है।
यही कारण है कि दिनकर के काव्य की प्रमुख भावना में राष्ट्रीयता, देश-प्रेम, वर्तमान पतन एवं शोषण के प्रति विद्रोह, उद्बोधन आदि हैं।
प्राचीन भारत के गौरव पूर्ण अतीत का गुणगान कर दिनकर जी देश में चेतना और जागृति भर देना चाहते हैं।
यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना करना ही इनके काव्य का मुख्य ध्येय है। प्रगतिवादी रचनायें बड़ी ओजपूर्ण एवं मार्मिक हैं। एक उदाहरण देखिए-
कही उठी दीन कृषकों की, मजदूरों की तड़प पुकारें,
अरे, गरीबों के लोह पर, खड़ी हुई तेरी दीवारें।
भारत के आर्थिक वैषम्य का एक नग्न चित्र देखिये –
श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक, ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं ।
के स्वर्णिम अतीत का इतिहास और वर्तमान का अध:पतन दिनकर के हृदय में विद्रोह भर देता है। वे कह उठते हैं
ओ मगध कहाँ तेरे अशोक, वह चन्द्रगुप्त बल धाम कहाँ।
री कपिलवस्तु, कह, बुद्धदेव के वे मंगल उपदेश कहाँ ।
वर्तमान दूषित व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिये, प्रलयकारी ताण्डव नृत्य के लिए वे शंकर का आह्वान करते हैं-
कहदे शंकर से आज करें, वे प्रलय नृत्य फिर एक बार।
सारे भारत में गूंज उठे, हर-हर, बम-बम का महोच्चार ।।
क्योंकि देश में
नारी-नर जलते साथ-साथ जलते हैं मांस रुधिर अपने।
जलती है वर्षों की उमंग, जलते हैं सदियों के सपने ||
भाषा
दिनकर जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। भावों के अनुसार भाषा में भी ओज, पौरुष एवं बल है। दिनकर की भाषा के प्रमुख गुण सरलता, सरसता स्वाभाविकता एवं बोधगम्यता है ।
संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भावों के अनुसार उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सुन्दर एवं मार्मिक है।
शैली
दिनकर जी की शैली बड़ी ओजस्वी, स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। उसे तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है-
- विवरणात्मक
- भावात्मक
- उद्बोधनात्मक
इनके प्रबन्ध काव्यों की रचना विवरणात्मक शैली में हुई है।
प्रगतिवादी रचनायें भावात्मक शैली में हैं तथा जागरण और चेतना से भरे हुए गीतों में उद्बोधनात्मक शैली के दर्शन होते हैं।
रस, छन्द तथा अलंकार
रस की दृष्टि से दिनकर के काव्य में सभी रसों का समावेश है। वीर तथा करुण रसों का प्राधान्य है।
छन्द-योजना में दिनकर जी ने प्राचीन छन्दों तथा कवित्त सवैये आदि भी प्रयोग किये हैं। प्रगतिवादी रचनाओं में आधुनिक छंद शैली का प्रयोग किया गया है।
दिनकर के काव्य के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आये हैं।
मानवीकरण, ध्वनि-चित्रण, विशेषण, विपर्यय आदि पाश्चात्य अलंकार की भाषा की शोभा वृद्धि में सहायक हुए हैं।
आपको हमारी आज की यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
रामधारी सिंह दिनकर की जीवन वृत्त क्या है ?
‘दिनकर’ का जन्म बिहार प्रान्त में, मुंगेर जिले के सिमिरिया घाट नामक गाँव में सन् 1907 ई० में हुआ था। 1932 ई० में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बी० ए० ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की।
जीवन के क्षेत्र में पदार्पण करने पर ये सब-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुये । कुछ दिनों तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और कुछ समय प्रोफेसर भी रहे।
केन्द्रीय राज्य परिषद् के ये मनोनीत सदस्य भी रह चुके थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे।
‘दिनकर’ जी को काव्य-रचना से बाल्यकाल से ही अगाध अनुराग था। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने ‘प्राण भंग’: नामक काव्य की रचना की थी, जो 1921 ई० में प्रकाशित हुई थी।
जीवन पर्यन्त दिनकर जी निरन्तर साहित्य सेवा में संलग्न रहे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिहार के सभापति भी रह चुके हैं।
जवान बेटे की मृत्यु ने इनके ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खण्डित कर दिया और पिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 24 अप्रैल 1974 को यह साहित्य सूर्य सदैव के लिये अस्त हो गया।
रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
दिनकर जी ने पद्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में अनेकों ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें प्रमुख कवि के रूप में ही हैं
काव्य– रेणुका, रसवन्ती, द्वन्द्व गीत, हुँकार, धूप-छाँह, सावधेनी, एकायन, इतिहास के आँसू, धूप और धुआँ आदि ।
खण्डकाव्य- कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ।
आलोचना- ‘मिट्टी की ओर।’
इतिहास- ‘संस्कृति के चार अध्याय’।
गद्य संग्रह- ‘मिट्टी की ओर’ ‘अर्धनारीश्वर’ ‘रेती के फूल’।
बाल साहित्य- चित्तौड़ का साका, मिर्च का मजा।
रामधारी सिंह दिनकर की भाषा क्या थी ?
दिनकर जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। भावों के अनुसार भाषा में भी ओज, पौरुष एवं बल है। दिनकर की भाषा के प्रमुख गुण सरलता, सरसता स्वाभाविकता एवं बोधगम्यता है ।
संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भावों के अनुसार उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सुन्दर एवं मार्मिक है।
रामधारी सिंह दिनकर की शैली कैसी है ?
दिनकर जी की शैली बड़ी ओजस्वी, स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। उसे तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है-
- विवरणात्मक
- भावात्मक
- उद्बोधनात्मक
इनके प्रबन्ध काव्यों की रचना विवरणात्मक शैली में हुई है।
प्रगतिवादी रचनायें भावात्मक शैली में हैं तथा जागरण और चेतना से भरे हुए गीतों में उद्बोधनात्मक शैली के दर्शन होते हैं।
रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है?
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms


कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है | हिन्दी निबंध |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- कविता की परिभाषा
- हिन्दी साहित्य के विभिन्न काल और उनका प्रभाव
- आदिकाल
- भक्तिकाल
- रीतिकाल
- आधुनिक काल
- उपसंहार
प्रस्तावना
कवि और उनके काव्य किसी दूसरे संसार से नहीं आते, कवि इसी धरातल पर अवतीर्ण होते हैं और उनके काव्य इसी समाज में बैठकर लिखे जाते हैं।
वे भी धरती के मानव हैं, और समाज और देश की अवस्था का उनके हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्तर इतना ही है कि साधारण मनुष्य उन्हें मूक होकर अनुभव करता है और कवि अपनी काव्य-प्रतिभा से उन्हें समाज के आगे अभिव्यक्त कर देता है।
समाज की प्रमुख प्रवृत्तियाँ सहसा ही उसके काव्य में अपना स्थान बना लेती हैं। वह अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है।
संसार के सभी साहित्यों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवियों ने अपने देश और समय की विभिन्न विचारधाराओं को ही अपने काव्य में स्थान दिया है तथा श्रोता तथा पाठक गण समाज उनका आदर करते हैं।
लोकरुचि और लोकप्रवृत्ति से भिन्न राग अलापने वाला कवि समाज में आदृत नहीं होता। उसे समाज के स्वर में स्वर मिलाकर चलना पड़ता है, समाज भी उसे अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहता, क्योंकि दोनों अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर सापेक्ष्य हैं।
कविता की परिभाषा / कवि,लेखक / कविता हिंदी में
कवि के मनोगत भाव जब संहसा स्वर लहरी के माध्यम से फूट पड़ते हैं, तब समाज उसे कविता की संज्ञा देता है। कवि के हृदय के उद्गार ही कविता है।
वह अपने हृदय के भावों और विचारों को कविता से कैसे पृथक् का सकता है।
प्रत्येक युग की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थायें: तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ करती हैं।
युग के परिवर्तन के साथ साहित्य की गति में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है।
इसीलिए विद्वान् साहित्य को समाज का दर्पण, प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप और प्रतिच्छाया स्वीकार करते हैं।
कवि अपने युग की सामाजिक चेतनाओं का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करता है |
हिन्दी साहित्य के विभिन्न काल और उनका प्रभाव
हिन्दी साहित्य का इतिहास चार भागों में विभाजित किया जाता है- आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल।
प्रत्येक काल की अपनी भिन्न-भिन्न विशेषतायें हैं। उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा कि उन कालों के विभिन्न कवियों ने अपनी युगीन विचारधाराओं का सफल प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया।
आदिकाल
हिन्दी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार से लडाई-झगडे का युग था। उसमें अशान्ति थी और एक प्रकार की राजनैतिक आँधी चल रही थी।
यवनों के आक्रमण आरम्भ हो गए थे। हिन्दू राजा लोग अपने-अपने राज्य की रक्षा में लगे हुए थे। यवनों की लूटमार जारी थी। गजनवी और गौरी के आक्रमणों ने राजपूतों को शिथिल-सा कर दिया था।
राजपूत राजा अपने-अपने गौरव की रक्षा में लगे हुए थे, देश के गौरव का उन्हें कम ध्यान था। उनमें वीरता थी, परन्तु वीरता का कोष पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताओं में खाली किया जा रहा था।
इन प्रतिद्वन्द्विताओं के कारण राजपूत एक सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति का परिचय न दे सके, यवनों के पैर धीरे-धीरे जमते गए। वह युद्ध का युग था।
वे युद्ध कभी विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए किये जाते थे, कभी पारस्परिक वीरता प्रदर्शन के लिए होते थे और कभी-कभी स्त्रियों का सौन्दर्याधिक्य भी इन युद्धों का कारण होता था।
अतः तत्कालीन साहित्य पर वीरता की छाप पड़ी। वीरगाथाओं के साथ-साथ तत्कालीन रचनाओं में शृंगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में रहता था, क्योंकि ‘प्रायः स्त्रियाँ ही पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता और झगड़े का कारण हुआ करती थीं।
इन काव्यों में युद्धों का बड़ा सुन्दर और सजीव वर्णन है। चन्द ने यदि पृथ्वीराज का वर्णन किया तो भट्ट केदार ने जयचन्द का यशोगान किया।
भक्तिकाल
आँधी हमेशा नहीं रहती, आँधी के बाद शान्ति और स्थिरता आ जाती है। भारतवर्ष के राजनीतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शान्ति स्थापित हुई।
राजपूतों में जब तक कुछ शक्ति थी, वीरता थी, साहस था, तब तक वीरगाथाओं से थोड़ा बहुत काम चला। किन्तु बल के क्षीण हो जाने पर उत्साह प्रदान से भी कोई काम नहीं चलता
“निर्वाह दीपे कि तैल्य दानम्” ।
शान्ति के समय एक-दूसरे ही प्रकार के काव्य की आवश्यकता थी। भारतवर्ष में यवन अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे।
हिन्दुओं पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। उन्हें जीवन भार मालूम पड़ रहा था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य फैल रहा था। घोर नैराश्य के कारण जनता ने परमात्मा का आश्रय लिया।
कुछ हिन्दू यह भी चाहते थे कि उनका धर्म इस रूप में आए कि मुसलमान उसका खण्डन न कर सकें। इतना ही नहीं यदि सम्भव हो सके तो विरोध को छोड़कर उनके साथ मिलें।
इसके अतिरिक्त एक प्रवृत्ति और भी थी। कुछ लोग अपना स्वत्व और व्यक्तित्व अलग चाहते थे। वे लोग मुसलमानों के विरोधी तो नहीं थे परन्तु ऐक्य की वेदी पर अपने इष्टदेवों के प्रति अनन्य भावना का बलिदान करना नहीं चाहते थे।
इन्हीं भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों ने भक्तिकालीन तीनों शाखाओं को जन्म दिया।
ज्ञानाश्रयी प्रेममार्गी तथा कृष्ण-राम भक्त कवि अपने-अपने ढंग से जनता की चित्तवृत्तियों का अपने काव्य में चित्र अंकित करने लगे। ज्ञानाश्रयो कवियों ने हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर करके उन्हें मिलाने का प्रयत्न किया।
प्रेममार्गी कवियों ने भी हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करके प्रेम सिद्धान्तों का प्रचार किया।
परन्तु इन दोनों शाखाओं के प्रमुख साहित्यकार जनता के हृदय का पूर्ण स्पर्श न कर सके। आगे चलकर सूर और तुलसी ने कृष्ण और राम का गुणगान सुनाकर जनता को मन्त्रमुग्ध कर दिया।
जनता भक्ति रस की धारा में अपने दुखों को भूल गई।
रीतिकाल
भक्तिकाल के पश्चात् हिन्दुओं को कुछ शांति मिली। मुगल बादशाह भी अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे तथा हिन्दुओं को छोटी-छोटी जागीरों का स्वामी बना दिया था।
सम्राट विलासिता की सरिता में गोते लगा रहे थे। जहाँगीर और शाहजहाँ की विलासिता की सीमा न थी। छोटे-छोटे हिन्दू राजा भी इसी रंग में रंग गये थे।
प्रजा भी सांसारिक भोग-विलासों में आनन्द ले रही थी। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन कवियों ने जनता का अपने काव्य में चित्र खींचना प्रारम्भ कर दिया।
हिन्दी काव्य में शृंगारपूर्ण, प्रेमी मादकारिणी रचनायें होने लगीं। नायिका भेद, नख-शिख वर्णन और ऋतु वर्णन में ही कवियों ने अपना काव्य चमत्कार दिखाना प्रारम्भ किया।
तत्कालीन काव्य में राजदरवारों की गुलगुली गिलमें और गलीचों के विलासमय जीवन की छाप थी। कविता में सुलाने की सामग्री अधिक थी, जगाने और जिलाने की कम |
आधुनिक काल
आधुनिक युग का आरम्भ अंग्रेजों की साम्राज्य स्थापना के साथ आरम्भ होता है। अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनता में प्रारम्भ से ही चेतना विद्यमान थी।
भारतीयों का जीवन दुःखी था। समाज की राजनैतिक और आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, अतः समाज में एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीयता की लहर उमड़ने लगी।
युग प्रतिनिधि होने के नाते कवियों के काव्य में भी राष्ट्रीयता गूंजने लगी। कविता राजसी दरबारों की वस्तु न रहकर किसानों और मजदूरों की वस्तु बन गई।
वर्तमान युग की कविता गाँधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुई। समाज की कुरीतियों, जैसे—अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा पर भी लेखनी चली।
मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्राकुमारी चौहान आदि की कवितायें राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण हैं।
उपसंहार
तात्पर्य यह है कि हिन्दी के ही नहीं, सभी भाषाओं के कवि अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
क्योंकि वे कवि भी प्राणी हैं और इसी भूमि पर रहते हैं, जहाँ एक ओर प्रसन्नता है और दूसरी ओर हाहाकार, जहाँ एक ओर जन्म है तो दूसरी ओर मरण सामाजिक विचार और समाज की परिस्थिति से वे कैसे दूर रह सकते हैं।
कवि जो कुछ समाज से ग्रहण करता है, उसे अपनी त से समाज को ही समर्पित कर देता है –
दुनिया ने तजुर्बात की सूरत में आज तक ।
जो कुछ मुझे दिया है, वो लौटा रहा हूँ मैं |
अतः कवि निःसन्देह अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कवि-धर्म और युग-धर्म दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। युगीन भावनायें अनायास ही कवि के काव्य में प्रतिबिम्बित हैं होने लगती हैं।
आपको हमारी आज की यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
हिन्दी साहित्य के विभिन्न काल और उनका प्रभाव क्या पड़ा ?
हिन्दी साहित्य का इतिहास चार भागों में विभाजित किया जाता है- आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल।
प्रत्येक काल की अपनी भिन्न-भिन्न विशेषतायें हैं। उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा कि उन कालों के विभिन्न कवियों ने अपनी युगीन विचारधाराओं का सफल प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया।
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms


हिन्दी साहित्य में महिला साहित्यकार | हिन्दी निबंध |
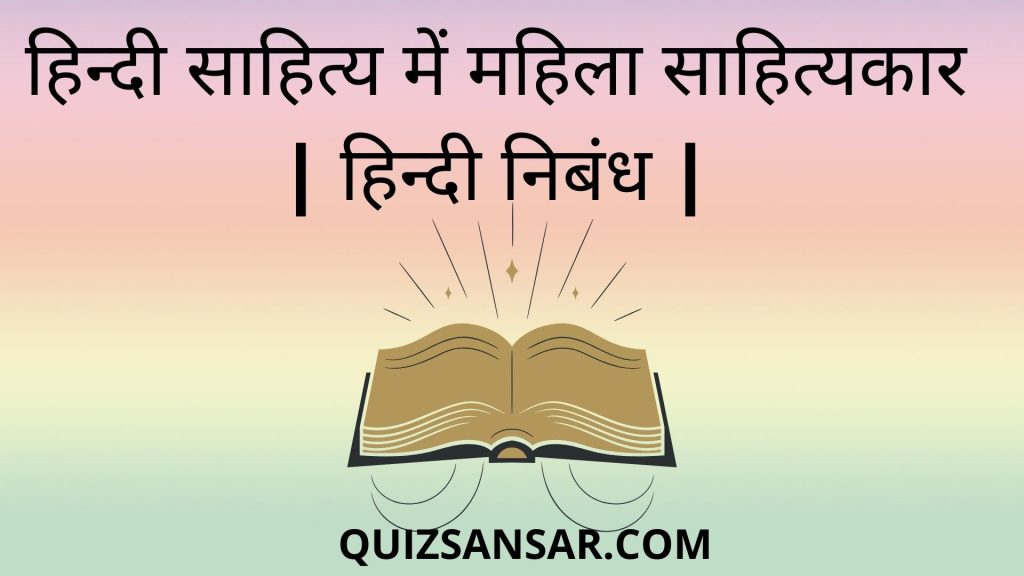
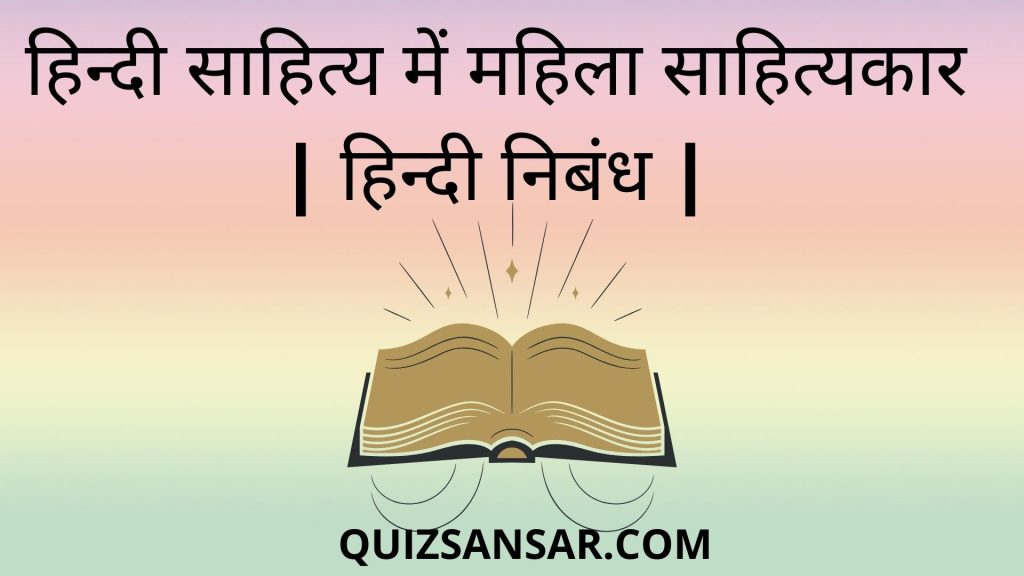
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है हिन्दी साहित्य में महिला साहित्यकार | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- आदिकाल
- भक्तिकाल
- रीतिकाल
- आधुनिक काल
- उपसंहार
प्रस्तावना
जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री ने पुरुष का साथ दिया है। वह उसकी सहधर्मिणी है, अर्धांगिनी है | वह उससे पीछे कैसे रह सकती है।
वीर क्षत्राणियों ने तो युद्ध भूमि में भी पुरुषों का साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयम् युद्ध संचालन किये।
साहित्य के क्षेत्र में जहाँ महाकवियों ने साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की वहाँ महिलाओं ने भी अपनी अमूल्य कृतियों से साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया, परन्तु वह भारत माँ का दुर्भाग्य था, कि यहाँ पुरुषों की भाँति स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का अभाव रहा अन्यथा यहाँ जितने पुरुष साहित्यकार हुए उनसे अधिक महिला साहित्यकार होतीं।
आदिकाल
हिन्दी साहित्य का आदिकाल वीरगाथा काल कहा जाता है। यह एक प्रकार से राजनैतिक आँधी और तूफान का युग था।
राजपूत राजे-महाराजे अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए थे। यवनों के भयानक आक्रमण भारतवर्ष पर हो रहे थे और वे शनैः शनैः अपना अधिकार जमाते आ रहे थे।
वह समय महिलाओं की कोमल भावनाओं के अनुकूल भी नहीं था। अतः हिन्दी साहित्य के आदिकाल में तो कोई महिला साहित्यकार प्रकाश में नहीं आई।
परन्तु उसके पश्चात् अन्य सभी कालों में महिलाओं ने साहित्य की वृद्धि में यथाशक्ति योगदान दिया है।
भक्तिकाल
भक्तिकाल की मधुर एवं कोमल साहित्यिक प्रवृत्तियाँ महिलाओं की रुचि के अनुकूल थीं। इस काल में कई उच्चकोटि की महिला कवियित्रियों के दर्शन होते हैं।
इन्होंने निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म श्रीकृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके अपने अन्तर्मन की भावनाओं को कोमलकान्द पदावली द्वारा व्यक्त किया।
भक्तिकालीन महिला काव्यकारों में सहजोबाई, दयाबाई और मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सहजबाई चरणदास की शिष्या थीं।
उन्होंने निराकार प्रियतम के प्रति अनूठी उक्तियाँ कही हैं। प्रियतम की भक्ति-माधुरी में प्रेमोन्मत्त होकर सहजो कहते लगतीं
बाबा नगरु बसाओ।
ज्ञान दृष्टि सूं घट में देखौ, सुरति निरति लौ लावो ।
पाँच मारि मन बसकर अपने, तीनों ताप नसावौ ॥
रीतिकाल
दयाबाई भी चरणदास की शिष्या थीं। उनका विषय वर्णन भी सहजोबाई की भाँति अपन निराकार प्रियतम का आह्वान और विरह निवेदन ही है।
मृतप्राय हिन्दू जाति पर इन कवियित्रियों ने अपनी रसमयी काव्य धारा द्वारा ऐसी पीयूष वर्षा की कि वह आज तक सानन्द जीवित है।
इसके पशचत् मीरा का नाम आता है। मीरा भक्ति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवियित्री थीं।
मौरा की कोमल वाणी ने भारतीय साहित्य में प्रेम और आशा से भरी हुई वह पावन सरिता प्रवाहित की जिसकी वेगवती धारा आज भी भारतीय अन्तरात्मा में ज्यों की त्यों अबाध गति से बह रही है।
मीरा ने अपने अनुभूत प्रेम और विरह वेदना को साहित्य में स्थान दिया। कितना लालित्य और माधुर्य है, इनके पदों में सभी जानते हैं।
आज भारत के घर-घर में इनके पदों का आदर है। स्त्री-पुरुष सभी इन पदों को समान भाव से गाकर आज भी आनन्द-विभोर हो उठते हैं।
श्रीकृष्ण के साथ मीरा का प्रेम दाम्पत्य-भाव का प्रेम था, श्रीकृष्ण उनके प्रियतम थे, जन्म-जन्म के साथी थे और वह उनको विरहिणी प्रेयसी थी।
यह स्पष्ट घोषणा करते हुए मीरा को न कोई संकोच था और न कोई लोकलाज-
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
सन्तन ढिंग बैठि-बैठि, लोक लाज खोई,
अब तो बेलि फैलि गई, अमृतफल होई।
मीरा की-सी वेदना, टीस और कसक सम्भवतः हिन्दी की किसी अन्य कवियित्री में नहीं मिल सकती। मीरा के पद हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। एक दूसरा पद देखिए-
हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दरद न जाने कोय,
दरद की मारी बन-बन डोलूँ वैद मिला नहि कोय।
सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होय,
मीरा की प्रभु पीर मिटै जब, वैद संवरिया होय।
मीरा के उपरान्त हिन्दी साहित्य में छत्र कुँवरि, विष्णु कुंवरि, राय प्रवीण तथा बृजवासी अनेक महिला कवियित्रियों के दर्शन होते हैं।
इन सभी महिलाओं ने अपनी पुनीत मधुर भावनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाने में पूर्ण योगदान दिया।
विष्णु कुँवरि का सुन्दर पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पद में वे अपने प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के विरह की व्याकुलता प्रकट करती हैं-
निरमोही कैसो हियौ तरसावै।
पहिले झलक दिखाय के हमकू, अब क्यों देगि न आवै ।।
कब सौ तड़फत तेरी सजनी, वाको दरद न जावै।
विष्णु कुँवरि उर में आ करके, ऐसी पीर मिटावै ।।
अकबर के शासनकाल में ‘राय प्रवीण’ एक वेश्या थी। नृत्य और गीत के साथ वह सुन्दर कविता भी करती थी। वह महाकवि केशव की शिष्या थी।
केशवदास जी ने ‘कविप्रिया’ में इसका वर्णन भी किया है। अकबर इसके रूप-लावण्य पर मुग्ध था। उसने एक दिन इनसे भरी सभा में गाने को कहा।
पहले तो इसने मना किया, परन्तु बाद में विवश होकर इन्हें गाना पड़ा। इसके तत्काल निम्नलिखित दोहा बनाकर सुनाया, जिससे अकबर बहुत लज्जित हुआ—
विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान।
जूठी पातर चखत है, बारी बायस स्वान ।।
इनके बाद ‘ताज’ का नाम आता है। यद्यपि ये मुसलमान थीं फिर भी इन्हें श्रीकृष्ण से प्रेम हो गया था। इनकी कविता भक्ति रस से ओत-प्रोत है।
ताज श्रीकृष्ण के चरणारविद में अपना तन, मन, धन समर्पित करने को उत्सुक है
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम,
दस्त हाँ बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं।
देव पूजा ठानी हों नमाज हूँ भुलानी,
तज कलमा कुरान, सारे गुनन कहूँगी मैं।
साँवला सलोना सरताज सिर कुल्लेदार,
तेरे नेह दाग में निदाग है दहंगी मैं।
नन्द के कुमार, कुरबान तेरी सूरत पै,
हों तो मुसलमानी, हिन्दुवानी है रहूँगी मैं।
ताज के पश्चात् शेख का नाम आता है। ये रंगरेजिन महिला थीं, इन्होंने एक ब्राह्मण कवि से विवाह कर लिया था और उसका नाम आलम रखा था।
दोनों पति-पत्नी आनन्द से कविता किया करते थे। शेख की कविता शृंगार रस में अद्वितीय हैं। निम्नलिखित उदाहरण पति-पत्नी के प्रश्नोत्तर के रूप में।
प्रथम पंक्ति में पति प्रश्न करते हैं, दूसरी पंक्ति से शेख उसका उत्तर देती हैं-
कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन ।
कटि को कंचन काटि के कुचन मध्य धरि दीन ।
हिन्दी के प्रसिद्ध ‘कुण्डलियाँ’ लेखक गिरधर कविराय की पत्नी का नाम ‘सॉई’ था। अपने पति की भाँति वे भी नीतिपूर्ण छन्दों में रचना किया करती थीं। उदाहरण देखिए-
साई अवसर के परे, को न सहै दुःख द्वन्द्व ।
जाय बिकाने डोम घर, वे राजा हरिचन्द ॥
आधुनिक काल
आधुनिक काल में नव-जागृति और नव चेतना का उदय हुआ। महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई, उनके हृदय में नवीन भावनाओं ने जन्म लिया।
साहित्य की सभी विधाओं पर महिलाओं ने लेखनी चलाई। आधुनिक युग की महिला कवियित्रियों में प्रथम नाम श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का आता है।
इन्होंने देश भक्ति पूर्ण रचनायें कीं। ‘झाँसी की रानी’ तथा ‘वीरों का कैसा हो बसन्त’ इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचनायें हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए-
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी।
बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी ।
गुमी हुई आजादी की, कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की, सबने मन में ठानी थी।
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी |
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।
इसके अनन्तर छायावादी युग की प्रमुख कवियित्री महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी जी के गीत अपनी सहज सहनशीलता, भावविदग्धता के कारण सजीव हैं। विरह की आग में ‘अनजान कविता उनके हृदय से वह निकलती है। देखिए उनकी करुणातुर प्रार्थना कितनी नारी। सुलभ है-
जो तुम आ जाते एक बार !
कितनी करुणा कितने सन्देश पथ में बिछ जाते बन पराग।
गाता प्राणों का तार-तार, अनुराग भरा उत्पाद राग ।
आँसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार ।।
महादेवी जी के गीत लोकप्रिय एवं हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं।
उनकी अपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है। इस करुणा के अनन्त, असीम सागर में वे केवल नीर भरी दुःख की क्षणिक बदली ही हैं-
मैं नीर भरी दुःख की बदली !
विस्तृत नभ का कोना-कोना मेरा न कभी अपना होना।
परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली ।
वे जीवन के शून्य क्षणों में विकल होकर गा उठती हैं—
अलि ! कैसे उनको पाऊँ ।
ये आँसू बनकर भी मेरे इस कारण ढल ढल जाते,
इन पलकों के बन्धन में मैं बाँध बाँध पछताऊँ ।
आधुनिक युग में महिला साहित्यकारों ने साहित्य की सभी विधाओं पर लिखना प्रारम्भ किया। कोई भी विधा-क्या कहानी, क्या उपन्यास, क्या आलोचना, ऐसी नहीं है, जिस पर महिला ने लेखनी न चलाई हो।
इन महिला साहित्यकारों में श्रीमती विद्यावती कोकिला, तारा पाण्डेय, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, राजेश्वरी देवी, रजनी पणिक्कर, कंचनलता, सब्बरवाल तथा शची रानी गुर्टू आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।
कविता के क्षेत्र में श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने अधिक ख्याति प्राप्त की है। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए-
क्या तुम अकेले मन !
देखो जल, रेती साथ रहे, हैं भिन्न, किन्तु कस हाथ गहे।
वे तो जड़ हैं, पर तुम चेतन, क्या तुम्हीं अकेले हो, ओ मन ॥
उपसंहार
आधुनिक युग में महिला साहित्यकारों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।
आशा है कि निकट भविष्य में हिन्दी साहित्य को इनकी नवीन साहित्य कृतियाँ और भी अधिक समृद्धिशाली बनायेंगी ।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
आदिकाल में महिला साहित्यकार का स्थान क्या था ?
हिन्दी साहित्य का आदिकाल वीरगाथा काल कहा जाता है। यह एक प्रकार से राजनैतिक आँधी और तूफान का युग था।
राजपूत राजे-महाराजे अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए थे। यवनों के भयानक आक्रमण भारतवर्ष पर हो रहे थे और वे शनैः शनैः अपना अधिकार जमाते आ रहे थे।
वह समय महिलाओं की कोमल भावनाओं के अनुकूल भी नहीं था। अतः हिन्दी साहित्य के आदिकाल में तो कोई महिला साहित्यकार प्रकाश में नहीं आई।
परन्तु उसके पश्चात् अन्य सभी कालों में महिलाओं ने साहित्य की वृद्धि में यथाशक्ति योगदान दिया है।
आधुनिक काल में महिला साहित्यकार का स्थान क्या है ?
आधुनिक काल में नव-जागृति और नव चेतना का उदय हुआ। महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई, उनके हृदय में नवीन भावनाओं ने जन्म लिया।
साहित्य की सभी विधाओं पर महिलाओं ने लेखनी चलाई। आधुनिक युग की महिला कवियित्रियों में प्रथम नाम श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान | का आता है।
इन्होंने देश भक्ति पूर्ण रचनायें कीं। ‘झाँसी की रानी’ तथा ‘वीरों का कैसा हो बसन्त’ इनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचनायें हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए-
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी।
बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी ।
गुमी हुई आजादी की, कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की, सबने मन में ठानी थी।
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी |
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।
इसके अनन्तर छायावादी युग की प्रमुख कवियित्री महादेवी वर्मा का नाम आता है।
महादेवी जी के गीत अपनी सहज सहनशीलता, भावविदग्धता के कारण सजीव हैं।
विरह की आग में ‘अनजान कविता उनके हृदय से वह निकलती है।
देखिए उनकी करुणातुर प्रार्थना कितनी नारी। सुलभ है-
जो तुम आ जाते एक बार !
कितनी करुणा कितने सन्देश पथ में बिछ जाते बन पराग।
गाता प्राणों का तार-तार, अनुराग भरा उत्पाद राग ।
आँसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार ।।
महादेवी जी के गीत लोकप्रिय एवं हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं।
उनकी अपनी शैली है, अपनी प्रवृत्ति है। इस करुणा के अनन्त, असीम सागर में वे केवल नीर भरी दुःख की क्षणिक बदली ही हैं-
मैं नीर भरी दुःख की बदली !
विस्तृत नभ का कोना-कोना मेरा न कभी अपना होना।
परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली ।
रीतिकाल में महिला साहित्यकार का स्थान क्या था ?
दयाबाई भी चरणदास की शिष्या थीं। उनका विषय वर्णन भी सहजोबाई की भाँति अपन निराकार प्रियतम का आह्वान और विरह निवेदन ही है।
मृतप्राय हिन्दू जाति पर इन कवियित्रियों ने अपनी रसमयी काव्य धारा द्वारा ऐसी पीयूष वर्षा की कि वह आज तक सानन्द जीवित है।
इसके पशचत् मीरा का नाम आता है। मीरा भक्ति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवियित्री थीं।
मौरा की कोमल वाणी ने भारतीय साहित्य में प्रेम और आशा से भरी हुई वह पावन सरिता प्रवाहित की जिसकी वेगवती धारा आज भी भारतीय अन्तरात्मा में ज्यों की त्यों अबाध गति से बह रही है।
मीरा ने अपने अनुभूत प्रेम और विरह वेदना को साहित्य में स्थान दिया। कितना लालित्य और माधुर्य है, इनके पदों में सभी जानते हैं।
आज भारत के घर-घर में इनके पदों का आदर है। स्त्री-पुरुष सभी इन पदों को समान भाव से गाकर आज भी आनन्द-विभोर हो उठते हैं।
श्रीकृष्ण के साथ मीरा का प्रेम दाम्पत्य-भाव का प्रेम था, श्रीकृष्ण उनके प्रियतम थे, जन्म-जन्म के साथी थे और वह उनको विरहिणी प्रेयसी थी।
यह स्पष्ट घोषणा करते हुए मीरा को न कोई संकोच था और न कोई लोकलाज-
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
सन्तन ढिंग बैठि-बैठि, लोक लाज खोई,
अब तो बेलि फैलि गई, अमृतफल होई।
मीरा की-सी वेदना, टीस और कसक सम्भवतः हिन्दी की किसी अन्य कवियित्री में नहीं मिल सकती। मीरा के पद हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। एक दूसरा पद देखिए-
हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दरद न जाने कोय,
दरद की मारी बन-बन डोलूँ वैद मिला नहि कोय।
सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होय,
मीरा की प्रभु पीर मिटै जब, वैद संवरिया होय।
मीरा के उपरान्त हिन्दी साहित्य में छत्र कुँवरि, विष्णु कुंवरि, राय प्रवीण तथा बृजवासी अनेक महिला कवियित्रियों के दर्शन होते हैं।
इन सभी महिलाओं ने अपनी पुनीत मधुर भावनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाने में पूर्ण योगदान दिया।
विष्णु कुँवरि का सुन्दर पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पद में वे अपने प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के विरह की व्याकुलता प्रकट करती हैं-
निरमोही कैसो हियौ तरसावै।
पहिले झलक दिखाय के हमकू, अब क्यों देगि न आवै ।।
कब सौ तड़फत तेरी सजनी, वाको दरद न जावै।
विष्णु कुँवरि उर में आ करके, ऐसी पीर मिटावै ।।
अकबर के शासनकाल में ‘राय प्रवीण’ एक वेश्या थी। नृत्य और गीत के साथ वह सुन्दर कविता भी करती थी। वह महाकवि केशव की शिष्या थी।
केशवदास जी ने ‘कविप्रिया’ में इसका वर्णन भी किया है। अकबर इसके रूप-लावण्य पर मुग्ध था। उसने एक दिन इनसे भरी सभा में गाने को कहा।
पहले तो इसने मना किया, परन्तु बाद में विवश होकर इन्हें गाना पड़ा। इसके तत्काल निम्नलिखित दोहा बनाकर सुनाया, जिससे अकबर बहुत लज्जित हुआ—
विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान।
जूठी पातर चखत है, बारी बायस स्वान ।।
इनके बाद ‘ताज’ का नाम आता है। यद्यपि ये मुसलमान थीं फिर भी इन्हें श्रीकृष्ण से प्रेम हो गया था। इनकी कविता भक्ति रस से ओत-प्रोत है।
भक्तिकाल में महिला साहित्यकार का स्थान क्या था ?
भक्तिकाल की मधुर एवं कोमल साहित्यिक प्रवृत्तियाँ महिलाओं की रुचि के अनुकूल थीं। इस काल में कई उच्चकोटि की महिला कवियित्रियों के दर्शन होते हैं।
इन्होंने निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म श्रीकृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके अपने अन्तर्मन की भावनाओं को कोमलकान्द पदावली द्वारा व्यक्त किया।
भक्तिकालीन महिला काव्यकारों में सहजोबाई, दयाबाई और मीराबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सहजबाई चरणदास की शिष्या थीं।
उन्होंने निराकार प्रियतम के प्रति अनूठी उक्तियाँ कही हैं। प्रियतम की भक्ति-माधुरी में प्रेमोन्मत्त होकर सहजो कहते लगतीं
बाबा नगरु बसाओ।
ज्ञान दृष्टि सूं घट में देखौ, सुरति निरति लौ लावो ।
पाँच मारि मन बसकर अपने, तीनों ताप नसावौ ॥


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त | Maithili Sharan Gupta | हिन्दी निबंध |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त | Maithili Sharan Gupta | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- जीवन वृत्त
- काव्य की पृष्ठभूमि
- रचनायें
- काव्य की विशेषतायें
- उपसंहार
जीवन वृत्त
वर्तमान काव्यधारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का जन्म संवत् 1943 में झाँसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था।
मैथिलीशरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण था। वैष्णव भक्त होने के साथ-साथ सेठ जी का कविता के प्रति भी असीम अनुराग था। वे‘कनकलता’ के नाम से कविता किया करते थे।
मैथिलीशरण गुप्त जी का पालन पोषण भक्ति एवं काव्यमय वातावरण में ही हुआ। वातावरण के प्रभाव से गुप्त जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचना करने लगे थे।
मैथिलीशरण गुप्त जी की शिक्षा व्यवस्था घर पर ही हुई। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे झाँसी आये किन्तु वहाँ उनका मन न लगा। काव्य रचना की ओर प्रारम्भ से ही उनकी प्रवृत्ति थी।
एक बार अपने पिता जी की उस कापी में, जिसमें वे कविता किया करते थे, अवसर पाकर एक छप्पय लिख दिया।
पिता जी ने जब कापी खोली और उस छप्पय को पढ़ा, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त को बुलाकर महाकवि होने का आशीर्वाद दिया।
काव्य की पृष्ठभूमि
मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनायें कोलकाता के जातीय पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी।
पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आने पर उनकी रचनायें ‘सरस्वती’ में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेजी ने समय-समय पर उनकी रचनाओं में संशोधन किया और उन्हें ‘सरस्वती’ में प्रकाशित कर उन्हें प्रोत्साहन दिया।
द्विवेजी जी से प्रोत्साहन पाकर गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा जाग उठी और शनैः शनैः उसका विकास होने लगा। आज के हिन्दी साहित्य को गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा पर गर्व है।
रचनाएं
मैथिलीशरण गुप्त जी जीवन के प्रथम चरण से ही काव्य रचना में प्रवृत्त रहे।
राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, राम, कृष्ण तथा बुद्ध सम्बन्धी पौराणिक आख्याओं एवं राजपूत, सिक्ख तथा मुस्लिम संस्कृति प्रधान ऐतिहासिक कथाओं को लेकर मैथिलीशरण गुप्त जी ने लगभग चालीस काव्य-ग्रन्थों की रचना की है।
गुप्त जी ने मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त बंगला के काव्य-ग्रन्थों का अनुपम अनुवाद भी किया है। अनुवादित रचनायें ‘मधुप’ के नाम से हैं।
उन्होंने फारसी के विश्व विश्रुत कवि उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी अंग्रेजी के द्वारा हिन्दी में किया है।
रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुन्तला, वैतालिका, पद्मावती, किसान, पंचवटी, स्वदेशी संगीत, हिन्दू-शक्ति, सौरन्ध्री, वन वैभव, वक संहार, झंकार, अनघ, चन्द्रहास, तिलोत्तमा, विकट भट, मंगल घट, हिडिम्बा, अंजलि, अर्ध्य प्रदक्षिणा और जय भारत उनके काव्य हैं।
‘ साकेत ‘ पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें ला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ‘जय भारत’ उनकी नवीनतम कृति थी।
काव्य की विशेषताएं
मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में आज के युग की समस्त चेतनाओं, मान्यताओं और समस्याओं का प्रतिनिधित्व किया।
मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में सामाजिक जीवन के लक्ष्यों का निरूपण है, राष्ट्रीय विचारों के सौन्दर्य की झलक है।
परिवर्तनशील पुकार तथा पद-दलित, परवश और निराश भारतवर्ष को पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त कराने के लिए जागरण का महान् उद्घोष है। उनकी रचनाओं में प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति को मधुर झंकार है।
मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपने काव्य में वर्तमान युग की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व है।
मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाओं में केवल इतिवृत्तात्मकता थी, न उनमें भाषा का सौन्दर्य था और न भाव का।
परन्तु जैसे-जैसे मैथिलीशरण गुप्त जी का कवित्व विकसित होता गया, वैसे-वैसे उनकी रचनायें अधिक प्रौढ़ और परिष्कृत होती गईं। मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाओं में ‘पंचवटी’ में प्रथम बार उनके प्रौढ़ कवित्व के दर्शन होते हैं।
साकेत, यशोधरा तथा द्वापर में हमें गुप्त जी के काव्य का चरम सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है। इन काव्यों में भाव पक्ष के साथ-साथ कला का सहज सौन्दर्य है।
बंगला से अनुवाद किए हुए प्रन्थों में मेघनाथ वध, विरहिणी ब्रजांगना, वीरांगना और प्लासी का युद्ध बहुत सुन्दर अनुवाद हैं।
एक दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त जी का यह अनुवाद कार्य उनकी मौलिक रचनाओं की अपेक्षा हिन्दी को कहीं बड़ी देन है।
मैथिलीशरण गुप्त जी गाँधीवाद से प्रभावित थे। उन्होंने अपने काव्य में यथास्थान सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया है। साकेत में राम के वन जाते समय अयोध्या की जनता से वे सत्याग्रह कराते हैं—
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना,
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना।
जाओ यदि जा सके रौंद हमको यहाँ,
यों कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ।
अछूतोद्धार की ओर संकेत करते हुए गुप्त जी ने पंचवटी में लिखा है
गृह निषाद, शबरी तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में,
क्या ही सरल वचन होते हैं, इनके भोले आनन में।
इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी,
इनमें भी मन और भाव हैं, किन्तु नही वैसी वाणी ।
मैथिलीशरण गुप्त जी की ‘भारत-भारती’ में देश-प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। अंग्रेजी शासन के विरोध में होने के कारण यह पुस्तक कुछ समय तक प्रतिबंधित भी रही थी।
इसमें उन्होंने अतीत गौरव की भव्य झाँकी प्रस्तुत की है। भारतवर्ष की तत्कालीन दुर्दशा पर दुःख प्रकट करते हुए आपने लिखा है-
हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्यायें सभी ||
अहिंसा का महत्त्व स्वीकार करते हुए मैथिलीशरण गुप्त जी ने यशोधरा में राहुल के मुख से कितने सुन्दर शब्दों में आदर्श उपस्थित कराया है –
कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे।
रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी ॥
गाँधी जी ने चर्खा कातकर शरीर ढँकने का संदेश, स्वदेशी वस्त्र पहनने का सिद्धान्त भारतीय निर्धन जनता को दिया, जिससे कि थोड़े व्यय में उनका खर्च चल जाये और साथ ही साथ भारत की बेकारी की समस्या भी हल हो जाये, लोगों में स्वावलम्बन की भावना बढ़े।
मैथिलीशरण गुप्त जी ने यही बात सीता के मुख से कोल, किरात और भील स्त्रियों के प्रति कहलवा दी-
तुम अर्द्ध नग्न क्यों रहो अशेष समय में,
आओ हम काते बुनै काम की लय में।
भारतवर्ष में स्त्री जाति चिरकाल से उपेक्षित रही है। मैथिलीशरण गुप्त जी उनकी इस दशा पर दुःखी हो उठते हैं
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।
परन्तु आज का कवि अबलाओं को अबला मानने को तैयार नहीं –
आँचल में था दूध किन्तु अब आँखों में पानी न रहा था।
उर में था देशानुराग और आज न अबला नाम रहा था।
स्वर्ग और नरक के विषय में जनता में बड़ी-बड़ी धारणायें हैं। कोई कहता है स्वर्ग ऊपर नरक नीचे है। कोई कहता है स्वर्ग में भगवान रहते हैं इसलिये उसे बैकुण्ठ भी कहते हैं।
कुछ धारणायें हैं कि पुण्य करने से मृत्यु के समय देवता उस पुण्यात्मा को लेने आते हैं और सीधा उसे स्वर्ग को ले जाते हैं और नारकीय व्यक्ति को यमराज दूत।
इस प्रकार की देश में न जाने कितनी दन्तकथायें प्रचलित हैं। अब आप मैथिलीशरण जी का स्वर्ग और नरक सुन लीजिए –
बना लो जहाँ भी, वही स्वर्ग हैं, स्वयम्-भूत थोड़े कही स्वर्ग है।
खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है, भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग है ।।
सुनो स्वर्ग क्या है ? सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।
नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है, जहाँ स्वर्ग का भाव है, स्वर्ग है।
सुखी नारकी जीव भी हो गए, वहाँ धर्मराज स्वयम् जो हो गए।
सदाचार ही गौरवागार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है ।
प्रजा के प्रति राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं, इस बात को गुप्त जी साकेत में स्वयं राम के मुख से स्पष्ट कराते हैं
निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी,
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी।
निज रक्षा का अधिकार रहे जन-जन को,
सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को।
मैं नहीं मुक्ति का मार्ग, दिखाने आया।
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।
मैं आर्यों का आदर्श बताने आया,
जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया।
सुख शान्ति हेतु मैं क्रान्ति मचाने आया,
विश्वासी का विश्वास जगाने आया।
मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपने ‘अनघ’ काव्य में ग्राम सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट की हैं। उसमें संघ को एक ग्राम सुधार के रूप में चित्रित किया है-
मरम्मत कभी कुओं घाटों की सफाई कभी हाटों-बाटों की,
आप अपने हाथों करता है।
कहीं-कहीं मैथिलीशरण गुप्त जी ने प्रकृति के भी सुन्दर चित्र अंकित किए हैं। उनकी प्रकृति सदा शान्त और नूतन है। गुप्त जी ने प्रकृति को आलम्बन मानकर उसका वर्णन किया है। पंचवटी की ये पंक्तियाँ कितनी सुन्दर हैं-
चारु चन्द्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल थल में।
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई थी, अवनि और अम्बर तल में ।।
फैलाए यह एक पक्ष लीला किए छाती पर बल दिए अंग ढीला किए।
देखो ग्रीवा भंग संग किस ढंग से, देख रहा है हमें विहंग उमंग से ।।
मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता की भाषा सरल और सुबोध है। उसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है।
मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता में कोमलता और माधुर्य का अभाव है। कहीं-कहीं तो रुखा गद्य-सा जान पड़ता है।
इनकी कविता की सफलता का रहस्य भाषा तथा भावों की सुबोधता है न कि उनका काव्य-सौन्दर्य एक आलोचक का विचार है कि गाँधी जी जो कुछ भी अपने भाषणों में कह देते थे प्रेमचन्द जी उसे अपने उपन्यासों में और मैथिलीशरण उसे अपनी कविता में ज्यों का त्यों कुछ उलट-फेर करके उतार दिया करते थे।
मैथिलीशरण गुप्त जी ने प्रबन्ध, मुक्त, खण्ड काव्य, गीत आदि सभी काव्य-प्रवृत्तियों पर लिखा परन्तु अधिक सफलता उन्हें प्रबन्ध काव्य के लिखने में मिली।
द्विवेदी जी के ‘कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता’ लेख से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखा।
साकेत के नवें सर्ग में गुप्त जी का काव्य सौन्दर्य, उर्मिला की भावात्मक अनुभूतियाँ, उसका त्यागमय विरह अत्यन्त उच्च कोटि का है।
उनमें वास्तव में हमें गुप्त जी के महाकवित्व के दर्शन होते हैं। उर्मिला ही साकेत की आत्मा है, स्वामिनी है और अधिक कहा जाए तो उर्मिला ही साकेत का सर्वस्व है।
कुछ प्रसंग उद्धृत करना उचित होगा। कल राज्याभिषेक होने वाला है। रात को देर तक जागने के कारण लक्ष्मण सुबह देर तक सोते रहे उर्मिला पहिले उठ बैठी। उर्मिला लक्ष्मण पर व्यंग्य करती है—
उर्मिला बोली “अजी तुम जग गए”
स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए।
लक्ष्मण ने तुरन्त शिष्ट उपहास करते हुए मार्मिक उत्तर दिया-
मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुआ,
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ।
साकेत में उर्मिला के भाव-सौन्दर्य की हमें पाँच झाँकियाँ मिलती हैं-
- राज्याभिषेक के दिन प्रभात में
- लक्ष्मण के वन जाते समय में
- चित्रकूट में
- विरहावस्था में
- लक्ष्मण के अयोध्या लौट आने पर पुनर्मिलन के अवसर पर
राज्याभिषेक के दिन प्रभात में
राज्याभिषेक के दिन उर्मिला प्रातः प्रासाद में खड़ी है-
अरुण पट पहिने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में।
प्रकट मूर्तिमती ऊषा ही तो नहीं, कान्ति की किरणें उजेला कर रहीं।
देखती है जब जिधर वह सुन्दरी चमकती है दामिनी-सी द्युति भरी ॥
लक्ष्मण के वन जाते समय में
दूसरा प्रसंग अत्यन्त कारुणिक है। राम वन को जा रहे हैं, सीता को भी साथ चलने की स्वीकृति मिल चुकी है, लक्ष्मण भी साथ जा रहे हैं, परन्तु उर्मिला का क्या होगा—
आह आह ! कितना सकरुण मुख था।
आर्द्रता-सरोज अरुण वह मुख था॥
चित्रकूट में
तीसरा प्रसंग चित्रकूट में आता है। गुप्त जी ने सीता के बहाने से लक्ष्मण को कुटिया में पड़ी हुई उर्मिला से मिलने का अवसर दिया है।
भीतर जाते ही लक्ष्मण ठगे से रह जाते हैं।अभिषेक के पहले की कनक लता उर्मिला अब केवल छायामात्र है-
तो दीख पड़ी-कोणस्थ उर्मिला रेखा,
यह काया है या शेष उसी की छाया।
क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया।
लक्ष्मण को अपने पास आने में झिझकता हुआ देखकर उर्मिला तुरन्त कह उठती है-
मेरे उपवन के हिरण, आज वनचारी,
मैं बाँध न लूंगी तुम्हे, तजो भय भारी।
विरहावस्था में
चौथे प्रसंग में अब आप उर्मिला का विरह देखिये। सखी भोजन का परोस कर लाती है परन्तु उर्मिला यह कह कर हटा देती है—
अरी व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई,
हटा थाल, तू क्यों इसे आप लाई।
बनाती रसोई, सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती।
रहा किन्तु मेरे लिए एक सेना, खिलाऊँ किसे मैं अलोना-सलोना ।।
शीतल-मन्द सुगन्धित वायु उर्मिला के निकट आती है पर यह उसका आनन्द कैसे ले सकती है। वह उससे पीछे लौट जाने की प्रार्थना करती है-
अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज।
तू है फूलों की पली, यह कोटों की सेज ॥
प्रिय के विरह से वो से ही अनुपात नहीं हो रहा, अपितु समस्त शरीर से स्वेद रूपी अश्रु बहने लगे है-
नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद |
टपक उठा है देख अ रोम-रोम से स्वेद ॥
चकवी जब पहले कभी रोया करती थी, उर्मिला समझती थी कि वह गा रही है, परन्तु आज जब अपने ऊपर आकर बोती, तब अनुभव हुआ कि चकवी रोती थी या गाया करती थी—
चातकि मुझको आज ही हुआ भाव का भान |
हा ! वह तेरा रुदन था में समझी थी गान।|
उर्मिला अपने मन को तरह-तरह से समझाती है कि प्रिय पास ही हैं, कहीं दूर नहीं गये, किन्तु आँखें फिर रोये बिना नहीं मानती-
नयनों को रोने दे,
मन तू संकीर्ण न बन प्रिय बैठे हैं।
आँखों से ओझल हो,
गए नहीं वे कही यही बैठे हैं। कभी सोचती है कि मैं भी उसी वन में जाकर बिना उन्हें बताये, वहाँ रहने लगूं, आखिर देखने भर को तो मिल जायेंगे-
यही आता है इस मन में,
छोड़ धाम-धन जाकर में भी रहूँ उसी वन में।
बीच-बीच में उन्हें देख लूँ, मैं झुरमुट की ओट,
जब वे निकल जाये तब लेटू उसी धूल में लोट ।।
रहें रत वे निज साधन में,
यही आता है इस मन में ।
अन्त में उर्मिला सखी से यही प्रार्थना करती है कि देख, प्रिय-विरह में में पागल हो जाऊं, तो तू मेरा कुछ उपचार न करना, चाहे मैं हँसती रहूँ या रोती रहूँ-
सजनि! पागल भी यदि हो सकें।
कुशल तो, अपनापन खो सकूँ ।।
शपथ है उपचार न कीजियो ।
बस इसी प्रिय कानन कुंज में ॥
अवधि की सुधि तुम लीजियो ।
मिलन भाषण के स्मृति पुँज में ॥
अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो,
हँसन रोदन से न पसीजियो ।
लक्ष्मण के अयोध्या लौट आने पर पुनर्मिलन के अवसर पर
पाँचवाँ प्रसंग अयोध्या में लक्ष्मण और उर्मिला का चौदह वर्ष बाद का पुनर्मिलन है। लक्ष्मण लौट आये हैं, वर्षों की मिलन की साथ आज पूरी होने वाली है।
आज छाया मात्र उर्मिला के रोम-रोम में आह्लाद और उल्लास है। सखी ने उर्मिला से शृंगार करने को कहा, परन्तु आज उसे शृंगार की आवश्यकता नहीं।
हाय ! सखी, शृंगार ? मुझे अब भी सोहेंगे।
क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे ?
उर्मिला ने चौदह वर्षों में अपने को जैसा रखा है और जैसी वह है उसी रूप में आज वह उनसे मिलेगी। वह सखी से कहने लगती है-
नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छले न जावें।
जैसी हूँ मैं नाथ मुझे वैसा ही पावें ॥
शूर्पणखा में नहीं, हाय तू तो रोती है ।
अरी हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है ।
सखी नहीं मानती, उर्मिला को विवश होकर वस्त्रालंकार धारण करने पड़ते हैं। परन्तु एक वास्तविक अभाव की ओर संकेत करती है-
तो ला भूषण वसन, इष्ट हो तुझको जितने ।
पर यौवन उन्माद कहाँ से पाऊँगी मैं ।
वह खोया धन आज कहाँ सखि पाऊँगी मैं।
परन्तु इतने में उर्मिला के हृदय में स्वाभाविक ओज उमड़ पड़ता है, कितनी सुन्दर और मार्मिक उक्ति है—
विरह रुदन में गया, मिलन में भी रोऊँ ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए पदरज घोऊँ ।।
जब थी तब थी अलि, उर्मिला उनकी रानी।
वह बरसों की बात, आज हो गई पुरानी ॥
अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी |
में शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी ॥
आज कितना परिवर्तन हो गया है उर्मिला के हृदय में वह अब केवल सेवा की प्यासी है। एक दिन था जब लक्ष्मण उर्मिला से स्वयं कहते थे—
धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ।
और उर्मिला इस पर स्वाभिमानपूर्ण उत्तर देती थी-
दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहाना इसलिए ?
उर्मिला आज दासी बनने में अपना गौरव समझ रही है। वास्तव में प्रारम्भ में स्त्री अपने को बहुत कुछ समझती है, उसे अपने पर बहुत गर्व होता है।
परन्तु कुछ समय पश्चात् जब उसके पास कुछ नहीं रहता और पुरुष के पास सब कुछ खोकर भी उसके लिए बहुत कुछ रहता है, तो वह पुरुष की दासी हो जाती है।
अभी लक्ष्मण मिलने के लिए उर्मिला के निकट आये नहीं थे, केवल सखी से ही उर्मिला की बातें हो रही थीं। सहसा लक्ष्मण आ जाते हैं और उर्मिला अपनी सुधबुध खो बैठती है जैसा कि प्रायः ऐसे अवसरों पर होता है।
मैथिलीशरण गुप्त जी की तूलिका ने कितना सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है, देखिए-
देखा प्रिय को चॉक प्रिया ने, सखी किधर थी ?
पैरों पड़ती हुई उर्मिला हाथों पर थी।
लेकर मानों विश्व बिरह उस अन्तःपुर में,
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में।”
परन्तु उर्मिला स्त्री ही थी। उसे सहसा ध्यान आया कि यौवन के कितने सुहावने दिन व्यर्थ में ही व्यतीत हो गए। उनका हृदय नीरव चीत्कार कर उठा क्रन्दन करती हुई वह कहने लगी-
स्वामी, स्वामी, जन्म-जन्म के स्वामी मेरे।
किन्तु कहाँ वे अहोरात्र, वे सांझ सवेरे ।।
खोई अपनी हाय ! कहाँ वह खिलखिल खेला।
प्रिय ! जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला ॥
लक्ष्मण केवल सामयिक सां भर दे पाए हैं-
वह वर्षा की बाढ़ गई, उसको जाने दो।
शुचि गम्भीरता प्रिये, शरद की यह आने दो ॥
ये चार चित्र लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन के क्षणों के बड़े मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं।
उपसंहार
साकेत में गुप्त जी निःसन्देह महान् हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जितना प्रबन्ध काव्य उन्होंने लिखा है, उतना हिन्दी के किसी अन्य कवि ने नहीं। प्रबन्ध काव्य में साधना की आवश्यकता होती है। गुप्त जी निःसन्देह हिन्दी के महान् साधक थे।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
मैथिलीशरण गुप्त का जीवन परिचय ?
वर्तमान काव्यधारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का जन्म संवत् 1943 में झाँसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था।
उनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। वैष्णव भक्त होने के साथ-साथ सेठ जी का कविता के प्रति भी असीम अनुराग था। वे‘कनकलता’ के नाम से कविता किया करते थे।
गुप्त जी का पालन पोषण भक्ति एवं काव्यमय वातावरण में ही हुआ। वातावरण के प्रभाव से मैथिलीशरण गुप्त जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचना करने लगे थे।
मैथिलीशरण गुप्त जी की शिक्षा व्यवस्था घर पर ही हुई। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे झाँसी आये किन्तु वहाँ उनका मन न लगा। काव्य रचना की ओर प्रारम्भ से ही उनकी प्रवृत्ति थी।
एक बार अपने पिता जी की उस कापी में, जिसमें वे कविता किया करते थे, अवसर पाकर एक छप्पय लिख दिया।
पिता जी ने जब कापी खोली और उस छप्पय को पढ़ा, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैथिलीशरण को बुलाकर महाकवि होने का आशीर्वाद दिया।
मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
मैथिलीशरण गुप्त जी जीवन के प्रथम चरण से ही काव्य रचना में प्रवृत्त रहे।
राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, राम, कृष्ण तथा बुद्ध सम्बन्धी पौराणिक आख्याओं एवं राजपूत, सिक्ख तथा मुस्लिम संस्कृति प्रधान ऐतिहासिक कथाओं को लेकर गुप्त जी ने लगभग चालीस काव्य-ग्रन्थों की रचना की है।
गुप्त जी ने मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त बंगला के काव्य-ग्रन्थों का अनुपम अनुवाद भी किया है। अनुवादित रचनायें ‘मधुप’ के नाम से हैं।
उन्होंने फारसी के विश्व विश्रुत कवि उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी अंग्रेजी के द्वारा हिन्दी में किया है।
रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुन्तला, वैतालिका, पद्मावती, किसान, पंचवटी, स्वदेशी संगीत, हिन्दू-शक्ति, सौरन्ध्री, वन वैभव, वक संहार, झंकार, अनघ, चन्द्रहास, तिलोत्तमा, विकट भट, मंगल घट, हिडिम्बा, अंजलि, अर्ध्य प्रदक्षिणा और जय भारत उनके काव्य हैं।
‘साकेत’ पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें ला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ‘जय भारत’ उनकी नवीनतम कृति थी।


युग-प्रवर्त्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | हिन्दी निबंध |
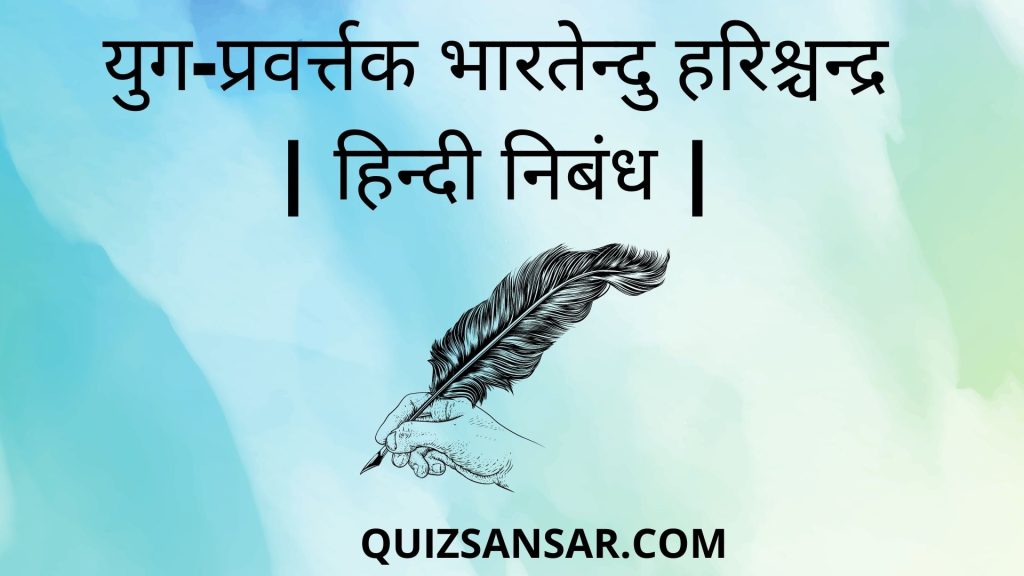
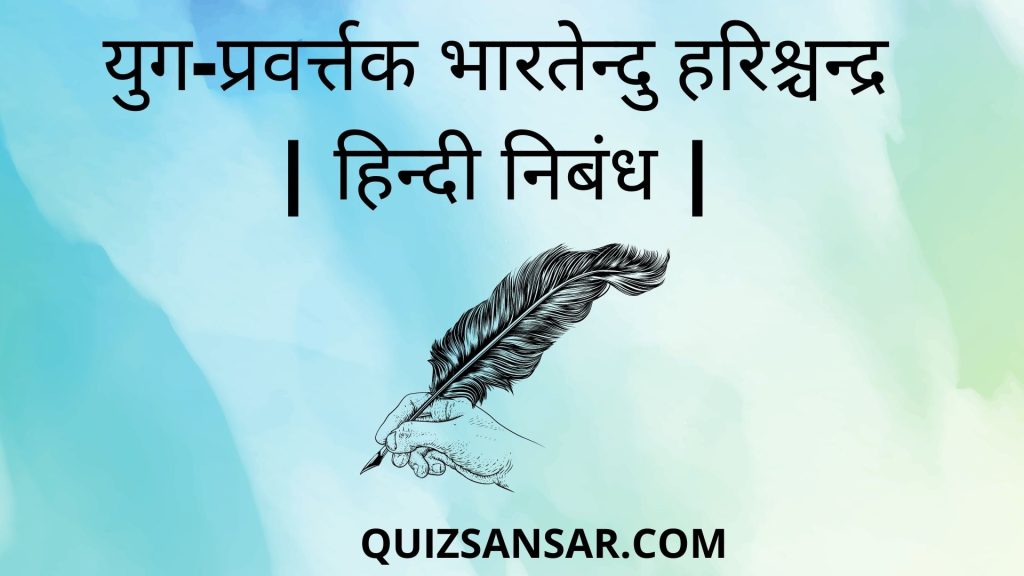
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है युग-प्रवर्त्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- जन्मकालीन परिस्थितियाँ
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- भाषा के क्षेत्र में नवयुग प्रवर्तक
- बहुमुखी साहित्य सेवा
- काव्यकार
- युग प्रवर्तक
- नाटक कार
- उपसंहार
जन्मकालीन परिस्थितियाँ
भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। शासन की भाषा अंग्रेजी स्वीकृत हो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र चुकी थी, पद-लालसा से लालायित भारतीय, अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता अपनाने में गौरव समझने थे।
सभ्य और सुशिक्षित भारतीय समाज हिन्दी को हेय दृष्टि से देखने लगा था। सर सैय्यद जैसे हिन्दी के नाम पर बॉसों उछल पड़ते थे और हिन्दी को “गँवारू बोली” कहकर सम्बोधित करने में अपने विद्वान होने की सार्थकता प्रकट करते थे।
हिन्दू सभ्यता, संस्कृति और साहित्य पर चारों ओर से कुठाराघात हो रहे थे। लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि हिन्दी पढ़कर भी कोई सभ्य और शिक्षित हो सकता है।
हिन्दी की दशा तो अव्यवस्थित थी ही परन्तु हिन्दी को भी लोग नापसन्द करने में गौरव का अनुभव करने लगे थे।
ऐसे समय में हिन्दी को एक ऐसे दृढ़ आत्मविश्वासी कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसमें युग परिवर्तन करने की क्षमता हो, जो राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकता हो, अथवा मातृभाषा की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता हो।
वह समय हिन्दी के लिए संक्रान्ति काल था। राजनीति तथा समाज में नवीन क्रान्ति हो रही थी।
ऐसे वातावरण में हिन्दी में नये युग के प्रवर्तक एवं हिन्दी साहित्य में स्वतन्त्रता के प्रथम उद्घोषक भारतेन्दु का भारत भूमि में अवतरण हुआ।
जीवन वृत्त
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंश में हुआ था। इनके पिता बापू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास) के प्रतिभा सम्पन्न कवि थे।
भारतेन्दु जी पर घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव था। उन्होंने पाँच वर्ष की अवस्था में निम्नलिखित दोहे की रचना की थी
लै ब्यौडा ठाड़े भये, श्री अनुरुद्ध सुजान।
वाणासुर की सेन को, हनन लगे भगवान ।।
उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। दस वर्ष की अवस्था में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया।
फलस्वरूप शिक्षा का क्रम बीच में ही टूट गया। तेरह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। तदनन्तर इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहाँ ये बंगला भाषा के सम्पर्क में आये।
अनेक तीर्थयात्रायें करने के कारण भारतेन्दु को और देश के विभिन्न प्रान्तों के सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने व समझने का अवसर मिला।
वह स्वतन्त्रता प्रेमी तथा प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में दयालुता थी। वे दानी थे। उनकी सत्यता के प्रति अटूट श्रद्धा थी।
उन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान रूप से कृपा थी। उन्होंने सरस्वती की सेवा में लक्ष्मी को पानी की तरह बहाया।
अपने जीवन काल में भारतेन्दु ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं, सभाओं, साहित्यिक गोष्ठियों तथा नवीन साहित्यकारों को जन्म दिया। तत्कालीन साहित्यकारों में भारतेन्दु सर्वप्रथम थे।
जीवन के अन्तिम दिनों में भारतेन्दु आर्थिक कष्टों से दब गये थे, उन्हें क्षय रोग हो गया था।
सम्वत् 1941 में हिन्दी साहित्य का यह प्रकाश पुंज सदैव के लिये समाप्त हो गया।
रचनाएं
भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने साहित्य की प्रत्येक दिशा को नई गति और नई चेतना प्रदान की।
नाटक, काव्य, इतिहास, निबन्ध, व्याख्यान आदि सभी विषयों पर अधिकारपूर्वक लिखा। अपने सत्रह अट्ठारह वर्ष के साहित्यिक जीवन में भारतेन्दु ने अनेक ग्रन्थों की रचना की।
भारतवीणा, वैजयन्ती, सुमनांजलि, सतसई, शृंगार, प्रेम-प्रलाप, होली, भारतेन्दु जी के उत्कृष्ट काव्य-प्रन्य हैं।
भारतेन्दु जी की सबसे बड़ी देन नाटकों के क्षेत्र में है‘चन्द्रावली’, ‘भारत दुर्दशा’, ‘नील देवी’, ‘अंधेर नगरी’, ‘प्रेम योगिनी’, ‘विषस्य विषमौषधम’ और ‘वैदिकी हिंसा न भवति ये भारतेन्दु जी केमौलिक नाटक हैं।‘विद्या सुन्दर’, ‘पाखण्ड विडम्बन’, ‘धनंजय विजय’, ‘कर्पूरमंजरी’,’मुद्रा राक्षस’, ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ और ‘भारत जननी’ आपके अनुदित नाटक हैं।
सुलोचना, शीलवती आदि आपके आख्यान हैं।‘परिहास पंचक’ में हास्य रस सम्बन्धी गद्य हैं। ‘काश्मीर कुसुम’ और ‘बादशाह दर्पण’ आपके इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ हैं।
भारतेन्दु जी ने अपने अल्प जीवनकाल में सौ से अधिक प्रन्थों की रचना की।
भाषा के क्षेत्र में नवयुग प्रवर्तक
भारतेन्दु जी का काव्य विविधतापूर्ण है, उनकी कुछ रचनायें भक्ति रस से भरी हुई हैं। कुछ रचनाओं में रीतिकाल की सी झलक दिखलाई पड़ती है।
अन्य रचनाओं में नवीन चेतनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार हम भारतेन्दु के समस्त काव्यों को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-
- भक्ति प्रधान
- शृंगार प्रधान
- देश-प्रेम प्रधान
- सामाजिक समस्या प्रधान
भक्ति प्रधान
उनकी भक्ति प्रधान रचनायें राधा-कृष्ण से सम्बन्धित हैं। इन रचनाओं में वे सूर, तुलसी की कोटि में आते हैं। एक उदाहरण देखिए
वाज्यों करै नुपुर खौननि के निकट सदा,
पदतल माँहि मन मेरी बिहयों करै।
बाज्यौ करै बंशी धुनि, पूरि रोम-रोम मुख,
मन्द मुस्कानि मन मनहि हय करे ।।
हरीचन्द चलनि, मुरनि बतरानि चित्त,
छाई रहै छवि जुग दृगनि भयों करै।
प्रानहुँ ते प्यारो रहै प्यारो तू सदाई प्यारे,
पीत पट सदा हिय बीच फहरयाँ करै ।।
श्रृंगार प्रधान
शृंगार प्रधान रचनाओं में ये पद्माकर, घनानन्द और रसखान की कोटि में आते हैं। भारतेन्दु को संयोग की अपेक्षा वियोग चित्रण में अधिक सफलता मिली है।
गोपिकाओं को है कि वे कृष्ण को एक बार भी प्यार से आँखें भर कर न देख पाईं।
इसलिए उनके अतृप्त नेत्र आज भी कृष्ण की प्रतीक्षा में खुले हुए हैं और मृत्यु के बाद ज्यों के त्यों खुले रहेंगे। कितना स्वाभाविक और मनोहारी वर्णन है
इन दुखियान को न सुख सपनेहू मिल्यौं,
यों ही सदा व्याकुल विकल अकुलायेंगी।
प्यारे हरिचन्दज की गौन जानि औधि जो पै
जैह प्रान तऊ ये तौ संग न समायेंगी।
देख्यो एक बार हूँ न नैन भरि तोहि यातें,
जौन-जौन लोक जैहै तहाँ पछितायेंगी।
बिना प्राण प्यारे भये दरस तिहारे हाय,
देखि लीजो आँखें ये खुली ही रह जायेंगी ।
संयोग का चित्रण भी कहीं-कहीं बहुत सुन्दर है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतेन्दु, गोपियों के मुख से अपनी ही बात कह रहे हैं। उदाहरण देखिए
रोकत हैं तो अमंगल होय, और प्रेम नस जो कहें प्रिय जाइये।
जो कहें जाहु न, तो प्रभुता, जो कछू न कहें तौ सनेह नसाइये ।
जो हरिचन्द कहें, तुमरे बिन, जियें न तो यह क्यों पतियाइये।
तासौ पयान समै तुमसौं हम का कहें प्यारे हमें समझाइये ।।
देश-प्रेम प्रधान
अपनी देश-प्रेम प्रधान रचनाओं द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय जागरण का प्रथम उद्घोष किया। भारतेन्दु भारत की दुर्दशा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं
गयो राज, धन, तेज, रोष, बल, शान नसाई,
बुद्धि वीरता, श्री उछाह सूरत बिलाई ।
आलस, कायरपनो, निरुद्यमता अब छाई,
रही मूढ़ता, बैर, परस्पर कलह, लड़ाई।
सब विधि नासी भारत प्रजा, कहूँ न रह्यो अवलम्बन अब |
जागो जागो करुनायतन, फेरि जागिहाँ, नाथ कब ।।
सामाजिक समस्या प्राधान
सामाजिक समस्याओं के चित्रण द्वारा भारतेन्दु ने कविता-कामिनी की रीतिकालीन विलासिता के झुरमुटों से निकालकर जन-जीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया।
भारतवर्ष की भिन्नता पर दुःख प्रकट करते हुए भारतेन्दु कहते हैं
भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात |
विविध बेस, मतहूँ विविध भाषा विविध लखात ॥
बहुमुखी साहित्य
हिन्दी के उत्थान के लिए भारतेन्दु ने अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया था। मातृ-भाषा के विषय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है-
अंग्रेजी पढ़ कै जदपि सब गुन होत प्रवीन |
पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ।।
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ।।
काव्यकार
भारतेन्दु की कविता में बृजभाषा और खड़ी बोली दोनों का रूप मिलता है, परन्तु इतना अवश्य है कि इन्होंने खड़ी बोली में बहुत कम रचना की।
ये भाषा की शुद्धता के पक्षपाती थे। इनकी भाषा बड़ी परिष्कृत, व्यवस्थित और प्रवाह युक्त है।
प्राकृत तथा अपभ्रंश काल के शब्दों का, जिन्हें कवि लोग अपनी कविताओं में स्थान देते चले आ रहे थे, इन्होंने बहिष्कार किया।
भारतेन्दु ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी के कर्णकटु शब्दों को मधुर बनाया तथा विदेशी शब्दों को हिन्दी के ढाँचे में ढालकर ग्रहण किया।
भारतेन्दु की रचनाओं में सभी रसों का सुन्दर समायोजन है। शृंगार, शान्त, रौद्र, भयानक, वीभत्स, करुण, वात्सल्य, अद्भुत और हास्य सभी रसों का उनको रचनाओं में सुन्दर परिपाक है।
रसों के साथ अलंकारों का सहजे सौन्दर्य भी देखने योग्य है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आये हैं।
भारतेन्दु की छन्द योजना अत्यन्त विस्तृत है। तुलसीदास की भाँति भारतेन्दु ने भी प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी शैलियों में रचनायें कीं।
इन्होंने भाव और भाषा के अनुरूप पद, कवित्त, सवैया, दोहा, रोला, छप्पय, चौपाई, बरवै, हरिगीतिका, बसन्त-तिलका आदि छन्दों का सफल प्रयोग किया।
युग प्रवर्तक
हिन्दी गद्य के क्षेत्र में भारतेन्दु जी की अमूल्य सेवायें हैं। आज हिन्दी का जो रूप हमारे सामने है वह भारतेन्दु की साहित्य साधना का ही प्रसाद है।
भारतेन्दु के साहित्य क्षेत्र में आने के समय भाषा का स्वरूप अस्थिर था, वह निष्माण और रूपहीन थी।
एक ओर राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द उसे उर्दू प्रधान बनाना चाहते थे, दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंह उसे संस्कृत प्रधान बनाना चाहते थे।
लल्लूलाल की भाषा में ब्रजभाषापन था और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वोपन की मात्रा अधिक थी। भारतेन्दु ने अस्थिर भाषा को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से स्थिर रूप प्रदान किया।
उन्होंने हिन्दी को सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने विदेशी शब्दों भी हिन्दी के ढाँचे में ढालकर महण किया। भारतेन्दु की भाषा में स्वाभाविकता थी और माधुर्य था।
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने अनेक साहित्य साधकों को जन्म दिया। भारतेन्दु अपने समय के हिन्दी साहित्य और भाषा के एकमात्र नेता थे।
उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिन्दी गद्य को विकासोन्मुख बनाया, उसका मार्ग प्रदर्शन किया, इसलिये वह युग भारतेन्दु युग के नाम से प्रसिद्ध है।
नाटक कार
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र गद्य की भाँति हिन्दी नाटकों के भी जन्मदाता हैं। वास्तव में उनसे पूर्व नाटकों का क्षेत्र बिल्कुल शून्य था। जो दो-चार नाटक थे भी उनमें न तो मौलिकता थी और न शास्त्रीय नाटकीय तत्त्व।
मुसलमानों के आधिपत्य के कारण भारतेन्दु से पूर्व नाटकों का समुचित विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि मुसलमानों की दृष्टि में किसी भी आधिभौतिक शक्ति का मंच पर लाना कुछ समझा जाता था, भारतेन्दु के समय में कुछ नाटकं कम्पनियाँ थीं, जो अश्लील अभिनयों से जनरुचि को विकृत करने में प्रयत्नशील थीं।
भारतेन्दु जी नाटक रचना में बंगला से सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने हिन्दी में भी नाटक लिखने का निश्चय किया।
उनके अनुवादित और मौलिक नाटकों की संख्या चौदह है।
प्रायः ये सभी नाटक अपने समय के लोकप्रिय नाटक थे तथा वे अपने नाटकों का निर्देशन और अभिनय स्वयं किया करते थे।
भारतेन्दु जी के सभी नाटक खड़ी बोली में लिखे गये हैं। उनके मौलिक नाटकों में ‘भारत दुर्दशा” का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतेन्दु जी के नाटकों के विषय में लिखा है कि “उन्होंने सामग्री जीवन के क्षेत्रों से ली है।” वास्तव में उनके नाटक स्वयं नाटककार के जीवन से एवं तत्कालीन सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित थे। ‘चन्द्रावली नाटिका’ भारतेन्दु जी को अपने नाटकों में सबसे अधिक प्रिय थी।
इसमें चन्द्रावली और कृष्ण के एक छोटे से आख्यान द्वारा प्रेम का सच्चा आदर्श प्रदर्शित किया गया है। “वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति” एक सुन्दर प्रहसन है।
यही इनका पहिला मौलिक नाटक कहा जाता है। भारतेन्दु जी केवल नाटकों के जन्मदाता मात्र थे।
नाट्यकला की दृष्टि से हमें उनमें कुशल नाटककार के दर्शन नहीं होते, अधिकांश उत्कृष्ट नाटक तो बाद में लिखे गये।
उपसंहार
भारतेन्दु जी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भावात्मक आदि सभी विषयों पर लेखनी चलाई।
उनकी प्रतिभा से हिन्दी साहित्य का कोना-कोना प्रकाशित हुआ। खेद है कि 35 वर्ष की अल्पायु में ही वे काल कवलित हो गये, परन्तु-
जयन्ति ते सुकृतिन: रससिद्धाः कवीश्वराः,
नास्ति येषाम् यशः काये, जरामरणजम् भयम् ॥
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन परिचय ?
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंश में हुआ था। इनके पिता बापू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास) के प्रतिभा सम्पन्न कवि थे।
भारतेन्दु जी पर घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव था। उन्होंने पाँच वर्ष की अवस्था में निम्नलिखित दोहे की रचना की थी
लै ब्यौडा ठाड़े भये, श्री अनुरुद्ध सुजान।
वाणासुर की सेन को, हनन लगे भगवान ।।
उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। दस वर्ष की अवस्था में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया।
फलस्वरूप शिक्षा का क्रम बीच में ही टूट गया। तेरह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। तदनन्तर इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहाँ ये बंगला भाषा के सम्पर्क में आये।
अनेक तीर्थयात्रायें करने के कारण भारतेन्दु को और देश के विभिन्न प्रान्तों के सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने व समझने का अवसर मिला।
वह स्वतन्त्रता प्रेमी तथा प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में दयालुता थी। वे दानी थे। उनकी सत्यता के प्रति अटूट श्रद्धा थी।
उन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान रूप से कृपा थी। उन्होंने सरस्वती की सेवा में लक्ष्मी को पानी की तरह बहाया।
अपने जीवन काल में भारतेन्दु ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं, सभाओं, साहित्यिक गोष्ठियों तथा नवीन साहित्यकारों को जन्म दिया। तत्कालीन साहित्यकारों में भारतेन्दु सर्वप्रथम थे।
जीवन के अन्तिम दिनों में भारतेन्दु आर्थिक कष्टों से दब गये थे, उन्हें क्षय रोग हो गया था।
सम्वत् 1941 में हिन्दी साहित्य का यह प्रकाश पुंज सदैव के लिये समाप्त हो गया।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की जन्मकालीन परिस्थितियां क्या थीं ?
भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। शासन की भाषा अंग्रेजी स्वीकृत हो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र चुकी थी, पद-लालसा से लालायित भारतीय,अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता अपनाने में गौरव समझने थे।
सभ्य और सुशिक्षित भारतीय समाज हिन्दी को हेय दृष्टि से देखने लगा था। सर सैय्यद जैसे हिन्दी के नाम पर बॉसों उछल पड़ते थे और हिन्दी को “गँवारू बोली” कहकर सम्बोधित करने में अपने विद्वान होने की सार्थकता प्रकट करते थे।
हिन्दू सभ्यता, संस्कृति और साहित्य पर चारों ओर से कुठाराघात हो रहे थे। लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि हिन्दी पढ़कर भी कोई सभ्य और शिक्षित हो सकता है।
हिन्दी की दशा तो अव्यवस्थित थी ही परन्तु हिन्दी को भी लोग नापसन्द करने में गौरव का अनुभव करने लगे थे।
ऐसे समय में हिन्दी को एक ऐसे दृढ़ आत्मविश्वासी कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसमें युग परिवर्तन करने की क्षमता हो, जो राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकता हो, अथवा मातृभाषा की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर सकता हो।
वह समय हिन्दी के लिए संक्रान्ति काल था। राजनीति तथा समाज में नवीन क्रान्ति हो रही थी।
ऐसे वातावरण में हिन्दी में नये युग के प्रवर्तक एवं हिन्दी साहित्य में स्वतन्त्रता के प्रथम उद्घोषक भारतेन्दु का भारत भूमि में अवतरण हुआ।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाएं कौन-कौन सी है ?
भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने साहित्य की प्रत्येक दिशा को नई गति और नई चेतना प्रदान की।
नाटक, काव्य, इतिहास, निबन्ध, व्याख्यान आदि सभी विषयों पर अधिकारपूर्वक लिखा। अपने सत्रह अट्ठारह वर्ष के साहित्यिक जीवन में भारतेन्दु ने अनेक ग्रन्थों की रचना की।
भारतवीणा, वैजयन्ती, सुमनांजलि, सतसई, शृंगार, प्रेम-प्रलाप, होली, भारतेन्दु जी के उत्कृष्ट काव्य-प्रन्य हैं।
भारतेन्दु जी की सबसे बड़ी देन नाटकों के क्षेत्र में है‘चन्द्रावली’, ‘भारत दुर्दशा’, ‘नील देवी’, ‘अंधेर नगरी’, ‘प्रेम योगिनी’, ‘विषस्य विषमौषधम’ और ‘वैदिकी हिंसा न भवति ये भारतेन्दु जी केमौलिक नाटक हैं।‘विद्या सुन्दर’, ‘पाखण्ड विडम्बन’, ‘धनंजय विजय’, ‘कर्पूरमंजरी’,’मुद्रा राक्षस’, ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ और ‘भारत जननी’ आपके अनुदित नाटक हैं।
सुलोचना, शीलवती आदि आपके आख्यान हैं।‘परिहास पंचक’ में हास्य रस सम्बन्धी गद्य हैं। ‘काश्मीर कुसुम’ और ‘बादशाह दर्पण’ आपके इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ हैं।
भारतेन्दु जी ने अपने अल्प जीवनकाल में सौ से अधिक प्रन्थों की रचना की।


पश्चात्ताप | हिन्दी निबंध |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है पश्चात्ताप | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- काहावत की सार्थकता
- पश्चाताप की निरर्थकता
- उपसंहार
प्रस्तावना
सृष्टि में मानव चेतना-युक्त प्राणी है। उसके पास बुद्धि का अक्षय कोष है। बुद्धि का सफल प्रयोग ही मानव को पशु वर्ग से अलग करने वाली सबल रेखा है।
अपने बुद्धि बल के सहारे ही वर्तमान में रहता हुआ मनुष्य, भूत और भविष्य में विचरण करता है। क्या हो चुका है और क्या होगा इस पर शान्तिपूर्वक विचार करता है तथा अपने लिए एक निरापद मार्ग खोज निकालता है।
कभी-कभी ऐसे भी क्षण आते हैं, जब उसे अपने किये हुए कार्य पर पछताना और दुःखी होना पड़ता है। इस दुःख की अग्नि की जलन से वह अपने वर्तमान स्वर्णिम क्षणों को भी दुःखद बना लेता है।
जब समय था, शान्ति थी. बुद्धि थी तब तो विचार नहीं किया, उस समय तो मद के उन्माद में आँखें बन्द रहीं, लेकिन जब हाथ से अवसर निकल गया तब आँखें भी खुलीं, विवेक भी आया, परन्तु अब कुछ होने का नहीं, अब तो केवल पश्चात्ताप की अग्नि ही अवशिष्ट है, जिसमें जीवन भर जलना पड़ता है।
परन्तु इस पश्चात्ताप से क्या लाभ ? जो कुछ होना था सो हो चुका। क्या लाभ थोड़े से बचे-बचाये को भी मिट्टी में मिलाने से इस आशय की द्योतक ये पंक्तियाँ हैं –
“अब पछिताये होत का, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।”
अंग्रेजी में इसका रूप है-
“It is no use crying over spilt milk”.
काहावत की सार्थकता
“जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, फिर पश्चात्ताप करने से क्या लाभ ?” तात्पर्य यह है कि काल रूपी चिड़िया जीवन के स्वर्णिम क्षण रूपी कणों को खाती रहती है, उस समय तो मनुष्य कुछ विचार नहीं करता, न उसकी रक्षा का कोई प्रयत्न ही करता है।
परन्तु जब कुछ भी पास नहीं रहता, चलने का समय निकट आ जाता है, तब वह चैतन्य होता है और पश्चात्ताप करता है।
जब खेत हरा-भरा था, उस समय ही उसकी रक्षा नहीं की तो फिर बाद में आठ-आठ आँसू बहाने से क्या लाभ ?
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छी प्रकार, सोच-समझकर कार्य करे, जिससे कि उसे अन्त में हाथ न मलना पड़े। गिरधर कवि कहते हैं कि
“बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय |
काम बिगारे आपनौ, जग में होत हँसाय ॥”
संस्कृत की भी एक उक्ति है –
“सहसा विवधीत न क्रियाम् अविवेका परमापदासम् पदम् ॥”
अर्थात् मनुष्य को कोई भी काम बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिये क्योंकि अविवेक हजारों आपत्तियों की जड़ होता है।
पहले कार्य और अकार्य पर उसकी सार्थकता और निरर्थकता पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये, क्योंकि कार्य समाप्त होने पर कुछ नहीं हो सकता, केवल पछतावा मात्र रह जाता है।
“अरविन्द को मार तुषार गया, मुस्कुराते हुए रवि आये तो क्या।”
जब कमल को पाला मार जाये, प्रातःकाल के समय कितनी ही मुस्कुराहट बिखराते हुए सूर्य आये, कोई लाभ नहीं होता।
अपने काम बिगड़ जाने पर रोने-धोने से न कुछ होता है और न पश्चात्ताप की अग्नि में स्वयं को जला डालने से ही कुछ बनता है।
एक स्थल पर तुलसीदास जी ने लिखा है-
“का वरषा जब कृषि सुखाने समय चूकि पुनि का पछिताने।”
पश्चाताप की निरर्थकता
एक बार जब समय चूक गया फिर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये कोई लाभ नहीं सकता। समय की गति पहचानकर तद्नुकूल आचरण करना तथा अपने अभीप्सित कार्य-क्षेत्र में विचारपूर्वक आगे बढ़ना ही सफलता का मन्त्र है।
पश्चात्ताप करना तो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करना है।
हमने पहली गलती तो यह की कि सोचा-समझा नहीं, दूसरी गलती यह करते हैं कि अपने शरीर और मन को पश्चात्ताप की अग्नि में जलाये डालते हैं, थोड़े बचे हुए जीवन के आनन्द को भी जान बूझकर खोये दे रहे हैं।
किसी विद्वान ने कहा है-
“गर्तं न शोचामि कृतम् न मन्ये।”
अर्थात् जो बात हो चुकी उस पर चिन्ता करना, खेद करना, व्यर्थ है। हाँ जब थोड़ा-सा भी समय बाकी था उस समय का थोड़ा-सा भी प्रयास, उस समय की थोड़ी-सी सावधानी हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती थी, परन्तु समय समाप्त हो जाने पर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये, कोई लाभ नहीं।
रहीम ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि समय रहते हुये ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिये। जब तक दूध, दूध है तब तक ही उसको मथकर मक्खन निकालने में बुद्धिमत्ता है, जब बिगड़ जाता है तब आप कितना भी परिश्रम करें, दूध में से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, दूध जाने पर खन निकालने का प्रयास शक्ति का अपव्ययमात्र ही होगा।
रहीम कहते हैं-
“रहिमन बिगरे दूध को, मथे न माखन होय।”
इतिहास साक्षी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को 17 बार हराया, परन्तु इस आक्रान्ता के विषैले दाँत न तोड़े, जिसके परिणामस्वरूप भारत शताब्दियों तक विदेशियों से पदाक्रान्त रहा।
आज भी भारतवासी पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि पर पश्चात्ताप करते हैं, पर क्या लाभ ?
यदि चौहान ने पहले ही सोच समझकर इस समस्या को सुलझा दिया होता तो भारत को इतने दुर्दिन न देखने पड़ते।
इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुये उन्होंने समय की गति को पहचाना ।
जो समय जिस कार्य के लिये उपयुक्त था वह उसी समय किया तभी उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त हुई, इसीलिये आज भी उनका नाम और उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है।
लोहे पर तभी चोट मारनी चाहिये जब वह गरम हो, तभी आप उससे अपने मनोनुकूल वस्तुयें बना सकते हैं।
यदि लोहा ठण्डा पड़ गया तो आप कितना ही पीटिये, उससे आप कोई वस्तु नहीं बना सकते, आपका हथौड़ा और छैनी भले ही टूट जायें।
अंग्रेजी की एक कहावत भी है-
“Strike while the iron is hot.”
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये। प्यास से व्याकुल होने पर जो व्यक्ति कुआँ खोदना प्रारम्भ करता है, वह प्यासा ही मर जाता है।
जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में तो सोता है, मौज उड़ाता है परन्तु बाद में पश्चात्ताप करता है, तो उसका पश्चात्ताप करना व्यर्थ है।
समय पर कार्य न करने वाले और समय पर न बोलने वाले को शंकराचार्य ने मूक और बधिर की उपाधि दी है-
“मूकस्तु को वा बधिरस्तु को वा वक्तुं न शक्तुं समये समर्थः ।”
अर्थात् जो व्यक्ति यथासमय न कार्य कर सकता है, न बोल सकता है, वह बहरा और गूंगा है।
अतः अपने को मनस्ताप और खेद से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि हम समय पर ही सावधान हो जायें अन्यथा केवल हाथ मलना ही हमारे हाथ रह जायेगा और कुछ नहीं।
उपसंहार
इसीलिये परिस्थितियों को पहचानने वाले तथा समय पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का ही सफलता सर्वदा वरण करती है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में अवसर आते हैं और चले जाते हैं।
ये प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई आगे बढ़े और उनका लाभ उठाए सजग व्यक्ति अवसर मिलते ही उसे पकड़ लेते हैं। यही सफलता की कुंजी है।
आपको हमारी आज की यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
पश्चात्ताप की सार्थकता क्या है ?
“जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, फिर पश्चात्ताप करने से क्या लाभ ?” तात्पर्य यह है कि काल रूपी चिड़िया जीवन के स्वर्णिम क्षण रूपी कणों को खाती रहती है, उस समय तो मनुष्य कुछ विचार नहीं करता, न उसकी रक्षा का कोई प्रयत्न ही करता है।
परन्तु जब कुछ भी पास नहीं रहता, चलने का समय निकट आ जाता है, तब वह चैतन्य होता है और पश्चात्ताप करता है।
जब खेत हरा-भरा था, उस समय ही उसकी रक्षा नहीं की तो फिर बाद में आठ-आठ आँसू बहाने से क्या लाभ ?
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छी प्रकार, सोच-समझकर कार्य करे, जिससे कि उसे अन्त में हाथ न मलना पड़े। गिरधर कवि कहते हैं कि
“बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय |
काम बिगारे आपनौ, जग में होत हँसाय ॥”
संस्कृत की भी एक उक्ति है –
“सहसा विवधीत न क्रियाम् अविवेका परमापदासम् पदम् ॥”
अर्थात् मनुष्य को कोई भी काम बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिये क्योंकि अविवेक हजारों आपत्तियों की जड़ होता है।
पहले कार्य और अकार्य पर उसकी सार्थकता और निरर्थकता पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये, क्योंकि कार्य समाप्त होने पर कुछ नहीं हो सकता, केवल पछतावा मात्र रह जाता है।
“अरविन्द को मार तुषार गया, मुस्कुराते हुए रवि आये तो क्या।”
जब कमल को पाला मार जाये, प्रातःकाल के समय कितनी ही मुस्कुराहट बिखराते हुए सूर्य आये, कोई लाभ नहीं होता।
अपने काम बिगड़ जाने पर रोने-धोने से न कुछ होता है और न पश्चात्ताप की अग्नि में स्वयं को जला डालने से ही कुछ बनता है।
एक स्थल पर तुलसीदास जी ने लिखा है-
“का वरषा जब कृषि सुखाने समय चूकि पुनि का पछिताने।”
पश्चात्ताप क्या है ?
सृष्टि में मानव चेतना-युक्त प्राणी है। उसके पास बुद्धि का अक्षय कोष है। बुद्धि का सफल प्रयोग ही मानव को पशु वर्ग से अलग करने वाली सबल रेखा है।
अपने बुद्धि बल के सहारे ही वर्तमान में रहता हुआ मनुष्य, भूत और भविष्य में विचरण करता है। क्या हो चुका है और क्या होगा इस पर शान्तिपूर्वक विचार करता है तथा अपने लिए एक निरापद मार्ग खोज निकालता है।
कभी-कभी ऐसे भी क्षण आते हैं, जब उसे अपने किये हुए कार्य पर पछताना और दुःखी होना पड़ता है। इस दुःख की अग्नि की जलन से वह अपने वर्तमान स्वर्णिम क्षणों को भी दुःखद बना लेता है।
जब समय था, शान्ति थी. बुद्धि थी तब तो विचार नहीं किया, उस समय तो मद के उन्माद में आँखें बन्द रहीं, लेकिन जब हाथ से अवसर निकल गया तब आँखें भी खुलीं, विवेक भी आया, परन्तु अब कुछ होने का नहीं, अब तो केवल पश्चात्ताप की अग्नि ही अवशिष्ट है, जिसमें जीवन भर जलना पड़ता है।
परन्तु इस पश्चात्ताप से क्या लाभ ? जो कुछ होना था सो हो चुका। क्या लाभ थोड़े से बचे-बचाये को भी मिट्टी में मिलाने से इस आशय की द्योतक ये पंक्तियाँ हैं –
“अब पछिताये होत का, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।”
अंग्रेजी में इसका रूप है-
“It is no use crying over spilt milk”.
पश्चात्ताप की निरर्थकता क्या है ?
एक बार जब समय चूक गया फिर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये कोई लाभ नहीं सकता। समय की गति पहचानकर तद्नुकूल आचरण करना तथा अपने अभीप्सित कार्य-क्षेत्र में विचारपूर्वक आगे बढ़ना ही सफलता का मन्त्र है।
पश्चात्ताप करना तो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करना है।
हमने पहली गलती तो यह की कि सोचा-समझा नहीं, दूसरी गलती यह करते हैं कि अपने शरीर और मन को पश्चात्ताप की अग्नि में जलाये डालते हैं, थोड़े बचे हुए जीवन के आनन्द को भी जान बूझकर खोये दे रहे हैं।
किसी विद्वान ने कहा है-
“गर्तं न शोचामि कृतम् न मन्ये।”
अर्थात् जो बात हो चुकी उस पर चिन्ता करना, खेद करना, व्यर्थ है। हाँ जब थोड़ा-सा भी समय बाकी था उस समय का थोड़ा-सा भी प्रयास, उस समय की थोड़ी-सी सावधानी हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती थी, परन्तु समय समाप्त हो जाने पर आप कितना ही पश्चात्ताप कीजिये, कोई लाभ नहीं।
रहीम ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि समय रहते हुये ही मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिये। जब तक दूध, दूध है तब तक ही उसको मथकर मक्खन निकालने में बुद्धिमत्ता है, जब बिगड़ जाता है तब आप कितना भी परिश्रम करें, दूध में से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, दूध जाने पर खन निकालने का प्रयास शक्ति का अपव्ययमात्र ही होगा। रहीम कहते हैं-
“रहिमन बिगरे दूध को, मथे न माखन होय।”
इतिहास साक्षी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी को 17 बार हराया, परन्तु इस आक्रान्ता के विषैले दाँत न तोड़े, जिसके परिणामस्वरूप भारत शताब्दियों तक विदेशियों से पदाक्रान्त रहा।
आज भी भारतवासी पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि पर पश्चात्ताप करते हैं, पर क्या लाभ ?
यदि चौहान ने पहले ही सोच समझकर इस समस्या को सुलझा दिया होता तो भारत को इतने दुर्दिन न देखने पड़ते।
इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुये उन्होंने समय की गति को पहचाना ।
जो समय जिस कार्य के लिये उपयुक्त था वह उसी समय किया तभी उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त हुई, इसीलिये आज भी उनका नाम और उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है।
लोहे पर तभी चोट मारनी चाहिये जब वह गरम हो, तभी आप उससे अपने मनोनुकूल वस्तुयें बना सकते हैं।
यदि लोहा ठण्डा पड़ गया तो आप कितना ही पीटिये, उससे आप कोई वस्तु नहीं बना सकते, आपका हथौड़ा और छैनी भले ही टूट जायें।
अंग्रेजी की एक कहावत भी है-
“Strike while the iron is hot.”
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये। प्यास से व्याकुल होने पर जो व्यक्ति कुआँ खोदना प्रारम्भ करता है, वह प्यासा ही मर जाता है।
जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में तो सोता है, मौज उड़ाता है परन्तु बाद में पश्चात्ताप करता है, तो उसका पश्चात्ताप करना व्यर्थ है। समय पर कार्य न करने वाले और समय पर न बोलने वाले को शंकराचार्य ने मूक और बधिर की उपाधि दी है-
“मूकस्तु को वा बधिरस्तु को वा वक्तुं न शक्तुं समये समर्थः ।”
अर्थात् जो व्यक्ति यथासमय न कार्य कर सकता है, न बोल सकता है, वह बहरा और गूंगा है।
अतः अपने को मनस्ताप और खेद से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि हम समय पर ही सावधान हो जायें अन्यथा केवल हाथ मलना ही हमारे हाथ रह जायेगा और कुछ नहीं।


साहित्य में आदर्शवाद और यथार्थवाद | हिन्दी निबंध |
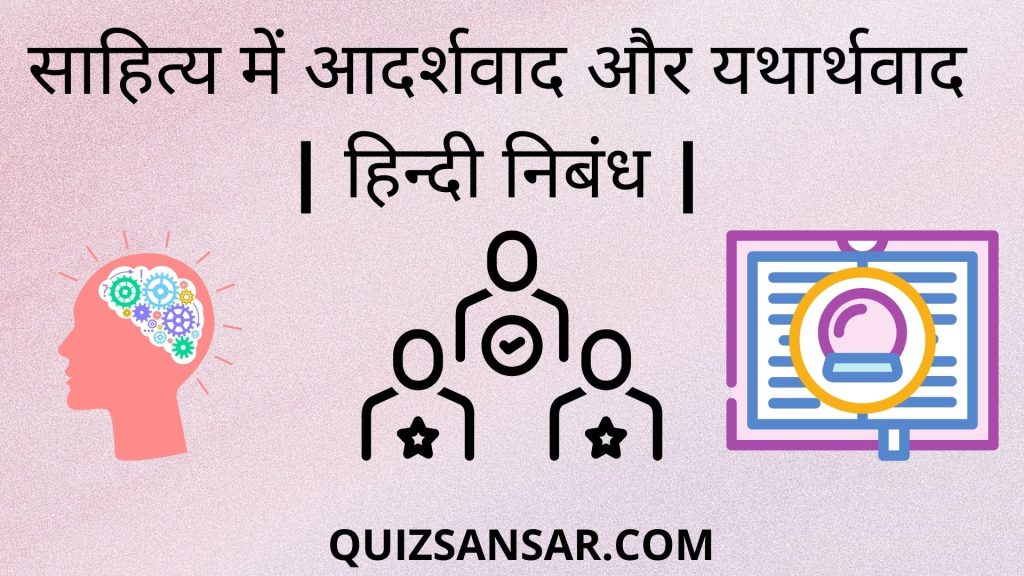
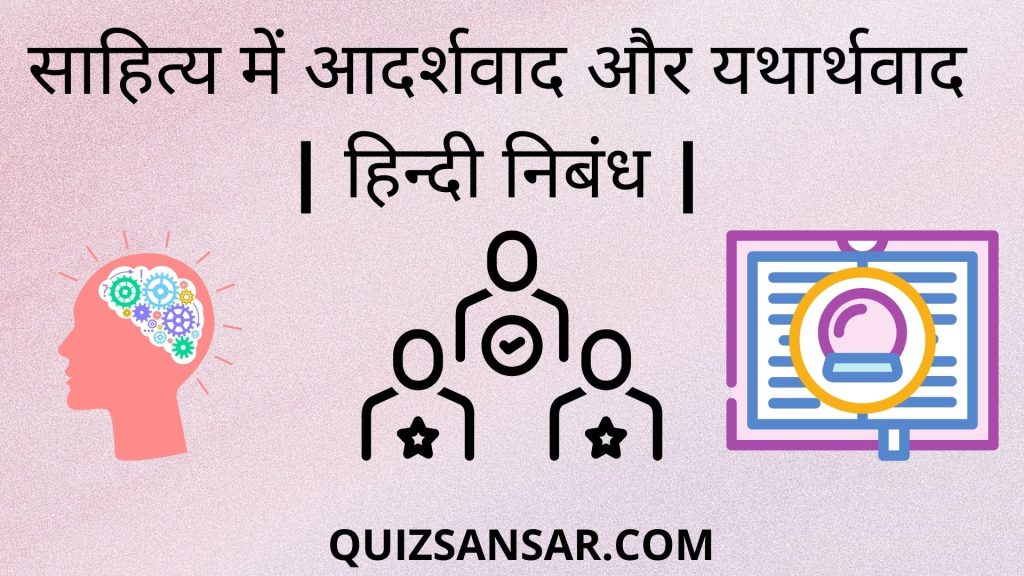
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है साहित्य में आदर्शवाद और यथार्थवाद | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिभाषा
- साहित्य का उद्देश्य
- आदर्शवाद द्वारा उसकी प्राप्ति
- प्राचीन भारतीय साहित्य पूर्णतः आदर्शवादी
- भारतीय साहित्य पर विदेशी प्रभाव
- साहित्यकारों का यथार्थवाद के प्रति आकर्षण
- उपसंहार
प्रस्तावना
समाज की नवचेतना और नवजागरण के साथ साहित्यिक विचारधारा में भी परिवर्तन हुए, दिशायें बदली और विद्वानों ने अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रबल समर्थन किया और वादों की परम्परा चल पड़ी।
किसी ने छायावाद को जन्म दिया, तो किसी ने रहस्यवाद को। किसी ने प्रगतिवाद का समर्थन किया तो किसी ने प्रतीकवाद का किसी ने प्रत्यक्षवाद की प्रशंसा की, तो किसी ने परोक्षवाद की।
इसी प्रकार यथार्थवाद और आदर्शवाद भी साहित्यिक अखाड़े में कूद आये। कुछ दर्शक यथार्थवाद को प्रोत्साहित करने के लिए तालियाँ बजाने लगे और कुछ आदर्शवाद को।
कुछ महानुभवों ने तटस्थता की नीति को अपनाया और दोनों के समन्वय में वाह-वाह करने लगे। आज का युग परीक्षण काल है।
साहित्य रूपी वृक्ष में से नित्य नवीन शाखायें फूट रही हैं, कुछ पल्लवित और कुसुमित हो जाती हैं, कुछ स्वयं सूखकर निष्ठाण हो जाती हैं। और किन्हीं को लोग तोड़कर ले जाते हैं।
यथार्थ और आदर्श की भी साहित्य के बाजार में बहुत कुछ धूम रही है।
आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिभाषा
कुछ विद्वान् इस बात के पक्षधर हैं कि साहित्य आदर्शवादी होना चाहिए। उनका विचार है। कि मानव-जीवन और संसार में जो श्रेष्ठ है और श्रेयस्कर है, उसी को साहित्य में स्थान मिलना चाहिए।
इसी से जन-कल्याण सम्भव है। समाज की कुरीतियों के दिग्दर्शन से उसके दुश्चरित्रों के नग्न-चित्रण से, उसके गर्हित, घृणित एवं निन्दनीय स्वरूपों को सिखाने का एक माध्यम बन जायेगा।
उदाहरणस्वरूप चलचित्रों के सभी चित्र किसी विशेष शिक्षा के आधार पर बनाए जाते हैं, परन्तु दृष्टा उन शिक्षाओं पर ध्यान न देकर चोरी करना, जेब काटना, अश्लील प्रेम में फँसना सरलता से सीख जाते हैं।
अतः यह आवश्यक है कि साहित्य में आदर्श की ही प्रस्तुति की जाये। उधर यथार्थवादियों का विचार है कि मानव जीवन और संसार का वास्तविक स्वरूप भी साहित्य में होना चाहिए।
साहित्यकारों का कर्त्तव्य है कि जैसा देखें वैसा लिखें।
मनुष्य को वास्तविक जगत् से दूर कल्पना के संसार में ले जाकर खड़े कर देने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता।
वह जिस भूमि पर रहता है, उसी के वातावरण में उसका हित और अहित सम्भव है। उसे यदि स्वर्ग का काल्पनिक चित्र दिखाया जाये तो उससे उसकी आत्म-संतुष्टि नहीं हो सकती।
हम जिस संसार में रहते हैं। उसमें सुख भी है और दुःख भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। यहाँ सुगन्धित पुष्पों के साथ काटे भी हैं और मधु के साथ विष भी, यथार्थवादियों का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविकता की ओर से आँख बन्द कर लेने से कल्याण नहीं हो सकता।
हमारे जीवन में सत्य का जितना महत्त्व है, उतना कल्पना या स्वप्नों का नहीं। आदर्शवादी अपनी कल्पना द्वारा संसार की कुरूपता को अपनी बुद्धि से ढककर एक सुन्दर और पवित्र जगत् की रचना करता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है’ के आधार पर साहित्य में समाज का नग्न, कुत्सित और वीभत्स चित्र प्रस्तुत करता है।
साहित्य का उद्देश्य
साहित्य जीवन की व्याख्या है, आलोचना है उसमें जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जीवन निर्वाह के सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं।
साहित्य समाज का मार्ग प्रदर्शन करता है, उसे असत् से हटाकर सत् की ओर लगाता है। इसीलिये हमारे प्राचीन साहित्य में अन्त में पाप और दुराचार की पराजय और उस पर सत्य, न्याय, धर्म आदि सद्गुणों की विजय दिखाई गई है।
“काव्य प्रकाश” में काव्य के लक्षण गिनाते समय काव्य प्रकाशकार ने “शिवेतरक्षतये” को ही प्रतिपादित किया है। अशिव की क्षति साहित्य का पवित्र कर्तव्य है।
अशिव की क्षति करना साहित्यकार का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। अशिव का अर्थ अमंगल या अकल्याण है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य जन-कल्याण करने वाला कहा जा सकता है।
दूसरे लोगों का विचार है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उनके अनुसार साहित्य समाज का वास्तविक और यथार्थ रूप ही हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि इस प्रकार साहित्य से लाभ क्या ?
जो वैद्य केवल मरीज के मर्ज को सामने रख दे क्या उस वैद्य से रोगी का कल्याण हो सकता है? कल्याण तो ऐसे वैद्य से हो सकता है जो उस मर्ज की अच्छी-से-अच्छी औषधि रोगी को दे और रोगी को यह अनुभव न होने दे कि वह इतने भयानक रोग से आक्रांत है।
ठीक यही बात साहित्य के विषय में है। जीवन और समाज के केवल पापमय चित्र को प्रस्तुत करने वाला साहित्य, साहित्य नहीं हो सकता।
साहित्य से तो सत्यम् शिवम्, सुन्दरम् की रक्षा होनी चाहिए। यह निश्चय है कि संसार में उत्तम और अधम सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, पाप और पुण्य भी रहता है।
साहित्य में सभी का थोड़ा-थोड़ा प्रतिनिधित्व सम्भव है, परन्तु लोक कल्याण के लिए नितान्त आवश्यक है कि पाप पर पुण्य की विजय दिखाई जाए।
इससे समाज में धर्मबुद्धि उद्बुद्ध होगी और अधार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य समाज की अधिक क्षति न कर सकेंगे। साहित्य में पूर्ण सत्य की रक्षा होनी चाहिए।
आदर्शवाद द्वारा उसकी प्राप्ति
साहित्य के उद्देश्य की पूर्ति इसी प्रकार के आदर्शवाद से होती है, क्योंकि कोरे आदर्शवाद का भी कोई मूल्य नहीं होता। सौन्दर्य का अस्तित्व कुरूपता पर आधारित है।
यदि संसार में कुरूपता नहीं होती तो सौन्दर्य का न तो इतना महत्व होता और न आकर्षण। इसी प्रकार पुण्य का अस्तित्व पाप पर है, धर्म का अधर्म पर।
साहित्य में लोकोपयोगी आदर्श उच्च कोटि के सिद्धान्त, आत्मोन्नति के साधन तथा लोक कल्याणकारी पीयूष धारा हो, परन्तु उसे अधार्मिक प्रवृत्तियों के द्वन्द्व द्वारा स्पष्ट किया जाये।
लोकोपयोगी साहित्य स्रष्टा इन दो रूपों का अपने साहित्य में विश्लेषण करता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह काव्य में सत्य-पक्ष की ही विजय देखना चाहता है चाहे स्वयं कितना ही दुष्ट हो।
असत् पक्ष के साथ उसकी सहानुभूति नहीं होती। प्राचीन भारतीय कवियों ने सच्चरित्र नायक और नायिकाओं को लेकर अनेक काव्यों और नाटकों की रचनायें कीं।
इन नायक और नायिकाओं के सामने अनेक विघ्न-बाधाएँ आईं किन्तु उन्हें न गिनते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले गए, अन्त में उनकी निश्चित रूप से विजय हुई।
पाठक के हृदय पर इसका प्रभाव यह पड़ता है कि सत्य की असत्य पर विजय होती है।
प्राचीन भारतीय साहित्य पूर्णतः आदर्शवादी
हमारे प्राचीन साहित्यकार पूर्णतः आदर्शवादी थे, समाज में क्या हो रहा है इसकी नग्न विवेचना उनके काव्यों में नहीं होती थी, अपितु यदि ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते थे। वे साहित्य सृजन तो करते थे इस भूमि पर रहकर, परन्तु आदर्श होता था स्वर्गीय।
जिनके पवित्र वचनामृत से अधर्म और पाप में डूबी हुई जनता अपने उद्धार की आशा करती है, उन सत् काव्यों के अध्ययन से मनुष्य का हृदय पवित्र होने लगता है।
तुलसी की रामायण ने आज संसार का कितना उपकार किया यह सर्वविदित है। संसार सागर में डूबने वाले कितने दुराचारियों की इन महाकाव्यों ने रक्षा की ?
विश्रृंखलित समाज को सुसंगठित होने की चेतना दी ? कितने मार्ग भ्रष्टों का पथ-प्रदर्शन किया ? क्या आज के यथार्थवादी नाटक और उपन्यासों में यह क्षमता है?
रामायण में भी सत् और असत् दोनों में द्वन्द्व दिखाकर पुण्य की पाप पर विजय उद्घोषित की गई है। इस प्रकार हमारा प्राचीन साहित्य आदर्शवाद की शिला पर आधारित है।
उस अमृत के समुद्र में आज तक जिसने भी स्नान किया उसने स्वर्गीय देवत्व प्राप्त किया, यह नि.सन्देह सत्य है।
अतः आदर्शवादी साहित्य स्रष्टा की दृष्टि में सदैव कल्याण होता है। वह जगत् का वीभत्स नग्न चित्रण करके समाज में आग लगाना नहीं चाहता। मैथिलीशरण गुप्त ने आदर्शवाद के समर्थन में एक स्थान पर लिखा—
हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा।
किन्तु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ ।
भारतीय साहित्य पर विदेशी प्रभाव
भारतीय नकल करने में प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति और वेशभूषा की नकल करने में उन्होंने अपने को सौभाग्यशाली समझा, उन्होंने उनके साहित्य का भी अनुकरण किया।
लन्दन की सामाजिक समस्याओं, प्रेम-लीलाओं, गर्भपात आदि का नग्न चित्र आज बाजारों में मिलता है।
भारतीय नवयुवक उन्हें पढ़कर आनन्द लेते हैं और अपने चरित्र को दूषित बनाते हैं। हमारे साहित्यकार भी पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से प्रभावित हैं।
आज जितने उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही हैं, सभी यथार्थवादी हैं, समाज के प्रेमी और प्रेमिकाओं का सर्वांग नग्न चित्र उपस्थित करके लेखनी को सफल मान रहे हैं। इनसे समाज का पतन हो रहा है उत्थान नहीं।
राजनैतिक विषयों में यथार्थवाद अवश्य लाभ करता है। ऐसे विषयों में ‘यथार्थवादी साहित्य’ की क्रान्ति की भूमिका होती है।
जब कोई देश या समाज दीर्घकाल से अन्याय और अत्याचारों से प्रस्त रहता है, तब कुछ प्रतिभाशाली यथार्थवादी लेखक अपनी ओजस्विनी लेखनी से उन दोषों की ओर संकेत करके जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।
शनैः शनैः उन बुराइयों के विरुद्ध लोकमत संगठित होता है। अन्त में जनता उन दोषों को एकदम समाप्त करने के लिए देश में क्रान्ति उपस्थित कर देती है।
देशभक्त अपने प्राणों तक का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रांस और रूस की क्रान्तियाँ इसी यथार्थवाद का परिणाम थीं।
परन्तु आजकल नकलची भारत में यथार्थवाद के नाम पर ऐसा कुत्सित साहित्य लिखा जा रहा है जिसको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारे संसार में अच्छाई और नैतिकता का नाम तक नहीं रहा है। यह एक पक्षीय यथार्थवाद सर्वथा पतन की ओर ले जाना वाला है।
साहित्यकारों का यथार्थवाद के प्रति आकर्षण
तात्पर्य यह है कि जीवन को शक्ति की प्रेरणा देने वाला साहित्य ही ‘सत्यम्’, ‘शिवम्’, ‘सुन्दरम्’ बन सकता है और लोक-कल्याण कर सकता है।
यह तभी होगा जब हमारा साहित्य आदर्शोन्मुख होगा। यथार्थवादी साहित्य में अपना स्थान रखें, परन्तु एकांगी बनकर नहीं।
उन्हें अपने साथ आदर्शवाद भी रखना होगा अन्यथा यह केवल हास्यास्पद बनकर रह जायेगा। प्रेमचन्द जैसा यथार्थवादी ही संसार में आदर प्राप्त कर सकता है।
वे भी कोरे यथार्थवादी नहीं थे, वे थे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अतः दोनों के सम्मिश्रण में ही समाज का कल्याण है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
आदर्शवाद और यथार्थवाद की परिभाषा क्या है ?
कुछ विद्वान् इस बात के पक्षधर हैं कि साहित्य आदर्शवादी होना चाहिए। उनका विचार है। कि मानव-जीवन और संसार में जो श्रेष्ठ है और श्रेयस्कर है, उसी को साहित्य में स्थान मिलना चाहिए।
इसी से जन-कल्याण सम्भव है। समाज की कुरीतियों के दिग्दर्शन से उसके दुश्चरित्रों के नग्न-चित्रण से, उसके गर्हित, घृणित एवं निन्दनीय स्वरूपों को सिखाने का एक माध्यम बन जायेगा।
उदाहरणस्वरूप चलचित्रों के सभी चित्र किसी विशेष शिक्षा के आधार पर बनाए जाते हैं, परन्तु दृष्टा उन शिक्षाओं पर ध्यान न देकर चोरी करना, जेब काटना, अश्लील प्रेम में फँसना सरलता से सीख जाते हैं।
अतः यह आवश्यक है कि साहित्य में आदर्श की ही प्रस्तुति की जाये। उधर यथार्थवादियों का विचार है कि मानव जीवन और संसार का वास्तविक स्वरूप भी साहित्य में होना चाहिए।
साहित्यकारों का कर्त्तव्य है कि जैसा देखें वैसा लिखें।
मनुष्य को वास्तविक जगत् से दूर कल्पना के संसार में ले जाकर खड़े कर देने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता।
वह जिस भूमि पर रहता है, उसी के वातावरण में उसका हित और अहित सम्भव है। उसे यदि स्वर्ग का काल्पनिक चित्र दिखाया जाये तो उससे उसकी आत्म-संतुष्टि नहीं हो सकती।
हम जिस संसार में रहते हैं। उसमें सुख भी है और दुःख भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। यहाँ सुगन्धित पुष्पों के साथ काटे भी हैं और मधु के साथ विष भी, यथार्थवादियों का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविकता की ओर से आँख बन्द कर लेने से कल्याण नहीं हो सकता।
हमारे जीवन में सत्य का जितना महत्त्व है, उतना कल्पना या स्वप्नों का नहीं। आदर्शवादी अपनी कल्पना द्वारा संसार की कुरूपता को अपनी बुद्धि से ढककर एक सुन्दर और पवित्र जगत् की रचना करता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है’ के आधार पर साहित्य में समाज का नग्न, कुत्सित और वीभत्स चित्र प्रस्तुत करता है।
भारतीय साहित्य पर विदेशी प्रभाव कैसे पड़ा ?
भारतीय नकल करने में प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति और वेशभूषा की नकल करने में उन्होंने अपने को सौभाग्यशाली समझा, उन्होंने उनके साहित्य का भी अनुकरण किया।
लन्दन की सामाजिक समस्याओं, प्रेम-लीलाओं, गर्भपात आदि का नग्न चित्र आज बाजारों में मिलता है।
भारतीय नवयुवक उन्हें पढ़कर आनन्द लेते हैं और अपने चरित्र को दूषित बनाते हैं। हमारे साहित्यकार भी पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से प्रभावित हैं।
आज जितने उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही हैं, सभी यथार्थवादी हैं, समाज के प्रेमी और प्रेमिकाओं का सर्वांग नग्न चित्र उपस्थित करके लेखनी को सफल मान रहे हैं। इनसे समाज का पतन हो रहा है उत्थान नहीं।
राजनैतिक विषयों में यथार्थवाद अवश्य लाभ करता है। ऐसे विषयों में ‘यथार्थवादी साहित्य’ की क्रान्ति की भूमिका होती है।
जब कोई देश या समाज दीर्घकाल से अन्याय और अत्याचारों से प्रस्त रहता है, तब कुछ प्रतिभाशाली यथार्थवादी लेखक अपनी ओजस्विनी लेखनी से उन दोषों की ओर संकेत करके जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।
शनैः शनैः उन बुराइयों के विरुद्ध लोकमत संगठित होता है। अन्त में जनता उन दोषों को एकदम समाप्त करने के लिए देश में क्रान्ति उपस्थित कर देती है।
देशभक्त अपने प्राणों तक का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रांस और रूस की क्रान्तियाँ इसी यथार्थवाद का परिणाम थीं।
परन्तु आजकल नकलची भारत में यथार्थवाद के नाम पर ऐसा कुत्सित साहित्य लिखा जा रहा है जिसको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारे संसार में अच्छाई और नैतिकता का नाम तक नहीं रहा है। यह एक पक्षीय यथार्थवाद सर्वथा पतन की ओर ले जाना वाला है।


सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- सूरदास जी के काव्य की विशेषता
- काव्य में बाल-वर्णन का कारण
- बाल वर्णन के विभिन्न रूप
- उपसंहार
सूरदास जी के काव्य की विशेषता
महाकवि सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का नाभादास जी ने अपने भक्तिमाल नामक ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख किया है—
उक्ति ओज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी।
बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक भारी ।।
प्रतिबिम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी ।
जनम करम गुण रूप राग रसना परकासी ॥
विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्रवननि करै ।
सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिरचालन करै ।।
इस पद्य में सूरदास की काव्य सम्बन्धी सभी विशेषतायें आ जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में श्रीकृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णन किया।
बज की वीथिकाओं में श्रीकृष्ण की बाल सुलभ क्रीडायें, कालिन्दी के कछारों में ग्वाल-बालों के साथ कृष्ण का मनोहर चांचल्य, हरे-भरे सघन कुंजों में बृजबालाओं के साथ प्रेमलीला, श्रीकृष्ण का मथुरा वात्सल्य रस के सिद्ध कवि सूरदास गमन तथा उनके वियोग में विहल बज-वनिताओं के मनोभावों के मार्मिक चित्रण तक ही सूर की दृष्टि उलझ कर रह गई।
तुलसी की भाँति सूरदास ने यद्यपि कृष्ण सम्पूर्ण जीवन का चित्र उपस्थित नहीं किया, फिर भी सूर ने जिस अंग का वर्णन किया, वह आज तक अद्वितीय है ।
सूर ने अपने काव्य में शृंगार और वात्सल्य के इन दो रसों को ही प्रधानता दी। शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के निरूपण में सूरदास ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की।
व्रज वनिताओं के साथ श्रीकृष्ण के प्रेम व्यवहार को कवि स्वयं अपने हृदय की आँखों से देखकर आनन्द विभोर होकर गा उठता है और इस प्रकार वे संयोग विरह के अनेक चित्र प्रस्तुत करने लगते हैं।
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में गोपियों के विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाओं का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।
इसी प्रकार वात्सल्य वर्णन में तो सूरदास नितान्त अद्वितीय हैं, आज तक कोई भी कवि इनकी समता में नहीं ठहरता।
आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में
“वे इस क्षेत्र का कोना-कोना झाँक आये हैं।”
सूरदास की प्रशंसा करते हुए श्रीवियोगिहरि ने लिखा है,
“सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया है, तो वात्सल्य ने को अपना एकमात्र आश्रय स्थान माना है।“
इस क्षेत्र में हिन्दी साहित्य का कोई भी कवि सूरदास को समता नहीं कर सकता।
काव्य में बाल-वर्णन का कारण
सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। शिष्य होने से पूर्व ये दास्य भाव के पद लिखा करते थे।
वल्लभाचार्य जी ने स्वयं कहा, “ऐसो घिघियात का को है, कछु भगवत् लीला को वर्णन कर।” उनके ही आदेश से सूरदास ने श्रीमद्भावगत् की कथाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया।
वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और कृष्ण के प्रति सखा भाव की भक्ति का प्रचार किया। वल्लभ सम्प्रदाय में बालकृष्ण की उपासना को ही प्रधानता दी जाती थी।
इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और शृंगार इन दोनों रसों का ही वर्णन अभीष्ट था, यद्यपि कृष्ण के कंसहारी और द्वारिकावासी रूप भी हैं, परन्तु जिस सम्प्रदाय में सूर दीक्षित थे, उनमें बालकृष्ण की महिमा थी। सूर ने वात्सल्य वर्णन बड़े विस्तार से किया।
इस वर्णन में न उन्होंने कहीं संकोच किया और न झिझके । बालक और युवक कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने बड़े ब्यौरों के साथ प्रस्तुतः किया। घोर से घोर शृंगार की बात करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया।
बाल वर्णन के विभिन्न रूप
कृष्ण जन्म की आनन्द बधाइयों के पश्चात् बाल लीलाओं का आरम्भ होता है। सूरदास ने शैशवावस्था से लेकर कौमार्यावस्था तक के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। उन चित्रों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है-
- रूप वर्णन
- चेष्टाओं का वर्णन
- क्रीड़ाओं का वर्णन
- अंतर्भावों का वर्णन
- संस्कारों, उत्सवों और समारोहों का वर्णन
रूप वर्णन
रूप-वर्णन में सूरदास ने कृष्ण के सौन्दर्य को अनेक उद्भावनायें की हैं। बज-बालायें कृष्ण के बाल-सौन्दर्य पर तन-मन-धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, पर कृष्ण का सामीप्य छोड़ना उन्हें रुचिकर नहीं –
हौं बलि जाऊं छवीले लाल की।
छिटक रही वह दिसि जो लटुरियाँ, लटकता लटकनि भाल की।
मोतिन सहित नासिका नथनी, कण्ठ, कमल दल माल की।
सूरदास प्रभु प्रेम मगन भई, ढिंग न तजहिं ब्रज बाल की ।।
चेष्टाओं का वर्णन
कृष्ण पालने में सोए हैं। यशोदा पालने को हिलाकर और लोरी गाकर कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं परन्तु कृष्ण भी कम चालाक नहीं हैं, जब तक पालना हिलता रहता है और यशोदा के मधुर गान की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रहती है तब तक मुँह बनाए आँखें बन्द किये पड़े रहते हैं, जैसे ही यशोदा मौन हो जाती है, कृष्ण आँख खोलकर देखने लगते हैं।
सूरदास ने कितना स्वाभाविक चित्रण किया है-
यशोदा हरि पालने झुलावै ।
हलरावै दुलरावै, मल्हावै जोई सोई कुछ गावै ॥
मेरे लाल को आउ निदरिया, काहे न आनि सुआवै।
कबहुँ पलक हरि मूँद लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावै ॥
सोवत जानि मान है रहि, करि करि सैन बतावै ॥
कृष्ण चलना सीख रहे हैं। देहरी लाँघने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर लाँध नहीं पाते, बार-बार गिर पड़ते हैं। यशोदा इस कार्य-कलाप को देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है।
यशोदा श्रीकृष्ण को नितान्त असमर्थ पाकर उनका हाथ पकड़कर लाँघना सिखाती हैं।
चलत देखि जसुमति सुख पावै ।
ठुमिक-दुमिक धरती पर रेंगत जननि देखि दिखावै ।
देहरि लो चलि जात बहुरि, फिरि फिरि इतही को आवै ।।
गिरि गिरि परत बनत नहि लाँघत, सुर मुनि सोच करावै।
तब जसुमति कर टेक स्याम को, क्रम-क्रम सों उतरावै ।।
बालक की अबोधता और भोलापन सूरदास की दृष्टि से कभी नहीं बचा। अपने प्रतिविम्ब को पकड़ने का कृष्ण का प्रयास कितना स्वाभाविक है-
मनिमय कनक नन्द के आँगन, बिम्ब पकिरबे धावत।
कबहुँ निरखि हरि आए छाँह को, कर सौ पकरन चाहत ।।
अपने बच्चे का बाल विनोद देखकर माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती प्रेम के आवे में कृष्ण का भोलापन दिखाने के लिये वह दौड़ी हुई सन्द को बुलाने जाती हैं।
बाल दसा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नन्द बुलावति ।
अंचला तर लै ढांकि सूर के प्रभु को दूध पियावति ॥
सूर के बाल वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण के साथ-साथ मातृ हृदय के सुन्दर चित्र भी खींचे हैं—
सुत मुख देखि जसोदा भूली।
हर्षित देखि दूध की दंतियों, प्रेम मगन तन की सुधि भूली।
बाहरि तै तब नन्द बुलाए देखो मुख सुन्दर सुखदाई ।।
पुत्र वियोग से संतप्त यशोदा देवकी को संदेश देती है। मातृत्व की इस सुन्दर भाषा को देखिये-
सन्देसो देवकी सौं कहियो ।
हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करति ही रहियो ।
जदपि टेब तुम जानत ही हो, तऊ मोही कहि आवै।
प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भाव ॥
सृष्टि के आरम्भ से आज तक माताओं को अपने बच्चों के विषय में प्रायः शिकायत करते सुना है कि “हमारा, तो मिट्टी बहुत खाता है।“ सूर ने इस शिकायत से यशोदा को भी नहीं छोड़ा, परन्तु एक विशेषता के साथ वह यह कि कृष्ण ने मुख में समस्त ब्रह्माण्ड के दर्शन करा दिये।
मोहन काहे न उगिलो माँटी।।
बार-बार अनरूचि उपजावति, महरि हाथ लिए साँटी ।।
माँ के बहुतेरा कहने पर भी बालक कहाँ मानकर देता है, ऊपर से दाँत और भींच लेता है। अगर माँ जबरदस्ती मुँह में उंगली डाल दे तो वह बिना काटे हुए बाहर नहीं निकलती। यशोदा ने भी छी, छी, थू, थू, बहुतेरा कहा पर कृष्ण ने एक न मानी-
महतारी को कह्यो न मानत, कपट चतुराई डाटी।
बदन पसारि दिखाइ आपने, नाटक की परिपाटी ।
सूर स्वभाव-चित्रण द्वारा रसोद्रेक में अद्वितीय हैं।
उन्होंने अपने काव्य में पग-पग पर अन्तर्भावों का चित्रण किया है। बालक के हृदय में अपने साथियों को देखकर कभी-कभी स्पर्धा भी उत्पन्न हो जाती है। बलदाऊ की चोटी लम्बी भी है और मोटी भी, परन्तु कृष्ण की चोटी प्रयास करने पर भी छोटी है, उसका उन्हें दुःख है। वो एकदम माँ से शिकायत कर बैठते हैं
मैया कर्बाहिँ बढ़ेगी चोटी।
किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहुँ है छोटी।
तू तो कहति बल की बेनी ज्यों है है लॉबी मोटी ॥
क्रीड़ाओं का वर्णन
क्रीड़ा वर्णन में सूरदास मानो सिद्धहस्त हैं।
एक दिन साथियों में क्षोभ बढ़ा क्योंकि कृष्ण ने दाव देने से मना कर दिया था, परन्तु बाल्यावस्था में साम्यवाद की प्रधानता रहती है।
वहाँ न कोई बड़ा है और न छोटा, न कोई धनी है और न मानी। सूर ने कितना स्वभावोक्ति पूर्ण चित्रण किया है-
खेलत में को काको गुसइयाँ ।
हरि हारे, जीते श्रीदामा बरबस की कल करत रिसैयाँ।
जाति पाँति हमसे बढ़ नाहि, नाहिन बसत तुम्हारी छैयाँ।
अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥
बात आज-की सी लगती है क्योंकि छोटे बच्चे को चिढ़ाने के लिए खासकर लड़कियों को घर वाले कह देते हैं कि तुझे हमने कंजरियों से दो रोटी में खरीदा था।
यही घटना कृष्ण के साथ भी सूरदास जी ने घटवा दी। जब क्रोध की सीमा न रही, तो आपने खेलने जाना भी बन्द का दिया।
माँ का हृदय इस बात पर द्रवित हो गया, वह रो उठी, गोवर्धन की शपथ खाई कि वास्तव में कृष्ण तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ।
मैया मोही दाऊ बहुत खिजायौ ।
मोसों कहत मोल को लीन्ही, तेहि जसुमति कब जायो ।
कहा कहाँ एहि रिस के मारे खेलत ही नहीं जात |
पुनि पुनि कहत कौन है माता, को, है तुमरो तात ॥
सुर स्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत।
अंतर्भावों का वर्णन
सूर के कृष्ण आयु में अवश्य छोटे हैं, परन्तु तर्क और प्रत्युत्पन्न मतित्व में वे बहुत बड़े हैं। बड़ों-बड़ों को चकमा दे सकते हैं। यह स्वाभाविक चित्र सूर ने गोचारण और माखन चोरी प्रसंग में प्रस्तुत किए हैं—
मैया मैं नहि माखन खायो |
ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो ।
देखि तुही छीके पर भाजन, ऊँचे घर लटकायो ।
तुही निरखि नान्हें कर अपने, मैं कैसे धरि पायो ।
कृष्ण की उद्दण्डता जब गोपियों को असह्य होने लगी, तो कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले आई और साफ-साफ कह दिया-
जब हरि आवत तेरे आगे, संकुचि तनक जात ।
कौन-कौन गुन कहुँ स्याम के नेक न काहु डरांत ।।
अवस्था के साथ-साथ हृदय के परिचय की भावना बढ़ी।अब तक ग्वालों तक ही परिचय सीमित था।
एक दिन सहसा राधा को रास्ते में अकेली पाकर कृष्ण पूछ बैठे, “गौरी! तुम कौन हो ? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा।” राधा ने, वह कृष्ण से यद्यपि छोटी थी, परन्तु कृष्ण को मुँह मोड़ उत्तर दिया कि शर्मदार के लिए मरना था, पर सूर के कृष्ण ने उस व्यंग्य का ऐसा उत्तर दिया कि राधा को जन्म-जन्मान्तर के लिये निरुत्तर होना पड़ा
बूझत स्याम कौन तू गोरी ।
कहाँ रहति, काकी हो बेटी, देखी नहीं कबहुं ब्रज खोरी ॥
काहे को हम ब्रज तन आवत खेलत रहत आपनी पौरी।
सुनत रहत खवननि नन्द ढोटा, करत रहत माखन दधि चोरी ॥
तुम्हरो कहा चोरि हम लहैं, खेलन चलौ हमारी पौरी।
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, बातन भुरइ राधिका भोरी ।।
संस्कारों, उत्सवों और समारोहों का वर्णन
इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, कालिया दमन आदि प्रसंगों में भी सूर के बाल वर्णन के दर्शन होते हैं। सूर का बाल वर्णन भक्ति और अध्यात्म का समन्वय है।
अनेक अलौकिक कार्य करते हुए भी कृष्ण यशोदा के लिए साधारण बालक की भाँति ही बने रहते हैं, भगवान नहीं।
इसका कारण यशोदा का पुत्र के प्रति अनन्य प्रेम और तन्मयता थी। इसलिए यशोदा, राधा और गोपियों के कृष्ण के साथ प्रेम सम्बन्ध पर विश्वास नहीं करती थीं, उपेक्षा भरी दृष्टि से केवल देखकर ही रह जाती हैं।
उपसंहार
सूर की अन्तर्भेदिनी दृष्टि कृष्ण की बाल्यावस्था के एक-एक क्षण पर हीपड़ती है। बाल्य जीवन की कोई वृत्ति इस महाकवि की विराट प्रतिभा के स्पर्श से अछूती नहीं रही। वास्तव में सूर का बाल वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का सुन्दर अध्ययन है।
सूर के वात्सल्य वर्णन पर डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है,
“यशोदा के वात्सल्य में सब कुछ है, जो माता शब्द को इतना महिमामय बनाये हुये है। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ-हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है, जिसे कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम-पोषक हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणाविगलित हृदय को छूने में भी समर्थ हुए हैं “
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
सूरदास जी के काव्य की विशेषता क्या है ?
महाकवि सूर की काव्यगत विशेषताओं का नाभादास जी ने अपने भक्तिमाल नामक ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख किया है—
उक्ति ओज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी।
बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक भारी ।।
प्रतिबिम्बित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी ।
जनम करम गुण रूप राग रसना परकासी ॥
विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्रवननि करै ।
सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिरचालन करै ।।
इस पद्य में सूर की काव्य सम्बन्धी सभी विशेषतायें आ जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में श्रीकृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णन किया।
बज की वीथिकाओं में श्रीकृष्ण की बाल सुलभ क्रीडायें, कालिन्दी के कछारों में ग्वाल-बालों के साथ कृष्ण का मनोहर चांचल्य, हरे-भरे सघन कुंजों में बृजबालाओं के साथ प्रेमलीला, श्रीकृष्ण का मथुरा वात्सल्य रस के सिद्ध कवि सूरदास गमन तथा उनके वियोग में विहल बज-वनिताओं के मनोभावों के मार्मिक चित्रण तक ही सूर की दृष्टि उलझ कर रह गई।
तुलसी की भाँति सूर ने यद्यपि कृष्ण सम्पूर्ण जीवन का चित्र उपस्थित नहीं किया, फिर भी सूर ने जिस अंग का वर्णन किया, वह आज तक अद्वितीय है ।
सूर ने अपने काव्य में शृंगार और वात्सल्य के इन दो रसों को ही प्रधानता दी। शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के निरूपण में सूर ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की।
व्रज वनिताओं के साथ श्रीकृष्ण के प्रेम व्यवहार को कवि स्वयं अपने हृदय की आँखों से देखकर आनन्द विभोर होकर गा उठता है और इस प्रकार वे संयोग विरह के अनेक चित्र प्रस्तुत करने लगते हैं।
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में गोपियों के विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाओं का जैसा वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।
इसी प्रकार वात्सल्य वर्णन में तो सूर नितान्त अद्वितीय हैं, आज तक कोई भी कवि इनकी समता में नहीं ठहरता।
आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि में
“वे इस क्षेत्र का कोना-कोना झाँक आये हैं।”
सूर की प्रशंसा करते हुए श्रीवियोगिहरि ने लिखा है,
“सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया है, तो वात्सल्य ने को अपना एकमात्र आश्रय स्थान माना है।“
इस क्षेत्र में हिन्दी साहित्य का कोई भी कवि सूर को समता नहीं कर सकता।
सूरदास जी के काव्यों में बाल-वर्णन का कारण क्या था ?
सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। शिष्य होने से पूर्व ये दास्य भाव के पद लिखा करते थे।
वल्लभाचार्य जी ने स्वयं कहा, “ऐसो घिघियात का को है, कछु भगवत् लीला को वर्णन कर।” उनके ही आदेश से सूरदास ने श्रीमद्भावगत् की कथाओं को गेय पदों में प्रस्तुत किया।
वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और कृष्ण के प्रति सखा भाव की भक्ति का प्रचार किया। वल्लभ सम्प्रदाय में बालकृष्ण की उपासना को ही प्रधानता दी जाती थी।
इसीलिए सूर को वात्सल्य और शृंगार इन दोनों रसों का ही वर्णन अभीष्ट था, यद्यपि कृष्ण के कंसहारी और द्वारिकावासी रूप भी हैं, परन्तु जिस सम्प्रदाय में सूर दीक्षित थे, उनमें बालकृष्ण की महिमा थी। सूर ने वात्सल्य वर्णन बड़े विस्तार से किया।
इस वर्णन में न उन्होंने कहीं संकोच किया और न झिझके । बालक और युवक कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने बड़े ब्यौरों के साथ प्रस्तुतः किया। घोर से घोर शृंगार की बात करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया।


” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है “हिन्दी-साहित्य के इतिहास” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- वीरगाथा काल
- भक्तिकाल
- रीतिकाल
- आधुनिक काल
- उपसंहार
प्रस्तावना
वर्तमान तो सदैव मानव के नेत्रों के समक्ष रहता ही है, साथ ही साथ वह भविष्य की भी कल्पना करता रहता है, परन्तु जब उसे अतीत की और “हिन्दी साहित्य के इतिहास” झाँकना पड़ता है, तब उसे एक विशेष आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। उसी आश्रय का नाम इतिहास है।
किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति या किसी भाषा के अतीत के उत्थान-पतन को यदि हम जानना चाहते हैं, तो हमें इतिहास की शरण में जाना पड़ता है।
प्राचीन तथ्यों संचित कोष इतिहास कहा जाता है, इसलिए संस्कृत में “इतिहासो पुरावृत्तः” कहकर इतिहास की व्याख्या की गई है।
जब हम हिन्दी साहित्य के अतीत पर दृष्टि डालते हैं, तब हमें विभिन्न भावनाओं और परम्पराओं के दर्शन होते हैं।
इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है—
- सम्वत् 1050 से1375 तक (वीरगाथा काल)
- सम्वत् 1375 से1700 तक (भक्तिकाल)
- सम्वत् 1700 से 1900 तक (रीतिकाल)
- सम्वत् 1900 से अब तक (आधुनिक काल)
आदिकाल (वीरगाथा काल)
हिन्दी साहित्य का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारतवर्ष पर उत्तर-पश्चिम की ओर से निरन्तर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे।
राजा और राजाश्रित कवि छोटे-छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझ बैठे थे। राजपूत राजाओं को अपने व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का अधिक ध्यान था, देश का कम।
राज्य एवं प्रभाव वृद्धि की आकांक्षा से ये लोग परस्पर युद्ध करते थे। कभी-कभी उनका उद्देश्य केवल शौर्य प्रदर्शन मात्र होता था या किसी सुन्दरी का अपहरण राजपूतों में शक्ति, पराक्रम एवं साहस की कमी न थी, परन्तु यह समस्त शौर्य और कोष पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताओं में समाप्त किया जा रहा था।
अतः राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने एक सूत्रबद्ध सामूहिक में शक्ति का परिचय न दे सके। मुहम्मद गौरी के भयानक आक्रमणों ने राजपूत राजाओं को जर्जर कर दिया।
सारांश यह है कि वह युग युद्ध का युग था। उस समय के साहित्यकार चारण या भाट थे, जो अपने आश्रयदाता राजा के पराक्रम, विजय और शत्रु-कन्याहरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे अथवा युद्ध-भूमि में वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरकर सम्मान प्राप्त करते थे।
साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप और प्रतिच्छाया होता है, इस नियम के अनुसार तत्कालीन साहित्य में वीरता की भावना आना अवश्यम्भावी था। इस काल में दो प्रकार के अपभ्रंश तथा देश भाषा काव्यों का निर्माण हुआ।
जैनाचार्य हेमचन्द, सौमप्रभसूरि, जैनाचार्य मेरुतुङ्ग, विद्याधर तथा शार्गंधर, आदि कवि अपभ्रंश काव्य के प्रमुख निर्माता थे। देश भाषा में वीरगाथा काव्य दो रूपों में मिलता है प्रबन्ध काव्य के साहित्यिक रूप में तथा वीर गीतों के रूप में। ये मन्थ रासो कहे जाते थे।
कुछ विद्वान रासो का सम्बन्ध “रहस्य” से मानते हैं और कुछ रास (आनन्द) से मानते हैं। देश भाषा काव्य में प्रमुख आठ पुस्तकें आती हैं-खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचन्द्रप्रकाश, जयमकरसचन्द्रिका परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति पदावली। इस काल में चन्द्रवरदायी भट्ट प्रतिनिधि एवम् प्रमुख कवि थे, जिन्होंने ‘पृथ्वीराज रासो’ नामक हिन्दी के प्रथम महाकाव्य का निर्माण किया।
इस ग्रन्थ में ढाई हजार पृष्ठ तथा 49 समय (सर्ग) हैं। इसमें कवित दूहा, तीमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, सभी छन्दों का व्यवहार किया गया है। यह प्रबन्ध काव्य उस काल का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जाता है, इसमें वीर-भावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति है, कल्पना को उड़ान तथा उक्तियों की चमत्कारिता का सामंजस्य है।
वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषतायें
- इस युग के साहित्यकार साहित्य-सृजन के साथ-साथ तलवार चलाने में भी दक्ष थे।
- साहित्य का एकांगी विकास हुआ।
- वीर काव्यों की प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों रूपों में रचनायें
- काव्यों में वीर रस के साथ शृंगार का पुट भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
- कल्पना की प्रचुरता एवं अतिशयोक्ति का आधिक्य है।
- काव्य का विषय युद्ध और प्रेम ।
- युद्ध का सजीव वर्णन।
- इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा काव्य की मात्रा का आधिक्य है।
- आश्रयदाताओं की भरपेट प्रशंसा।
- केवल वीर काव्य था, राष्ट्रीय काव्य नहीं।
- साहित्यकारों में वैयक्तिक भावना की प्रधानता तथा राष्ट्रीयता की भावना का अभाव।
भक्तिकाल
राजपूतों में जब तक शक्ति थी, साहस था, तब तक वीर गाथाओं से काम चलता रहा, परन्तु शक्ति के समाप्त हो जाने पर उत्साह प्रदान करने से भी कोई काम नहीं चलता।
भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण में अपेक्षाकृत कुछ शान्ति उपस्थित हुई। लोगों को दम लेने की फुरसत मिली। युद्ध से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थक चुके थे।
दोनों जातियों के हृदय में परस्पर मिलन को प्रवृत्ति जागृत हो रही थी। समय की विभिन्न गतियों से पूर्ण परिचित भक्ति काव्य जनता के अशान्त हृदय को सांत्वना और धैर्य देने के लिए उनकी भक्ति भावना को जगाने लगे।
शनैः शनैः भक्ति का प्रवाह इतना विस्तृत हो गया कि उसके प्रवाह में केवल हिन्दू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमान भी आ मिले।
कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐक्य की बलिवेदी पर अपने आराध्य के प्रति अनन्य भावना का बलिदान नहीं करना चाहते थे। अपने धार्मिक व्यक्तित्व को पृथक् रखकर मृतप्रायः हिन्दू जाति में नव-जीवन एवं नव स्फूर्ति संचार करना ही उनका अभीष्ट था।
इस प्रकार, देश में निर्गुण और सगुण नाम के भक्ति काव्य की दो धाराएँ विक्रम की १५वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी के अन्त तक समानान्तर चलती रहीं।
निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई— ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेममार्गी शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि ‘सन्त कवि’ कहलाये और प्रेममार्गी शाखा के ‘सूफी’। निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर प्रधान कवि थे तथा प्रेममार्गी शाखा के मलिक मुहम्मद जायसी।
इसी प्रकार सगुण धारा भी रामोपासना तथा कृष्णोपासना के भेद से दो शाखाओं में विभाजित हो गयी। राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास थे।
निर्गुणधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा
ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों एवम् उनके काव्य की निम्नलिखित विशेषतायें थीं
- ये एकेश्वरवाद के मानने वाले थे।
- निराकार ईश्वर की उपासना करते थे।
- जाति-पाँति, छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे।
- धार्मिक बाह्याडम्बरों का खण्डन करते थे।
- मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
- इनका निर्गुण ब्रह्म न वेदान्तियों का निर्गुण ब्रह्म था और न मुसलमानों का।
- हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये सामान्य भक्ति मार्ग का प्रदर्शन किया।
- इनके काव्य का प्रेम-तत्त्व सूफियों का है, वैष्णवों का नहीं ।
- वैष्णवों ने केवल अहिंसा और प्रपत्ति ही ग्रहण किया।
- इनके सिद्धान्तों पर बज्रयानी सिद्धों तथा नाथ पंथियों का विशेष प्रभाव है।
- इनके अनुयायी अशिक्षित अधिक थे, शिक्षित कम ।
- गुरु को गोविन्द से भी अधिक महत्त्व दिया गया।
- काव्य की भाषा पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी तथा विभिन्न बोलियों का मिश्रण थी।
- भाषा अपरिष्कृत थी।
- सन्त काव्य का प्रधान रस शान्त था, वैसे अद्भुत और वीभत्स भी पाये जाते हैं।
- इनके काव्य में रहस्यवाद की उद्भावना पाई जाती है।
- मौलिकता का अभाव, पिष्टपोषण। सभी कवियों द्वारा एक-सी बातें दुहराई गई हैं।
- साखी, झूलना, सबद, सवैया, हंसपद आदि छन्दों का प्रचार रहा।
प्रेममार्गी शाखा
सूफी लोग सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करते थे। सूफी शब्द का अर्थ है सफेद ऊन। ये लोग सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे।
सूफियों का सिद्धान्त है कि ईश्वर हमारा प्रियतम है, जो जगत् के कण-कण में व्याप्त है, उसके पास तक पहुँचने का साधन लौकिक प्रेम है जो साधन के रूप में आगे चलकर अलौकिक हो जाता है।
ये सर्वेश्वरवाद के मानने वाले थे। इनका विश्वास था कि जीवन और जगत् भी ब्रहा हैं। इन्होंने ‘तत्वमसि’ के ज्ञान को स्वीकार किया।
एकेश्वरवाद के कट्टर पक्षपाती मुसलमान इनसे घृणा करते थे। प्रेममार्गी परम्परा वैसे तो उषा अनिरुद्ध की कथा से प्रारम्भ होती है, परन्तु उसका प्रौढ़ रूप इन मुसलमान कवियों में ही दृष्टिगोचर होता है।
प्रेममार्गों कवियों ने प्रेम कथानकों पर अवधी भाषा में ही अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे।
प्रेममार्गी शाखा की विशेषतायें
- सूफी कवि मुसलमान थे।
- अपने काव्यों में हिन्दू जीवन का अच्छा चित्रण किया |
- लोगों में प्रचलित कथाओं द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया।
- इन प्रेम आख्यानों में कल्पना का प्राचुर्य है।
- शुद्ध प्रेम का सामान्य मार्ग प्रदर्शन करके साम्प्रदायिक जाति भेद दूर किया।
- लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया।
- रचनाओं में कल्पना के साथ ऐतिहासिकता का भी पुट है।
- प्रत्येक कथा रूपक पर आधारित है।
- विरह वर्णन उच्च कोटि का है।
- इनका रहस्यवाद भावात्मक है।
- ये प्रबन्ध काव्य फारसी की मनसबी शैली पर आधारित हैं।
- दोहा, चौपाई आदि विभिन्न छन्दों की ही प्रचुरता है।
- इन प्रबन्ध काव्यों की भाषा अवधी है।
- उसमें साहित्यिकता का अभाव है।
- शृंगार रस की ही प्रधानता है।
- नायिका के नाम पर ही रचनाओं के नाम रखे गए हैं।
सगुण धारा की राम भक्ति शाखा
भगवत् प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी भारतवर्ष में सदैव से प्रवाहित होती आई है। वैसे तो तीनों की धारायें संसार के कल्याण के लिए हैं, परन्तु भक्ति की धारा सरल और सुगम है तथा मानव प्रकृति के अनुकूल है।
देवर्षि नारद इस भक्तियोग के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। वैष्णव भक्ति के सम्यक् प्रचार के लिए रामानुजाचार्य (सम्वत्1073) ने दृढ़ आधार उपस्थित किए।
उत्तरी भारत में भक्ति को सक्रिय रूप देने का श्रेय स्वामी रामानन्द जी को है जो रामानुजाचार्य की 14 वीं शिष्य परम्परा में थे।
रामानन्द जी की शिष्य परम्परा के द्वारा यद्यपि देश में रामभक्ति का प्रचार खूब हो रहा था, परन्तु हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का पूर्ण विकास विक्रम की 17 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी के द्वारा हुआ।
रामभक्ति काव्य की विशेषतायें
- उस समय तक प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचना हुई।
- रचनाओं की भाषा अवधी तथा बज थी।
- प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए।
- सर्वांगीण मत-मतान्तरों में दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय हुआ।
- नैतिक तथा सामाजिक आदर्श स्थापित किये गए।
- ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया।
- इन कवियों की उपासना सेवक सेव्य भाव की थी।
- लोक संग्रह की भावना को प्रमुखता दी गयी।
- इस शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे।
कृष्ण-भक्ति शाखा
उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का सबसे अधिक प्रचार श्री वल्लभाचार्य जी ने किया। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य का प्रचार किया।
ये शुद्धाद्वैतवादी थे, इनके सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म, जीव और जड़ जगत् में अन्तर नहीं है। इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्त्व दिया, आत्म-चिन्तन के स्थान पर आत्म-समर्पण को श्रेष्ठ समझा।
इनकी भक्ति परम्परा में कृष्ण की उपासना सखा के रूप में की जाती थी और कृष्ण के बाल और युवक प्रेमी रूप ग्रहण किये जाते थे।
वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग चलाया। इनके पुत्र बिट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्गी कवियों में से आठ कवियों को चुनकर ‘अष्टछाप’ की संज्ञा दी।
इनमें से चार-सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास और कुम्भनदास, श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तथा चार-चतुर्भुजदास, छीत, स्वामी नन्ददास और गोविन्ददास, श्री विठ्ठलनाथ जी के शिष्य थे।
अष्टछाप के कवियों में तथा कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास प्रमुख कवि थे।
“सुर, नन्द कुम्मन, चतुर, छीत, कृष्ण गोविन्द |
अष्टछाप के ये कवि हैं, अरु परमानन्द || “
कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषतायें
- गीतिकाव्य की परमोन्नति हुई।
- वात्सल्य और शृंगार, दो रसों का ही प्राधान्य रहा।
- श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना प्रमुख रही।
- काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही।
- मुक्त काव्य ही लिखा गया।
- कृष्ण का लोकरंजक रूप ही आकर्षण का विषय रहा।
- ज्ञान मार्ग की निस्सारता और भक्ति मार्ग की महानता दिखाई गई।
- कूट पादों का निर्माण हुआ।
रीतिकाल
भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति और शृंगार मिले हुए थे। भक्तिकाल के साहित्यकारों का शृंगार वर्णन उनकी प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक था।
जिस शृंगार की सुरा ने मृतप्राय हिन्दू समाज को अनुप्राणित करने में रामबाण का काम किया था उसी सुरा और सुन्दरी का सहयोग आगे चलकर एक घातक अभिशाप सिद्ध हुआ।
जिस शृंगार वर्णन को भक्तिकालीन साहित्यकार अपने आराध्य की आराधना का अंग मानकर किया करते थे, आगे चलकर यह एक व्यसनमात्र रह गया।
भक्त कवियों में भक्ति भावना का था, कवित्व चमत्कार उनके लिए गौणातिगौण वस्तु थी। आगे के कवियों में कवित्व प्रधान हो गया, भक्ति उनकी विलास एवम् वासनामयी प्रवृत्तियों की यवनिकामात्र (परदा) थी।
कला और कविता का मूल्यांकन उस समय होता है, जब वातावरण शान्त हो, अन्न, वस्त्र की चिन्ता से कलाकार और कला-प्रेमी मुक्त हों, इन दोनों ही बातों का उस युग में अभाव था।
कवि को जीवनयापन के लिए राज्याश्रय स्वीकार करना पड़ता था। साहित्यकारों की जीविका आश्रयदाताओं की हाँ में हाँ मिलाने तथा उनके पाप कर्मों को पुण्य बताने पर आश्रित थी।
अब साहित्यकार की व्याख्या का प्रिय विषय जीवन नहीं था अपितु नारी था राजा ही नहीं, राज्याश्रित कवि भी अपने प्रतिद्वन्द्वी से आगे बढ़ना चाहते थे।
इसके लिए उन्हें संस्कृत और प्राकृत साहित्य के अध्ययन में कठोर प्रयत्न करना पड़ता और प्राचीन विषयों को नया रंग देकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था।
एक बात और थी, वह यह कि हिन्दी में लक्ष्य ग्रन्थ पर्याप्त लिखे जा चुके थे, परन्तु लक्षण ग्रन्थों का साहित्य में अभाव था।
साहित्यकारों की प्रवृत्ति इस ओर जाना स्वाभाविक ही थी, क्योंकि लक्ष्य ग्रन्थों के पश्चात् लक्षण ग्रन्थ आते हैं। ये हिन्दी कवि लक्षण प्रस्तुत करने में तो नहीं, परन्तु उदाहरण देने में अपने पूर्ववर्ती कवियों से आगे निकल गये।
हिन्दी में नवीन सिद्धान्तों का विवेचन सम्भव न हो सका, इसका प्रथम कारण तो यह था कि कवियों में मौलिकता का अभाव था।
दूसरा कारण यह था कि उस समय जो कुछ लिखा जाता था पद्य में ही लिखा जाता था, क्योंकि हिन्दी गद्य का विकास नहीं हुआ था और पद्य में किसी विषय की सम्यक् मीमांसा या तर्क वितर्क करना सम्भव नहीं था।
इस काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने लक्षण मन्थ न लिखकर लक्ष्य ग्रन्थ लिखे।
‘इस प्रकार के कवियों में से कुछ ने तो प्रबन्ध काव्य लिखे, कुछ ने नीति भक्ति या ज्ञान सम्बन्धी कवितायें लिखीं, कुछ ने शृंगार की स्फुट रचनायें कीं।
कुछ ऐसे भी थे जो सिंह और सपूत की भाँति लकीर छोड़कर चलना जानते थे, उन्होंने इस घोर शृंगार काल में भी वीरता के गीत गाए।
नारी के कटाक्ष और नृत्य के स्थान पर तलवार का नृत्य दिखाया। इस प्रकार इस काल में रीति-बद्ध और रीति-मुक्त दो प्रकार के कवि हुए।
रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास थे तथा अन्य कवियों में चिंतामणि, बेनी, बिहारी, मतिराम, देव, भूषण आदि प्रमुख थे।
रीतिकालीन काव्य की विशेषतायें
- संस्कृत साहित्य के आधार पर रीति ग्रन्थों की रचना हुई।
- प्रमुख रूप में रस, अलंकार, छन्द और नायिका भेद का ही विवेचन हुआ।
- नाट्यशास्त्र तथा शब्द-शक्ति का यथोचित विवेचन नहीं हुआ।
- विचारों में नवीनता और मौलिकता का अभाव रहा।
- इस काल के प्रमुख छन्द कवित्त और सवैया ही रहे ।
- बिहारी आदि कुछ कवियों ने ही दोहे लिखे।
- लक्षणों की अपेक्षा उदाहरण अधिक सुन्दर लिखे।
- इस काल का प्रधान रस शृंगार रहा।
- शृंगार के साथ वीर रस की भी श्रेष्ठ रचनायें हुई।
- भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया।
- प्रबन्ध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक काव्यों की अधिक रचना हुई।
- इस काल की भाषा बृज और अवधी थी।
- मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों का भी मिश्रण हुआ।
- रीतिबद्ध कवियों में से कुछ ने लक्षण ग्रन्थ लिखे और कुछ ने केवल लक्ष्य ग्रन्थ ।
- रीति मुक्त कवियों ने भक्ति, नीति, प्रेम, वीर, शृंगार आदि विविध विषयों पर लेखनी चलाई।
आधुनिक काल
भारतीय विलासिता और विग्रह के फलस्वरूप, व्यापार की प्रवंचना से आए हुए अंग्रेज जब भारतवर्ष में शासक के रूप में जम गए तब भारतीयों का ध्यान जीवन के कटु सत्य की ओर गया।
दो विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं के संघर्ष से जनजीवन में जाग्रति की भावना उठने लगी। लोगों का ध्यान अपने राजनैतिक दायित्वों पर गया और राष्ट्रीय भावों को प्रकट करने की भावना बलवती हो उठी।
यद्यपि राष्ट्रीय उद्बोधन के भाव भूषण के समय में ही दृष्टिगोचर होने लगे थे, परन्तु उस अंकुरित बीज में अब पल्लवित और कुसुमित होने की इच्छा तीव्र होने लगी थी।
साहित्यिक जागरण के साथ जनता में सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक जागृति भी होने लगी थी। विदेशी शासक शासन के साथ-साथ इस देश में अपने धर्म का प्रचार भी करने लगे थे, किया मुसलमानों ने भी था, परन्तु उनमें और इनमें अन्तर केवल इतना ही था कि उनका प्रचार तलवार के जोर पर आधारित था, इनका बुद्धिवाद पर।
अपने-अपने धार्मिक विचारों के प्रचार प्रसार, खण्डन मण्डन के लिए पद्य उपयुक्त माध्यम नहीं था।
प्राचीन काल में मुद्रण-यन्त्रों के अभाव में साहित्य की सुरक्षा के लिये पुस्तकें कण्ठस्थ की जाती थीं। पद्य की संगीतात्मकता के कारण वह सरलता से याद हो जाता था।
अंग्रेजों के साथ-साथ इस देश में मुद्रण-यन्त्र भी आये। पुस्तकों का कण्ठस्थ करना अनावश्यक समझा जाने लगा।
यद्यपि गद्य की परम्परा ब्रजभाषा तथा उससे पूर्व भी थी, परन्तु उसकी वास्तविक धारा जन सम्पर्क स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर शासन की सुविधा के लिए अंग्रेज अफसरों के द्वारा प्रवाहित को गई।
लल्लूलाल तथा सदल मिश्र ने जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से तथा मुंशी सदासुखलाल और इंशाअल्ला खाँ ने स्वान्तः सुखाय खड़ी बोली में प्रारम्भिक गद्य लिखा।
भारतेन्दु युग
नवोत्थान काल के सबसे अधिक व्यापक एवम् प्रभावोत्पादक स्वरूप के दर्शन हमें भारतेन्दु-युग में होते हैं।
इस युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से गद्य साहित्य को समस्त विधाओं पर उनके समकालीन लेखकों ने तथा उन्होंने स्वयम् लेखनी चलाई।
भारतेन्दु ने विवादास्पद गद्य के स्वरूप को निश्चित किया। इस युग में नाटकों की प्रधानता रहीं। भारतेन्दु से पूर्व भी दो चार नाटक लिखे गये थे, परन्तु वे नाटक कहलाने योग्य न थे।
भारतेन्दु जी ने स्वयम्14 नाटकों की रचना की, इनमें कई प्रहसन भी हैं। इसमें सत्य हरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, नौलदेवी, भारत दुर्दशा, चन्द्रावती आदि प्रमुख हैं। भारतेन्दु के नाटक उनके जीवनकाल में ही खेले गए थे।
उस काल में भारतेन्दु के अतिरिक्त बाबू तोताराम, बाबू राधाकृष्णदास, बाबू गोलकचन्द्र आदि प्रमुख नाटककार थे।
भारतेन्दु काल के गद्य लेखकों में पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, पण्डित बद्रीनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास तथा पण्डित अम्बिकादत्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
द्विवेदी युग
यह युग आलोचनात्मक युग था। भारतेन्दु के समय में लेखकों ने व्याकरण तथा वाक्य-विन्यास की ओर कम ध्यान दिया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे जो लोग श्रद्धा तथा भक्ति के कारण हिन्दी के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे, व्याकरण के नियमों से अनभिज्ञ थे।
‘सरस्वती’ के सम्पादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने में पूर्ण योगदान दिया।
वे अशुद्ध लेखों को काट-छाँट कर लेखकों के दोष बताने में चूकते न थे। उनकी प्रेरणा से नवीन विषयों पर खोजपूर्ण निबन्ध लिखे गए।
द्विवेदी युग में हिन्दी साहित्य ने अपनी शैशवावस्था छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया। भारतेन्दु युग में भी जो बंगला साहित्य का अनुकरण हुआ था, वह द्विवेदी युग में अधिक न रहा।
लेखकों में मौलिकता आई और उन्होंने ठोस साहित्य का निर्माण किया। भाषा भी परिष्कृत और सुसंस्कृत हुई तथा शैली का भी परिमार्जन हुआ।
प्रसाद युग
यह युग कहानी तथा नाटक प्रधान था। बाबू जयशंकर प्रसाद जी ने अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, विशाख, कामता आदि उच्चकोटि के नाटक लिखे जिनमें प्रसाद जी की महान् साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार द्विजेन्द्र लाला राय ने मुगलकालीन भारत का चित्र उपस्थित किया है उसी प्रकार प्रसाद जी ने विशेष रूप से बौद्धकालीन भारत के इतिहास को अपनाया।
प्रसाद जी ने हिन्दुओं की सभ्यता तथा नैतिक श्रेष्ठता दिखाई। प्रसाद जी के नाटकों में मनोवैज्ञानिकता पर्याप्त मात्रा में है।
कहीं-कहीं बड़े सुन्दर अन्तर्द्वन्द्व दिखाये गये हैं। इस युग में प्रसाद जी के अतिरिक्त पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद ‘मिलिंद’, पण्डित गोविन्दबल्लभ पन्त तथा श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
प्रेमचन्द युग
यह युग उपन्यासों का युग था। यद्यपि प्रसाद जी ने भी ‘कंकाल’ और‘तितली’ उपन्यास लिखे थे, परन्तु नाटककार के रूप में प्रसाद जी अधिक सफल हुए।
उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचन्द जी आते हैं। इनके प्रतिज्ञा, गबन, गोदाम, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवासदन, निर्मला प्रेमाश्रम आदि उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हैं।
चरित्र-प्रधान उपन्यास लिखने में आप सिद्धहस्त थे। इन्होंने निम्न तथा मध्य कोटि के लोगों में मानवता के दर्शन कराये।
प्रेमचन्द जी कहानी लिखने में भी उतने ही सफल हुए जितने उपन्यास लिखने में कुछ लोगों का यहाँ तक विचार है कि वे कहानी लिखने में उपन्यासों की अपेक्षा अधिक सफल हुए।
प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों में समाज के उपेक्षित लोगों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है।
प्रेमचन्द के युग के अन्य कलाकारों में पण्डित विशम्भरनाथ कौशिक, सुदर्शन, वृन्दावनलाल वर्मा, मुंशी प्रतापनारायण श्रीवास्तव चण्डी, ‘हृदयेश’ तथा बेचन शर्मा उम्र आदि प्रमुख हैं।
उपसंहार
वर्तमान को किसी विशेष विधा का युग नहीं कहा जा सकता और न कोई ऐसा प्रकाण्ड लेखक ही है, जिसने इस काल पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी हो।
केवल प्रेम भरी छोटी-छोटी कवितायें तथा प्रेमी और प्रेमिकाओं से पूर्ण अश्लील कहानियाँ तथा इसी प्रकार छोटे-छोटे उपन्यास चल रहे हैं।
वर्तमान के बारे में अभी कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। निराला, महादेवी, पन्त और गुप्त जी के काव्य अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं, परन्तु उसके भी पढ़ने वाले आज कितने लोग हैं?
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
रामभक्ति काव्य की विशेषतायें क्या है ?
ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया।
इन कवियों की उपासना सेवक सेव्य भाव की थी।
लोक संग्रह की भावना को प्रमुखता दी गयी।
इस शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे।
रीतिकालीन काव्य की विशेषतायें क्या हैं ?
प्रमुख रूप में रस, अलंकार, छन्द और नायिका भेद का ही विवेचन हुआ।
नाट्यशास्त्र तथा शब्द-शक्ति का यथोचित विवेचन नहीं हुआ।
विचारों में नवीनता और मौलिकता का अभाव रहा।
इस काल के प्रमुख छन्द कवित्त और सवैया ही रहे ।
बिहारी आदि कुछ कवियों ने ही दोहे लिखे।
लक्षणों की अपेक्षा उदाहरण अधिक सुन्दर लिखे।
इस काल का प्रधान रस शृंगार रहा।
शृंगार के साथ वीर रस की भी श्रेष्ठ रचनायें हुई।
भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया।
प्रबन्ध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक काव्यों की अधिक रचना हुई।
इस काल की भाषा बृज और अवधी थी।
मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों का भी मिश्रण हुआ।
रीतिबद्ध कवियों में से कुछ ने लक्षण ग्रन्थ लिखे और कुछ ने केवल लक्ष्य ग्रन्थ ।
रीति मुक्त कवियों ने भक्ति, नीति, प्रेम, वीर, शृंगार आदि विविध विषयों पर लेखनी चलाई।


