

सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
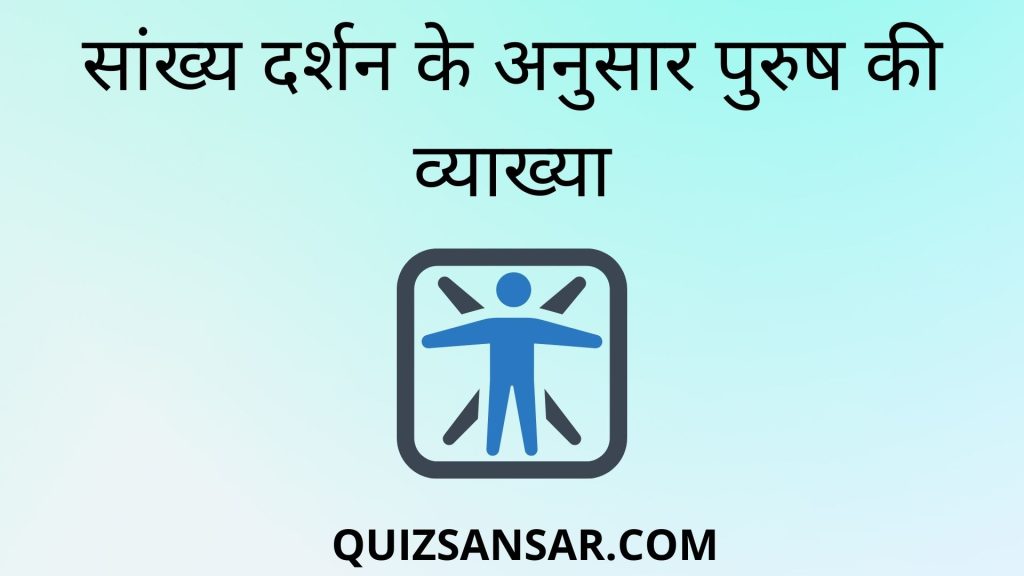
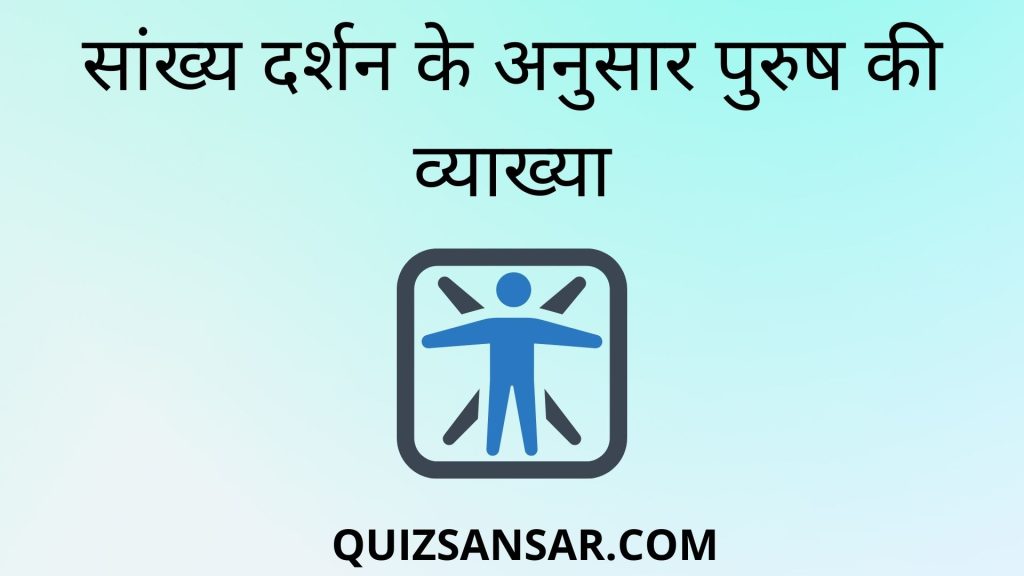
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
पुरुष (आत्मा) का अस्तित्त्व
पुरुष या आत्मा-स्वरूप-सांख्य दर्शन का एक तत्त्व तो प्रकृति है, दूसरा तत्त्व पुरुष या आत्मा है। ‘मैं’ ‘मेरा’ यह सभी व्यक्तियों का सहज स्वाभाविक अनुभव है जिसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्त्व अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए सांख्य कहता है कि आत्मा (पुरुष) का अस्तित्त्व स्वयंसिद्ध (स्वतः प्रकाश) है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया जा सकता।
जहाँ तक आत्मा के अस्तित्त्व में सभी सम्प्रदायों में मतैक्य है वही आत्मा के स्वरूप में नाना मत मतान्तर है। जहाँ तक सांख्य का प्रश्न है सांख्य के अनुसार आत्मा (पुरुष) शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। यह सांसारिक विषय नहीं है। मस्तिष्क, स्नायुमंडल या अनुभव-समूह को आत्मा समझना भूल है। आत्मा वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप में रहता है वह कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं, किन्तु स्वतः चैतन्य स्वरूप नहीं। चैतन्य इसका गुण नहीं स्वभाव है। सांख्य वेदान्त की तरह आत्मा को आनन्दस्वरूप नहीं मानता। आनन्द और चैतन्य दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं अतएव उन्हें एक ही पदार्थ का तत्त्व मानना उचित नहीं। पुरुष या आत्मा केवल द्रष्टा है जो प्रकृति से परे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उनका ज्ञान प्रकाश सर्वदा बना रहता है, जबकि ज्ञान विषय बदलते रहते हैं, किन्तु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता है वह नहीं बदलता। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। वह निष्क्रिय और अविकारी होता है। वह स्वयं नित्य और अविकारी होता है। वह स्वयं नित्य और सर्वव्यापी सत्ता है जो सभी विषयों से असंपृक्त और राग-द्वेष से रहित है। जितने कर्म या परिणाम हैं जितने सुख या दुःख हैं, वे सभी प्रकृति और उसके विकारों के धर्म हैं। जब अज्ञान के कारण पुरुष अपने को शरीर या इन्द्रिय समझ बैठता है तो उसे आभास होता है कि वह धर्म या परिवर्तन के प्रवाह में पड़कर नाना प्रकार के दुःखों, क्लेशों के दलदल में फँस गया है।
सांख्यकारिका में पुरुष के अस्तित्त्व को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ दी गई हैं –
संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्या अधिष्ठानात्,
पुरुषोंस्तिभोक्तृ भावत् कैवल्यार्थ प्रवृतेश्च ।
संघात परार्थत्वात्
सभी संघात अर्थात अवयवीय पदार्थ किसी अन्य के लिये होते हैं अचेतन तत्त्व इनका उपभोग नहीं कर सकता। अतः यह सब पदार्थ आत्मा अथवा पुरुष के लिये हैं। शरीर, इन्द्रियाँ मानस तथा बुद्धि यह सभी पुरुष के लिये साधन मात्र हैं। त्रिगुण प्रकृति सूक्ष्म शरीर सभी से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है। विकास प्रयोजनमय है। यह प्रयोजन पुरुष का कार्य ही है। पुरुष के कार्य साधन के लिये ही प्रकृति जगत् के रूप में अभिव्यक्त होती है।
त्रिगुणादि विपर्ययात्
सभी पदार्थ तीनों गुणों से निर्मित हैं, अत: पुरुष का भी होना आवश्यक है जो कि इन तीनों गुणों का साक्षी है और स्वयं इनसे परे है, तीनों गुणों से बने पदार्थ निस्तैगुण को उपस्थिति सिद्ध करते हैं जो कि उनसे परे है।
अधिष्ठानात्
समस्त अनुभवों का समन्वय करने के लिए एक अनुभवातीत समन्वयात्मक शुद्ध चेतना होनी चाहिए। सभी ज्ञान पर निर्भर है। पुरुष सभी व्यावहारिक ज्ञान का अधिष्ठाता है। सभी प्रकार की स्वीकृति एवं निषेध में उसका होना आवश्यक है।
भोक्तृभावात्
अचेतन प्रकृति अपनी कृतियों का उपभोग नहीं कर सकती। उसका उपभोग करने के लिए एक चेतन तत्त्व की आवश्यकता है। प्रकृति भोग्या है, अतः उसे एक भोक्ता की आवश्यकता पड़ती है। संसार के समस्त पदार्थ सुख दुःख अथवा उदासीनता उत्पन्न करते हैं, परन्तु सुख-दुःख और उदासीनता का अनुभव करने के लिए एक चेतन तत्त्व की आवश्यकता है। अतः पुरुष का होना अनिवार्य है।
केवल्यार्थ प्रवृते
शिष्ट पुरुषों की युक्ति के लिए प्रकृति होती है और यह दिखाई भी पड़ता है कि यह युक्ति त्रिगुण होने से सुख-दुःखात्मक प्रकृत्यादि पदार्थों की नहीं हो सकती। इसलिए मुमुक्षुजनों की प्रवृत्ति के उद्देश्य रूप मुक्ति का आधार त्रिगुणातीत चेतन पुरुष को मानना आवश्यक है।
इस प्रकार सांख्य ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त प्रमाण दिये हैं। अद्वैत वेदान्त के विरुद्ध और जैन तथा मीमांसा के समान सांख्य भी पुरुष को अनेक मानता है। तत्त्व रूप में वे सब एक ही हैं, परन्तु उनकी संख्या अनेक हैं। उनका तत्त्व चैतन्य है। यह सभी आत्माओं में समान रूप से है। इस अनेकात्मवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका में निम्नलिखित श्लोक मिलता है।
जन्ममरणकरणानाम् प्रतिनियमात् युगपत्प्रवृतेश्च
पुरुष बहुत्वं सिद्धंगण्यविपर्धयाच्चैव |
(1,2,3) जन्म, मरण, करणानां प्रतिनियमात् प्रत्येक पुरुष का जन्म मरण तथा करण अर्थात् इन्द्रियों का कार्य व्यापार भिन्न-भिन्न रूप से नियमित है। एक उत्पन्न होता है तो दूसरा मरता है। एक अन्या है तो दूसरा आँख वाला है। एक के अंधे या बहरे होने से सभी व्यक्ति अंधे या बहरे नहीं हो जाते यह भेद तभी सम्भव है जबकि पुरुष अनेक हैं। यदि एक ही पुरुष होता तो एक के मरने से सभी मर जाते एक के अन्ये या बहरे होने से सभी अन्धे या बहरे हो जाते, परन्तु ऐसा अनुभव में नहीं होता। अतः सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है।
अयुगपत्प्रवृतेश्च
सभी व्यक्तियों में समान प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। प्रत्येक व्यक्ति में पृथक्-पृथक् प्रवृत्ति दिखाई देती है। किसी में एक समय प्रवृत्ति है तो दूसरे में उसी समय निवृत्ति है। जब एक उपर्युक्त किसी समय सोया रहता है तो दूसरा उसी समय काम करता रहता है। जब एक रोता है तो दूसरा हँसता रहता है। इस प्रकार जीवों में एक ही समय प्रवृत्ति न दिखाई देने से यह सूचित होता है कि पुरुष अनेक है। यदि एक ही पुरुष या आत्मा होती तो जीवों में एक ही समय में एक ही प्रकार की निवृत्ति अथवा प्रवृत्ति दिखाई पड़ती।
त्रैगुण्यविनर्ययात्
संसार के सभी जीवों में तीनों गुण भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलते हैं। वैसे प्रत्येक वस्तु में सत्व, रजस और तमस में तीनों ही गुण उपस्थित है, परन्तु फिर भी कोई व्यक्ति सात्त्विक है, कोई राजसिक तथा कोई तामसिक जो सात्विक है उसमें शान्ति, प्रकाश तथा सुख प्रधान है। जो राजसिक है उसमें दुःख, अशान्ति तथा क्रोध प्रधान है तथा जो तामसिक है उसमें मोह तथा अज्ञान प्रधान है। यदि एक ही पुरुष होता तो सभी सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होते, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। अतः पुरुष अनेक हैं।
स्त्री, पुरुष जहाँ एक तरफ पशु-पक्षियों से ऊपर की श्रेणी में हैं वहीं दूसरी तरफ देवताओं से नीचे की श्रेणी में हैं। यदि पशु, पक्षी, मनुष्य देवता सभी में एक ही आत्मा का निवास होता तो ये विभिन्नताएँ नहीं होतीं। इन बातों से सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। ये आत्मा या पुरुष नित्य द्रष्टा या ज्ञाता स्वरूप रहते हैं। प्रकृति एक है पुरुष अनेक प्रकृति विषयों का जड़ आधार है, पुरुष उनका चेतन द्रष्टा है। प्रकृति प्रमेय है पुरुष प्रमाता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
पुरुष (आत्मा) का अस्तित्त्व क्या है ?
पुरुष या आत्मा-स्वरूप-सांख्य दर्शन का एक तत्त्व तो प्रकृति है, दूसरा तत्त्व पुरुष या आत्मा है। ‘मैं’ ‘मेरा’ यह सभी व्यक्तियों का सहज स्वाभाविक अनुभव है जिसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्त्व अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अस्वीकार करने के लिए भी चेतन आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए सांख्य कहता है कि आत्मा (पुरुष) का अस्तित्त्व स्वयंसिद्ध (स्वतः प्रकाश) है और इसकी सत्ता का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया जा सकता।
त्रिगुणादि विपर्ययात् क्या है ?
सभी पदार्थ तीनों गुणों से निर्मित हैं, अत: पुरुष का भी होना आवश्यक है जो कि इन तीनों गुणों का साक्षी है और स्वयं इनसे परे है, तीनों गुणों से बने पदार्थ निस्तैगुण को उपस्थिति सिद्ध करते हैं जो कि उनसे परे है।


सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
सांख्य दर्शन की द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष के अतिरिक्त द्वितीय तत्त्व अव्यक्त या प्रकृति है। यह इस विश्व का मूल कारण है। सम्पूर्ण विविधताओं से परिपूर्ण यह जगत् प्रकृति से ही उत्पन्न है।
“सांख्य दर्शन विश्व के मूल कारण की खोज के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करता है।“
सांख्य दार्शनिकों की मान्यता है कि विश्व में दो प्रकार की वस्तुएँ दिखाई देती है स्थूल पदार्थ (मिट्टी, जल, वृक्ष, पहाड़, भौतिक शरीर आदि) तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ (बुद्धि, इन्द्रिय, मन, अहंकार आदि)। विश्व का मूल कारण केवल वही तत्व हो सकता है जो स्थूल पदार्थों को उत्पन्न करने के साथ सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों को भी उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। सांख्य दर्शन के अनुसार चैतन्यस्वरूप पुरुष इस विश्व का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह कारण कार्य श्रृंखला से परे वह न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य। अत: कोई अचेतन तत्व ही इस जगत का कारण हो सकता है। सांख्य दर्शन इस प्रसंग में चार्वाक, जैन, बौद्ध एवं न्याय-वैशेषिक दर्शन की उस मान्यता को भी अस्वीकार करता है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु महाभूतों को अथवा उनके परमाणुओं को इस विश्व का कारण स्वीकार किया जाता है। उसके अनुसार इन परमाणुओं से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति सम्भव है, किन्तु इनसे मन, बुद्धि आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार का मूलभूत कारण केवल वही तत्त्व हो सकता है जो स्थूल और सूक्ष्म, दोनों प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न कर सके। सांख्य दर्शन विश्व के इस मूल कारण को प्रकृति या अध्यक्त अथवा प्रधान कहता है। यह प्रकृति पुरुष का विरुद्धधर्मी है। यह चेतनस्वरूप, त्रिगुणातीत एवं उदासीन पुरुष के विपरीत है।
“सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है।“
इसमें तीन गुण पाये जाते हैं। ये गुण स, रज और तमम्। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ये गुण क्या है? प्रकृति और तीनों गुणों में क्या सम्बन्ध है? क्या इनमें द्रव्य गुण-सम्बन्ध है? सामान्यतः‘गुण’ शब्द का जो अर्थ किया जाता है उस अर्थ में सत्त्व, रजम् और तमस् गुण नहीं है। वस्तुतः मे प्रकृति के गुण नहीं हैं, अपितु उसके संघटक तत्त्व हैं। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन प्रकृति और उसके गुणों में द्रव्य गुण भेद नहीं स्वीकार करता है। यहाँ सांख्य दर्शन की मान्यता न्याय वैशेषिक दर्शन की उस विचारधारा है विपरीत है जिसमें पदार्थ में द्रव्य गुण भेद स्वीकार किय जाता है। तात्पर्य यह है कि सत्त्व, रजस् और तमस् द्रव्य रूप हैं। ये इसलिए भी द्रव्य है, क्योंकि सांख्य दर्शन में इनके भी गुणों का विवेचन प्राप्त होता है। सांख्यप्रवचनभाष्य के अनुसार सत्त्व रजस् और तमस इस अर्थ में गुण हैं कि ये रस्सी के तीनों गुणों (रेशों) के समान पुरुष को बाँधने का काम करते हैं। चूँकि ये पुरुष के उद्देश्य साधन में गौण रूप से सहायक है, इसलिए भी उन्हें ‘गुण’ कहा जाता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार पुरुष की अपेक्षा गौण होने के कारण भी इन्हें गुण कहते हैं। डॉ० राधाकृष्णन के अनुसार ये इसलिए भी गुण है, क्योंकि अकेली प्रकृति विशेष्य है और ये उसके अन्दर केवल अवयव रूप से अवस्थिति है।
सांख्य दर्शन में प्रकृति के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। इनसे भी प्रकृति के स्वरूप का परिचय प्राप्त लेता है। सांख्य दार्शनिक इसे प्रधान कहते हैं, क्योंकि यह विश्व का प्रथम मूलभूत कारण है। प्रकृति अव्यक्त भी है, क्योंकि इसमें यह सम्पूर्ण जगत् अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। प्रकृति को अजा कहते हैं, क्योंकि यह अनुत्पत्र है और इसका कोई कारण नहीं है। यद्यपि यह सम्पूर्ण जड़-जगत् का कारण है, किन्तु इसका कोई कारण नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अनुमान भी कहा जाता है। इसकी सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से न होकर केवल अनुमान से होता है। यह जड़ है, क्योंकि यह मूलभूत भौतिक पदार्थ है। यह अचेतन होने के कारण अविवेकी भी है। यह विषय या ज्ञेय है, क्योंकि यह पुरुष द्वारा भोग्य एवं जानी जाती है। यह सामान्य है, क्योंकि यह सम्पूर्ण भौतिक जगत् में व्याप्त है और यह भौतिक जगत् अपने आविर्भाव के पूर्व प्रकृति में ही निहित था। चूँकि प्रकृति अकारण और अनुत्पन्न है, अत: यह नित्य एवं शाश्वत हैं। यह स्वतन्त्र है, क्योंकि यह किसी अन्य तत्त्व पर आश्रित नहीं है। चूँकि संपूर्ण जगत् प्रकृति से प्रसूत है, अतः वह प्रसवधर्मी है। उपर्युक्त लक्षणों के कारण प्रकृति को एक व्यक्तित्वविहीन सत्ता स्वीकार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सांख्यकारिकों में प्रकृति का स्वरूप बताते समय कतिपय ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं कि मानों वह कोई चेतन व्यक्तित्वयुक्त सत्ता हो। जैसे, प्रकृति स्त्री है, प्रसवधार्मिणी है। वह अत्यन्त सुकुमार है, लज्जाशील है। पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पुनः उसके समने कभी नहीं आती है। वह गुणवती है, उपकारिणी है, आदि।
प्रकृति के अस्तित्त्व के लिए प्रमाण
सांख्य दर्शन युक्तियों के आधार पर प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रसंग में –
भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च ।
कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूपस्य ।।
साख्यकारिका में निम्नलिखित कार्रिका प्राप्त होती है इस कारिका में प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित पाँच युक्तियाँ प्राप्त होती हैं –
भेदानां परिमाणत्
बुद्धि एवं मन से लेकर पृथ्वी पर्यन्त, संसार के सभी सूक्ष्मतिसूक्ष्म और स्थूल पदार्थ परिमित, परिच्छिन्त्र, परतन्त्र एवं सापेक्ष हैं। इनका कारण कोई परिमित्त, परिच्छिन्न परतन्त्र एवं सापेक्ष तत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं सकारण है। चूँकि परिमित अपरिमित के विचार की ओर, परतन्त्र स्वतन्त्र के विचार की ओर, परीच्छिन्न अपरिच्छित्र के विचार की ओर तथा सापेक्ष निरपेक्ष के विचार की ओर संकेत करता है। अतः इन परिमित परतन्त्र, परिच्छिन्न एवं सापेक्ष पदार्थों का कारण एक ऐसा अपरिमित, स्वतन्त्र, अपरिच्छिन्त्र एवं निरपेक्ष तत्त्व ही हो सकता है जो स्वयं अकारण हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्त्व प्रकृति ही है।
समन्वयात्
संसार के सभी परिमित विषय, सूक्ष्मातिसूक्ष्म और स्थूल विषय, सुख, दुःख और अज्ञान उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि सुख सत्त्व गुण से, दुःख रजोगुण से और अज्ञान तमोगुण से उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि संसार के सभी विषय सत्त्वरजस्तमसात्मक हैं। अतः इनका कारण एक ऐसा तत्त्व ही हो सकता है जिसमें सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों का समन्वय होता हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्त्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति है।
शक्तित: प्रवृत्तेः
कारण की शक्ति से, समर्थ कारण से ही किसी कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। असमर्थ कारण किसी भी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। जैसे, दही को उत्पन्न करने में दूध ही समर्थ है, पानी से दही की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शक्तिमान कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। इसके आधार पर संसार के सभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म और स्थूल पदार्थों का कारण एक ऐसा तत्त्व हो हो सकता है कि जिसमें उन्हें उत्पन्न करने की शक्ति हो। सांख्य दर्शन के अनुसार यह समर्थ कारण अव्यक्त प्रकृति है।
कारणकार्यविभागात्
संसार में कारण और कार्य में भेद दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है। उस कारण का भी एक कारण होता है। कार्य-कारण की यह शृंखला अनन्त तक नहीं जा सकती है, अन्यथा अनवस्था दोष (The Fallacy of Infinite Regress) उत्पन्न होता है। अतः संसार की सभी वस्तुओं का एक मूलभूत कारण है जिसका कोई अन्य कारण नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति है।
अविभागाद्वैश्वरूपस्य
सांख्य दर्शन कारण कार्य सम्बन्ध के विषय में दो तथ्यों को स्वीकार करता है-प्रथम, कारण से कार्य उत्पन्न होता है और द्वितीय, नष्ट होने पर कार्य पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जैसे, सोने से निर्मित सोने की अंगूठी नष्ट होने पर पुनः सोने में मिल जाती है। तात्पर्य यह है कि तत्त्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। इस आधार पर सांख्य दर्शन का कथन है कि यह सम्पूर्ण विश्व एक ऐसे कारण से उत्पन्न होना चाहिए जिसमें वह प्रलयावस्था में पुनः विलीन हो सके। सांख्य दर्शन इस कारण को प्रकृति कहता है।
सांख्य दर्शन उपरोक्त युक्तियों के आधार पर प्रकृति को सत्ता को सिद्ध करता है जो चेतन पुरुष के अतिरिक्त समस्त जड़ जगत् का कारण है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है ?


सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
विकास की प्रक्रिया-प्रकृति-पुरुष संबंध
संसार की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया से निष्पादित होती है अर्थात् जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है तभी संसार की उत्पत्ति होती है प्रकृति और पुरुष का संयोग दो भौतिक द्रव्यों जैसा साधारण संयोग नहीं है। यह एक प्रकार का विलक्षण संयोग है। प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव वैसा ही पड़ता है जैसे विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर जब तक दोनों का किसी तरह सम्बन्ध नहीं होता, जब तक संसार की सृष्टि नहीं हो सकती, किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति और पुरुष तो एक-दूसरे से भिन्न और विरुद्ध धर्म के हैं। तब फिर उनका पारस्परिक सहयोग कैसे सम्भव है? सांख्य इसके उत्तर में कहता है जैसे एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों मिलकर परस्पर सहयोग के साथ जंगल पार कर सकते हैं, उसी प्रकार जड़ प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष में दोनों परस्पर मिलकर एक-दूसरे की सहायता से अपना कार्य सम्पादित कर सकते प्रकृति दर्शनार्थ पुरुष की अपेक्षा रखती है और पुरुष कैवल्यार्थ प्रकृति की सहायता लेता है।
सृष्टि के पूर्व सभी गुण साम्यावस्था में रहते हैं। प्रकृति और पुरुष का सानिध्य होने पर इस मायावस्था में विकार उत्पन्न होता है। इस अवस्था को गुण-क्षोम कहते स्वभावतः क्रियात्मक है परिवर्तनशील होता है और तक उसके कारण और गुणों में भी स्पन्दन होने सर्वप्रथम रजोगुण जो लगता है और इसी प्रकार क्रमश: तीनों गुणों का पृथवकरण और संयोजन होता है और न्यूनाधिक अनुपातों में उनके संयोगों के फलस्वरूप नाना प्रकार के संसारिक विषय उत्पन्न होते हैं।
महत् अथवा बुद्धि = महर्षि कपिल के अनुसार सांख्य में विकास की प्रथम कृति महत् या ‘बुद्धि’ का प्रादुर्भाव है। यह प्रकृति का प्रथम विकार है, बाह्य जगत् की दृष्टि से यह विराट बीज स्वरूप है अतएव महत् कहलाता है। आन्तरिक दृष्टि से यह वह बुद्धि है तो जीवों में विद्यमान रहती है। बुद्धि का विशेष कार्य निश्चय और अवधारण है। उसके द्वारा हो ज्ञाता-ज्ञेय का भेद और किसी विषय का निर्णय निश्चित होता है। सत्वगुण के अधिक्य से बुद्धि का उदय होता है। उसका स्वाभाविक धर्म स्वयं को तथा वस्तुओं को प्रकाशित करना है। तत्त्व की अधिक वृद्धि होने से बुद्धि में सत्त्वगुण की अधिकता होती है और इसी प्रकार तक की वृद्धि की सहायता से पुरुष अपना और प्रकृति का भेद समझकर अपने यथार्थ स्वरूप की विवेचना कर सकता है। बुद्धि आत्मा से भिन्न है क्योंकि पुरुष या आत्मा समस्त भौतिक द्रव्यों और गुणों से परे है। इन्द्रियों और मन का व्यापार बुद्धि के लिए है और बुद्धि का व्यापार आत्मा के लिए है।
अहंकार
प्रकृति का दूसरा विकार ‘अहंकार’ है। अहंकार महत् से उत्पन्न होता है। कपिल ने कहा है‘अभिमानोहेकार’ अभिमान ही अहंकार है। अहंकार के कारण ही पुरुष अपने को कर्त्ता, कामी और स्वामी समझने लगता है। अहंकार ही समस्त व्यवहारों का मूल है। इन्द्रियों द्वारा सर्वप्रथम विषयों का प्रत्यक्ष होता है फिर वह विषयों पर विचार करके उनका स्वरूप निर्धारित करता है। उन विषयों में हमारा, मेरा और मेरे लिए का अहंकार जाग्रत हो सकता है।
‘अहंकार’ तीन प्रकार के माने गये हैं –
वैकारिक अथवा सात्त्विक
इसमें सत्वगुण प्रधान होता है। सार्वभौम रूप से यह मनस, पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न करता है।
भूतादि या तामस
इसमें तमस गुण प्रधान होता है। विश्वरूप में यह पञ्च तन्मात्राओं की उत्पत्ति करता है।
तैजस अथवा राजस्
इसमें राजस गुण प्रधान होता है। विश्व रूप में यह सात्त्विक और तामस गुणों के लिए शक्ति प्रदान करता है।
अहंकार से सृष्टि या उपरोक्त क्रम सांख्यकारिका में दिया गया है, परन्तु विज्ञानभिक्षु ने सांख्य में दिया गया है। परन्तु विज्ञानभिक्षु ने सांख्य प्रवचन भाष्य में मन को ही एकमात्र ऐसी इन्द्रिय माना है जो कि सत्वगुण प्रधान है और सात्विक अहंकार होता है। शेष दस इन्द्रियाँ राजस अहंकार का और मंच तन्मात्र तामस अहंकार का परिणाम है।
मन
मन का सहयोग ज्ञान और कर्म दोनों में आवश्यक है। यह आभ्यान्तकि इन्द्रिय है और यही अन्य इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर प्रेरित करता है। सूक्ष्म होते हुए भी यह सावयव है और भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो सकता है। ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ बाह्य कारण हैं। प्राण की क्रिया अन्तःकरण है। प्राण की क्रिया अन्तःकरण से प्रवर्तित होती है। अन्तःकरण को बाह्य इन्द्रियाँ प्रभावित करती हैं। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्रहीत प्रत्यक्ष निर्विकल्प होता है। मन उसका स्वरूप निर्धारित करके उसे सविकल्प प्रत्यक्ष के रूप में परिणित करता है। अहंकार प्रत्यक्ष विषयों पर स्वत्व जमाता है। वह उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल विषयों में राग तथा प्रतिकूल विषयों से द्वेष रखता है। बुद्धि इन विषयों का ग्रहण या त्याग करने का निश्चय करती है। तीन अन्तःकरण और दस बाह्य करण मिलकर त्रयोदशकरण कहलाते हैं। बाह्य इन्द्रियाँ वर्तमान विषयों से ही सम्बन्ध रखती हैं जबकि आभ्यन्तरिक इन्द्रियाँ भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कालों के विषयों से सम्बन्ध रखती हैं।
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ
नेत्र, श्रवण, घ्राण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनसे क्रमशः रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श का ज्ञान होता है। ये अहंकार के परिणाम हैं और पुरुष के निमित्त उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण एक-दूसरे को दबाने की चेष्टा करता है। जिस वस्तु में जो गुण प्रबल रहता है वैसा ही उस वस्तु का स्वभाव बन जाता है। इन्हीं गुणों के कारण ही संसार की समस्त वस्तुओं को इष्ट, अनिष्ट तथा तटस्थ इन तीन वर्गों में बाँटा जाता है। ये तीन गुण निरंतर परिवर्तनशील है। ये एक क्षण भी अविकृत नहीं रह सकते क्योंकि विकार उसका स्वभाव है।
सरूप और विरूप परिणाम
गुणों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं-सरूप और विरूप। प्रलयावस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खिंचकर स्वयं अपने में परिणत हो जाता है। इस प्रकार सत्व, सत्व में, रज-रज में और तम, तम में परिणत हो जाता है। यह परिणामस्वरूप परिणाम कहलाता है। पृथक्-पृथक् रहने के कारण इस अवस्था में गुण कोई काम नहीं करता। सृष्टि के पूर्व भी यही साम्यावस्था रहती है। दूसरे शब्दों में, वे अस्फुटित रूप से ऐसे अव्यक्त पिंडरूप में रहते हैं जिसमें न रूपान्तर है, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गन्ध और न कोई विषय होता है। यही साम्यावस्था सांख्य की ‘प्रकृति’ है। दूसरे प्रकार के परिणाम तब उत्पन्न होता है जब गुणों में से एक प्रबल हो उठता है और शेष दो उसके अधीन हो जाते हैं। इस स्थिति में ही विषयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का परिणाम विरूप परिणाम कहलाता है। इसी से सृष्टि का प्रारम्भ होता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
- सुखवाद क्या है?
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
अहंकार क्या है ?
प्रकृति का दूसरा विकार ‘अहंकार’ है। अहंकार महत् से उत्पन्न होता है। कपिल ने कहा है‘अभिमानोहेकार’ अभिमान ही अहंकार है।
सरूप और विरूप के क्या परिणाम हैं ?
गुणों में दो प्रकार के परिणाम होते हैं-सरूप और विरूप। प्रलयावस्था में प्रत्येक गुण अन्य से खिंचकर स्वयं अपने में परिणत हो जाता है। इस प्रकार सत्व, सत्व में, रज-रज में और तम, तम में परिणत हो जाता है। यह परिणामस्वरूप परिणाम कहलाता है। पृथक्-पृथक् रहने के कारण इस अवस्था में गुण कोई काम नहीं करता। सृष्टि के पूर्व भी यही साम्यावस्था रहती है। दूसरे शब्दों में, वे अस्फुटित रूप से ऐसे अव्यक्त पिंडरूप में रहते हैं जिसमें न रूपान्तर है, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गन्ध और न कोई विषय होता है। यही साम्यावस्था सांख्य की ‘प्रकृति’ है। दूसरे प्रकार के परिणाम तब उत्पन्न होता है जब गुणों में से एक प्रबल हो उठता है और शेष दो उसके अधीन हो जाते हैं। इस स्थिति में ही विषयों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का परिणाम विरूप परिणाम कहलाता है। इसी से सृष्टि का प्रारम्भ होता है।


सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
सांख्य दर्शन में कार्यकारण सिद्धान्त को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कार्य कारण सिद्धान्त के सम्मुख एक प्रश्न उठता है कि क्या कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में वर्तमान रहती है? संख्या का सत्कार्यवाद इस प्रश्न का भावात्मक उत्तर है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप से मौजूद रहता है। यह बात सत्कार्यवाद के शाब्दिक विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाती है। सत्कार्यवाद शब्द सत्, कार्य और वाद के संयुक्त होने से बना है। इसलिये सत्कार्यवाद उस सिद्धान्त का नाम हुआ जो उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता स्वीकार करता है। यदि ‘क’ को कारण माना जाय और ‘ख’ को कार्य माना जाय तो सत्कार्यवाद के अनुसार‘ख’, ‘क’ में अव्यक्त रूप से निर्माण के पूर्व अन्तर्भूत होगा। कार्य और कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। वस्तु के निर्माण का अर्थ है अव्यक्त कार्य का, जो कारण में निहित है कार्य में पूर्णतः अभिव्यक्त होना उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है और इसके विपरीत विनाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति को आविर्भाव और विनाश को तिरोभाव कहा जा सकता है।
न्याय-वैशेषिक का कार्य-कारण सिद्धान्त सांख्य के कार्य-कारण सिद्धान्त का विरोधी है। न्याय-वैशेषिक के कार्य-कारण सिद्धान्त को असत्कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है- असत्कार्यवाद क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है-नामक प्रश्न आभावात्मक उत्तर है। असत्कार्यवाद, अ, सत्, कार्य, बाद के संयोग से बना है। इसलिए असत्कार्यवाद, अ सत् कार्य वाद के संयोग से बना है। इसलिए असत्कार्यवाद का अर्थ होगा वह सिद्धान्त जो उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में अस्वीकार करता है। यदि ‘क’ को कारण और ‘ख’ को कार्य माना जाय तो इस सिद्धान्त के अनुसार‘ख’ का ‘क’ में उत्पत्ति के पूर्व अभाव होगा। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य, कारण की नवीन सृष्टि है। असत्कार्यवाद को आरम्भवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धान्त कार्य को एक नई वस्तु (आरम्भ) मानता है।
सांख्य सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग करता है इन पुत्तियों को सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क कहा जाता है। ये तर्क भारतीय दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध है –
- यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत् माना जाय तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। जो असत् है उससे सत् का निर्माण असम्भव है। (असदकरणात्) आकाश कुसुम का आकाश में अभाव है। हजारों व्यक्तियों के प्रयत्न के बावजूद आकाश से कुसुम को निकालना असम्भव है। नमक में चीनी का अभाव है। हम किसी प्रकार भी नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। लाल रंग में पीले रंग का अभाव रहने के कारण हम लाल रंग से पीले रंग का निर्माण नहीं कर सकते। यदि असत् को सत् में लाया जाता तो बन्धया-पुत्र की उत्पत्ति भी सम्भव हो जाती। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है। यहाँ पर आक्षेप किया जा सकता है कि यदि कार्य कारण में निहित है तो निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि निमित्त कारण का कार्य सिर्फ उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को कार्य में व्यक्त कर देना है। अप्रत्यक्ष कार्य को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करना निमित्त कारण का उद्देश्य है।
- साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिये विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। (उपादानग्रहणात्) यह उपादान-नियम है। एक व्यक्ति जो दही का निर्माण करना चाहता है वह दूध की याचना करता है। मिट्टी का घड़ा बनाने के लिये मिट्टी की माँग की जाती है। कपड़े का निर्माण करने के लिए व्यक्ति सूत की खोज करता है। तेल के निर्माण के लिये तेल के बीज को चुना जाता है, कंकड़ को नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिये हम किसी विशेष वस्तु की माँग नहीं करते। एक व्यक्ति जिस चीज से, जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता, कर लेता। दही बनाने के लिए दूध की माँग नहीं की जाती। एक व्यक्ति पानी या मिट्टी जिस चीज से चाहता दही का सृजन कर लेता। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में मौजूद है।
- यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाय तो कार्य के निर्मित हो जाने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत् से सत् का निर्माण हुआ। परन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है। जो असत् है उससे सत् का निर्माण कैसे हो सकता है? शून्य से शून्य का ही निर्माण होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता है। कार्य की सत्ता का हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अन्तर्भूत है।
- प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का निर्माण नहीं होता है। केवल शक्त कारण में ही अभीष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। शक्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो शक्त हो। (शक्तस्य शक्यकरणात्) यदि ऐसा नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से (शक्त) कारण में अभिव्यक्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। उत्पादन का अर्थ है सम्भाव्य का वास्तविक होना। यह तर्क दूसरे तर्क (उपादान ग्रहणात्) की पुनरावृत्ति नहीं है। उपादान ग्रहणात् में कार्य के लिये कारण की योग्यता पर जो दिया गया है और इस तर्क अर्थात् शक्तस्य शक्यकारणात् में कार्य की योग्यता की व्याख्या कारण की दृष्टि से हुई है।
- यदि कार्य को उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत् माना जाय तो उसका कारण से सम्बन्धित होना असम्भव हो है। । सम्बन्ध उन्हीं वस्तुओं के बीच हो सकता है जो सत् हों। जाता यदि दो वस्तुओं में एक अस्तित्त्व हो और दूसरे का अस्तित्त्व नहीं हो तो सम्बन्ध कैसे हो सकता है? बन्ध्या-पुत्र का सम्बन्ध किसी देश के राजा से सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ सम्बन्ध के दो पदों में एक बन्ध्या-पुत्र असत् है। कारण और कार्य के बीच सम्बन्ध होता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व सूक्ष्म रूप से कारण में अन्तभूत है।
- कारण और कार्य में अभेद है। (कारणभावात्) दोनों की अभिन्नता को सिद्ध करने के लिये सांख्य अनेक प्रयास करता है। यदि कारण और कार्य तत्त्वतः एक दूसरे से भिन्न होते तो उनका संयोग तथा पार्थक्य होता। उदाहरणस्वरूप, नदी, वृक्ष से भिन्न है इसलिये दोनों का संयोजन होता है। फिर हिमालय को विन्ध्याचल से पृथक् कर सकते हैं क्योंकि यह विन्ध्याचल से भिन्न है। परन्तु कपड़े का सूतों से, जिससे वह निर्मित है, संयोजन और पृथक्करण असम्भव है।
फिर परिणाम की दृष्टि से कारण और कार्य समरूप हैं। कारण और कार्य दोनों का वजन समान होता है। लकड़ी का जो वजन होता है वही वजन उससे निर्मित टेबुल का भी होता है। मिट्टी और उससे बना घड़ा वस्तुतः अभिन्न है। अतः जब कारण की सत्ता है तो कार्य की भी सत्ता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है।
सच पूछा जाय तो कारण और कार्य एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएँ हैं। द्रव्य की अव्यक्त अवस्था को कारण तथा द्रव्य की व्यक्त अवस्था को कार्य कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जब कारण की सत्ता है तब कार्य की सत्ता भी उसमें अन्तर्भूत है।
उपरि वर्णित भिन्न-भिन्न युक्तियों के आधार पर साँख्य अपने कार्य-कारण सिद्धान्त सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धान्त को भारतीय दर्शन में सांख्य के अतिरिक्त योग, शंकर, रामानुज ने पूर्णतः अपनाया है। भगवद्गीता के –
“नासतो विद्यते भावो माभावो विधते सत:”
का भी यही तात्पर्य है। इस प्रकार भगवद्गीता से भी सांख्य के सत्कार्यवाद की पुष्टि हो जाती है।
सत्यकार्यवाद के विरुद्ध आपत्तियाँ
सत्कार्यवाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किये गये हैं। ये आक्षेप मुख्यतः असत्कार्यवाद के समर्थकों के द्वारा दिये गये हैं, जिनमें न्याय-वैशेषिक मुख्य हैं।
- सत्कार्यवाद को मानने से कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असम्भव हो जाता है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में व्याप्त है तो फिर इस वाक्य का, कि ‘कार्य की उत्पत्ति में क्या अर्थ है?’ यदि सूतों में कपड़ा वर्तमान है तब यह कहना कि ‘कपड़े का निर्माण हुआ’, अनावश्यक प्रतीत होता है।
- यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा सम्भव हुई है। परन्तु संख्यि का कार्य-कारण सम्बन्धी विचार निमित्त कारण का प्रयोजन नष्ट कर देता है। यदि तिलहन के बीज में तेल निहित है तो फिर तेली की आवश्यकता का प्रश्न निरर्थक है।
- यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण निहित है तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि वह कारण है और यह कार्य है। यदि घड़ा मिट्टी में ही मौजूद है तो घुड़ा और मिट्टी को एक दूसरे से सत्कर्यावाद कारण और कार्य के भेद को नष्ट कर देता है। से अलग करना असम्भव है।
- सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है। यदि ऐसी बात है तो कारण और कार्य के लिए अलग-अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। यदि मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा वस्तुतः एक हैं तो फिर मिट्टी और घड़े के लिए एक ही नाम का प्रयोग करना आवश्यक है।
- सत्कार्यवाद का सिद्धान्त आत्मविरोधी है। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कारण और कार्य कार में भिन्नता का रहना इस सिद्धान्त का के आकार खंडन करता है। कार्य का आकार कारण से भिन्न होता है। इसका अर्थ है कि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है। यदि कार्य का आकर नवीन सृष्टि है तब यह सिद्ध होता है कि कार्य का आकार कारण में असत् था। जो कारण में असत् था उसका प्रादुर्भाव कार्य में मानकर सांख्य स्वयं सत्कार्यवाद का खण्डन करता है।
- सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न हैं। यदि कारण और कार्य अभिन्न है तब कारण और कार्य से एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए। परन्तु हम पाते हैं कि कार्य और कारण के अलग-अलग प्रयोजन है। मिट्टी से बने हुए घड़े में जल रखा जाता है, परन्तु मिट्टी से यह प्रयोजन पुरा नहीं हो सकता।
- यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण में अन्तर्भूत है तो हमें यह कहने की अपेक्षा कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई, हमें कहना चाहिए कि कार्य उत्पत्ति कार्य से हुई। यदि मिट्टी में ही घड़ा निहित है, तब घड़े के निर्मित हो जाने पर हमें यह कहना चाहिए कि घड़े का निर्माण घड़े से हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद का सिद्धान्त असंगत है।
सत्कार्यवाद की महत्ता
सत्यकार्यवाद के विरुद्ध ऊपर अनेक आपत्तियाँ पेश की गई हैं। परन्तु इन आपत्तियों से यह निष्कर्ष निकालना कि सत्कार्यवाद का सिद्धान्त महत्त्वहीन है, सर्वथा अनुचित होगा। सांख्य का सारा दर्शन सत्कार्यवाद पर आधारित है। सत्कार्यवाद के कुछ महत्त्वों पर प्रकाश डालना अपेक्षित होगा।
सत्कार्यवाद की प्रथम महत्ता यह है कि सांख्य अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त, ‘प्रकृति’ की प्रस्थापना सत्कार्यवाद के बल पर ही करता है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य जितने तकों का सहारा लेता है उन सभी तर्कों में सत्कार्यवाद का प्रयोग है।
डॉ० राधाकृष्णन् का यह कथन कि –
“कार्य-कारण सिद्धान्त के आधार पर विश्व का अन्तिम कारण अव्यक्त प्रकृति को ठहराया जाता है।”
–इस बात की पुष्टि करता है।
सत्कार्यवाद की दूसरी महत्ता यह है कि विकासवाद का सिद्धान्त सत्कार्यवाद की देन है। विकासवाद का आधार प्रकृति है। प्रकृति से मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच महाभूत, इत्यादि तत्त्वों का विकास होता है। ये तत्त्व प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। विकासवाद का अर्थ इन अव्यक्त तत्त्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है। विकासवाद का अर्थ सांख्य के अनुसार नूतन सृष्टि नहीं है। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद में सत्कार्यवाद का पूर्ण प्रयोग हुआ है। सत्कार्यवाद के अभाव में विकासवाद के सिद्धान्त को समझना कठिन है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
- सुखवाद क्या है?
- काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
सत्कार्यवाद की महत्ता क्या है ?
सत्कार्यवाद की प्रथम महत्ता यह है कि सांख्य अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त, ‘प्रकृति’ की प्रस्थापना सत्कार्यवाद के बल पर ही करता है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य जितने तकों का सहारा लेता है उन सभी तर्कों में सत्कार्यवाद का प्रयोग है।


नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
स्वतन्त्रता नैतिक मूल्यांकन को पूर्व मान्यता है तात्पर्य यह है कि जिस कार्य को हमने अपने स्वतन्त्र संकल्प से नहीं किया है उसके प्रति हमें उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता। लाचार और विवशता में, भय या प्रलोभन के कारण किया गया कार्य नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा नहीं समझा जा सकता। परन्तु यहाँ एक आवश्यक प्रश्न यह है कि हम संकल्प करने में कहाँ तक स्वतन्त्र है? क्या हम जो चाहते हैं वही संकल्प कर लेते हैं? अथवा मारा संकल्प मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों से नियंत्रित होता है। कोई भी कार्य किसी प्रवृत्ति या प्रेरणा से होता है परन्तु प्रेरणा को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियाँ भी होती है। प्रश्न यह है कि हम सभी परिस्थितियों अथवा विरोधी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर कोई संकल्प करते हैं अथवा परिस्थिति और परिवेश के अनुसार हम कोई संकल्प करते हैं? नीतिशास्त्र में इसके दो उत्तर दिये जाते हैं। प्रथम को नियतिवाद और दूसरे को अनि तिवाद या स्वतन्त्रतावाद कहते हैं। दोनों के पक्ष और विपक्ष में अनेकानेक तर्क दिये जाते हैं।
नियतिवाद
नियतिवाद संकल्प को पहले से नियत मानता है। इसके अनुसार हमारा संकल्प परिस्थितियों से निर्धारित होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। यह परिस्थिति के अनुसार ही संकल्प करता है। परिस्थिति के अतिकूल संकल्प करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। हम परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। नियतिवाद के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये जाते –
- मनोवैज्ञानिक तर्क,
- ज्ञानशास्त्रीय तर्क,
- दार्शनिक तर्क,
- जड़वादी तर्क,
- धार्मिक तर्क,
मनोवैज्ञानिक तर्क
मनुष्य अपनी प्रवृत्ति या प्रयोजन के अनुसार ही कोई ऐच्छिक कर्म करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति के मन में अभाव का अनुभाव होता है। अभाव से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा को पूर्ति के लिए मनुष्य संकल्प करता है। संकल्प के पूर्व अभाव, इच्छा, आवेग आदि का होना अनिवार्य है। इस प्रकार व्यक्ति का संकल्प इन मानसिक क्रियाओं के अनुसार ही होता है। इस प्रकार उसका संकल्प स्वतंत्र नहीं वरन मानसिक क्रियाओं के अधीन है। हम किसी परिस्थिति में वैसा ही संकल्प करते हैं जैसे इमारी प्रवृत्ति और प्रेरणा होती है। अतः संकल्प तो प्रवृत्ति और प्रेरणा के अधीन है। हमारी प्रवृत्त और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले भी अनेक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है, जैसे आनुवंशिकता वातावरण आदि। प्रायः हमारी प्रवृत्ति हमारे वंश या कुल प्रथा के अनुसार होती है। इसी प्रकार गातावरण के अनुकूल भी हममें प्रवृत्त होती है। इससे स्पष्ट है कि हमारा संकल्प मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अधीन है। हम संकल्प करने में स्वतन्त्र नहीं है। हम अपनी आन्तरिक प्रवृत्ति और बाहा वातावरण के अनुकूल ही संकल्प करते हैं। इनके प्रतिकूल संकल्प करना सामाजिक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं।
ज्ञानशास्त्रीय तर्क
जिस वस्तु या विषय का हमें ज्ञान होता है, वह वस्तु तेय है। ज्ञेय वस्तु ज्ञान के नियमों से बँधी है। ज्ञान का नियम यह बतलाता है कि कोई भी विषय स्वतन्त्र नहीं। एक विषय का दूसरे से सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य कारण का सम्बन्ध है। अतः किसी विषय का ज्ञान होने का अर्थ उस विषय के कारण को जानना है। कारण का ज्ञान होने पर उस विषय या वस्तु को स्वतंत्र नहीं, वरन कारण के अधीन माना जाता है। मानव का संकल्प भी स्वतन्त्र नहीं। हमारे ऐच्छिक कार्य भी कारणाधीन है। इससे नियतिवाद का समर्थन होता है।
दार्शनिक तर्क
दार्शनिक तुकों में कार्य कारण नियम सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस नियम के अनुसार संसार का कोई भी विषय या विश्व की कोई भी घटना अकारण नहीं। प्रत्येक विषय का कारण अवश्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई कार्य अकस्मात् नहीं उत्पन्न होता। यदि विश्लेषण किया जाय तो उस कार्य का कारण अवश्य मिलेगा। मानव संकल्प भी एक कार्य है, इसका भी कारण अवश्य होना चाहिये। यदि यह सकारण है तो स्वतन्त्र नहीं।
जड़वादी तर्क
जड़वाद के अनुसार संसार का मूल रूप जड़ात्मक है। जड़ तत्व ही परम तत्त्व है। इन्हीं जड़ तत्वों से क्रमशः विश्व का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में हो शरीर बुद्धि, संकल्प आदि का भी आविर्भाव होता है। शरीर के बिना संकल्प की कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर भौतिक है, अत: संकल्प भी भौतिक है। सभी भौतिक पदार्थ सकारण है, अकारण नहीं सकारण होने से स्वतन्त्र नहीं। संकल्प भी भौतिक है। सकारण है अतः स्वतन्त्र नहीं।
धार्मिक तर्क
धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर ही जगत् का कुर्ता, धर्ता और हर्ता है। परमात्मा ही मानव को जन्म देता है तथा मानव से संकल्प शक्ति भी प्रदान करता है। अतः मानव के संकल्प का कारण ईश्वरेच्छा है। इस प्रकार संकल्प स्वतन्त्र नहीं, वरन ईश्वर की इच्छा से नियन्त्रित है |
उपरोक्त सभी तसंकल्प की स्वतन्त्रता के विरोधी है। इनसे नियतिवाद सिद्ध होता है। नियतिवाद के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क हैं –
- मनोवैज्ञानिक तर्क के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि हमारा संकल्प वातावरण, वंश, परम्परा आदि से प्रभावित होता है, परन्तु वातावरण तथा वंश परम्परा से मुक्त होने की शक्ति भी मनुष्य में है। इसके बिना भी व्यक्ति संकल्प करता है। किसी परिस्थिति पर वातावरण का प्रभाव स्वाभाविक है, परन्तु विवेक के कारण व्यक्ति वातावरण के विरुद्ध भी संकल्प करता है। इससे स्पष्ट है कि संकल्प की स्वतन्त्रता व्यक्ति में है।
- ज्ञानशास्त्रीय तथा दार्शनिक तर्क में कार्य-कारण नियम की प्रधानता है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में सब कुछ कारण के अधीन है। संकल्प भी कारण के अधीन है, परन्तु कारण के अधीन होने से ही किसी वस्तु की स्वतन्त्रता समाप्त नहीं हो जाती। संकल्प सकारण होकर भी स्वतन्त्र हो सकता है। हमारे सकल्प का कोई कारण हो सकता है परन्तु संकल्प करते समय हम कारण से नहीं बँध सकते। हम कारण से मुक्त होकर भी संकल्प कर सकते हैं।
- जड़वादी तथा धार्मिक तर्क जड़, तत्त्व तथा ईश्वर को सभी वस्तुओं का कारण मानकर संकल्प स्वतन्त्र नहीं मानते। जुड़वादी संसार का स्वरूप जड़ात्मक मानते हैं। परन्तु संकल्प अगड़, मन या आत्मा का धर्म है। इसका कारण जड़ या भौतिक वस्तु नहीं हो सकता। ईश्वरवादी ईश्वर को सबका कर्त्ता मानते हैं। संकल्प का सृष्टा भी वही है। मानव में संकल्प शक्ति का दाता ईश्वर हो सकता है, परन्तु इस शक्ति का प्रयोग करने में में मनुष्य स्वतन्त्र है।
- नियतिवाद मानव की सभी क्रिया कलापों को नियत या पहले से निश्चित मानता है। अतः मानव के सभी व्यवहार, समस्त संकल्प पहले से नियत है, परन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य नियति का दास बन जाता है। वास्तव में मनुष्य नियति का नियामक है, नियति मनुष्य की नियामक नहीं। प्रबल संकल्प से मनुष्य नियति को बदल देता है।
- नियतिवाद निष्क्रियता का जनक है, अकर्मण्यता का पोषक है। यह भाग्यवाद का समर्थन करता है, पुरुषार्थवाद का नहीं। यदि सब कुछ पहले से नियत है तो हमारे कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं। फल यदि हमारे भाग्य में होगा तो अवश्य मिलेगा। यह विचार हमारे प्रयास को शिथिल कर देता है, उत्साह को कम कर देता है। अतः हम कर्म के मार्ग से पीछे हट जाते हैं।
- नैतिक दृष्टि से नियतिवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। नैतिक दृष्टि से हम उसी कार्य के लिये उत्तरदायी है, जिसे हमने अपने स्वतन्त्र संकल्प से किया हो अर्थात् जो हमारा ऐच्छिक कार्य हो । यदि हम अपनी इच्छा से कर्म नहीं करते, स्वतः संकल्प कर कोई कर्म नहीं करते, तो कार्य की जिम्मेदारी या कार्य का उत्तरदायित्व हमारे पर नहीं। यदि हमारा संकल्प किसी के अधीन है तो कार्य का फल भी किसी के अधीन है। अतः अच्छे या बुरे फल का भागी मैं नहीं है। यदि संकल्प मेरा नहीं तो कार्य भी हमारी इच्छा से नहीं हुआ, अतः फल का भाजन भी मैं नहीं।
- नियतिवाद नैतिक मापदण्डों का अवमूल्यन तो करता ही है, साथ ही साथ कानून को व्यर्थ बना देता है। यदि कोई कार्य मैने स्वतः अपनी इच्छा से नहीं किया, परन्तु मुझसे किसी प्रकार हो गया तो हम इसके लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं माने जा सकते। साथ ही साथ अच्छे कार्य के लिए न तो पुरस्कार दिया जा सकता है, और न बुरे कार्य के लिये दण्ड यदि कार्य मैने अपने संकल्प से नहीं किया, परन्तु मुझसे किसी प्रकार हो गया, तो हम इसके लिये दण्डित या पुरस्कृत क्यों होंगे ?
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं
यह भी जाने
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
- सुखवाद क्या है?
- काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त
- काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
जड़वादी तर्क किसे कहतें हैं ?
जड़वाद के अनुसार संसार का मूल रूप जड़ात्मक है। जड़ तत्व ही परम तत्त्व है। इन्हीं जड़ तत्वों से क्रमशः विश्व का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में हो शरीर बुद्धि, संकल्प आदि का भी आविर्भाव होता है।
धार्मिक तर्क क्या है ?
धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर ही जगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। परमात्मा ही मानव को जन्म देता है तथा मानव से संकल्प शक्ति भी प्रदान करता है। अतः मानव के संकल्प का कारण ईश्वरेच्छा है। इस प्रकार संकल्प स्वतन्त्र नहीं, वरन ईश्वर की इच्छा से नियन्त्रित है |


संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
स्वतन्त्रता नैतिक मूल्यांकन को पूर्व मान्यता है तात्पर्य यह है कि जिस कार्य को हमने अपने स्वतन्त्र संकल्प से नहीं किया है उसके प्रति हमें उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता। लाचार और विवशता में, भय या प्रलोभन के कारण किया गया कार्य नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा नहीं समझा जा सकता। परन्तु यहाँ एक आवश्यक प्रश्न यह है कि हम संकल्प करने में कहाँ तक स्वतन्त्र है? क्या हम जो चाहते हैं वही संकल्प कर लेते हैं? अथवा मारा संकल्प मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों से नियंत्रित होता है। कोई भी कार्य किसी प्रवृत्ति या प्रेरणा से होता है परन्तु प्रेरणा को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियाँ भी होती है। प्रश्न यह है कि हम सभी परिस्थितियों अथवा विरोधी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर कोई संकल्प करते हैं अथवा परिस्थिति और परिवेश के अनुसार हम कोई संकल्प करते हैं? नीतिशास्त्र में इसके दो उत्तर दिये जाते हैं। प्रथम को नियतिवाद और दूसरे को अनि तिवाद या स्वतन्त्रतावाद कहते हैं। दोनों के पक्ष और विपक्ष में अनेकानेक तर्क दिये जाते हैं।
नियतिवाद
नियतिवाद संकल्प को पहले से नियत मानता है। इसके अनुसार हमारा संकल्प परिस्थितियों से निर्धारित होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। यह परिस्थिति के अनुसार ही संकल्प करता है। परिस्थिति के अतिकूल संकल्प करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। हम परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। नियतिवाद के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये जाते –
- मनोवैज्ञानिक तर्क,
- ज्ञानशास्त्रीय तर्क,
- दार्शनिक तर्क,
- जड़वादी तर्क,
- धार्मिक तर्क,
मनोवैज्ञानिक तर्क
मनुष्य अपनी प्रवृत्ति या प्रयोजन के अनुसार ही कोई ऐच्छिक कर्म करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति के मन में अभाव का अनुभाव होता है। अभाव से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा को पूर्ति के लिए मनुष्य संकल्प करता है। संकल्प के पूर्व अभाव, इच्छा, आवेग आदि का होना अनिवार्य है। इस प्रकार व्यक्ति का संकल्प इन मानसिक क्रियाओं के अनुसार ही होता है। इस प्रकार उसका संकल्प स्वतंत्र नहीं वरन मानसिक क्रियाओं के अधीन है। हम किसी परिस्थिति में वैसा ही संकल्प करते हैं जैसे इमारी प्रवृत्ति और प्रेरणा होती है। अतः संकल्प तो प्रवृत्ति और प्रेरणा के अधीन है। हमारी प्रवृत्त और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले भी अनेक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है, जैसे आनुवंशिकता वातावरण आदि। प्रायः हमारी प्रवृत्ति हमारे वंश या कुल प्रथा के अनुसार होती है। इसी प्रकार गातावरण के अनुकूल भी हममें प्रवृत्त होती है। इससे स्पष्ट है कि हमारा संकल्प मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अधीन है। हम संकल्प करने में स्वतन्त्र नहीं है। हम अपनी आन्तरिक प्रवृत्ति और बाहा वातावरण के अनुकूल ही संकल्प करते हैं। इनके प्रतिकूल संकल्प करना सामाजिक व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं।
ज्ञानशास्त्रीय तर्क
जिस वस्तु या विषय का हमें ज्ञान होता है, वह वस्तु तेय है। ज्ञेय वस्तु ज्ञान के नियमों से बँधी है। ज्ञान का नियम यह बतलाता है कि कोई भी विषय स्वतन्त्र नहीं। एक विषय का दूसरे से सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य कारण का सम्बन्ध है। अतः किसी विषय का ज्ञान होने का अर्थ उस विषय के कारण को जानना है। कारण का ज्ञान होने पर उस विषय या वस्तु को स्वतंत्र नहीं, वरन कारण के अधीन माना जाता है। मानव का संकल्प भी स्वतन्त्र नहीं। हमारे ऐच्छिक कार्य भी कारणाधीन है। इससे नियतिवाद का समर्थन होता है।
दार्शनिक तर्क
दार्शनिक तुकों में कार्य कारण नियम सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस नियम के अनुसार संसार का कोई भी विषय या विश्व की कोई भी घटना अकारण नहीं। प्रत्येक विषय का कारण अवश्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई कार्य अकस्मात् नहीं उत्पन्न होता। यदि विश्लेषण किया जाय तो उस कार्य का कारण अवश्य मिलेगा। मानव संकल्प भी एक कार्य है, इसका भी कारण अवश्य होना चाहिये। यदि यह सकारण है तो स्वतन्त्र नहीं।
जड़वादी तर्क
जड़वाद के अनुसार संसार का मूल रूप जड़ात्मक है। जड़ तत्व ही परम तत्त्व है। इन्हीं जड़ तत्वों से क्रमशः विश्व का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में हो शरीर बुद्धि, संकल्प आदि का भी आविर्भाव होता है। शरीर के बिना संकल्प की कल्पना नहीं की जा सकती। शरीर भौतिक है, अत: संकल्प भी भौतिक है। सभी भौतिक पदार्थ सकारण है, अकारण नहीं सकारण होने से स्वतन्त्र नहीं। संकल्प भी भौतिक है। सकारण है अतः स्वतन्त्र नहीं।
धार्मिक तर्क
धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर ही जगत् का कुर्ता, धर्ता और हर्ता है। परमात्मा ही मानव को जन्म देता है तथा मानव से संकल्प शक्ति भी प्रदान करता है। अतः मानव के संकल्प का कारण ईश्वरेच्छा है। इस प्रकार संकल्प स्वतन्त्र नहीं, वरन ईश्वर की इच्छा से नियन्त्रित है |
उपरोक्त सभी तसंकल्प की स्वतन्त्रता के विरोधी है। इनसे नियतिवाद सिद्ध होता है। नियतिवाद के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क हैं –
- मनोवैज्ञानिक तर्क के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि हमारा संकल्प वातावरण, वंश, परम्परा आदि से प्रभावित होता है, परन्तु वातावरण तथा वंश परम्परा से मुक्त होने की शक्ति भी मनुष्य में है। इसके बिना भी व्यक्ति संकल्प करता है। किसी परिस्थिति पर वातावरण का प्रभाव स्वाभाविक है, परन्तु विवेक के कारण व्यक्ति वातावरण के विरुद्ध भी संकल्प करता है। इससे स्पष्ट है कि संकल्प की स्वतन्त्रता व्यक्ति में है।
- ज्ञानशास्त्रीय तथा दार्शनिक तर्क में कार्य-कारण नियम की प्रधानता है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में सब कुछ कारण के अधीन है। संकल्प भी कारण के अधीन है, परन्तु कारण के अधीन होने से ही किसी वस्तु की स्वतन्त्रता समाप्त नहीं हो जाती। संकल्प सकारण होकर भी स्वतन्त्र हो सकता है। हमारे सकल्प का कोई कारण हो सकता है परन्तु संकल्प करते समय हम कारण से नहीं बँध सकते। हम कारण से मुक्त होकर भी संकल्प कर सकते हैं।
- जड़वादी तथा धार्मिक तर्क जड़, तत्त्व तथा ईश्वर को सभी वस्तुओं का कारण मानकर संकल्प स्वतन्त्र नहीं मानते। जुड़वादी संसार का स्वरूप जड़ात्मक मानते हैं। परन्तु संकल्प अगड़, मन या आत्मा का धर्म है। इसका कारण जड़ या भौतिक वस्तु नहीं हो सकता। ईश्वरवादी ईश्वर को सबका कर्त्ता मानते हैं। संकल्प का सृष्टा भी वही है। मानव में संकल्प शक्ति का दाता ईश्वर हो सकता है, परन्तु इस शक्ति का प्रयोग करने में में मनुष्य स्वतन्त्र है।
- नियतिवाद मानव की सभी क्रिया कलापों को नियत या पहले से निश्चित मानता है। अतः मानव के सभी व्यवहार, समस्त संकल्प पहले से नियत है, परन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य नियति का दास बन जाता है। वास्तव में मनुष्य नियति का नियामक है, नियति मनुष्य की नियामक नहीं। प्रबल संकल्प से मनुष्य नियति को बदल देता है।
- नियतिवाद निष्क्रियता का जनक है, अकर्मण्यता का पोषक है। यह भाग्यवाद का समर्थन करता है, पुरुषार्थवाद का नहीं। यदि सब कुछ पहले से नियत है तो हमारे कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं। फल यदि हमारे भाग्य में होगा तो अवश्य मिलेगा। यह विचार हमारे प्रयास को शिथिल कर देता है, उत्साह को कम कर देता है। अतः हम कर्म के मार्ग से पीछे हट जाते हैं।
- नैतिक दृष्टि से नियतिवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। नैतिक दृष्टि से हम उसी कार्य के लिये उत्तरदायी है, जिसे हमने अपने स्वतन्त्र संकल्प से किया हो अर्थात् जो हमारा ऐच्छिक कार्य हो । यदि हम अपनी इच्छा से कर्म नहीं करते, स्वतः संकल्प कर कोई कर्म नहीं करते, तो कार्य की जिम्मेदारी या कार्य का उत्तरदायित्व हमारे पर नहीं। यदि हमारा संकल्प किसी के अधीन है तो कार्य का फल भी किसी के अधीन है। अतः अच्छे या बुरे फल का भागी मैं नहीं है। यदि संकल्प मेरा नहीं तो कार्य भी हमारी इच्छा से नहीं हुआ, अतः फल का भाजन भी मैं नहीं।
- नियतिवाद नैतिक मापदण्डों का अवमूल्यन तो करता ही है, साथ ही साथ कानून को व्यर्थ बना देता है। यदि कोई कार्य मैने स्वतः अपनी इच्छा से नहीं किया, परन्तु मुझसे किसी प्रकार हो गया तो हम इसके लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं माने जा सकते। साथ ही साथ अच्छे कार्य के लिए न तो पुरस्कार दिया जा सकता है, और न बुरे कार्य के लिये दण्ड यदि कार्य मैने अपने संकल्प से नहीं किया, परन्तु मुझसे किसी प्रकार हो गया, तो हम इसके लिये दण्डित या पुरस्कृत क्यों होंगे ?
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं
यह भी जाने
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
जड़वादी तर्क किसे कहतें हैं ?
जड़वाद के अनुसार संसार का मूल रूप जड़ात्मक है। जड़ तत्व ही परम तत्त्व है। इन्हीं जड़ तत्वों से क्रमशः विश्व का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में हो शरीर बुद्धि, संकल्प आदि का भी आविर्भाव होता है।
धार्मिक तर्क क्या है ?
धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर ही जगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। परमात्मा ही मानव को जन्म देता है तथा मानव से संकल्प शक्ति भी प्रदान करता है। अतः मानव के संकल्प का कारण ईश्वरेच्छा है। इस प्रकार संकल्प स्वतन्त्र नहीं, वरन ईश्वर की इच्छा से नियन्त्रित है |


नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
नैतिकता की पूर्व मान्यताएं
प्रत्येक विज्ञान की कुछ मान्यताएं होती है। इसे स्वयं सिद्धियों भी कहते हैं। ये मान्यताएँ ऐसी होती है जिन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता, मान लिया जाता है। इन्हें किसी प्रमाण से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मान्यताएँ आधार या नींव का काम करती हैं। ये तर्क से सिद्ध नहीं होती, परन्तु तर्क संगत कही जा सकती है। किसी तथ्य या घटना की व्याख्या के लिए इन्हें सत्य मान लिया जाता है। जैसे तर्कशास्त्र में विचार से नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वंश परम्परा का नियम परिणाम का नियम या समानुपात का नियम आदि। वैसे ही नीतिशास्त्र में भी कुछ मान्यताएँ है। नीतिशास्त्र की यही मान्यताएँ नैतिकता का आधार है। इन्हें बिना स्वीकार किये नैतिक जीवन की व्याख्या संभव नहीं है। काण्ट ने नैतिकता की तीन मान्यताओं को स्वीकार किया है –
- संकल्प की स्वतंत्रता,
- आत्मा को अमरता,
- ईश्वर का अस्तित्त्व |
संकल्प की स्वतंत्रता
काण्ट नैतिक जीवन के लिए संकल्प की स्वतंत्रता को अनिवार्य मान्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। काण्ट ने अपने नैतिक सूत्रों में यथा स्वतंत्रता के नियम, स्वयं साध्य के नियम और साध्यों के राज्य के नियम द्वारा सिद्ध करते हैं कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और मनुष्य नैतिक नियमों का निर्माता भी है और उसका पालन करने वाला भी है। नैतिक नियम के निर्माण और पालन में ऐसी कोई बाह्य शक्ति नहीं है जो मनुष्य को उसके लिए बाध्य करती है या कर सकती है। संकल्प की स्वतंत्रता की प्रामाणिकता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती। इसको केवल प्रागनुभविक रूप से ही सिद्ध किया जा सकता है। बौद्धिक प्राणी संकल्प की स्वतंत्रता को पूर्वमान्यता के अन्तर्गत ही कार्य कर सकता है। कहना यह चाहिए कि संकल्प की स्वतंत्रता और नैतिक नियम में अनिवार्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वतंत्रता नैतिकता का आधार है। यदि मनुष्य अपने कर्म के लिए स्वतंत्र न माना जाय तो उसे कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकता। साथ ही उसके कर्मों को उचित या अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। अत: संकल्प की स्वतंत्रता नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। संकल्प को स्वतंत्रता की अनिवार्यता इससे तो सिद्ध होती ही है, इसके अतिरिक्त काण्ट का यह कथन भी इसकी अनिवार्यता को ही सिद्ध करता है।
“तुम्हें करना चाहिए अतः तुम कर सकते हो।”
काण्ट के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को चाहे तो कर सकता है चाहे छोड़ सकता है। यहाँ‘चाहिए’ शब्द ही संकल्प की स्वतंत्रता को व्यक्त कर देता है। यदि मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता को न स्वीकार किया जाय तो ‘चाहिए’ शब्द का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता अर्थात् व्यक्ति का संकल्प स्वतंत्र है, चाहे तो यह कार्य कर सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। अन्यथा यह कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं सिद्ध होता कि तुम्हें करना चाहिए, अतः तुम कर सकते हो। यदि मनुष्य के दबाव में या इच्छाओं, वासनाओं के वशीभूत होकर ही कोई कार्य करता है तो ‘कर्त्तव्य’ और ‘चाहिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं सिद्ध होगा। इतना ही नहीं यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता तो प्रशंसा या निन्दा के लिए उत्तरदायी भी नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसीलिए काण्ट ने संकल्प को स्वतंत्रता को नैतिकता के लिए आवश्यक और अनिवार्य पूर्वमान्यता के रूप स्वीकार किया है। काण्ट की इस मान्यता के आधार पर संकल्प की स्वतंत्रता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है-
“मनुष्य के संकल्प का बाढ़ा शक्तियों से नियन्त्रित न होना ही संकल्प की स्वतंत्रता है।“
संकल्प मी स्वतंत्रता की यह नकारात्मक परिभाषा है। इसको स्वीकारात्मक परिभाषा भी दी जा सकती है। इसकी नकारात्मक परिभाषा से संतुष्ट नहीं हैं। स्वतंत्रता आदि नियम विहीन है तो कोई नहीं। अतः भावात्मक रूप से का संकल्प की स्वतंत्रता की परिभाषा इस प्रकार करते है –
“स्वतंत्र संकल्प वह संकल्प है जो सदैव आत्म-प्रेरित नियमों के अधीन रहकर कर्म करता है।”
काण्ट संकल्प को स्वतंत्र इसी अर्थ में मानते है कि बौद्धिक पाणी का संकल्प उन्हीं नियमों का पालन करता है जिन्हें वह अपने इस को अपने ऊपर आरोपित करता है। स्वतंत्र के किसी शक्ति द्वारा आरोपित नहीं किये आते।
काण्ट के संकल्प-स्वातन्त्रय के विरोध में नियन्त्रणाद एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके आधार पर इसके अस्तित्व को स्वीकार करना है। एक प्रश्न है। इस समस्या का हल करना यहाँ उद्देश्य नहीं है। हम इतना ही देखना चाहेंगे कि काष्ट की यह मान्यता नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है और उसी संकल्प की स्वतंत्रता की शक्ति के कारण ही मानव की गरिमा बनी हुई है। पशुजीवन में इस प्रकार की शक्ति नहीं है। इसीलिए मनुष्य का पशु-जीवन से अलगाव है। इतना ही नहीं, मात्र यही मानव-गौरव की अपूर्व शक्ति है।
सी० डी० ब्रॉड द्वारा आलोचना
काण्ट के संकल्प स्वातन्त्रय की सबसे अधिक कट आलोचना सी० डी० ब्रॉड ने की है। उनके अनुसार काण्ट अपने इस मत की स्थापना गम्भीर दार्शनिक तर्क के आधार पर नहीं करते। ब्रॉड के अनुसार मनुष्य के जीवन में इन दोनों तत्त्वों का जाता है। वास्तव में इन दोनों तत्त्वों को यथार्थ मानना चाहिए। काण्ट ‘पूर्ण शुभ संघर्ष भी देखा जाता संकल्प’ और ‘अपूर्ण शुभ संकल्प’ के विचार में इसकी झलक देते भी हैं। परन्तु नैतिकता की सिद्धि के लिए र और मानव को स्वतंत्र संकल्प की शक्ति को प्रमाणित करने के लिये भावात्मक पहल को भावावेग, त्याग दिया है।
ब्राड शब्दों में –
“स्पिनोजा की भाँति काण्ट प्रभावित हैं, जैसे कि मनुष्य । मनुष्य की द्विज भी प्रकृति से अत्यधिक , आवेग, सहज प्रवृत्ति और संवेदन का अंशत: एक विवेकशील प्राणी है। दोनों यह मानते हैं कि मानव प्रकृति का विवेकशील पक्ष अधिक मौलिक है। दोनों के बीच के संबंध की किसी ने सन्तोषजनक व्याख्या नहीं की। ब्रॉड आगे कहते हैं कि मानव की इस मिश्रित प्रकृति का उचित प्रस्तुतीकरण न हो सकने से काण्ट का स्वतंत्रता का सिद्धान्त तर्क रगत नहीं प्रतीत होता।”
ब्राड की उक्ति है कि –
“काण्ट के स्वतंत्रता अधिकांश सिद्धान्त द्विशृङ्गक के शुद्धों के बीच तेजो से झूलते हुए दीख पड़ते हैं और तीनतशा की कलाबाजी के अनिपुण खेल से मिलते-जुलते हैं, न कि सिर्फ गम्भीर दार्शनिक तर्क समान प्रतीत होते हैं।”
यहाँ ब्रॉड की यह आलोचना कुछ सीमा तक तो सत्य प्रतीत होती है किन्तु यह भी सत्य है कि संकल्प की स्वतंत्रता की मान्यता भी सत्य है। इसके अभाव में नैतिकता की बात ही नहीं की जा सकती। काण्ट ने इसी का प्रतिपादन किया है और उसे स्वीकार करना मानव के लिए अनिवार्य है। इसके अभाव में नैतिक जीवन की व्याख्या करना सम्भव ही नहीं है।
आत्मा की अमरता
नैतिक जीवन के लिए काण्ट की दूसरी पूर्वमान्यता आत्मा है। काण्ट के अनुसार नैतिक जीवन की पूर्णता के लिए आत्मा की अमरता आवश्यक है। नैतिक पूर्णता का अर्थ है सदैव शुभ संकल्प से कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य’ की भावना से प्रेरित होकर हो कर्म करना। अर्थात् व्यक्ति का नैतिक जीवन तभी पूर्ण माना जा सकता है जब वा कोई भी कार्य अनुचित रूप से। न करे। जब तक सक्ति में अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी तब तक वह नैतिक जीवन में पूर्ण नहीं। कहा जा सकता है तथा यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति विशुद्ध विवेकशील विशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है तथा नैतिक जीवन को पूर्ण बना सकता है। यही भावनाएँ और वासनाएँ ही मनुष्य को नैतिक कार्य से विचलित करती हैं। जब भी व्यक्ति इनसे प्रेरित होकर कर्म करता है, उसका कर्म अनैतिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में आना मनुष्य के लिए अत्यन्त कठिन कार्य है। नैतिक जीवन की पूर्णता की आकांक्षा करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। इसको प्राप्त करना संभव हो सकता है। काण्ट के अनुसार नैतिक पूर्णता समय सापेक्ष है इसकी पूर्ति में अपरिमित समय लग सकता है। मनुष्य नैतिक पूर्णता को एक ही जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिये अनेक जन्मों तक प्रयास करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब वह अनेक जीवन प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में उसकी आत्मा अमर है। बिना आत्मा को अमरता के यह सम्भव नहीं हो सकता। यही कारण है। कि काण्ट ने नैतिक जीवन की पूर्णता के लिये आत्मा की अमरता को पूर्वमान्यता के रूप में स्वीकार किया है।
ब्रॉड द्वारा आलोचना
बॉड ने दो आधारों पर काण्ट की आत्मा की अमरता सम्बन्धी पूर्वमान्यता का खण्डन किया है। एक तो काण्ट ने जिसे “नैतिक पूर्णता” कहा है, उसे यदि स्वीकार भी कर लिया गया तो मी आत्मा की अमरता को स्वीकार आवश्यक नहीं है। दूसरे आत्मा की अमरता के पक्ष में जो तर्क काण्ट द्वारा दिये गये हैं वह विरोधपूर्ण है। ब्रांड के अनुसार दोनों आलोचनाएँ इस प्रकार है –
- हमें अपने आपको पूर्ण बनाने के आदेश को अक्षरशः उसी रूप में नहीं समझना चाहिए। यह कहने की केवल आलंकारिक प्रणाली है- ‘नैतिक उपलब्धि के अपने वर्तमान स्तर से कभी भी सन्तुष्ट नहीं रहा। निस्सन्देह जब तक हम जीवित है, हम अपने नैतिक चरित्र को समुद्रत कर सकते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम कभी उसे पूर्ण बनाने में भी समर्थ हो सकते हैं।
- काण्ट के कथन में विरोध है। एक ओर तो वह कहते हैं कि नैतिकपूर्ण प्राप्य होनी चाहिये, अन्यथा इसके हेतु साधना करना हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि ‘अन्तकाल के उपरान्त ही यह प्राप्य है।’ ब्रॉड के अनुसार काण्ट का यह कथन निश्चित ही इसके तुल्य है कि यह प्राप्य है ही नहीं। इस प्रकार ब्रॉड काण्ट की अमरता की धारणा का खण्डन करते हैं।
ब्रॉड के तर्कों का निराकरण
यदि मनुष्य के अन्तर्निहित पूर्णता के विचार आज्ञा शतत् प्रयास और आध्यात्मिक प्रेरणा तथा जीवन की नवीनता की सम्भावना को स्वीकार करते हैं तो काण्ट के तर्कों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि मनुष्य का ‘पूर्णता का विचार’ सामान्य दैनिक जीवन में क्रियाशील रहता है और लक्ष्य की प्राप्ति कर सन्तोष प्रकट करता है तो नैतिक जीवन की पूर्णता को केवल आलंकारिक कथन मात्र ही मान कर क्यों छोड़ दिया जाय? इसके लिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करने में जीवन में आशा का संचार होता है। बुराइयों के निवारण का अवसर मिलता है। जीवन में किये गये कार्यों का इसीलिए महत्त्व है। दूसरी ओर नैतिक पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए और इसके लिए अनन्त काल की कामना को असंभावना में परिणत कर दिया है। मनुष्य को इस बात की आशा है कि अनन्त काल के प्रवाह में कोई समय तो आयेगा जब पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। उसे असंभव क्यों समझा जाय? यहाँ ब्रॉड निश्चित रूप से काण्ट की आलोचना कठोरवादी और हठवादी दृष्टि से करते हैं। यदि मनुष्य भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक तत्त्वों से भी निर्मित है तो आत्मा की अमरता में विश्वास करना होगा।
ईश्वर का अस्तित्त्व
काण्ट के नैतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निपेक्षवादी है। काण्ट नैतिकता को किसी बाह्य से आरोपित नहीं मानते। यहाँ तक कि ईश्वर जैसी सत्ता भी नैतिकता का न तो निर्माण कर सकती है और न ही उसके भय से किया गया कार्य नैतिक कहा जा सकता है। इतना होते हुए भी काण्ट ने नैतिक जीवन की पूर्व मान्यता के रूप में ईश्वर के अस्तित्त्व को स्वीकार किया है। इस मान्यता का मूल कारण है कर्तव्य तथा आनन्द में सामंजस्य तथा न्यायकर्त्ता की समस्या इस विषय में काण्ट तर्क देते हैं कि जीवन में प्राय: यह देखा जाता है कि बहुत ही कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, जो ‘कर्तव्य के लिए कर्तव्य’ की भावना से कर्म करता है, आनन्द से वंचित रह जाता है, इसके विपरीत जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है वह जीवन में सुखी दिखलाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमय तथा न्यायी व्यक्ति को आवश्यकता है जो कर्त्तपरायण व्यक्ति को आनन्द प्रदान कर सके तथा अनाचार करने वाले व्यक्ति को दुःख दे सके। निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति मानव के बीच में होना सम्भव नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्तिशाली सत्ता ईश्वर ही है जो अनाचारी को दुःख तथा सदाचारी को आनन्द दे सके। कर्तव्यों के अनुसार निष्पक्ष रूप से न्याय करके आनन्द और दुःख का बँटवारा करना मनुष्य का काम नहीं ईश्वर का ही कार्य हो सकता है। अतः नैतिक जीवन के लिए ईश्वर का अस्तित्त्व स्वीकार करना आवश्यक है। बिना ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किये ‘पूर्ण शुभ’ के प्रत्यय को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पूर्णमंगल की कामना ईश्वर से ही रित होगी। पूर्णमंगल में कर्त्तव्य और आनन्द का समन्वय रहता है। यह ईश्वर पर ही आधारित है। अतः ईश्वर नैतिक जीवन के लिए अनिवार्य मान्यता है।
ईश्वर के अस्तित्त्ववाद की आलोचना-ईश्वर के अस्तित्व की आलोचना निम्नलिखित रूप में की गई है –
- काण्ट की ईश्वर सम्बन्धी पूर्व मान्यता की यह कहकर आलोचना की जाती है कि जहाँ एक और काण्ट नैतिकता के लिए संकल्प की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं किसी बाह्य दबाव को स्वीकार नहीं करते, वहीं दूसरी ओर ईश्वर की सत्ता ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके अप्रत्यक्ष रूप में धार्मिकता को नैतिकता के लिए आवश्यक मानते हैं। इस मान्यता से काष्ट का नैतिक सिद्धान्त विशुद्ध रूप से नहीं रह जाता ईश्वर और आत्मा आस्था के विर है। क्या इनकी मान्यता से नैतिकता को धार्मिक आस्था का विषय नहीं कहा जा सकता? क्या धार्मिकता के प्रभाव में नैतिकता में पाये जाने वाले सामान्य तत्त्व सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता, स्वयंसाध्यता और निरपेक्षता समाप्त नहीं हो जाते?
- इस सम्बन्ध में ब्रॉड की यह आलोचना है कि काण्ट को कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को आनन्द देने के लिए एक ईश्वर की आवश्यकता है। प्रश्न यह होता है कि एक नीतिपरायण व्यक्ति जो नैतिक पूर्णता प्राप्त कर चुका है और अपनी इच्छाओं, वासनाओं को नष्ट कर चुका है, फिर उसे आनन्द का अनुभव कैसे होगा? इतना ही नहीं नैतिक पूर्णता को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए आनन्द का महत्व ही क्या है? अतः दोनों ही रूपों में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ब्रॉड के शब्दों में –
“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तर्क में काण्ट की स्थिति में और अमरता के उसके तर्क की स्थिति में कुछ असंगति है। उपर्युक्त में यह माना गया है कि में नैतिक रूप से हम तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक हम अपनी प्रकृति के निष्क्रिय, एन्द्रिय और संवेगात्मक पक्ष से पूर्णरूप से मुक्त नहीं हो जाते हैं। ईश्वर सम्बन्धी तक के विषय में यह मान लिया गया है कि वह आनन्द, जो परमहित का एक अनिवार्य अंग है, सद्गुण की मात्र चेतना नहीं, किन्तु सद्गुण के पुरस्कार स्वरूप इसमें कुछ और जोड़ दिया गया है। परन्तु इस आनन्द का हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, यदि हममें संवेदन और संवेग हो नहीं रह जाता?”
उपर्युक्त आलोचनाओं के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि काण्ट ने ईश्वर की मान्यता व्यक्ति में नैतिक जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए स्वीकार किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह जगत् अनियन्त्रित रूप से चाहे अंधेरे में नहीं भटक रहा है। मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर के अभाव में निरर्थक सिद्ध होगा। ईश्वर की सत्ता स्वतः में एक आश्वासन है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सुखवाद क्या है?
- काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त
- काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना
- काण्ट के ‘कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य सिद्धान्त’ की पूर्ण व्याख्या
- एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में अन्तः प्रज्ञावाद का मूल्यांकन
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या हैं ?
प्रत्येक विज्ञान की कुछ मान्यताएं होती है। इसे स्वयं सिद्धियों भी कहते हैं। ये मान्यताएँ ऐसी होती है जिन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता, मान लिया जाता है। इन्हें किसी प्रमाण से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मान्यताएँ आधार या नींव का काम करती हैं।
ईश्वर का अस्तित्त्व क्या है ?
काण्ट के नैतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निपेक्षवादी है। काण्ट नैतिकता को किसी बाह्य से आरोपित नहीं मानते। यहाँ तक कि ईश्वर जैसी सत्ता भी नैतिकता का न तो निर्माण कर सकती है और न ही उसके भय से किया गया कार्य नैतिक कहा जा सकता है।


सुखवाद क्या है?


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सुखवाद क्या है? उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
सुखवाद का अर्थ
सुखवाद को अंग्रेजी भाषा में ‘हीडनिज्म’ (Hedonism) कहा जाता है। ‘हीडनिज्म’ यूनानी शब्द हीडन (Hedone) से बना है। होडन का अर्थ है सुखा अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि वह मत जो सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता है, सुखवाद कहलाता है। सुखवाद नैतिक जीवन के क्षेत्र में एक मापदण्ड के रूप में प्रचलित है। कुछ दार्शनिकों ने जीवन के अन्तिम उद्देश्य को ही नैतिकता का चरम मापदण्ड स्वीकार किया है। उनके मत को प्रयोजनवाद कहा जाता है। प्रयोजनवाद यह मानता है कि मनुष्य के कर्मों का औचित्य- अनौचित्य उसके जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति पर ही निर्भर है। यह प्रश्न विवादास्पद है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कुछ लोग सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं और कुछ लोग आत्मपूर्णता को सुखवादी मानव जीवन का चरम लक्ष्य सुख की प्राप्ति को ही मानते हैं। जीवन का प्रयोजन सुख को प्राप्त करना है। अतः इस मापदण्ड के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि जो कम सुख की प्राप्ति में सहायक होता है, वह नैतिक, शुभ या उचित है और जो इसकी प्राप्ति में बाधा डालता है वह अनैतिक, अशुभ या अनुचित है। अतः सुखवाद नैतिक मापदण्ड के रूप में वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है। जो कर्म सुख की प्राप्ति में सहायक होता है वह शुभ होता है और जो बाधक सिद्ध होता है, वह अशुभ कहलाता है।
मनोवैज्ञानिक सुखवाद
मनोवैज्ञानिक सुखवाद, सुखवाद का यह रूप है, जिसके अनुसार मनुष्य स्वभाववश सदैव सुख की इच्छा करता है। इसके अनुसार सुख हो मनुष्य के कर्मों का प्रेरक तत्त्व है। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना ही इस प्रकार है कि वह स्वभाव से हो सुख को इच्छा करता है। यही सुख की भावना मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सुख ही कर्म का विषय है। इच्छाओं की तृप्ति सुख है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुख ही मनुष्य के कर्मों का प्रेरक विषय तथा फल है। जिस प्रकार मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है, उसी प्रकार वह सदैव दुःख से पीछा भी छुड़ाता है। उसका प्रयत्न रहता है कि सदैव दुःख से बचें और सुख की प्राप्ति करें मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव उसी वस्तु की इच्छा करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो वस्तु की इच्छा वस्तु के लिए नहीं होती बल्कि उस वस्तु से मिलने वाले सुख के लिए होती है। वस्तु सुख का साधन है। हम धन की इच्छा इसलिए करते हैं कि उससे सुख प्राप्त होगा। धन सुख का साधन है। अतः इच्छा का स्वाभाविक विषय सुख है।
अपवाद
मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की ही खोज करता है-मनोवैज्ञानिक सुखवाद का यह सिद्धान्त किसी अपवाद से असत्य नहीं सिद्ध होता जैसे कंजूस का रूपए के लिए प्रेम (रुपया सुख का साधन है। सुख साध्य है परन्तु कभी-कभी साधन तथा साध्य इस तरह घुले-मिले रहते हैं कि व्यक्ति साध्य को भूलकर साधन में ही लग जाता है। जैसे कंजूस का रुपए के लिए प्रेम प्रारम्भ में तो व्यक्ति सुख के लिए ही रुपए को चाहता है, परन्तु बाद में व्यक्ति रुपए के लिए रुपया चाहने लगता है। केजूस को रुपया रखने में ही सुख मिलता है। ऐसी स्थिति मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार अपवाद की स्थिति है। कुछ ही उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें व्यक्ति रुपए को रखने के लिए रुपया चाहता है। सामान्यतः तो व्यक्ति सुख के लिए ही रुपया चाहता है। अतः इस अपवाद को इस सिद्धान्त में स्थान नहीं है। वास्तव में वस्तु की प्राप्ति साधन है और सुख की प्राप्ति साध्य है। सारांश में मनोवैज्ञानिक सुखवाद के निम्नलिखित मत हैं –
- इच्छा का अन्तिम विषय सुख है। सुख ही मनुष्य के कर्म का प्रेरक है।
- मनुष्य सदैव सुख की खोज करता है और दुःख का त्याग कर्म का विषय सुख है।
- प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की कामना सुख की प्राप्ति के लिए करता है।
- सुख साध्य है, वस्तु साधन साधन की कामना अपवाद की स्थिति है।
मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज करता है। इच्छा की तृप्ति सुख है।
मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना
मनोवैज्ञानिक सुखवाद के सिद्धान्त की निम्नलिखित रूप से आलोचना की गई है –
सभी कर्मों का प्रेरक सुख नहीं है
मनोवैज्ञानिक सुखवादी मनुष्य के कर्मों का प्रेरक सुख को मानते हैं। सुख प्रेरक के रूप में तीन प्रकार से हो सकता है एक तो मनुष्य वही कर्म करता है जिससे उसको वर्तमान काल में अधिक से अधिक सुख हो, दूसरे मनुष्य वही कर्म करता है जिससे भविष्य में सुख मिले। तीसरे मनुष्य वही कर्म करता है जिससे समग्र जीवन का सबसे अधिक सुख मिलें। यदि इन तीनों स्थितियों की छानबीन की जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धान्त सत्य नहीं सिद्ध होता।
मनोवैज्ञानिक सुखवाद अमनोवैज्ञानिक है
मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार हम सदैव सुख की इच्छा करते हैं परन्तु जब इसका विश्लेषण किया जाय तो पता चलता है कि मनुष्य सामान्य रूप से पहले किसी वस्तु की इच्छा करता है और जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तब उसे सुख की अनुभूति होती है। मनोवैज्ञानिक क्रम से यदि देखा जाय तो पहले
- किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति होती है,
- तब उस वस्तु की इच्छा होती है जिससे अभाव मिटेगा,
- फिर वस्तु की प्राप्ति होती है,
- अन्त में वस्तु-प्राप्ति के पश्चात् सुखानुभूति होती है।
उदाहरण के लिए भूखे रहने पर हम भोजन की इच्छा करते हैं, भोजन प्राप्त होने पर ही सुख की अनुभूति होती है। क्या भूख लगने पर सुखानुभूति की इच्छा करते हैं या भोजन की? निश्चित है कि हम भोजन की ही इच्छा करते हैं परन्तु मनोवैज्ञानिक सुखवाद इससे विपरीत विचार करता है, जो मानसिक क्रिया के क्रम के अनुकूल सिद्ध नहीं होता। इसके अनुसार तो हम पहले सुख की इच्छा करते हैं इसके बाद वस्तु को पाने की इच्छा करते हैं। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह मत गलत सिद्ध होता है। इसीलिए यह अमनोवैज्ञानिक है।
सुखवाद का विरोधाभास
मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खण्डन करने के लिए सिजविक ने इसके बहुत बड़े दोष की ओर ध्यान दिलाया है। वह है सुखवाद का विरोधाभास मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार हम सदैव सुख की इच्छा करते हैं। सिजविक का कथन है कि –
“अगर हम सुख की इच्छा करें भी तो उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका प्रायः उसे भूल जाना होता है। यदि हम स्वयं सुख की ही बात सोचते रहें, तो यह निश्चित-सा है कि हम उसे नहीं पा सकेंगें, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को बाहरी साध्यों की ओर लगाए रखें तो सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाता है।”
सिजविक ने खेल तथा खिलाड़ी का उदाहरण देते हुये अपने मत को और भी स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि एक खिलाड़ी को अपने खेल में तभी सुख प्राप्त होता है जब वह सुख की ओर ध्यान न देकर अपने खेल में तल्लीन रहता है। यदि खिलाड़ी खेल से मिलने वाले सुख के विषय में ही सोचता रहे तो निश्चित है कि उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह आगे कहते हैं पूरा आनन्द लेने के लिए उपेक्षा का भाव भी कुछ मात्रा में जरूरी लगता है। जो आदमी खेल के दौरान में बराबर सुखान्वेषी को मनोवृत्ति रखता है, अर्थात् सुख पर ही ध्यान जमाए रखता है, वह खेल की भावना को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। उसकी व्यग्रता उत्तेजना की उस राकाष्ठा पर नहीं पहुँच पाती जो सुख को अधिकतम रस प्रदान करती है। यहाँ एक बात दिखाई देती है जिसे हम सुखवाद का आधारभूत विरोधाभास कह सकते हैं और यह है कि सुख की और हमारी वृत्ति का बहुत ही एकमुखी होना स्वयं अपने लिए घातक होता है। सिजविक के इन कथनों का यही तात्पर्य है कि जितना हम सुख के पीछे दौड़ेंगे वह उतना ही हमसे दूर निकलता जाएगा। सुख प्राप्त करने की चेतना जितनी ही तीव्र होगी, सुखानुभूति उतनी ही कम होगी। यदि हम कोई नाटक या सिनेमा देखने जाँय तो जाते ही वहाँ सुख को ढूँढ़ने लगें तो सुख कहाँ मिलेगा? नाटक या सिनेमा का सुख पाने के लिए सिनेमा को देखना होगा, तभी सुख को अतः सिद्ध है कि सुख पाने के लिए हमें उस वस्तु की ओर ध्यान देना होगा प्राप्ति होगी। जिससे सुख की प्राप्ति होती है, न कि सुख पर यही सुखवाद का विरोधाभास है।
कर्म का विषय सुख नहीं वस्तु है
मनोवैज्ञानिक निक सुखवाद मानता है कि मनुष्य के प्रत्येक कम का विषय सुख है, परन्तु उसका यह मत उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इतना तो बहुत स्पष्ट है कि किसी कर्म का विषय कोई वस्तु होती है न कि सुख है। हाँ वस्तु की प्राप्ति से सुख अवश्य होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म का लक्ष्य सुख नहीं होता। सुख तो वस्तु-प्राप्ति का परिणाम होता है। अतः कर्म का विषय सुख नहीं है।
सुख इच्छा का साध्य (End) नहीं अन्त (End) है
मनोवैज्ञानिक सुखवाद यह मानता है कि इच्छा की तृप्ति सुख है। अर्थात् सुख इच्छा की तृप्ति का परिणाम है। प्रत्येक इच्छा का अन्त या परिणाम सुख होता है, यहाँ तक कहना तो ठीक है, परन्तु मनोवैज्ञानिक सुखवाद यह भी कहता है कि सुख इच्छा का साध्य (end) है। इच्छा का साध्य सुख नहीं वरन् वस्तु तू की प्राप्ति है। वस्तु मिलने पर सुख की अनुभूति होती है। अतः कहना चाहिये कि सुख इच्छा का साध्य नहीं बल्कि अन्त (end) है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद गलती से इच्छा के साध्य और इच्छा के अन्त को एक ही मान लेता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में साध्य और अन्त दोनों के लिए एक ही शब्द ‘एण्ड’ (End) का प्रयोग होता है।
मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद के लिए घातक सिद्ध होता है
मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव स्वभाववश सुख की इच्छा करता है। नैतिक सुखवाद की मान्यता है कि मनुष्य को सुख प्राप्त करना चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि जब हम सदैव स्वभाववश सुख की ही इच्छा करते हैं तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि हमें ‘सुख प्राप्त करना चाहिए।’ सिद्ध है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद को गलत सिद्ध कर देता है। नैतिक सुखवाद के लिए यह घातक है। इसका नैतिक सुखवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।
क्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का आधार कहा जा सकता है?
यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखबाद के लिए घातक सिद्ध होता है, तथा बैडले के अनुसार यह अनैतिक सिद्धान्त है, जिसे हमारी सामान्य व्यवहारिक नैतिक बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती, तो फिर एक एकांगी और अपूर्ण सिद्धान्त नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता। इन दोनों में कोई तार्किक सम्बन्ध नहीं है। जब मनुष्य सदैव सुख की इच्छा स्वभाववश करता है तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि ‘सुख प्राप्त करना चाहिए’ परन्तु सुखवाद के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि मिल तथा बेन्थम एक ओर मनोवैज्ञानिक वादको मानते हैं और दूसरी और नैतिक सुखवाद का भी प्रचार करते हैं।
यह सत्य है कि सुखवादी मनोवैज्ञानिक सुखवाद को भी स्वीकार करते हैं परन्तु हुन दोनों में तार्किकता की दृष्टि से सामंजस्य सम्भव नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि क्या इन दोनों में सामंजस्य सम्भव है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाय तो सामंजस्य सम्भव है। अर्थात् मनोवैज्ञानिक सुखवाद का यह अर्थ होना चाहिए कि हम किसी प्रकार के सूख’ (Pleasure of Some Sorr) की खोज करते हैं, और नैतिक सुखवाद के अनुसार यह कि हमें अपने अधिकतम सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। इसी तरह मनोवैज्ञानिक दूसरों के सुखवाद और नैतिक परार्थमूलक सुखवाद में सामंजस्य किया जा सकता है कि सुखम हमें अपने सुख की प्राप्ति हो। नैतिक सुखवादी जब अपना सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित करते हैं तब उनका यह मतलब होता है कि जब मनुष्य स्वभाववश सुख को ही इच्छा करता है तो उसे अपने अथवा सामान्य के अधिकतम सुख की इच्छा करनी चाहिए। अर्थ में परिवर्तन कर देने पर भी कुछ विचारक जैसे सिजविक यह मानने को तैयार नहीं है कि दोनों में सामंजस्य सम्भव हो सकता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त
- काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना
- काण्ट के ‘कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य सिद्धान्त’ की पूर्ण व्याख्या
- एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में अन्तः प्रज्ञावाद का मूल्यांकन
- बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की व्याख्या | Animism explanation of buddhist philosophy |
सुखवाद का अर्थ क्या है ?
मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद के लिए घातक सिद्ध होता है क्यों ?
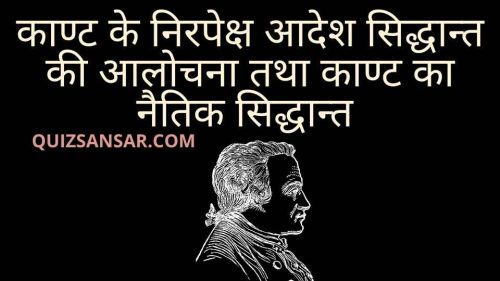
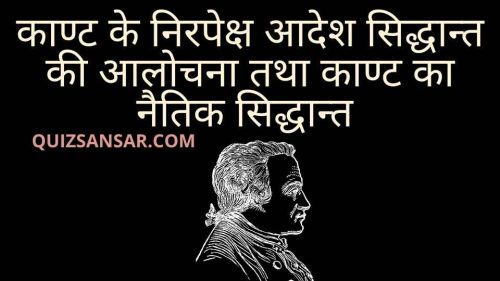
काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त
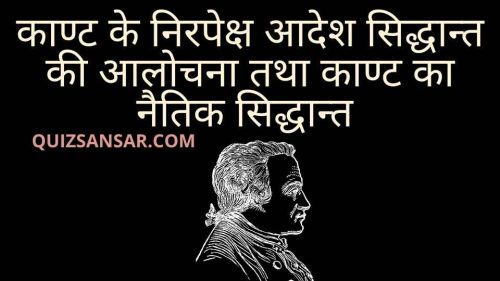
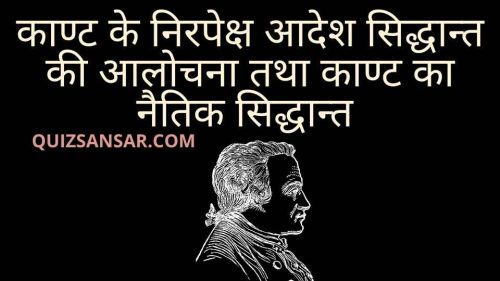
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है काण्ट के निरपेक्ष आदेश सिद्धान्त की आलोचना तथा काण्ट का नैतिक सिद्धान्त उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
काण्ट का नैतिक सिद्धान्त (अहैतुक आदेश)
काण्ट ने देखा कि केवल “कर्त्तव्य के लिये कर्तव्य” के निरपेक्ष आदेश में जीवन से व्यावहारिक आचरण के लिये समुचित निर्देश नहीं मिलता। नैतिक नियम आकार मात्र है, उनके करने के लिये उनको व्यवहार में उतारने के लिये व्यावहारिक नियमों की आवश्यकता है। अतः काण्ट ने तीन न व्यावहारिक सूत्र उपस्थित किये जिन्हें अहेतुक आदेश के नाम से जाना जाता है।
पहला नैतिक सूत्र
“सदा उस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करो और केवल उसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करो जिससे तुम सार्वभौम नियम बन जाने की इच्छा कर सको।”
इस वाक्य को समझने के लिये काण्ट शपथ तोड़ने का उदाहरण देते हैं। यदि शपथ तोड़ने का कोई सार्वभौम हो जाये अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति शपथ तोड़ने लगे तो शपथ लेने का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। इसी प्रकार अत्यन्त निराश होने पर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच सकता है। परन्तु यह इसलिये अनुचित है कि वह सार्वभौम नियम नहीं बन सकता। यदि सभी मनुष्य आत्महत्या करने लगेंगे तो शीघ्र ही कोई भी मनुष्य आत्महत्या करने के लिये नहीं बचेगा।
काण्ट के इस प्रश्न सूत्र की आलोचना में निम्नलिखित बातें कहीं जा सकती हैं –
इस सिद्धान्त से निश्चित नैतिक नियम नहीं निकलते
इस सिद्धान्त के द्वारा काण्ट नैतिक नियम को एक निश्चित स्वरूप देना चाहता था परन्तु इससे यह काम नहीं बनता। किसी की नैतिकता उसकी परिस्थिति पर निर्भर रहती है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, अत: यह कैसे कहा जा सकता है कि मैं एक परिस्थिति में जो कुछ कहता हूँ वह सभी को करना चाहिये।
पहला नैतिक सूत्र
यह नियम अपवाद को कोई स्थान नहीं देता और इस कारण कठोरतावादी बन जाता है। जैसा कि जैकोबी ने कहा था –
“नियम मनुष्य के लिये बनते हैं, मनुष्य नियम के लिये नहीं बनते।”
कभी-कभी अपवाद भी नियम होते हैं
काण्ट यह भूल जाता है कि कभी-कभी अपवाद ही सर्वश्रेष्ठ नियम होते हैं। यदि किसी देश के सब के सब नागरिक शहीद हो जायें तो फिर देश ही कहाँ रहेगा। शहीदों की श्रेष्ठता इसी बात में है कि सभी शहीद नहीं बन सकते।
अव्यावहारिक
इस सूत्र की विशेषता यह है कि वह नीतिशास्त्र के सामाजिक पक्ष पर जोर देता है, परन्तु नियमवादी होने के कारण यह अव्यावहारिक बन जाता है।
दूसरा नैतिक सूत्र
काण्ट का दूसरा नैतिक सूत्र इस प्रकार है –
“इस प्रकार कार्य करो कि मानवता की चाहे वह तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में हो अथवा किसी दूसरे व्यक्तित्व में सदैव साध्य के रूप में प्रयोग करो, साधन के रूप में नहीं।”
इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। आत्महत्या करना इसलिये बुरा है क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी अन्तस्य मानवता का समुचित आदर नहीं करता और स्वर्ग को सुखभोग का एक साधन मात्र बनाता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को अपना शोषण करने दे। झूठ बोलना इसलिये युरा है, क्योंकि ऐसा करके झूठ बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है और उसे अपने स्वार्थ के साधन के ऊपर है-इस रूप में प्रयोग करता है। हमें अपने और दूसरों के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिये।
अतः उपरोक्त सूत्र से काण्ट एक उपनियम निकलता है –
“सदैव अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करो और अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करके दूसरे को सुखी बनाने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम दूसरों को पूर्ण नहीं बना सकते।”
पूर्णता प्राप्ति के हेतु संकल्प शक्ति और संयम की आवश्यकता है और कोई भी मनुष्य दूसरे को संयमित नहीं कर सकता। अतः वह पूर्ण भी नहीं बन सकता। वह केवल ऐसी परिस्थितियाँ जुटा सकता है जिससे उनका आनन्द बढ़े।
अपने और दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान करने की शिक्षा देने के कारण काण्ट का यह सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार कभी-कभी व्यक्तियों को अन्य जनों के लिये साधन रूप में प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिये प्लेग के अथवा अन्य संक्रामक रोग के रोगियों को नगर के बाहर अन्य लोगों से दूर रखना पड़ता है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिये साधन रूप में प्रयोग किया जाता है, परन्तु इसको कोई भी अनैतिक नहीं कह सकता।
वास्तव में मनुष्य को साधन के रूप में प्रयोग करने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सभी आत्म-लाभ की और उन्मुख हों और किसी के आत्म-लाभ में बाघा न पड़े। परन्तु यह आत्म लाभ कभी-कभी बलिदान ही अधिक सहायक होता है। अतः यह नियम नहीं बन सकता कि अपने को या दूसरे को साधन रूप में प्रयोग करना सदैव अनैतिक है। इस नियम का उपनियम पूर्णतावाद का समर्थन करता है, परन्तु यह समझना कठिन है कि संवदेनशीलता के अभाव में व्यक्ति किस प्रकार पूर्ण हो सकता है। इसी प्रकार यह समझ में नहीं आता कि जब व्यक्तियों में संवेगशीलता ही अवाछनीय हो तब उनके आनन्द को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।
तीसरा नैतिक सूत्र
काण्ट का तीसरा नैतिक सूत्र इस प्रकार है-एक साध्यों के राज्य के एक सदस्य के में काम करो। इसका अर्थ है, इस प्रकार कार्य करो कि स्वर्ग को और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को आंतरिक मूल्य वाला समझ कर व्यवहार करो, एक ऐसे समाज सदस्य के रूप व्यवहार करो जिसमें कि प्रत्येक दूसरे के शुभ को अपने में की समझता हो और उसके साथ बाकी लोग भी इसी प्रकार करें, व्यवहार सम्पन्न मूल्य जिसमें कि प्रत्येक साध्य और साधन दोनों हों जिसमें कि दूसरे के शुभ की वृद्धि करते हुये प्रत्येक अपना शुभ प्राप्त करे। इस प्रकार काण्ट एक ऐसे साध्यों के राज्य की स्थापना करता है जो कि आदर्श समाज है और सभी सदस्य नैतिक नियम का पालन करते हैं। उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वशासित है और स्वयं ही अपने ऊपर नैतिक नियम को लागू करता है, जो कि उसका आन्तरिक बौद्धिक नियम है। बौद्धिक नियम सार्वभौम है नैतिक नियम न तो वाह्य नियम है और न देवी आदेश है। वह आत्म आरोपित है। उसका पालन किसी बाहरी दबाव पर आधारित नहीं है। इस प्रकार पूरे समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र, बुद्धिपरक और सुखी होंगे।
इस प्रकार काण्ट सद्गुण और आनन्द का सामंजस्य आवश्यक मानता है। यह नैतिकता को किसी श्रद्धा की वस्तु नहीं बनाता है और यदि उसका कुछ आन्तरिक मूल्य भी हो तो एक ऐसे समाज के अस्तित्त्व की कल्पना करनी ही पड़ेगी जिनमें सद्गुण और आनन्द का सामंजस्य हो। सभी नैतिक नियम कर्मों के सच्चे प्रेरक बन सकते हैं। नैतिक शुभ का लक्ष्य परम-शुभ है। नैतिक शुभ की “कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य” करना ही है। उसे पूर्ण तटस्थता की आवश्यकता है। उसका आनन्द से कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु शुभ में सद्गुण और आनन्द दोनों ही है। यद्यपि काण्ट यह मानता है कि वह इस एक जीवन में सम्भव नहीं है, परन्तु अन्ततोगत्त्वा नैतिक शुभ परम-शुभ को अवश्य प्राप्त करता है। यह विश्वास नैतिकता का आधार है।
काण्ट के तृतीय नैतिक सूत्र की आलोचना में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं –
बुद्धि और संवेगशीलता में मनोवैज्ञानिक द्वैत
काण्ट के नैतिकता के सिद्धान्त में बुद्धि और संवेगशीलता मनोवैज्ञानिक द्वैत की कल्पना पर आधारित है। वह इन दोनों को परस्पर विरोधी मानता है। वह इस तथ्य को भूल जाता है कि ये दोनों ही आत्मा के अभिन्न अंग हैं।
आकार मात्र
अतः संवेगशीलता की अनुपस्थिति में काण्ट के नीति वाक्य आकार मात्र है। काण्ट का तृतीय नीति सूत्र भी आकार मात्र है। हमको एक साध्य के राज्य के नागरिक के समान सभी को साध्य रूप में प्रयोग करना चाहिये साधन रूप में नहीं ? हमें किस प्रकार उसकी चेष्ठा करनी चाहिये ? इस विषय में इस सूत्र से कुछ भी पता नहीं चलता।
संवेगशीलता के अभाव में आनन्द सम्भव नहीं
काण्ट ने आनन्द में सुख को भी सम्मिलित किया है, परन्तु यदि आनन्द में सुख भी हो तो इच्छाओं के दमन के पश्चात् कैसे सम्भव है और फिर कैसे ईश्वर नैतिक व्यक्ति को आनन्द देता है तथा कैसे पूर्ण शुभ में गुण के साथ आनन्द की भी कल्पना की जा सकती है ?
एकांगी नैतिक सिद्धान्त
काण्ट का विशुद्ध नैतिकतावाद एकांगी है। वह सम्पूर्ण परिस्थिति के नैतिक मूल्य को भूल जाता है। परन्तु परिणाम की सर्वथा उपेक्षा करके कर्तव्य पालन केवल सत्यासंवाद ही नहीं, बल्कि अनुचित भी हो सकता है। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी निर्दोष से के प्राण बचते हों तो उस व्यवस्था में सत्य बोलकर उसके प्राणों से खेलना कैसे नैतिक हो सकता है ? कर्म स्वयं ही नैतिक नहीं हो सकता। उसमें प्रेरणा और परिणाम दोनों का ही महत्त्व है।
काण्ट को कठोरतावादी क्यों माना जाता है
काण्ट के नीतिशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता कठोरतावादी है। यह कठोरतावाद दो प्रकार का है एक तो काण्ट नैतिक जीवन में भावना को कोई स्थान नहीं देना चाहता। दूसरे काण्ट नैतिक नियम में कोई भी अपवाद स्वीकार नहीं करता। काण्ट के अनुसार भावना से प्रेरित प्रत्येक कार्य अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति किसी के दुःख से दुःखी होता है या रोता है तो वह सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि ऐसा करके वह संसार के दु:ख के बोझ को और भी बढ़ाता है। उसे तो यह चाहिये कि वह दूसरों का दुःख दूर करे, न कि उनके दुख में दुःखी हो। काण्ट के अनुसार कार्य शुद्ध कर्त्तव्य को प्रेरणा से किया जाना चाहिये। उसके अलावा किसी भी भावना से किया कार्य, चाहे वह भावना कितनी भी ऊँची क्यों न हो, सवर्चा अनैतिक होगा। काण्ट का तात्पर्य यह नहीं था कि कर्तव्य कहना था कि कार्य के साथ किसी भी भावना का होना बुरा है, उसका केवल यही को प्रेरणा भावना नहीं बल्कि बुद्धि होनी चाहिये। अतः यह मत किसी प्रकार की निर्बुद्धि हठवाद नहीं है बल्कि बौद्धिक कठोरतावाद है। वास्तविक जीवन में दूसरों के दुःख से दुःखो व्यक्तियों को बुरा नहीं कहा जाता, भावना मनुष्य की दुर्बलता है परन्तु उसकी भावना से मनुष्य, मनुष्य है अन्यथा वह देवता या पशु होता। जब तक मनुष्य इनमें से कोई नहीं हो जाता, नैतिक जीवन में भावना का मूल्य मानना ही होगा क्योंकि नैतिक स्तर पशु पापाण अथवा देवता का स्तर न होकर मानव का ही स्तर है। काण्ट के कठोरतावाद का दूसरा प्रकार नियमों के अपवाद न मानना है क्योंकि कभी-कभी अपवाद नियम से बेहतर होते हैं और फिर आखिरकार नियम भी तो मनुष्य के लिये ही बनाये जाते हैं।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना
- काण्ट के ‘कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य सिद्धान्त’ की पूर्ण व्याख्या
- एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में अन्तः प्रज्ञावाद का मूल्यांकन
- बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की व्याख्या | Animism explanation of buddhist philosophy |
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
संवेगशीलता के अभाव में आनन्द सम्भव नहीं है क्यों ?
काण्ट ने आनन्द में सुख को भी सम्मिलित किया है, परन्तु यदि आनन्द में सुख भी हो तो इच्छाओं के दमन के पश्चात् कैसे सम्भव है और फिर कैसे ईश्वर नैतिक व्यक्ति को आनन्द देता है तथा कैसे पूर्ण शुभ में गुण के साथ आनन्द की भी कल्पना की जा सकती है ?
बुद्धि और संवेगशीलता में मनोवैज्ञानिक द्वैत क्या हैं ?
काण्ट के नैतिकता के सिद्धान्त में बुद्धि और संवेगशीलता मनोवैज्ञानिक द्वैत की कल्पना पर आधारित है। वह इन दोनों को परस्पर विरोधी मानता है। वह इस तथ्य को भूल जाता है कि ये दोनों ही आत्मा के अभिन्न अंग हैं।


काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है काण्ट के सदेच्छा सिद्धान्त की आलोचना उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
शुभ संकल्प या सदेच्छा
अपने नैतिक दर्शन में काण्ट ने सर्वप्रथम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है कि ऐसी कौन-सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है और जिसका शुभत्त्व देश, काल, परिस्थितियों तथा मनुष्य की भावनाओं अथवा इच्छाओं पर निर्भर नहीं है अर्थात् जो सर्वत्र एवं सर्वदा निरपेक्ष रूप से शुभ है।
इस प्रश्न के उत्तर में उनका कथन है कि केवल शुभ-संकल्प हो ऐसा निरपेक्ष तथा अप्रतिबंधित शुभ है। उनके मतानुसार ‘संकल्प’ मूलतः बौद्धिक होने के कारण संवेग, भावना, इच्छा, प्रवृत्ति आदि से पूर्णतया भिन्न है। वृद्धि ही संकल्प का उद्गम है, अत: संकल्प वह बुद्धिमूलक तत्त्व है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संकल्प का अर्थ मनुष्य को क्षणिक इच्छा मात्र नहीं है, अपितु किसी कर्म को करने का उसका दृढ़ निश्चय है, जिसके कारण वह उस कर्म को करने के लिए यथासम्भव सभी साधन एकत्र करने का प्रयास करता है इस प्रकार काण्ट ने शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करने के लिए यथा संभव समस्त साधनों का उपयोग करना भी बहुत आवश्यक माना है।
काण्ट के मतानुसार विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही नैतिक अथवा शुभ संकल्प है। इस प्रकार बौद्धिक शक्ति होने के कारण संकल्प इच्छा से भिन्न है जो मूलतः भावनात्मक होती है। जहाँ तक हमें ज्ञात है काण्ट ने शुभ संकल्प की कोई स्पष्ट और निश्चित परिभाषा नहीं दी। फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि वे विशुद्ध कर्त्तव्य चेतना द्वारा प्रेरित संकल्प को ही नैतिक अथवा शुभ संकल्प मानते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य का संकल्प केवल विशुद्ध कर्त्तव्य चेतना पर आधारित होता है तो कान्ट के विचार में उसे नैतिक अथवा शुभ संकल्प कहा जा सकता है।
ऐसे शुभ संकल्प को ही काण्ट अप्रतिबन्धित तथा निरपेक्ष शुभ मानते हैं। उनका मत है कि यह शुभ संकल्प ही सर्वत्र एवं सर्वदा अपने आप में शुभ है और इसका शुभत्त्व देश काल, परिस्थितियों तथा इससे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर निर्भर नहीं है। इस शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को काण्ट स्वतः साध्य शुभ तथा निरपेक्ष शुभ नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस विश्व में अथवा इससे बाहर शुभ संकल्प के अतिरिक्त ऐसी किसी अन्य । अन्य वस्तु की कल्पना करना ही नितान्त असम्भव है जो अपने-आप में तथा निरपेक्ष रूप से नरपेक्ष हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि काण्ट शुभ संकल्प को ही एकमात्र स्वतः साध्य शुभ तथा शुभ मानते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि काण्ट केवल शुभ संकल्प को ही शुभ नहीं मानते, । यह स्वीकार करते हैं कि विश्व में शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शुभ हैं। वे उदाहरणार्थ, उनका कथन है कि ज्ञान, तर्क शक्ति प्रतिभा, धैर्य, साहस, आत्मसंयम, सुख, स्वास्थ्य, सम्मान, घन, यश आदि सभी निश्चय ही कुछ परिस्थितियों में शुभ है। कान्ट मनुष्य के जीवन में इन सब की वांछनीयता को पूर्णतया स्वीकार करते हैं और इन्हें सामान्य परिस्थितियों में शुभ भी मानते हैं। परन्तु उनका यह निश्चित मत है कि ये शुभ संकल्प की भांति स्वतः साध्य शुभ तथा निरपेक्ष शुभ नहीं है इनका शुभत्व देश-काल, परिस्थितियों और इनके परिणामों पर ही निर्भर है। इसका अभिप्राय यही है कि ऊपर जिन वस्तुओं को शुभ कहा गया है सर्वत्र और सर्वदा शुभ न होकर केवल सीमित रूप में ही शुभ हैं। इन सब का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, उदाहरणार्थ स्वस्थ, साहसी और बलवान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, साहस और बल का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए कर ग अशुभ सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने ज्ञान और धन का दूसरों के न्याय संगत अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोग कर सकता है। स्पष्ट है कि उक्त अशुभ उद्देश्यों के कारण स्वास्थ्य, साहस, बल, बुद्धि सत्ता आदि को अशुभ ही माना जाएगा। इसी कारण काण्ट का कथन है कि शुभ संकल्प के अतिरिक्त विश्व में अन्य सभी वस्तुओं का शुभत्व सीमित और सापेक्ष ही है। संक्षेप में काण्ट के मतानुसार शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ वस्तुएँ तभी तक शुभ हैं जब तक उनका प्रयोग नैतिक नियम के विरुद्ध तथा अशुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नहीं किया जाता।
केवल शुभ संकल्प को ही स्वतः साध्य शुभ तथा निरपेक्ष शुभ मानने के कारण काण्ट ने उसे नैतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व दिया है। उनका विचार है कि शुभ संकल्प ही अन्य सभी वस्तुओं के शुभत्व का मूल आधार है। इसके बिना कोई भी वस्तु शुभ नहीं हो सकती। शुभ संकल्प से युक्त होने पर ही कोई वस्तु वास्तव में शुभ मानी जा सकती है। इसी कारण काण्ट शुभ संकल्प को नैतिक दृष्टि से उच्चतम शुभ माना है। उनका मत है कि उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जिसके मूल में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित है। उस कर्म के परिणामों का शुभ संकल्प के शुभत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि सदैव अपने आप में शुभ होने के कारण शुभ संकल्प पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष है।
उसका शुभत्व उसके परिणामों द्वारा निर्धारित नहीं होता। काण्ट का कथन है कि किसी कर्म के परिणामों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते. अतः शुभ संकल्प द्वारा प्रेरित प्रत्येक कर्म शुभ है-फिर चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। शुभ संकल्प के इसी परिणाम निरपेक्षता को स्पष्ट करते हुये उन्होंने लिखा है कि शुभ संकल्प अपने परिणामों के कारण शुभ नहीं है अपितु वह अपने आप में शुभ है। यदि दुर्भाग्य अथवा प्राकृतिक कठिनाई के कारण इस संकल्प के कोई शुभ परिणाम नहीं निकलते और यदि अधिकतम प्रयास कर के भी यह संकल्प कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता तो भी यह एक बहुमूल्य रत्न की भाँति अपने ही प्रकाश से स्वयं आलोकित होगा और अपने आप में इसका महत्त्व पूर्णरूपेण बना रहेगा। इस प्रकार काण्ट के मतानुसार शुभ संकल्प अपनी उपयोगिता के कारण शुभ न होकर स्वयं अपने आप में शुभ है, इसी कारण इसे निरपेक्ष और उच्चतम शुभ माना गया है।
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि काण्ट शुभ नहीं मानने। उनका कथन है कि पूर्ण शुभ या सर्वोत्तम शुभ में शुभ संकल्प के साथ-साथ आनन्द का भी समावेश होता है।
जो इच्छा कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य करती है वह सदिच्छा या शुभेच्छा है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदिच्छा अनिवार्यता कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य करती ही है। ऐसी सदिच्छा जो पूर्णतया शुभ या श्रेय है वह कदापि कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य नहीं करती है। पूर्णतया सदिच्छा पूतेच्छा है। उसके कर्त्तव्य कर्म स्वभावतः होते हैं। उसका कर्म मार्ग या कर्त्तव्य मार्ग है। अकर्तव्य का मार्ग उसके लिये असंभावित है। अतएव यह कर्त्तव्य वैसे ही करती है, जैसे अग्नि जलती है या सूर्य प्रकाश देता है। ऐसी पूतेच्छा ईश्वरेच्छा या सन्तों की इच्छा है। जिन्होंने पूर्णतया कामनाओं से अपने को मुक्त कर लिया है या जो पूर्णतया आत्मकाम और कृतकृत्य है। यह साधारण मानवों की इच्छा नहीं है। साधारण मानवों की इच्छा के सामने दो मार्ग रहते है। कर्त्तव्य मार्ग और अकर्त्तव्य मार्ग। इसलिए इन्हीं को कर्त्तव्य करने के लिये कर्तव्य करने की नैतिक आवश्यकता है। पूतेच्छा सम्पूर्ण श्रेय के लिये कर्म करती है और सदिच्छा कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य करती है। काण्ट के नीतिशास्त्र में सदिच्छा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यही उसके नीतिशास्त्र का आदि और अन्त भी है।
काण्ट का मानना है कि बुद्धि मानव स्वभाव का आवश्यक तत्त्व है तथा इंद्रियपरता मनुष्य के अन्दर पाशविकता का अवशेष है। वह उसकी वास्तविक प्रकृति के लिये विजातीय है। सच्चरित ही मंगल है सच्चरित सदिच्छा में सन्निहित है। सदिच्छा वौद्धिक इच्छा है। बौद्धिक इच्छा नैतिक नियम का पालन करने की इच्छा है। इच्छा व्यावहारिक बुद्धि अथवा सक्रिय बुद्धि है। प्रवृत्ति सदिच्छा स्वतंत्र है। सदिच्छा नैतिक नियम के प्रति विशुद्ध सम्मान पूर्वक कर्म में होती है। जो इच्छा किसी बाह्य लक्ष्य की कामना से प्रेरित होती है वह परतंत्र होती है। भाव कामना बुद्धि के बाहर की वस्तु है, बुद्धि आत्मा का आवश्यक तत्त्व है। अतः संकल्प का प्रत्येक भाव कामना को नहीं होना चाहिये। प्रेम और सहानुभूतिपूर्वक किया गया कर्म अनैतिक है। सदिच्छा भौतिक है। यह निरपेक्ष विधि या नियम का पालन करती है। नैतिक नियम कोई उद्देश्य का साधन है।
सदिच्छा स्वयं शासित इच्छा, लक्ष्यहीन इच्छा है। सदिच्छा पूर्वेच्छा है, पूतेच्छा को भगवतगीता ने त्रिगुणातीत पुरुष या पुरुषोत्तम की इच्छा कहा है। इसके लिये कुछ कर्त्तव्य नहीं है क्योंकि यह आत्म काम है। परन्तु फिर भी यह सदा यान्त्रिक गति से कर्तव्य कर्म करती रहती है। ऐसा प्रतेच्छा कहती है त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ कर्तव्य शेष रहा है और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गयी है तो भी ये कर्म करती रहती है।
न में पार्थस्त कर्त्तव्यत्रिषु लोकेषु किन्चन |
नान वाप्त माप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि ।।
इस प्रकार पूतेच्छा वाला प्राणी शुभ है। संसार में जो भी कर्म मनुष्य करता है वह केवल इच्छा द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार अध्ययन करने पर केवल यही निष्कर्ष सत्य है कि पूतेच्छा सम्पूर्ण श्रेय के लिये कर्म करती है और सदिच्छा कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य करती है।
सदिच्छा परम श्रेय या शुभ है। इस प्रकार श्रेय के विषय में कहा गया है कि श्रेय और प्राणि है तथा प्रेम और चीज है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुये भी पुरुष को बाँधते हैं। उन दोनों में से श्रेय का ग्रहण करने वालों का शुभ होता है और जो प्रेम का वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है।
अन्यच्छेयोऽन्य दुतैव प्रेय
स्ते उभे नाथार्थे पुरुषे सिवीदाः ।
तयो श्रेयः आददनास्य साधु
भवति हीयतेर्थाद्य उ प्रेमोवृणीते।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- काण्ट के ‘कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य सिद्धान्त’ की पूर्ण व्याख्या
- एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में अन्तः प्रज्ञावाद का मूल्यांकन
- बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की व्याख्या | Animism explanation of buddhist philosophy |
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
शुभ संकल्प या सदेच्छा क्या है ?
अपने नैतिक दर्शन में काण्ट ने सर्वप्रथम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है कि ऐसी कौन-सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है और जिसका शुभत्त्व देश, काल, परिस्थितियों तथा मनुष्य की भावनाओं अथवा इच्छाओं पर निर्भर नहीं है अर्थात् जो सर्वत्र एवं सर्वदा निरपेक्ष रूप से शुभ है।
