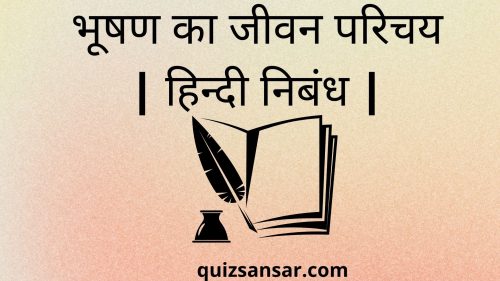
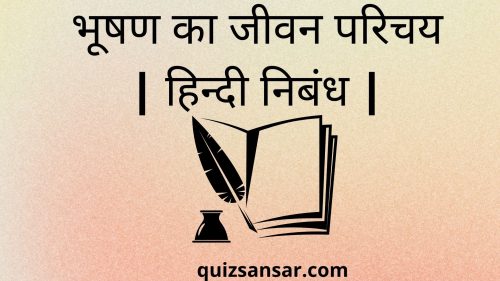
महाकवि भूषण का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | bhushan ka jivan parichay |
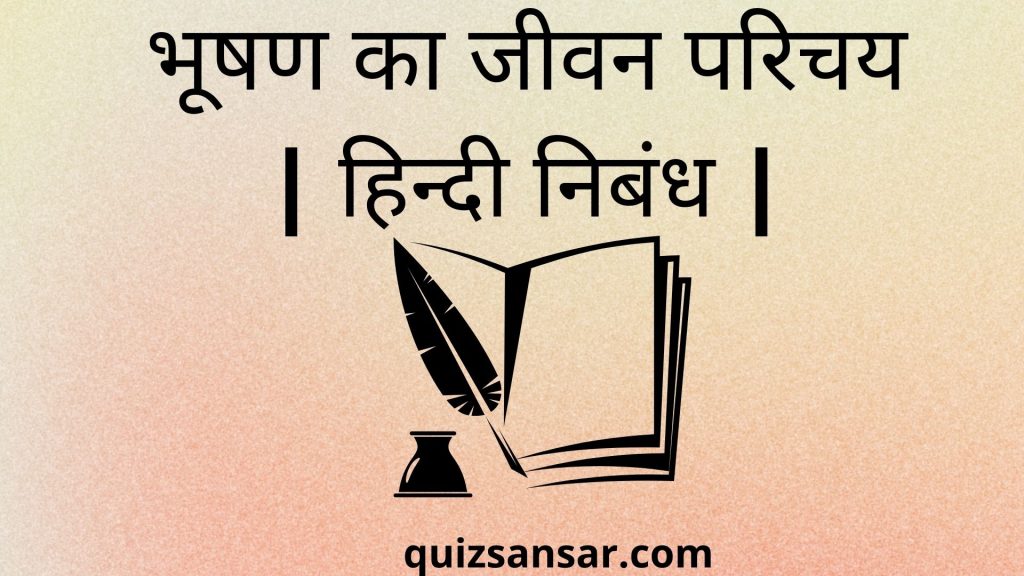
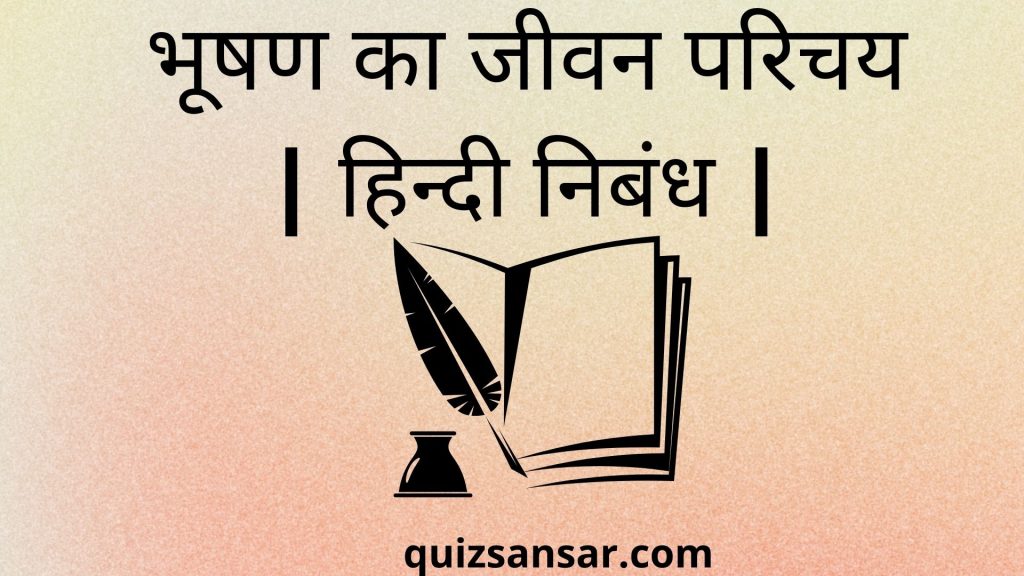
नमस्कार दोस्तों हमारी महाकवि भूषण का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | bhushan ka jivan parichay |उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- काव्यगत विशेषताएं
- भाषा
- शैली
- रस, छंद एवं अलंकार
- उपसंहार
प्रस्तावना
महापुरुष, परिस्थिति एवं समय के दास नहीं होते। उनमें युग परिवर्तन और परिस्थिति एवं समय को अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता होती है।
महाकवि भूषण ने रीतिकाल में जन्म लेकर रीतिकालीन घोर श्रृङ्गारवादी परम्पराओं का विरोध कर वीर रस पूर्ण राष्ट्रीय जागरण का महान् उद्घोष किया। भूषण, भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्रकवि थे।
जीवन वृत्त
युग प्रवर्त्तक महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवाँपुर नामक गाँव में सन् 1613 ई. में हुआ था। इनके पिता रत्नाकार त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे।
भूषण के अतिरिक्त, काव्य प्रतिभा सम्पन्न उनके तीन पुत्र चिंतामणि, मतिराम और नीलकण्ठ थे।
जीवनी सामग्री अप्राप्त होने के कारण भूषण के वास्तविक नाम का तो पता नहीं चल सका, इतना अवश्य है कि इन्हें सर्वप्रथम भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रराम से प्राप्त हुई थी और इनकी यही उपाधि नाम के स्थान पर प्रसिद्ध हो गई।
ये औरंगजेब आदि अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे, परन्तु जो आदर महाराजा शिवाजी और बुंदेले वीर छत्रसाल से इन्हें प्राप्त हुआ वह किसी से नहीं हुआ।
एक बार छत्रसाल ने इनकी पालकी के नीचे अपना कंधा लगा दिया था। इस पर भूषण ने कहा था कि
“शिवा को बखानी कि बखानी छत्रसाल को “
और राजा राव एक मन में न ल्याऊँ अब,
साहू को सराहों के सराहाँ छत्रसाल को।
छद्म वेश में भगवान शंकर के दर्शनार्थ आये हुए महाराजा शिवाजी से मन्दिर में इनकी प्रथम भेंट ही निम्न कविता के माध्यम से हुई थी।
उन्होंने इसे अट्ठारह बार सुना था, फिर इन्हें अपन वास्तविक परिचय देकर पुरस्कृत किया था। कविता की आद्यन्त पंक्ति इस प्रकार हैं
इन्द्र जिमि जंभ पर, वाडव सुअंभ पर।
त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है ।।
“यदि तुम्हारी कविता से मेरा हाथ मूँछ पर न गया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा लूँगा”
इस शर्त पर भूषण ! की वीर रस पूर्ण ओजस्विनी कविता ने औरंगजेब का भी : हाथ मूँछ पर ला दिया था और उसने प्रसन्न होकर इन्हें दरबार में रख लिया था।
भूषण की वीरता, शौर्य एवम् पराक्रमपूर्ण ओजस्विनी वाणी ने सन् 1715 में सदा-सदा के लिए मौन धारण कर लिया था।
रचनायें
भूषण के तीन काव्य-ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है–
- शिवराज भूषण
- शिवा बावनी
- छत्रसाल-दशक
‘शिवराज भूषण’ इनका अलंकार सम्बन्धी ग्रंथ है जिसमें शिवाजी की प्रशंसा के छंद, अलंकारों के उदाहरणों के रूप में दिये गये हैं।
शिवसिंह सरोज ने भूषण की दो और पुस्तकों का उल्लेख किया है जिनके नाम ‘भूषण हजारा’ और ‘भूषण उल्लास” हैं, परन्तु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं ।
इसके अतिरिक्त भूषण की अनेकों स्फुट रचनायें हैं।
काव्यगत विशेषतायें
भूषण की काव्यगत भावनाओं में राज्याश्रय प्रदान करने वाले राजा महाराजाओं के गुणगान हैं।
विशेषता यह है कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों की घोर शृङ्गारवादी परम्परा का अनुसरण करके राज-दरबारों में अपनी कवित-कामिनी का नग्न नृत्य नहीं कराया।
इनके तेजस्वी और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व ने तत्कालीन साहित्य में एक नवीन युग और एक मौलिक विचार परम्परा का सूत्रपात किया।
आश्रयदाताओं के विलासी जीवन का मनोरंजन एवं व्यय की चाटुकारिता न करके उनके वीरत्व, शौर्य, साहस एवं पराक्रम आदि का चित्रण किया गया है।
उनके दया, दान, औदार्य एवं धर्मपरायणता के चित्र दिये गये हैं। रण का चित्रण देखिये
ताव दै-दै मूँछन कँगूरन पै पाँव दै-दै, अरि मुख घाव दे-दै कूद परै कोटि में।
शिवाजी के पराक्रम प्रभाव वर्णन में वीर रस की अभिव्यक्ति देखिये-
भूषण भनत महावीर बलकन लागो, सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे ।
तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भये, स्याह मुख नौरंग, सिपाही मुख पियरे ||
भयभीत अरि-महिलाओं की वस्तु स्थिति का सजीव चित्र –
ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनिवारी, ऊँचे घोर मन्दिर के अंदर रहती हैं।
भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं।
भाषा
भूषण की भी भाषा बृजभाषा थी। बृजभाषा में कोमलकान्त पदावली द्वारा वीर रस का वर्णन करना, यह भी भूषण की अनन्य काव्य प्रतिभा का ही द्योतक है।
इनकी भावानुगामिनी भाषा वीर भावों को वहन करने में पूर्णतया समर्थ है। भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली, बुन्देलखण्डी, प्राकृत, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है।
भावों की तीव्रता वेग एवं प्रवाह के अनुरूप ही भाषा में तीव्रता प्रवाह एवं वेग है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने में भूषण पर्याप्त सफल हुए हैं।
आवश्यकतानुसार शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है। एक उदाहरण देखिये –
ऐल फैल खेल भैल खनक में गैल गैल, गजन की टेल पैल सैल उसलत हैं।
शैली
भूषण की शैली रीतिकालीन शैली है। इनकी शैली का शरीर रीति-कालीन अवश्य है परन्तु आत्मा में राष्ट्र की पुकार और युग-वाणी है।
शैली ओजपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। व्यंजकता, ध्वन्यात्मकता एवम् चित्रमयता इनकी शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं।
भूषण की शैली सरल, सजीव एवम् प्रभावोत्पादक है।
रस, छंद एवं अलंकार
भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। वीर-रस का सर्वाङ्गपूर्ण सफल परिपाक जैसा इनके काव्य में हुआ वैसा अन्यत्र नहीं हुआ।
चरित्र नायक शिवाजी की युद्ध वीरता के साथ-साथ उनकी दानवीरता, दयावीरता और धर्मवीरता का भी चरित्रांकन किया गया है।
भयानक एवम् रौद्र रसों का भी परिपाक इनकी रचनाओं में सुन्दर शैली में हुआ है।
छंद-योजना में भूषण ने कवित्त, दोहा, रोला, छप्पय तथा हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। भूषण की छन्द-व्यवस्था सुन्दर है। कवित्त इनके अधिक निकट थे।
उपसंहार
काव्य के आन्तरिक रूप में भूषण जहाँ मौलिक एवं मुक्त हैं वहाँ बाह्य रूप में रीतिकाल के प्रवाह से युक्त हैं।
अन्य कवियों की भाँति इन्होंने भी काव्य की शक्ति के साथ कला का चमत्कार प्रदर्शित किया है, अनुप्रास, यमक श्लेष और उपमा का बाहुल्य है।
भूषण की प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई अलंकार अवश्य निहित होगा।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
भूषण की जीवन वृत्त क्या है ?
युग प्रवर्त्तक महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवाँपुर नामक गाँव में सन् 1613 ई. में हुआ था। इनके पिता रत्नाकार त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे।
भूषण के अतिरिक्त, काव्य प्रतिभा सम्पन्न उनके तीन पुत्र चिंतामणि, मतिराम और नीलकण्ठ थे।
जीवनी सामग्री अप्राप्त होने के कारण भूषण के वास्तविक नाम का तो पता नहीं चल सका, इतना अवश्य है कि इन्हें सर्वप्रथम भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रराम से प्राप्त हुई थी और इनकी यही उपाधि नाम के स्थान पर प्रसिद्ध हो गई।
ये औरंगजेब आदि अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे, परन्तु जो आदर महाराजा शिवाजी और बुंदेले वीर छत्रसाल से इन्हें प्राप्त हुआ वह किसी से नहीं हुआ।
भूषण की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
भूषण के तीन काव्य-ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है–
शिवराज भूषण
शिवा बावनी
छत्रसाल-दशक
‘शिवराज भूषण’ इनका अलंकार सम्बन्धी ग्रंथ है जिसमें शिवाजी की प्रशंसा के छंद, अलंकारों के उदाहरणों के रूप में दिये गये हैं।
शिवसिंह सरोज ने भूषण की दो और पुस्तकों का उल्लेख किया है जिनके नाम ‘भूषण हजारा’ और ‘भूषण उल्लास” हैं, परन्तु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं ।
इसके अतिरिक्त भूषण की अनेकों स्फुट रचनायें हैं।
भूषण की भाषा क्या थी ?
भूषण की भी भाषा बृजभाषा थी। बृजभाषा में कोमलकान्त पदावली द्वारा वीर रस का वर्णन करना, यह भी भूषण की अनन्य काव्य प्रतिभा का ही द्योतक है।
इनकी भावानुगामिनी भाषा वीर भावों को वहन करने में पूर्णतया समर्थ है। भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली, बुन्देलखण्डी, प्राकृत, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है।
भावों की तीव्रता वेग एवं प्रवाह के अनुरूप ही भाषा में तीव्रता प्रवाह एवं वेग है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने में भूषण पर्याप्त सफल हुए हैं।
भूषण की शैली कैसी थी ?
भूषण की शैली रीतिकालीन शैली है। इनकी शैली का शरीर रीति-कालीन अवश्य है परन्तु आत्मा में राष्ट्र की पुकार और युग-वाणी है।
शैली ओजपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। व्यंजकता, ध्वन्यात्मकता एवम् चित्रमयता इनकी शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं।
भूषण की शैली सरल, सजीव एवम् प्रभावोत्पादक है।
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
