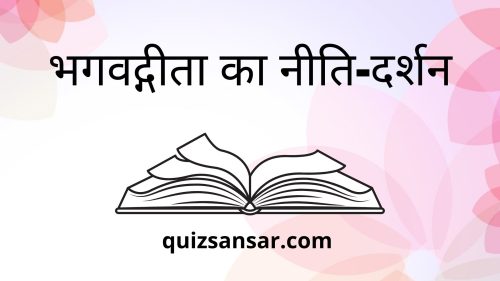
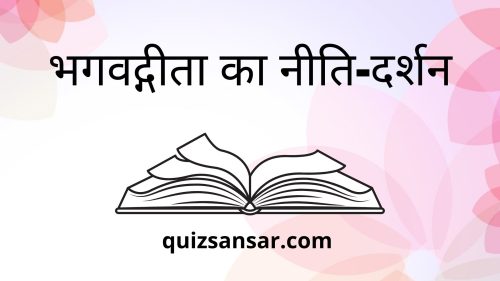
भगवद्गीता का नीति-दर्शन
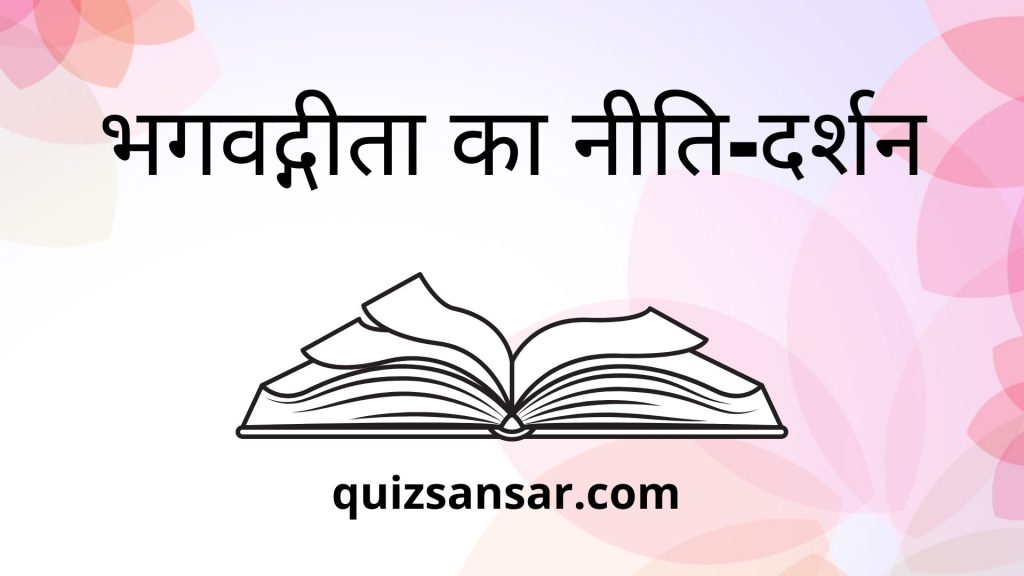
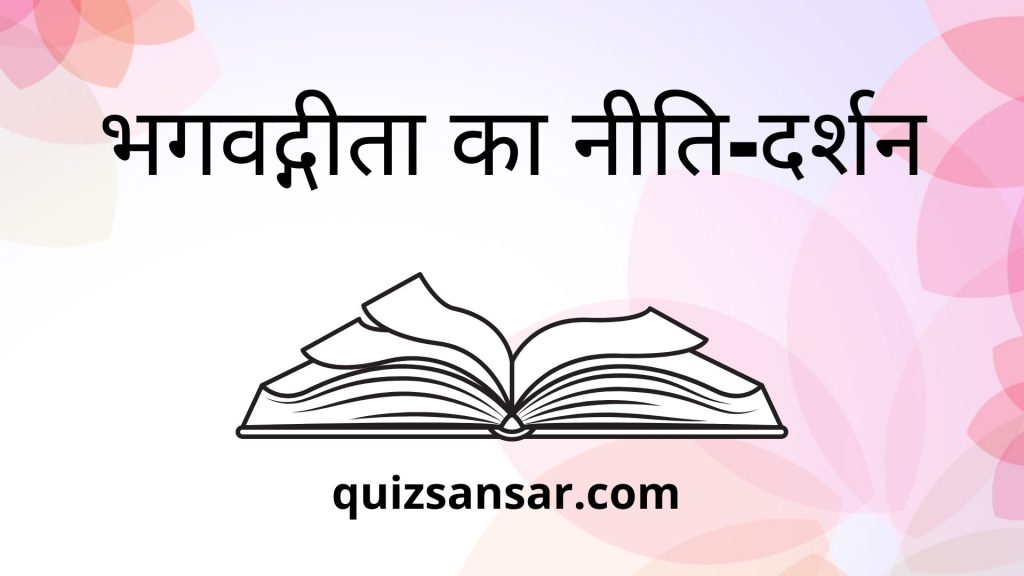
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है भगवद्गीता का नीति-दर्शन उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
गीता का नैतिक सिद्धान्त ( नीतिशास्त्र)
कर्तव्य-अकर्तव्य के द्वैत में फँसे हुये अर्जुन को कर्त्तव्य पथ पर उद्यत होने के लिए तथा मोहपाश के भ्रमजाल से निकलने के लिए दिये गये भगवान् कृष्ण के उपदेश ने भारतीय दर्शन में जिस नवीन विचारधारा का सृजन किया उसे गीता का निष्काम कर्मयोग कहा जाता है।
गीता के निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवान् कृष्ण ने समस्त मानव जाति को एक ऐसा प्रकाश मार्ग दिया जिससे अकर्मण्यता का तिमिर तिरोहित हो गया तथा फल भावना से रहित निष्काम कर्म का स्थाई मार्ग प्रकाशित हुआ। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने सांसारिक विषयों से लिप्त अर्जुन को यह रहस्य बताने की सफल चेष्टा की है कि उन्हें एक ओर तो तत्त्व ज्ञात नहीं और दूसरी ओर वह अपने उचित मार्ग से भी दूर हैं।
क्योंकि उन्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं। श्रीकृष्ण ऐसे मार्ग से भटके तथा जीवन जगत् के रहस्यों से अनभिज्ञ अर्जुन को तत्त्व ज्ञान भी देते हैं, जीवन के चरम लक्ष्य को भी निर्धारित करते हैं और उसकी प्राप्ति के उपाय भी बताते हैं।
गीता में अर्जुन को समझाने तथा उन्हें माया मोह छोड़कर कर्त्तव्य पालन अर्थात् युद्ध में लग जाने के सम्बन्ध में जो आदर्श दिये गये हैं उनमें दर्शन भी है और मनोविज्ञान भी, किन्तु इस सबके साथ एक विशेष प्रकार का अपूर्व नीतिशास्त्र भी मिलता है जो मानव जीवन के ज्ञानात्मक, भावात्मक अर्थात् जीवन के तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों का समन्वयात्मक रूप है। गीता के नैतिक विचार की मुख्य विशेषता इसकी व्यावहारिकता है जो काण्ट के कठोरवादिता सिद्धान्त से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हम गीता के नैतिक विचारों अथवा निष्काम कर्म योग का संक्षेप में वर्णन करेंगे।
गीता का निष्काम कर्म
गीता ने मानव जीवन को एकांगी जीवन न मानकर एक बहुअंगीय जीवन माना है क्योंकि गीता का ज्ञान, भक्ति और कर्म जो व्यक्ति बौद्धिक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पहलुओं से सम्बन्धित है उन पर समान दृष्टि डाली है और कहा गया है कि हमें बिना कर्म फल की चिन्ता किये अपना कर्त्तव्य करना चाहिये।
मनुष्य अपना विशेष स्थान रखता है उसे अपने स्थान के अनुसार कर्त्तव्य करना चाहिये। परन्तु कर्त्तव्य पालन में हमें किसी निम्न स्तर के साधन मात्र उद्देश्य से प्रेरित न होना चाहिये वरन् हमें निर्लिप्त एवं कर्म फल के प्रति उदासीन होकर कर्म करना चाहिये। फलदाता तो परमेश्वर है, हमारा कर्त्तव्य पालन में ही उद्धार है हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने चाहिये।
गीता का मनोविज्ञान
गीता में मानव जीवन के तीनों पक्षों में सामंजस्य स्थापित करने में बल दिया गया है अतः बुद्धि, भावना और कर्म तीनों का महत्त्व है इसमें से किसी पक्ष को दबा देना अस्वाभाविक होता है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। निष्काम कर्म तथा कर्त्तव्य पालन सम्भव तभी होंगे जब बुद्धि पथ प्रदर्शन करें तथा भक्ति और आस्था के प्रकाश में हम आगे बढ़ें और अपने के चरम लक्ष्य ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लें।
गीता का अध्यात्मदाद
गीता मनुष्य के सम्मुख एक ऐसा विचार रखती है जो न तो भौतिकवादी या सुखवादी है न उपयोगितावादी और न काण्ट की भाँति बुद्धिवादी या संन्यासवादी ही है। वरन् इसमें अध्यात्मवाद की पूर्णता का तत्त्व मिला है। क्योंकि मानव जीवन एक उपयोगी तथा सामाजिक जीवन उसी समय बन सकता है जब हम अपने कर्तव्यों को जाने, अपना स्थान पहचाने तथा ईश्वर में आस्था रखते हुये निष्काम कर्म करें।
इससे हमारा जीवन या व्यक्तित्त्व पूर्ण होगा। यह कारण प्रतीत होता है कि गीता में जिसे “ब्रह्म विद्यमान योगशास्त्र” की संज्ञा दी गयी है उससे अभिप्राय यही है कि गीता ब्रह्म ज्ञान पर अवलम्बित है और ब्रह्म से योग करने पर बल देती है।
गीता इन्द्रियों के विरुद्ध है
काण्ट ने जीवन के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष का बहिष्कार किया है और व्यक्ति को संन्यासवाद की ओर ले जाता है परन्तु गीता इन्द्रियों को बुद्धि द्वारा नियन्त्रित करने या उन्हें अनुशासित करने पर बल देती है और कर्मयोग को श्रेष्ठ मानती है।
सद्गुणों का अभ्यास
दैवीय गुणों को अपनाने तथा आसुरी गुणों को त्यागने पर बल देती है क्योंकि अध्यात्मवाद का उत्थान इसी से सम्भव है।
गुणों के आधार पर समाज का वर्गीकरण
गीता के सत्, रज तथा तम गुणों के आधार पर समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथ इनके कर्त्तव्य भी निर्धारित किये हैं। मोक्ष की प्राप्ति अपने-अपने स्थान से सम्बन्धित कर्मों के करने से हो सकती है।
गीता के नीतिशास्त्र सर्वाङ्गवाद है। गीता में मानव के समस्त अंगों के पूर्णरूपेण विकास को व्यवस्था है। सर्वाङ्गवाद में केवल ज्ञान और कर्म ही नहीं वरन भक्ति का भी समन्वय है। गीता के आत्मसमर्पण में योग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य समस्त धर्मों का परित्याग कर दे और ईश्वर की शरण में चला जाये तब उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। गीताकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार से ईश्वर की भक्ति करने तथा उसी को पूर्ण आत्मसमर्पण करने का उपदेश दिया है।
गीता के नीतिशास्त्र की मुख्य विशेषताएँ
गीता के नीतिशास्त्र की कतिपय मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –
व्यक्ति तथा समाज का समन्वय
गीता के नीतिशास्त्र में वैयक्तिक तथा सामाजिक हितों के साथ-साथ वैयक्तिक तथा सामाजिक हितों के समन्वय पर बल दिया गया है। पर व्यक्ति की आत्मा तथा परमात्मा के मध्य कोई अन्तर नहीं माना गया है। आत्मा तथा परमात्मा के मध्य जो भेद दृष्टिगोचर होता है वह अज्ञान के कारण ही है। व्यक्ति की सर्वांपूर्णता परम श्रेय है। तथापि व्यक्ति की सर्वाङ्गपूर्णता लोकसंग्रह तथा भगवद् प्राप्ति में प्राप्त की जा सकती है।
श्रम विभाजन का सिद्धान्त
गीता का वर्णाश्रम धर्म का विचार श्रम विभाजन की वैज्ञानिक व्यवस्था की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि ईश्वर को अर्पित बुद्धि से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से मनुष्य कर्म-बन्धन में पुनः नहीं फँसता। इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र तथा समाजशास्त्र का भी गीता में अद्भुत तथा अनुपम समन्वय किया गया है।
व्यावहारिक दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट
गीता का निष्काम कर्मयोग का सिद्धान्त न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वरन् व्यावहारिक तथा सांसरिक दृष्टिकोण से भी सर्वोत्कृष्ट साधन है। गीता के निष्काम कर्मयोग में कर्मवाद तथा संन्यास, भोग तथा वैराग्य का अनुपम समन्वय है। निष्काम कर्म में सतत् रूप से कर्त्तव्यारूढ़ रहने की अखण्ड शक्ति प्राप्त होती है।
वासनाओं का रूपान्तर
यद्यपि गीता में अनाशक्ति योग पर बल दिया गया है तथा गीता का मार्ग स्वाभाविक तथा सर्वांग है। उसमें वासनाओं का बहिष्कार न होकर इनका रूपान्तर तथा दैवीकरण किये जाने का उपदेश दिया गया है।
कर्तव्यों का वर्णन
गीता में विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए कर्त्तव्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इससे दैनिक जीवन में कर्तव्यों को समझने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।
तत्त्वज्ञान पर आधारित
गीता के नीतिशास्त्र का आधार ठोस है। गीता के नीतिशास्त्र में ईश्वरवादिता है तथा अन्य भक्ति को कहीं भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है।
स्वतन्त्रेच्छावाद तथा निर्धारणवाद
गीता में स्वतन्त्रेच्छावाद तथा निर्धारणवाद का सुन्दर सुमन्वय प्रस्तुत किया गया है। कर्मों का फूल तथा संसार की व्यवस्था का संचालन का कर्तव्य है कि उस व्यवस्था को समझकर ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करे तथा दैवी चेतना के कर्म का सफल यन्त्र बनने के लिए दृढ़ संकल्प तथा बुद्धि पूर्वक कार्य करे। दैवी चेतना के यन्त्र बनने का अर्थ है आन्तरिक चेतना के अनुसार कर्म करना क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा मूल रूप में एक ही है। अतएव दैवी निर्धारण में ही वास्तविक स्वतन्त्रता निहित है।
गीता का सार्वभौम सन्देश
गीता का सन्देश केवल भारत को अथवा किसी विशेष धर्म के लिए नहीं वरन अखिल विश्व के लिए है। यह सन्देश शाश्वत है। वर्तमान आणविक युग में गीता का “निष्काम कर्म योग” तथा “सर्वभूतहितरेत:” और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण यह है कि गीता में वे तत्त्व विद्यमान है जो प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में मानव को प्रेरणा देने वाले है।
निष्कर्ष
गीता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन यह है कि उसके अनुसार नीतिशास्त्र सामाजिक तथा वैयक्तिक दोनों है। नीतिशास्त्र में शक्ति की स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा समाज की सुरक्षा दोनों प्रयोजनों की सिद्धि होती है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
कर्तव्यों का वर्णन कजिये |
गीता में विभिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए कर्त्तव्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इससे दैनिक जीवन में कर्तव्यों को समझने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।
गीता का सार्वभौम सन्देश क्या है ?
गीता का सन्देश केवल भारत को अथवा किसी विशेष धर्म के लिए नहीं वरन अखिल विश्व के लिए है। यह सन्देश शाश्वत है। वर्तमान आणविक युग में गीता का “निष्काम कर्म योग” तथा “सर्वभूतहितरेत:” और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण यह है कि गीता में वे तत्त्व विद्यमान है जो प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में मानव को प्रेरणा देने वाले है।
वासनाओं का रूपान्तर क्या है ?
यद्यपि गीता में अनाशक्ति योग पर बल दिया गया है तथा गीता का मार्ग स्वाभाविक तथा सर्वांग है। उसमें वासनाओं का बहिष्कार न होकर इनका रूपान्तर तथा दैवीकरण किये जाने का उपदेश दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय आयोजित होने वाले खेल | International organized sports |
- खेल जगत | एथलेटिक्स | मैराथन |
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms

Excellent