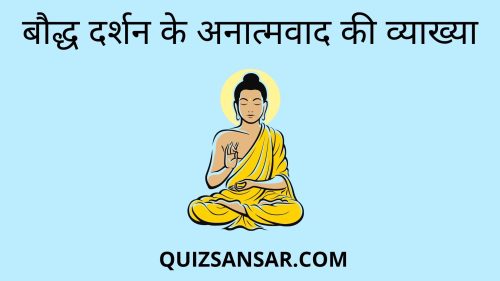
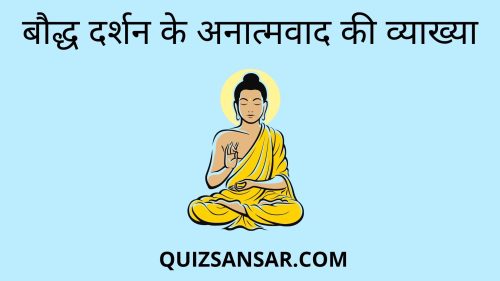
बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की व्याख्या | Animism explanation of buddhist philosophy |
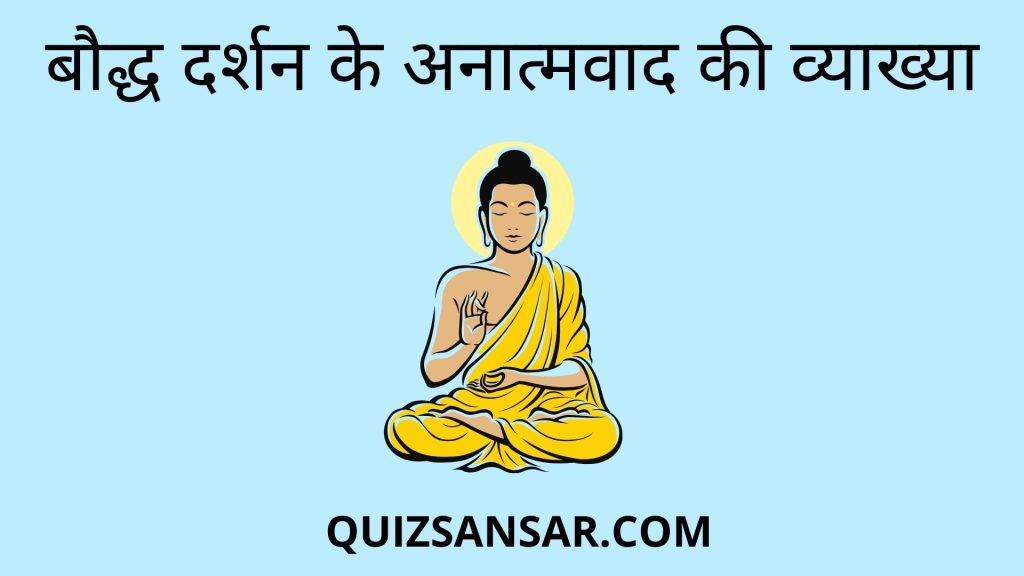
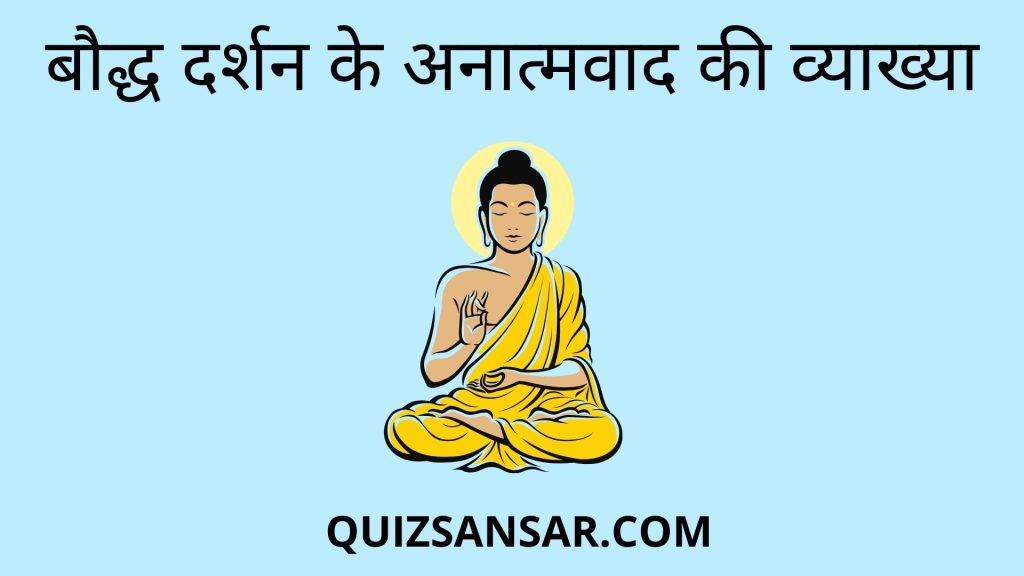
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की व्याख्या | Animism explanation of buddhist philosophy | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद (Animism of Buddhist Philosophy)
बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धान्त गौतम बुद्ध के प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त से ही सिद्ध होता है। इसे ‘ नैरात्म्यवाद ‘ भी कहा जाता है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि अनात्मवाद का सिद्धान्त केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत् दोनों की ही व्याख्या होती है।
जब गौतम बुद्ध ‘ सर्व अनात्कम् ‘ कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्त्व का अस्तित्त्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पनामात्र हैं।
सत् केवल क्षणिक धर्म हैं। ये क्षणिक धर्म मिलकर संघात बनाते रहते हैं जो निरन्तर परिवर्तनशील हैं। उल्लेखनीय है कि बौद्ध दर्शन में पंचस्कन्ध माने जाते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनमें रूप-स्कन्द भौतिक है जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनता है। शेष चारों स्कन्ध मानसिक हैं। इस क्षणिक पंच स्कन्ध संघात को ‘ पुद्गल ‘ या ‘ आत्मा ‘ कहते हैं और क्षणिक परमाणु संघात को ‘ भौतिक पदार्थ ’। ये दोनों संघात इसलिए अनात्म हैं क्योंकि इनकी नित्य एवं स्थायी सत्ता नहीं है। ये दोनों संघात उपचारमात्र है। वास्तविक सत्ता केवल क्षणिक विद्वानों एवं क्षणिक परमाणुओं की है जिनका प्रवाह निरन्तर चल रहा है। यह अनात्मवाद का व्यापक अर्थ है।
बौद्ध दर्शन में ‘ अनात्मवाद ‘ शब्द एक अन्य अर्थ में भी आता है। इससे गौतम बुद्ध के आत्मा सम्बन्धी विचारों का बोध होता है। इसमें औपनिषदिक एवं अन्यान्य पारम्परिक ब्राह्मण विचारधारा के आत्मा सम्बन्धी विचारों (आत्म-सिद्धान्त) को अस्वीकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण विचारधारा एक अजर-अमर, कूटस्थ, नित्य एवं अपरिवर्तनशील आत्म के अस्तित्त्व में विश्वास करती है। शरीर के परिवर्तन का ऐसी आत्मा की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं में पड़ता है। उसकी सत्ता जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात् भी कायम रहती है।
कभी-कभी आत्मा को उपनिषदों में सभी प्रकार के भेदों से रहित एक अमूर्त सत्ता के रूप में भी स्वीकार किया जाता गौतम इसलिए गौतम । बुद्ध ने इस प्रकार की अजर-अमर आत्मा का निषेध किया है। म बुद्ध ने आत्मा सम्बन्धी विचारों को अनात्मवाद या नैरात्मवाद कहते हैं। यहाँ एक अन्य तथ्य भी उल्लेखनीय है। अनात्मवाद का यह अर्थ नहीं है कि गौतम बुद्ध आत्मा के अस्तित्व का निषेध करते हैं। वे उस रूप में स्वीकृति करते हैं।
अ में आत्मा के अस्तित्व का निषेध करते हैं जिसकी लेकिन उनकी आत्मा की अवधारणा नितान्त भिन्न है। गौतम बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के सार्वभौमिक सिद्धान्त के आधार पर केवल परिवर्तनशील दृष्ट पदार्थों को स्वीकार किया। उन्होंने इस परिवर्तनशील दृष्ट धर्मों के अतिरिक्त किसी अदृष्ट, अपरिवर्तनशील, नित्य तत्त्व की सत्ता को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने इसी के आधार पर आत्म तत्व का विश्लेषण किया और अजर-अमर कूटस्थ नित्य आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हुए आत्मतत्व का प्रतिपादन किया। उनके इस विश्लेषण का आधार मनोवैज्ञानिक है।
गौतम बुद्ध इस बात पर बल देते हैं कि जब हम घटनाओं की पृष्ठभूमि में किसी स्थायी आत्मा की सत्ता की कल्पना करते हैं तब हम अपने अनुभव की सीमा का अतिक्रमण करते हम आत्म तत्व का विश्लेषण करते हुए जब अन्दर की ओर देखते हैं तो हमें सर्दी या गर्मी, रोशनी या छाया प्रेम या घृणा, दुःख या सुख आदि का ही अनुभव होता है। सामान्यतः यह विश्वास कर लिया जाता है कि ये संवेदन और विचार निरा अकेले नहीं आते, बल्कि एक अपरिवर्तनशील सत्ता से सम्बद्ध होते हैं जिसे आत्मा एवं कभी-कभी जीव भी कह दिया जाता है।
गौतम बुद्ध का कथन है कि केवल इन क्षणिक संवेदनों एवं विचारों की ही सत्ता है। इनकी पृष्ठभूमि में किसी नित्य आत्मा या जीव की कल्पना अनुचित एवं अनावश्यक है। अनुभव से इन संवेदनों के अतिरिक्त किसी अपरिवर्तनशील एवं नित्य आत्म तस्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त होता वस्तुतः क्षणिक विचारों या विज्ञानों की निरन्तर धारा प्रवाहित होती रहती है।
हम जिसे आत्मा कहते हैं, वह इन्हीं क्षणिक विचारों की धारा का नाम है या परिवर्तनशील क्षणिक विज्ञानों का प्रवाहमात्र है। गौतम बुद्ध नित्य आत्मा तत्त्व की सत्ता हमारे साधारण विश्वास का स्पष्टीकरण करते। कहते हैं कि क्षणिक एवं परिवर्तनशील विज्ञानों की धारा निरन्तर प्रवाहित हो रही विज्ञानों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में एक सामान्य रूप दिखाई देता है। हम इसी भाव को, जो विज्ञानों की सभी अवस्थाओं में सामान्य व्यापक तत्व है, आत्मा कह देते हैं।
जैसे, जिस प्रकार हम रथ आदि पदार्थों का वर्णन करते समय गुणों की पृष्ठभूमि में निहित एक वस्तु की कल्पना कर लेते हैं उसी प्रकार हम मानसिक अवस्थाओं की अमृत नित्य आत्मा तत्त्व की कल्पना कर लेते हैं जो अनुचित है। गौतम बुद्ध के अनुसार यह पृष्ठभूमि में एक आत्मा का असली रूप है हम आत्मा का असली स्वरूप न समझने के कारण उसे अजर अमर एवं नित्य मानते हैं। इससे उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है और हम उसे मोक्ष दिलाकर सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। बुद्ध का कथन है कि जिस प्रकार किसी अदृष्ट एवं अप्रमाणिक आत्मा से भी प्रेम रखना हस्यास्पद है। पुनः अदृष्ट आत्मा के प्रति अनुराग रखना वैसे ही है जैसे एक ऐसे प्रासाद पर चढ़ने के लिए सीधी तैयार करना जिस प्रसाद को कभी किसी ने देखा भी नहीं है।
गौतम बुद्ध आत्मा का विश्लेषण उसके घटकों में करते हैं। मिलिन्दपको नामक बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थ में प्राप्त नागसेन मिलिन्द संवाद’ से ज्ञात होता है कि आत्मा पंचस्कन्धों का संघात’ है। ये पाँच स्कन्ध हैं-रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये स्कन्ध आत्मा के घटक है। रूप स्कन्ध आत्मा का भौतिक घटक है और वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, संस्कार स्कन्ध एवं विज्ञान स्कन्ध उसके मानसिक घटक है। इस संवाद से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार चक्र, पुरी, नेमि, पताका आदि के समूह के लिए ‘रथ’ शब्द का प्रयोग होता है. उसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान स्कन्धों के संघात के लिए ‘आत्मा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आत्मा भौतिक एवं मानसिक तत्वों की एक समष्टि का नाम है।
बौद्ध दर्शन के अनुसार समस्त जड़ पदार्थ, उनके गुण, इन्द्रियाँ, उनके विषय एवं मनुष्य के सन्दर्भ में उसके शरीर का आकार, रंग आदि रूप-स्कन्ध के अन्तर्गत आते हैं। वेदना-स्कन्ध के अन्तर्गत मुखात्मक, दुःखात्मक एवं उदासीनता की अनुभूतियाँ आती हैं। संज्ञा स्कन्ध वस्तु की निश्चित ज्ञान आता है। पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न प्रवृत्तियाँ संस्कार कहलाती है। यह स्कन्ध रूप. वेदना और संज्ञा-स्कन्धों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली मानसिक शक्ति है। विज्ञान का अर्थ है ‘चेतना’। इन पंच स्कन्धों के संचात को आत्मा कहते हैं।
जब तक इन स्कन्धों का संघात कायम रहता तब तक आत्मा का अस्तिता कायम रहता है। इस संघात के नष्ट होते ही आत्मा तत्त्व का भी विलोप हो जाता है। इस संघात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस संघात को उपनिषदों की शब्दावली में कभी-कभी ‘नाम-रूप’ भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि नाम के अन्तर्गत रूपेतर चारों स्कन्ध आते हैं। संक्षेप में, पंचस्कन्थों का संघात ही आत्मा है। हम मस्तिष्क में इन्द्रियों के अवशेषों में व्यक्तित्व को बनाने वाले तत्वों में अथवा अनुभवों की पृष्ठभूमि में व्यर्थ ही आत्मा की खोज करते हैं।
पाश्चात्य दर्शन में भी कई दार्शनिकों ने गौतम बुद्ध की शब्दावली में आत्मा का विवेचन किया है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में हाम का भी कथन है कि निता आत्मा की कोई सचा नहीं है। हम अपने अनुभव में कभी भी नित्य आत्मा के विचार के अनुरूप कुछ भी नहीं पाते हैं। उसके अनुसार, जब में अपनी आत्मा को पकड़ने के लिए अपने भीतर अन्य गहराई से प्रवेश करता हूँ तो मैं किसी भी आत्मा को नहीं पकड़ पाता हूँ।
मैं कुछ संवेदनाओं से टकराकर रह जाता हूँ जो सुख दुःख इच्छा आदि के होते हैं। तथाकथित आत्मा विज्ञानों के प्रवाह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विलियम जेम्स ने ‘आत्मा’ शब्द को एक आलंकारिक भाषा कहा हा जो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है। उसके अनुसार, ‘आत्मा शब्द किसी की व्याख्या नहीं कर सकता और न कोई निश्चित भाव ही दे सकता है। इसके पीछे आने वाले पदार्थों को एकमात्र बोधगम्य पदार्थ है। लांजे के अनुसार भी संवेदनाओं, मानसिक आवेगों एवं भावनाओं के एकत्रीभूत पुंज को आत्मा का नाम दे दिया गया है।
बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद की समीक्षा
भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया हुई जो इस प्रकार –
- अनात्मवाद के आधार पर ज्ञान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि क्षणिक विद्वानों की संतति का नाम आत्मा है। उससे भिन्न कोई नित्य आत्मा नहीं तो प्रश्न है कि ज्ञान किसे राप्त होता है? क्या एक विज्ञान दूसरे विज्ञान को जानता है। वस्तुतः क्षणिक विज्ञान वज्ञान दूसरे क्षणिक विज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता। एक नित्य आत्मा के अभाव में संबेदन तो होते रहेंगे, किन्तु वे ज्ञान नहीं कहलायेंगे। ज्ञान की यह अवधारणा यह उपलक्षित करती है कि विज्ञानों की संतति का एक ऐसे विषयों से सम्बन्ध होता है जो उस सन्तति के पूर्ण पर क्रम का अंग नहीं है। यदि आत्मा या विषयों द्वारा अनुभवों का संश्लेषण हो तो वह संवेदन मात्र होगा, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता।
- आलोचकों के अनुसार पुनर्जन्म की अवधारणा की अनात्मवाद के साथ संगति नहीं बैठती है, क्योंकि पुनर्जन्म के लिए नित्य आत्मा को सत्ता में विश्वास आवश्यक है। गौतम बुद्ध का कथन है कि अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास अससंगत नहीं है। यद्यपि किसी नित्य आत्मा की सत्ता नहीं है, तथापि व्यक्ति का जीवन विभिन्न क्रमबद्ध एवं अव्यवहित अवस्थाओं की एक संतति है। इस संतति में किसी अवस्था का प्रादुर्भाव उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होता है और वह अवस्था स्वयं भावी अवस्था को उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्णापर कारण कार्य सम्बन्ध होने के कारण मनुष्य में व्यक्तित्व का सातत्य बना रहता है। अतः बौद्ध दर्शन अनात्मवाद के साथ भी पुनर्जन्म को अवधारणा में विश्वास न्याय संगत मानता है।
- बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के विरुद्ध यह भी आक्षेप किया जाता है कि अनात्मवाद में विश्वास कर्मवाद के नैतिक सिद्धान्त को भी अप्रांसगिक बना देता है। कर्मवाद के अनुसार कर्मफल का भोक्ता वही होना चाहिए जो कर्म का कर्त्ता से हो। यह तभी सम्भव है जब एक नित्य आत्मा का अस्तित्व हो। किन्तु बिना नित्य आत्मा की सत्ता स्वीकार किये कर्मवाद को प्रासंगिक नहीं माना जा सकता।
यह भी आक्षेप किया जाता है कि क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद से प्रत्यभिज्ञा और स्मृति को व्याख्या नहीं होती। प्रत्यभिज्ञा का सम्बन्ध पहचानने’ से है। यदि प्रत्येक वस्तु क्षणिक एवं परिवर्तनशील है और आत्मा की प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तो हम यह कैसे कहते है कि –
‘यह वह कुर्सी है जिसे मैंने पाँच वर्ष पूर्ण खरीदा था’ या ‘यह वही व्यक्ति है जो मेरे साथ पचीस वर्ष पूर्व हाईस्कूल में पढ़ता था।’ बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सादृश्य के आधार पर सम्भव है। आलोचकों के अनुसार जब हम यह कहते हैं कि ‘यह वह कुर्सी है’ या ‘यह वही देवदत्त है’ तो यह कथन सादृश्य से कुछ अधिक है। इसकी व्याख्या केवल विज्ञान नैरन्तर्य से सम्भव नहीं है। इसकी व्याख्या नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने पर ही सम्भव है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
अनात्मवाद को और किस नाम से जाना जाता है ?
बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धान्त गौतम बुद्ध के प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त से ही सिद्ध होता है। इसे ‘नैरात्म्यवाद’ भी कहा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय आयोजित होने वाले खेल | International organized sports |
- खेल जगत | एथलेटिक्स | मैराथन |
- Cable T.V.: A Blessing Or A Bane | Essay |
- Craze of Twenty-20 Cricket | Essay |
- Smoking: A Health Hazard | Essay |
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms
- Branches of science and its meaning
- ONE LINER CURRENT AFFAIRS
