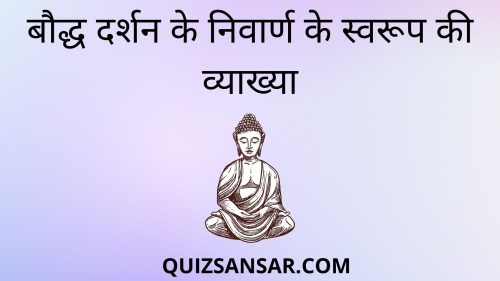
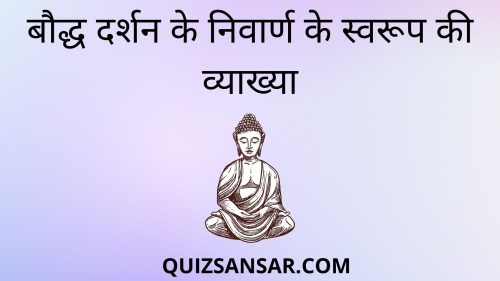
बौद्ध दर्शन के निवार्ण के स्वरूप की व्याख्या


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है बौद्ध दर्शन के निवार्ण के स्वरूप की व्याख्या उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
बौद्ध दर्शन के निर्वाण का स्वरूप
उत्तर द्वितीय आर्य-सत्य में बुद्ध ने दुःख के कारण को माना है। इससे प्रमाणित होता है कि यदि दुःख के कारण का अन्त हो जाय तो दुःख का भी अन्त अवश्य होगा। जब कारण का ही आभाव होगा, तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? वह अवस्था जिसमें दुःखों का अन्त होता है ‘दुःख निरोध’ कही जाती है।
दुःख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ‘निर्वाण’ को पाली में ‘निब्बान’ कहा जाता है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि भारत के अन्य दर्शनों में जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है उसी सत्ता को बौद्ध-दर्शन में निर्वाण की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस प्रकार निर्वाण और मोक्ष समानार्थक हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यही बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की विशेषताओं का उल्लेख है।
निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी सम्भव है। एक मानव इस जीवन में भी अपने दुःखों का निरोध कर सकता है। एक व्यक्ति यदि अपने जीवनकाल में ही राग, द्वेष, मोह आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है। मुक्त व्यक्ति को अर्हत् कहा जाता है।
अर्हत् बौद्ध दर्शन में एक आदरणीय सम्बोधन है। महात्मा बुद्ध ने पैतीस वर्ष की अवस्था में बोधि को प्राप्त किया था। उसके बाद भी वे पैंतालिस वर्ष तक जीवित थे। बुद्ध की तरह दूसरे लोग भी निर्वाण को जीवनकाल में प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण-प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है, क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते हैं, शरीर विद्यमान रहता है।
बुद्ध की यह धारणा उपनिषदों की जीवन-मुक्ति से मेल खाती है। बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी जीवन-मुक्ति और विदेह-मुक्ति की तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं। परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के उपरान्त निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति अस्सी वर्ष की अवस्था में हुई जब उनका देहान्त हुआ। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अन्त नहीं है, अपितु यह एक ऐसी अवस्था है जो जीवनकाल में ही प्राप्य है।
निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर बुद्ध के चार आर्य-सत्यों को मनन करना पड़ता है। परन्तु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। इसके विपरीत वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्यान्वित दीख पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को अकर्मण्य रहने का विचार हुआ था।
परन्तु संसार के लोगों को दुःखों से पीड़ित देखकर उन्होंने अपने विचार को बदला। जिस नाव पर चढ़कर उन्होंने दुःख-समुद्र को पार किया था, उस नाव को तोड़ने के बजाय उन्होंने अन्य लोगों के हित के लिए रखना आवश्यक समझा। लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बुद्ध ने घूम-घूमकर अपने उपदेशों को जनता के बीच रखा दुःखों से पीड़ित मानव को आशा का सन्देश दिया। उन्होंने अनेक संघों की स्थापना की। धर्म प्रचार के लिए अनेक शिष्यों को विदेशों में भेजा। इस प्रकार बुद्ध का सारा जीवन कर्म का अनोखा उदाहरण रहा है। अतः निर्वाण का अर्थ कर्म-संन्यास समझना प्रान्तिमूलक है।
यहाँ पर एक आक्षेप उपस्थित किया जा सकता है यदि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार के कर्मों में भाग लेता है तो किये गये कर्म संस्कार का निर्माण कर उस व्यक्ति को बन्धन को अवस्था में क्यों नहीं बाँधते? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है बुद्ध ने दो प्रकार के कर्मों को माना है। एक प्रकार का कर्म वह है जो राग, द्वेष तथा मोह से संचालित होता है। इस प्रकार के कर्म को आसक्त कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म मानव को बन्धन की आवस्था में बाँधते हैं जिसके फलस्वरूप मानव को जन्म ग्रहण करना पड़ता है।
दूसरे प्रकार का कर्म वह है जो राग, द्वेष एवं मोह से रहित होकर तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है। इस प्रकार के कर्म को अनासक्त कर्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है वह जन्म ग्रहण नहीं करता।
इस प्रकार के कर्मों की तुलना बुद्ध ने भूंजे हुए बीज से की है जो पौधे की उत्पत्ति में असमर्थ होता है। आसक्त कर्म की तुलना बुद्ध ने उत्पादक बीज से की है जिसके वपन से पौधे की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाते हैं, उनके कर्म अनाशक्ति की भावना से संचालित होते हैं। इसलिए कर्म करने के बावजूद उन्हें कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाता है। बुद्ध की अनासक्त-कर्म-भावना गीता की निष्काम कर्म भावना से मिलती-जुलती है।
बुद्ध ने निर्वाण के सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया। उनसे जब भी निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तब वे मौन रहकर प्रश्नकर्ता को हतोत्साहित करते थे। उनके मौन रहने के फलस्वरूप निर्वाण के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएँ विकसित हुई।
कुछ विद्वानों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ लिया। कुछ अन्य विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया। इस प्रकार निर्वाण के शाब्दिक अर्थ को लेकर विद्वानों के दो दल हो गये। इन दो दलों के साथ-ही-साथ निर्वाण के समबन्ध में दो मत हो गए। जिन लोगों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा उन लोगों ने निर्वाण के सम्बन्ध में जो मत दिया, उसे निषेधात्मक मत कहा जाता है। जिन लोगों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ शीतलता समझा उन लोगों ने निर्वाण के सम्बन्ध में जो मत दिया उसे भावात्मक मत कहा जाता है। सर्वप्रथम हम निर्माण के निषेधात्मक मत पर प्रकाश डालेंगे।
निषेधात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा है। उन लोगों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अन्त हो जाता है उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुःख मिट जाते हैं। निर्माण के इस अर्थ को प्रभावित होकर कुछ बौद्ध अनुयायी एवं अन्य विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश समझा है।
इन लोगों के कथनानुसार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अस्तित्त्व का विनाश हो जाता है। अतः इन लोगों ने निर्वाण का अर्थ जीवन का अन्त समझा है। इस मत के समर्थकों ने ओल्डनबर्ग, बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय और पौल दहल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। निर्वाण का यह निषेधात्मक मत तर्कसंगत नहीं है।
यदि निर्वाण का अर्थ पूर्ण-विनाश अर्थात् जीवन का अन्त माना जाय, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया बुद्ध के सारे उपदेश इस बात के प्रमाण हैं कि इन्होंने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण को अपनाया था। यदि इस विचार का खंडन किया जाय, तब बुद्ध के सारे उपदेश एवं उनके निर्वाण प्राप्ति के विचार कल्पनामात्र हो जाते हैं। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अन्त समझना भ्रमात्मक है।
क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्त्व मृत्यु के पश्चात् रहता है? बुद्ध से जब यह प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौन हो जाते थे। उनके मौन रहने के कारण कुछ लोगों ने यह अर्थ निकाला कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अस्तित्त्व नहीं रहता है। परन्तु बुद्ध के मौन रहने का यह अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है। उनके मौन रहने का सम्भवतः यह अर्थ होगा कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अवर्णनीय है।
प्रो० मैक्समूलर और चाइलडर्स ने निर्वाण-विषयक वाक्यों का सतर्क अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्वाण का अर्थ कहीं भी पूर्ण विनाश नहीं है। यह सोचना कि निर्वाण व्यक्तित्त्व-प्रणाश की अवस्था है बुद्ध के अनुसार एक दुष्टतापूर्ण विमुखता है। यह जान लेने के बाद कि निर्वाण अस्तित्त्व का उच्छेद नहीं है, निर्वाण सम्बन्धी भावात्मक मत की काद व्याख्या करना परमावश्यक है।
भावात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया है। बौद्ध दर्शन में वासना, , क्रोध, मोह, भ्रम, दुःख इत्यादि को अग्नि के तुल्य माना गया है। निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुःख रूपी आग का ठण्डा हो जाना है। निर्वाण के इस अर्थ पर जोर देने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने निर्वाण को आनन्द की अवस्था कहा है। इस मत के मानने का वालों में प्रो० मैक्समूलर, चाइलडर्स्, श्रीमती रायज डेविड्स, डॉक्टर राधाकृष्णन्, पूसिन इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।
रायज डेविड्स ने निर्वाण को इस प्रकार व्यक्त किया है –
“निर्वाण मन की पापहीन शान्तावस्था के समरूप है जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता, क पूर्ण शान्ति, शिवत्त्व और प्रज्ञा कहा जा सकता है।”
पूसिन ने निर्वाण को –
“पर, द्वीप, अत्यन्त, अमृत, अमृतपद और निःश्रेयस् कहा है।”
डॉक्टर राधाकृष्णन् के शब्दों में –
” निर्वाण , जो आध्यात्मिक संघर्ष की सिरि है , भावात्मक आनन्द की अवस्था है।”
इन विद्वानों तरिक्त पाली ग्रन्थों में भी निर्वाण को आनन्द की अवस्था माना गया है। के अतिरिक्त धम्मपद में निर्वाण को आनन्द, चरम सुख, पूर्ण शान्ति तथा लोभ, घृणा और भ्रम से रहिव अवस्था कहा गया है। (निब्बानं परमं सुखम्)। अंगुत्तर निकाय में निर्वाण को आनन्द एवं अवस्था के रूप में चित्रित किया गया है।
निर्वाण को आनन्दमय अवस्था मानने के फलस्वरूप पवित्रता के कुछ विद्वानों ने बौद्ध दर्शन पर पर सुखवाद का आरोप लगाया है। निर्वाण को आनन्द को अवस्था मानने के कारण बुद्ध को सुखवादी कहना भ्रमात्मक अनुभूति सुख की अनुभूति से भिन्न है। सुख की अनुभूति अस्थायी और दुःखप्रद है, परन्तु क्योंकि आनन्द की आनन्द की अनुभूति आमृत तुल्य है।
निर्वाण का मुख्य स्वरूप यह है कि वह अनिर्वचनीय है तक और विचार के माध्यम से इस अवस्था को चित्रित करना असम्भव है। डॉक्टर दास गुप्त ने कहा है-लौकिक अनुभव के रूप में निर्वाण का निर्वाचन मुझे एक असाध्य कार्य प्रतीत होता है यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ सभी लौकिक अनुभव निषिद्ध हो जाते हैं, इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से शायद ही सम्भव है। डॉक्टर कीथ ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है सभी व्यावहारिक शब्द अवर्णनीय का वर्णन करने में असमर्थ है।
बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मोपदेशक नागसेन ने यूनान के राजा मिलिन्द के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से की है। निर्वाण को उन्होंने सागर की तह गहरा, पर्वत की तरह ऊँचा और मधु की तरह मधुर कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि निवार्ण के स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे इसकी अनुभूति प्राप्त है। जिस प्रकार अन्धे को रंग का ज्ञान कराना सम्भव नहीं है उसी प्रकार जिसे निर्वाण की अनुभूति अप्राप्य है, उसे निर्वाण का ज्ञान कराना सम्भव नहीं है। अतः निर्वाण की जितनी परिभाषाएँ दी गई हैं वे निर्वाण के यथार्थ स्वरूप बतलाने में असफल हैं।
निर्वाण की प्राप्ति मानव के लिए लाभप्रद होती है। इससे मुख्यत: तीन लाभ प्राप्त होते हैं।
निर्वाण से सर्वप्रथम लाभ
यह है कि इससे समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है। दुःखों के समस्त कारणों का अन्त कर निर्वाण मानव को दुःखों से मुक्ति दिलाता है।
निर्वाण का दूसरा लाभ
यह है कि इससे पुनर्जन्म की सम्भावना का अन्त हो जाता है। जन्म-ग्रहण के कारण नष्ट हो जाने से निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म-ग्रहण के बन्धन से छुटकारा पा जाता है। कुछ विद्वानों ने निर्वाण के शाब्दिक विश्लेषण से यह प्रमाणित किया है कि निर्वाण पुनर्जन्म का अन्त है।‘निर्वाण’ शब्द‘निर्’ और वाण शब्द के सम्मिश्रण से बना है। ‘निर्’ का है अर्थ है ‘नहीं’ और ‘वाण’ का अर्थ है ‘पुनर्जन्म-पथ’। अतः निर्वाण का अर्थ पुनर्जन्म रूपी पथ का अन्त हो जाना है।
निर्वाण का तीसरा लाभ
यह है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का शेष जीवन शान्ति से बीतता है। निर्वाण से प्राप्त शान्ति और सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त शान्ति में अन्तर है। सांसारिक वस्तुओं से जो शान्ति प्राप्त होती है वह अस्थायी एवं दुःखदायी है। परन्तु निर्वाण से प्राप्त शान्ति आनन्ददायक होती है। निर्वाण के ये भावात्मक लाभ हैं, जबकि अन्य दो वर्णित लाभ निषेधात्मक हैं।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
बौद्ध दर्शन के निर्वाण का स्वरूप क्या है ?
द्वितीय आर्य-सत्य में बुद्ध ने दुःख के कारण को माना है। इससे प्रमाणित होता है कि यदि दुःख के कारण का अन्त हो जाय तो दुःख का भी अन्त अवश्य होगा। जब कारण का ही आभाव होगा, तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? वह अवस्था जिसमें दुःखों का अन्त होता है ‘दुःख निरोध’ कही जाती है। दुःख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है।
निर्वाण से सर्वप्रथम लाभ क्या होता है ?
यह है कि इससे समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है। दुःखों के समस्त कारणों का अन्त कर निर्वाण मानव को दुःखों से मुक्ति दिलाता है।
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms
- विकासवादी सुखवाद के समबन्ध में स्पेन्सर का योगदान
- उपयोगितावाद का सिद्धान्त और सिजविक का योगदान
- अद्वैत वेदांत के आधार पर आत्मा के स्वरुप की विवेचना | आत्मा एवं जीव के मध्य सम्बन्ध |
