

सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
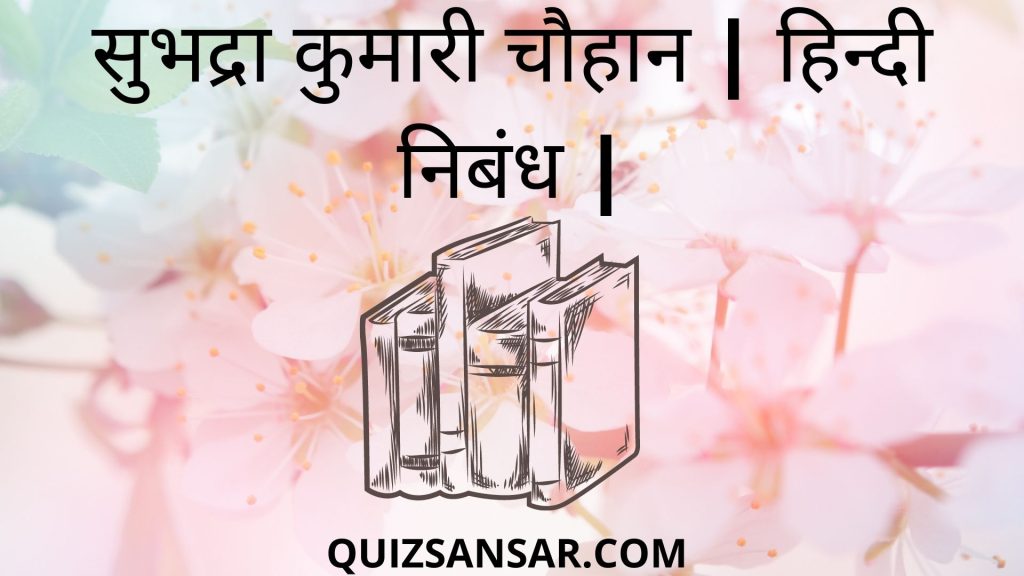
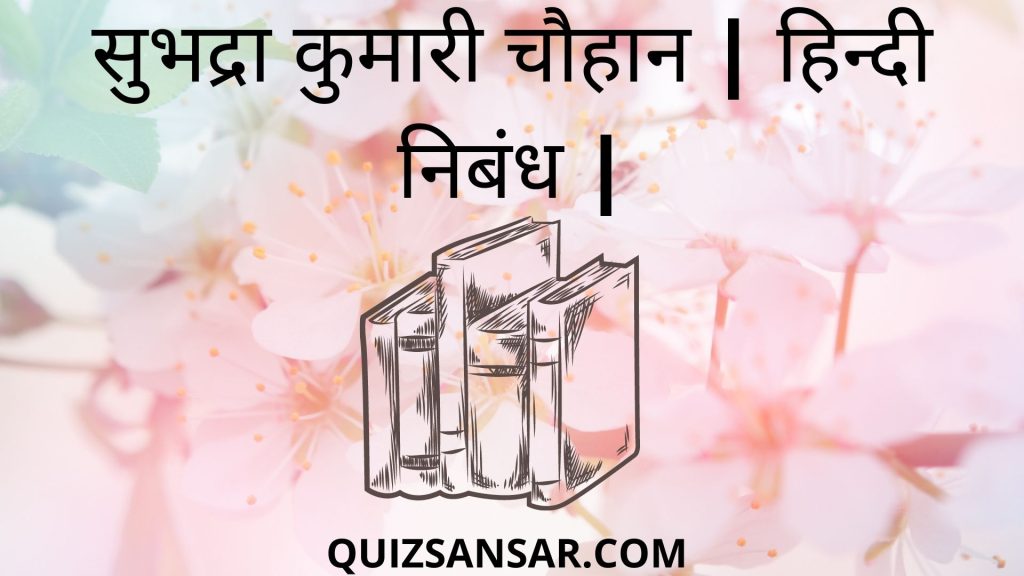
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- काव्य विशेषताएं
- भाषा
- शैली
- रस, छंद एवं अलंकार
- उपसंहार
जीवन वृत्त
सुभद्रा जी का जन्म प्रयाग में सन् 1904 ई० में हुआ था। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह ने इनकी शिक्षा की व्यवस्था ब्राथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में की थी।
15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह खण्डवा निवासी ठा० लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ सम्पन्न हो गया था। विवाहोपरान्त काशी में इनका अध्ययन पुनः प्रारम्भ हुआ।
परन्तु असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी और शिक्षा फिर बीच में ही छूट गई।
ये आजीवन देश-सेवा में लगी रहीं। मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये ये सदस्य निर्वाचित हुई।
सन् 1947 ई० में, विधान सभा जाते हुए मुर्गी के बच्चों की प्राण रक्षा के लिये कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई।
रचनायें
सुभद्रा जी की रचनायें तीन रूपों में उपलब्ध होती हैं-
- काव्य
- कहानी
- बाल साहित्य
‘मुकुल’ तथा‘त्रिधारा’ इनकी काव्य-कृतियाँ हैं। ‘मुकुल’ पर इन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से “सेक्सरिया पुरस्कार”: प्राप्त हुआ था।
‘बिखरे मोती’ तथा ‘उन्मादिनी’ इनके कहानी संग्रह हैं। ‘सभा के खेल’ तथा ‘सीधे-सादे चित्र’ इनके बाल साहित्य सम्बन्धी ग्रंथ हैं।
काव्य विशेषतायें
सुभद्रा जी की रचनाओं में तीन भावों का प्रतिपादन हुआ है-
- राष्ट्र भक्ति
- वात्सल्य-प्रेम
- प्रणय-भावना
राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत रचनाओं में सुभद्रा जी को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई।
इनकी कुछ रचनाओं में भारतीय विगत वैभव शौर्य एवं पराक्रम के दर्शन होते हैं, ‘जलियों वाला बाग’, ‘वीरों का कैसा हो: बसन्त’, ‘झांसी की रानी’ आदि रचनायें इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
‘झांसी वाली रानी’ की कविता तो देश के सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों में गले का हार है ही। इनकी लेखनी की शक्ति के दो उदाहरण देखिये-
भूषण अथवा कवि चन्द नहीं,
बिजली भर दें वह छन्द नहीं,
है कलम बेंबी स्वच्छन्द नहीं
फिर हमें बतावे कौन हन्त !
वीरों का कैसा हो वसन्त ?
मातृ भूमि की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली महारानी लक्ष्मी बाई की समाधि को देखकर सुभद्रा जी कह उठीं-
बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से।
मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से।।
रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी।
यहाँ निहित है स्वतन्त्रता की आशा की चिंगारी ।।
वात्सल्य एवं प्रणय सम्बन्धी रचनाओं में सुभद्रा जी की नारी सुलभ भावुकता का प्राधान्य है, वासना के स्थान पर त्याग और आत्म समर्पण की भावना है।
वात्सल्य भावना में बालिका का हृदय-स्पर्शी चित्र देखिये-
ओ माँ, कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आयी थी।
कुछ मुँह में, कुछ लिये हाथ में, मुझे खिलाने आयी थी।
दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा-सी उजियाली,
ऊपा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली।
मर्मस्पर्शी आत्म समर्पण-
पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो,
दान, दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो।
भाषा
सुभद्रा जी की भाषा सरल, सुबोध एवम् सरल खड़ी बोली है। उसमें कला के कृत्रिम सौन्दर्य और कल्पना की ऊँची उड़ानों का अभाव है।
भावों की भाँति भाषा भी आडम्बरहीन और स्वाभाविकता से युक्त हैं। भाषा में ओज, प्रसाद एवम् माधुर्य गुण सर्वत्र विद्यमान है।
अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, उन्हें लाने का कोई प्रयास एवम् प्रयत्न नहीं किया गया। उर्दू के प्रचलित शब्द भी ग्रहण किये गये हैं।
शैली
काव्य के क्षेत्र में इनकी शैली सरल, मधुर एवम् प्रभावशालिनी है। कहानी के क्षेत्र में शैली भावात्मक एवम् वर्णनात्मक है।
रस, छन्द एवम् अलंकार
वात्सल्य एवं वीर रस की निष्पत्ति बड़े सजीव ढंग से की गई है। छन्द-योजना में आधुनिक तुकान्त छन्दों का प्रयोग किया गया है।
अर्ध-बोध के सहायक के रूप में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आये हैं, उनके लिये कोई श्रम या प्रयास नहीं किया गया।
उपसंहार
‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी’ की लेखिका को ऐसा कौन है जो न जानता हो।
इसी एक कविता ने सभी आबाल-वृद्धों से सुभद्रा जी का परिचय करा दिया।
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को और कुछ बाद हो या न हो पर यह कविता अवश्य याद होगी।
हिन्दी साहित्य में राष्ट्र प्रेम से पूर्ण काव्यकारों में सुभद्रा जी का विशेष स्थान है और महिला काव्यकारों में तो प्रथम |
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
इसे भी पढ़ें
सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन वृत्त क्या है ?
सुभद्रा जी का जन्म प्रयाग में सन् 1904 ई० में हुआ था। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह ने इनकी शिक्षा की व्यवस्था ब्राथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में की थी।
15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह खण्डवा निवासी ठा० लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ सम्पन्न हो गया था। विवाहोपरान्त काशी में इनका अध्ययन पुनः प्रारम्भ हुआ।
परन्तु असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी और शिक्षा फिर बीच में ही छूट गई।
ये आजीवन देश-सेवा में लगी रहीं। मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये ये सदस्य निर्वाचित हुई। सन् 1947 ई० में, विधान सभा जाते हुए मुर्गी के बच्चों की प्राण रक्षा के लिये कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई।
सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा क्या थी ?
सुभद्रा जी की भाषा सरल, सुबोध एवम् सरल खड़ी बोली है। उसमें कला के कृत्रिम सौन्दर्य और कल्पना की ऊँची उड़ानों का अभाव है।
भावों की भाँति भाषा भी आडम्बरहीन और स्वाभाविकता से युक्त हैं। भाषा में ओज, प्रसाद एवम् माधुर्य गुण सर्वत्र विद्यमान है।
अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, उन्हें लाने का कोई प्रयास एवम् प्रयत्न नहीं किया गया। उर्दू के प्रचलित शब्द भी ग्रहण किये गये हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान की शैली कैसी थी ?
काव्य के क्षेत्र में इनकी शैली सरल, मधुर एवम् प्रभावशालिनी है। कहानी के क्षेत्र में शैली भावात्मक एवम् वर्णनात्मक है।
सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाये कौन-कौन सी हैं ?
कहानी
बाल साहित्य
यह भी जाने
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
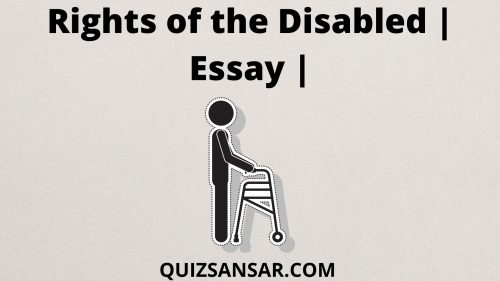
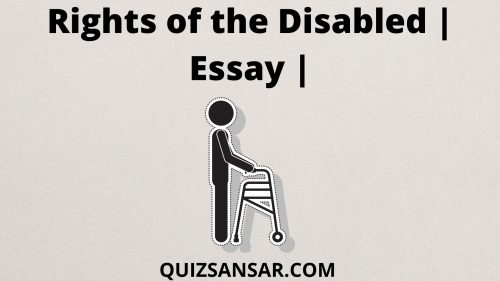
Rights of the Disabled | Essay |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है Rights of the Disabled | Essay | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
“Disability is a class in itself that any one may fall victim at any time. It can come about as a result of a sudden accident, a fall down a flight of stairs or disease. Disability maintains no socio-economic boundaries. Since disability catches up with most people in its fold in old age, it is a class that any of us may fall in it someday.”
Even today the disabled in India see their physical or mental limitations as either a source of shame or a source of inspiration for others. By concentrating on overcoming the disability, we fail to notice that a disability itself cannot be overcome by a disabled person, however, heroic she or he may be. In the West, the Disability Rights Movement has realised this and, therefore, they proclaim that “it is okay, even good, to be disabled”.
The Disability Rights Movement
Unlike other movements like Feminism or Lesbian Movements which have distinct agendas of either gender justice or the right to sexual orientation, the Disability Rights Movement does not have systematic path. Disability Rights Movement even in the West has a very recent origin and tries to draw strength from the traditional legal order rather than by critiquing or deconstructing it. Joseph Shapiro neatly summarises the characteristics of this movement in the West –
“The disability movement is a mosaic movement for the 1990s. Diversity is its critical characteristic. No leader or organisation can claim to speak for all the disabled”.
The Disability Rights Movement in India and in Third World countries is discursive and disorganised and there is no written documents to trace its origin. Instead of coming together, sections of disabled viz. blind persons, persons with physical disability, deaf and dumb persons and those with mental disabilities have launched their movements and struggles separately, mainly through NGOs.
It was all the much difficult for all disabled groups to come together with the stupendous diversities in their problems. Two important reasons can be assigned for such a scenario. Firstly, in our country, the disabled are bound to struggle to fulfil the basic needs like food, shelter and education and therefore, they are bound to be disable specific in their struggles. Secondly, the Advocates of Disability Rights in India do not have any coherence in their agenda, some stress solely on Rehabilitation and Research, others are solely concerned with generation of employment and still others are wholly occupied by efforts in the education sector.
A few in India ever talk of about the ‘Civil Rights’ or Crisis of Identity’ of the disabled. Under such circumstances the various groups have to work segregated, and so they could not come together chalk out a common agenda.
Actually in India the Disability Rights Movement has been launched by NGOs and therefore, a large number of NGOs have mushroomed all over the country. Instead of working together to strengthen the movement, there is often seen unwarranted and unhealthy rivalry between NGOs. Similar conflicts was also noted across different sections of the disabled. While there are a number of organisations making serious rehabilitation efforts and genuinely working for the upliftment of the disabled there are also NGOs that are simply cashing in on the cause just trying to pocket the funds and doing nothing for the disabled.
Assumptions about the disabled
Some stereotyped presumptions prevailed about the disabled in our country like –
- Disabled people are the most vulnerable section of society and have been ignored by state and society alike since long.
- Disabled people have always been dependent and, therefore, need helping hands and gracious charity.
- Disabled people are victims of their own bad luck.
- Disableness is the punishment for sins he has never committed in this life.
Such assumptions about the disabled do nothing to help them. This approach perpetuates the stereotype of the disabled as victims and objects of pity and charity.
Persons with disability are considered to have a very small sphere to operate within owing to their limitations. So if a disabled person achieves something beyond his/her small sphere’ he/she is considered to have almost overcome his/her disability. He/She is then presented as a role model and a source of inspiration for the non disabled community even. This image hits the average disabled person very hard who does not have the capacity to live up to such heroic standards. Average disabled people tend to compare their ‘little successes to the large successes’ of his fellow disabled. This leads to an inferiority complex among them.
Government’s Solace for the disabled
Until 1995 there was no law that even defined discrimination against people with disabilities. It is only with the Persons with Disabilities Act,’ passed in 1995 that discrimination specifically against persons with disabilities came under the purview of the law.
Till 1995, most of the welfare measures taken by the States were by way of affirmative action. The Ministry of Social Welfare was largely concerned with problems of persons with disability and with providing them privileges.
Rehabilitation of people with disability by opening shelter workshops and educational and research institutions like the National Institute of Visually Handicapped, Dehra Dun, the National Institute for the Mentally Handicapped ,
Secunderabad, the National Institute for the Orthopaedically Handicapped , Calcutta and the Ali Anwar Jung National Institute for Hearing Handicapped, Mumbai providing basic education to individuals with disability by funding NGOs, opening special schools and awarding scholarships for students with disability, providing employment through job reservations mainly in Class 3 and 4 in Central and State Government Departments and giving disabled people travel concessions and installing awards for disabled workers and institutions working for the welfare of the disabled . During early 80’s some major developments in the International Disability Rights Movement brought about a change in the attitude of the Government of India.
The first carnest sign was the enactment of the “Mental Health Act, 1987”. The Act is aimed at protecting mentally ill persons in matters of admission and detention in psychiatric hospitals and the custody of his/her persons, his/her property and its management and human rights.
Persons with Disabilities Act 1995
A meeting was convened by the Economic and Social Commission for the Asia Pacific region in Beijing in December 1992 to launch the Asia-Pacific decade of disabled persons. The meeting declared 1993-2000 as the Asia-Pacific decade and proclaimed the –
“full participation and equality of people with disabilities”
as the objective. To give legislative effect to the above proclamation, the ‘Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Civil Rights, and Full Participation) Act was enacted in India in 1995 and came into force on 1st January 1996.
Objectives of the Act
To spell out the responsibility of the State towards the prevention of disabilities, protection of rights, provision of medical care, education, training, employment and rehabilitation of persons with disabilities.
- To create a barrier-free environment for disabled persons.
- To remove any discrimination against disabled people in the sharing of development benefits vis-à-vis non-disabled persons.
- To counteract any situation of abuse and the exploitation of disabled persons.
- To lay down strategies for the development of comprehensive programmes and services and the equalisation of opportunities for disabled persons.
- To make special provisions for the integration of persons with disabilities into the social mainstream.
Critics
A close study of the Act makes us feel –
“as if the Government is a gracious donor and disabled persons are absolute dependents”.
This is a major stumbling block in the process of providing equal opportunities to the disabled. Instead of focussing on the capabilities of disabled people, the Act focuses very much on activity limitations of the disabled and perpetuates the victim image of disabled people.
Unfortunately the Act does not pay any serious attention to securing some basic rights like the right to human dignity, right to equal concern and respect, right against discrimination in public employment and educational institutions, right against exploitation, right against victimisation etc.
The Acthas completely ignored some vital aspects such as:Pre-school education of disabled children, special problems of the parents of the disabled, special problems of the female disabled, games, sports and cultural activities, exploitation of disabled by their own families, higher education of the disabled .
Although the implement of the Act has been gradual, it does not mean that the Act has not helped the disabled at all. It has provided a platform to unite and mobilize disabled individuals across the country. It is also significant to witness the participation of the disabled in decision-making processes through their representation in various policy making and shaping bodies under the Act.
The success of this Act would, however, depend much upon the extent to which the political leaders and bureaucratic executive internalises the values, sensibilities and goals enshrined in the Act. If persons with disability are to be regarded as full citizens of India, their right to equal concern and respect must find its expression in the supreme law of the land.
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
What is the Disability Rights Movement?
“The disability movement is a mosaic movement for the 1990s. Diversity is its critical characteristic. No leader or organisation can claim to speak for all the disabled”.
What was the purpose of the Act?
To create a barrier-free environment for disabled persons.
To remove any discrimination against disabled people in the sharing of development benefits vis-à-vis non-disabled persons.
To counteract any situation of abuse and the exploitation of disabled persons.
To lay down strategies for the development of comprehensive programmes and services and the equalisation of opportunities for disabled persons.
To make special provisions for the integration of persons with disabilities into the social mainstream.
What was the government’s consolation for the disabled?
Till 1995, most of the welfare measures taken by the States were by way of affirmative action. The Ministry of Social Welfare was largely concerned with problems of persons with disability and with providing them privileges.
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
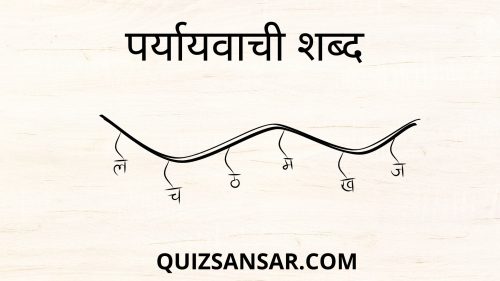
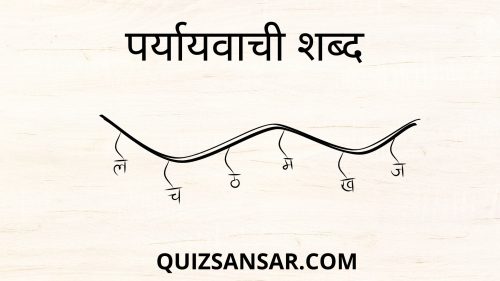
पर्यायवाची शब्द | Paryavachi Shabd |
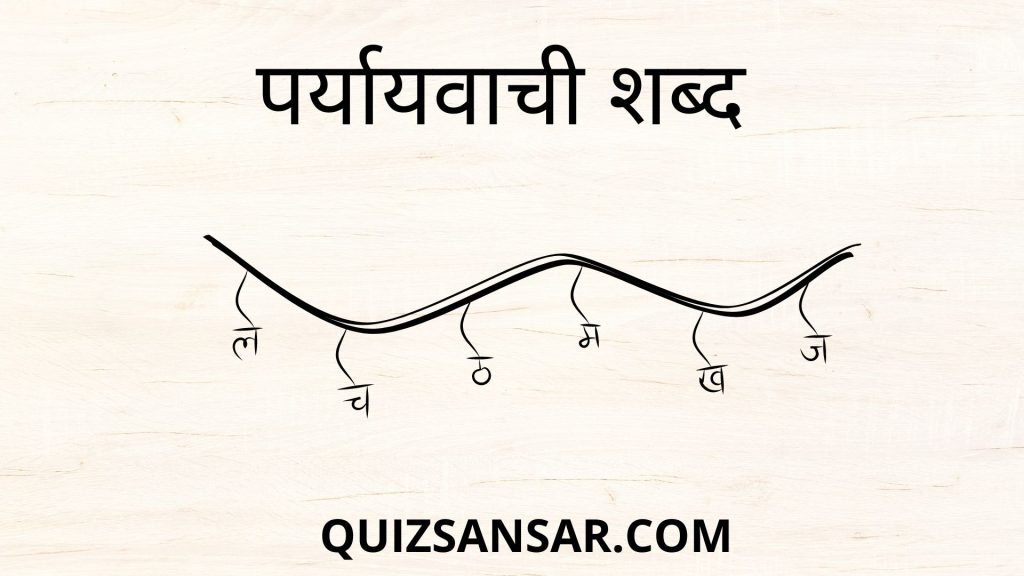
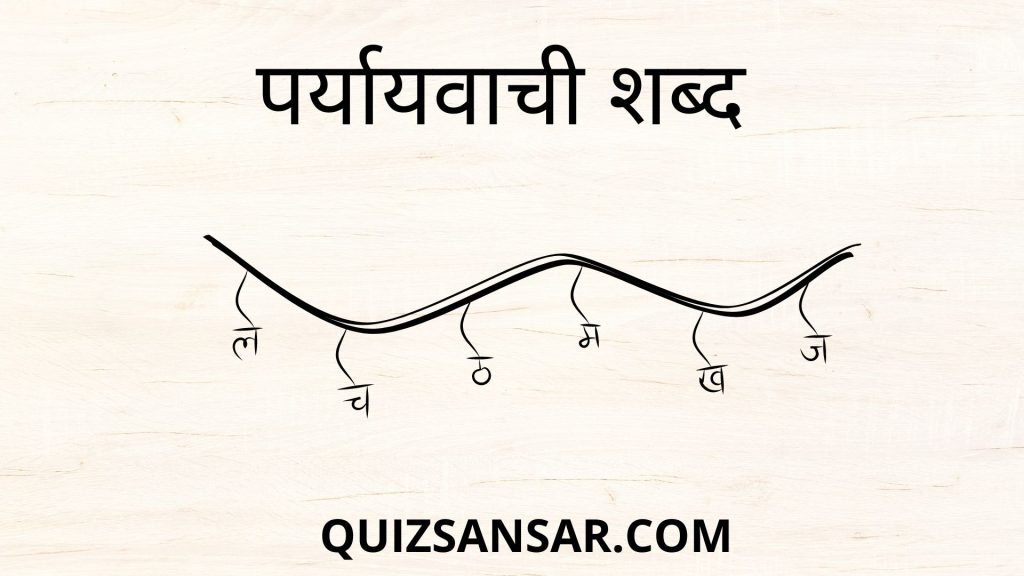
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है पर्यायवाची शब्द | Paryavachi Shabd | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ को समानता होती है, फिर भी प्रत्येक विशिष्टता अवश्य लिए होता है। इसीलिए प्रत्येक शब्द कुछ-न-कुछ पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रत्येक स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
यह कथन उचित है कि पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों, किन्तु इनमें सूक्ष्म अर्थगत अन्तर होता है। जैसे–जल और पानी एक-दूसरे के पर्यायवाची है, किन्तु जल का प्रयोग पूजा में होता है तथा पानी का प्रयोग पीने के लिए या खेत की सिंचाई के लिए होता है। जल में जो पवित्रता एवं स्वच्छता का भाव निहित है, वह पानी में नहीं है। अतः इनमें अर्थगत सूक्ष्म अन्तर विद्यमान है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय एवं स्थान के अनुसार ही होती है।
पर्यायवाची शब्द के भेद
- पूर्ण पर्याय |
- पर्णापूर्ण पर्याय |
- अपूर्ण पर्याय |
पूर्ण पर्याय
जब वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाये और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे ‘पूर्ण पर्याय’ कहते हैं, जैसे-अग्नि, दहन आदि।
पर्णापूर्ण पर्याय
जब किन्हीं दो समानार्थी शब्दों का प्रयोग किसी कार्य-विशेष के प्रसंग में किया जाये, परन्तु एक शब्द दूसरे समानार्थी के प्रसंग में असमान अर्थ प्रकट करे, तो ‘पर्णापूर्ण पर्याय’ का बोध प्रकट होता है, जैसे-अभिलाषा, मर्जी आदि।
अपूर्ण पर्याय
जब दो समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अन्तर प्रकट हो तथा दोनों के भाव तथा अर्थ में भिन्नता प्रकट हो, तो उन्हें ‘अपूर्ण पर्याय’ कहते हैं। किन्तु अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है, जैसे-घर, भवन आदि।
महत्त्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द
(अ, आ, इ,……)
- अंग अंश, अवयव, हिस्सा, भाग।
- अंधकार तम, तमिस्रा तिमिर, ध्वात।
- अग्नि पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वहि, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृशानु, जातदेव, आग
- अनुपम अनुण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भूत, अतुल, अनोखा
- अन्वेषण अनुसंधान, खोज, गवेषण, जाँच, छानबीन, पूछताछ, शोध
- अभिमान अस्मिता, अहं, अहंकार, अहंभाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान।
- अमृत सोम, सुधा, अमिय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग
- अरण्य जंगल, वन, कानन, अटवी, कान्तार, विपिन
- अश्व तुरंग, हय, घोड़ा, घोटक, बाजि, सैन्धव
- असुर दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, रजनीचर, यातुधान, इन्द्रारि, तमीचर, निशाचर, सुरारि
- अनी कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनीकिनी।
- आँख नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षि
- आँगन अंगना, अजिरा, प्राङ्गण
- आकाश गगन, नभ, अम्बर, व्योम, अन्तरिक्ष, अनन्त, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यौ, तारापथ।
- आनन्द सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास आह्लाद।
- आम आम्र, रसाल, पिकबन्धु, सहकार, अतिसौरभ, अमृतफल |
- आश्रम मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ।
- इच्छा आकांक्षा, वाञ्छा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, ईहा, वासना
- इन्द्र सुरपति, देवराज, महेन्द्र, मधवा, शचीपति, पुरन्दर, सुरेश, देवेन्द्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव।
- इन्द्राणि इन्द्रवधू, इन्द्राणी, मधवानी, शची, शतावरी, पोलोमी।
- ईश्वर परमात्मा, परमेश्वर, भगवान ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनन्त, जगन्नाथ, परमेश, जगतप्रभु।
- उक्ति कथन, वचन, सूक्ति
- उग्र प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट।
- उचित ठीक, मुनासिब वाजिब समुचित युक्तिसंगत, न्यायसंगत, तर्कसंगत, योग्य।
- उच्छृंखल उद्दड, अक्खड़, आवारा, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी।
- उजड्ड अशिष्ट, असभ्य, गँवार, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश |
- उजला उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल |
- उजाड़ जंगल, बियावान, वन।
- उजाला प्रकाश, रोशनी, चांदनी ।
- उत्कर्ष समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान।
- उत्कृष्ट उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा
- उत्कोच घूस, रिश्वत
- उत्पत्ति उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय |
- उद्धार मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई।
- उपाय युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न
- ऊधम उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़।
- ऋषि मुनि, साधु, यती, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी |
- ऐक्य एकत्व, एका, एकता, मेल |
- ऐश्वर्य समृद्धि, विभूति।
- ओज तेज, शक्ति, बल, वीर्य |
- औचक अचानक, यकायक, सहसा |
- औरत स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली।
(क वर्ग)
- कपड़ा चीर, बसन, पट, अम्बर, वस्त्र ।
- कमल कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अम्बुज, वारिज, इन्द्रीवर, राजीव, उत्पल, अरविन्द ।
- कामदेव काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचशर, मन्मथ, रतिपति, मनसिज, मीनकेतु, मकरध्वज
- कार्तिकेय कुमार, षडानन, शरभव, स्कन्द |
- किरण रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा |
- कुबेर अनद, यक्षराज, धनाधिप, किन्नरेश, राजराज |
- कोकिल कोयल, पिक, बसन्तद्, कोकिला, परभूत |
- कपोत कबूतर, हारीत, रक्तलोचन।
- कुत्ता श्वा, श्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेव |
- कृष्ण मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर केशव वासुदेव, नन्दनन्दन, राधारमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीघर, द्वारिकाधीश यदुनन्दन, कंसारि, रणछोड़, बंशीधर |
- कल्पद्रुम देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मन्दार, हरिचन्दन ।
- काक कौआ, वायस, काग, करठ, पिशुन।
- कृपा दया, अनुग्रह, अनुकम्पा |
- क्रोध कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश |
- खग विहग, विहंग, चिड़िया, पंछी, शकुनि, पक्षी, द्विज, पखेरू ।
- खम्भा स्तूप, स्तम्भ, खम्भ |
- खल दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल |
- खून रक्त, लहू, शोणित, रुधिर |
- गंगा सुरसरि, सुरसरिता, अमरतरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी ।
- गणेश गणपति, गजबदन, गजानन लम्बोदर एकदन्त, भवानीनन्दन, वक्रतुण्ड, गौरीसुत, मोदकप्रिय, विनायक।
- गरुड़ खगेश, पन्नगारि, उरगारि, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख।
- गधा खर, गर्दभ, बैसाखनन्दन, रासभ, धूसर, वेशर, चक्रीवान।
- गाय गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। घड़ा, कलश, कुम्भ, निपा
- घट घड़ा, कलश, कुम्भ, निप |
- घर आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन।
- घृत घी, अमृत, नवनीत
- घास तृण, दुर्वा, दूब, कुश, शाद।
च वर्ग
- चतुर विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य |
- चन्द्रमा सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इन्दु, मृगांक
- चंद्रिका चाँदनी, ज्योत्स्ना, कौमुदी।
- चांदी रजत, सौध, रूपा, रूपक, रौप्य, चन्द्रहास।
- चोटी मूर्धा, शीश, सानु श्रृंग
- चोर खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोषक
- छतरी छत्र, छाता, छत्ता |
- छली छलिया, कपटी, धोखेबाज |
- छवि शोभा, सौंदर्य, काति, प्रभा |
- छैला सजीला, बाँका, शौकीन।
- छोर नोक, कोर, किनारा, सिरा |
- जल पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक, वारिय |
- जंगल विपिन, कानन, अरण्य, वन।
- जहाज पोत, जलयान।
- झरना उत्स, स्रोत, प्रताप, निर्झर, प्रस्त्रवाणा |
- झण्डा ध्वजा, पताका, केतु।
(ट वर्ग)
- टक्कर मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला।
- टहलुआ नौकर सेवक, खिदमतगार |
- टांग पाँव पैर टंक
- टीका तिलक, चिह्न, दाग, धब्बा
- टोना टोटका, जादू, यंत्रमंत्र, लटका।
- ठंड शीत, सर्दी।
- ठग छली, धूर्त, धोखेबाज |
- ठाँव स्थान, जगह, ठिकाना।
- ठिगना बौना, वामन, नाटा।
- ठीक उपयुक्त, उचित, मुनासिब |
- ठेठ निपट, निरा, बिल्कुल |
- डंडा सोटा, छड़ी, लाठी।
- डाली भेट, उपहार।
- ढब ढंग, रीति, तरीका, ढर्रा
- ढांचा पंजर, ठठरो।
- ढील शिथिल, सुस्ती, अतत्परता।
- ढूंढ खोज, तलाश |
- ढोर चौपाया, मवेशी |
त वर्ग
- तरकस तूण, तूणीर, त्रोण, निषेग, इषुधी |
- तलवार असि, करवाल, चन्द्रहास, खड्ग, कृपाण, शमशीर |
- तालाब सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृद , सरसी |
- तामरस कमल, पंकज, सरसिज, नीरज, पुण्डरीक, इन्दीवर |
- तिमिरी तम, अंधकार, अंधेरा, तमिस्त्रा।
- तीर शर, बाण, सायक, नाराच, शिलीमुख।
- तोता शुक्र, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुण्ड, दाड़िमप्रिय।
- थोड़ा अल्प, न्यून, जरा, कम।
- थाती जमापूँजी, घरोहर, अमानत ढेर, समूह।
- थप्पड़ तमाचा, झापड़।
- दया अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना ।
- दांत दन्त, दशन, द्विज, रद, रदन।
- दास नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचारक, किकर |
- दिन दिवा, दिवस, वासर |
- दीन दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन।
- दुःख शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा, व्यथा |
- दुर्गा चण्डिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी ।
- दूध दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत |
- देव अमर, देवता, सुर, निर्जर, वृन्दारक, आदित्य |
- द्रव्य धन, सम्पत्ति, दौलत, विभूति, सम्पदा, वित्त |
- धन द्रव्य, वित्त, दौलत, सम्पदा, सम्पत्ति, विभूति |
- धनुष धनु, कोदण्ड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान।
- धरती भू, धरा, पृथ्वी, अवनि, वसुधा, वसुन्धरा, मेदिनी, इला |
- नदी सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरिणी, निम्नगा, वाहिनी।
- नर्क यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय।
- नर जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज |
- नाव नौका, पतंग, तरणि, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान।
- निंदा दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना ।
- नेत्र चक्षु, लोचन, नयन, अक्षि, चख, आँख |
प वर्ग
- पती नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश |
- पत्नी कान्ता, भार्या, वल्लभा, अर्द्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, तिय, प्राणप्रिया, जाया।
- पत्थर पाहन, पाषाण, प्रस्त उपल।
- पथ मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता।
- पर्वत पहाड़, गिरि, शैल, अचल, नग, भूधर, महिघर, धराधर |
- पार्वती गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्या, अम्बिका।
- पिता जनक, तात, पितृ, बाप।
- पुत्र बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नन्दन, पूत, नन्द।
- पुत्री बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नन्दिनी, तनुजा, दुहिता |
- पृथ्वी भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनि, मेदिनी, वसुन्धरा, उर्वी |
- पवन वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान, मारुता |
- पंडित बुध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण।
- पुष्प प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, फूल |
- पुरुष आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव, मानुष |
- प्रकाश ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति |
- पेड़ तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रूक्ष |
- पैर पाँव पद, चरण, पाद, पग |
- पक्षी विहग, विहंग, खग, पखेरू, परिन्दा, पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून, द्विज, पतंग
- बगीचा बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी |
- बन्दर कपि, मर्कट, कीश, बानर, हरि, शाखामृग |
- बाण सर, वीर, सायक, विशिख, शिलीमुख, नाराच |
- बादल घन, जलद, जलघर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर |
- बाल कच, केश, चिकुर, चूल |
- बिजली चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजुरा, क्षणप्रभा, घनवल्ली।
- ब्रह्मा विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंचि, अज, कर्तार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ |
- बलदेव बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिणेया |
- बहुत अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अत्यन्त, असंख्या |
- ब्राह्मण द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिसुर, भूमिदेव।
- भय भीति, डर, विभीषिका।
- भौंरा मधुप, मधुकर, द्विरेप, अलि, षट्पद, भृंग, भ्रमर।
- भाई तात, अनुज, अग्रज प्राता, भ्राता |
- मछली मत्स्य, मीन, झख, सफरी, जलजीव |
- मदिरा शराब, मद्य, मधु, हाला, आसव, वारुणी, सुरा।
- मनुष्य नर, मानव, मनुज, मानुष, जन, आदमी।
- महादेव शिव शम्भ शंकर, कैलाशनाथ, उमापति, शम्भू, महेश, आशुतोष चन्द्रशेखर, पशुपति ।
- माँ अंबा, अम्बिका, अम्मा, जननी, धात्री , प्रसू |
- मेघ घन, बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, वारिधर, पयोधर, जलजीवन, अभ्र |
- मुर्गा तमचूक, अरुणशिखा, ताम्रचूड, कुक्कुट |
- मोर केकी, शिखी, शिखण्डी, नीलकंठ, मयूर, कलापी।
- मोक्ष मुक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, परमधाम, परमपद, सद्गति, निर्वाण |
- मग पन्थ, मार्ग, बाट, पथ, राह।
- मृत्यु निधन, मरण, मौत, देहान्त, देहावसान, पंचत्व, इतकाल, काशीवास, गंगालाभ, निर्वाण, स्वर्गवास |
- मीत सहचर, सखा, सहद, सपक्ष, मित्र।
- मूढ़ मूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार |
- मैना सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरालाषा |
- मूंगा प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि।
(य, र, ल, व)
- यम सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अन्तक, धर्मराज, दण्डघर, कीनाश।
- यमुना कालिन्दी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणि-तनुजा, तरणिजा, अर्कजा, भानुजा |
- युवती सुन्दरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना |
- रमा इन्दिरा, हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी, कमला पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्रीभार्गवी, क्षीरोदतनया।
- राजा भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेन्द्र, नृप, नरनाह।
- रात्री निशा, क्षया, रैन, रात, यामिनी, शर्वरी, तमस्विनी, विभावरी ।
- रामचंद्र अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुबीर, रावणारि, जानकीवल्लभ, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन।
- रावण दशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीश, दशकंघ, दैत्येन्द्र ।
- राधिका राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा |
- लड़का बालक, शिशु, सुत, किशोर कुमार।
- लड़की बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला।
- लता बल्लरी, बल्ली, बेली।
- लक्ष्मी रमा, कमला, इन्दिरा, श्री, कमलासना, पद्मा, पद्मजा, सिन्धुसुता |
- लक्ष्मण लखन, शेषावतार, सौमित्र, रामानुज, शेष।
- लौह अयस, लोहा, सार |
- वर्षा पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षाऋतु।
- वसंत मधुमास, माघव, कुसुमाकर, ऋतुराजा |
- विष्णु माधव, केशव, गोविन्द, चतुर्भुज, उपेन्द्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, नारायण, मधुरिपु |
- वायु हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत |
- वसन अम्बर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर।
- विधवा अनाथा, पतिहीना, राँड |
- विश्व जगत, जग, भव, संसार, लोक, दुनिया।
- विद्युत चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बीजुरी, घनवल्ली, क्षणप्रभा, करका |
- वारिश वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस, बरसात।
- वीर्य जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज।
- वज्र कुलिस, पवि, अशनि, दभोलि |
- विशाल विराट, दीर्घ, वृहत्, बड़ा, महा, महान।
- वृक्ष गाछ, तरु, पेड़, द्रुम, पादप, विटप, शाखी।
(श,ष, स, ह)
- शरीर देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया।
- शत्रु विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र, रिपु |
- शेर केहरि, केशरी, वनराज सिंह, शार्दूल, हरि, मृगराज |
- शेषनाग अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणीश, सारंग |
- शुभ्र गौर, श्वेत, अमल वलक्ष, धवल शुक्ल, अवदात |
- शहद पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरन्द |
- षन्ड हिंजड़ा , नपुंसक, नामर्द।
- षडानन षद्मुख, कार्तिकेय, षाण्यातुर ।
- सभा अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा |
- सर्प अहि, नाग, भुजंग, विषघर, व्याल, उरग, पन्नग, साँप, सारंग।
- स्वर्ण सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, सोना, तामरस, हिरण्या |
- सरस्वती गिरा, शारदा, भारती, वीणापाणि, विमला, वागीश, वागेश्वरी।
- समुद्र सागर, सिन्धु, उदधि, नदीश, वारीश, अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधी, अर्णव तोयनिधि, सरित्पति।
- सूर्य दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणि, पतंग, आदित्य, सविता, हस, अंशुमाली, मार्तण्ड |
- सम सर्व , समस्त , सम्पूर्ण, पूर्ण, समय, अखिल, निखिल |
- समूह दल, झुण्ड, समुदाय, टोली, जत्था, मण्डली, वृन्द, गण, संघ, समुच्चय |
- सिंह शेर, केहरि, मृगेन्द्र, मृगराज, केशरी, नखायुध, बहुबल, व्याघ्र |
- सुन्दर कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य |
- संध्या सायकाल, शाम, साँझ, प्रदोषकाल, गोधूलि
- स्त्री सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता |
- स्वर्ग सुरलोक, देवलोक, दिव्यघाम, बह्मभोज हाघाम |
- सीता वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनकतनया, जनकनन्दिनी, रामप्रिया।
- सहेली आली. सखी सहचरी, सजनी सैरन्ध्री।
- संसार लोक, जग, जहान, जगत, विश्व समीप सन्निकट, आसन्न निकट, पास।
- सेना ऊनी, कटक, दल, चमू, अनीक, अनीकिनी।
- साधू सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलोन।
- सलिल अम्बु, जल, नौर, तोय, पानी, वारि |
- सगर्भ बन्धु , भाई, सजात, सहोदर, भ्राता, सोदर ।
- सगर्भा भगिनी, सजाता, सहोदरा |
- हांथी कुजर, गज, हस्ति, करि, नाग, मतंग, दन्ती, वारण।
- हिमालय नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्रि, हिमगिरि, गिरिराज |
- हिरण सुरभी, कुरंग, मृग, सारंग, हिरन |
- होंठ अधर, ओष्ठ, ओठ।
- हनुमान पवनसुत पवनकुमार, महावीर, अंजनीपुत्र, रामदूत , मारुततनय, आजनेय, कपीश्वर, केशरीनंदन, बजरंगबली, मारुति।
- हिमांशु हिमकर निशाकर, क्षपानाथ, चन्द्रमा, चन्द्र निशिपति।
- हंश कलकंठ, मराल, सिपपक्ष, मानसौका |
- ह्रदय उर, छाती, वक्ष, हिय, हिया |
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
सलिल की पर्यावाची क्या होती है ?
गरुड़ की पर्यावाची क्या होती है ?
पूर्ण पर्याय किसे कहतें हैं ?
पर्यावाची किसे कहतें हैं ?
यह कथन उचित है कि पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर भले ही समानार्थी हों, किन्तु इनमें सूक्ष्म अर्थगत अन्तर होता है। जैसे–जल और पानी एक-दूसरे के पर्यायवाची है, किन्तु जल का प्रयोग पूजा में होता है तथा पानी का प्रयोग पीने के लिए या खेत की सिंचाई के लिए होता है। जल में जो पवित्रता एवं स्वच्छता का भाव निहित है, वह पानी में नहीं है। अतः इनमें अर्थगत सूक्ष्म अन्तर विद्यमान है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय एवं स्थान के अनुसार ही होती है।
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |


पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
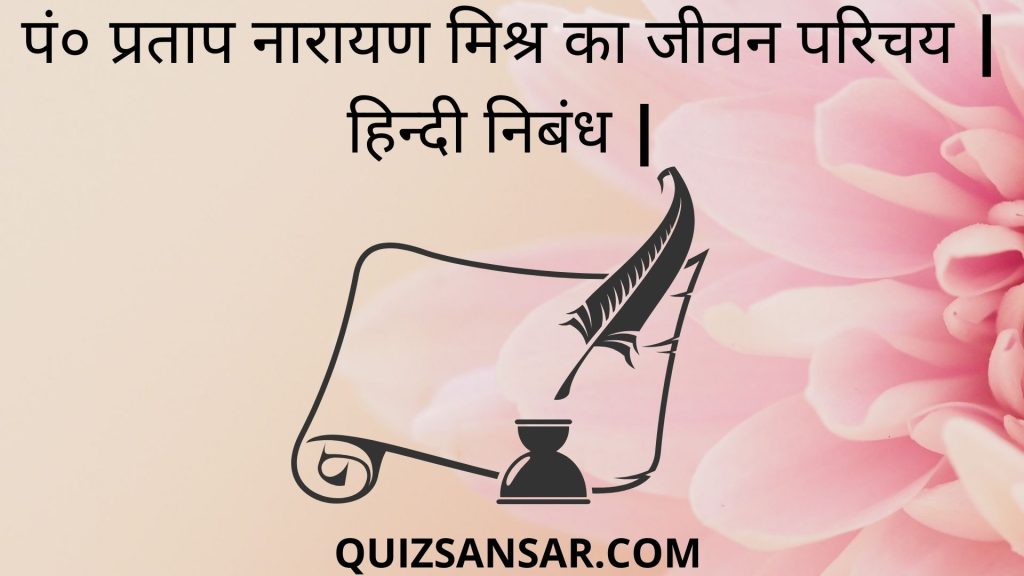
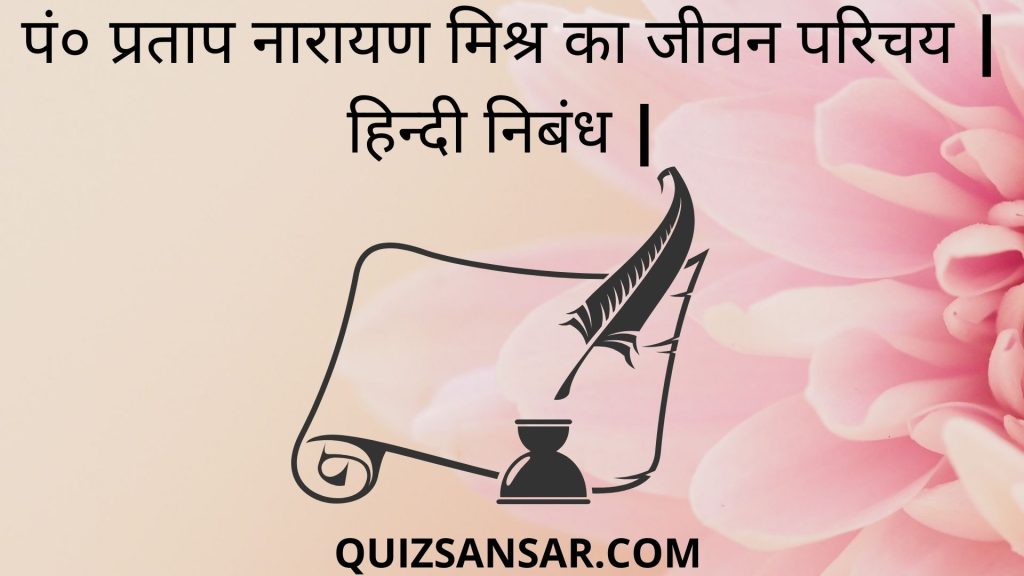
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- परिचय
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- भाषा
- शैली
परिचय
भारतेन्दु युग में उत्पन्न होकर भी उस समय के विकास और परिष्कार से सिंह और सपू की भाँति यदि कोई लेखक अप्रभावित रहा तो वह पं० प्रताप नारायण मिश्र ही थे।
उन्हें अपना अक्खड़पन और मनमौजीपन, मस्ती और सैलानीपन ही पसन्द था। व्यंग्य-विनोद उनकी प्रकृति के मुख्य तत्व थे, चिन्तन और विचार उनके स्वभाव के विपरीत थे।
हिन्दी और हिन्दी साहित्य को पिटारे में बन्द न करके वे सामान्य जन जीवन के बीच में खींच लाये थे।
निःसन्देह प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिन्दी भाषा-भाषी समाज का तथा स्वयं हिन्दी के प्रचार और प्रसार का उस समय बहुत बड़ा काम किया था, जबकि खड़ी बोली हिन्दी अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
जीवन वृत्त
पं० प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे गाँव में सन् 1856 में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० संकटा प्रसाद था।
प्रताप नारायण मिश्र ke पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गये थे और ज्योतिष का काम करते थे। वे अपने पुत्र को ज्योतिषी ही बनाना चाहते थे परन्तु प्रताप नारायण की रुचि गणित के शुष्क अंकों में न रमी।
प्रताप नारायण मिश्र बचपन से ही स्वच्छन्द प्रकृति के होने के कारण तथा बाल्यावस्था में पिता जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनका प्रारम्भिक शिक्षा क्रम अव्यवस्थित रहा।
घर पर ही रहक़र इन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञानोपार्जन किया। बचपन से ही प्रताप नारायण मिश्र जी की रुचि साहित्य अनुशीलन और सृजन की ओर थी।
काव्य प्रतिभा बचपन से ही उनमें विद्यमान थी, वे उर्दू तथा हिन्दी दोनों में ही कविता किया करते थे, स्वभाव से भावुक थे फक्कड़पन, मनामौजीपन, मस्ती उनके स्वभाव की सहज विशेषतायें थीं।
समाचार पत्रों और पत्रकारिता की ओर उनकी हार्दिक रुचि थी। फलस्वरूप इन्होंने “ब्राह्मण” नामक मासिक पत्र निकाला और बाद में “हिन्दी हिन्दोत्थान” नामक पत्र का भी सफल सम्पादन किया । इन्हीं दोनों पत्रों में इनकी अधिकांश रचनायें प्रकाशित हुआ करती थीं।
सन् 1894 में, 38 वर्ष की अल्पायु में ही माँ भारती का यह मनमौजी पुत्र भारत भूमि से सदा-सदा के लिये चल बसा।
रचनायें
प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने छोटे जीवन काल में लगभग चालीस पुस्तकों की रचना की। मिश्र जी साहित्य की अन्य विधाओं की भी अपनी प्रतिभा से श्री वृद्धि की थी।
कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट मिश्र के नाटक हैं तथा भारत दुर्दशा, कवि कौतुक, मन की लहर, शृंगार विलास, मानस विनोद, इनके काव्य ग्रन्थ हैं।
इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र जी ने अनेक निबन्धों की रचना की जो “निबन्ध नवनीत” में संग्रहीत हैं। ये निबन्ध ही मिश्र जी के कीर्ति स्तम्भ हैं।
विषयों की विविधता और अनेकरूपता की दृष्टि से उनका निबन्ध-साहित्य अत्यधिक सम्पन्न है। निबन्धों के विषय बड़े निराले एवं आकर्षक होते हैं जैसे- भौं, दाँत, नाक, पेट, आप, बात आदि।
भाषा
प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा जन साधारण की भाषा है। उन्होंने जो कुछ लिखा वह विद्वत्समाज के लिये न होकर सर्वसाधारण के लिये है। उसमें कृत्रिमता, सजावट अथवा प्रयत्न के स्थान पर नैसर्गिकता अधिक है।
भाषा लिखने का उनका अपना एक मौलिक ढंग था, जिसका वे अन्त तक निर्वाह करते रहे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा पं० बालकृष्ण भट्ट के प्रयत्न से उस समय तक भाषा का पर्याप्त विकास एवं परिष्कार हो चुका था, परन्तु मिश्र जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।
अतः उनकी भाषा में अव्यवस्था, ग्रामीणता एवं व्याकरण की भूलें आ जाना स्वाभाविक है। मिश्र जी ने शब्द शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया।
विराम चिन्हों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है, यदि कहीं हुआ भी है। तो अशुद्ध ही है। खुशामद, निहायत, लफज, खामहखाह आदि उर्दू फारसी के शब्द, सेतमेंत, रितु, .खौखियाना आदि ग्रामीण शब्द, आत्माभिमान प्राबल्यता आदि संस्कृत शब्दों के अशुद्ध रूप भी मिलते हैं।
कहावतों और मुहावरों का जैसा प्रयोग मिश्र जी ने किया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मिश्र जी का भाषा पर पूर्वीपन और पण्डिताऊपन का अधिक प्रभाव है।
सब कुछ होते हुए भी मिश्र जी की भाषा में सशक्तता, रोचकता, आत्मीयता और चुलबुलापन है। भाषा के प्रवाह की तीव्रता में कहीं भी कमी नहीं आने पाई।
शैली
हास्य, विनोद और व्यंग्य के मिश्र जी अवतार थे। यही हास्य और विनोद इनकी शैली का प्राण है। भाषा की भाँति शैली पर भी मिश्र जी के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है।
मिश्र जी की शैली का प्रमुख रूप एक ही है, वह है व्यंगात्मक शैली अथवा प्रसादात्मक शैली। दूसरा स्वरूप विवेचनात्मक शैली का है, परन्तु इस शैली में मिश्र जी ने बहुत कम लिखा क्योंकि स्वभाव के अनुकूल तो वे ही विषय आते थे जिनमें उन्हें अपने विनोदी स्वभाव का ह्रास-परिहास और व्यंग का चमत्कार दिखाने का अवसर मिल सकता था।
मिश्र जी की शैली को दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है-
विवेचनात्मक शैली
मिश्र जी ‘इस शैली में ‘शिव मूर्ति’ निबन्ध आता है। इसमें उनकी मननशीलता का रूप कुछ उभरा है। तर्क, प्रमाण और विषय विवेचन भी दृष्टिगोचर होता है।
भाषा भी शुद्ध, सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित है। वाक्य सुलझे हुये और विचार स्पष्ट हैं, परन्तु यह निबन्ध मिश्र जी के स्वभाव का अपवाद ही कहा जा सकता है।
प्रसादात्मक शैली अथवा व्यंगात्मक शैली
यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि एवं स्वाभाविक शैली है। उनके प्रायः सभी निबन्ध इसी शैली में लिखे गये हैं। इसमें वाणी की वक्रता, चुलबुलापन, उछल कूद और वेग विद्यमान है।
मुहावरों और कहावतों के प्रयोग द्वारा व्यंजनता और भी बढ़ जाती है। इस शैली में बिना किसी प्रकार के छिपाव के स्पष्ट और धड़ल्ले के साथ बात कहने की प्रवृत्ति है।
वैयक्तिक्ता और आत्मीयता इस शैली के प्रधान गुण हैं। व्यंग विनोद के समावेश से उनकी इस शैली का आकर्षण जहाँ बढ़ा है, वहाँ उसकी रोचकता और प्रभाव में भी वृद्धि हुई है।
निःसन्देह उनकी यह शैली बड़ी सजीव और सरस है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
पं० प्रताप नारायण मिश्र का सामान्य परिचय दीजिये |
उन्हें अपना अक्खड़पन और मनमौजीपन, मस्ती और सैलानीपन ही पसन्द था। व्यंग्य-विनोद उनकी प्रकृति के मुख्य तत्व थे, चिन्तन और विचार उनके स्वभाव के विपरीत थे।
हिन्दी और हिन्दी साहित्य को पिटारे में बन्द न करके वे सामान्य जन जीवन के बीच में खींच लाये थे।
निःसन्देह मिश्र जी ने हिन्दी भाषा-भाषी समाज का तथा स्वयं हिन्दी के प्रचार और प्रसार का उस समय बहुत बड़ा काम किया था, जबकि खड़ी बोली हिन्दी अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट मिश्र के नाटक हैं तथा भारत दुर्दशा, कवि कौतुक, मन की लहर, शृंगार विलास, मानस विनोद, इनके काव्य ग्रन्थ हैं।
इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने अनेक निबन्धों की रचना की जो “निबन्ध नवनीत” में संग्रहीत हैं। ये निबन्ध ही मिश्र जी के कीर्ति स्तम्भ हैं।
विषयों की विविधता और अनेकरूपता की दृष्टि से उनका निबन्ध-साहित्य अत्यधिक सम्पन्न है। निबन्धों के विषय बड़े निराले एवं आकर्षक होते हैं जैसे- भौं, दाँत, नाक, पेट, आप, बात आदि।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की शैली कैसी है ?
मिश्र जी की शैली का प्रमुख रूप एक ही है, वह है व्यंगात्मक शैली अथवा प्रसादात्मक शैली। दूसरा स्वरूप विवेचनात्मक शैली का है, परन्तु इस शैली में मिश्र जी ने बहुत कम लिखा क्योंकि स्वभाव के अनुकूल तो वे ही विषय आते थे जिनमें उन्हें अपने विनोदी स्वभाव का ह्रास-परिहास और व्यंग का चमत्कार दिखाने का अवसर मिल सकता था।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की भाषा क्या थी ?
भाषा लिखने का उनका अपना एक मौलिक ढंग था, जिसका वे अन्त तक निर्वाह करते रहे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा पं० बालकृष्ण भट्ट के प्रयत्न से उस समय तक भाषा का पर्याप्त विकास एवं परिष्कार हो चुका था, परन्तु मिश्र जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।
अतः उनकी भाषा में अव्यवस्था, ग्रामीणता एवं व्याकरण की भूलें आ जाना स्वाभाविक है। मिश्र जी ने शब्द शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया।
विराम चिन्हों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है, यदि कहीं हुआ भी है। तो अशुद्ध ही है। खुशामद, निहायत, लफज, खामहखाह आदि उर्दू फारसी के शब्द, सेतमेंत, रितु, .खौखियाना आदि ग्रामीण शब्द, आत्माभिमान प्राबल्यता आदि संस्कृत शब्दों के अशुद्ध रूप भी मिलते हैं।
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- परिचय
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- भाषा
- शैली
परिचय
भारतेन्दु युग में उत्पन्न होकर भी उस समय के विकास और परिष्कार से सिंह और सपू की भाँति यदि कोई लेखक अप्रभावित रहा तो वह पं० प्रताप नारायण मिश्र ही थे।
उन्हें अपना अक्खड़पन और मनमौजीपन, मस्ती और सैलानीपन ही पसन्द था। व्यंग्य-विनोद उनकी प्रकृति के मुख्य तत्व थे, चिन्तन और विचार उनके स्वभाव के विपरीत थे।
हिन्दी और हिन्दी साहित्य को पिटारे में बन्द न करके वे सामान्य जन जीवन के बीच में खींच लाये थे।
निःसन्देह प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिन्दी भाषा-भाषी समाज का तथा स्वयं हिन्दी के प्रचार और प्रसार का उस समय बहुत बड़ा काम किया था, जबकि खड़ी बोली हिन्दी अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
जीवन वृत्त
पं० प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे गाँव में सन् 1856 में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० संकटा प्रसाद था।
प्रताप नारायण मिश्र ke पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गये थे और ज्योतिष का काम करते थे। वे अपने पुत्र को ज्योतिषी ही बनाना चाहते थे परन्तु प्रताप नारायण की रुचि गणित के शुष्क अंकों में न रमी।
प्रताप नारायण मिश्र बचपन से ही स्वच्छन्द प्रकृति के होने के कारण तथा बाल्यावस्था में पिता जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनका प्रारम्भिक शिक्षा क्रम अव्यवस्थित रहा।
घर पर ही रहक़र इन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञानोपार्जन किया। बचपन से ही प्रताप नारायण मिश्र जी की रुचि साहित्य अनुशीलन और सृजन की ओर थी।
काव्य प्रतिभा बचपन से ही उनमें विद्यमान थी, वे उर्दू तथा हिन्दी दोनों में ही कविता किया करते थे, स्वभाव से भावुक थे फक्कड़पन, मनामौजीपन, मस्ती उनके स्वभाव की सहज विशेषतायें थीं।
समाचार पत्रों और पत्रकारिता की ओर उनकी हार्दिक रुचि थी। फलस्वरूप इन्होंने “ब्राह्मण” नामक मासिक पत्र निकाला और बाद में “हिन्दी हिन्दोत्थान” नामक पत्र का भी सफल सम्पादन किया । इन्हीं दोनों पत्रों में इनकी अधिकांश रचनायें प्रकाशित हुआ करती थीं।
सन् 1894 में, 38 वर्ष की अल्पायु में ही माँ भारती का यह मनमौजी पुत्र भारत भूमि से सदा-सदा के लिये चल बसा।
रचनायें
प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने छोटे जीवन काल में लगभग चालीस पुस्तकों की रचना की। मिश्र जी साहित्य की अन्य विधाओं की भी अपनी प्रतिभा से श्री वृद्धि की थी।
कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट मिश्र के नाटक हैं तथा भारत दुर्दशा, कवि कौतुक, मन की लहर, शृंगार विलास, मानस विनोद, इनके काव्य ग्रन्थ हैं।
इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र जी ने अनेक निबन्धों की रचना की जो “निबन्ध नवनीत” में संग्रहीत हैं। ये निबन्ध ही मिश्र जी के कीर्ति स्तम्भ हैं।
विषयों की विविधता और अनेकरूपता की दृष्टि से उनका निबन्ध-साहित्य अत्यधिक सम्पन्न है। निबन्धों के विषय बड़े निराले एवं आकर्षक होते हैं जैसे- भौं, दाँत, नाक, पेट, आप, बात आदि।
भाषा
प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा जन साधारण की भाषा है। उन्होंने जो कुछ लिखा वह विद्वत्समाज के लिये न होकर सर्वसाधारण के लिये है। उसमें कृत्रिमता, सजावट अथवा प्रयत्न के स्थान पर नैसर्गिकता अधिक है।
भाषा लिखने का उनका अपना एक मौलिक ढंग था, जिसका वे अन्त तक निर्वाह करते रहे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा पं० बालकृष्ण भट्ट के प्रयत्न से उस समय तक भाषा का पर्याप्त विकास एवं परिष्कार हो चुका था, परन्तु मिश्र जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।
अतः उनकी भाषा में अव्यवस्था, ग्रामीणता एवं व्याकरण की भूलें आ जाना स्वाभाविक है। मिश्र जी ने शब्द शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया।
विराम चिन्हों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है, यदि कहीं हुआ भी है। तो अशुद्ध ही है। खुशामद, निहायत, लफज, खामहखाह आदि उर्दू फारसी के शब्द, सेतमेंत, रितु, .खौखियाना आदि ग्रामीण शब्द, आत्माभिमान प्राबल्यता आदि संस्कृत शब्दों के अशुद्ध रूप भी मिलते हैं।
कहावतों और मुहावरों का जैसा प्रयोग मिश्र जी ने किया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मिश्र जी का भाषा पर पूर्वीपन और पण्डिताऊपन का अधिक प्रभाव है।
सब कुछ होते हुए भी मिश्र जी की भाषा में सशक्तता, रोचकता, आत्मीयता और चुलबुलापन है। भाषा के प्रवाह की तीव्रता में कहीं भी कमी नहीं आने पाई।
शैली
हास्य, विनोद और व्यंग्य के मिश्र जी अवतार थे। यही हास्य और विनोद इनकी शैली का प्राण है। भाषा की भाँति शैली पर भी मिश्र जी के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है।
मिश्र जी की शैली का प्रमुख रूप एक ही है, वह है व्यंगात्मक शैली अथवा प्रसादात्मक शैली। दूसरा स्वरूप विवेचनात्मक शैली का है, परन्तु इस शैली में मिश्र जी ने बहुत कम लिखा क्योंकि स्वभाव के अनुकूल तो वे ही विषय आते थे जिनमें उन्हें अपने विनोदी स्वभाव का ह्रास-परिहास और व्यंग का चमत्कार दिखाने का अवसर मिल सकता था।
मिश्र जी की शैली को दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है-
विवेचनात्मक शैली
मिश्र जी ‘इस शैली में ‘शिव मूर्ति’ निबन्ध आता है। इसमें उनकी मननशीलता का रूप कुछ उभरा है। तर्क, प्रमाण और विषय विवेचन भी दृष्टिगोचर होता है।
भाषा भी शुद्ध, सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित है। वाक्य सुलझे हुये और विचार स्पष्ट हैं, परन्तु यह निबन्ध मिश्र जी के स्वभाव का अपवाद ही कहा जा सकता है।
प्रसादात्मक शैली अथवा व्यंगात्मक शैली
यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि एवं स्वाभाविक शैली है। उनके प्रायः सभी निबन्ध इसी शैली में लिखे गये हैं। इसमें वाणी की वक्रता, चुलबुलापन, उछल कूद और वेग विद्यमान है।
मुहावरों और कहावतों के प्रयोग द्वारा व्यंजनता और भी बढ़ जाती है। इस शैली में बिना किसी प्रकार के छिपाव के स्पष्ट और धड़ल्ले के साथ बात कहने की प्रवृत्ति है।
वैयक्तिक्ता और आत्मीयता इस शैली के प्रधान गुण हैं। व्यंग विनोद के समावेश से उनकी इस शैली का आकर्षण जहाँ बढ़ा है, वहाँ उसकी रोचकता और प्रभाव में भी वृद्धि हुई है।
निःसन्देह उनकी यह शैली बड़ी सजीव और सरस है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
पं० प्रताप नारायण मिश्र का सामान्य परिचय दीजिये |
उन्हें अपना अक्खड़पन और मनमौजीपन, मस्ती और सैलानीपन ही पसन्द था। व्यंग्य-विनोद उनकी प्रकृति के मुख्य तत्व थे, चिन्तन और विचार उनके स्वभाव के विपरीत थे।
हिन्दी और हिन्दी साहित्य को पिटारे में बन्द न करके वे सामान्य जन जीवन के बीच में खींच लाये थे।
निःसन्देह मिश्र जी ने हिन्दी भाषा-भाषी समाज का तथा स्वयं हिन्दी के प्रचार और प्रसार का उस समय बहुत बड़ा काम किया था, जबकि खड़ी बोली हिन्दी अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट मिश्र के नाटक हैं तथा भारत दुर्दशा, कवि कौतुक, मन की लहर, शृंगार विलास, मानस विनोद, इनके काव्य ग्रन्थ हैं।
इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने अनेक निबन्धों की रचना की जो “निबन्ध नवनीत” में संग्रहीत हैं। ये निबन्ध ही मिश्र जी के कीर्ति स्तम्भ हैं।
विषयों की विविधता और अनेकरूपता की दृष्टि से उनका निबन्ध-साहित्य अत्यधिक सम्पन्न है। निबन्धों के विषय बड़े निराले एवं आकर्षक होते हैं जैसे- भौं, दाँत, नाक, पेट, आप, बात आदि।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की शैली कैसी है ?
मिश्र जी की शैली का प्रमुख रूप एक ही है, वह है व्यंगात्मक शैली अथवा प्रसादात्मक शैली। दूसरा स्वरूप विवेचनात्मक शैली का है, परन्तु इस शैली में मिश्र जी ने बहुत कम लिखा क्योंकि स्वभाव के अनुकूल तो वे ही विषय आते थे जिनमें उन्हें अपने विनोदी स्वभाव का ह्रास-परिहास और व्यंग का चमत्कार दिखाने का अवसर मिल सकता था।
पं० प्रताप नारायण मिश्र की भाषा क्या थी ?
भाषा लिखने का उनका अपना एक मौलिक ढंग था, जिसका वे अन्त तक निर्वाह करते रहे। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तथा पं० बालकृष्ण भट्ट के प्रयत्न से उस समय तक भाषा का पर्याप्त विकास एवं परिष्कार हो चुका था, परन्तु मिश्र जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।
अतः उनकी भाषा में अव्यवस्था, ग्रामीणता एवं व्याकरण की भूलें आ जाना स्वाभाविक है। मिश्र जी ने शब्द शुद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया।
विराम चिन्हों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है, यदि कहीं हुआ भी है। तो अशुद्ध ही है। खुशामद, निहायत, लफज, खामहखाह आदि उर्दू फारसी के शब्द, सेतमेंत, रितु, .खौखियाना आदि ग्रामीण शब्द, आत्माभिमान प्राबल्यता आदि संस्कृत शब्दों के अशुद्ध रूप भी मिलते हैं।
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
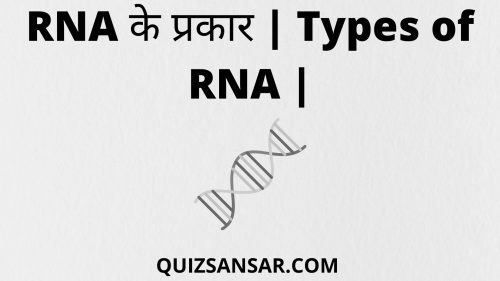
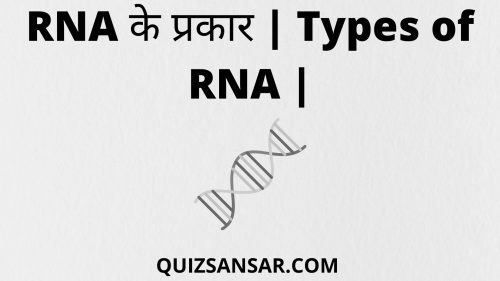
RNA के प्रकार | Types of RNA |
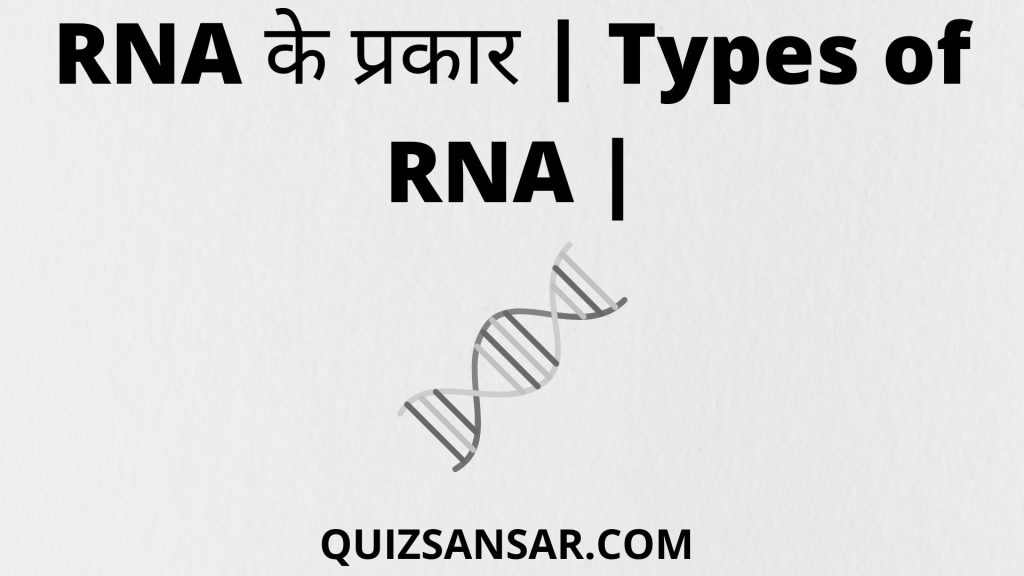
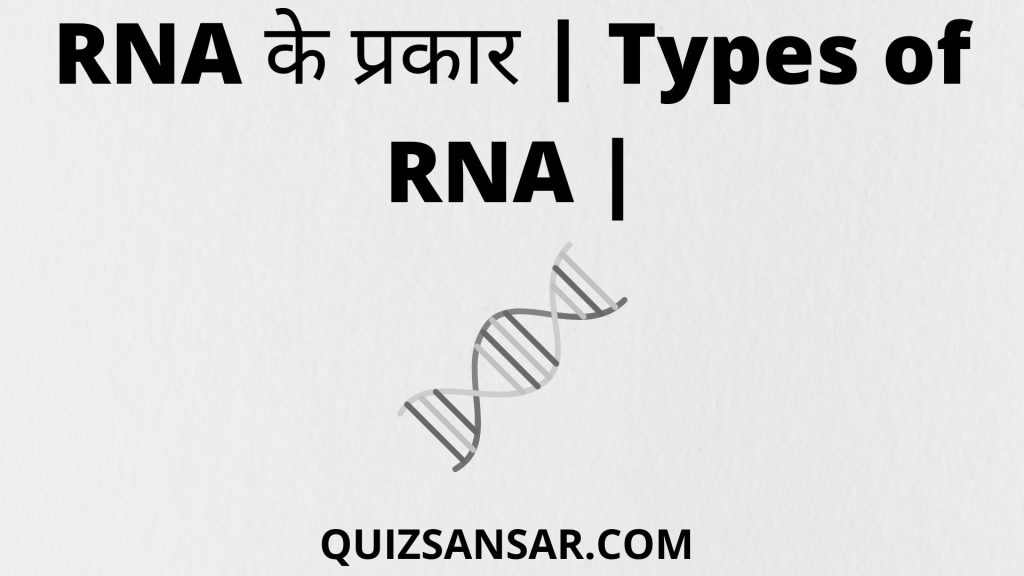
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है RNA के प्रकार | Types of RNA | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
RNA अधिक अणुभार वाली पालीन्युलियोटाइड से मिलकर बना है | यह DNA से भिन्न होता है, क्योंकी इसमें डीओक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर युरेसिल होता है | प्रत्येक कोशिका में RNA निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं-
संदेशवाहक RNA (m-RNA)
इनका निर्माणकेन्द्रक में उपस्थित DNA पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है | ये कोशिका की कुल RNA का 3-5% होते हैं और इनका आणविक-भार 500,000 से 2,000,000 होता है | केन्द्रक में DNA साँचे पर इनका निर्माण होता है | सन 1961 में फ्रैंसिस जैकब तथा जैक्यू मोनाड ने इन्हें संदेशवाहक RNA अणुओं का नाम दिया |
कार्य –
संदेशवाहक RNA अणु केन्द्रक से बाहर कोशिकाद्रव्य में आ जाता है | यहाँ यह केन्द्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनता है |
राइबोसोमल RNA (r-RNA)
ये RNA के संरचनात्मक अणु होते हैं | यह कोशिका की कुल RNA का 80% होता है | rRNA केन्द्रक में DNA से उत्पन्न होता है | तीनों प्रकार के RNA में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है | प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग rRNA का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है |
कार्य –
rRNA राइबोसोम्स की रचना में भाग लेते हैं | यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है |
स्थानान्तरण RNA(t-RNA or s-RNA)
यह कोशिका की कुल RNA का 15-18% होता है | यह कोशिकाद्रव्य में पाया जाता है | ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं; अतः इन्हें विलेय RNA अणु भी कहते हैं | इनका निर्माण केन्द्रक में DNA के सांचे पर होता है |
कार्य –
ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है |
t-RNA की संरचना
वलन के कारण इनके अणुओं में द्वितीयक तथा तृतीयक स्तरों की संरचना होती है | इसके फलस्वरूप साइटोसाल में इन अणुओं की तृतीयक स्तर की त्रिविम आकृति अत्यधिक कुण्डली “एल(L)” जैसी होती है | राबर्ट होले ने सन 1964 में tRNA की संरचना का क्लोवर लीफ माडल प्रस्तुत किया | इस माडल के अनुसार tRNA के प्रत्येक अणु की द्विविम आकृति मटर कुल के एक पौधे तिपतिया चारा की पत्ती जैसी होती है | ये चारों भुजाएं सभी tRNA अणुओं में एक सी होती हैं | तीन भुजाओं के सिरे लूप सदृश पाँचवी भुजा भी प्रायः होती है जिसे लम्प कहतें हैं | परन्तु यह सामान नहीं होती | tRNA की चार भुजाएं निम्न हैं-
अंगीकार भुजा
इस भुजा को एमिनो अम्ल भुजा भी कहतें हैं, इस भुजा के छोर पर लूप नहीं होता, बल्की द्विकुण्डलिनी का एक सूत्र 5’ सिरे वाला तथा दूसरा 3’ सिरे वाला होता है | 3’ सिरे वाले सूत्र के छोर पर साइटोसीन- साइटोसीन-एडीनीन (CCA) समाक्षरों वाले राइबोन्युक्लिओटाइड्स का अनुक्रम होता है |
20 में से किसी एक विशेष प्रकार का एमीनो अम्ल अणु, अपने कार्बोक्सिल समूह (-COOH) द्वारा, साइटोसीन- साइटोसीन-ऐडेनीन (CCA) की ऐडीनोसीन के 2’ या 3’ नम्बर के हाइड्राक्सिल समूह (-OH) से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है | यह ATP की सहायता से बनने वाला एक उच्च-ऊर्जा एस्टर बंध होता है जिसका उत्प्रेरण एक मैग्नीशियमयुक्त (Mg2+) ऐमीनोऐसिल-tRNA सिन्थेटेज नामक एंजाइम करता है |
प्रत्येक प्रकार के एमीनो अम्ल को निर्दिष्ट tRNA से जोड़ने के लिए पृथक सिन्थेटेज एंजाइम होता है | अतः 20 प्रकार के एमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के मिलते-जुलते सिन्थेटेज एन्जाइम्स होते हैं | निर्दिष्ट एमिनो अम्ल से जुड़े tRNA को ऐमीनोऐसिलेटेड tRNA कहतें हैं |
एन्टीकोडॉन भुजा
एन्टीकोडॉन भुजा के छोर में लूप होता है | लूप के छोर पर तीन समाक्षरों का अनुक्रम होता है जी mRNA अणु के उसी त्रिगुण कोड का सम्पूरक होता है जिसमे कि AA भुजा से जुड़े एमिनो अम्ल की संकेत सूचना होती है | इसलिए, इस त्रिगुणी समाक्षर अनुक्रम को ऐंटीकोडॉन कहतें हैं |
DHU भुजा
DHU भुजा एक एंजाइम से जुड़ती है अर्थात यह एंजाइम स्थल है |
T C भुजा
यह भुजा tRNA अणु को राइबोसोम से जुडती है |
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
संदेशवाहक RNA (m-RNA) किसे कहतें हैं ?
इनका निर्माणकेन्द्रक में उपस्थित DNA पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है | ये कोशिका की कुल RNA का 3-5% होते हैं और इनका आणविक-भार 500,000 से 2,000,000 होता है | केन्द्रक में DNA साँचे पर इनका निर्माण होता है | सन 1961 में फ्रैंसिस जैकब तथा जैक्यू मोनाड ने इन्हें संदेशवाहक RNA अणुओं का नाम दिया |
संदेशवाहक RNA के क्या कार्य हैं ?
संदेशवाहक RNA अणु केन्द्रक से बाहर कोशिकाद्रव्य में आ जाता है | यहाँ यह केन्द्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनता है |
एन्टीकोडॉन भुजा क्या है ?
एन्टीकोडॉन भुजा के छोर में लूप होता है | लूप के छोर पर तीन समाक्षरों का अनुक्रम होता है जी mRNA अणु के उसी त्रिगुण कोड का सम्पूरक होता है जिसमे कि AA भुजा से जुड़े एमिनो अम्ल की संकेत सूचना होती है | इसलिए, इस त्रिगुणी समाक्षर अनुक्रम को ऐंटीकोडॉन कहतें हैं |
राइबोसोमल RNA (r-RNA) किसे कहतें हैं ?
ये RNA के संरचनात्मक अणु होते हैं | यह कोशिका की कुल RNA का 80% होता है | rRNA केन्द्रक में DNA से उत्पन्न होता है | तीनों प्रकार के RNA में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है | प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग rRNA का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है |
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |


अकाउंट के प्रकार |Types of Accounts in Hindi


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है अकाउंट के प्रकार |Types of Accounts | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
किसी बिजनेस में बुक कीपिंग का मतलब कम्पनी के सम्पूर्ण लेन-देन के रिकॉर्ड को संगृहीत किया जा सके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे पास बुक कीपिंग से सम्बंधित समूह निम्न हैं –
The object of book-keeping is to keep a complete record of all the transactions that place in the business. To achieve this object, business transactions have been classified into three categories :
- Transactions relating to persons .
- Transactions relating to properties and assets .
- Transactions relating to incomes and expenses .
The accounts falling under the first heading are known as ‘Personal Accounts’. The accounts falling under the second heading are known as ‘Real Accounts’, the accounts falling under the third heading are called ‘Nominal Accounts’. The accounts can also be classified as personal and impersonal . The following chart will show the various types of accounts .
Personal Accounts
Accounts recording transactions with a person or group of persons are known as personal accounts . These accounts are necessary, in particular, to record credit transactions. Personal accounts are of the following types :
एक नगद अकाउंट एक व्यक्ति के साथ या कारपोरेट बाडिज के साथ अकाउंट या इंस्टिट्यूशन के साथ जो एक बिजनेस को डील करने में परिचित कराता है | (उदाहरण- ग्राहक, लेनदार, देनदार, बैंक, पूँजी, फर्म और व्यक्ति के नाम आदि |)
Natural persons :
An अकाउंट recording transactions with an individual human being is termed as termed as a natural persons personal account. eg., Kamal’s account, Sharma’s accounts. Both males and females are included in it .
Artificial or legal persons :
An account recording financial transactions with an artificial person created by law or otherwise is termed as an artificial person, personal account, e.g. Firms’ accounts, limited companies’ accounts, educational institutions’ accounts, Co-operative society account .
Group/ Representative personal Accounts :
An अकाउंट indirectly representing a person or persons is known as representative personal account . When accounts are of a similar nature and their number is large, it is better tot group them under one head and open representative personal accounts e.g., prepaid insurance, outstanding salaries, rent, wages etc. When a person starts a business, he is known as proprietor . This proprietor is represented by capital account for that entire he invests in business and by drawings accounts for all that which he withdraws from business. So, capital accounts and drawings account are also personal accounts .
The rule for personal accounts is: Debit the receiver, Credit the giver .
Real Accounts
अकाउंट relating to properties or assets are known as ‘Real Accounts’, A separate अकाउंट is maintained for each asset e.g., Cash Machinery, Building, etc., Real accounts can be further classified into tangible and intangible .
वह खाता जो चीजों से सम्बंधित होता है, जिसे हम छू सकतें हैं, महसूस कर सकतें हैं, नाप सकतें हैं, फिक्स्ड कर सकतें हैं या करेन्ट नेचर में कर सकतें हैं | (उदाहरण- नगद, फर्नीचर, स्टॉक, क्रय, विक्रय आदि |)
Tangible Real Accounts:
These अकाउंट represent assets and properties which can be seen, touched, felt, measured, purchases and sold. e.g. Machinery account Cash account, Furniture account, stock account etc.
Intangible Real Accounts:
These accounts represent assets and properties which cannot be seen, touched or felt but they can be measured in terms of money .e.g., Goodwill accounts, patents account, Trademarks account, Copyrights account, etc.
The rule for real accounts is: Debit what comes in , Credit what goes out
Nominal Accounts
Accounts relating to income, revenue, gain expenses and losses are termed as nominal accounts . These accounts are also known as fictitious accounts as they do not represent any tangible asset . A separate account is maintained for each head or expense or loss and gain or income. Wages account, Rent account Commission account, Interest received account are some examples of nominal account .
ये खाता व्यय या हानि और आय या लाभ के साथ डील करता है | ये खाते बैंक में खुलतें हैं | इस खाते का साधारण आदान-प्रदान के नेचर में वर्णन होता है | (उदाहरण- मकान मालिक को व्यापार करने के लिए भाड़ा देना | )
The rule for Nominal accounts is : Debit all expenses and losses , Credit all incomes and gains .
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
What is Personal Account?
Accounts recording transactions with a person or group of persons are known as personal accounts . These accounts are necessary, in particular, to record credit transactions. Personal accounts are of the following types :
एक नगद अकाउंट एक व्यक्ति के साथ या कारपोरेट बाडिज के साथ अकाउन्टस या इंस्टिट्यूशन के साथ जो एक बिजनेस को डील करने में परिचित कराता है | (उदाहरण- ग्राहक, लेनदार, देनदार, बैंक, पूँजी, फर्म और व्यक्ति के नाम आदि |)
What is real account?
Accounts relating to properties or assets are known as ‘Real Accounts’, Aseparate account is maintained for each asset e.g., Cash Machinery, Building, etc., Real accounts can be further classified into tangible and intangible .
वह खाता जो चीजों से सम्बंधित होता है, जिसे हम छू सकतें हैं, महसूस कर सकतें हैं, नाप सकतें हैं, फिक्स्ड कर सकतें हैं या करेन्ट नेचर में कर सकतें हैं | (उदाहरण- नगद, फर्नीचर, स्टॉक, क्रय, विक्रय आदि |)
What is meant by artificial or legal person?
An account recording financial transactionswith an artificial person created by law or otherwise is termed as an artificial person, personal account, e.g. Firms’ accounts, limited companies’ accounts, educationalinstitutions’ accounts, Co-operative society account .
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |


आनुवांशिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी | Genetic Engineering or Technology |
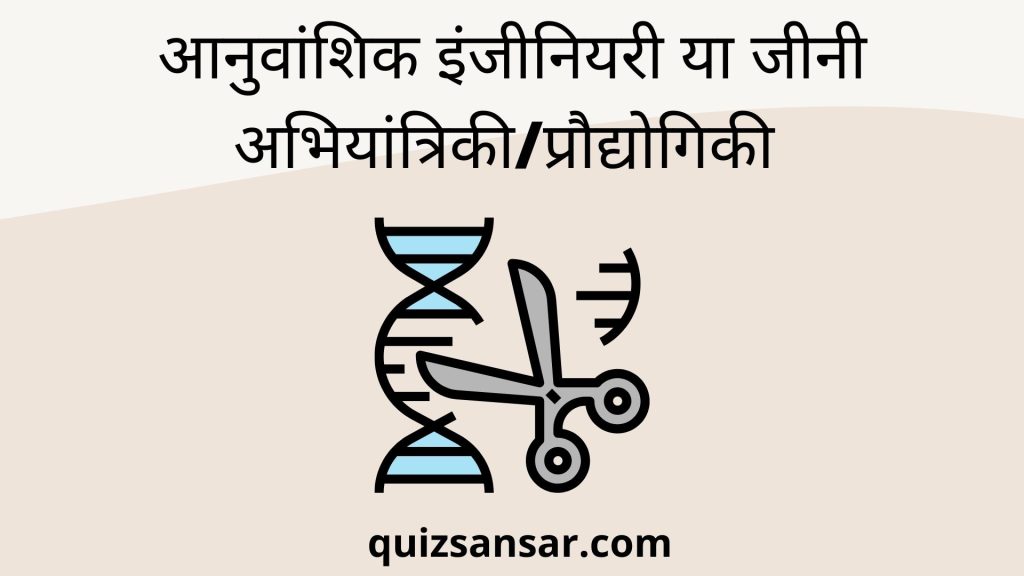
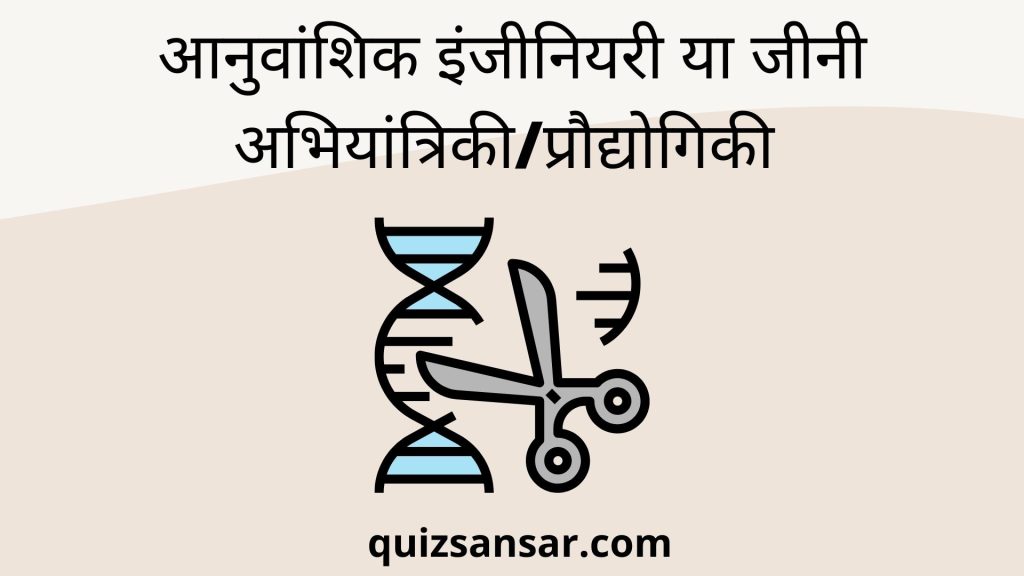
आनुवांशिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी – नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है आनुवांशिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी | Genetic Engineering or Technology | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
आनुवंशिक अभियन्त्रिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियन्त्रिकी को जीन क्लोनिंग भी कहतें हैं | जीवों में संलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना आनुवांशिक इंजीनियरी का उद्देश्य है | क्योंकी DNA अणुओं में जोड़-तोड़ जीनी अभियांत्रिकी का आधार होता है, इसे पुनर्संयोजी DNA प्रद्योगिकी भी कहतें है |
जीन अभियांत्रिकी में आनुवंशिक पदार्थ का हेर-फेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है अर्थात जीवों के आनुवांशिक पदार्थ (DNA) में जोड़-तोड़ करके उनके दोषपूर्ण आनुवंशिक लक्षणों के जींस को हटाकर, उनके स्थान पर DNA में उत्कृष्ट लक्षणों के जींस को समाविष्ट करना ही जीनी अभियन्त्रिकी है |
इस तकनीकी में दो DNA अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केन्द्रक से पृथक किया जाता है और एक या अधिक प्रकार के विशेष एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उनके टुकड़े किये जातें हैं | इसके बाद इन टुकड़ों को इच्छानुसार जोड़कर कोशिका में पुनरावृत्ती व जनन के लिए पुनः स्थापित कर दिया जाता है | संक्षेप में जीन क्लोनिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग विदेशी DNA के एक विशिष्ट टुकड़े को कोशिका में स्थापित करना होता है |
आर्बर ने बैक्टीरिया कोशिकाओं में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नामक ऐसे पदार्थ की उपस्थिती की जानकारी प्राप्त की जो किसी भी बाह्य DNA को विशिष्ट टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक तीव्र रसायन का कार्य करता है | यह न्यूक्लिक अम्ल की फास्फेट-शर्करा बंधता को तोड़ता है | किसी बैक्टीरिया पर जब कोई विषाणु आक्रमण करता है तब यह प्रक्रिया उसमे रक्षास्थल का कार्य करती है |
स्मिथ ने ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विलगित किया और सन 1971 में नैथंस ने बन्दर के ट्यूमर विषाणु (एसवी 40) के DNA को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया | सन 1978 तक लगभग 100 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या निर्बन्धन एंडोन्युक्लिएज विलगित करके लक्षणित किये जा चके थे | इस प्रकार इसकी खोज सन 1970 में आर्बर, नैथंस एवं स्मिथ ने की | इसके लिए उन्हें वर्ष 1978 ई. में नोबेल पुरस्कार भी मिला | इसी से जीन अभियांत्रिकी की नींव पड़ी |
जीनी अभियन्त्रिकी के विभिन्न उपयोग
आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग उत्पादनों, अनेक मानव जींस की खोज, रोगों के कारण व उनके इलाज की सहायता में हो रहा है | हम जींस के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले अनेक लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं | इस प्रद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रयोज्य इस प्रकार हैं-
जींस का निर्माण
किसी विशेष कोशिका से m-RNA अणु को अलग करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिपटेज एंजाइम की सहायता से इस पर DNA श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है |
जीन का विश्लेषण तथा संग्रह
DNA अणुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका संग्रह करके किसी भी जीव के सम्पूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है | इसे “जीनी संग्रह” के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है | संग्रह की इस विधि को “शाटगन विधि” कहतें हैं |
जीन्स का प्रतिस्थापन
जीनी चिकित्सा से अवांछित जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नये वांछित जीन्स को प्रवेश कराया जा सकता है | इस प्रकार व्यक्ति लम्बाई, बुद्धि, ताकत आदि को नियंत्रित किया जा सकता है |
रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण
रोगजनक विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके कैंसर, एड्स आदि रोगों के विषाणुओं को रोगजनक के बजाय इन्ही रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है |
विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां
जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती हैं |
व्यक्तिगत जीन्स को अलग करना
कुछ जींस को अलग करने की तकनीक विकसित की गयी, जो निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है-
- विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने वाली जीन,
- r-RNA की जींस तथा
- नियंत्रण करने वाली जींस; जैसे- प्रोमोटर जीन तथा रेगुलेटरी जीन | चूजों में ओवोएल्ब्युमीन की जीन, चूहों में ग्लोबिन तथा इम्यूनोग्लोबिन जींस, अनाजों व लेग्युम्स में प्रोटीन संग्रह की जीन्स आदि को पृथक किया जा चुका है |
समुद्री तेल फैलाव का सफाया
इसमें पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित DNA बनाया जाता है और इसका पुंजकीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है | यह जीवाणु समुद्री सतह पर फैले तेल का सफाया कर देता है | इसे उच्चझक्की जीवाणु कहतें हैं |
पौधों में नाइट्रोजन अनुबंधन
पुनर्संयोजी DNA प्रद्योगिकी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखने वाले जीवाणुओं का संवर्धन करके इन्हें फलीरहित पादपों में प्रविष्ट कराया जाता है |
आनुवांशिक रोगों का पता लगाना
अनेक रोगों का गर्भ में ही एम्नीओसेन्टसिस तकनीक द्वारा पता लगाया जाता था, किन्तु DNA पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा पुन्जकीकृत DNA क्रम के उपलब्ध होने से गर्भस्थ शिशु के पुरे जीनोटाइप का निरिक्षण किया जा सकता है | इस विधि के द्वारा बिंदु उत्परिवर्तन, विलोपन आदि सभी उत्परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है | इस विधि का प्रयोग गर्भस्थ शिशु में थैलेसीमिया , फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि रोगों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है | आनुवांशिक रोगों का पता लगाने का यह सबसे उचित तरीका है |
औद्योगिक रसायन
पेट्रोल, ईंधन, कीटनाशी, आसंजक, प्रणोदक, विलायक, रंजक, विस्फोटक आदि कई प्रकार के पदार्थ हमें खनिज तेल पदार्थों से प्राप्त होतें हैं | इन्हें हम जीनी अभ्यांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणुओं की सहायता से पादपों के किण्वन से प्राप्त कर सकते हैं |
इस तकनीक के द्वारा इन्सुलिन तथा मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किया जा रहा है |इस तकनीक द्वारा मानव इंटरफेरांन (ल्युकोसाइटिक इंटरफेरॉन, फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरान, प्रतिरक्षक इंटरफेरान) का उत्पादन किया जा रहा है |
आपको हमारी यह post – आनुवांशिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी कैसी लगी नीचे कमेन्ट में अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सूरदास और उनकी भक्ति भावना | हिन्दी निबंध |
- ” हिन्दी-साहित्य के इतिहास ” पर एक दृष्टि | हिन्दी निबंध |
- जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | JAGANNTH DAS RATNAKAR |
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी | हिन्दी निबंध | ACHARYA MAHAVIR PRASAD DVIVEDI |
- महादेवी वर्मा का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | MAHADEVI VERMA |
- रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी निबंध |
- राष्ट्रभाषा हिन्दी पर निबंध | RASHTRA BHASHA HINDI PAR NIBANDH |
- हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग | भक्तिकाल | Bhaktikal |
- सुभद्रा कुमारी चौहान | हिन्दी निबंध | SUBHADRA KUMARI CHAUHAN |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
आनुवांशिक इंजीनियरी क्या है ?
जीन अभियांत्रिकी में आनुवंशिक पदार्थ का हेर-फेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है अर्थात जीवों के आनुवांशिक पदार्थ (DNA) में जोड़-तोड़ करके उनके दोषपूर्ण आनुवंशिक लक्षणों के जींस को हटाकर, उनके स्थान पर DNA में उत्कृष्ट लक्षणों के जींस को समाविष्ट करना ही जीनी अभियन्त्रिकी है |
जींस का निर्माण कैसे होता है ?
आनुवांशिक रोगों का पता कैसे चलता है ?
जीन्स का प्रतिस्थापन कैसे किया जाता है ?
समुद्री तेल फैलाव का सफाया कैसे किया जाता है ?
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
- भगवद्गीता का नीति-दर्शन
- विकासवादी सुखवाद के समबन्ध में स्पेन्सर का योगदान
- उपयोगितावाद का सिद्धान्त और सिजविक का योगदान
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
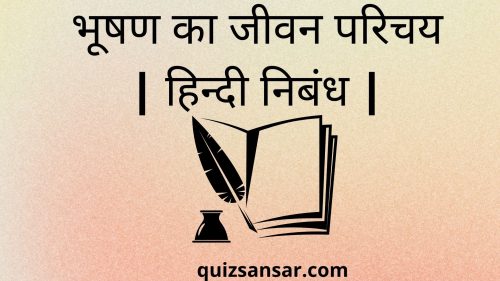
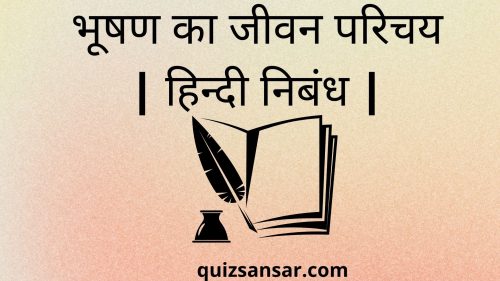
महाकवि भूषण का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | bhushan ka jivan parichay |
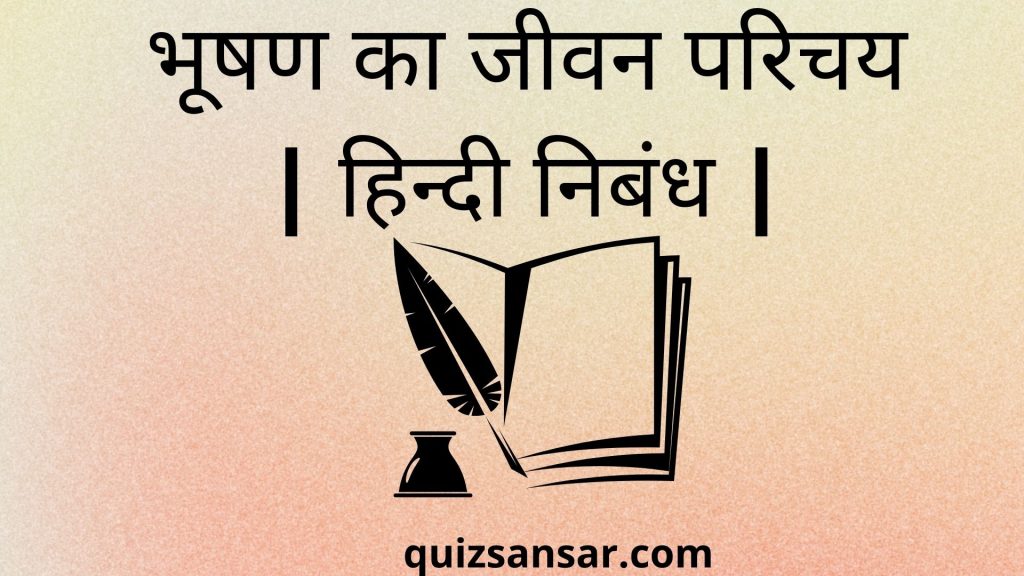
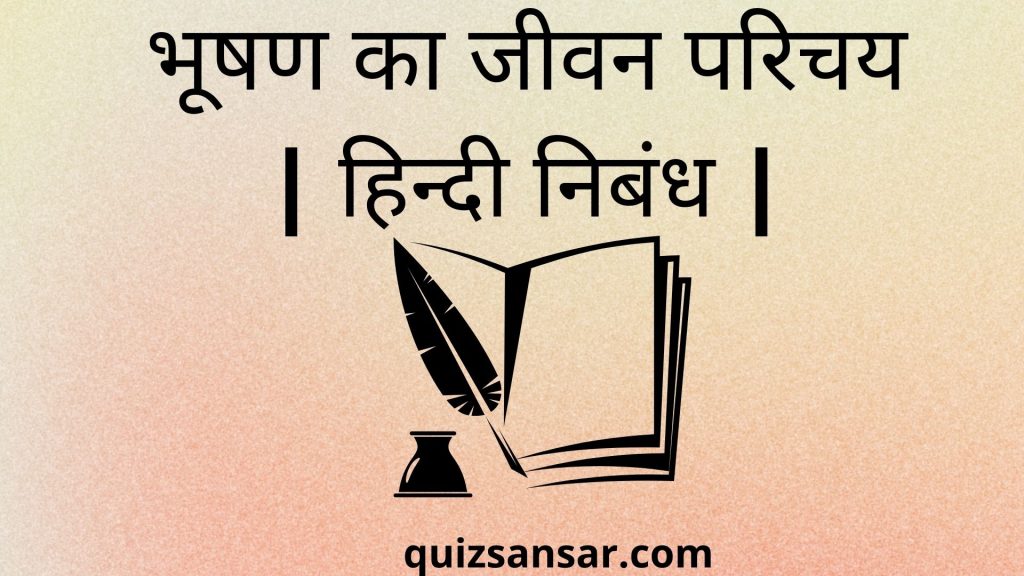
नमस्कार दोस्तों हमारी महाकवि भूषण का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | bhushan ka jivan parichay |उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- जीवन वृत्त
- रचनाएं
- काव्यगत विशेषताएं
- भाषा
- शैली
- रस, छंद एवं अलंकार
- उपसंहार
प्रस्तावना
महापुरुष, परिस्थिति एवं समय के दास नहीं होते। उनमें युग परिवर्तन और परिस्थिति एवं समय को अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता होती है।
महाकवि भूषण ने रीतिकाल में जन्म लेकर रीतिकालीन घोर श्रृङ्गारवादी परम्पराओं का विरोध कर वीर रस पूर्ण राष्ट्रीय जागरण का महान् उद्घोष किया। भूषण, भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्रकवि थे।
जीवन वृत्त
युग प्रवर्त्तक महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवाँपुर नामक गाँव में सन् 1613 ई. में हुआ था। इनके पिता रत्नाकार त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे।
भूषण के अतिरिक्त, काव्य प्रतिभा सम्पन्न उनके तीन पुत्र चिंतामणि, मतिराम और नीलकण्ठ थे।
जीवनी सामग्री अप्राप्त होने के कारण भूषण के वास्तविक नाम का तो पता नहीं चल सका, इतना अवश्य है कि इन्हें सर्वप्रथम भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रराम से प्राप्त हुई थी और इनकी यही उपाधि नाम के स्थान पर प्रसिद्ध हो गई।
ये औरंगजेब आदि अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे, परन्तु जो आदर महाराजा शिवाजी और बुंदेले वीर छत्रसाल से इन्हें प्राप्त हुआ वह किसी से नहीं हुआ।
एक बार छत्रसाल ने इनकी पालकी के नीचे अपना कंधा लगा दिया था। इस पर भूषण ने कहा था कि
“शिवा को बखानी कि बखानी छत्रसाल को “
और राजा राव एक मन में न ल्याऊँ अब,
साहू को सराहों के सराहाँ छत्रसाल को।
छद्म वेश में भगवान शंकर के दर्शनार्थ आये हुए महाराजा शिवाजी से मन्दिर में इनकी प्रथम भेंट ही निम्न कविता के माध्यम से हुई थी।
उन्होंने इसे अट्ठारह बार सुना था, फिर इन्हें अपन वास्तविक परिचय देकर पुरस्कृत किया था। कविता की आद्यन्त पंक्ति इस प्रकार हैं
इन्द्र जिमि जंभ पर, वाडव सुअंभ पर।
त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है ।।
“यदि तुम्हारी कविता से मेरा हाथ मूँछ पर न गया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा लूँगा”
इस शर्त पर भूषण ! की वीर रस पूर्ण ओजस्विनी कविता ने औरंगजेब का भी : हाथ मूँछ पर ला दिया था और उसने प्रसन्न होकर इन्हें दरबार में रख लिया था।
भूषण की वीरता, शौर्य एवम् पराक्रमपूर्ण ओजस्विनी वाणी ने सन् 1715 में सदा-सदा के लिए मौन धारण कर लिया था।
रचनायें
भूषण के तीन काव्य-ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है–
- शिवराज भूषण
- शिवा बावनी
- छत्रसाल-दशक
‘शिवराज भूषण’ इनका अलंकार सम्बन्धी ग्रंथ है जिसमें शिवाजी की प्रशंसा के छंद, अलंकारों के उदाहरणों के रूप में दिये गये हैं।
शिवसिंह सरोज ने भूषण की दो और पुस्तकों का उल्लेख किया है जिनके नाम ‘भूषण हजारा’ और ‘भूषण उल्लास” हैं, परन्तु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं ।
इसके अतिरिक्त भूषण की अनेकों स्फुट रचनायें हैं।
काव्यगत विशेषतायें
भूषण की काव्यगत भावनाओं में राज्याश्रय प्रदान करने वाले राजा महाराजाओं के गुणगान हैं।
विशेषता यह है कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों की घोर शृङ्गारवादी परम्परा का अनुसरण करके राज-दरबारों में अपनी कवित-कामिनी का नग्न नृत्य नहीं कराया।
इनके तेजस्वी और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व ने तत्कालीन साहित्य में एक नवीन युग और एक मौलिक विचार परम्परा का सूत्रपात किया।
आश्रयदाताओं के विलासी जीवन का मनोरंजन एवं व्यय की चाटुकारिता न करके उनके वीरत्व, शौर्य, साहस एवं पराक्रम आदि का चित्रण किया गया है।
उनके दया, दान, औदार्य एवं धर्मपरायणता के चित्र दिये गये हैं। रण का चित्रण देखिये
ताव दै-दै मूँछन कँगूरन पै पाँव दै-दै, अरि मुख घाव दे-दै कूद परै कोटि में।
शिवाजी के पराक्रम प्रभाव वर्णन में वीर रस की अभिव्यक्ति देखिये-
भूषण भनत महावीर बलकन लागो, सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे ।
तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भये, स्याह मुख नौरंग, सिपाही मुख पियरे ||
भयभीत अरि-महिलाओं की वस्तु स्थिति का सजीव चित्र –
ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनिवारी, ऊँचे घोर मन्दिर के अंदर रहती हैं।
भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं।
भाषा
भूषण की भी भाषा बृजभाषा थी। बृजभाषा में कोमलकान्त पदावली द्वारा वीर रस का वर्णन करना, यह भी भूषण की अनन्य काव्य प्रतिभा का ही द्योतक है।
इनकी भावानुगामिनी भाषा वीर भावों को वहन करने में पूर्णतया समर्थ है। भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली, बुन्देलखण्डी, प्राकृत, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है।
भावों की तीव्रता वेग एवं प्रवाह के अनुरूप ही भाषा में तीव्रता प्रवाह एवं वेग है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने में भूषण पर्याप्त सफल हुए हैं।
आवश्यकतानुसार शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है। एक उदाहरण देखिये –
ऐल फैल खेल भैल खनक में गैल गैल, गजन की टेल पैल सैल उसलत हैं।
शैली
भूषण की शैली रीतिकालीन शैली है। इनकी शैली का शरीर रीति-कालीन अवश्य है परन्तु आत्मा में राष्ट्र की पुकार और युग-वाणी है।
शैली ओजपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। व्यंजकता, ध्वन्यात्मकता एवम् चित्रमयता इनकी शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं।
भूषण की शैली सरल, सजीव एवम् प्रभावोत्पादक है।
रस, छंद एवं अलंकार
भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। वीर-रस का सर्वाङ्गपूर्ण सफल परिपाक जैसा इनके काव्य में हुआ वैसा अन्यत्र नहीं हुआ।
चरित्र नायक शिवाजी की युद्ध वीरता के साथ-साथ उनकी दानवीरता, दयावीरता और धर्मवीरता का भी चरित्रांकन किया गया है।
भयानक एवम् रौद्र रसों का भी परिपाक इनकी रचनाओं में सुन्दर शैली में हुआ है।
छंद-योजना में भूषण ने कवित्त, दोहा, रोला, छप्पय तथा हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। भूषण की छन्द-व्यवस्था सुन्दर है। कवित्त इनके अधिक निकट थे।
उपसंहार
काव्य के आन्तरिक रूप में भूषण जहाँ मौलिक एवं मुक्त हैं वहाँ बाह्य रूप में रीतिकाल के प्रवाह से युक्त हैं।
अन्य कवियों की भाँति इन्होंने भी काव्य की शक्ति के साथ कला का चमत्कार प्रदर्शित किया है, अनुप्रास, यमक श्लेष और उपमा का बाहुल्य है।
भूषण की प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई अलंकार अवश्य निहित होगा।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
भूषण की जीवन वृत्त क्या है ?
युग प्रवर्त्तक महाकवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवाँपुर नामक गाँव में सन् 1613 ई. में हुआ था। इनके पिता रत्नाकार त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे।
भूषण के अतिरिक्त, काव्य प्रतिभा सम्पन्न उनके तीन पुत्र चिंतामणि, मतिराम और नीलकण्ठ थे।
जीवनी सामग्री अप्राप्त होने के कारण भूषण के वास्तविक नाम का तो पता नहीं चल सका, इतना अवश्य है कि इन्हें सर्वप्रथम भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रराम से प्राप्त हुई थी और इनकी यही उपाधि नाम के स्थान पर प्रसिद्ध हो गई।
ये औरंगजेब आदि अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे, परन्तु जो आदर महाराजा शिवाजी और बुंदेले वीर छत्रसाल से इन्हें प्राप्त हुआ वह किसी से नहीं हुआ।
भूषण की रचनाएँ कौन-कौन सी हैं ?
भूषण के तीन काव्य-ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है–
शिवराज भूषण
शिवा बावनी
छत्रसाल-दशक
‘शिवराज भूषण’ इनका अलंकार सम्बन्धी ग्रंथ है जिसमें शिवाजी की प्रशंसा के छंद, अलंकारों के उदाहरणों के रूप में दिये गये हैं।
शिवसिंह सरोज ने भूषण की दो और पुस्तकों का उल्लेख किया है जिनके नाम ‘भूषण हजारा’ और ‘भूषण उल्लास” हैं, परन्तु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं ।
इसके अतिरिक्त भूषण की अनेकों स्फुट रचनायें हैं।
भूषण की भाषा क्या थी ?
भूषण की भी भाषा बृजभाषा थी। बृजभाषा में कोमलकान्त पदावली द्वारा वीर रस का वर्णन करना, यह भी भूषण की अनन्य काव्य प्रतिभा का ही द्योतक है।
इनकी भावानुगामिनी भाषा वीर भावों को वहन करने में पूर्णतया समर्थ है। भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली, बुन्देलखण्डी, प्राकृत, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है।
भावों की तीव्रता वेग एवं प्रवाह के अनुरूप ही भाषा में तीव्रता प्रवाह एवं वेग है। शब्द चित्र प्रस्तुत करने में भूषण पर्याप्त सफल हुए हैं।
भूषण की शैली कैसी थी ?
भूषण की शैली रीतिकालीन शैली है। इनकी शैली का शरीर रीति-कालीन अवश्य है परन्तु आत्मा में राष्ट्र की पुकार और युग-वाणी है।
शैली ओजपूर्ण और प्रभावपूर्ण है। व्यंजकता, ध्वन्यात्मकता एवम् चित्रमयता इनकी शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं।
भूषण की शैली सरल, सजीव एवम् प्रभावोत्पादक है।
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |


Election – A Lesson to the Ruling Party | essay |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है Election – A Lesson to the Ruling Party | essay |उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Introduction
“The world’s largest democracy has produced one of the most extraordinary electoral turnarounds. The people’s verdict is the product of a three-week-long election in which one million officials moved more than one million tamper-proof voting machines around this vast country , delivering democracy to even the furthest flung region by camel, elephant, boat and helicopter was pretty damning”.
Social justice or change
Election are over. Was it a vote for development, social justice or change? The answer is complicated as can be expected from a country as diverse and layered as India.
But it can be said that rural and poor India voted against the government because it found the India Shining’, ‘Feel Good Factor’ campaign offensive and insulting to their poverty and hunger. India was left out of economic liberalisation so that this election was about their voice resounding in the nation’s consciousness.
In this sense Election can be argued that it was a vote against economic policies that marginalised and neglected many particularly the rural and lower middle class and favoured the few particularly the affluent.
However Election doesn’t explain why the rich cities of India supposedly beneficiaries of this growth voted against their providers. Did cities vote against the politics of exclusion and division? Or simply, assert that even in urban India the shining is illusionary and that more people are feeling bad’ compared to those feeling good? If Election was not so then, was this a vote for effective governance? but the defeat of the S.M.
Krishna government (in Karnataka), arguably, more efficient and productive than the Naveen Patnaik government in Orissa does conform to this notion. Perhaps it is better not to look for an overarching rationality. India is a country full of diversities, contradictions and this election was no different.
Voting after Survey
In this context the post-poll survey on how India voted’, conducted by the Centre for the Study of Developing Societies and its Lokniti network, makes interesting reading. It shows there is much more to the vote than obvious political lessons, the caste-class arithmetic and alliances.
In Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and some other States the polling pattern shows that drought and shortage of drinking and irrigation water and unemployment were important campaign issues. In Tamil Nadu, for instance, about 50 per cent of voters felt that drinking water facilities had deteriorated; 62 per cent felt that irrigation supply had gone down. A staggering 71 per cent saw worsened employment opportunities.
In high-tech Andhra Pradesh, 57 per cent of the young voters going to opponent Congress meant that the resentment against unemployment had boiled over. Yet another issue sneaks through this analysis. Corruption still matters when people vote. It is not obvious, nor is it talked about. But somewhere Naveen Patnaik whose reputation is as spotless as his performance scores over other achieving Chief Ministers.
Now the people have spoken that the agenda for change is clear, it must be formulated and implemented. People want their governments to invest in issues that matter to them; water to drink and to irrigate their crops; education and health and deal with the massive challenge of unemployment in this young country. Investment must be made in a manner that the benefits reach people and are not siphoned off along the circuitous and leaky corridors of power.
This, however, will demand the reform of the State more than the economic reforms on which so much time and energy is expended, this real reform still awaits the government’s notice. It demands the reform of the bureaucratic apparatus so that people are assured of the benefits meant for them. apparande.
Government’s top priorities
The two top priorities of this government must be: water and employment. The water agenda will demand governments to go much beyond the rhetoric of supply and targets to implement policies that put water in the hands of communities on the one hand and reduce waste and want on the other. Similarly, the agenda of growth with jobs will demand looking at solutions way out of the industrial-service sector conclave.
Jobs have to be created from the sustainable use of natural resources. Jobs to be created to the rural people and this is not an easy task. We need long-term commitment to reform and highest political will, indeed, devotion to the details of change.
Election 2004
The verdict of Election 2004 projected the ideals of India, where there was always space for dissent and which believed in the challenge of the balance. The strength of India lay in the fact that there were never in this country any glaring winners.
In this scenario, governance was about balancing contesting and competing interests, with no absolute resolution. When nobody really won then nobody really even lost that way the spoils were shared across a wider platform. The challenge now is to ensure that more and more people ‘get’ bigger and bigger gains so that all of India can win.
The new Congress government should continue with the major policy initiatives in the areas of international trade, foreign investment and even controversial ones, like labour legislation, that the BJP had started.
The ultimate objective of economic policy must be to improve the conditions of the poorest people and this will mean special effort to arrest the increasing inequality of incomes (absolute poverty has declined over the last decade) both inter personal and inter-regional. This will need a lot of imagination, for such a policy will succeed only if it is done while respecting market incentives and continuing to strive for more openness and free trade.
Conclusion
With a coalition of so many parties, there will be demand to give away basic goods at a loss (Andhra Pradesh’s new leader, Rajasekhar Reddy, has already promised free electricity to rural areas) and to subsidise a variety of services. The ultimate aim fan economic policy should be the upliftment of the poor’ and reducing inequality of incomes’. The reforms though good have not produced any tangible results for the vast majority of Indians.
There has also been a backlash against the communal politics of the BJP. This is heartening as it proves that the vast majority of Indians are secular in their outlook and not theocratic. The Congress also should not think that they have given the mandate to rule as the vote is more against the communal policies of the BJP and the failure of economic liberalisation to reach the Indian poor rather than an endorsement of the Congress party. The writing is on the wall. Efforts have to be made to provide for the hard core poor in India while pushing ahead with reforms. Basic issues like education, health, clean water and electricity, employment must be guaranteed. If not this government too will be booted out in the next elections.
Vocabulary
- verdict- judgment, finding, decision.
- damning- amaging, ruinous, fatal.
- diverse- several, assorted, different, distinct.
- offensive- assaulting, attacking.
- marginalized- to exclude or ignore.
- exclusion- keeping out, rejection.
- overarching- forming an arch above or overhead.
- miniscule- tiny, microscopic.
- debacle- downfall, collapse, fiasco.
- reveals- disclose, divulge, tell.
- deteriorated- breaking up, breaking down.
- sneaks- gym shoes, tennis shoes, running shoes.
- siphoned- pull, drag, attract, move, bring, convey.
- circuitous- complicated, roundabout.
- rhetoric- composition, discourse, oratory, oration.
- dissent- nonconformity, difference.
- incentives- spur, inducement, motivation, motive.
- subsidise- support, finance, back.
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
What should be the top priorities of the government?
The two top priorities of this government must be: water and employment. The water agenda will demand governments to go much beyond the rhetoric of supply and targets to implement policies that put water in the hands of communities on the one hand and reduce waste and want on the other. Similarly, the agenda of growth with jobs will demand looking at solutions way out of the industrial-service sector conclave.
Jobs have to be created from the sustainable use of natural resources. Jobs to be created to the rural people and this is not an easy task. We need long-term commitment to reform and highest political will, indeed, devotion to the details of change.
What will be the effect of voting after the survey?
In this context the post-poll survey on how India voted’, conducted by the Centre for the Study of Developing Societies and its Lokniti network, makes interesting reading. It shows there is much more to the vote than obvious political lessons, the caste-class arithmetic and alliances.
In Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and some other States the polling pattern shows that drought and shortage of drinking and irrigation water and unemployment were important campaign issues. In Tamil Nadu, for instance, about 50 per cent of voters felt that drinking water facilities had deteriorated; 62 per cent felt that irrigation supply had gone down. A staggering 71 per cent saw worsened employment opportunities. In high-tech Andhra Pradesh, 57 per cent of the young voters going to opponent Congress meant that the resentment against unemployment had boiled over. Yet another issue sneaks through this analysis. Corruption still matters when people vote. It is not obvious, nor is it talked about. But somewhere Naveen Patnaik whose reputation is as spotless as his performance scores over other achieving Chief Ministers.
How is social justice or change possible?
Election are over. Was it a vote for development, social justice or change? The answer is complicated as can be expected from a country as diverse and layered as India.
But it can be said that rural and poor India voted against the government because it found the India Shining’, ‘Feel Good Factor’ campaign offensive and insulting to their poverty and hunger.
India was left out of economic liberalisation so that this election was about their voice resounding in the nation’s consciousness. In this sense it can be argued that it was a vote against economic policies that marginalised and neglected many particularly the rural and lower middle class and favoured the few particularly the affluent.
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
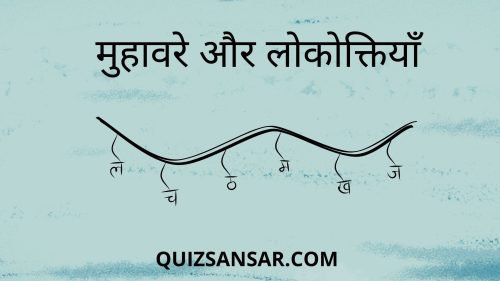
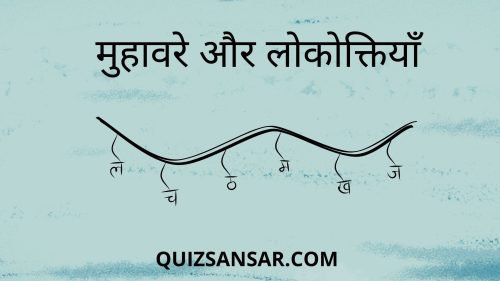
100 + मुहावरे और लोकोक्तियाँ | muhavare aur lokoktiyan |


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ | muhavare aur lokoktiyan |उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
मुहावरे
‘मुहावरा’ अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है- ‘अभ्यास’। इस प्रकार मुहावरा ऐसे शब्दों का समुच्चय होता है, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे।
मुहावरा अपने कोशगत अर्थ को छोड़कर कुछ भिन्न अर्थ देता है।
मुहावरा भाषा में प्रयुक्त ऐसा पद अथवा वाक्यांश है, जिसका हम अर्थ ग्रहण नहीं करते बल्कि उस सन्दर्भ में अनूठा, विशेष स्वाभाविक अथवा चमत्कारिक भाव ग्रहण करते हैं।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार –
“मुहावरा उस गढ़े हुए वाक्यांश को कहते हैं, जिससे कुछ लक्षणात्मक अर्थ निकलता है। और जिसके गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर वह लक्षणात्मक अर्थ नहीं निकलता।“
‘अक्ल’ सम्बन्धी मुहावरे
- अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना (समझाने पर भी न मानना) अरे पत्नी को ऐसे डाँटा जाता है, तुमने तो अक्ल के पीछे लाठी ले रखी है।
- अक्ल चरने जाना (कुछ न सोचना) उस कर्मचारी को अक्ल चरने गई थी, जो अपने वरिष्ठ अधिकारी से जा भिड़ा।
- अक्ल बड़ी या भैंस (शारीरिक शक्ति का महत्त्व कम होता है, बुद्धि का अधिक) किसी विद्वान से वार्ता करने पर पता लगता है कि अक्ल बड़ी या भैस |
- अक्ल का दुश्मन (मूर्ख) अरे अगल के दुश्मन तीन और पाँच आठ होते है।
‘आँख’ सम्बन्धी मुहावरे
- आँख का तारा (अत्यन्त प्यारा) दिव्यांशु, मेरा पुत्र मेरी आँखों का तारा है।
- आँखें चार होना (दृष्टि का मिलना) जैसे ही आँखे चार हुई, पप्पू पागल हो गया |
- आँखों से गिरना (मान घटाना) कायर व्यक्ति सबको आँखों से गिर जाता है।
- आँख में धूल झोंकना (धोखा देना) झूठ बोलकर माता-पिता की आंखो में धूल झींकना गलत बात है।
‘कान’ सम्बन्धी मुहावरे
- कान में तेल डालना (ध्यान न देना) सॉरीन तो कानों में तेल डालकर बैठी है, फिर उसे कौन समझा सकता है।
- कान काटना (दूसरों से अच्छा काम करना) हरीश केवल आठ वर्ष का है, किन्तु गाने में अच्छे-अच्छों के कान काटता है।
- कानों कान खबर न होना (गुप्त रहना) मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव मेरठ आए, कोई किन्तु किसी को
- कान पर जून रेगना (कोई असर न होना) मां-बाप के समझाने पर भी उसके कान पर नरेगी।
‘नाक’ सम्बन्धी मुहावरे
- नाक रगड़ना (दोनतापूर्वक प्रार्थना/ विनती करना) उसको तो हर एक के सामने नाक एण्ड़ने की आदत है।
- नाक कटना (प्रतिष्ठा नष्ट होना) तुम्हारे बुरे कार्यों के कारण इस परिवार को तो नाक ही कट गई।
- नाक रख लेना (इज्जत बचाना मेरे पुत्र परीक्षा में श्रेष्ठक प्राप्त की नाक रख लो।
- नाक का बाल होना (अतिप्रिय) राम अपने भाइयों की नाक का बाल है।
‘दाँत’ सम्बन्धी मुहावरे
- दांत खट्टे करना (हरा देना) भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे।
- दाँतों तले अंगुली दबाना (आश्चर्यचकित होना) महारानी लक्ष्मीबाई के रण-कौशल को देखकर अंग्रेजों ने दांतों तलेअंगुली दबा ली |
- दाँत पीसना (अत्यधिक क्रोष दिखाना) उसे गरीब समझकर क्यों दाँत पीस रहे हो |
‘सिर’ सम्बन्धी मुहावरे
- सिर पीटना (पछताना) अब सिर पीटने से क्या लाभ ? जो होना था सो तो हो गया |
- सिर नीचा होना (शर्मिन्दा होना) जीवन में कोई ऐसा काम मत करना कि सिर नीचा हो जाए |
- सिर की बाजी लगाना (मौत से न डरना) देश की स्वतन्त्रता के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों ने सिर की बाजी लगा दी थी।
‘मुँह’ सम्बन्धी मुहावरे
- मुँह सी लेना (चुप हो जाना) अपनी दादी की जली फटी सुनकर उसने तो अपना मुँह सी लिया था।
- मुँह पर कालिख पोतना (कलंक लगाना) उसके पौत्र ने तो अपनी अधम प्रवृत्तियों के कारण अपने दादा के मुँह पर कालिख ही पोत दी।
- मुँह तोड़ जवाब देना (कढ़ा उत्तर देना) पड़ोसी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जीवन भर भुला भी नहीं सकेगा।
- मुँह में पानी भर आना (लालच करना) एक पड़ोसी को आम खाता देखकर हरि के मुंह में पानी भर आया।
गर्दन‘ सम्बन्धी मुहावरे
- गर्दन झुकना (लज्जित होना) रामेश्वर जब चुनाव में हार गया तो गर्दन झुकाकर बैठ गया।
- गर्दन पर सवार होना (पीछे पढ़ना) मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम मेरी गर्दन पर सवार हो रहे हो।
- गर्दन पर छुरी फेरना (अत्याचार करना) उससे बचकर रहना; पता नहीं कब वह गर्दन पर छुरी फेर दे |
- गर्दन फाँसाना (चक्कर में पढ़ना) रामादीन के साथ रियाज ने भी अपनी गर्दन फंसा रखी है।
‘हाथ’ सम्बन्धी मुहावरे
- हाथ मलना (पछताना) चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई।
- हाथ-पाँव मारना (अन्तिम शक्ति भर उपाय करना) खूब हाथ-पाँव मारने पर भी तुम मकान नहीं बनवा पाए।
- हाथ साफ करना (चोरी करना) उसने तो मेरी मोटर साइकिल पर हाथ साफ कर दिया।
‘अँगुली’ सम्बन्धी मुहावरे
- अंगुली पकड़ते पहुंचा पकड़ना (थोड़ा प्राप्त करने पर अधिक अधिकार जमाना) पहले कौशिक, कभी-कभी बाइक माँग कर ले जाता था, किन्तु अब उसने अंगुली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लिया है।
- अंगुली उठाना (दोष दिखाना) मेरे चरित्र पर आज तक कोई भी अंगुली नहीं उठा सका।
- अंगुली पर नचाना (संकेत पर कार्य करना) में अपनी पत्नी को अंगुलियों पर नचाता हूँ।
- पाँचों अंगुलियाँ घी में होना (लाभ-ही-लाभ होना) बुद्ध के अवसर पर जमाखोरों की पाँचो अंगुलियाँ भी में होती है।
‘कलेजा’ सम्बन्धी मुहावरे
- कलेजा ठण्डा होना (सन्तुष्ट एवं शान्त होना) दुश्मन की अपराधियों द्वारा हत्या होने पर ही उसका कलेजा ठण्डा हुआ।
- कलेजे पर पत्थर रखना (दिल मजबूत करना) पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही सहन कर पाते है।
- कलेजे पर साँप लोटना (अन्तदहि होना) पड़ोसी का मकान बनता देख श्यामलाल के कलेजे पर साँप लोटने लगा।
- कलेजा मुँह को आना (घबरा जाना) किसी भी दुर्घटना को देखकर महिलाओं का कलेजा मुँह को आ जाता है।
‘खून’ सम्बन्धी मुहावरे
- खून खौलना (क्रोधआना) पड़ोसी के सिर पर मोटर दुर्घटना द्वारा चोट देखकर मोटर के ड्राइवर के प्रति उसका खून खौलने लगा।
- खून का प्यासा होना (प्राण लेने को तत्पर) विभिन्न झगड़ों में राम और श्याम भी एक-दूसरे के खून के प्यारे हो गए।
- खून का घूंट पीना (क्रोष को दबाना) अपनी सास के समक्ष पत्नी द्वारा लताड़ने पर दिलशाद खून का घूँट पीकर रह गया।
- खून-पसीना एक करना (कठिन परिश्रम करना) परीक्षा में कु. सुनीता ने खून-पसीना एक कर दिया।
‘पानी’ सम्बन्धी मुहावरे
- पानी-पानी हो जाना (बहुत शर्मिन्दा होना) जब कालू, मोबाइल चुराते पकड़ा गया तो वह पानी-पानी हो गया।
- पानी फेर देना (निराश कर देना) मेरा मेरे सारे किए-कराए पर पानी फेर गया।
- पानी में आग लगाना (असम्भव को सम्भव करना) पूरे जिले में टॉप करके उसने पानी में आग लगा दी है।
- पानी पी-पी कर कोसना (बहुत बुरा-भला कहना) अगर हिमांशु को मेरा कोई भी परिचित मिलता है तो वह मुझे पानी पी-पी कर कोसता है।
‘हवा’ सम्बन्धी मुहावरे
- हवाई किले बनाना (ऊँची कल्पना) रहीम वार्ड मेम्बर का चुनाव हार गया, परन्तु अब वह ‘एम.पी.’ चुनाव के लिए हवाई किले बना रहा है।
- हवा निकलना (बहुत डरना) बड़े बहादुर बन रहे हो, अरविन्द केजरीवाल के मुख्यमन्त्री बनते ही तुम्हारी हवा क्यों निकल रही है?
- हवा हो जाना (गायब हो जाना) राचा और प्रतिभा देखते ही देखते हवा हो गई।
- हवा लगना (संगति का प्रभाव नकारात्मक अर्थ में) अरे! आजकल के लड़कों को ऐसी हवा लगी है, कि पढ़ते ही नहीं।
‘अपना’ सम्बन्धी मुहावरे
- अपना घर समझना (संकोच न करना) प्रिय पुत्रवधू तुम्हें इस घर को अपना घर समझकर ही रहना है।
- अपना उल्लू सीधा करना (स्वार्थ पूरा करना) आजकल अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति ही समझदार माना जाता है।
- अपना राग अलापना (अपनी ही बात कहना) कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थवश अपना ही राग अलापते रहते हैं।
- अपना सा मुँह लेकर रह जाना (लज्जित होना) वास्तविकता का पता चलने पर अपना सा रह गया।
‘आसमान’ सम्बन्धी मुहावरे
- आसमान टूट पड़ना (अचानक मुसीबत आना) माता जी की मृत्यु के उपरान्त रमेश की तीनों पुत्रियों पर आसमान टूट पड़ा है।
- आसमान से बातें करना (बहुत ऊँचा होना) भारतीय ध्वज आसमान से बातें करता हुआ बहुत सुन्दर लग रहा है।
- सातवें आसमान पर दिमाग होना (अहंकारी होता) प्रोमोशन होते ही हलीम का दिमाग आसमान पर हो गया है।
- आसमान पर चढ़ा देना (अधिक प्रशंसा करके ऊपर उठाना) बातों ही बातों में मोहन ने कल्लू को आसमान पर चढ़ा दिया।
‘रंग’ सम्बन्धी मुहावरे
- रंग उतरना (रौनक खत्म होना) चुनाव में हारने के कारण प्रत्याशी के चेहरे का रंग उतर गया।
- रंग जमाना (धाक जमाना) अमिताभ बच्चन ने आज भी फिल्मी क्षेत्र में अपना रंग जमा रखा है।
- रंग में भंग पढ़ना (आनन्द में विघ्न होना) चौराहे पर दुर्घटना होने पर यात्रियों में रंग में भग पड़ गया।
- रंग में रंगना (प्रभावित होना) आजकल सभी छात्र टी. वी. और बाइक के रंग में रंगे हुए हैं।
‘प्राण’ सम्बन्धी मुहावरे
- प्राण फूंकना (जीवन प्रदान करना) महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन अपने प्राण फूंक दिए।
- प्राण हथेली पर लेना (मृत्यु के लिए तैयार रहना) भारतीय सैनिक शत्रुओं का सामना प्राण हथेली पर लेकर करते हैं।
- प्राणों की बाजी लगाना (बलिदान के लिए तत्पर रहना) झांसी की रानी ने आजादी लिए प्राणों की बाजी लगा दी।
‘बात’ सम्बन्धी मुहावरे
- बात बनना (कार्य सिद्ध होना) यदि आप नगरपालिका अध्यक्ष से मेरी सिफारिश कर दें तो मेरी बात बन जाएगी।
- बात बनाना (गम मारना) वास्तविक रूप से कार्य करने में आनन्द आता है बातें बनाने में नहीं।
- बात की बात (चर्चा या प्रसंग के कारण किसी बात का कहा जाना) बात की बात से ही अनेकों बातों की उत्पत्ति होती है।
- बात जमना (समझ में आना) मुझे पुत्री की शादी को वाराणसी से जमी लग रही है।
‘अंक’ सम्बन्धी मुहावरे
- एक और एक ग्यारह होना (संगठन से शक्ति बढ़ जाना) तुम्हें अपने ताऊ जी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि एक और एक ग्यारह होते हैं।
- दो-दो हाथ करना (पुद्ध करना, लड़ना) पाकिस्तान से दो-दो हाथ किए बिना कश्मीर समस्या नहीं सकती।
- तीन तेरह होना (बिखर जाना) श्यामू का कितना बड़ा परिवार था पर अब तो तीन तेरह हो गया।
- चार चाँद लगना (सुन्दरता बढ़ना) नए भवन में फर्नीचर को शोभा से चार चाँद लग गए है।
- पाँचों उँगलियाँ घी में होना (लाभ-ही-लाभ होना) चिन्ता मत करो, मेरे पतिदेव पुलिस महानिदेशक हो गए है; अब तो हमारी पाँचो उँगलियों घी मे है।
- छठी का दूध याद आना (अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना) अंग्रेजी का प्रश्न पत्र देखते हो मुझे छठी का दूध याद आ गया।
- आठ-आठ आँसू रोना (पछतावे में रोना) मेरा मित्र जब से माता-पिता से अलग हुआ तो वह आठ आठ आँसू रोता रहता है।
- नौ दो ग्यारह होना (भाग जाना) दिल्ली को देखक हो गए।
कुछ विभिन्न मुहावरे
- आस्तीन का साँप (विश्वासघाती मित्र) रमेश पक्का आस्तीन का साँप है, उससे सतर्क रहना।
- काठ का उल्लू (मूर्ख) सिर्फ काठ के उल्लू रह जाओगे, यदि आज के युग में कम्प्यूटर और अंग्रेजी नहीं सीखोगे।
- चूड़ियाँ पहनना (कायरता दिखाना) देश की रक्षा न कर पाने से तो अच्छा कि भ्रष्ट नेता चूड़ियाँ पहनकर घर बैठे।
- पेट में दाड़ी होना (कम उम्र में अधिक जानना) दिव्यांशु को कम मत समझो, इसके पेट में दाड़ी है।
- पौ बारह होना (अत्यधिक लाभ होना) सोने के व्यापार में उमा के पौ बारह हो गए है।
- लुटिया डुबोना (काम बिगाड़ना) शेयर बाजार ने इस बार बड़े-बड़ों को लुटिया डुबो दी।
- सिर ऊंचा करके चलना (स्वाभिमान से जीना) जे. के. रस्तोगी अपने दोनो पुत्री के आई. ए. एस. बनने पर स्वाभिमान से जी रहे हैं।
- हिरन हो जाना (दूर भाग जाना) अब हिरन हो जाओ, नहीं तो पिट जाओगे।
- सफेद झूठ (बिल्कुल झूठ) उसके पी. सी. एस. में चयन होने का समाचार सफेद झूठ है |
- दूध की मक्खी होना (किसी को तुच्छ समझकर अलग कर देना) सोनू सेठ अपने नौकर टोनू को घर से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया।
- बगुला भगत होना (निरा पाखण्डी) आजकल अनेक लोग पीले वस्त्र धारण कर बगुला भगत बन बैठे हैं।
- पापड़ बेलना (कष्ट झेलना) हरि को अपने पुत्र की नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े।
- पत्थर की लकीर (अमिट बात) महापुरुषों के कथन पत्थर की लकीर होते हैं।
- तलवे चाटना (खुशामद करना) कामचोर रमेश अपने अधिकारों के सदैव तलवे चाटता रहता है।
- झाँसे में आना (धोखे में आ जाना) पहले मैं उसको वास्तविकता नहीं जानता था, पर अब झांसे में नहीं आऊंगा।
- खेत रहना (मारा जाना) धन्नाराम बड़ी डाँग मार रहा था, पर एक लाठी पड़ी ही खेत रह गया।
- कलम घिसना (बेकार की मेहनत) आजकल के बच्चों का पढ़ना-लिखना हो क्या रहा? कलम पिसना चल रहा है।
लोकोक्ति
लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव पर आधारित वे कथन है, जिनका प्रयोग परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यंजना शक्ति को प्रधानता होती है, जैसे मुँह में राम बगल में छुरो, काला अक्षर भैसक आदि। इनके क्रमशः अर्थ है-कपटी व्यक्ति और बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति |
भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है।
लोकोत्तियां प्रायः किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है। लोकोक्तियाँजीको है। इनका प्रयोग बोलचाल की अधिक होने के कारण इन्हें भी है।
लोकोत्तियाँ वभिन्न विषयों से सम्बन्धित होती है। विद्वानों ने लोकोत्तियों को कृषि सम्बन्धी समयक कर उनका विस्तृत अध्ययन किया है।
प्रमुख लोकोक्तियाँ एवं उनके अर्थ
यहाँ कुछ लोकप्रिय लोकोक्तियाँ दी गई है-
- एक पन्य दो काज- एक हो उपाय से दो कार्य करना।
- एक थाली के चट्टे-बट्टे- सबका एक-सा होना।
- एक और एक ग्यारह होते हैं- एकता में शक्ति होती है।
- एक चुप्पी सौ को हराए- चुप रहने वाला अच्छा होता है।
- एक तन्दुरुस्ती हजार नियामत- स्वास्थ्य का अच्छा रहना सभी सम्पत्तियों में श्रेष्ठ होता है।
- एक म्यान में दो तलवारे नहीं समा सकती- एक स्थान पर दो विचारधाराएँ नहीं रह सकती।
- कूपमण्डूक होना- संकीर्ण विचारों का व्यक्ति |
- कागा चला हंस की चाल- अयोग्य व्यक्ति का योग्य बनने का प्रयत्न करना।
- कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा-भानुमती ने कुनबा जोड़ा- आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं का एक साथ संग्रह करना।
- कंगालों में आटा गीला- विपत्ति पर विपत्ति आना।
- कभी भी चना, कभी मुट्ठी पर बना, कभी वह भी मना- जो कुछ मिले उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिए।
- कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर- समय पड़ने पर एक-दूसरे की मदद पर करना।
- का बरखा जब कृषि सुखाने- काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है।
- अन्धेर नगरी चौपट राजा- मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय का बोलबाला होना।
- होनहार विरवान के होत चीकने पात- महानता के लक्षण प्रारम्भ में हो प्रकट हो जाते हैं।
- शौकोन बुड़िया चटाई का लहंगा- विचित्र शौख।
- मुख में राम बगल में छुरी- कपटपूर्ण व्यवहार |
- मेडकी को जुकाम- अपनी औकात से ज्यादा नखरे |
- पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े- ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं।
- प्यादे ते फरजी भयो हो जाए- व्यक्ति पद पाने पर इतराने लगता है।
- बीरबल की खिचड़ी- अत्यधिक विलम्ब से कार्य होना।
- नाच न आए आँगन टेढ़ा- गुण अथवा योग्यता न होने पर बहाने बनाना।
- जैसा देश वैसा भेष- परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना।
- सकी उसकी भैंस- किसी भी वस्तु आदि पर शक्तिशाली का ही अधिकार होना।
- खरी मजूरी चोखा काम- उचित मजदूरी देने से काम भी अच्छा होता है।
- गुड़ न दें. गुड़ की बात तो करे- चाहे कुछ न दे, परन्तु वचन तो मीठे बोले।
- घर की मुर्गी दाल बराबर- घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता |
- घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या?- मजदूरी मांगने में संकोच करना व्यर्थ है।
- गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज- दिखावटी परहेज |
- चमड़ जाए पर दमड़ो न जाए- कंजूस होना |
- चिकने मुँह को सभी चूमते है- धनवान की सभी चापलूसी करते है |
- चूहे का जाया बिल ही खोदता है- बच्चे में पत्रिक्गुन ही आते हैं |
- चलती का नाम गाड़ी- जिसका नाम चल जाए, वही योग्य है।
- घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने- झूठी शान दिखाना।
- कोयले की दलाली में हाथ काले- कुसंगति से कलक ही लगता है।
- कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली- दो असमान वस्तुओं की तुलना करना।
- कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता- हाथी मनुष्य दूसरे के कहने से काम नहीं करता है।
- मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊँ- आश्रयदाता को आँखें दिखाना।
- भई मति साँप छयूदर केरी- असमंजस की स्थिति में रहना।
- दूध का दूध पानी का पानी- सही न्याय करना।
- दाल भात में मूसलचन्द- व्यर्थ में दखल देना।
- नीम हकीम खत्तराए जान- अल्पज्ञान खतरनाक होता है।
- बद अच्छा बदनाम बुरा- बुरे कमों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा है।
- इस हाथ दे उस हाथ ले- कर्म का फल शीघ्र मिलता है।
- थोथा चना बाजे घना- ओछा आदमी अपने महत्त्व का अधिक प्रदर्शन करता है।
- चिराग तले अंधेरा- अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता।
- नाम बड़े दर्शन छोटे- प्रसिद्धि के अनुरूप गुण न होना।
- नेकी और पूछ-पूछ– बिना कहे ही भलाई करना |
- आया है तो जाएगा- राजा रंक फकीर सबको मृत्यु सुनिश्चित है।
- कानी के ब्याह में सौ जोखीम- कमी होने पर अनेक बाधाएँ आती है।
- चित भी मेरी पट्ट भी मेरी- शक्तिशाली अपना लाभ हर तरफ से चाहता है।
- डेढ़ पाव आटा पुल पै रसोई- थोड़ी सम्पत्ति पर भारी दिखावा |
- जैसे नागनाथ वैसे साँपनाथ- दुष्टी की प्रवृत्ति एक जैसी होना।
- तन पर नहीं लत्ता, पान खाप अलवता- झूठी रईसी दिखाना।
- तीन लोक से मथुरा न्यारी- सबसे अलग रहना।
- चट मंगनी पट ब्याह- शुभ कार्य तुरन्त सम्पन्न कर देना चाहिए।
- ओछे की प्रीत बालू की भीत- ओछे व्यक्ति से मित्रता निभती नहीं है।
- छछूंदर के सिर में चमेली का तेल- कुरूप के लिए सौन्दर्य प्रसाधन |
- तिरिया तेल हमोर हठ चढ़े न दूजी बार- प्रतिज्ञ लोग अपनी बात पर डटे रहते है।
- पाँव मारिए जेती लम्बी सौर- सामर्थ्य के भीतर कार्य करना।
- उठी पैठ आठवें दिन लगती है- अगसर रोज-रोज नहीं आता है।
- अन्या क्या चाहे दो आँखें उपयोगी- वस्तुओं का मिल जाना |
- ऊँट के मुंह में जीरा- आवश्यकता से कम प्राप्त होना।
- एक पूड़े बैल को कौन बाँध भुस देय- अकर्मण्य को कोई नहीं रखता है।
- काला अक्षर भैस बराबर- निरक्षर या अनपढ़ |
- काम का न काज का दुश्मन अनाज का- निकम्मा व्यक्ति |
- काठ की हंडिया बार-बार नहीं चढ़ती- कपटी व्यवहार हमेशा नहीं जा सकता |
- खिसियानी बिल्ली खम्म नोचे- व्यर्थ झुंझलाना |
- उल्टे बाँस बरेली को- विपरीत कार्य करना।
- ऊंट को चोरी निहुरे निहुरे- बड़ा काम लुक छिपकर नहीं होता है।
- खग जाने खग की ही भाषा- समान प्रकृति वाले लोग एक-दूसरे को समझ पाते हैं।
- अंगूर खट्टे है- वस्तु न मिलने पर उसमे दोष निकालना।
- बाँझ क्या जाने प्रसव की पीर- भुक्तभोगी ही दुःख का अनुमान सकता है।
- हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और- करनी और कथनी में अन्तर होना।
- विधि का लिखा को मेटन हारा- भाग्य में लिखा होकर रहता है।
- मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त- जिसका काम वही ढीला।
- मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक- सीमित पहुँच होना।
- पढ़े फारसी बेचे तेल- यह देखो किस्मत का खेल-अधिक योग्य कम योग्यता का काम करना।
- नौ नकद न तेरह उधार- वर्तमान पर ध्यान देना ही उचित है।
- अधजल गगरी छलकत जाए- अल्पज्ञ अहंकारी होता है।
- आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक- विरागी धन दौलत की चिन्ता नहीं करता है।
- अन्धा बाँटे रेवड़ी, अपने-अपने को देय- पक्षपात करना।
- अन्धी पीसे कुत्ता खाय- देखभाल न करने से फल दूसरे ले जातें हैं |
- आँख का अन्धा नाम नैनसुख- नाम के विपरीत गुण।
- दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम- दो कार्यों में भटकना अच्छा नहीं।
- न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी- काम न करने के उद्देश्य से बहाने बनाना।
- भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय- अपात्र से बात न करो।
- राम-राम जपना पराया माल अपना- धोखा देकर माल हड़पना।
- गोदी में छोरा गाँव में ढिंढोरा- पास की वस्तु को न देख पाना।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं-
यह भी जाने
- पूर्णतावाद का सिद्धान्त
- ग्रीन के सर्वगत कल्याण सिद्धान्त की आलोचना
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय | Nature and subject of moral judgment in Hindi
- प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त | Principle of dependent origination in Hindi
- नीतिशास्त्र तथा धर्म के मध्य सम्बन्ध | relationship between ethics and religion in Hindi
मुहावरे क्या होते हैं ?
लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिये |
मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का क्या अर्थ है ?
हिरन हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है ?
- पद परिचय | पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण |
- जैव-प्रौद्योगिकी क्या है ? | Biotechnology in hindi | आनुवंशिक अभियान्त्रिकी | Genetic Engineering in hindi |
- जैव विकास एवं आनुवंशिकी | Genetics and Evolution in hindi | डार्विनवाद | लैमार्कवाद |
- हृदय-स्पन्दन या हृदय की धड़कन | Heart Beat in hindi | रक्त चाप | Blood Pressure in hindi |
- मनुष्य में रुधिर परिसंचरण | Blood Circulation in Human in hindi |
