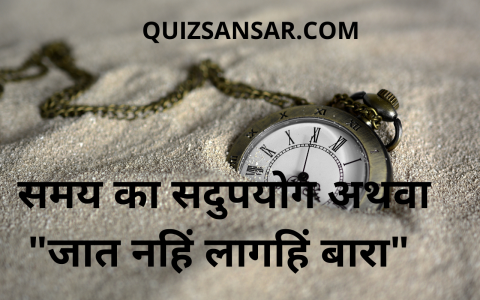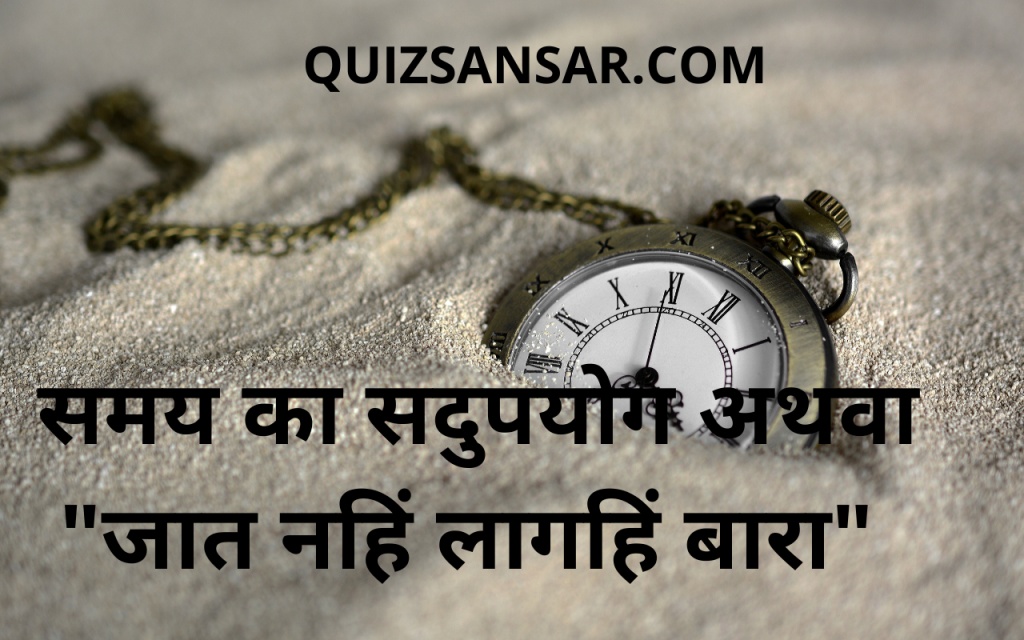“जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना” | essay in hindi | निबंध |
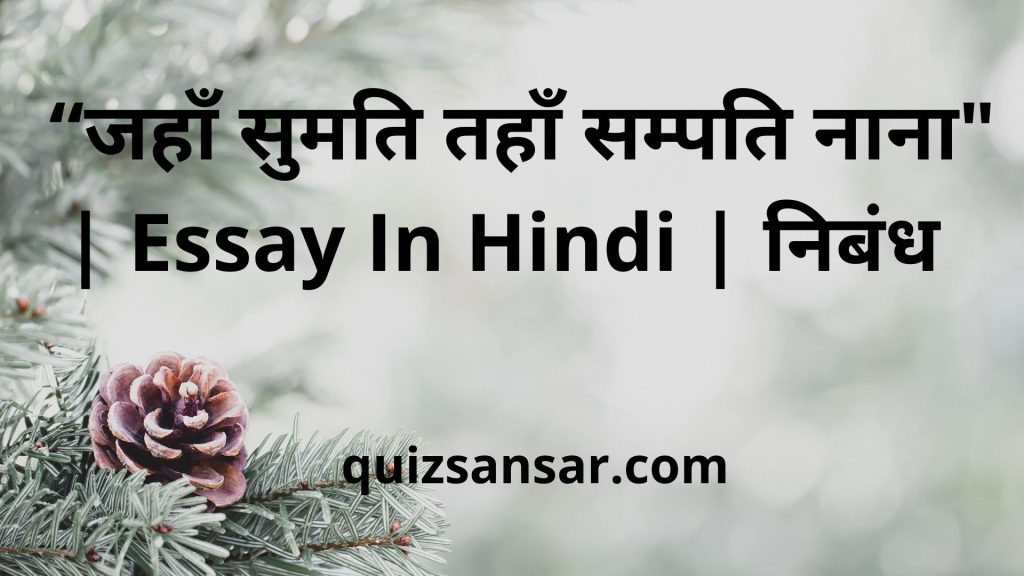
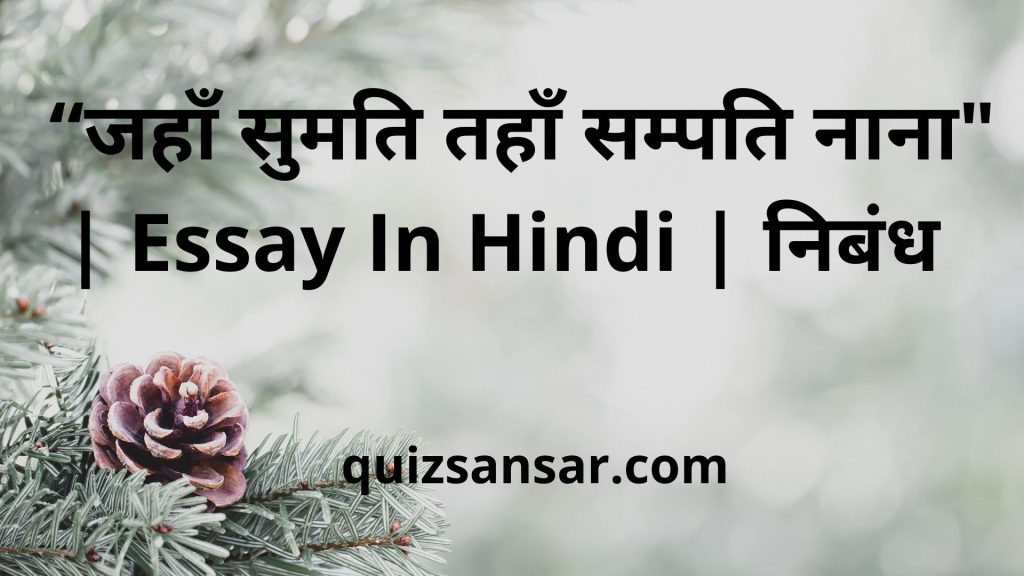
नमस्कार दोस्तों आज की post का शीर्षक है निबंध | “जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना” | Essay In Hindi | उम्मीद करतें हैं की आपको यह अवश्य पसंद आयेगा | धन्यवाद |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- सुमति की शक्ति
- सुमति से धन
- सुमति से ऐश्वर्य
- सुमति से सुख और शांती
- सुमति से हानि
- उपसंहार
प्रस्तावना
“वन्दनीय वह देश, जहाँ के वासी निज अभिमानी हों।
बान्धवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो ।”
वास्तव में वह देश वन्दनीय है, जहाँ के निवासियों को अपने देश पर गर्व हो, जिनमें स्वाभिमान हो और जो परस्पर बन्धुत्व की भावना से बंधे हुए हों ।
वह देश निःसन्देह उन्नति के चरम शिखर में स्वयं समर्थ होगा। एकता के सूत्र में बंधा देश कभी पर पहुंचेगा, वह शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपनी रक्षा करने परतन्त्र और पराधीन नहीं हो सकता।
उसमें शत्रु को धराशायी करने की शक्ति होती है। किसी की ताकत नहीं कि उनकी तरफ आँख उठाकर भी देख ले।
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की समृद्धियाँ उसे सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं और वह अन्य देशों में शिरोमणि देश गिना जाता है।
परन्तु देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये जनता में एकता होनी चाहिये। वह एकता विचारों की एकता हो, भावों की एकता हो, भाषा की एकता हो अथवा धार्मिक एकता हो।
एक धागे को आसानी से तोड़ा जा सकता है, परन्तु वे सभी धागे मिलकर जब एक मोटी रस्सी बन जाते हैं, तो उससे केवल कुयें में से पानी ही नहीं हाथी भी बँधे चले आते हैं।
इसलिये कहा गया है कि-
“संघे शक्तिः कलियुगे।”
कलियुग में संघ में ही शक्ति है। अकेला मनुष्य यदि कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पीछे एक सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति न हो।
देश की स्थिति के समान ही घर की स्थिति समझनी चाहिये। जिस घर में सदैव कलह और झगड़े बने रहते हैं वहाँ सदैव दरिद्रता निवास करती है, एक न एक दिन उस घर का विनाश हो जाता है।
जिस घर में सभी मेल-जोल से हिल-मिलकर रहते हैं, वह घर दिन पर दिन उन्नति करता है, वहाँ लक्ष्मी, सुख और शान्ति निवास करती है।
जहाँ हृदय की एकता और विचारों का साम्य होगा, वहाँ धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति, यश-गौरव स्वयं खिचे चले आयेंगे।
इसीलिये तुलसीदास जी ने लिखा है-
“जहाँ सुमति तह सम्पति नाना।
जहाँ कुमति तह विपति निदाना || “
सुमति का शाब्दिक अर्थ है “अच्छी मति” अर्थात् सद् विचार, मतैक्य, मेलजोल, सद्भावना, आपसी सहयोग सभी लक्षण सुमति के अन्तर्गत आते हैं।
सुमति की शक्ति
सुमति से मनुष्य में शक्ति आती है। आये दिन समाज में देखा जाता है कि जिस घर में एक ही आदमी होता है।
उसको सड़क पर पकड़ कर कोई भी पीट लेता है और जिसके चार-छह भाई होते हैं, सभी मिल-जुलकर रहते हैं, उनसे मुहल्ले वाले भी डरते हैं।
वे जानते हैं कि अगर एक से भी कुछ कह दिया तो सभी लड़ने चले आयेंगे और जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। यह प्रताप घर में सुमति का है, एकता का है।
आप अपनी एक उंगली किसी पर उठायें, उस उंगली को आसानी से पकड़कर कोई भी तोड़-मरोड़ सकता है, परन्तु जब चारों उंगली मिलकर घूंसा बना लेती हैं और ऊपर से उनका सरदार अंगूठा मजबूती से उनकी रक्षा को उनके ऊपर बैठ जाता है, तो बड़े-बड़े शत्रु भी उस घूंसे को देखकर दहल जाते हैं।
यह है एकता और सुमति की शक्ति। इसीलिए एकता को ही बल कहा गया है।
अंग्रेजी में कहते हैं “Unity is strength” संस्कृत की परिभाषा तो स्पष्ट है ही “संघे शक्ति: कलियुगे” फिर अर्जन करने में सुमति की बड़ी आवश्यकता है।
दसवीं शताब्दी में विदेशी यवनों ने भारत पर आक्रमण किये और यहाँ के राजपूत सरदार पराजित होते चले गये। कारण क्या था ?
देश में सुमति का अभाव। सभी राजपूत राजे-महाराजे अपनी-अपनी रियासतों को ही स्वतन्त्र राष्ट्र मान बैठे थे, उन्हें आत्म-गौरव का तो ध्यान था, परन्तु देश के गौरव का किसी को ध्यान नहीं था।
उन्हें व्यक्तिगत मान-मर्यादा की चिन्ता थी, परन्तु सामूहिक रूप से अपनी जाति, अपने देश और अपने धर्म का बिल्कुल ध्यान नहीं था।
फलस्वरूप शत्रु के सामने एक सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति का परिचय न दे सके और यहाँ यवनों का झण्डा फहराने लगा।
यही अंग्रेजों ने किया, उन्होंने “Divide and Rule” को कूटनीति के आधार पर लगभग दो सौ वर्ष तक भारत पर अपना अधिकार रखा।
यह सब सुमति और एकता के अभाव का ही परिणाम था।
सुमति से धन
अकेला व्यक्ति कितना ही परिश्रम करे उतना पैसा पैदा नहीं कर सकता, जितना कि घर के चार छः व्यक्ति मिलकर एक व्यापार को ऊपर उठा ले जाते हैं।
कहावत भी है कि, “अकेला बना भाड़ नहीं फोड़ता।” जिस घर में सुमति का साम्राज्य होता है, उस घर की आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है और जहाँ कुमति होती है वहाँ सभी अपनी-अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं।
परिणाम यह होता है कि व्यापार में लगाई गई असल पूँजी भी कुछ दिनों में साफ हो जाती है क्योंकि उन सभी के सामने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और व्यक्तिगत लक्ष्य हैं।
जहाँ सुमति होती है, वहाँ अलग-अलग स्वार्थ और लक्ष्य नहीं होते। सभी का एक लक्ष्य होता है कि हमारे घर हमारे परिवार और हमारे पूर्वजों का नाम हो यश फैले।
घर के बड़े आदमी के इशारे पर भी चलते हैं। परिणाम यह होता है कि कुछ दिनों में ही परिवार कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यही स्थिति देश की है।
जिस देश की जनता में सुमति है, एकता है, वह देश धन-धान्य से सम्पन्न होता है। एक समय था जब भारत में सुमति थी, एकता थी, तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
विश्व के जितने भी समृद्धिशाली देश हैं,
जैसे- अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि वहाँ देशवासियों में सुमति है, विचारों की एकता है, भाषा की एकता है, भावनाओं की एकता है।
वे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का देशहित के लिए बलिदान करना जानते हैं, इसलिए आज विश्व के कोने-कोने में उनकी तूती बोल रही है।
सुमति से ऐश्वर्य
संसार में दो शक्तियों महान् है–एक जनशक्ति, दूसरी धनशक्ति जिसके पास दोनों हों उसका दूसरे पर स्वयं ही प्रभाव जम जाता है।
उसे स्वयं कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप मेरा मान कीजिए या प्रतिष्ठा कीजिये। उसका ऐश्वर्य और उसका गौरव सर्वत्र स्वयं ही छा जाता है।
आज अमेरिका, इंग्लैण्ड या रूस को किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि हम तुम से बड़े हैं बल्कि स्वयं ही विश्व के समस्त देशों पर उनका ऐश्वर्य छाया हुआ है।
यहाँ स्थिति परिवार की है, जिस परिवार में घन-जन की शक्ति पर्याप्त होती है, उसका यश और ऐश्वर्य मुहल्ले में क्या सारे नगर में छा जाता है, चारों ओर कीर्ति फैलने लगती है।
जिस जाति, जिस समाज और जिस देश में लोग परस्पर मेल-जोल, बन्धुत्व की भावना, परस्परावलम्बन, सहयोग तथा सहानुभूति से कार्य करते हैं, पारस्परिक स्वार्थों और मतभेदों में नहीं उलझते, उस जाति, उस देश और समाज का उज्ज्वल यश संसार में फैलता है, वह एक सार्वभौम, प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र माना जाता है।
सुमति से सुख और शांती
जहाँ सुख और शान्ति नहीं होती वह स्थान मनुष्य के लिये नर्क बन जाता है, दिन-रात झगड़े होते हैं, कलह होती है, एक की बात दूसरे को सहन नहीं होती, एक का खाया दूसरा देख नहीं सकता, एक की अच्छी कही हुई बात भी दूसरों को काँटे की तरह चुभती है।
जहाँ एक-दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार बैठा रहता है, जहाँ कुमति का गहन अन्धकार छाया हुआ है, वहाँ स्वर्ग को कल्पना कैसे की जा सकती है, वह तो पोर नर्क है।
मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग की सृष्टि कर लेता है और अपने कर्मों से ही नर्क की। जहाँ मुमति है, वहाँ स्वर्ग है, सुख है, शान्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ नर्क है, कलह है, अशान्ति है।
गुप्त जी ने लिखा है-
“बना लो जहाँ, हाँ, वहीं स्वर्ग है, स्वयं भू थोड़ा कहीं स्वर्ग है।
खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है, भलों के लिए तो यही स्वर्ग है |”
जीवन में सफलता की कुंजी सुमति है। जहाँ सुमति है वहाँ धन-धान्य, सम्पत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, यश, गौरव सभी कुछ है फिर भला मनुष्य को सुख और शान्ति कैसे नहीं मिलेगी ?
जीवन को असफलतायें मनुष्य को दुःखी, अशान्त बना दिया करती हैं परन्तु सफलता तो सुमति की दासी है, जहाँ सुमति होगी, वहाँ सफलता अवश्य होगी और जहाँ सफलता होगी वहाँ सुख और शान्तिः भी अवश्य होगी।
श्रीधर पाठक का भाव देखिये-
“जन-जन सरल सनेह सुजन व्यवहार व्याप्त नहिं
निर्धारित नर नारि उचित उपचार आप्त नहि।
कलि-मल मूलक कलह कभी होवे समाप्त नहि
वह देश मनुष्यों का नहीं प्रेतों का ही घेरा है।
नित नूतन अद्य उद्देशयल भूतल नरक निवेश है । “
सुमति से हानियाँ
जिस परिवार में या जिस देश में कुमति घुसी हुई है, वह कभी फल-फूल नहीं सकता। कुमति से मनुष्य को कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती।
समाज में वह अपमान का पात्र बना रहता है। कलहपूर्ण घर की धन जन शक्ति नष्ट हो जाती है। एक समय वह आ जाता है कि पेट भरने के लिये रोटियाँ भी नहीं मिल पाती औरुन शरीर ढकने के लिए कपड़े।
जो मनुष्य कलहप्रिय होता है, उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है, उनके मन और मस्तिष्क जर्जर हो जाते हैं, वह हँसने के समय भी रोता है।
कुमतिपूर्ण घर, परिवार या कुमतिपूर्ण देश समझ लीजिये कि वह विनाश के कगार पर खड़ा हुआ एक धक्के की प्रतीक्षा कर रहा है।
कुमति विनाश का घर है। झगड़ालू और कलहप्रिय व्यक्ति का जीवन भार बन जाता है, वह विश्व में आँखें फाड़कर देखता है पर दूर-दूर तक उसे अपना कोई दिखाई नहीं पड़ता, वह जीवन भर अशान्ति और विद्रोह की अग्नि में जलता रहता है।
उपसंहार
आज भारतवर्ष की स्थिति बड़ी विचित्र है। शत-शत जातियों और उपजातियों में विभक्त इस देश की अशिक्षित जनता न जाने इस देश को कहाँ ले जाकर पटकेगी ?
व्यक्तिगत स्वार्थ इतने बढ़ गये हैं कि एकता को कहीं प्रश्रय भी नहीं मिल पा रहा और लोग अपनी अपनी ढपली पर अपना-अपना राग अलापते जा रहे हैं।
पृथक्ता एकदम बढ़ती जा रही है। एकता समाप्ति की ओर अपसर होती जा रही है। देश में सुमति का नाम तक नहीं रहा।
देश की जनता में न परस्पर सहयोग है, न सहानुभूति, एक दूसरे का गला काटने को अहर्निश तैयार बैठे हैं।
भारतवर्ष जैसे विशाल देश में अनेक जातियों रहती हैं, उनकी अनेक भाषायें हैं और वे भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी हैं।
भारतीय होने के नाते राष्ट्रीयता की भावना सभी में होनी चाहिये देश हित का ध्यान सभी को रखना चाहिए।
जिस देश में हम पैदा हुए, जिसकी धूलि में लेट लेटकर हम बड़े हुए, जीवन प्राप्त किया, क्या उस मातृभूति के प्रति हमारा यहाँ कर्तव्य है कि उसके टुकड़े-टुकड़े कर दें और विनाश के मुँह में झोंक दें? लज्जा की बात है।
आज एक जाति दूसरी जाति से घृणा करता है, एक धर्मानुयायी दूसरे धर्मानुयायी को देखना तक नहीं चाहता।
एक भाषा-भाषी दूसरे भाषा-भाषों की बात सुनना भी पसन्द नहीं करता। प्रान्तीयता इतनी घुस गई कि इसके बारे में जितना कहा जाये उतना थोड़ा है।
अब विचार कीजिये कि जिस देश में कुमति घर किए हुए हो, और सुमति का कहीं नाम तक न हो उस देश का क्या भविष्य होगा ?
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना का क्या अर्थ है ?
वह निरंतर अपने कार्यों में सफलता अर्जित करता रहता हैं | इस तरह का व्यक्ति स्वहित को एक तरफ रखकर लोकहित तथा लोक भलाई के कर्म करता है. ऐसे इंसान में दूर तक देखने की शक्तियों के गुणों का भंडार होता है इसलिए इस तरह के व्यक्ति भविष्य में घटित घटना को पूर्व में ही पता कर अंजाम के लिए तैयारी कर लेते हैं |
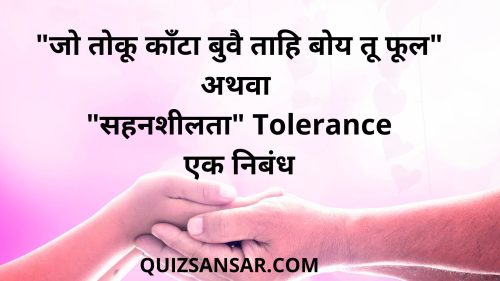
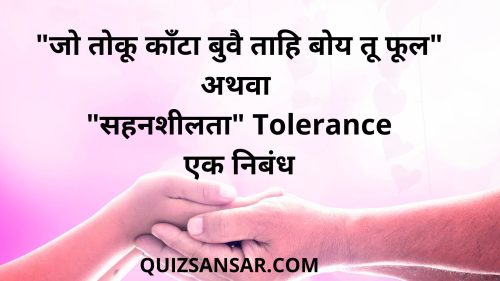
सहनशीलता अथवा “जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल” एक निबंध / Tolerance ESSAY IN HINDI
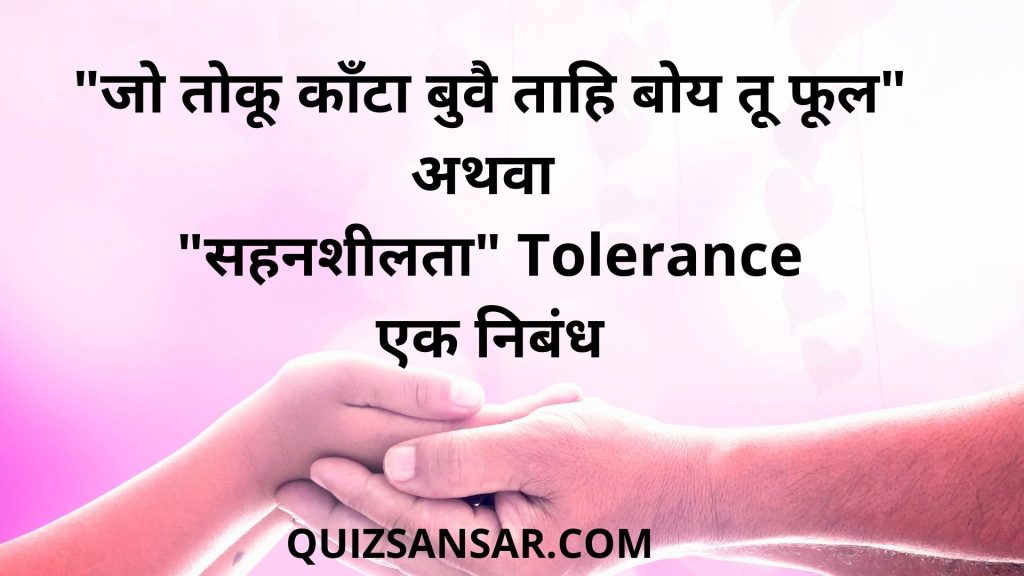
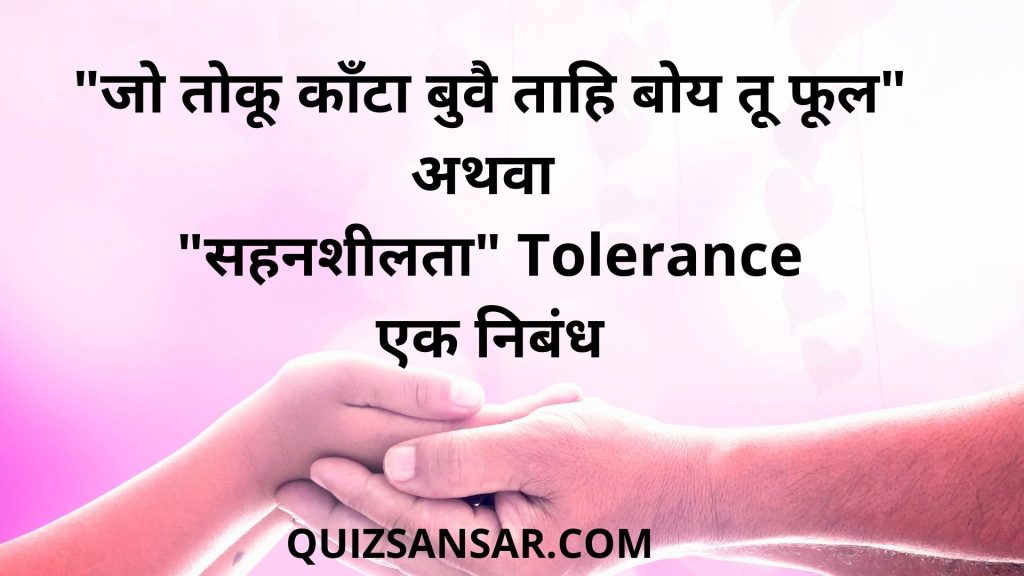
सहनशीलता अथवा “जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल”, एक सहनशीलता अथवा “जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल” एक निबंध / Tolerance ESSAY IN HINDI बहुत ही महत्त्वपूर्ण निबंध है जो हम आपके के लिए लेकर आए हैं |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- इसके लाभ
- कुछ आदर्श उदाहरण
- अभिमानी का पतन
- उपसंहार
प्रस्तावना
अजातशत्रुता एक दैवी गुण है। संसार के महान् पुरुष अजातशत्रु हुए हैं, उनकी कीर्ति आज भी विश्व के कोने-कोने में गाई जाती है।
अजातशत्रु का अर्थ है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही na हुआ हो।
जब आप किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी के मार्ग में विघ्न बनकर खड़े नहीं होंगे, या अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों के स्वार्थ को क्षति नहीं पहुँचायेंगे, तब कौन आपका शत्रु हो सकता है ?
परन्तु आज का युग ऐसे व्यक्तियों पर भी कृपा उक्ति का अर्थ और नहीं करता, उन्हें भी नहीं छोड़ता, आप भले ही किसी का अहित-चिन्तन या स्वार्थ में क्षति न करें, फिर भी ऐसे-ऐसे महापुरुष आपको मिलेंगे जो बिना किसी प्रयोजन के ही आपके मार्ग में आकर खड़े हो जायेंगे और एक विघ्न उपस्थित कर देंगे।
चाहे इस विघ्न के डालने से उनका कोई लाभ न होता हो, फिर भी उन नर पिशाचों को इन कुकृत्यों में आनन्द आता है।
“बिल्ली खायेगी नहीं तो गिरा अवश्य देगी” आदि कहावतों से ऐसे लोग अपने इन नीचतापूर्ण कृत्यों में मानसिक शान्ति प्राप्त करते हैं और अपनी विजय पर फूले नहीं समाते।
ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भर्तृहरि जी ने लिखा है कि ऐसे लोग जो निरर्थक ही दूसरों का अहित करते हैं, मैं नहीं जानता किस कोटि के हैं। वे लिखते हैं-
“ये निघ्नन्ति निरर्थक परहितम् ते के न जानीमहे ।”
सहनशीलता के लाभ
आज का संसार आपको अजातशत्रु नहीं रहने देगा। आप भले ही किसी का अहित या किसी से शत्रुता न रखें परन्तु इस घृणित समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जायेंगे, जो व्यर्थ में ही शत्रुता मान लेंगे, छिपकर आपके ऊपर तीर पर तीर चलाये जायेंगे, कभी तो आपको वह तीर लगेगा ही और आप तिलमिला उठेंगे।
इसके पश्चात् आपके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधकने लगेगी, क्योंकि मानव स्वभाव से ही प्रतिशोधपूर्ण होता है बस इस स्थिति पर विजय पाने के लिये ही प्रस्तुत निबन्ध के शीर्षक की उक्ति है।
उक्ति का अर्थ है, “जो तुम्हारे लिये काँटे बोता है, तुम उसके लिए फूल बोओ”, अर्थात् जो तुम्हारा अहित करता है तुम उसका हित करो , जो तुम्हें दुःख देता है तुम उसे सुख दो, जो तुमसे द्वेष रखता है तुम उससे प्रेम करो, जो तुम्हें हानि पहुँचा रहा है। तुम सहनशीलता रखो |
तुम उसे लाभ पहुंचाओ , जो तुम्हें गिरा रहा है तुम उसे उठाओ।
निःसन्देह एक दिन ऐसा आयेगा कि वह अपने धूर्ततापूर्ण कुकृत्यों को छोड़कर तुम्हारा प्रशंसक और सहायक बन जायेगा।
प्रतिशोध की भावना पशुओं का गुण है।
आप जाते हुए सर्प पर छोटा-सा ईंट या पत्थर का टुकड़ा फेंककर देखिए, यदि वह उसको थोड़ा-सा भी लग गया और उसने आपको देख लिया तो फिर वह आपको छोड़ नहीं सकता, चाहे आप दुनिया के किसी पर्दे पर क्यों न चले जायें।
आप किसी भैंस या बिजार या बैल की ओर लाठी उठा लीजिए , वह भी आपको सींग उठाकर मारने दौड़ेगा।
यदि आप इस पाश्विक प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप अपने को पशुओं की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान जीव समझते हैं, यदि आप शुद्ध रूप से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको इस उक्ति के अनुसार अपना जीवनयापन करना होगा, इस उक्ति को अपने जीवन की सहचरी बनाना होगा, फिर देखिये कि यह आपकी किस तरह सेवा करती है, और आपको उठाकर कहाँ से कहाँ ले जाती है।
यदि आप जीवन में उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावनाओं को तिलांजलि देनी ही होगी और उसके स्थान पर सहनशीलता, सहयोग, सहानुभूति, संवेदना और दुःख, कातरता आदि देवी गुणों को जीवन में लाना होगा।
प्रतिशोध और प्रतिहिसा की भावना से मनुष्य की आत्मा का पतन हो जाता है।
क्रोध से उसकी बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि भ्रष्ट होने से वह भिन्न-भिन्न जघन्य कुकृत्य और कुकर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसका पतन अवश्यम्भावी हो जाता है।
“कीर्तिर्यस्य स जीवति”
यश / कीर्ति
जिस मनुष्य को संसार में कोर्ति होती है, वह सदैव जीवित रहता है, भले ही वह पार्थिव शरीर से इस संसार में न रहा हो।
कोर्ति का भागी वही मनुष्य होता है, जिसमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, जो अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज की तन, मन, धन से सेवा करता है।
जो मनुष्य बुराई के बदले में सदा भलाई ही करता है, जो ईंट का उत्तर फूल से देता है, जो अपने सुकर्मों और सरल स्वभाव से घृणा को प्रेम में बदल देता है, उससे बढ़कर कौन गुणवान हो सकता है, उससे अधिक कौन समाजसेवी हो सकता है?
समाज सेवा ही वह व्यक्ति कर सकता है, जो समदृष्टय हो, सहनशील हो, सहानुभूति रखने वाला हो।
जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है यदि उसके बदले में आपने उससे सद्व्यवहार किया, जिस व्यक्ति ने आपकी निन्दा की है, यदि आपने उसको प्रशंसा की तो आप समाज के अन्य व्यक्तियों में कोर्ति के पात्र होंगे।
समाज में आपका यश बढ़ेगा, घर-घर में आपका गुणगान होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वे निन्दक ही आपके प्रशंसक बन जायेंगे।
‘क्षमाशस्त्रं कर पस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।
अतृणे पतितो बहि स्वयमेवोपशाम्यति ।।
” अर्थात् जिस मनुष्य के हाथ में समा रूपी शस्त्र है उसका दुष्ट मनुष्य क्या करेगा अर्थात् कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे बिना तिनकों वाली भूमि पर गिरी हुई अग्नि स्वयं हो बुझ जाती है |”
समाज प्रतिष्ठा
समाज ऐसे ही व्यक्ति को मूर्धन्यता प्रदान करता है, उसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जो स्वर्ण की भाँति अग्नि-परीक्षा के बाद भी मुस्कुरा रहा हो, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में भी जिसकी भौहों में सिकुड़न न पड़ी हाँ, गालियाँ खाने और पिटने के बाद भी जिसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जापत न हुई हो, चोरी करके जाते हुए तथा पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर श्री जिस धनी ने उन चोरों को अपना रिश्तेदार तथा अपहत धन को अपने हाथ से दिया हुआ उपहार बता दिया हो, इतिहास ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने स्वयं कितना ही कष्ट सह लिया, परन्तु कष्ट देने वाले के साथ थोड़ा सा भी कठोर व्यवहार नहीं किया, व्यक्तियों को उनके जीवनकाल में भी और आज भी जबकि वे नहीं रहे ज्यों-को-त्यों प्रतिष्ठा बनी हुई है।
आज भी जनता उनका हृदय से आदर करती है और उनको प्रशंसा करने में अपनी वाणी को धन्य समझती है। आज भी वे महापुरुष समाज में श्रद्धा और आदर के पात्र बने हुये हैं।
जो मनुष्य शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करता है, जो मनुष्य दुष्ट के साथ भी सज्जन जैसा आचरण करता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है।
ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और वैमनस्य हो मनुष्य की आत्मा के पतन के मुख्य कारण हैं। जो मनुष्य बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करता है, उसको आत्मा दिव्यलोक में विचरण करती है।
वह कभी आत्म-ग्लानि और आत्म-पराजय की अग्नि में नहीं जलता। सबके साथ समानता का व्यवहार करना, शान्ति और सज्जनता का व्यवहार करना, संसार का सबसे बड़ा तप है, दान है और ज्ञान है।
वह सबसे बड़ा आत्म-ज्ञानी है, जो संसार की समस्त आत्माओं को अपनी ही आत्मा समझता है। गीता में कहा गया है कि-
“आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः ।“
सुख और शान्ती
जो मनुष्य समस्त संसार को अपनी ही आत्मा के समान समझता है, वही पण्डित है अर्थात् ज्ञानी है।
जब सभी अपनी आत्मा हैं, अपने ही हैं, फिर किसके साथ प्रतिहिंसा और कैसा प्रतिशोध जो लोग हिंसा और प्रतिहिंसा, अपना और पराया आदि की भावना में फँसे रहते हैं, वे संसार के क्षुद्र और निम्न कोटि के प्राणी होते हैं।
उनकी आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो पाता।
वे आत्मशुदि और आत्म-संस्कार के कार्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते।
“अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदार चरिताप्त, वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
आत्म-शुद्धी
मनुष्य की आत्मिक शुद्धि से उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उसके हृदय में दिव्य भावनायें उत्पन्न होती हैं और वह प्रेम पारावार में गोते लगाकर जीवन भर आनन्द का अनुभव करता है।
आनन्द को नष्ट करने वाला शोक उसके पास तक नहीं आता, क्योंकि शोक उत्पन्न करने वाले शत्रु और स्वार्थ उसके निकट नहीं आते।
वह किसी का बुरा नहीं चाहता, वह किसी से शत्रुता नहीं चाहता, वह किसी का अहित चिन्तन नहीं करता, वह किसी के मार्ग में बा उपस्थित नहीं करता।
वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है। ईर्ष्या की आग और द्वेष का धुँआ उससे कोसों दूर रहता है।
शत्रु की ईट के द्वारा फूटे हुए मस्तक से बहने वाली रक्त की धारा को वह अपने गले का हार समझता है, क्यों न इस व्यक्ति को जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी।
रहीम की पंक्तियों में उसका अडिग विश्वास प्रकट होता है
“प्रीति रीति सब सो भली, बैर न हित मित गोत |
रहिमन याही जनम में बहरि न संगति होत ॥”
सहनशीलता के कुछ आदर्श उदाहरण
महात्मा गांधी के निधन पर जितना हिन्दू रोये उतने ही मुसलमान, जितने सिक्ख रोये उतने ही पारसी, जितना इंग्लैण्ड को दुःख हुआ उतना ही अमेरिका को ।
जब हम सोचते हैं कि गाँधी बी तो हिन्दू थे, हिन्दुओं को ही दुःख होना चाहिये था, तब हमारे सामने केवल यही उत्तर आता है कि उन्होंने जो कुछ किया वह सबके लिए किया।
जिन्होंने विदेशों में उन्हें मारा-पीटा और तरह-तरह की यातनायें दी, उनकी भी उन्होंने कल्याण-कामना की उनकी भलाई के लिए भी उन्होंने सोचा और प्रयत्न किया। इसीलिए आज उन्हें विश्वबन्धु कहा जाता है। गाँधी जी ने “जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल” वाली उक्ति को जीवन में ग्रहण किया था।
वे कहा करते थे कि जो व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, तुम उसके आगे दूसरा गाल भी मारने के लिये कर दो, वह एक बार में नहीं तो दूसरी बार में अवश्य लज्जित होगा और अपने किए हुए कुकर्म पर अवश्य पश्चात्ताप करेगा।
महात्मा बुद्ध के जीवनकाल में बौद्ध धर्म के विरोधी शासकों ने उनका घोर विरोध किया। भिक्षा माँगते समय भिक्षुओं पर ईंट-पत्थर फेंके जाते, भिक्षु बेचारे खून से लथपथ हो जाते, परन्तु मुँह से एक शब्द भी न कहते।
भगवान बुद्ध को मारने के लिये अनेक भयानक डाकुओं को भेजा जाता। बुद्ध को जब यह पता लगता तो वह स्वयं उनके पास पहुंच जाते और कहते कि लो मारो, मैं आ गया हूँ।
भगवान बुद्ध यदि चाहते तो अपने अनुयायी शासकों से उनको समाप्त भी करा सकते थे परन्तु नहीं, यदि वे ऐसा करते तो सम्भवतः आज बुद्ध को भगवान् कोई न कहता। शान्ति, प्रेम और अहिंसा से उन्होंने अपने कट्टर विरोधियों पर विजय प्राप्त की।
प्रभु ईसामसीह के जीवन काल में भी उनके विरोधियों ने उन पर कितने भयानक अत्याचार किये, परन्तु उन्होंने सदैव भगवान से उनकी मंगलकामना ही की। परिणाम यह हुआ कि आज संसार में ईसाई धर्मावलम्बियों की संख्या सबसे अधिक है।
इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध बिशेप की कैंडलस्टिक चुराने के लिये जेल मे भागा हुआ खूंखार डाकू खुली हुई खिड़की के रास्ते से जब भीतर आ गया, तब बिशप ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कई दिनों से भूखे होंगे, बैठिये में आपके लिये भोजन बनवाता हूँ आप स्नान तो नहीं करेंगे ?
इस व्यवहार को देखकर डाकू भी दंग रह गया।
चोरी करके भागते हुये. उसी डाकू को पुलिस ने पकड़ लिया और जब वह विशप के पास लाया गया तो बिशप ने यही कहा कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये चीजें चुराई नहीं बल्कि उपहारस्वरूप मैंने ही भेंट की। थी।
धन्य है रे बिशप तेरी महान् साधुता आचार्य विनोबा भावे ने भी डाकुओं के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखकर उन्हें सभ्य नागरिक बनाने का प्रयत्न किया था।
अभिमानी का पतन / सहनशीलता ना होने का परिणाम
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि इस प्रकार की विचारधारा से मनुष्य में कायरता और भीरता आ जाती है, वह अपने स्वाभिमान को खो बैठता है।
विपत्तियाँ उसे चारों ओर से घेरती हैं।
वह उनका कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकता, इस प्रकार वह एक नपुंसक बन जाता है।
“शठें शाठ्य समाचरेत्” या “मायाचारी मायया वर्तितव्यः ।”
ये उक्तियों, अर्थात् दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिये या मायावी के साथ मायावी बनना चाहिये, उचित नहीं क्योंकि-
“Two wrongs cannot make one right.”
उपसंहार
कटुता से कटुता बढ़ती है, क्रोध से क्रोध कभी शान्त नहीं होता। बैर को प्रेम से ही जीता। जा सकता है न कि बेर से वैर से तो बैर और बढ़ेगा।
अतः मानव जीवन में शान्ति, संतोष, दया, क्षमा, सहानुभूति आदि आदर्श एवं उदान गुणों की नितान्त आवश्यकता है बदला लेना तो parshvik प्रवृत्ति है।
प्रतिशोध की भावना मनुष्य को चैन से नहीं रहने देती –
“He who preacheth revenge keeps his own wound green.”
आपको हमारी यह post – सहनशीलता अथवा “जो तोकू काँटा बुवै ताहि बोय तू फूल” एक निबंध / Tolerance ESSAY IN HINDI कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
- समय का सदुपयोग अथवा “जात नहिं लागहिं बारा”
- विद्यार्थी और अनुशासन
- देशाटन से लाभ
- रामचरितमानस की देन अथवा मेरा प्रिय ग्रन्थ और उसकी विशेषतायें
ये भी जाने
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
सहनशीलता के क्या लाभ हैं ?
णित समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जायेंगे, जो व्यर्थ में ही शत्रुता मान लेंगे, छिपकर आपके ऊपर तीर पर तीर चलाये जायेंगे, कभी तो आपको वह तीर लगेगा ही और आप तिलमिला उठेंगे।
यश किसे कहतें हैं ?
जिस मनुष्य को संसार में कोर्ति होती है, वह सदैव जीवित रहता है , भले ही वह पार्थिव शरीर से इस संसार में न रहा हो। कोर्ति का भागी वही मनुष्य होता है, जिसमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, जो अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज की तन, मन, धन से सेवा करता है।
“जो तुम्हारे लिये काँटे बोता है, तुम उसके लिए फूल बोओ” उक्ति का क्या अर्थ है ?
उक्ति का अर्थ है, जो तुम्हारा अहित करता है तुम उसका हित करो, जो तुम्हें दुःख देता है तुम उसे सुख दो, जो तुमसे द्वेष रखता है तुम उससे प्रेम करो, जो तुम्हें हानि पहुँचा रहा है।
तुम उसे लाभ पहुंचाओ, जो तुम्हें गिरा रहा है तुम उसे उठाओ।
“बिल्ली खायेगी नहीं तो गिरा अवश्य देगी” कहावत का क्या अर्थ है ?
इस कहावत का अर्थ है की , ऐसे लोग अपने इन नीचतापूर्ण कृत्यों में मानसिक शान्ति प्राप्त करते हैं और अपनी विजय पर फूले नहीं समाते। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भर्तृहरि जी ने लिखा है कि ऐसे लोग जो निरर्थक ही दूसरों का अहित करते हैं, मैं नहीं जानता किस कोटि के हैं।
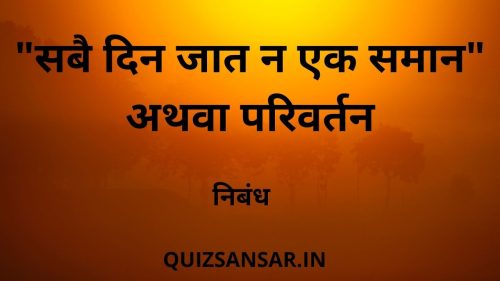
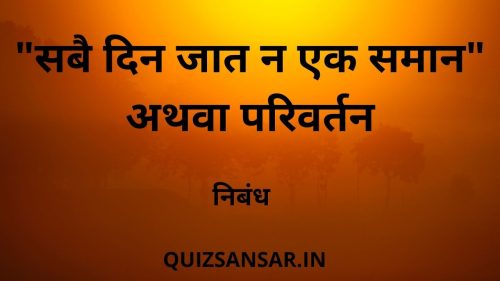
परिवर्तन अथवा “सबै दिन जात न एक समान”
नमस्कार दोस्तों हमारी आज की post का विषय है परिवर्तन अथवा “सबै दिन जात न एक समान” उम्मीद है की आपको यह पसन्द आयेगी | इसे अवश्य पढ़ें |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- संसार की परिवार्तनशीलता
- मानव जीवन में सुख-दुःख का मिश्रण
- सोदाहरण विवेचना
- उपसंहार
प्रस्तावना
खोलता इधर जन्म लोचन मूदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण अभी उत्सव औ, हास- हुलास अभी अवसाद, अश्रु उच्छ्वास!
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। इसके कण-कण में प्रत्येक क्षण परिवर्तन का चक्र चला करता है।
कुछ परिवर्तन स्थूल होते हैं, जिन्हें हम नित्य देख सकते हैं और कुछ सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते।
मेज पर रखे हुए फूलदान के फूल आज ताजे थे और जब वे सूख जायेंगे का तब हमें स्पष्ट परिवर्तन दीख जायेगा, परन्तु फूलदान वाली मेज में भी नित्य परिवर्तन हो रहा है, इसे हम नित्य अनुभव नहीं करते।
कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणभंगुर संसार को प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, परिवर्तनशील है।
कल तक जहाँ भयानक वन थे आज उन्हीं स्थानों पर सुन्दर सुन्दर भवन, विद्युत प्रकाश से जगमगाती गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं और जहाँ जन रब से परिपूर्ण सुन्दर नगर थे, वहाँ कोसों तक दीपक का प्रकाश भी दिखाई नहीं पड़ता।
कल तक जिन वृक्षों पर हरे-भरे फल और फूल आते थे आज वे काष्ठ बने हुए अरण्यरोदन कर रहे हैं।
कल तक जो बच्चे थे, जिन्हें पाठ याद न होने पर कक्षा में खड़ा कर दिया जाता था, इतना ही नहीं कभी-कभी पीट भी दिया जाता था आज हम उनको सफेद बालों से घिरे हुए चेहरे और चार-चार छह-छह बच्चों के पिता के रूप में देखते हैं, तो संसार के तीव्र परिवर्तन चक्र पर आश्चर्य होता है।
आज उनकी आकृति पर न वह तेज है और न शरीर में वह स्फूर्ति, न वह बालसुलभ – उच्छृंखलता है और न उद्दण्डता।
आज बचपन का कोमल गात जरा सा पीला पात | चार दिन सुखद चाँदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात ।।
ध्वंसावशेष मन्दिरों, मस्जिदों को जिनमें इस समय वन्य पक्षियों ने अपने आवास बना रखे हैं जब कभी देखता हूँ तो तुरन्त उनका निर्माण काल और निर्माता की भक्ति और श्रद्धा नेत्रों के आगे नृत्य करने लगती है कि इनमें भी कभी शंख ध्वनि घण्टा वादन और दीपदान होता होगा और नमाज पढ़ी जाती होगी, परन्तु आज इन्हें कोई झाँककर देखने वाला तक नहीं।
कल की सधवा को आज विधवा बनते देर नहीं लगती। कल का राजा आज देखते-देखते भिखारी बन जाता है।
संसार की परिवर्तनशीलता
इस परिवर्तन का ही नाम संसार है। यदि संसार में एक ही रास्ता हो तो मानव ऊब उठे ।
मनुष्य के सामने कभी सुख आते हैं, तो कभी दुःख, कभी निराशा का साम्राज्य होता है, तो कभी आशा की सुन्दर झलक।
सुख-दुःख की धूप एवं छाया में संसार उठता बैठता है। सुख-दुःख दोनों अन्योन्याश्रित हैं।
एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार नमकीन खाने के बाद मिठाई अच्छी लगती है और रात के बाद ऊया की लालिमा नवस्फूर्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार दुःख के बाद सुख अच्छा लगता है।
किसी के दिन एक से नहीं रहते अन्यथा मानव अपने को किसी दिन समाप्त कर ले। उसे यही आशा रहती है कि-
“जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगिह देर।”
मानव जीवन में सुख-दुःख का मिश्रण
रथ के चक्र के समान सुख-दुःख दोनों ऊपर-नीचे आते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुःख। इसलिए कहा गया है-
“चक्रवत् परिवर्तन्ते, दुःखानि च सुखानि ।”
यही आशा की किरण मानव को जीवन से निराश नहीं होने देती, वह जानता है कि कटा हुआ वृक्ष भी एक बार फिर हरा-भरा होकर भूले-भटके पथिकों को अपनी सघन छाया प्रदान करेगा।
क्षीण हुआ चन्द्रमा भी धीरे-धीरे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है-
“छिन्नोऽपि रोहतितरू क्षीणोऽच्युपचीयते पुनश्चंद्र इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विषया।”
अगर सभी दिन एक से ही बीतें तो मानव का जीवन आकर्षणहीन बन जाए। प्रकृति के सुकुमार कवि पन्त की ये पंक्तियाँ कितनी सुन्दर हैं-
“मैं नहीं चाहता चिर सुख में नहीं चाहता चिर दुःख। सुख दुःख की आँख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख ॥”
और फिर वे इस परिवर्तन चक्र की तीव्रता को देखकर सहसा कह उठते हैं-
“आह रे, निष्ठुर परिवर्तन एक सौ वर्ष, नगर उपवन एक सौ वर्ष विजन-वन यही तो है संसार असार, सृजन, सिंचन, संहार!”
संसार की परिवर्तनशीलता पर अस्थिरता और प्रसाद जी का एक व्यंग्य चित्र देखिये-
“सुख दुःख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा। मुड़ कर न कभी देखेगा, किसका हित अनहित होगा।”
इस परिवर्तन की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाये। एक दिन भारत विश्व गुरु था, इसे‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता था।
ह्वेनसांग और मेगस्थनीज आदि विदेशी यात्रियों ने अतीत भारत की सुसम्पन्नता का बहुत सुन्दर चित्र उपस्थित किया था।
देश में पूर्ण राम राज्य था। गोस्वामी जी के शब्दों में-
“नहि दरिद्र कोउ दुःखी न होना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन होना।”
परन्तु आज वह भारत न सोने की चिड़िया और न विश्व-गुरु । कितना भयंकर परिवर्तन है है देश की स्थिति में समय की क्रूरता बड़े-बड़े पुरुषों को नत कर देती है।
इसी का नाम तो परिवर्तन है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र का ड्रोम के घर दास बनना, भगवान राम को चौदह वर्ष का अरण्यवास नल र दमयन्ती का जंगलों में मारे-मारे फिरना, सीता का गर्भावस्था में गृह परित्याग आदि सभी घटनायें परिवर्तन की निष्ठुरता की याद दिलाती हैं।
यह परिवर्तन प्रकृति में सदा गतिशील रहता है। आज बसन्त की हरीतिमा है, पुष्पों में विकास है, भ्रमरों का मथुर गुंजन है तो पतझड़ का रौद्र रूप प्रकृति के समस्त यौवनपूर्ण वैभव को विनष्ट करता हुआ वीरान बना देता है।
परन्तु वहाँ भी भ्रमर के हृदय में आशा की धुंधली किरण अपना प्रकाश किए रहती है।
पतझड़ को रौद्रता भ्रमर को निराश नहीं बना पाती, वह जानता है कि मुझे दुःख के बाद सुख अवश्य मिलेगा, इसीलिए-
“इहि आस अटक्यो रहो, अलि गुलाब के मूल। अइहै बहुरि बसन्त ऋतु इन डारनि ये फूल | “ – बिहारी लाल
सोदाहरण विवेचना
नित्य के जीवन में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य यदि कल धनवान था, तो आज वह निर्धन है, यदि कल वह उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा था, तो आज अवनति के गर्त में पड़ा हुआ है।
कल यदि किसी का उत्कर्ष काल था जो आज उसका अपकर्ष काल है। महान् से महान् वैभवशाली राष्ट्र जो उन्नति के शिखर पर थे, वहीं समय के परिवर्तन के साथ धराशायी हो गये।
विश्व की कितनी सभ्यताओं ने अपने वैभव पर गर्व किया, परन्तु समय के प्रवाह में आज उनका नाम भी सुनाई नहीं पड़ता।
किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुःख कल ही ब्याज काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल इन्द्र धनुष की सी छटा विशाल विभव की विद्युत् ज्वाल चमक, छिप जाती है तत्काल |
यही उत्थान और पतन का क्रम सृष्टि में अनवरत रूप से चलता रहता है।
इसीलिये कहा गया है कि “सबै दिन जात न एक समान।” परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या इस परिवर्तन से मनुष्य को अपना साहस, धैर्य और शान्ति खो देनी चाहिये? कभी नहीं यह तो पशुओं का लक्षण हैं।
“खुशीगर हुई हंस लिये दो घड़ी अगर गम हुआ रोके चुप हो रहे।”
उसे दृढ़ता के साथ विपत्तियों से संघर्ष करना चाहिये। धैर्यशाली व्यक्ति दुःख को भी सुख मान सकता है।
मनुष्य को सम्पत्ति और विपत्ति में समान रहना चाहिये जैसे सूर्य जब उदय होते हैं, तब उनकी आभा लाल होती है, और जब अस्त होते हैं, तब भी उनकी लालिमा में कोई अन्तर नहीं आता। कहा भी है-
“उदेति सविता ताम्रस्तान एवास्तमेति च | सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता।”
उपसंहार
गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है—
“सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो। भरुयर्पितमनोबुद्धिर्भत्ति मान्यः स मे प्रियः “
अर्थात् सुख-दुःख में लाभ-हानि में, जय-पराजय में समान भाव रहते हुए अपना मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर देने वाला भक्त मुझे प्रिय है।
कहने का तात्पर्य यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति में भी मनुष्य को हतोत्साहित और बड़े से बड़े सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिये।
यह तो समय है आता है और चला जाता है। अंग्रेजी में कहावत है-
“It comes to go.”
समय की शिला पर मधुर लेख कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए।
परन्तु अन्त में पन्त जी के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है
आहे निष्ठुर परिवर्तन! तुम्हारा ही ताण्डव नर्तन विश्व का तरुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन ।।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
ये भी जाने
- environment polution essay
- देशाटन से लाभ
- रामचरितमानस की देन अथवा मेरा प्रिय ग्रन्थ और उसकी विशेषतायें
परिवर्तन पर श्लोक व दोहे |
परिवर्तन क्या है ?
संसार की परिवर्तनशीलता क्या है ?
मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्या प्रभाव पड़ता है ?
रथ के चक्र के समान सुख-दुःख दोनों ऊपर-नीचे आते रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुःख। आशा की किरण मानव को जीवन से निराश नहीं होने देती, वह जानता है कि कटा हुआ वृक्ष भी एक बार फिर हरा-भरा होकर भूले-भटके पथिकों को अपनी सघन छाया प्रदान करेगा।

विद्यार्थी और अनुशासन


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता
- अनुशासनहीनता के कारण
- अनुशासन स्थापना के उपाय
- उपसंहार
प्रस्तावना
प्रासाद की चिरस्थिरता और उसकी दृढ़ता जिस प्रकार आधारशिला की दृढ़ता पर आधारित है, लघु पादपों का विशाल वृक्षत्व जिस प्रकार बाल्यावस्था के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होता है, उसी प्रकार युवक की सुख-शान्तिमय समृद्धि का संसार छात्रावस्था पर आधारित होता है।
यह अवस्था नवीन वृक्ष की वह मृदु और कोमल शाखा है, जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही रहेगी।
अवस्था प्राप्त विशाल वृक्षों की शाखायें चाहे टूट भले ही जाएँ पर मुड़ती नहीं, क्योंकि समय, अनुभव और जीवन के सुख-दुःख उन्हें कठोर बना देते हैं।
अतः मानव जीवन की इस प्रारम्भिक अवस्था को सच्चरित्रता और सदाचारिता आदि उपायों से सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है।
छात्रावस्था अबोधावस्था होती है, इसमें न बुद्धि परिष्कृत होती है और न विचार माता-पिता तथा गुरुजनों के दबाव से पहले वह कर्त्तव्य पालन करना सीखता है।
माता-पिता तथा गुरुजनों की आज्ञाएँ ज्यों की त्यों स्वीकार करना ही अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ शासन के पीछे चलना है, अर्थात् गुरुजनों और अपने पथ-प्रदर्शकों के नियन्त्रण में रहकर नियमबद्ध जीवनयापन करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही अनुशासन कहा जा सकता है।
अनुशासन विद्यार्थी जीवन का प्राण है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न तो देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और न अपने व्यक्तिगत जीवन में ही सफल हो सकता है।
वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन परमावश्यक है, परन्तु विद्यार्थी जीवन के लिये यह सफलता की एकमात्र कुंजी है।
विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता
आज विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है क्या घर क्या स्कूल, क्या बाजार, क्या मेले और क्या उत्सव, क्या गालियाँ और क्या सड़कें, आज का विद्यार्थी घर में माता-पिता की आज्ञा नहीं मानता, उनके सदु का आदर करता, उनके बताये हुये मार्ग पर नहीं चलता।
उदाहरणस्वरूप पिता जी ने कहा बेटा। शाम को घूम कर जल्दी लौट आना, पर कुँवर साहब दस बजे का शो देखकर ही लौटेंगे।
माता-पिता के मना करने पर भी आज का बालक उसी के साथ उठता-बैठता है, जिसके साथ उसकी तबियत आती है।
परिणाम यह होता है कि उसमें कुसंगतिजन्य दूषित संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। कॉलेज की चारदीवारी में विद्यार्थियों के लिये अनुशासन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं।
कक्षा में पढ़ाई हो रही है, आप बाहर गेट पर, पनवाड़ी की दुकान पर खड़े खड़े सिगरेट में दम लगा रहे हैं।
जब मन में आया कक्षा में आ बैठे और जब मन में आया उठकर चले आये, अगर तबियत इतने पर भी मचली तो साईकिल उठाई और सिनेमा तक हो आये तस्वीरों को देखकर मन तो बहल हो जाता है।
अगर अध्यापक ने कुछ कहा, तो उस पर बिना उचित-अनुचित का विचार किये जो मन में आया कह दिया, अगर ज्यादा बात बढ़ी तो फिर आगे के कुकृत्यों की कुमन्त्रणायें होने लगा।
अनुशासनहीनता का नग्न नृत्य उस समय देखिये, जब कोई सभा हो, मीटिंग हो, कवि सम्मेलन या कोई एकांकी नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो।
विद्यार्थियों की उद्दण्डता और उच्छ श्रृंखलता के कारण कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते।
परीक्षा आजकल अध्यापक की जान लेने वाली बन गई है, या तो विद्यार्थी को मनचाही नकल कर लेने दीजिये या फिर हाथापाई को तैयार हो जाइये।
सामूहिक मेलों और उत्सवों में विद्यार्थियों की चरित्रहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। किसी भी महिला के साथ अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार करना साधारण-सी बात है।
पुलिस की मार से चोरियों में जब नाम खुलते हैं तो उनमें दो-चार विद्यार्थियों के नाम भी होते हैं। यही हाल डकैतियों का है।
रेलों में बिना टिकट सफर करने में छात्र अपना गौरव समझते हैं। शहर के किसी कोने में जहाँ आप चाहें दंगा करवा लीजिये।
लूटमार करवा लीजिए। किसी को बीच चौराहे पर खड़ा होकर पिटवा लीजिये। कहाँ गया गुरु और शिष्य का वह पवित्र स्नेह और कहाँ गई वह सच्चरित्रता ?
देश के भावों नागरिक अगर ऐसे हो रहे, तो निश्चित ही भारतवर्ष आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों गड्ढे में जा गिरेगा और ऐसा गिरेगा कि युगों तक फिर न निकल सकेगा।
अनुशासनहीनता के कारण
अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता-पिता को ढिलाई है। माता-पिता के संस्कार ही बच्चे पर पड़ते हैं। बच्चे की प्राथमिक पाठशाला घर होती है।
वह पहले घर में ही शिक्षा लेता है, उसके बाद वह स्कूल और कॉलेज में जाता है, उसके संस्कार घर में खराब हो जाते हैं।
पहले तो प्यार के कारण माता-पिता कुछ कहते नहीं वह जहाँ चाहे बैठे और जहाँ चाहे खेले, जो मन में आये वह करे पर जब हाथी के दाँत बाहर निकल आते हैं, तब उन्हें चिन्ता होती है, फिर वे अध्यापक और कॉलेजों की आलोचना करना आरम्भ करते हैं।
दूसरा कारण आज की अपनी शिक्षा प्रणाली है। इसमें नैतिक या चारित्रिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। पहिले विद्यार्थियों को दण्ड का भय बना रहता था, क्योंकि-
“भय बिन होय न प्रीति”।
पर अब आप विद्यार्थियों को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि शारीरिक दण्ड अवैध है। केवल जबानी जमा खर्च कर सकते हैं।
इसमें विद्यार्थी बहुत तेज होता है, आप एक कहेंगे वह आपको चार सुनायेगा। शिक्षा संस्थाओं का कुप्रबन्ध भी छात्रों को अनुशासनहीन बनाता है।
परिणामस्वरूप कभी वे विद्यालय के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और कभी अध्यापकों की अवज्ञा।
अधिकांश कक्षा भवन छोटे होते हैं और छात्रों की संख्या सीमा से अधिक होती है। कॉलेजों में तो एक-एक कक्षा में सौ-सौ विद्यार्थी होते हैं।
ऐसी दशा में न तो अध्ययन होता है और न अध्यापन। कभी-कभी राजनीतिक तत्व विद्यार्थियों को भड़काकर नगर और कॉलेजों में उपद्रव खड़ा करवा देते हैं।
“खाली दिमाग शैतान की घर” वाली कहावत् बिल्कुल ठीक है। कॉलेजों में छात्रों के दैनिक कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
यदि उनके रोजाना के पढ़ने-लिखने की देखभाल हो और उसी पर उनको वार्षिक उन्नति आधारित हो तो विद्यार्थी के पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि वह व्यर्थ की बातों में अपना समय खर्च करे।
दूसरी बात यह है कि कक्षाओं में छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उनकी कार्यपद्धति पर कोई नियन्त्रण होता है।
अनुशासन स्थापना के उपाय
विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की पुनः स्थापना करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हो और विद्यार्थी की नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना जाए, जिससे छात्र को अपने कर्त्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो सके।
नैतिक शिक्षा का समावेश हाई स्कूली पाठ्यक्रम में सब राज्यों में किया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
हमारी शिक्षा प्रणाली में कक्षा 1 से लेकर एम० ए० तक के विद्यार्थियों के नैतिक उत्थान की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिवाय इसके कि वे कबीर और रहीम के नीति दोहे पढ़ लें, वह भी परीक्षा में अर्थ लिखने की दृष्टि से दूसरी बात यह है कि शारीरिक दण्ड का अधिकार होना चाहिये, क्योंकि बालक तो माता-पिता की तरह गुरु के भय से ही अपने कर्तव्य का पालन करता है।
तीसरी बात यह है कि माता-पिता को बचपन से ही अपने बच्चों के कार्यों पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि गुण और दोष संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं।
“संसर्गजा दोष गुणा: भवन्ति।”
हमारी शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
आज का विद्यार्थी हाई स्कूल पास कर लेने पर कहीं का भी नहीं रह जाता। न वह अपना निर्वाह कर सकता है और न ही अपने परिवार के व्यक्तियों का।
जो विद्यार्थी कॉलेज की ऊँची शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते, उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार के अभाव में वह देश में अनुशासनहीनता फैलाता है।
उपसंहार
अतः शासन को देश के उद्योग-धन्धों को आगे बढ़ाना चाहिए तथा उद्योग-धन्धों के संचालन की भी उचित शिक्षा देनी चाहिए।
विद्यार्थियों को अध्ययन और इसके अतिरिक्त अन्य शिष्ट एवं कल्याणप्रद कार्यों में भी व्यस्त रखना चाहिए और मास में एक परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, वार्षिक परीक्षा बन्द कर देनी चाहिए और मासिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही छात्र को वार्षिक उन्नति मिलनी चाहिए।
इस प्रकार वह पूरे वर्ष पढ़ता रहेगा। अब तो वह परीक्षा से तीन-चार दिन पहले गैस पेपर खरीदता है और परीक्षा में बैठकर पास हो जाता है।
क्या आवश्यकता है आज अध्यापक की? उसके अध्यापक तो “गैस पेपर और सरल अध्ययन” हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित किये बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता।
आज का विद्यार्थी कल का सभ्य नागरिक नहीं हो सकता, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे।
देश के नागरिकों का निर्माण अध्यापकों के हाथों में है। उन्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।
आपको हमारी यह post कसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |