

देशाटन से लाभ


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- यात्रा से पूर्व उचित तैयारियां
- देशाटन के लाभ
- उपसंहार
प्रस्तावना
“देशाटन का अर्थ असल में देश भ्रमण करना है।
देशाटन के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त करना है।
सारनाथ, रामेश्वर देखें, देखें मथुरा काशी।
पंजाबी, मद्रासी देखें, देखें बंग निवासी ॥
घूम-घूमकर भारत माँ के हम सब अंग विलोकें।
कर्म भूमि गांधी, नेहरू की आओ हम अवलोकें ॥”
गति जीवन का लक्षण है। गतिशीलता जीवन है और गतिहीनता मृत्यु गतिशील जीवन ही भविष्य में पल्लवित और पुष्पित होता हुआ संसार को सौरभमय बना देता है।
मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन परम आवश्यक है और ज्ञानार्जन के लिए आवश्यक है मानव हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की उत्कण्ठा, जिज्ञासा और पिपासा।
यह निर्विवाद सत्य है कि गुरु वाणी अथवा पुस्तक पठन से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयं नेत्रों से अवलोकन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चिरस्थायी तो होता ही है उसको प्राप्त करना सरल और सुगम भी है।
अतः आवश्यक है व्यक्ति के लिए भ्रमण की स्वतन्त्रता और अवसर की उपलब्धता के साथ मानव हृदय में कौतूहल और जिज्ञासा की मनोवृत्ति जो राष्ट्र और देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। देशाटन इसी मनोवृत्ति की देन है।
नवीन नगरों व स्थानों, नये देशों और उनकी वेशभूषा तथा बोलियों को देखने तथा सुनने की लालसा मानव के हृदय में जन्म से ही उदित हो जाती है।
नवीन स्थानों में तथा विदेशों में भ्रमण करना ही देशाटन कहा जाता है। देशाटन से मनुष्य को भिन्न-भिन्न स्थानों को देखने का सुअवसर प्राप्त होता है, अनेक नवीन विचारों की उत्पत्ति होती है।
उसके हृदय में उदारता की भावना का जन्म हो जाता है। मस्तिष्क को चिन्तनशील एवं क्रियाशील बनाने के लिए देशाटन परमावश्यक है।
इससे कुछ समय के लिए वातावरण और वायुमण्डल बदल जाने से मनुष्य के मन और मस्तिष्क में नवीनता आ जाती है।
यात्रा से पूर्व उचित तैयारियां
प्रस्थान से पूर्व हमें एक ऐसा सहयात्री भी निश्चित कर लेना चाहिए, जो उस स्थान को, जहाँ हम जा रहे हैं, भाषा से परिचित हो, वहाँ की रीति-नीति को भली-भाँति जानता हो।
हमें उस स्थान के दर्शनीय, ऐतिहासिक स्मारकों का भी ज्ञान यथावत् होना चाहिए। इसके लिए उस स्थान का मानचित्र तथा एक ऐसी पुस्तक, जिसमें उस स्थान की समस्त विशेषताओं का वर्णन हो, अपने पास रखनी चाहिए।
वह पुस्तक एक प्रकार की गाइड का काम करती रहेगी और आपको उस स्थान के भ्रमण में कोई कठिनाई न होगी।
स्थान विशेष पर अधिक नहीं रुकना चाहिए। आप वहाँ उतना ही ठहरिए जितना आवश्यक हो।
जिस स्थान की यात्रा आप कर रहे हैं, वहाँ को जलवायु का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार वस्त्र इत्यादि का प्रबन्ध भी पहले से कर लेना चाहिए. जिससे वहाँ पहुँचकर आपको कोई असुविधा न हो।
देशाटन से लाभ
देशाटन से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं।
मनोरंजन संबंधी
एक स्थान पर रहते-रहते जब मन ऊब जाता है तब मानव हृदय में नई-नई वस्तुओं को देखने की, नये स्थानों पर जाने की इच्छा होती है क्योंकि नित्य प्रति दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में इतना आकर्षण नहीं होता जितना नवीन में वह अपना मन बहलाने के लिए निकल पड़ता है।
पर्वतीय प्रदेश के शान्तिपूर्ण वातावरण में रहने वाला मैदान के नगरों में और मैदान के नगरों का निवासी पर्वतीय उपत्यका और अधित्यकाओं के मनोरम दर्शनों के लिए निकल पड़ता है।
सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ।
जिदंगानी भी सही तो नौजवानी फिर कहाँ ।।
शिक्षा संबंधी
देशाटन से मनुष्य शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करता है। हम जिन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को केवल पाठ्य-पुस्तक में ही पढ़ पाते हैं, उन स्थानों को जब हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं तब हमारा ज्ञान और भी अधिक विस्तृत हो जाता है।
प्लासी और पानीपत का मैदान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सारनाथ के भग्नावशेष, अजन्ता और ऐलोरा की गुफायें, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, बौद्धगया का मन्दिर, आदि का साक्षात् ज्ञान हम देशाटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
सूर और रसखान के पदों को पढ़कर ब्रजभूमि का वह प्राकृतिक सौन्दर्य हमारे हृदय में द्विगुणित हो उठता है, जब हम कृष्ण की लीला भूमि मथुरा और वृन्दावन को अपने नेत्रों से देख लेते हैं।
बोकारो, भिलाई और राउरकेला का इस्पात उद्योग, ट्रॉम्बे और नरौरा आदि के परमाणु संयंत्र, विशाखापत्तनम का पोत निर्माण, टिहरी तथा कावेरी बाँध आदि के अवलोकन से देश के विकास का ज्ञान होने के अतिरिक्त भौतिक ज्ञान की वृद्धि होती है।
रामेश्वरम् जाकर सूर्योदय और सूर्यास्त का आलौकिक दृश्य सहसा नैसर्गिक सुख की अनुभूति करा देता है।
देशाटन से हम अन्य देशों की शासन प्रणाली और सभ्यता से भी परिचय प्राप्त करते हैं। वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
अतः राजनीतिक ज्ञान और समाज-सुधार के लिए भी देशाटन आवश्यक है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वही होती है, जो हमें हमारे अनुभव से प्राप्त होती है।
अतः अनुभवों के लिए देश-देशान्तर का भ्रमण अत्यन्त आवश्यक है।
स्वास्थ्य संबंधी
हृदय की प्रसन्नता का हमारे स्वास्थ्य से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। देशाटन के समय अनेक सुन्दर दृश्यों एवं मनोरम वस्तुओं को देखने से हमारा हृदय कमल विकसित हो जाता है।
चित्त की प्रफुल्लता से हमारा स्वास्थ्य भी सुन्दर रहता है। कई स्थान ऐसे होते हैं, जिनकी जलवायु स्वास्थ्य ‘ को लाभ पहुंचाती है।
देशाटन के समय हम पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त होते हैं, इससे भी स्वास्थ्य पर सुन्दर प्रभाव पड़ता है।
प्रायः देखा जाता है कि देशाटन से लौटकर जब मनुष्य घर आते हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत सुन्दर हो जाता है। परन्तु घर पर रहकर फिर ज्यों-का-त्यों हो जाता है।
अतः देशाटन से मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है।
चरित्र संबंधी
देशाटन मनुष्य की चारित्रिक उन्नति में पर्याप्त सहायक होता है। मनुष्य को कष्ट सहने का अभ्यास हो जाता है।
देशाटन से मनुष्य में सहिष्णुता आती है। वह धैर्यवान और शक्ति सम्पन्न हो जाता है। उसके हृदय की संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाती है।
स्नेह और भ्रातृत्व की भावना के साथ-साथ उसमें उदारता की भावना का भी उदय होता है। उसका चरित्र उज्ज्वल और उन्नत हो जाता है। उसके विचारों में दृढ़ता आ जाती है।
आत्म-निर्भरता
आत्मनिर्भर बनने के लिए देशाटन बहुत आवश्यक है। मनुष्य घर से बाहर निकलकर स्वावलम्बी हो जाता है।
उसमें व्यवहार कुशलता आ जाती है। व्यवहार कुशलता के साथ-साथ मनुष्य के व्यक्तित्व को मौलिकता तथा विचारों को दृढ़ता प्राप्त होती है।
विद्यार्थियों को अपने लम्बे अवकाश के दिनों में देशाटन अवश्य करना चाहिए। इससे उनमें बौद्धिक जागृति उत्पन्न होगी, मृदु भाषण का गुण आयेगा, विश्व बन्धुत्व की भावना में वृद्धि होगी।
उपसंहार
इस क्षणभंगुर संसार में आकर मनुष्य ने यदि संसार के भिन्न-भिन्न भागों को न देखा, तो उसका अमूल्य मानव जीवन वास्तव में व्यर्थ है।
परमेश्वर सौन्दर्यमयी सृष्टि के दर्शन हमें देशाटन से ही प्राप्त हो सकते हैं। हम विभिन्न भाषा-भाषियों तथा विभिन्न जातियों के मनुष्यों के सम्पर्क में आते हैं, उन्हें हमें निकट से देखने का अवसर प्राप्त होता है।
देशाटन से हमारे बहुत से अन्ध-विश्वास समाप्त होते हैं। बहुत से व्यक्तियों के विषय में हमारी भ्रमात्मक धारणायें समाप्त हो जाती है।
इस प्रकार देशाटन हमारे हृदय में विश्वबन्धुत्व की भावना जाग्रत करते हुए हमें सुशिक्षा प्रदान करता है।
अतः यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार देशाटन से ज्ञानार्जन करके जीवन को सफल बनायें।
हमारे देश में निर्धनता के कारण जनता में देशाटन की मनोवृत्ति कुछ कम है। आशा है कि निकट भविष्य में जब देश धन-धान्य से पूर्ण हो जायेगा तब जनता की मनोवृत्ति इस दिशा में भी असर होगी।
“देश भ्रमण है ज्ञान-वृद्धि का उत्तम साधन ।
अतः चाहिये हमें कभी करना देशाटन || “
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi


रामचरितमानस की देन अथवा मेरा प्रिय ग्रन्थ और उसकी विशेषतायें


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- तत्कालीन स्थिती और रचना की उद्देश्य
- रामचरितमानस से शिक्षा
- पूर्ववर्ती और परवर्ती जनता का कल्याण
- उपसंहार
प्रस्तावाना
रामचरितमानस क्या है ? इसका संक्षिप्ततम उत्तर है-
“चार वेद, पुराण अष्टदस छयशास्त्र सब ग्रंथन को रस”
अर्थात् चारों वेद, अठारह पुराण, छः शास्त्र तथा शेष जितने भी प्रन्थ हैं क्या गीता या बाईबिल, गुरु ग्रन्थ साहब अथवा कुरान शरीफ, जितने भी संभव ग्रन्थ हो सकते हैं उन सभी का रस अर्थात् निचोड़ रामचरितमानस है।
वर्तमान में सभी सिद्धान्तों का सर्वमान्य सिद्धान्तों का उपदेश है। तुलसीदास जी ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और उपलब्ध सभी ग्रन्थों का आश्रय लेकर – रामचरितमानस की रचना की।
हिन्दी साहित्य में ही नहीं विश्व भर के साहित्य में इसका स्थान निराला है। का इसके अनुरूप काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के लिए समान उपयोगी सभी तत्वों के अत्यन्त सरल, सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य कला की से तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, पारिवारिक जीवन, पतिव्रत धर्म मानव धर्म, मातृधर्म के साथ, भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके रोचक तथा ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला दूसरा जनता का में आज तक नहीं लिखा गया।
यही कारण है कि इतने प्रन्थ हिन्दी भाषा में ही नहीं संसार की किसी भी भाषा चाव से धनी अथवा निर्धन शिक्षित अथवा अशिक्षित, गृहस्थ अथवा संन्यासी, स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध सभी इस ग्रन्थ को पढ़ते हैं तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार इस ग्रन्थ से हुआ है उतना कदाचित ही किसी और ग्रन्थ से हुआ हो।
“भारी भव सागर से उतारती कवन पार |
जो पै यह रामायण तुलसी न गावतौ ॥ “
तत्कालीन स्थिती और रचना की उद्देश्य
बेनी कवि को यह उक्ति अपने में कितनी सत्य है, इसका अनुमान आज के घोर अनैतिक समय में भी रामचरितमानस के प्रचार एवं प्रसार से लगाया जा सकता है।
कदाचित् ही कोई हिन्दू घर ऐसा हो, जिसमें रामचरितमानस की एक प्रति न हो, चाहे वह छोटी हो या मोटी, फटी हो या पुरानी।
बड़े से बड़े महलों से लेकर निर्धन की वैभवहीन झोपड़ी तक में इसके प्रति सम्मान, आदर और श्रद्धा है।
सभी लोग, चाहे वे थोड़े पढ़े-लिखे हों या बहुत, चाहे वे धार्मिक दृष्टि से पढ़ते हो या ज्ञान की दृष्टि से, चाहे वे ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ते हों या राजनीतिक दृष्टि से, इससे समान रूप से लाभान्वित होते हैं।
निःसन्देह रामचरितमानस का गम्भीरतापूर्वक मनन करने वाला व्यक्ति एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, एक श्रेष्ठ समाजसेवी बन सकता है, एक श्रेष्ठ गृहस्थ बन सकता है, एक श्रेष्ठ समाज सुधारक बन सकता है, एक श्रेष्ठ राजनैतिज्ञ बन सकता है और एक परम विनम्र भगवद-भक्त बन सकता है और एक ज्ञानी बन सकता है तथा एक कुशल कर्मकाण्डी बन सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस के अनुसार अपना जीवनयापन करने वाला क्या नहीं बन सकता ?
रामचरितमानस केवल लौकिक उन्नति का ही साधन नहीं है, पारलौकिक उन्नति और समृद्धि का भी साधन है।
संसार रूपी समुद्र के सन्तरण के लिए रामचरितमानस एक विशाल नौका है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य सरलता से ही भवसागर से पार उतर जाता है।
यह वह रसायन है जिसका सेवन करने के बाद संसार के भयानक रोग भी मनुष्य पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते।
यह वह चिन्तामणि है, जिसके हाथ में आते ही मनुष्य के आगे प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अन्धकार ठहरता तक नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष उस व्यक्ति से दूर खड़े रहते हैं जो रामचरितमानस को अपने जीवन का पथ-प्रदर्शक मानता है और उसकी बताई हुई रीति और नीतियों पर चलता है।
रामचरितमानस का महत्त्व आज केवल भारतवासियों की दृष्टि में ही नहीं अपितु विदेशी विद्वानों ने भी इसके महत्त्व को समझा है और अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया है तथा अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं।
यह एक ऐसा अमूल्य रत्न है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य को और कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती।
तुलसी ने रामचरितमानस में शाश्वत धर्म और विश्व धर्म की स्थापना की है।
धर्म और अधर्म की परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं-
“परहित सरिस धरम नहि भाई।
परपीड़ा सम नहि अधमाई || “
रामचरितमानस की रचना ऐसे समय में हुई थी, जबकि हिन्दू जनता समस्त शौर्य और पराक्रम खो चुकी थी। विदेशियों के चरण भारत में जम चुके थे।
हताश और हतप्रभ जनता अपना नैराश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। सामाजिक जीवन एक विषैली गैस बन गया था।
वह समय दो विरोधी संस्कृतियों, साधनाओं, सभ्यताओं और जातियों का सन्धिकाल था। देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति विशंखलित हो गई थी।
पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की खाइयाँ इतनी गहरी होती जा रही थीं कि उनका पटना असम्भव नहीं, तो मुश्किल अवश्य था।
अपने उचित पथ-प्रदर्शक के अभाव में जनता किंकर्तव्यविमूढ़ बन गई थी। ईश्वरवाद बढ़ता जा रहा था।
कुछ लोग भगवान् की वेदी पर विष्णु और शिव का बलिदान करके एकता का नारा बुलन्द कर रहे थे, जो कि जनता के अनुकूल नहीं था।
इन्हीं परिस्थितियों में लोकनायक तुलसीदास भारत-भूमि पर अवतरित हुए और इन्हीं परिस्थितियों की काली छाया में रामचरितमानस का सृजन हुआ, जिसने दूबती हुई हिन्दू जनता को नष्ट होती हुई सामाजिक मर्यादा को विखलित होती हुई वर्ण-व्यवस्था को बढ़ती हुई भयानक अमित्रता को असामयिक आारिक कलह को और लुप्त होती हुई आशा को बचा लिया।
जात-पाँत चीन्हें नहि कोई हरि को भजे सो हरि का होई ।।
रामचरितमानस से शिक्षा
आचरण की शिक्षा
गोस्वामी जी भगवान् राम के अनन्य भक्त होते हुए भी, एक सच्चे महान समाज सुधारक तथा लोकनायक थे।
उन्होंने राम के रूपक के द्वारा जनता को आत्म-कल्याण और आत्म-रक्षा के अमोघ मन्त्र प्रदान किए।
भिन्न-भिन्न प्रकार के चरित्र-चित्रण से भिन्न-भिन्न आचरणों की शिक्षा प्रदान की जो कि मानव जीवन की उन्नति के लिए परम आवश्यक है।
तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र द्वारा मनुष्य के उत्कृष्ट आचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी विशेष गुण और किसी आदर्श आचरण की प्रतिष्ठा करता है।
राम का बाल्यकाल, गुरु-गृह-गमन, विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा, सीता स्वयंवर, परशुराम जी को क्षमा करना, वनगमन, राक्षस-संहार, सुप्रीव और विभीषण की मैत्री, रावण वध तथा अयोध्या के राजा के रूप में राम के आदर्श चरित्र से तुलसी पग-पग पर अपने पाठकों को एक श्रेष्ठ आचरण और मर्यादित जीवन को शिक्षा देते हैं।
राम का अपने कनिष्ठ भ्राताओं के साथ व्यवहार, प्राणपण से पिता की आज्ञा-पालन, माताओं की समान भाव से सेवा, एक आदर्श भ्रातृ-प्रेम, पितृ-भक्ति और मातृ-सेवा के उदाहरण हैं।
सीता भारतीय महिलाओं के समक्ष ऐसा आदर्श उपस्थित करती हैं, जो उन्हें युगों तक प्रकाश प्रदान करता हुआ सदाचरण की शिक्षा देता रहेगा।
पति-सेवा व पतिव्रत धर्म का ऐसा उज्ज्वलतम उदाहरण भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिगोचर नहीं होता। ‘भरत का त्याग’ भी भारतीय संस्कृति में सभ्यता की एक प्रकाशपूर्ण ज्योति है।
रामचरितमानस पढ़ने के पश्चात् किसके मन में अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उदात्त भावनायें जागृत नहीं होतीं या कौन-सी स्त्री अपने आचरण को सीता के समान शुद्ध और पवित्र बनाना नहीं चाहती ?
राम का बालि-वध और सुग्रीव मैत्री की घटनायें एक आदर्श मित्रता का स्वरूप उपस्थित करती हैं।
प्रत्येक मित्र मानस श्रवण के पश्चात् यह अनुभव करने लगता है कि मेरी भी मित्रता राम और सुप्रीव जैसी हो।
विभीषण की रक्षा से तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को प्राणपण से अपने शरणागत की रक्षा करनी चाहिए।
कृतज्ञता का हनुमान और राम जैसा प्रसंग दूसरा क्या हो सकता है? साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि हमारे साथ भलाई करता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम कृतज्ञ बनें।
वनवास के समय राक्षसों का संघर्ष, सीताहरण, लक्ष्मणमूर्छा आदि ऐसे प्रसंग हैं, जिनमें राम का चरित्र अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की भाँति शुद्ध रूप में पाठक के समक्ष आ जाता है जिससे वह धीरता, वीरता, कृतज्ञता आदि गुणों को स्वयं ही अपनाने लगता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना और प्रत्येक कथा किसी न किसी विशेष गुण और शुद्धाचरण की शिक्षा देती है।
धार्मिक शिक्षा
रामचरितमानस भारतीय जनता का एक महान् धार्मिक ग्रन्थ है। आज तुलसी के प्रताप से ही राम-भक्ति समस्त भारत में व्याप्त है।
राम ब्रह्म के रूप में देखे जाते हैं। अशक्त और निर्धन व्यक्ति भी ‘निर्बल के बल राम’ कहकर शान्ति और सुख की श्वाँस लेता है।
यद्यपि तुलसी के पूर्व महाकवि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण में राम का जीवन वृत्त प्रतिपादित किया था, परन्तु वह संस्कृत भाषा में होने के कारण केवल संस्कृतज्ञों तक ही सीमित रहा।
तुलसी ने अपने महाकाव्य में ज्ञान, भक्ति और धर्म की विभिन्न धार्मिक धाराओं का समन्वय स्थापित कर आर्य-धर्म का फिर से प्रतिपादित किया है।
हमारा धर्म एक-दूसरे से लड़ने की और परस्पर ईर्ष्या करने की शिक्षा नहीं देता। यह सहयोग और समन्वय सिखाता है।
तुलसी ने शैव, शक्ति और वैष्णवों के पारस्परिक धार्मिक मत-मतान्तरों को समाप्त कर तथा कोरे ब्रह्मज्ञानियों को अपने उक्ति-वैचित्र्य से हतप्रभ करके समाज के समक्ष एक ऐसे सरल धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया कि जनता स्वतः ही इस ओर आकर्षित हो उठी और तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर कहने लगी कि-
“सियाराममय सब जग जानी, करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ “
रामचरितमानस के धार्मिक उपदेश, दुराचारी, पापी, अत्याचारी और अधार्मिक व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर लाकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं।
कितने पथ भ्रष्ट व्यक्ति रामचरितमानस के प्रताप से ही महान् बन गये, यह बताने की आवश्यकता नहीं।
सामाजिक शिक्षा
तुलसी ने रामचरितमानस में तत्कालीन भ्रष्ट समाज का चित्र भी उपस्थित किया है और यह बताया है कि समाज कैसा होना चाहिए, सुसंगठित समाज की स्थापना और व्यवस्था कैसे हो सकती है।
एक समाज-सुधारक के नाते तुलसीदास जी ने समाज की भी पुनर्व्यवस्था की। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की वर्ण-व्यवस्था तथा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम व्यवस्था को सुसंगठित समाज के लिए आवश्यक बताया है।
वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित समाज कभी विशृंखलित नहीं हो सकता। सामाजिक उन्नति के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं आज से शताब्दियों पूर्व गोस्वामी जी ने भी वही प्रयत्न किये थे।
अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा, लोकतन्त्रात्मक भावनायें, प्रत्येक जाति और वर्ण की मर्यादा आदि की शिक्षा के लिये ही राम ने सीता का परित्याग किया, गुरु को प्रणाम न करने पर काकभुशुण्ड का अधपतन, छोटे भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के फलस्वरूप बालि का वध, ऐसे सभी प्रसंग सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं।
तुलसीदास जी ने लिखा है-
“अनुज वधू भगिनी, सुत नारी।
सुन सठ ये कन्या सम चारी ॥”
राजनीतिक शिक्षा
रामचरितमानस और राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। तत्कालीन समाज में दूषित राजनीति का कुचक्र चल रहा था।
रामचरितमानस के पात्रों और घटनाओं के माध्यम से तुलसीदास जी ने जनता को वह मन्त्र दिया जिससे वह जीवित रहकर अत्याचारियों का दमन कर सके।
किस प्रकार राजा को प्रजा की सुख-समृद्धि का ध्यान रखना चाहिये, प्रजा के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए राजा को क्या-क्या करना पड़ता है और राजा के कार्य से असंतुष्ट प्रजा राजा को अपदस्थ भी कर सकती है— इन सब बातों का पूर्ण विवेचन रामचरितमानस में यथा स्थान प्राप्त होता है।
गोस्वामी जी के अनुसार राजा का जीवन प्रजा का जीवन है, इसलिए राजा और प्रजा के जीवन में कोई व्यवधान रेखा नहीं होनी चाहिए, राजा का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन एक होना चाहिए।
साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतियों में निपुण होते हुए राजा को आदर्श और सच्चरित्र होना चाहिए।
वह अपनी प्रजा का एकमात्र पिता है।
जिस राजा के राज्य में प्रजा दुःखी रहती है वह नर्कगामी होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है-
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अबस नरक अधिकारी ।।”
यदि राजा समदृष्टा होगा, तो प्रजा सुखी और शान्त रहेगी और यदि राजा की नीति भेद-भाव की हुई तो समाज में एक दिन वैषम्य की अग्नि भड़क उठेगी।
गोस्वामी जी ने लिखा है-
“मुखिया मुख सौं चाहिए, खान पान कहें एक।
पाले पोस सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ “
पूर्ववर्ती और परवर्ती जनता का कल्याण
हिन्दू-धर्म, हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्कृति और सभ्यता का जितना उपकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के द्वारा किया है, कदाचित ही किसी दूसरी साहित्यिक कृति ने किया हो।
उनके दिव्य सन्देश ने मृतप्राय हिन्दू जाति के लिये संजीवनी का कार्य किया, जिससे जनता में संगठन व सामंजस्य की भावना उत्पन्न हुई।
आज भी वह इसी दिव्य संदेश से अनुप्राणित हो रही है।
उपसंहार
आज भी हमारे कर्तव्यों की दिशा का निर्धारण गोस्वामी जी की सूक्तियों पर आधारित रहता है।
परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमने अपने पूर्वजों के अनुभव-सिद्ध उपदेशों को ग्रहण करना छोड़ दिया है और विदेशियों के चमक-दमक के सिद्धान्तों को ग्रहण करते जा रहे हैं।
यही कारण है कि समाज उत्तरोत्तर अशान्ति और कलह का घर बनता जा रहा है, आपस में असहयोग और असमानता बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि की लपटें हमें झुलसाये डाल रही हैं।
यदि हम अपना, अपने समाज का और अपने देश का कल्याण चाहते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के दर्शाये हुये मार्ग पर चलना होगा, रामचरितमानस जैसे महान ग्रन्थों की शिक्षाओं को आत्मसात् करना होगा, तभी हमारी सर्वागीण उन्नति सम्भव है।
रामचरितमानस की महानता और कल्याणकारिता के विषय में बेनी कवि ने लिखा है-
“वेदमत सोधि, सोधि, सोधि के पुरान सबै सन्त औ असन्त के भेद को बतावता।
कपटी कुराही कूप कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलावतौ ।।
बेनी कवि कहै मानो-पानी हो प्रतीति यह पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतौ ।
भारी भवसागर उतारतौ कवन पार, जो पै यह रामायण तुलसी न गावतौ ।।”
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण


चाँदनी रात में नौका विहार
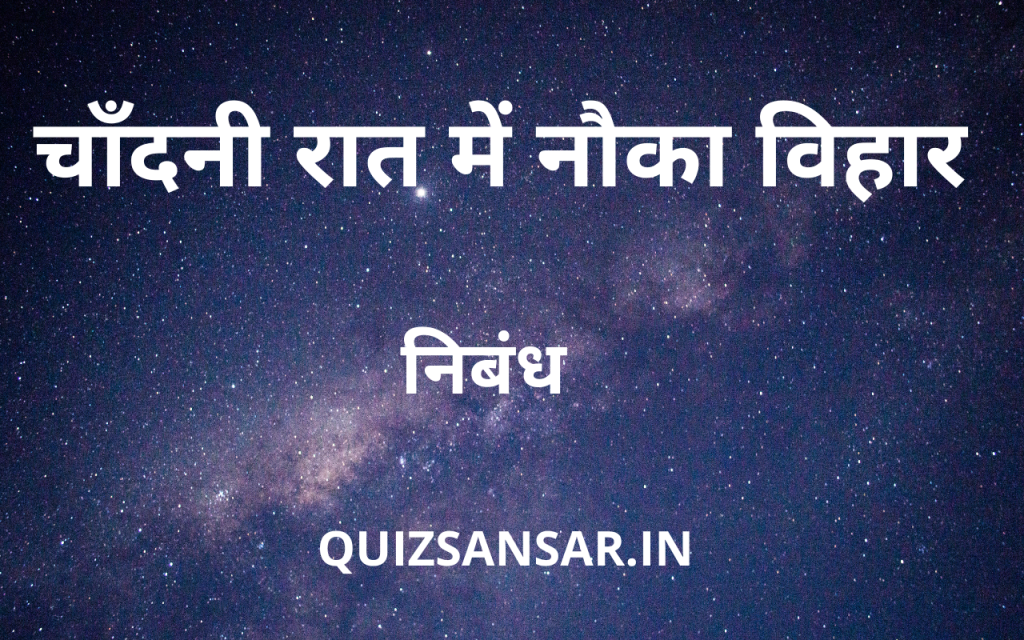
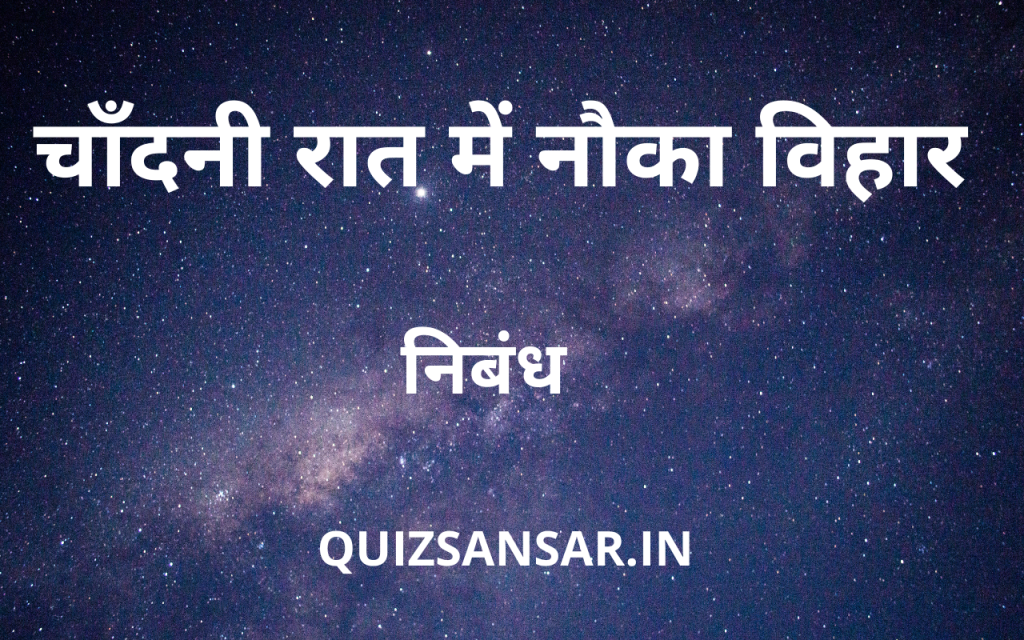
YAH एक निबंध है – चाँदनी रात में नौका विहार | जोकि आपके exam में निबंध lekhan की शैली को सुधारने में सहायक होगा |
रूपरेखा
- भूमिका
- प्रस्थान
- प्राकृतिक स्थिती
- उपसंहार
भूमिका
पूर्णिमा थी, चन्द्रदेव अपनी मुस्कुराहट से भूतल को आनन्द-विभोर कर रहे थे। शीतल-मन्द सुगन्धित वायु धीरे-धीरे गवाक्षों से मेरे कक्ष में प्रवेश करती और मेरे श्रांत मस्तिष्क को फिर से ताजा बना देती।
सहसा तीन-चार साथियों ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, “हमारा आज पढ़ने का मूड नहीं है, पढ़ने तुम्हें भी नहीं देंगे, आज हम लोगों ने नौका-विहार का .! निश्चय किया है, बोलो तुम्हारा क्या विचार है ?”
मैं भी पढ़ते-पढ़ते ऊब चुका था, बोला-“जरूर चलूँगा।” धीरे-धीरे हम लोग दस साथी हो गये, दो-तीन साथी ऐसे भी लिये जो गाने-बजाने में निपुण थे।
हम दशाश्वमेघ घाट की ओर चल दिये। विशाल घाटों के नीचे पंक्तिबद्ध नौकाएँ एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं।
काशी की नौकाएँ दो मंजिलें मकान की तरह होती हैं, बहुत बड़ी एक सुन्दर-सी नौका तय की गई, चतुर नाविक ने मुस्कराकर पचास रुपये माँगे, मामला चालीस रुपये में तय हुआ।
नाव अच्छी थी, चाँदनी बिछी हुई थी, मसनद लगी हुई थी।
बैठने से पूर्व कुछ शंकर-भक्त साथियों ने भंग की फंकी लगाई और गंगाजल चढ़ाया और नौका में बैठना प्रारम्भ किया।
प्रस्थान
निपुण नाविक ने “जय गंगे” कहकर नाव को किनारे से खोल दिया। पतवार के संकेत पर, नृत्य करने वाली नर्तकी की तरह डगमगाती हुई नौका अपने चरण बढ़ाने लगी।
क्षितिज की गोद से चन्द्रदेव कुछ ऊपर उठ चुके थे, अवनि अम्बर पर शुभ्र ज्योत्सना फैल रही थी। थिरक-थिरक कर नृत्य करने वाली तरंग मालाओं से पवन अठखेलियाँ कर रहा था।
ऐसा प्रतीत होता था मानो हम स्वर्ग में पहुँच गये हों। इस किनारे पर विश्वनाथ की काशी और उस किनारे पर रामनगर।
वातावरण शान्त और स्निग्ध था। गायक और वादक मित्रों से आग्रह किया गया, बस फिर क्या था संगीत छिड़ा, गंगा की हिलोरों के साथ हृदय भी हिलोरें लेने लगा।
यदि सिनेमा का संगीत होता था तो समझ में आ जाता था और यदि कभी पक्के गाने की बारी आ जाती तो समझ में न आता, परन्तु उसकी लय और ध्वनि हमें मंत्रमुग्ध कर देती थी।
बीच-बीच से तालियाँ बजती, वाह-वाह की आवाजें लगतीं और कोई कोई मनचला साथी कभी-कभी पंक्ति विशेष की पुनरावृत्ति की प्रार्थना भी करता।
प्राकृतिक दृश्य
चन्द्रिकाचर्चित यामिनी की निस्तब्धता चारों ओर फैली हुई थी। दोनों किनारों के बीच श्वेतसलिला भागीरथी अपनी तीव्र गति से प्रियतम जलनिधि से मिलने के लिए मिलन गीत गाती, इठलाती, पूर्व की ओर अग्रसर हो रही थी।
जहाँ तक दृष्टि जाती जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। एक किनारे पर काशी विद्युत बल्बों से जगमगाती दिखाई पड़ रही थी, दूसरी ओर रामनगर राजसी वैभव की याद दिला रहा था, परन्तु चाँदनी के प्रकाश में विद्युत बल्ब धूमिल प्रतीत हो रहे थे।
दूर दिशाओं में वृक्षों की फैली हुई मौन पंक्तियों को देखकर सहसा साधनारत साधक स्मरण हो जाता था।
भागीरथी के वक्षस्थल पर हिलोरें लेती हुई छोटी-छोटी लहरें तथा उन पर पड़ता हुआ चन्द्र प्रकाश उन्हें हीरे के हार की समता दे रहा था और हमारी नौका हंसिनी की तरह मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही थी।
चन्द्र और तारागणों का प्रतिबिम्ब गंगा जल में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था मानो चन्द्रमा जान्हवी के पवित्र जल में अनेक प्रकार से क्रीड़ा कर रहा हो।
कभी-कभी मछलियाँ हमारी नाव के पास आकर अपना मुख दिखा जातीं, परन्तु हमें खाली हाथ देखकर तुरन्त डुबकी लगा लेतीं और हमारी रिक्तहस्तता की निन्दा करती हुई चली जातीं।
सर्वत्र निस्तब्धता का साम्राज्य था, प्रकृति सुन्दरी लहरों के नुपूर बजा रही थी।
चंचल जल पर इन्दुलक्ष्मी नृत्य-रत थी और हमारी नाव दक्षिणी किनारे की ओर चली जा रही थी।
कुछ समय के लिए संगीत बीच बन्द कर दिया गया परन्तु साथियों के हृदय में फिर इच्छा हुई कि कार्यक्रम चलना चाहिए, गायक बन्धुओं से कुछ सुनाने का निवेदन किया गया।
बस फिर क्या था संगीत की स्वर-लहरियाँ आकाश में स्वरमत हो उड़ने लगी। कौन-सा राग गाया जा रहा था इसका तो कुछ पता ही नहीं, परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि मेरा मन बाँसों उछल रहा था।
संगीत की मधुर ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हम लोग ही नहीं, हमारा नाविक भी मस्ती से झूमने लगा।
उसके हाथ की पतवार जो प्रत्येक क्षण बड़ी शीघ्रता से घूमती थी, अब उसमें न उतनी तीव्रता थी और न त्वरा थी, न जाने वह अपने जीवन के अतीत की कौन-सी. मधुर स्मृति में अपने को भूले जा रहा था।
तभी हम लोगों ने उसकी तंद्रा भंग करते हुये कहा, “हम लोग कुछ क्षणों के लिए उस पार उतरना चाहते हैं, बोलो रुकोगे?” उसने मस्तक नीचे किये हुए ही कुछ देर हाथ की उंगली से आँखों की कोर पोंछते हुए स्वीकारात्मक सिर हिला दिया।
अब नौका का प्रवाह दूसरे किनारे की ओर था, जहाँ नीरवता थी, जंगल था और जंगली जानवर थे। उस शून्य तट पर हम उतर पड़े।
मुझे सहसा प्रसाद की ये पंक्तियाँ स्मरण हो आई-
“नाविक ! इस सूने तट पर, किन लहरों में खे लाया,
इस बीहड़ बेला में क्या, अब तक था कोई आया ॥ “
हम लोग लघुशंका इत्यादि से निवृत्त होकर प्रसन्न मुद्रा में आकाश को देख रहे थे। सुधास्नात चन्द्रिका मन को मुग्ध किये दे रही थी।
सहसा आकाश के कोने में एक काली बदली दिखाई पड़ी, हवा तेजी से चल रही थी, परन्तु अब उसमें कुछ धीमापन आ गया था।
हमारे देखते ही देखते उस छोटी-सी बदली ने समस्त आकाश को आच्छादित कर दिया, कालिमा की गहनता क्षण-क्षण बढ़ती जा रही थी।
सभी ने विचार किया कि जल्दी ही लौटना चाहिये, कहीं ऐसा न हो कि वर्षा होने लगे। गंगा का कल-कल निनाद अब कुछ भयंकरता धारण कर रहा था।
हम लोग तुरन्त नाव पर चढ़ गये और नाविक से शीघ्रता करने के लिए प्रार्थना की बड़ी कठिनाई से हमारी नाव 50%) गज की दूरी तय कर पाई होगी कि एक-दो बूँदें गिरी।
जिसके ऊपर गिरों वहीं पहले चिल्लाया, वर्षा आ गई। सब ऊपर को देख ही रहे थे कि बूँदें पड़ने लगीं।
नाविक बड़ी तेजी से पतवार चला रहा था। रुक-रुक कर बादल गरजते और बीच-बीच में बिजली चमक जाती।
गंगा का जल बीच-बीच में गोलाकार होकर भयानक भंवरों की सूचना दे रहा था। केवल बिजली की गड़गड़ाहट और जंगली जानवरों के रोने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी।
अब वर्षा के वेग में भयानकता थी और जल-बिन्दुओं के आकार में स्थूलता। परन्तु किनारा अब अधिक दूर नहीं था, कुछ ही क्षणों में नाव किनारे पर आ लगी।
हम लोगों ने कूद-कूद कर भागना शुरू किया और घाट पर बने हुए सामने वाले मन्दिर में आकर शरण ली।
नाविक अब भी हमारे साथ था, क्योंकि उसे हमसे किराया लेना था। उसे किराया देकर हमने रिक्शे लिए। वर्षा और रात का समय देख रिक्शे वालों ने हमसे दुगुने पैसे माँगे ।
इस समय और दूसरा कोई उपाय न देखकर हमने उनकी माँग स्वीकार कर ली।
उपसंहार
सारा जनसमूह निद्रा देवी की गोद में स्वप्निल संसार में विचरण कर रहा था। केवल नगर के प्रहरी, कुत्ते तथा सड़कों के विद्युत बल्ब ही जाग रहे थे, मानो वे हमारी प्रतीक्षा में हों।
हॉस्टल के बन्द द्वार पर जाकर हमने चौकीदार को आवाज लगाई। वह बेचारा वास्तव में हमारी प्रतीक्षा में बैठा था।
अपने चिरसहचर हुक्के को हाथ में लिए उसने दरवाजा खोला और हमने अपने-अपने कमरों में शरण ली।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi


मनोरंजन के आधुनिक साधन


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- मनोरंजन के साधन
- सरकार का कर्तव्य
- उपसंहार
प्रस्तावना
अपने जीवनयापन के लिए मनुष्य को संसार में क्या-क्या नहीं करना पड़ता। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए मिलों में काम करने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक, सुबह से शाम तक बोलने वाले वकील, नगर के प्रमुख चौराहों और ताँगों के अड्डों पर चाट बेचने वाले चौदह वर्षीय बालक, थले पर जम कर बैठने वाला लाला अपना मनोरंजन के आधुनिक साधन खून और पसीना एक करते हैं।
दिवस के अवसान और संध्या आगमन के क्षणों में सुबह से शाम तक थका हुआ मानव शारीरिक विश्राम के साथ-साथ मानसिक विश्राम भी चाहता है, जिससे उसका बका-मांदा मन किसी तरह बहल जाये, और वह फिर प्रफुल्लित हो उठे।
मनोरंजन की पृष्ठभूमि में यही प्रवृत्ति काम करती है। यदि मनुष्य की रुचि के अनुकूल उसे मनोविनोद प्राप्त हो जाता है, तो वह दूसरे दिन फिर नये उत्साह और उल्लास से कार्य करने की क्षमता एकत्रित कर लेता है।
इससे उसके स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिना मनोरंजन के जीवन भार मालूम पड़ने लगता है।
मनुष्य नित्य एक से कामों से ऊबने लगता है और जीवन के प्रति उसका घृणात्मक दृष्टिकोण हो जाता है।
कोल्हू के बैल की तरह रोज सुबह से शाम तक एक ही काम में जुठना और शाम को थक कर पड़ जाना, ऐसा जीवन, जीवन नहीं, मनुष्य के लिए बोझ का एक गट्टर बन जाता है।
आखिर आकर्षणहीन भार को मनुष्य कब तक उठाये। इससे उसको कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।
मनोरंजन के साधन
प्राचीन समय में मानव का जीवन और जीवन यापन के साधन सरल थे। दिनभर के कठोर परिश्रम के उपरान्त घर पर शान्त और सुखमय वातावरण उसकी थकान दूर कर देता था।
अतः उसे मनोरंजन की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी, परन्तु आज के व्यस्त एवम् संघर्षमय जीवन में उसे मनोविनोद के साधनों की परम आवश्यकता है।
मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य के मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन आये हैं। विज्ञान के आविष्कार ने इन साधनों में आमूलचूल परिवर्तन उपस्थित कर दिया है।
रेडियो और सिनेमा इसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।
मनोरंजन के साधनों को हम अलग-अलग कई भागों में बाँट सकते हैं कुछ मनोरंजन के साधन ऐसे हैं, जिनका हम घर बैठे-बैठे ही आनन्द ले सकते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिनके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और इनके अतिरिक्त कुछ साधन ऐसे होते हैं, जिनके लिए मित्र मंडली तलाश करनी पड़ती है।
मैदान के खेल
क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, बास्केटबाल, बैडमिण्टन, टैनिस और कबड्डी आदि मैदान के खेलों से खिलाड़ी एवं दर्शकों का अच्छा मनोरंजन होता है।
छात्रों के लिये ये खेल अत्यन्त लाभकारी हैं। इससे मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है।
बड़े-बड़े नगरों में जब ये खेल होते हैं तो लाखों दर्शनार्थी एकत्रित होकर अपना मनोरंजन करते हैं।
कमरे के अन्दर के खेल
कैरम, चौपड़, शतरंज आदि खेलों से आप घर बैठे-बैठे ही अपना मनोरंजन कर सकते हैं।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति इन्हीं खेलों से अपना मन बहलाया करते हैं।
परन्तु इनमें कुछ खेल तो दुर्व्यसनों की कोटि में भी आते हैं, जैसे ताश खेलना। जब इसकी आदत अधिक हो जाती है, तो मनुष्य जुआ खेलने की ओर प्रवृत्त होता है और चौपड़, शतरंज खेलने में तो मनुष्य खाना-पीना, सोना सब कुछ भूल जाता है।
अपने मनोनुकूल साहित्य का अध्ययन भी घर के मनोरंजन में ही आता है। रेडियो के मनोमुग्धकारी विभिन्न कार्यक्रम और टेलीविजन के मनोहारी दृश्य आज के युग के सस्ते और सुलभ मनोरंजन के साधन हैं, जो घर बैठे-बैठे ही मनुष्य को आनन्द प्रदान करते रहते हैं।
भारतवर्ष में मनोरंजन के साधनों की कमी
कुछ व्यक्तियों का अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करने में ही मनोरंजन होता है। बहुत-से बड़े-बड़े बाबुओं को देखा गया है कि शाम को दफ्तर से लौटने के बाद कुछ खा-पीकर छोटी-सी खुरपी ली और अपनी कोठी के छोटे से बाग की क्यारियों में जा बैठे।
नित्य ही उनके घंटों इसी काम में व्यतीत हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह शौक हो जाता है कि कैमरा कन्धे पर लटकाया और चल दिये जंगल की ओर जहाँ का दृश्य मन को अच्छा लगा वहीं का फोटो ले लिया। उनका मनोविनोद इसी में है।
कुछ लोगों को अधिकांश छात्र वर्ग को, तरह-तरह के और विभिन्न देशों के पुराने स्टाम्प एकत्रित करने का शौक होता है।
उन्हें पुराने लिफाफे और सड़ी हुई रद्दी को ढूंढने में ही आनन्द आता है। कुछ व्यक्ति विभिन्न प्रकार के चित्र एवं सिक्के संकलित करते हैं।
उनका मन इसी कार्य में लगता है और वे इसमें ही आनन्द का अनुभव करते हैं।
भ्रमण
भ्रमण करना भी मनोरंजन के साधनों में एक उत्तम साधन है। अनेक व्यक्ति प्रातः एवम् सायं परिभ्रमण के लिए जाते हैं और प्रकृति का उन्मुक्त परिहास देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है।
छोटे-छोटे पिकनिक और बड़ी-बड़ी यात्राएं इसी उद्देश्य के साधन हैं। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है।
उसे प्रसन्न देखकर मनुष्य भी एक बार आत्मविभोर हो उठता है और क्षणभंगुर जगत् के सुख-दु:खमय क्षणों को कुछ समय के लिये भूल जाता है।
निर्झरों का फेनिल प्रपात, कल-कल करती नदियों का प्रवाह, बौराई हुई वनराशि समोर को सुरभित करते पुष्प और मुस्कुराती हुई कलियों को देखकर कौन होगा जो प्रसन्न न हो उठे।
इनके अतिरिक्त, कलाप्रिय मनुष्य के लिए कलात्मक मनोरंजन रुचिकर होते हैं। सिनेमा और नाटक इसी प्रकार के कलात्मक मनोरंजन के साधन हैं।
आज के भौतिकवादी युग में सिनेमा से असंख्य व्यक्तियों का मनोरंजन होता है। मुग्धकारी संगीत, मनोहारी नृत्य और कर्ण-सुखकारी चाद्य मनोविनोद के साधनों में सर्वोपरि है।
यदि चित्रकारी चित्रकार के हृदय की वीणा के तारों को झंकृत करने में समर्थ है, तो शिल्पकारी भी शिल्पकार को असीम आनन्द देने में पीछे नहीं है।
सरकार का कर्तव्य
आज का युग उपन्यास एवम् कहानियों का युग है। आज के शिक्षित वर्ग के मनोरंजन के है ये मुख्य साधन हैं।
नित्य नये-नये उपन्यासों का प्रकाशन और उनके हाथों-हाथ बिक जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज के उपन्यासों और कहानियों से जनता का मनोविनोद तो होता है परन्तु पाठक इनसे पथ भ्रष्ट भी खूब होते हैं।
शिक्षा तो गूलर का फूल हो गई है। धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य आज भी रामायण का पाठ कर लेते हैं।
मित्र मण्डली में बैठकर गप्पे लगाना, मेले-तमाशों में जाना, पर्वतारोहण करना, शिकार खेलना, इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न मनोरंजन के साधन हैं।
नशेबाजों का मनोरंजन नशे में होता है चाहे वह भांग का हो या गाँजे का वास्तव में बात तो यह ही है कि-
“काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।
व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा ॥”
इसका सीधा-साधा अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का मनोविनोद सुन्दर सुन्दर पुस्तकों के अध्ययन में होता है और मूर्खों का लड़ने सोने और संसार के अनेक दुर्व्यसनों में फंसकर |
दीर्घकालीन परतन्त्रता के कारण अभी हमारा देश मनोरंजन के साधनों में इतना समुन्नत नहीं है जितने कि विकसित देश रूस और अमेरिका आदि देशों में मिल-मजदूरों तक के लिये मनोरंजन के समुचित साधन उपलब्ध है, फिर सम्पन्न व्यक्तियों की तो बात ही क्या ?
इन साधनों से मजदूरों के हृदय में एक बार फिर उत्साह, उल्लास एवं स्फूर्ति आ जाती है। भारतवर्ष मामों का देश है।
भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, परन्तु उसके लिये कोई मनोरंजन के साधन नहीं है और यदि दो-एक है भी तो ये भी पुरातन काल के पिष्टपेषण हैं, आज भी उनके लिए सबसे बड़े मनोरंजन कबड्डी और कुश्तियाँ ही हैं।
यदि आप और आगे बढ़े भी तो नाटक और स्वांग तक बस |
उपसंहार
आधुनिक समय में सर्वाधिक लोकप्रिय घरेलू मनोरंजन दूरदर्शन है।
दूरदर्शन के विभिन्न मनोहारी कार्यक्रम दर्शकों का पर्याप्त मनोरंजन करते हैं जिनसे ज्ञानवर्धन भी होता है और जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतीक रूप में मार्ग दर्शन भी मिलता है।
मानव कल्याण की दिशा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के निदेशक इस दिशा में बधाई के पात्र हैं।
भोजन व वस्त्र के समान ही मनोरंजन भी मानव जीवन की एक आवश्यकता है, पर इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सारा समय मनोरंजन में ही न बीत जाए क्योंकि जीवन के क्षण अमूल्य है।
कहीं परिश्रम से अर्जित किए हुए द्रव्य का मनोरंजन के साधन जुटाने में ही अपव्यय न हो जाए और साथ ही साथ मनोरंजन इस प्रकार का न हो कि जिससे हमारी भावनाओं और विचारधाराओं पर दूषित प्रभाव पड़े।
कोमल-बुद्धि बालकों के मनोरंजन में माता-पिता की देखभाल आवश्यक है।
अन्यथा अनुभवहीनता के कारण वे अपना अहित भी कर सकते हैं।
प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए कि उसके मनोविनोद को सौमा दूसरों की मान-मर्यादा एवं सुख-सुविधा का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है।
आपको हमारे यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi


आदर्श विद्यार्थी


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- आदर्श विद्यार्थी के गुण
- आधुनिक गुण का विद्यार्थी
- उपसंहार
प्रस्तावना
विद्यार्थी अवस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। यदि नींव दृढ़ है तो उस पर प्रासाद भी चिरस्थायी बन सकेगा अन्यथा सांसारिक झंझावात की भयानक आँधियों के थपेड़े, तूफान और अनवरत वर्षा उसे थोड़े ही दिनों में धराशायी कर देंगे।
इस प्रकार यदि बच्चे का छात्र जीवन परिश्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमित रूप से व्यतीत हुआ है, यदि छात्रावस्था में उसने मन लगाकर विद्याध्ययन किया है, यदि उसने गुरुओं की सेवा की है, यदि वह अपने माता-पिता तथा गुरुजनों के साथ विनम्र रहा है, तो निश्चय ही उसका भावी जीवन सुखद एवं सुन्दर होगा।
जिस वृक्ष का बाल्यावस्था में सम्यक सिंचन होता है वह भविष्य में पल्लवित और पुष्पित होता हुआ एक न एक दिन संसार को सौरभमय अवश्य बना देता है।
आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा। सभ्य नागरिक के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों की प्राथमिक पाठशाला विद्यार्थी जीवन ही है।
संसार में गुणों से ही मनुष्य का आदर-सत्कार एवं प्रतिष्ठा होती है क्योंकि ‘गुणैर्हि सर्वत्र पदं निघीयते” अर्थात् गुणों से ही मनुष्य हर जगह ऊँचा पद प्राप्त करता है।
विद्या ही वह कोष है, जिसमें अमूल्य गुण रूपी रत्न विद्यमान है। उसे प्राप्त करने के लिये हमें साधना करनी होगी और साधना के लिये समय आवश्यक है।
विद्यार्थी जीवन उसी सुन्दर साधनावस्था का समय है. जिनमें बालक अपने जीवनोपयोगी अनन्त गुणों का संचय करता है, ज्ञानवर्धन करता है और अपने मन एवं मस्तिष्क का परिष्कार करता है।
पशु और मनुष्य की विभाजन रेखा यदि कोई है तो यही – विद्यार्थी जीवन, अन्यथा पशुओं को वे सभी अवस्थायें प्राप्त हैं, जो मनुष्य को क्या वचपन और क्या गृहस्थ ?
अतः मानव-जीवन में विद्यार्थी जीवन का विशेष महत्त्व है।
आदर्श विद्यार्थी के गुण
नम्रता और अनुशासन
विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता परम आवश्यक है। यदि विद्यार्थी उद्दण्ड है, उपद्रवी है, उच्छृंखल है, या कटुभाषी है तो वह कभी भी अपने अध्यापकों का कृपापात्र नहीं हो सकता।
मेरी समझ में यह नहीं आता कि विद्यार्थी कटुभाषी या उच्छृंखल हो कैसे जाता है ? क्योंकि विद्या तो उसे यह सिखाती नहीं कहा गया है कि-
“विद्या ददाति ज्ञानम् ज्ञानम् च शीलम् .: शीलम् च गुणम्”
अर्थात् विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से शील उत्पन्न होता है और शील से गुण प्राप्त होते हैं। विद्या के पास देने को यदि कुछ है तो वह विनय है, जो विद्यार्थी का ही नहीं समस्त मानव जीवन का आभूषण है। गुरुजनों से विद्या प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आप विनम्र रहिए। विद्वानों ने कहा भी है कि-
“तद् विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया”
अर्थात् गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के तीन उपाय हैं- नम्रता जिज्ञासा और सेवा। इसमें नम्रता का स्थान प्रथम है।
अतः एक आदर्श विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। नम्रता के साथ-साथ उसे अनुशासनप्रिय भी होना चाहिए।
जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं वे अपने देश, अपनी जाति, अपने माता-पिता अपने गुरुजन और अपने कॉलिज के लिए अप्रतिष्ठाकारी होते हैं।
अनुशासनहीन छात्र का न तो मानसिक विकास होता है और न बौद्धिक ही। वह उन गुणों से सदैव सदैव के लिए वंचित रह जाता है, जो मनुष्य को प्रतिष्ठा के पद पर आसीन करते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र ही आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकता है।
आज के युग का छात्र अनुशासनहीनता दिखाने में अपना गौरव समझता है, इसलिए देश में सभ्य नागरिकों का अभाव-सा होता चला जा रहा है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक नेता, शासक तथा गुरु है।
प्रेम की राह दिखा दुनिया को रोके जो नफरत की आंधी।
तुममें ही कोई नेहरू होगा, तुममें ही कोई होगा गाँधी ।।
श्रद्धा और जिज्ञासा
बिना श्रद्धा के न आप कुछ पा सकते हैं और न कुछ दे सकते हैं। श्रद्धा से पाषाण तक फल देने लगता है, फिर कोमल हृदय गुरुजनों की तो बात ही क्या, क्योंकि ‘श्रद्धावान् ज्ञानम्।’ ज्ञान तो श्रद्धावान् को ही प्राप्त होता है।
यदि आप में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो आप उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे विद्यार्थी में श्रद्धा के साथ-साथ जिज्ञासा भी होनी. चाहिए।
यदि आपके अध्यापक एक बात बता रहे हैं, तो उसकी समाप्ति पर उसी विषय पर आप चार बात पूछिये, इससे आपका ज्ञानवर्द्धन होगा, जिसका अर्थ है, जानने की इच्छा, अर्थात् आदर्श विद्यार्थी में नवीन वस्तु और नये विषय के प्रति उत्कण्ठा एवं जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वह कुछ प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि ज्ञान का भण्डार अमिट है, गुरु भी आपको कहाँ तक देंगे। हाँ, आपकी नवीन शंकाओं का समाधान अवश्य कर देंगे।
जिन विद्यार्थियों में जिज्ञासा को प्रवृत्ति नहीं होती वे कक्षा में मूर्ख बने बैठे रहते हैं और दूसरों का मुँह ताका करते हैं।
संयम और नियम
विद्यार्थी जीवन संयमित तथा नियमित होना चाहिए। जीवन के नियमों का उचित रीति से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी असफल नहीं होते।
विद्यार्थी को अपनी इन्द्रियों और अपने मन पर संयम रखना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमित रूप से विद्याध्ययन करना, सन्तुलित भोजन करना, सदैव अपने से बड़ों की संगति में बैठना, दूषित एवम् कलुषित विचारों से दूर रहना, ये आदर्श विद्यार्थी के आवश्यक गुण हैं।
जो विद्यार्थी अपने जीवन में संयम नियम का ध्यान नहीं रखते। वे अस्वस्थ रहते हैं, उनका मुँह पीला पड़ा रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, सदैव नींद या दुर्व्यसन घेरे रहते हैं, उनका मन चंचल होता है।
इसलिए विद्यार्थी जीवन की सफलता की कुंजी संयम और नियम है।
श्रम और स्वास्थ्य
विद्यार्थी को स्वाध्यायी और परिश्रमी होना चाहिए। बिना परिश्रम किये विद्या आ नहीं सकती।
सुखार्थी और विद्यार्थी में बहुत अन्तर है, विद्यार्थी को परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं और सुखार्थी इस प्रकार के उत्तम श्रम से विमुख रहता है।
नीतिविशारदों की सूक्ति है-
“सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्
सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम् ॥”
अर्थात् न विद्यार्थी को सुख है न सुखार्थी को विद्या विद्यार्थी को सदैव परिश्रम करना चाहिए।
कक्षा में पढ़ाये गये विषयों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें समझने और मनन करने का प्रयत्न करना चाहिए।
कक्षा में ही नहीं, घर जाकर भी परिश्रम से उस विषय को याद करना चाहिए।
कक्षा की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे अन्य साहित्यिक पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए जिससे साहित्य के विभिन्न अंगों का ज्ञानवर्द्धन होता रहे। स्वाध्याय के प्रति मनुष्य को कभी भी प्रसाद या आलस्य नहीं करना चाहिए।
समय का सदुपयोग
मनुष्य की थोड़ी-सी आयु, उसमें भी बहुत थोड़ा विद्यार्थी जीवन और उसमें भी अनन्त विघ्न, फिर क्या यह विद्यार्थियों के लिए उचित है कि वे अपने अमूल्य समय का अपव्यय और दुरुपयोग करें।
अच्छे विद्यार्थी कभी भी अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं बिताते । उनके जीवन का ध्येय अध्ययन होता है न कि समय का अपव्यय ।
‘क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्।’
एक एक पैसा जोड़े बिना कोई धनवान नहीं हो सकता। धन के निरन्तर संग्रह करने वाले को ही धनवान कहते हैं।
अगर मनुष्य एक एक कण छोड़ता जाये तो धनवान नहीं बन सकता। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी एक-एक क्षण नष्ट करता रहे तो वह विद्याध्ययन नहीं कर सकता।
शिक्षा के साथ क्रीड़ा
पढ़ते-पढ़ते थक जाने पर मस्तिष्क को आराम देने के लिए थोड़ा खेल लेना भी आवश्यकः है। इससे शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है और विद्यार्थी का मनोरंजन भी हो जाता है।
समय पुस्तकों में लगा रहना भी कभी-कभी हानिकारक सिद्ध हो जाता है। अधिक परिश्रम करने से विद्यार्थी ऐसे समय में बीमार पड़ जाते हैं जब उनकी परीक्षायें सिर पर होती हैं।
इसलिये पहले से ही खूब पढ़िये और थोड़ा खेल भी लीजिए। इससे विद्यार्थी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। संस्कृत साहित्य में अच्छे विद्यार्थी के पाँच लक्षण बताये हैं
“काकचेष्टा वकोध्यानं श्वान निद्रा तथैव च।
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम् ॥”
अर्थात् कौए की चेष्टा वाला, बगुला के से ध्यान वाला, कुत्ते की सी निद्रा वाला, थोड़ा खाने वाला और घर से मोह न रखने वाला, इन लक्षणों से युक्त विद्यार्थी ही समुचित विद्याध्ययन कर सकता है।
आधुनिक गुण का विद्यार्थी
आज विद्यार्थियों में एक वर्ग ऐसा है जो विचित्र प्रकार का जीवन बिताना चाहता है। न उसे अध्यापक समझ पा रहे हैं और न अभिभावक ही।
न उसके ऊपर शासन का नियन्त्रण है, न जनता का। सर्वत्र स्वतन्त्र होकर पतन के कगार पर खड़ा हुआ वह एक धक्के की प्रतीक्षा करता है।
न उसे माता-पिता की लज्जा है और न गुरुजनों की न समाज का भय है और न साथियों का, न मान की चिन्ता है, न मर्यादा की, न शासन का भय है और न न्याय का न पुस्तक का ध्यान है और न कुञ्जियों का ‘सादा जीवन उच्च विचार’ वाला सिद्धान्त उससे कोसों दूर खड़ा कॉप रहा है।
आत्म-संयम तो न जाने उससे कहाँ बिछुड़ गया। आज का विद्यार्थी क्या कर सकता है यह तो पूछने का प्रश्न ही नहीं रहा। इस समय तो प्रश्न है कि यह विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता।
संसार के जघन्य और घृणित से घृणित कुकृत्य करने में आज वह अपसर है। सिगरेट के कश, शराब के घूँट और सिनेमा के स्वरों ने उसे मुग्ध कर लिया है।
विद्याध्ययन के स्थान पर वह तेल, पाउडर और सूट-बूट का विधिवत् अध्ययन करता है। विनम्रता, अनुशासन और आज्ञा पालन से उसे स्वाभाविक घृणा होती जा रही है।
कितनी लज्जा आती है, जबकि लोगों को यह कहते हुये सुना जाता है कि अमुक डकैती इतने लड़के उस कॉलिज के थे, या अमुक विद्यार्थी ने अमुक अध्यापक को मार डाला।
आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। आज के ही विद्यार्थी समुदाय में ही देश के भावी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, शासक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, सेनानायक, समाज सुधारक सभी सम्मिलित हैं।
वे ही राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं और राष्ट्र के जीवन स्तम्भ हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए उच्चतम शिखर तक पहुँचने की।
उपसंहार
यदि आज का विद्यार्थी देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता है, यदि वह जीवन में सफल होना चाहता है, यदि उसे अपनी आत्मोन्नति की इच्छा है, यदि वह अपने और अपने माता-पिता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहता है, तो उसे वे गुण अपनाने होंगे, जिनमें उसका उत्थान निहित है।
उसे अपना चरित्र सुधारना होगा, उसे अपने गुरु के प्रति वे ही पुरातन सम्बन्ध स्थापित करने होंगे जो आज से दौ सौ वर्ष पहले थे। तभी भारतवर्ष का विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी कहलाने का अधिकारी हो सकता है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
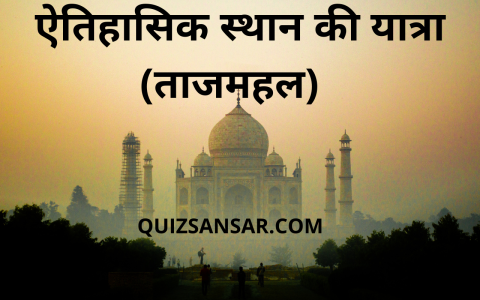
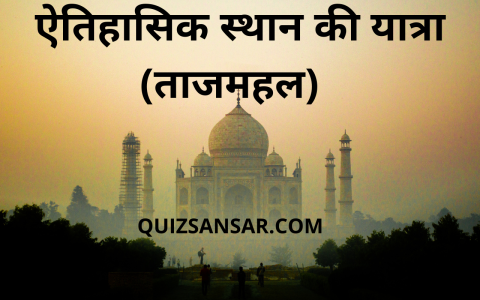
ऐतिहासिक स्थान की यात्रा (ताजमहल)


रूपरेखा
- प्रस्तावना
- आगरे के लिए प्रस्थान
- ताजमहल का दृश्य
- रचना काल
- आधुनिक चमत्कारों में ताज का स्थान
- उपसंहार
प्रस्तावना
अभी पूरी छुट्टियाँ समाप्त नहीं हुई थीं, लगभग चौदह दिन शेष थे।
वर्षा प्रारम्भ हो चुकी थी, कई दिनों से बादल आसमान पर घिरे हुए थे, कभी कोई छोटी बदली बरस जाती और कभी तीव्र वायु के झोंके सभी बादलों को उड़ा ले जाते परन्तु आज सुबह से ही रिम-झिम शुरू हो गई थी, मन चाह रहा था कि कहीं घूम आऊँ पर प्रश्न यह था कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि छुट्टियाँ भी समाप्त हो रही थीं।
फिर कौन जाता है, और कौन जाने देता है, पढ़ने-लिखने से ही अवकाश नहीं मिलता।
यदि कभी जाने का विचार भी किया जाये तो अटैन्डेंस शॉर्ट (उपस्थिति कम) होने का भय लगा रहता है, इसलिए कहीं जाने पर भी आनन्द नहीं आता।
दोपहरी होने वाली थी, लगभग ग्यारह बजे होंगे, नीचे से एक साथ आवाजें आई। मैं एकदम से नीचे आया।
मालूम हुआ कि एक आवाज तो खाने के लिए माँ ने दी थी और दूसरी दरवाजे पर खड़े पोस्टमैन ने। माँ ने कहा, “खाना खाओ।” बाहर जाकर पोस्टमैन से चिट्ठी ली।
पढ़ा तो मालूम हुआ कि मेरे एक पुराने साथी का पत्र है, जो हाई स्कूल पास करने के बाद आगरे में रोडवेज के दफ्तर में क्लर्क हो गया था।
यद्यपि वह पढ़ने में कमजोर था, परन्तु मेरा घनिष्ठ मित्र था। पत्र में लिखा था |
“मेरा विवाह तारीख 1 जुलाई को है, बारात आगरे से आगरे में ही जायेगी, चाहे तुम एक दिन को आओ, पर आना अवश्य।”
बस, माँ से आज्ञा लेने के बाद मैं, विवाह में जाने की तैयारियाँ करने में लग गया।
आगरे के लिए प्रस्थान
छुट्टियाँ थीं ही, घर पर भी कोई विशेष काम नहीं था, इसलिए निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व ही आगरे को रवाना हो गया और मित्र को सूचित कर दिया कि मैं आ रहा हूँ।
सूचित इसलिये किया था। क्योंकि मैंने उसका घर नहीं देखा था। टूण्डला से जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो आगरा देखने की इच्छा तीव्र होने लगी।
आगरे का इतना आकर्षण नहीं था, जितना कि ताजमहल देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करने का अभी आगरा 8-10 किलोमीटर दूर था कि ताजमहल की स्निक्त दुग्ध-धवल, गगनचुम्बी मीनारें दिखाई पड़ने लगीं।
डिब्बे के सारे यात्री ‘ताज़-ताज’ कहकर खिड़कियों से सिर निकाल कर झाँकने लगे।
ताजमहल का दृश्य
स्टेशन पर मित्र मिला, मुझे देखकर वह गद्गद् हो गया। सामान लेकर हम लोग घर पहुँचे। दूसरे दिन पूर्णिमा थी।
दो-तीन रिश्तेदारों को साथ लेकर मैं सन्ध्या के समय प्रेम की अमर समाधि ताज को देखने के लिए गया। मार्ग में शाहजहाँ और मुमताज के विषय में अनेक भावनायें उठने लगीं।
दुर्भाग्य के सम्मुख सुकोमल मानव हृदय की विवशता पर विचार कर हृदय द्रवित हो उठा। अब तो ताज की लाल पत्थर की ऊँची-ऊँची चहारदीवारी भी दिखाई पड़ने लगी थी।
सहसा हम उस विशाल द्वार पर जाकर रुके जो ताजमहल का प्रवेश द्वार है। द्वार में घुसते ही सुन्दर-सुन्दर फव्वारे और मनोहर उद्यान दिखाई पड़ने लगे।
हरे-भरे वृक्षों का कलात्मक शृंगार देखकर हम लोग मुग्ध हो गये। इस स्वर्गीय उद्यान के सामने ही एक वम्राकार चौड़े चबूतरे पर ताजमहल का भव्य प्रासाद स्थित है, जो सदियों से अपने अमर प्रेम की कहानी कहता हुआ आज भी नहीं थकता।
मुगल साम्राज्य के आहत यौवन के उस अमर स्मारक ताज के चारों ओर चार गगनचुम्बी मीनारें हैं, मानो वे आज भी अनिमेष दृष्टि से आकाश की ओर देखती हुई अपने रचयिता के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में हों।
ताज के पश्चिमी भाग में कल-कल निनादिनी, नीलसलिला यमुना अपनी प्रमत्त गति से प्रवाहित होती है। पूर्णिमा का चन्द्रमा आकाश में मुस्कुरा रहा था।
चाँदनी में ताज की शोभा कई गुना अधिक हो जाती है। यहाँ के निर्मल जल में ताज का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था।
कुछ क्षणों के लिए हम लोग वहीं चबूतरे पर बैठ गये और मन्त्र मुग्ध होकर उस अनुपम सौन्दर्य को देखने लगे।
कितनी शान्ति और सुख था उस मूक सौन्दर्य में मुगलकालीन वैभव की वर्षा करता हुआ वह ताज सहसा ही अपने दर्शनार्थी यात्रियों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
ताज के आन्तरिक भाग का दृश्य देखकर मनुष्य एक क्षण के लिये संसार की क्षणभंगुरता के विषय में सोचने लगता है।
काल न बड़ों को छोड़ता है और न छोटों को सबसे नीचे वाले भाग में प्रेमी और प्रेयसी पास-पास लेटे हुए हैं।
उनके ऊपर यद्यपि कब का आवरण पड़ा हुआ है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो उनमें से शहंशाह शाहजहाँ और उनकी प्रियतमा मुमताज अभी उठकर विहार करने वाले हैं।
भग्न मानव प्रेम की उस समाधि पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। श्वेत संगमरमर पर नाना प्रकार की पच्चीकारियों हो रही हैं, बेल-बूटे बने हुए हैं।
इस कब्र के कक्ष में ऊपर भी एक ऐसा ही कक्ष है, जो सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सुना जाता है कि इनके चारों ओर पहले सुनहरी जालियाँ लगी हुई थीं, परन्तु औरंगजेब ने धन के लोभ में आकर -उन्हें निकलवा लिया और उनके चारों ओर संगमरमर की जालियाँ लगवा दीं।
मीनारों की ऊँचाई कितनी है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु, हाँ, इतना अवश्य है कि उन पर चढ़कर नीचे को देखने से आदमी चिड़िया जैसा दिखाई पड़ता है।
सुना जाता है कि जीवन से निराश, संघर्षों से थके हुए व्यक्ति इन पर चढ़ जाते हैं और नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, इसलिए अब इनके द्वार कभी-कभी ही खोले जाते हैं, प्रायः बन्द ही रहते हैं।
रचना काल
शाहजहाँ ने अपने राज्यकाल में मुमताज बेगम की स्मृति के रूप में इसका निर्माण कराया था। ताज शाहजहाँ की भावभरी भावनाओं का साकार रूप है।
राजकीय कोष का समस्त धन इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया गया। विश्व के समस्त अंचलों से कुशल कलाकार इसके निर्माण के लिए बुलाये गये थे।
तीस हजार मजदूरों द्वारा वर्षों अनवरत परिश्रम का फल ताज आज दर्शकों के नेत्रों को मुग्ध ही नहीं करता अपितु कठोर-से-कठोर हृदय के मुख से संवेदना के रूप में दो शब्द भी सुन लेता है।
इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि इसमें उस समय तीस लाख रुपये व्यय हुए थे।
आधुनिक चमत्कारों में ताज का स्थान
ताजमहल विश्व के आठ आश्चर्यों में से एक होते हुए भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। संसार में और भी बहुत से स्मारक हैं, परन्तु ताज अद्वितीय है।
देश-विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं और इस अनुपम स्मारक की भूरि-भूरि प्रशंसा करके लौटते हैं।1960 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेजीडेन्ट आइजनहाइर और उनके कुछ दिनों के बाद रूस के प्रेसीडेन्ट वोरोशीलोव दिल्ली आये थे, परन्तु वे अपने-अपने देशों से अपने साथ ताज देखने की इच्छा लाये थे, फिर वे कैसे दिल्ली में रहते।
उन्होंने ताजमहल देखा और भूरि-भूरि सराहना की। 2006 में अमेरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश सपत्नीक ताज को देखने की इच्छा का संवरण नहीं कर पाए थे।
जो भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष, उद्योगपति अथवा वैज्ञानिक भारत आते हैं, ताजमहल की एक झलक देखना उनके कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होता है।
इसी भाँति प्रतिवर्ष असंख्य विदेशी पर्यटक इसके दर्शन करके सुख एवं शान्ति का अनुभव करते हैं।
विशेष रूप से शरद पूर्णिमा पर असंख्य जनसुमदाय एकत्रित होता है, कुछ लोग सारी-सारी रात यहाँ मनोविनोद करते हैं और कुछ आधी रात गए चले जाते हैं।
“क्षणे दाणे यन्नवतामुपैति तदेवरूप रमणीयतायाः।”
उपसंहार
श्रेष्ठ सौन्दर्य वही है जो क्षण-क्षण नवीन-सा प्रतीत हो। आज कई सौ वर्ष हो गये, ताज अपने अनन्त सौन्दर्य से आज भी युवा प्रतीत हो रहा है, न उस पर जरा का प्रभाव है और न आँधी-तूफान का सूर्य की उत्तप्त किरणें, न उसके श्वेत शरीर को श्यामल कर सकीं और न उसकी त्वचा में झुर्रियाँ ही डाल सकी।
विश्व को पावन प्रेम का अमर सन्देश देता हुआ, स्नेह की अमरता को अपने हृदय की गहराइयों में छिपाये हुए, मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर मानो अट्टाहास कर रहा हो ।
चन्द्रदेव जब निशा की कोमल पलकों को खोलकर अपनी चाँदनी से धोने लगते हैं तब ताज की मधुर मुस्कान संसार और समाज के प्रहारों से दुःखी और बिछुड़े हुए प्रेमियों को धैर्य और सन्तोष का पाठ पढ़ाती है।
“समय की शिला पर मधुर लेख कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए।”
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
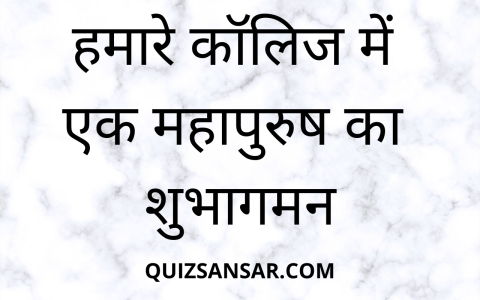
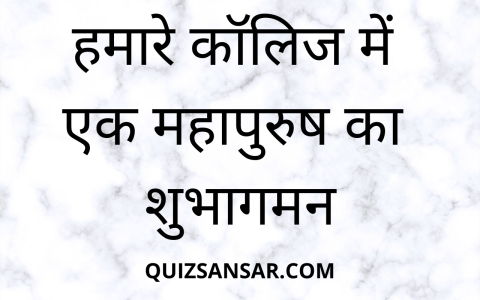
हमारे कॉलिज में एक महापुरुष का शुभागमन
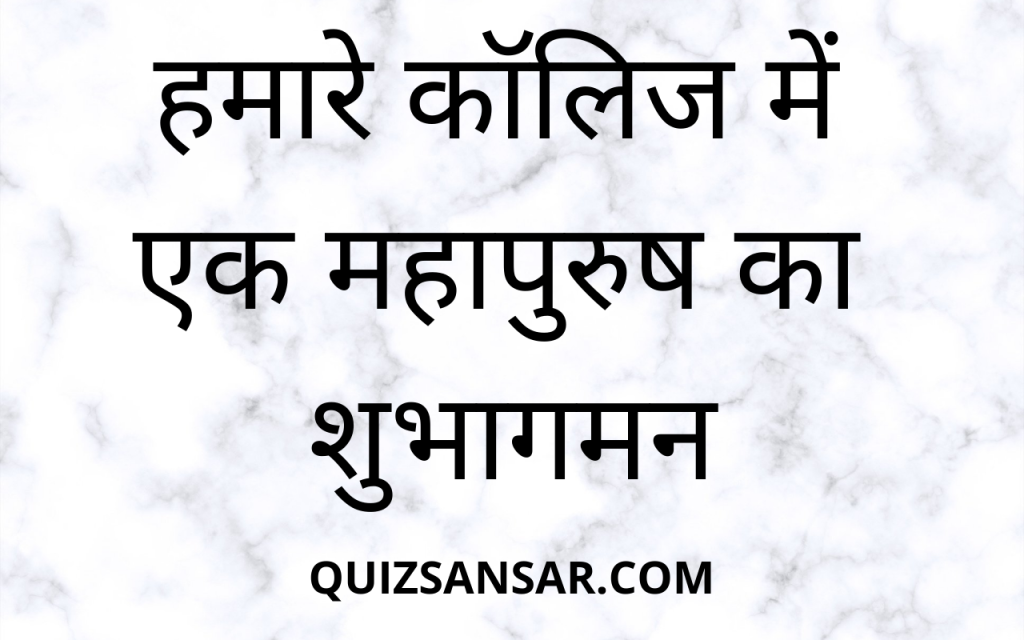
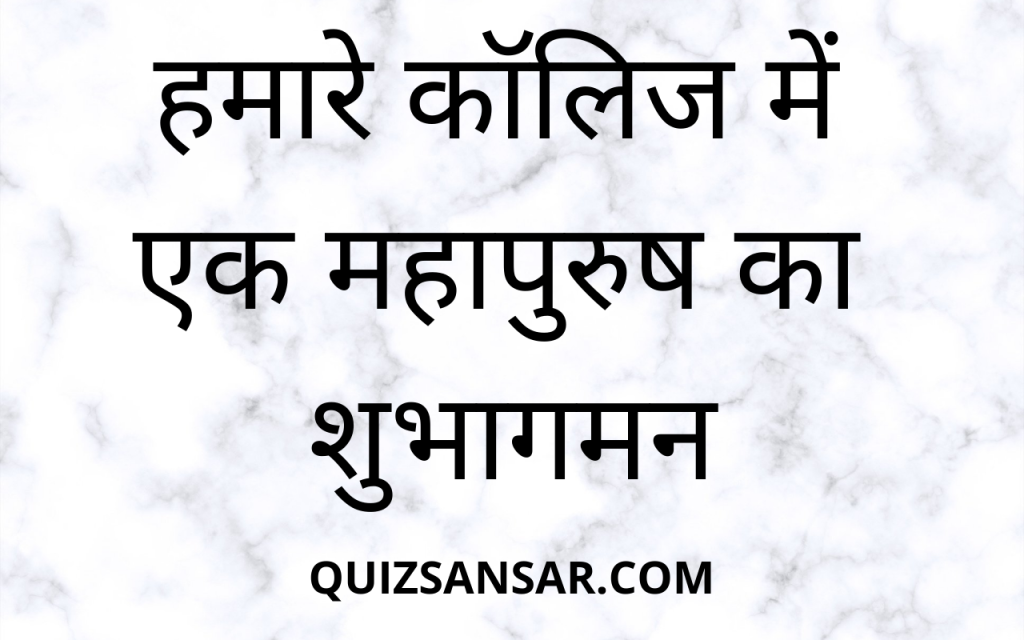
हमारे कॉलिज में एक महापुरुष का शुभागमन
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- स्वागत की तैयारियाँ
- शुभागमन
- अभिनन्दन
- अतिथि महोदय का भाषण
- उपसंहार (प्रस्थान)
प्रस्तावना
कुछ घटनायें मानव जीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं।
सम्भवतः मैं उस दिन को कभी न भूल सकूँगा, जिस दिन भारत के राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम हमारे कॉलिज में आये थे।
विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों का हमारे नगर में एक सम्मेलन होने जा रहा था।
हमारा नगर प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से गंगा किनारे एक सुरम्य स्थान है।
भारत के राष्ट्रपति डॉ० अब्दुल कलाम उसी में भाग लेने के लिये दिल्ली से आ रहे थे।
हमारे प्रधानाचार्य जी ने नगर के प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं हमारे कॉलिज में एक महापुरुष ! से प्रार्थना की कि मिसाइल मैन डॉ॰ कलाम साहब को कुछ क्षणों के लिये कॉलिज में भी यदि ले आया जाये, तो बड़ी कृपा होगी।
कई बार प्रार्थना करने पर नगर के नेताओं ने बात मान ली और कॉलिज के लिये पाँच मिनट का समय कार्यक्रम में निर्धारित कर दिया गया।
स्वागत की तैयारियाँ
केवल दो दिन का समय शेष रह गया था। बहुत सुन्दर ढंग से स्वागत करने का निश्चय किया गया।
कॉलिज के हॉल की तृतिया से पुताई आरम्भ हो गई। दरवाजों और खिड़कियों पर वार्निश होने लगी।
पुताई के पश्चात् जमीन पर फर्श बिछा दिये गये और उन पर अभी नया फर्नीचर आया था,
लगा दिया गया। आगे अतिथियों एवम् महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई।
उनके लिये हत्थे वाली कुर्सियाँ थीं और उनके पीछे कॉलिज के छात्रों के लिये स्टूल थे।
सामने मंच बनाया गया था, काफी ऊँचे दो तख्त थे, जो मिलाकर बिछाये गये थे।
उनके चारों ओर बांस लगाकर ऊपर छत बनाई गई थी।
बासों के ऊपर लाल कपड़ा तथा गोटा लगाया गया था।
मण्डप की छत सुनहरी साड़ियों से सजाई गई थी।
उसमें तरह-तरह के फूलों के गुच्छे लटकाये गये थे, मंच पर बहुत सुन्दर मुगलकालीन कालीनें बिछाई गई थीं
और सलमा सितारों के कामदार तकिये थे।
मंच के पीछे की दीवार पर भारतवर्ष का एक बड़ी मानचित्र लगाया गया,
अन्य दीवारों पर राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सजाये गये और बीच-बीच में तिरंगे झण्डे लगा दिए गये थे।
कॉलिज के मुख्य द्वार पर हरी पत्तियों का बहुत बड़ा द्वार बनाया गया,
जिस पर स्वागतम् और शुभागमन के बोर्ड लगा दिए गए।
दिल्ली से फूल-मालाओं का प्रबन्ध किया गया था।
ढाई सौ फूल-मालायें मँगाई गई थीं।
जिनमें से डेढ़ सौ तो मंच की सजावट में खर्च हो गई थी और भिन्न-भिन्न पुष्पों की सौ मालायें राष्ट्रपति को पहिनाने और कुछ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिये रख ली गई थीं।
शुभागमन
अब वे क्षण कुछ ही दूर थे, जबकि हमारे मान्य अतिथि हमारे मध्य में आने वाले थे। दर्शकों की भीड़ कॉलिज में उमड़ी चली आ रही थी।
चारों ओर सशस्त्र पुलिस लगी हुई थी। सिपाही और दीवानों की तो बात ही क्या, वहाँ थानेदार और डी० एस० पी० घण्टों से ड्यूटी दे रहे थे।
सी० आई० डी० चारों ओर घूम रही थी। खद्दर की टोपियाँ और खद्दर के कुर्ते ही अधिक दिखाई पड़ रहे थे।
गणमान्य नागरिक और आमन्त्रित नेता तथा कॉलिज के छात्र पहले से ही हॉल में बैठा दिए गए थे। द्वार पर केवल स्वागत करने वाले अधिकारी थे।
सभी लोगों की दृष्टि उसी मार्ग पर लगी हुई थी, जिधर से राष्ट्रपति की कार आने वाली थी। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे।
इतने में ही लाल झण्डे वाली मोटर साइकिल दनदनाती हुई आई, जिस पर आगे पायलैट चलता है। चारों ओर शोर मच गया राष्ट्रपति आने वाले हैं।
“दो-तीन मिनट के बाद ही चौदह-पन्द्रह कार एक साथ कॉलिज के द्वार पर आकर रुकीं। एक में डी० एम० थे, दूसरी में एस० पी० कुछ कारों में उत्तर प्रदेश के कुछ मन्त्री थे और कुछ में राष्ट्रपति के निजी व्यक्ति । बीच की कार में से मुस्कुराते हुये राष्ट्रपति बाहर आये।”
“राष्ट्रपति की जय” के गगन भेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उनके स्वागत में धांय-धांय ग्यारह तोपों की सलामी दी गई।
प्रधानाचार्य तथा अन्य गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति जी को पुष्पहार पहनाये। कमरों के ऊपर से छात्रों ने पुष्प वर्षा की।
एन० सी० सी० और पी० ई० सी० के छात्र सैनिकों का निरीक्षण करते हुये राष्ट्रपति जी सीधे मंच की ओर पहुंचे राष्ट्रपति जी बहुत तीव्र गति से चल रहे थे।
उनके शरीर में स्फूर्ति थी, मुख-मण्डल तेजोमय था।
अंगरक्षक पीछे खड़े रह गए और राष्ट्रपति जी भीड़ को चीरते हुए तेजी से मंच पर पहुंचे। मुस्कुराते हुए उन्होंने सबको नमस्कार किया।
अभिनन्दन
प्रधानाचार्य जी ने एक सूक्ष्म भाषण में राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन किया,
फिर कॉलिज के विद्यार्थी परिषद के मन्त्री ने अभिवादन पत्र पढ़कर सुनाया और राष्ट्रपति जी को सादर भेंट किया।
अतिथी महोदय का भाषण
अभिनन्दन-पत्र भेंट किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति जी भाषण देने के लिये खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा।
फिर एकदम पूर्ण शान्ति हो गई। चारों ओर हॉल के भीतर तथा बाहर माइक का प्रबन्ध था। सर्वप्रथम उन्होंने हमारे द्वारा किए गये स्वागत का धन्यवाद दिया।
अपने सारगर्भित भाषण में पहले तो छात्रों के कर्तव्य और अनुशासन पर प्रकाश डाला। स्वतन्त्रता संग्राम में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों को प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का भावी नागरिक है। हम लोग सदैव शासन को नहीं चलाते रहेंगे। विद्यार्थी के लिए सच्चरित्रता बहुत आवश्यक है।
इस तरह उन्होंने हम लोगों के समक्ष लगभग दस मिनट तक भाषण दिया। भाषण समाप्त होते ही हॉल में एक बार तालियों का सामूहिक स्वर गूंज उठा।
मंच से उन्होंने सबको फिर नमस्कार किया और तेजी से चल दिये। मैंने देखा कि राष्ट्रपति जी को न पुलिस चाहिये थी और न स्वयं सेवक।
उनको सामने देखकर भीड़ रवयं हट जाती थी। भीड़ में कितनी ही गड़बड़ी हो वे स्वयं ही झगड़ा दूर करते चले जाते थे।
उन्हें न कोई भय था और न संकोच। भौड़ को पार करते हुए वे सीधे अपनी कार तक पहुंचे। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जनता हाथ बाँधे खड़ी थी।
उन्होंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और गाड़ी में बैठ गये। सर-सर करती हुई सभी कारें एक के पीछे एक चलने लगो, देखते-देखते कार हमारी दृष्टि से ओझल हो गई।
दर्शनार्थियों की भीड़ अपने-अपने घर जाने लगी। राष्ट्रपति जी के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का मेरे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ा।
उनका श्याम वर्ण, उनके उन्नत ललाट, दूर दिशा में अनावत को झाँकती हुई आँखें और गम्भीर मुद्रा, मुझे सदैव स्मरण रहेगी।
मैंने यह अनुभव किया कि उनकी वाणी में कोई जादू था। जनता मंत्रमुग्ध होकर उनके एक-एक वाक्य को वेद वाक्य के समान सुनती थी।
उस पर विचार करती थी। उनके ओजस्वी एवम् सारगर्भित भाषण | को एक-एक पंक्ति विद्वानों और कूटनीतिज्ञों के मनन का विषय हो जाती है।
उपसंहार
राष्ट्रपति जी का तपोमय जीवन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिये एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। उनका शान्ति और अहिंसा का संदेश विश्व के कोने कोने में गूंज रहा है।
यह हमारे कॉलिज का सौभाग्य था कि उन जैसे महापुरुष ने हमारे यहाँ पधारने की कृपा की।
उनके मुख से निकले हुये महत्त्वपूर्ण शब्दों का आज तक मेरे हृदय पर प्रभाव है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
महत्वपूर्ण
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi
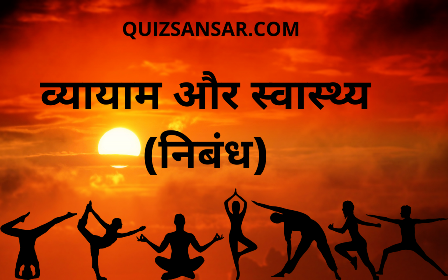
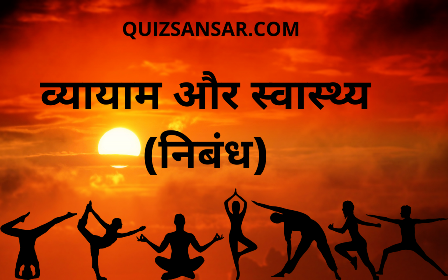
व्यायाम और स्वास्थ्य
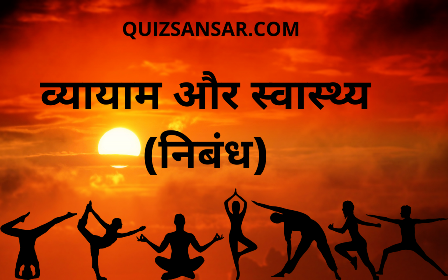
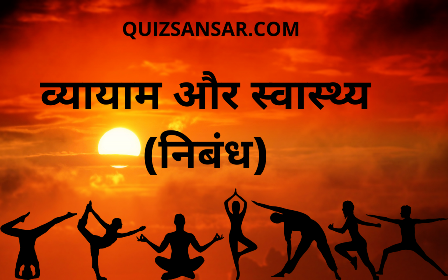
व्यायाम और स्वास्थ्य पर निबंध निम्नलिखित है |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- स्वास्थ्य रक्षा के साधन और व्यायाम
- व्यायाम के भेद
- व्यायाम से लाभ
- व्यायाम की उचित विधि
- उपसंहार
प्रस्तावना
“धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् “
महर्षि चरक ने लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों का मूल आधार स्वास्थ्य हो हैं। यह बात अपने में नितान्त सत्य है।
मानव जीवन की सफलता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में ही निहित है, परन्तु सबकी आधारशिला मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसका निरोग जीवन है।
रुग्ण और अस्वस्थ मनुष्य न धर्म चिन्तन कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, न काम प्राप्त कर सकता है, और न मानव जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, मोक्ष की ही उपलब्धि कर सकता है क्योंकि इन सबका मूल आधार शरीर है, इसलिये कहा गया है कि-
“शरीरमाद्यम् खलु धर्मसाधनम् ।”
अस्वस्थ व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकता है, न अपने परिवार का न अपने समाज की उन्नति कर सकता है और न देश की।
जिस देश के व्यक्ति अस्वस्थ और अशक्त होते हैं, वह व्यायाम और स्वास्थ्य , देश न आर्थिक उन्नति कर सकता है और न सामाजिक ।
देश का निर्माण, देश की उन्नति, बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा, देश का समृद्धिशाली होना वहाँ के २. स्वास्थ्य रक्षा के साधन और नागरिकों पर निर्भर होता है।
सभ्य और अच्छा नागरिक वही हो सकता है, जो तन, मन, धन से देशभक्त हो । और मानसिक और आत्मिक दशा में उन्नत हो ।
इन दोनों ही क्रमों में शरीर का स्थान प्रथम है। बिना शारीरिक उन्नति के मनुष्य न देश की रक्षा कर सकता है और न अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है।
अस्वस्थ विद्यार्थी कभी श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं हो सकता, अस्वस्थ अध्यापक कभी आदर्श अध्यापक नहीं हो सकता, अस्वस्थ व्यापारी का व्यापार कभी समुन्नत नहीं हो सकता, अस्वस्थ वकील भी अच्छी बहस नहीं कर सकता, अस्वस्थ नौकर कभी यथोचित स्वामी सेवा नहीं कर सकता, अस्वस्थ स्त्री कभी आदर्श गृहिणी नहीं हो सकती, अस्वस्थ संन्यासी कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, अस्वस्थ नेता व भी देश की बागडोर मजबूती से अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता।
अतः स्वास्थ्य प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिये महत्त्वपूर्ण वस्तु है।
अंग्रेजी में कहावत है “Health is Wealth” अर्थात् स्वास्थ्य ही धन है।
स्वास्थ्य रक्षा के साधन और व्यायाम
स्वास्थ्य रक्षा के लिये विद्वानों ने वैद्यों ने और शारीरिक विज्ञान-वेत्ताओं ने अनेक साधन बताये हैं, जैसे- सन्तुलित भोजन, पौष्टिक पदार्थों का सेवन, शुद्ध जलवायु का सेवन, परिभ्रमण, संयम-नियम पूर्ण जीवन, स्वच्छता, विवेकशीलता, पवित्र भाषण, व्यायाम, निश्चिन्तता इत्यादि।
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साधन स्वास्थ्य को समुन्नत करने के लिए रामबाण की तरह अमोघ हैं परन्तु इन सबका ‘गुरु’ व्यायाम है।
व्यायाम के अभाव में स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक पदार्थ विष का काम करते हैं।
व्यायाम के अभाव में केवल पवित्र आचरण या विवेकशीलता भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तब आप विवेकशील हो ही नहीं।
सकते क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर अस्वस्थ होने पर मस्तिष्क स्वस्थ रह ही नहीं सकता।
ज्ञान, बुद्धि, विवेक, परिमार्जित मस्तिष्क, ये सब स्वास्थ्य की ही देन होती हैं।
अस्वस्थ व्यक्ति अविवेकी, विचारशून्य, मूर्ख, आलसी, अकर्मण्य, हठी, क्रोधी, झगड़ालू आदि सभी दुर्गुणों का भण्डार होता है। स्वास्थ्य का मूल मन्त्र व्यायाम है-
“व्यायामान्पुष्ट गात्राणी”
व्यायाम के भेद
अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ तथा शास्त्रीय गहन विचारों में उलझा हुआ प्रोफेसर, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह क्या कर रहा है।
आप कहेंगे कि वह पढ़ाने के लिये पढ़ रहा है या भाषण देने के लिये पढ़ रहा है या अपने ज्ञान-वर्धन के लिये पढ़ रहा है।
परन्तु आप समझ लीजिये कि वह पढ़ने के साथ-साथ व्यायाम भी कर रहा है। व्यायाम केवल दण्ड-बैठक करना ही नहीं होता, पुस्तक पढ़ना भी व्यायाम होता है।
इस व्यायाम को बौद्धिक व्यायाम कहते हैं। इससे मस्तिष्क के पुर्जों में शक्ति आती है और वे पुष्ट हो जाते हैं। इस व्यायाम से मनुष्य महान् विचारक और ज्ञानवान बन जाता है।
दूसरा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हैं, शरीर बलवान बन जाता है और मनुष्य तेजस्वी दिखाई पड़ने लगता है।
शारीरिक व्यायाम में वे सभी क्रियायें आ जाती हैं, जिनसे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं। कोई प्रातःकाल खुली हवा में दौड़ लगाना पसन्द करता है, तो कोई बन्द कमरे में तेल मालिश करके दण्ड और बैठक करना।
कोई जीन कसे हुए घोड़े पर सवार होकर सपाटे भरना पसन्द करता है, तो कोई नदी के शीतल जल में हाथ-पैर उछाल कर और श्वांस रोक कर तैरना कोई अखाड़े में कुश्ती लड़ना पसन्द करता है, तो कोई मुग्दर घुमाकर घर आ जाता है।
कोई ऊँची कूद कूदता है, तो कोई लम्बी कूद | कोई लाठी चलाने का अभ्यास करता है, तो कोई तीर चलाकर निशाना लगाने का।
कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की सभी क्रियायें, जिनमें शरीर के अंग पुष्ट होते हों, व्यायाम के अन्तर्गत आ जाती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल भी एक प्रकार का व्यायाम ही हैं।
उनसे भी खिलाड़ी का शरीर पुष्ट होता हैं, और छाती चौड़ी होती है। कबड्डी, रस्साकशी, मलखम्भ आदि भारतीय खेल हैं।
फुटबाल, बालीबॉल, हॉकी, टैनिस, बैंडमिन्टन, स्केटिंग आदि पाश्चात्य खेल हैं। स्त्रियों के लिये सर्वश्रेष्ठ व्यायाम चक्की चलाना है, जिससे आजकल की स्त्रियाँ कोर्सों दूर भागती हैं और ऐसी बातों को दकियानूसी ख्याल बताती हैं।
यही कारण है कि आजकल की स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है और पीली पड़ी रहती हैं।
आज के युग में योगासनों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी योग आसनों को बड़े चाव से और मन से अपनाय जा रहा है।
इनसे दो लाभ होते हैं। एक तो शरीर की माँसपेशियाँ पुष्ट होती हैं, दूसरे मानव को ध्यानावस्थित होकर मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है।
धनुरासन, हलासन, सर्वांगासन, पदमासन आदि ऐसे आसन हैं जिनसे मानसिक शक्ति तो पुष्ट होती ही है साथ ही शरीर भी पुष्ट होता है।
इन सब योगासनों में प्राणायाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
व्यायाम से लाभ
व्यायाम से मनुष्य को असंख्य लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह वृद्धावस्था में भी जीर्ण नहीं होता और दीर्घजीवी होता है।
जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं घेरता, अन्तिम समय तक शरीर में शक्ति बनी रहती है।
आजकल तो 20-22 साल के बाद ही शरीर और मुँह की खाल पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और मनुष्य वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगता है।
व्यायाम करने से हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती हैं। भोजन पचने के बाद ही वह रक्त, मज्जा, माँस आदि में परिवर्तित होता है।
शरीर में रक्तसंचार हमारे जीवन के लिये परम आवश्यक है। व्यायाम से शरीर में रक्तसंचार नियमित रहता है।
इससे शरीर और मस्तिष्क पुष्ट होते हैं। व्यायाम से मनुष्य का शरीर सुगठित और स्फूर्ति सम्पन्न होता है।
मनुष्य में आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता और वीरता आदि गुणों का आविर्भाव होता है।
“वीरभोग्या वसुन्धरा”
वसुन्धरा सदा वीर व्यक्तियों द्वारा भोगी जाती है, यह एक प्राचीन सिद्धान्त है। जिसमें शक्ति होती है, समाज उसका आदर करता है, उसका अनुगमन करता है।
यह शक्ति व्यायाम द्वारा ही मनुष्य प्राप्त करता है। प्राचीन भारतवर्ष में राजपूत बालकों को विद्याध्ययन के लिये गुरुकुल में भेजा जाता था, जहाँ वे महर्षियों द्वारा शास्त्रीय ज्ञान और आचार-विचार की शिक्षा प्राप्त करते थे. राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन करते थे, परन्तु इसके साथ उन्हें मल्ल-विद्या का भी अध्ययन कराया जाता था।
व्यायाम की विधिवत् शिक्षा दी जाती थी। तभी वे शत्रुओं को मुँह तोड़ उत्तर देने में समर्थ होते थे। उस समय भारतवर्ष एक शक्ति सम्पन्न और वीरों का देश समझा जाता था।
अन्य देशों के नर-नारी यहाँ के वीर पुरुषों का कीर्तिगान करके अपने बच्चों को भी वैसा हो बनने के लिये प्रेरित करते थे।
यह “वीरों का देश” अपनी शक्ति पर गर्व करता था और उस शक्ति का मूल स्रोत था दैनिक व्यायाम।
व्यायाम की उचित विधि
व्यायाम का उचित समय प्रातःकाल और सायंकाल होता है। प्रायः शौच-इत्यादि से निवृत्त होकर, बिना कुछ खाये, शरीर पर थोड़ी तेल मालिश करके व्यायाम करना चाहिये।
व्यायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शरीर के सभी अंग-प्रत्यगों का व्यायाम हो, शरीर के कुछ ही अंगों पर जोर पड़ने से वे पुष्ट हो जाते हैं, परन्तु अन्य अंग कमजोर ही बने रहते हैं।
इस तरह शरीर बैडोल हो जाता है। व्यायाम करते समय जब श्वांस फूलने लगे तो व्यायाम करना बन्द कर देना चाहिये, अन्यथा शरीर की नसें टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर कुरूप लगने लगता है, जैसा कि अधिकांश पहलवानों में देखा जाता है किसी को टाँगें टेढ़ी तो किसी के कान व्यायाम करते समय मुँह से श्वांस कभी नहीं लेना चाहिये सदैव नासिका से श्वांस लेनी चाहिये।
व्यायाम के लिये उचित स्थान वह है, जहाँ शुद्ध वायु और प्रकाश हो और स्थान खुला हुआ हो, क्योंकि फेफड़ों में शुद्ध वायु आने से उनमें शक्ति आती है, एक नवीन स्फूर्ति आती है और उनकी अशुद्ध वायु बाहर निकलती है।
व्यायाम के पश्चात् कभी नहीं नहाना चाहिये, अन्यथा गठिया होने का भय होता है। व्यायाम के पश्चात् फिर थोड़ा तेल मालिश करनी चाहिये, जिससे शरीर की थकान दूर हो जाए।
फिर प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध वायु में कुछ समय तक विश्राम और विचरण करना चाहिये। जब शरीर का पसीना सूख जाये और शरीर की थकान दूर हो जाए तब स्नान करना चाहिये।
इसके पश्चात् दूध आदि कुछ पौष्टिक पदार्थों का सेवन परम आवश्यक है। बिना पौष्टिक पदार्थों के व्यायाम से अधिक लाभ नहीं होता।
व्यायाम का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। यदि प्रथम दिन ही आपने सौ दण्ड और सौ बैठकें कर ली तो आप दूसरे दिन खाट से उठ भी नहीं सकेंगे लाभ के स्थान पर हानि होने की ही सम्भावना अधिक होगी।
उपसंहार
आज देश में वीरता का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे नवयुवक बुरी तरह विफल होते हैं।
पदक तालिका में अपना स्थान पाने के लिए तरसते हैं। कारण संतान निस्तेज उत्पन्न होती है और जीवन भर निस्तेज ही बनी रहती है।
इसका मुख्य कारण बच्चों के माता-पिता में शारीरिक शक्ति का अभाव है। आज उनमें अपने पूर्वजों का-सा पराक्रम न शौर्य, न धीरता है और न वीरता। इसका कारण है कि हम पंगु और अकर्मण्य हो गये, शरीर से परिश्रम लेने का काम हमने छोड़ दिया।
आज के युग में घी, दूध तो प्रायः समाप्त हो गया। इतने पर भी शरीर सुचारू रूप से चलता रहे तथा जीवन यात्रा में कोई भयानक विघ्न उपस्थित हो, इसलिये थोड़ा-सा व्यायाम कर लेना परम आवश्यक है।
जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है और स्वास्थ्य व्यायाम पर। स्वस्थ व्यक्ति कभी पराश्रित या दुःखी नहीं रह सकता, वा जो काम चाहे कर सकता है।
अतः हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस स्वास्थ्य रूपी धन को व्यर्थ है नष्ट न करें, जिससे हमें जीवन भर पश्चात्ताप की अग्नि में न जलना पड़े।
प्राण रूपी पक्षी शरीर रूपी पिंजड़े में सुरक्षित रखने के लिये स्वास्थ्य रूपी मजबूत सींकचों की आवश्यकता जीवन में प्रसन्नता के लिये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिये व्यायाम नितान्त आवश्यक है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
- मानवकृत तन्तु रेयॉन का इतिहास | History of Humanized Fiber Rayon in Hindi
- ऊन की भौतिक एवं रासायनिक विशेषतायें
- सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- TOP 10 best portable folding washing machines under 2000
- Top 10 best selling earbuds under 2000 | Amazing Deal at Amazon
- AFFORDABLE MAKEUP PRODUCTS | MAKEUP PRODUCTS STARTING JUST RS.300
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त | Principles of Curriculum Construction in Hindi
- पाठ्यचर्या का चयन | Selection of Curriculum in Hindi


आदर्श मित्र पर निबंध


आदर्श मित्र पर निबंध व आदर्श मित्र के कर्तव्य निम्नलिखित है |
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- मित्र के कर्तव्य
- आज के मित्र
- उपसंहार
प्रस्तावना
“एकाकी बादल रो देते, एकाकी रवि जलते रहते ।”
वास्तव में जीवन में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मनुष्य कभी-कभी आत्महत्या तक करने को उतारू हो जाता है।
सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में रहना चाहता है, भावनाओं का आदान-प्रदान करना चाहता है, अपने सुख-दुःख का साथी बनाना चाहता है।
परिवार में सभी सम्बन्धी होने पर भी उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे दिल खोलकर वह सब बातें कर सके।
परिवार के सदस्यों की भी कुछ सीमायें होती हैं।
कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो केवल पिताजी से कही जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं,
जिन्हें केवल माता जी से ही कह सकते हैं, कुछ बातें भाई-बहनों को भी बताई जाती हैं, कुछ बातों में पत्नी से परामर्श लिया जाता है,
और कुछ बातों में घर के अन्य वयोवृद्ध सदस्यों से।
परन्तु वे आदर्श मित्र सभी बातें चाहे अच्छी हों या बुरी, गुण की हो या अवगुण की,
हित की हों या अहित की, कल्याण की। हों या विनाश की, उत्थान की हों या पतन की,
उत्कर्ष की हों या अपकर्ष की, यदि किसी से जी खोलकर कही जा सकती हैं तो केवल मित्र से।
मित्र के अभाव में मनुष्य कुछ खोया खोया सा अनुभव करता है, किससे अपने सुख-दुःख की कहे, किसके सामने वह अपने रखना, हृदय की गठरी को खोले ?
अपने मनोविनोद और हास-परिहास के समय को वह किसके साथ बिताए विपत्ति के समय वह किसकी सहायता ले, सत्परामर्श: ले और सहानुभूति प्राप्त करे ? अपनी रक्षा का भार वह किसे सौंप ?
क्योंकि मित्र की रक्षा, उन्नति, उत्थान सभी कुछ एक सच्चे मित्र का दायित्व होते हैं
“कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्षमणि ।
अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते ॥ “
अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य के दोनों हाथ शरीर की अनवरत रक्षा करते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती और न कभी शरीर ही कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर गिरूँ तब तुम आगे आ जाना और बचा लेना;
परन्तु वे एक सच्चे मित्र की भाँति सदैव शरीर की रक्षा में संलग्न रह हैं।
इसी प्रकार आप पलकों को भी देखिए, नेत्रों में एक भी धूलि का कण चला जाए, पलकें तुरन्त बन्द हो जाती हैं।
हर विपत्ति से अपने नेत्रों को बचाती हैं। इसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी बिना कुछ कहे-सुने मित्र का सदैव हित-चिन्तन किया करता है
मित्र के कर्तव्य
मित्र के अनेक कर्त्तव्य होते हैं जिनमें से केवल कुछ प्रमुख कर्त्तव्यों पर नीचे विचार किया जायेगा।-
सन्मार्ग पर चलना
एक सच्चा मित्र सदैव अपने साथी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वह कभी नहीं देख सकता कि उसकी आँखों के सामने ही उसके मित्र का घर बर्बाद होता रहे, उसका साथी पतन के पथ पर अग्रसर होता रहे, कुवासनायें और दुर्व्यसन उसे अपना शिकार बनाते रहें, कुरीतियाँ उसका शोषण करती रहें, कुविचार उसे कुमार्गगामी बनाते रहे।
वह उसे समझा-बुझाकर, लाड़ से, प्यार से और फिर, प्यार से और मार से किसी-न-किसी तरह उसे उस मार्ग को छोड़ने के लिये विवश कर देगा।
तुलसीदास ने मित्र की जहाँ और पहचान बताई है वहाँ एक यह भी है-
“कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा।
गुण प्रगटहि अवगुणहिं दुरावा ॥”
तात्पर्य यह है कि यदि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं या हममें इसी प्रकार की और बुरी आदतें हैं, तो एक श्रेष्ठ मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, हमें अपने दोषों के प्रति जागरूक कर दे तथा उनको दूर करने का निरन्तर प्रयास करता रहे।
विपत्ती में सहायता
जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति के काले बादल घनीभूत अन्धकार के समान छा जाते हैं और चारों दिशाओं में निराशा के अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब केवल सच्चा मित्र ही एक आशा की किरण के रूप में सामने आता है।
तन से, मन से, धन से वह मित्र की सहायता करता है और विपत्ति के गहन गर्त में डूबते हुए अपने मित्र को निकालकर बाहर ले आता हैं।
रहीम ने लिखा है-
“रहिमन सोई मीत हैं, भीर परे ठहराई।
मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाई ॥”
मित्रता होनी चाहिये मीन और नीर जैसी। सरोवर में जब तक जल रहा; मछलियाँ भी क्रीड़ा तथा मनोविनोद करती रहीं: परन्तु जैसे जैसे तालाब के पानी पर विपत्ति आनी आरम्भ हुई; मछलियाँ उदास रहने लगीं, जल का अन्त तक साथ नहीं छोड़ा उसके साथ संघर्ष में रत रहीं, और जब मित्र न रहा, तो स्वयं भी अपने प्राण त्याग दिये, परन्तु अपने साथी जल का अन्त तक विपत्ति में भी साथ न छोड़ा।
मित्रता दूध और जल की-सी नहीं होनी चाहिये कि जब दूध पर विपत्ति आई और वह जलने लगा तो पानी अपना एक ओर को किनारा कर गया, अर्थात् भाप बनकर भाग गया, बेचारा अकेला दूध अन्तिम क्षण तक जलता रहा।
स्वार्थी मित्र सदैव विश्वासघात करता है, उसकी मित्रता सदैव पुष्प और भ्रमर जैसी होती है। भंवरा जिस तरह रस रहते हुये फूल का साथी बना रहता है और इसके अभाव में उसकी ओर देखता तक नहीं।
इसी प्रकार स्वार्थी मित्र भी विपत्ति के क्षणों में मित्र का सहायक सिद्ध नहीं होता। इसलिये तुलसीदास जी ने अच्छे मित्र की कसौटी विपत्ति ही बताई है –
“धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपति काल परख यहि चारी।
जे न मित्र दुःख होंहि दुःखारी। तिनहिं विलोकत पातक भारी ॥ “
अंग्रेजी में कहा गया है “A friend in need is a friend indeed.” संस्कृत में कहा गया है कि “आपदगतं च न जहाति ददाति काले” अर्थात् विपत्ति के समय सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ता, अपितु सहायता के रूप में कुछ देता ही है।
जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा सर्वप्रथम कसौटी पर घिसने से होती है, उसी प्रकार मित्र की विपत्ति के समय त्याग से होती है।
इतिहास साक्षी है कि ऐसे मित्र हुये हैं, जिन्होंने अपने मित्र की रक्षा में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी।
गुणों को प्रकट करना
मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के गुणों को प्रकाशित करे जिससे कि मित्र का समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़े।
सच्चा मित्र अपने मित्र के मान को अपना ही मान समझता है, उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति को अपनी प्रतिष्ठा और ख्याति समझता है।
इसीलिये वह अपने मित्र के गुणों का नगाड़े की चोट पर गान करता है और अवगुणों को छुपाने का प्रयत्न करता है।
साथ-साथ उन अवगुणों को दूर करने का भी प्रयास करता है। उसकी “छिद्रान्वेषण-प्रकृति” नहीं होती, अर्थात् वह अपने मित्र की कमियों को ढूंढकर प्रकाश में लाने का प्रयास नहीं करता।
वह जानता है कि इससे मेरे मित्र का समाज में अपमान और अपयश होगा। तुलसीदास जी कहते हैं-
“गुण प्रकटहिं अवगुणहिं दुरावा”
अथवा
“गुह्यानि गृहाति गुणान् प्रकटीकरोति ।“
सदैव सहयोग और सहानुभूति रखना
जीवन का कोई भी क्षेत्र हो कोई भी कार्य या व्यापार हो, किसी भी प्रकार की सम या विषम परिस्थिति हो, मित्र को अपने मित्र के साथ सहानुभूति रखनी चाहिये और उसके साथ सहयोग भी बनाये रखना चाहिये।
भले ही मित्र न कुछ दे और न ले, परन्तु सहानुभूति एक ऐसी वस्तु है, जिससे मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों को भी हँसते हँसते झेल लेता है, विपत्तियों में भी मुस्कुरा देता है।
सहानुभूति और संवेदना के अभाव में मानव का जीवन एक नैराश्यपूर्ण नारकीय जीवन बन जाता है, और जीवन भार मालूम पड़ने लगता है। गुप्त जी ने लिखा है-
“सहानुभूति चाहिए महा विभूति है यही ॥ “
निःस्वार्थ हितचिंतन
निःस्वार्थ हित-चिन्तन करना कोई साधारण बात नहीं है। पत्नी पति का, माता पुत्र का पिता पुत्र का हित-चिन्तन करते हैं परन्तु उस हित-चिन्तन में स्वार्थ की कोई न कोई कोर हृदय के किसी-न कोने में छिपी रहती ।
प्रत्येक सम्बन्धी परिवार का प्रत्येक सदस्य आपका हित चिन्तन अवश्य करेगा, परन्तु बदले में अवश्य कुछ चाहेगा, लेकिन सच्चा मित्र जो कुछ करेगा उसका बदला नहीं चाहेगा।
वह तो यहीं कहेगा- मैंने ऐसा किया, क्यों किया? क्योंकि मेरा कर्तव्य था।
आज के मित्र
आज के अधिकांश मित्रों को मित्र कहने की अपेक्षा यदि शत्रु कहा जाये तो अधिक उचित होगा।
साधारणतः आज का मित्र स्वार्थी है, वह आपके सामने मीठा बना रहकर आपका जितना भी अहित चिन्तन कर सकता है, करता है।
जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि, उसकी वासनाओं की शान्ति, उसकी तृष्णा की पूर्ति, आपके द्वारा होती है, तब तक वह आपके साथ आपका सहयोगी है, आपसे सहानुभूति रखता है, आपका प्रशसंक है और जहाँ उसको स्वार्थपूर्ति हुई या उस पूर्ति में, कोई विघ्न दिखाई पड़ा, वह आपके पास फटकता भी नहीं।
ऐसे मित्रों को यदि “चापलूस शत्रु” की संज्ञा दी जाये, तो कहीं अच्छा होगा। ऐसे भी प्रमाण हैं कि आज तक यदि किसी वीर की मृत्यु हुई या वह बन्धन में फँसा, तो वह मित्र के ही द्वारा बड़े-बड़े क्रान्तिकारी विदेशियों को पकड़ में आये, परन्तु केवल अपने मित्रों की कृपा के फलस्वरूप हो।
उर्दू का एक शेर है, जो इसी प्रसंग पर प्रकाश डालता है-
“खाके जो तीर देखा कमीगाह की तरफ।
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई । “
कमीगाह उस स्थान को कहते हैं, जहाँ से छुपकर तीर चलाया जाता है। पीछे से किसी ने तीर चलाया, पीठ में आकर लगा भी, दर्द हुआ, पीछे मुड़कर कमीगाह की तरफ जब देखा, तो वहाँ कोई अपना ही दोस्त बैठा हुआ यह तीरंदाजी करते दिखाई पड़ा।
आज के मित्रों का चित्रण इस उर्दू के शेर से अधिक और क्या हो सकता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज के युग में देखना एक कल्पना मात्र है।
आज तो ऐसे मित्र हैं कि मुख पर कहेंगे कि आप अच्छे आदमी हैं, आप जैसे मित्र को पाकर मैं सौभाग्यशाली हूँ और जहाँ पीठ मुड़ी और कोई दूसरा मिला तो कहने लगे, देखो – एक नम्बर बदमाश है, पचासों बदमाशियाँ तो इसकी मेरी डायरी में नोट हो रही हैं, आने दो कभी मौका, ऐसे हाथ लगाऊँगा कि याद रहे।
इसलिये संस्कृत में एक विद्वान् ने लिखा है
“परीक्षे कार्यहन्तारं, सन्मुखे प्रियवादिनम् ।
वर्जयेत् तादृशं मित्रं, विषकुम्भं पयोमुखम् ॥
अर्थात् जो सामने मीठा बोलता है और पीछे काम बिगाड़ता है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिये।
वह मित्र इस प्रकार है, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े के मुख पर दूध लगा दिया गया हो। गोस्वामी जी के शब्दों में-
“विषरस भरा कनक घट जैसे।”
उपसंहार
मित्र को सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और सहनशील होना चाहिये। यदि दो मित्रों में सहनशीलता नहीं है, तो मित्रता अधिक समय तक नहीं चल सकती।
इसलिये चिरस्थायी मैत्री के लिये सहनशीलता परम आवश्यक है। श्रेष्ठ मित्र के क्या लक्षण हैं इसको भर्तृहरि ने एक श्लोक में लिख दिया है-
“पापन्निवारयति योजयते हिताय,
गुह्यानि गृहति, गुणान् प्रगटीकरोति ।
आपदरतं च न जहाति ददाति काले,
सन्मित्रलक्षणमिदम् प्रवदन्ति सन्तः ॥ “
अर्थात् जो बुरे मार्ग पर चलने से रोकता है, हितकारी कामों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है तथा गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता तथा समय पड़ने पर कुछ देता है, विद्वान् इन्हीं गुणों को श्रेष्ठ मित्र के लक्षण बताते हैं।
हमारी दृष्टि में इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने मित्र के कर्त्तव्यों के विषय में सब कुछ कह दिया है।
मित्र को, यदि वह मैत्री सम्बन्धों में स्थायित्व चाहता है, ध्यान रखना चाहिये कि वह मित्र से कभी वाणी का विवाद न करे, पैसे का सम्बन्ध भी अधिक न करे तथा मित्र की पत्नी से कभी परोक्ष में सम्भाषण न करे, अन्यथा मैत्री सम्बन्ध चिरस्थायी नहीं रह सकते, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है-
“यदीच्छेत् विपुलां प्रीति, त्रीणि तत्र न कारयेत् ।
बाग्विवादोऽर्थ सम्बन्धः एकान्ते दारभाषणम् ॥”
इस संदर्भ में महाकवि बिहारी की उक्ति भी प्रशंसनीय है-
“जो चाहो चटक न घंटै मैलो होय न मित्त ।
रज राजसु न छुवाइए नेह चीकने चित्त ॥”
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं |
IMPORTANT


