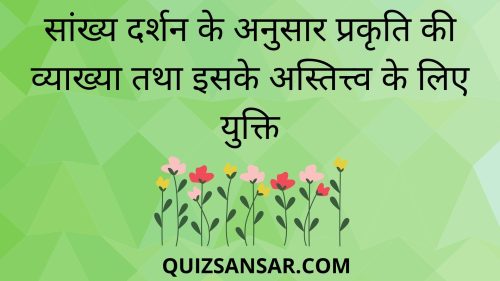
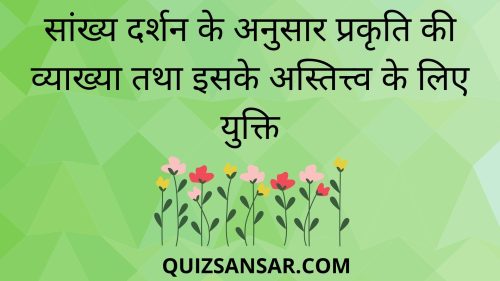
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति


नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की व्याख्या तथा इसके अस्तित्त्व के लिए युक्ति उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
सांख्य दर्शन की द्वैतवादी विचारधारा में पुरुष के अतिरिक्त द्वितीय तत्त्व अव्यक्त या प्रकृति है। यह इस विश्व का मूल कारण है। सम्पूर्ण विविधताओं से परिपूर्ण यह जगत् प्रकृति से ही उत्पन्न है।
“सांख्य दर्शन विश्व के मूल कारण की खोज के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करता है।“
सांख्य दार्शनिकों की मान्यता है कि विश्व में दो प्रकार की वस्तुएँ दिखाई देती है स्थूल पदार्थ (मिट्टी, जल, वृक्ष, पहाड़, भौतिक शरीर आदि) तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ (बुद्धि, इन्द्रिय, मन, अहंकार आदि)। विश्व का मूल कारण केवल वही तत्व हो सकता है जो स्थूल पदार्थों को उत्पन्न करने के साथ सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों को भी उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। सांख्य दर्शन के अनुसार चैतन्यस्वरूप पुरुष इस विश्व का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह कारण कार्य श्रृंखला से परे वह न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य। अत: कोई अचेतन तत्व ही इस जगत का कारण हो सकता है। सांख्य दर्शन इस प्रसंग में चार्वाक, जैन, बौद्ध एवं न्याय-वैशेषिक दर्शन की उस मान्यता को भी अस्वीकार करता है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु महाभूतों को अथवा उनके परमाणुओं को इस विश्व का कारण स्वीकार किया जाता है। उसके अनुसार इन परमाणुओं से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति सम्भव है, किन्तु इनसे मन, बुद्धि आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार का मूलभूत कारण केवल वही तत्त्व हो सकता है जो स्थूल और सूक्ष्म, दोनों प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न कर सके। सांख्य दर्शन विश्व के इस मूल कारण को प्रकृति या अध्यक्त अथवा प्रधान कहता है। यह प्रकृति पुरुष का विरुद्धधर्मी है। यह चेतनस्वरूप, त्रिगुणातीत एवं उदासीन पुरुष के विपरीत है।
“सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है।“
इसमें तीन गुण पाये जाते हैं। ये गुण स, रज और तमम्। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ये गुण क्या है? प्रकृति और तीनों गुणों में क्या सम्बन्ध है? क्या इनमें द्रव्य गुण-सम्बन्ध है? सामान्यतः‘गुण’ शब्द का जो अर्थ किया जाता है उस अर्थ में सत्त्व, रजम् और तमस् गुण नहीं है। वस्तुतः मे प्रकृति के गुण नहीं हैं, अपितु उसके संघटक तत्त्व हैं। उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन प्रकृति और उसके गुणों में द्रव्य गुण भेद नहीं स्वीकार करता है। यहाँ सांख्य दर्शन की मान्यता न्याय वैशेषिक दर्शन की उस विचारधारा है विपरीत है जिसमें पदार्थ में द्रव्य गुण भेद स्वीकार किय जाता है। तात्पर्य यह है कि सत्त्व, रजस् और तमस् द्रव्य रूप हैं। ये इसलिए भी द्रव्य है, क्योंकि सांख्य दर्शन में इनके भी गुणों का विवेचन प्राप्त होता है। सांख्यप्रवचनभाष्य के अनुसार सत्त्व रजस् और तमस इस अर्थ में गुण हैं कि ये रस्सी के तीनों गुणों (रेशों) के समान पुरुष को बाँधने का काम करते हैं। चूँकि ये पुरुष के उद्देश्य साधन में गौण रूप से सहायक है, इसलिए भी उन्हें ‘गुण’ कहा जाता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार पुरुष की अपेक्षा गौण होने के कारण भी इन्हें गुण कहते हैं। डॉ० राधाकृष्णन के अनुसार ये इसलिए भी गुण है, क्योंकि अकेली प्रकृति विशेष्य है और ये उसके अन्दर केवल अवयव रूप से अवस्थिति है।
सांख्य दर्शन में प्रकृति के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। इनसे भी प्रकृति के स्वरूप का परिचय प्राप्त लेता है। सांख्य दार्शनिक इसे प्रधान कहते हैं, क्योंकि यह विश्व का प्रथम मूलभूत कारण है। प्रकृति अव्यक्त भी है, क्योंकि इसमें यह सम्पूर्ण जगत् अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। प्रकृति को अजा कहते हैं, क्योंकि यह अनुत्पत्र है और इसका कोई कारण नहीं है। यद्यपि यह सम्पूर्ण जड़-जगत् का कारण है, किन्तु इसका कोई कारण नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को अनुमान भी कहा जाता है। इसकी सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से न होकर केवल अनुमान से होता है। यह जड़ है, क्योंकि यह मूलभूत भौतिक पदार्थ है। यह अचेतन होने के कारण अविवेकी भी है। यह विषय या ज्ञेय है, क्योंकि यह पुरुष द्वारा भोग्य एवं जानी जाती है। यह सामान्य है, क्योंकि यह सम्पूर्ण भौतिक जगत् में व्याप्त है और यह भौतिक जगत् अपने आविर्भाव के पूर्व प्रकृति में ही निहित था। चूँकि प्रकृति अकारण और अनुत्पन्न है, अत: यह नित्य एवं शाश्वत हैं। यह स्वतन्त्र है, क्योंकि यह किसी अन्य तत्त्व पर आश्रित नहीं है। चूँकि संपूर्ण जगत् प्रकृति से प्रसूत है, अतः वह प्रसवधर्मी है। उपर्युक्त लक्षणों के कारण प्रकृति को एक व्यक्तित्वविहीन सत्ता स्वीकार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सांख्यकारिकों में प्रकृति का स्वरूप बताते समय कतिपय ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं कि मानों वह कोई चेतन व्यक्तित्वयुक्त सत्ता हो। जैसे, प्रकृति स्त्री है, प्रसवधार्मिणी है। वह अत्यन्त सुकुमार है, लज्जाशील है। पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पुनः उसके समने कभी नहीं आती है। वह गुणवती है, उपकारिणी है, आदि।
Table of Contents
प्रकृति के अस्तित्त्व के लिए प्रमाण
सांख्य दर्शन युक्तियों के आधार पर प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रसंग में –
भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च ।
कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूपस्य ।।
साख्यकारिका में निम्नलिखित कार्रिका प्राप्त होती है इस कारिका में प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित पाँच युक्तियाँ प्राप्त होती हैं –
भेदानां परिमाणत्
बुद्धि एवं मन से लेकर पृथ्वी पर्यन्त, संसार के सभी सूक्ष्मतिसूक्ष्म और स्थूल पदार्थ परिमित, परिच्छिन्त्र, परतन्त्र एवं सापेक्ष हैं। इनका कारण कोई परिमित्त, परिच्छिन्न परतन्त्र एवं सापेक्ष तत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं सकारण है। चूँकि परिमित अपरिमित के विचार की ओर, परतन्त्र स्वतन्त्र के विचार की ओर, परीच्छिन्न अपरिच्छित्र के विचार की ओर तथा सापेक्ष निरपेक्ष के विचार की ओर संकेत करता है। अतः इन परिमित परतन्त्र, परिच्छिन्न एवं सापेक्ष पदार्थों का कारण एक ऐसा अपरिमित, स्वतन्त्र, अपरिच्छिन्त्र एवं निरपेक्ष तत्त्व ही हो सकता है जो स्वयं अकारण हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्त्व प्रकृति ही है।
समन्वयात्
संसार के सभी परिमित विषय, सूक्ष्मातिसूक्ष्म और स्थूल विषय, सुख, दुःख और अज्ञान उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि सुख सत्त्व गुण से, दुःख रजोगुण से और अज्ञान तमोगुण से उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि संसार के सभी विषय सत्त्वरजस्तमसात्मक हैं। अतः इनका कारण एक ऐसा तत्त्व ही हो सकता है जिसमें सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों का समन्वय होता हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा तत्त्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति है।
शक्तित: प्रवृत्तेः
कारण की शक्ति से, समर्थ कारण से ही किसी कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। असमर्थ कारण किसी भी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। जैसे, दही को उत्पन्न करने में दूध ही समर्थ है, पानी से दही की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शक्तिमान कारण ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। इसके आधार पर संसार के सभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म और स्थूल पदार्थों का कारण एक ऐसा तत्त्व हो हो सकता है कि जिसमें उन्हें उत्पन्न करने की शक्ति हो। सांख्य दर्शन के अनुसार यह समर्थ कारण अव्यक्त प्रकृति है।
कारणकार्यविभागात्
संसार में कारण और कार्य में भेद दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है। उस कारण का भी एक कारण होता है। कार्य-कारण की यह शृंखला अनन्त तक नहीं जा सकती है, अन्यथा अनवस्था दोष (The Fallacy of Infinite Regress) उत्पन्न होता है। अतः संसार की सभी वस्तुओं का एक मूलभूत कारण है जिसका कोई अन्य कारण नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति है।
अविभागाद्वैश्वरूपस्य
सांख्य दर्शन कारण कार्य सम्बन्ध के विषय में दो तथ्यों को स्वीकार करता है-प्रथम, कारण से कार्य उत्पन्न होता है और द्वितीय, नष्ट होने पर कार्य पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जैसे, सोने से निर्मित सोने की अंगूठी नष्ट होने पर पुनः सोने में मिल जाती है। तात्पर्य यह है कि तत्त्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। इस आधार पर सांख्य दर्शन का कथन है कि यह सम्पूर्ण विश्व एक ऐसे कारण से उत्पन्न होना चाहिए जिसमें वह प्रलयावस्था में पुनः विलीन हो सके। सांख्य दर्शन इस कारण को प्रकृति कहता है।
सांख्य दर्शन उपरोक्त युक्तियों के आधार पर प्रकृति को सत्ता को सिद्ध करता है जो चेतन पुरुष के अतिरिक्त समस्त जड़ जगत् का कारण है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीचे कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
- सांख्य दर्शन के विकासवाद की व्याख्या
- सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद की व्याख्या
- नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय
- संकल्प की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध की आलोचना व नियतिवाद
- नैतिकता की मान्यताओं के आधार पर आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्त्व की व्याख्या
