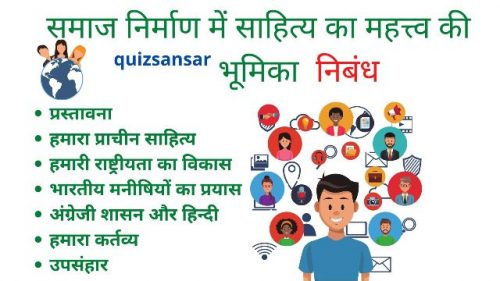
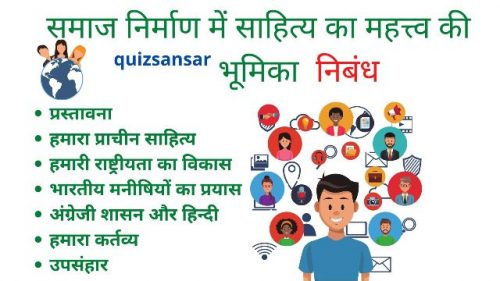
समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका
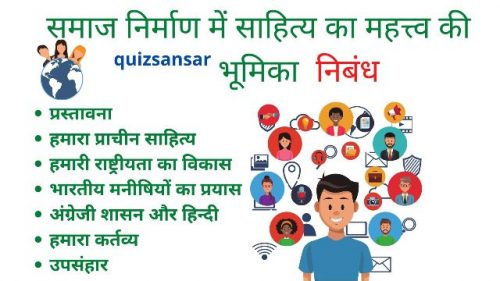
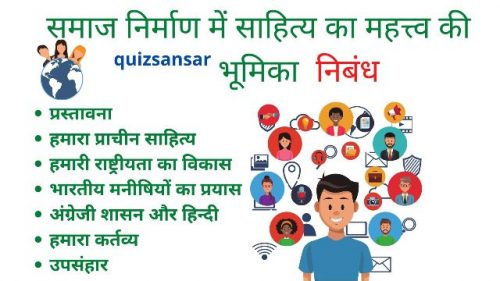
नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए नई post ले कर आए हैं जिसका नाम है समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका पर निबंध | राष्ट्र निर्माण में साहित्य का महत्त्व पर निबन्ध | उम्मीद करते हैं आपको यह post पसंद आएगी | .
साहित्य का महत्त्व batane ki awashyakta nhi hai क्यूंकि साहित्य वह है जिससे किसी भी भाषा का महत्व बढ़ जाता है | समाज के निर्माण में साहित्य का महत्त्व बहुत है समाज और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य एक अहम् भूमिका निभाता है अब आगे हम निबंध पढेंगे समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व |
Table of Contents
रूपरेखा
- प्रस्तावना
- हमारा प्राचीन साहित्य
- हमारी राष्ट्रीयता का विकास
- भारतीय मनीषियों का प्रयास
- अंग्रेजी शासन और हिन्दी
- हमारा कर्तव्य
- उपसंहार
प्रस्तावना
जिस प्रकार शब्द से अर्थ को और अर्थ से शब्द को तथा शरीर से प्राण को और प्राण से शरीर को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम राष्ट्र को भी साहित्य से पृथक् नहीं कर सकते और न साहित्य को राष्ट्र से। इसलिए समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में साहित्य का महत्त्व है |
जिस प्रकार शरीर और प्राण अन्योन्याश्रित हैं, बिना शरीर के प्राणों का अस्तित्व नहीं और बिना प्राणों के शरीर का महत्त्व नहीं ठीक उसी प्रकार साहित्य प्राण है और राष्ट्र उसका शरीर।
जिस प्रकार निर्जीव शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार साहित्यहीन राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं |
“मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।”
यदि हमारा साहित्य उन्नत है, समृद्धिशाली है तो हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा, समृद्धिशाली होगा और यदि हमारे यहाँ साहित्य का अभाव है, तो राष्ट्र का जीवित रहना भी कठिन है।
आज नहीं तो कल उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता निश्चित ही नष्ट हो जायेगी। निर्जीव राष्ट्र चिरस्थायी नहीं रह सकता।
हमारा प्राचीन साहित्य
हमारा प्राचीन साहित्य, संसार के अन्य किसी साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। हमारे देश को विश्व के लोग जगत गुरु कहते थे।
विश्व के समस्त अंचलों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम विद्या और बुद्धि में शक्ति और साहित्य में संसार के सिरमौर थे, अग्रगण्य और अग्रगामी थे।
हमने सभी देशों का अज्ञानान्धकार नष्ट करके उन्हें ज्ञानलोक दिया और उनका मार्ग-प्रदर्शन किया था। विश्व हमें धर्मगुरु मानता था।
हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी और तुलना में संसार का कोई ज्ञान नहीं ठहर सका। इंग्लैण्ड और जर्मनी निवासियों ने तो यहाँ आकर संस्कृत साहित्य का महत्त्व का गहन अध्ययन किया है।
संस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण कोष हमारे भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। इसी उच्चकोटि के साहित्य के बल पर राष्ट्र उन्नतिशील था, विश्व इसके सामने नतमस्तक होता था।
हमारी राष्ट्रीयता का विकास
संसार परिवर्तनशील है, जो वस्तु आज है, कल वह उस अवस्था में नहीं रह सकती। समय बदलता है, समय के साथ-साथ मनुष्य की बुद्धि, विचार और उसके कार्य-कलाप भी बदल जाते हैं। सदैव किसी के दिन एक से नहीं रहते।
ऐश्वर्य, धनधान्य और अनन्त महिमा सम्पन्न भारतवर्ष का भाग्याकाश विदेशी आक्रान्ताओं से आच्छादित हो उठा। देश का सौभाग्य-सूर्य प्रभावहीन-सा दृष्टिगोचर होने लगा।
यदि आप किसी राष्ट्र को अपनी दासता में आबद्ध करना चाहते हैं और यदि आपकी यह भी इच्छा है कि यह दासता चिरस्थायी हो और उस राष्ट्र के नागरिक आपके अन्ध-भक्त बन जायें तब आपको सर्वप्रथम उस देश का उस जाति का साहित्य नष्ट कर देना चाहिए तथा वहाँ की भाषा को नष्ट कर देना चाहिए।
यदि आप किसी जाति की जातीयता और राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं को अतीत के गर्भ में सुला देना चाहते हैं तो आप उस देश और जाति की अमूल्य निधि साहित्य को समाप्त कर दीजिए।
विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए। नालन्दा और तक्षशिला के जगत्-प्रसिद्ध पुस्तकालय अग्नि को समर्पित कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि साहित्य के अभाव में हमारी राष्ट्रीयता विलुप्त-सी हो गई। हम आश्रयहीन, निरालम्ब और असहाय बन कर मूक पशु की भाँति अत्याचार और अन्याय सहन करते रहे।
भारतीय मनीषियों के प्रयत्न
समय ने पलटा खाया। भारतीयों में चेतना और स्फूर्ति फैली। जन-जीवन में जागरण का उद्घोष हुआ। विदेशी आक्रान्ताओं के विरुद्ध आत्म-संगठन के विचार जनता के मानस सागर में हिलोरे लेने लगे, परिस्थितियों से विवश मृतप्राय आर्य जाति ने फिर करवट ली और अंगड़ाई लेकर उठ बैठी।
शिवाजी ने हिन्दुओं की रोटी और बेटी की रक्षा करने की शपथ ली, भूषण जैसे राष्ट्र कवियों का जन्म हुआ। शिवाजी की प्रशंसा में वे गा उठे-
“राखी हिन्दुवानी, हिन्दुवान को तिलक राख्यौ।”
भूषण ने अपनी अनेक मार्मिक उक्तियों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी को सचेष्ट कर दिया। वे कहने लगे-
“साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। “
बस, फिर क्या था कुछ समय में ही आर्य जाति फिर हुंकार भरने लगी।
“भुज भुजगेस की वैसंगिनी भुजंगिनी-सी,
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के || “
इत्यादि उक्तियों में भूषण ने महाराजा छत्रसाल को भी शत्रुओं से भिड़ने के लिए आगे बढ़ाया, परन्तु यह सब कुछ तो राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव मात्र था।
सबसे कठिन समस्या उस समय भाषा की थी, क्योंकि समस्त देश की भाषा एक नहीं थी। इस कारण समस्त देश का सामूहिक संगठन दुर्लभ-सा प्रतीत हो रहा था। फिर भी सूर, तुलसी, दादू, कबीर, राज, चैतन्य महाप्रभु, नानक आदि महापुरुषों ने भिन्न-भिन्न भाषाओं का आश्रय लेकर देश में सामाजिक और जातीय संगठन का सूत्रपात किया।
अपने साहित्य द्वारा इन महापुरुषों ने संत्रस्त मानवता की रक्षा की। विदेशियों के अत्याचार, पक्षपात, हृदयहीनता आदि चरमसीमा पर थे। इन राष्ट्र-निर्माताओं ने अपने अनवरत प्रयासों से भयभीत जनता के हृदय में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास को जागृत किया। जनता के लिए स्नेह और संगठन का मार्ग प्रदर्शित किया।
युगों से जनता के हृदय में घर कर गयी संकीर्ण विचारधाराओं को समाप्त करके संगठन का अमोघ मन्त्र प्रदान किया। तुलसी ने राम कथा द्वारा जनता को संगठित रहने तथा आततायी को समूल नष्ट कर देने का जो पाठ पढ़ाया वह अद्वितीय था। शक्ति, शील और सौन्दर्यपूर्ण राम जनता के दुःख-सुख के साथी बन गए।
रामचरित मानस ने विनाश के कगार पर खड़ी हुई हिन्दू जाति को बचा लिया। कवि प्रशंसा में गा उठा –
“भारी भवसागर से उतारतौ कवन पारि,
जो पै यह रामायन तुलसी न गावतौ || “
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की चेतावनी देखिये-
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है ।
मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ जो भारतवर्ष में उपद्रवी बन कर आई थीं, इन महापुरुषों के प्रयत्नों और उपदेशों से प्रभावित होकर आर्यों के साथ मिल-जुल गईं। साहित्य का प्रभाव अमिट होता है।
अंग्रेजी शासन और हिन्दी
अंग्रेजों के पदार्पण ने देशवासियों की देश-प्रेम भावना को और भी बढ़ा दिया।
परन्तु फिर भी यही समस्या थी कि कोई भी देशी भाषा ऐसी नहीं थी जिसका देशव्यापी प्रभाव हो। क्योंकि समस्त देश के लिए एक भाषा और उसी भाषा में उसका साहित्य होना परम आवश्यक है।
भारतीयों की अनन्त साधनाओं, तपस्याओं एवं बलिदानों की पृष्ठभूमि में भारतीय साहित्यकारों का देश प्रेम पूर्ण साहित्य था, जिसके फलस्वरूप देश विदेशियों से मुक्त हुआ।
आज हम स्वतन्त्र हैं। देश की राष्ट्र भाषा के सिंहासन पर हिन्दी को प्रतिष्ठित किया जा चुका है। राष्ट्र भाषा के अभाव में राष्ट्रीय संगठन में जो बाधायें उपस्थित हो रही थीं अब वे समाप्त हो जायेंगी।
हमारा कर्तव्य
आज भारतीय साहित्यकारों का पवित्र कर्तव्य है कि वे ऐसे साहित्य का निर्माण करें जिससे राष्ट्र के आत्म-गौरव और गरिमा की वृद्धि हो।
देश का सर्वांगीण विकास और सामूहिक चारित्रिक पुनरुत्थान सत्साहित्य पर ही निर्भर करता है। आज देश का साहित्यकार अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए देशवासियों का ईमानदारी से पथ-प्रदर्शन नहीं कर रहा है।
यही कारण है कि देश का चारित्रिक विकास रुक गया है, कर्त्तव्यहीनता और स्वार्थ-लोलुपता सर्वत्र व्याप्त है।
उपसंहार
सारांश यह है कि भारतवर्ष की उन्नति, उसकी गौरव गरिमा, राष्ट्र भाषा हिन्दी के साहित्य की समृद्धि पर निर्भर है।
साहित्य की अवनत अवस्था में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, यह निःसन्देह सत्य है। अर्थात हम कह सकते हैं की समाज के निर्माण में साहित्य का महत्त्व एक अहम् भूमिका का निर्वहन करता है
साहित्य का महत्त्व के साथ साथ ही राष्ट्र हित भी जुड़ा हुआ है |
महत्वपूर्ण लिंक
- Branches of science and its meaning
- ONE LINER CURRENT AFFAIRS
- 60 FAMOUS WRITERS AND THEIR BOOKS { प्रसिद्ध लेखक व उनकी पुस्तकें }
- one liner current affairs
- Computer ( कंप्यूटर )
- उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण ( Achievement Tests in hindi )
- निबंध क्या है इसकी परिभाषा एवं प्रकार | निबंध कैसे लिखें ?
कैसी लगी आपको हमारी post समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका |
अगर आपके पास समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका से जुड़ा हुआ कोई सुझाव हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर दें |
समाज निर्माण में साहित्य का महत्त्व की भूमिका
- हिन्दी काव्य/कविता में प्रकृति चित्रण | कवियों की दृष्टि में प्रकृति
- जल के गुण , प्रकार एवं संरचना
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन परिचय , रचनाएँ एवं lekhan शैली
- महाकवि बिहारी का जीवन परिचय
- साहित्य समाज का दर्पण है ?
साहित्य का महत्त्व
साहित्य और समाज की रूपरेखा में साहित्य का महत्त्व
हमारी राष्ट्रीयता का विकास
भारतीय मनीषियों का प्रयास
अंग्रेजी शासन और हिन्दी
हमारा कर्तव्य in सभी साहित्य का महत्त्व के टॉपिक को पढने के लिए visit करें quizsansar .
