

कर्मचारी भर्ती से आपका क्या तात्पर्य है? कर्मचारी आपूर्ति के स्त्रोत
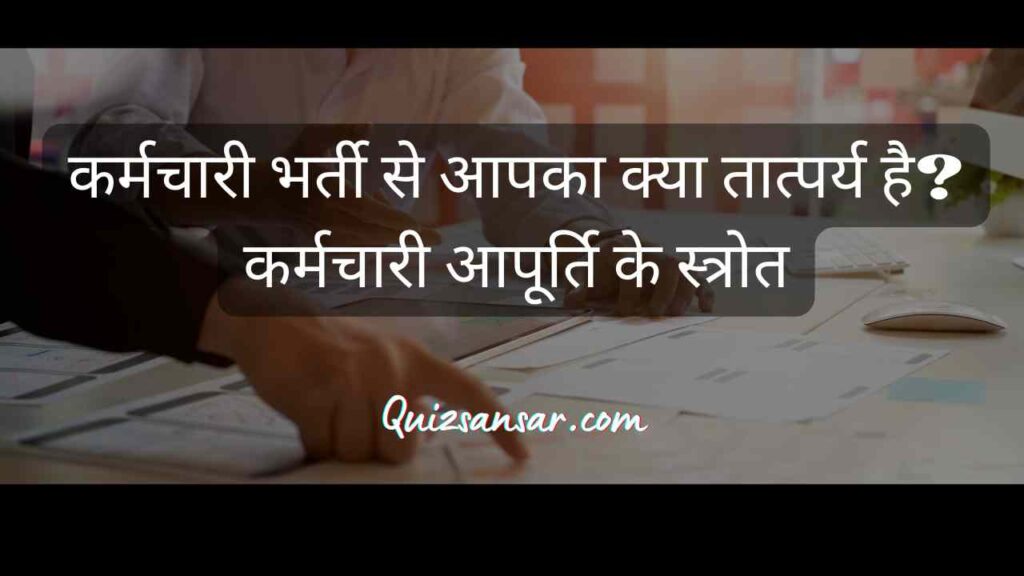
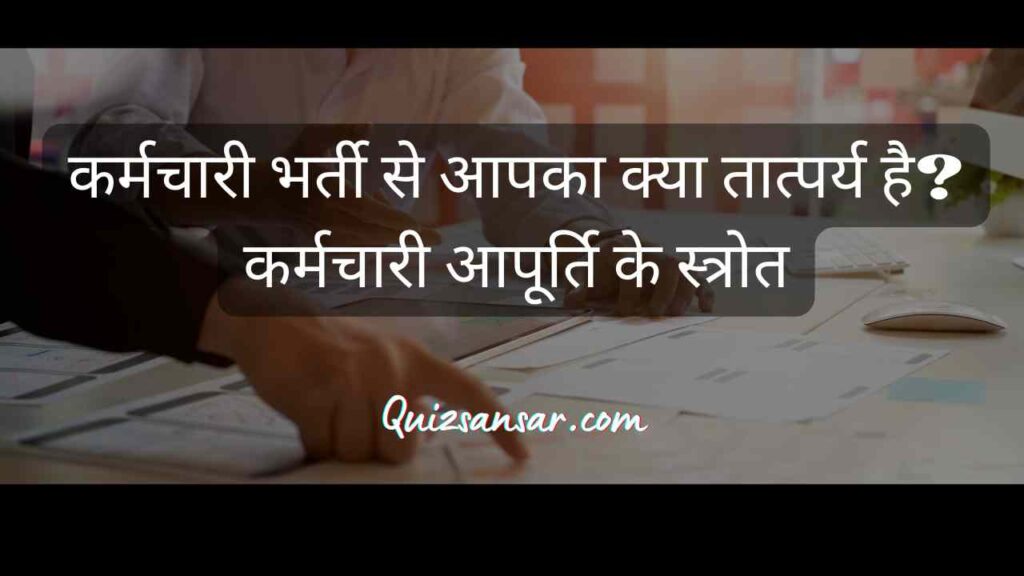
कर्मचारी भर्ती से आपका क्या तात्पर्य है?
एडविन बी० फिल्प्पिो के अनुसार, “भरती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा किसी संगठन में सेवा नियोजन हेतु उन्हें आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है।” प्रायः भरती की क्रिया को धनात्मक तथा चयन की क्रिया को ऋणात्मक क्रिया की संज्ञा दी जाती है। भरती को धनात्मक क्रिया इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतम व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे चयन-अनुपात बढ़ता है, जबकि चयन एक ऋणात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों को काटने-छांटने का प्रयास होता है जिससे कि नियुक्ति के लिए केवल उतने ही कर्मचारी शेष रह जायं, जो वास्तव में सर्वोत्तम है।
संगठन के लिए सही कर्मचारियों की खोज, संगठन, कर्मचारी और समाज सबकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। संगठन की दृष्टि से सही संख्या ओर गुणवत्ता के कर्मचारियों की खोज आवश्यक है क्योंकि इससे कार्यों की गुणवत्ता एवं लागत और संगठन का अनुशासन, व्यवस्था और वातावरण प्रभावित होता है। कर्मचारी की दृष्टि से एक पद पर सही कर्मचारी की खोज उसके मनोबल, कार्यसंतोष, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है और समाज की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रोजगार की समस्या सीधे रूप से जुड़ी होती है। फिर आज के बदलते हुए परिवेश में सरकार भी रोजगार के प्रति बहुत सजग है। विभिन्न वर्गों और जातियों के लिए रोजगार में आरक्षण होते हैं और संगठन को इन सरकारी नीतियों और प्रतिबन्धों को भी कर्मचारी खोज की प्रक्रिया में समायोजित करना पड़ता है। आन्तरिक स्रोतों, (पदोन्नति एवं स्थानान्तरण) और बाहरी स्रोतों के बीच एक न्यासंगत संतुलन भी बनाए रखना होता है। साथ ही संगठन की विषम और बदलती हुई परिस्थितियों, विकास की भावी आवश्यकताओं और कर्मचारी हितों का भी कर्मचारी खोज की नीति बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। अतः कर्मचारी खोज की नीति का निर्धारण सोच-समझकर किया जाना चाहिए।
कर्मचारी आपूर्ति के स्त्रोत (Sources of Manpower Supply)
अच्छे कर्मचारियों की खोज के लिए यह आवश्यक है कि सेविवर्गीय विभाग को मानव-शक्ति आपूर्ति के स्रोतों की जानकारी हो। सामान्यतः इन स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : (अ) आन्तरिक तथा (ब) बाह्य।
(अ) आन्तरिक स्रोत (Internal Sources) – संगठन के पदों पर नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम संगठन के कर्मचारियों में ही खोज की जानी चाहिए। इसका वास्तव में अर्थ यह होगा कि वर्तमान कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। इस नीति के अग्रलिखित लाभ होते हैं:
प्रथम, इससे कर्मचारी चयन की समस्या सरल हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी पूर्व परिचित होता है। कार्य-निष्पादन से अच्छी कोई दूसरी जांच-विधि नहीं है। इसमें प्रबन्धक कर्मचारी के व्यवहार, रुचि, गुण, निष्ठा, आशाओं और आवश्यकताओं के बारे में सही और शीघ्र सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इससे चयन का कार्य सरल हो जाता है और सही कर्मचारी के मिलने की सम्भावना भी बढ़ जाती है।
दूसरे, इससे वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलता है जिससे वे अधिक कार्य करने अनुशासित रहने और संगठन एवं अधिकारियों के प्रति निष्ठावान रहने की ओर प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति के प्रलोभन में अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण, निपुणता, आदि को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे प्रबन्धकों के समक्ष अपने पदोन्नति के अधिकार को उचित ठहरा सकें। फिर प्रबन्धकों की दृष्टि से यह नीति इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि इससे अनुशासन की समस्याएं कम होती हैं, कर्मचारियों का मनोबल उठता है, शिकायतों और परिवेदनाओं में कमी आती है, श्रमिक परिवर्तन कम होते हैं, तथा कर्मचारी निष्ठा एवं रुचि में वृद्धि होती है। कर्मचारी प्रबन्धकों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा अपने को अधिक सुरक्षित, संतुष्ट और आशान्वित अनुभव करते हैं। संक्षेप में, इससे कर्मचारियों की मनोवृत्ति एवं आचरण पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जो प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों दोनों के लिए बहुत हितकर होता है।
तीसरे, पदोन्नति द्वारा कर्मचारियों की खोज न केवल वर्तमान कर्मचारियों और अच्छा प्रभाव डालती है, बल्कि इसका प्रभाव भावी कर्मचारियों पर भी पड़ता है। जो संगठन अपने यहां पदोन्नति की स्पष्ट रेखाएं और नियम बना देते हैं, तथा कर्मचारियों की नियमित एवं न्यायसंगत पदोन्नति करते रहते हैं, उनकी बाह्य जगत में प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है, तथा भावी कर्मचारी इसी साख के आधार पर ऐसे संगठनों में कार्य करने के लिए लालायित रहते हैं। इससे संगठन में कुशल कर्मचारियों की उपलब्धि की सम्भावना बढ़ जाती है। और अन्त में, इससे प्रवेश और प्रशिक्षण के समय और लागत में कमी होती है क्योंकि ऐसे कर्मचारी पहले से ही अधिकतर बातों से परिचित होते हैं।
लेकिन इस नीति में अग्रलिखित कठिनाइयां एवं दोष भी हैं-प्रथम, इससे प्रबन्धकों के ऊपर वर्तमान कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के सुव्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की भारी जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि यदि कर्मचारी का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ एवं सही नहीं हुआ है, तो इससे दोषपूर्ण निर्णय एवं पक्षपात की समस्याएं संगठन में उठ खड़ी होंगी। दूसरे, पूर्णरूपेण योग्यता पर आधारित पदोन्नति से कभी-कभी कर्मचारी संघर्ष एवं अशान्ति उत्पन्न हो जाती है और उनका मनोबल गिर जाता है, विशेषरूप से तब जब कोई कर्मचारी सही या गलत यह अनुभव करता है कि पदोन्नति में उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तीसरे, नए कार्यों पर उचित नियुक्तियों के लिए संस्था में कभी-कभी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध ही नहीं होते। चौथे, किसी कर्मचारी की भूतकालीन निष्ठा और कार्यकुशलता इस बात की गारन्टी नहीं है कि वह भविष्य में ऊँचे पद पर भी उतना ही योग्य और निष्ठावान सिद्ध होगा। और अन्त में, यदि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है और जो प्रायः विवाद, असन्तोष और पक्षपात को दूर करने के लिए होता है, तो सम्भव है कि पदोन्नति किए हुए कर्मचारी में उस पद पर कार्य करने के लिए अपेक्षित शारीरिक और मानसिक योग्यता और निपुणता न हो। और यदि गुणों के आधार पर की जाती है, तो सम्भव है कि कर्मचारी असंतोष एवं विरोध इसलिए उत्पन्न हो, कि उनके गुणों का मूल्यांकन सही नहीं हो सका है, अथवा उन्हें ऐसा विश्वास है, अथवा वे वरिष्ठता के आधार को अधिक उचित समझते हैं। इन दोषों और कठिनाइयों के उपरान्त भी संगठन में उच्च पदों की पूर्ति के लिए आन्तरिक कर्मचारियों की पदोन्नति एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। अतः प्रबन्धकों को चाहिए कि पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के सुनिश्चित नियम एवं रेखाएं बनाएं तथा कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन एवं वरिष्ठता के सही अभिलेख रखें।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


स्टाफ के प्रभाव को सशक्त बनाने के उपाय | Ways to strengthen staff influence


स्टाफ के प्रभाव को सशक्त बनाने के उपाय
स्टाफ अधिकारी का आदेश श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रभाव होते हुए भी कुछ हठी और सशक्त रेखाधिकारी उसकी राय की अवहेलना कर मनमानी निर्णय और कार्यवाही करने से नहीं चूकते। ऐसे अधिकारी स्टाफ की राय या तो बहुत विषम और उलझे हुए मामलों में लेते हैं या तब मान लेते हैं जब वह उनके अनुकूल होती है। अतः स्टाफ के विचारों और सुझावों को संगठन में वह महत्त्व नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए स्टाफ के प्रभाव को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रेषित हैं।
(1) स्टाफ परामर्श की अनिवार्यता (Compulsory Staff Consultation) –
इस व्यवस्था में सटाफ का परामर्श लेना, कार्यवाही करने के पूर्व अनिवार्य कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, उपाध्यक्ष किसी कम्पनी के प्रसंविदे पर हस्ताक्षर तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसे कम्पनी के वकील ने पढ़कर अपनी स्वीकृति न दे दी हो। इसी प्रकार कम्पनी का कोई प्रतिनिधि सार्वजनिक भाषण तब तक नहीं दे सकता, जब तक उसे कम्पनी के जन सम्पर्क अधिकारी ने पढ़कर अनुमोदित न कर दिया हो। वस्तुतः स्टाफ परामर्श अनिवार्यता के अन्तर्गत किसी अधिकारी को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने से रोका नहीं जाता, बल्कि उसे कुछ समय के लिए रूककर – एक दूसरे दृष्टिकोण से एक विशेषज्ञ के विचारों को सुनने के लिए कहा जाता है। यह अनिवार्यता परस्पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करती है और रेखाधिकारी की अबाध स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाती है।
इसी के समानान्तर एक विधि यह भी है कि स्टाफ अधिकारियों से रेखा विभागों के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कम्पनी का अध्यक्ष आन्तरिक अंकेक्षक से लेखाविभाग की कार्यविधि के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कह सकता है। यह अनिवार्यता स्टाफ को बड़े धर्मसंकट में डाल देती है, क्योंकि बहुत बार वह निम्नस्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कमियों और त्रुटियों को पकड़ लेता है, किन्तु, वरिष्ठ अधिकारी से छिपाना चाहता है। यदि वह रिपोर्ट करता है तो उसे इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि दोबारा आने पर लोग उसका स्वागत नहीं करेंगे और सम्भव है कि किसी जंजाल में फंसाकर उससे प्रतिशोध लें या उसे किसी मुसीबत में डाल दें। फिर रिपोर्ट से उसके किसी मित्र सहयोगी का स्थाईरूप से अहित भी हो सकता है। अतः वह रिपोर्ट करने में संकोच करता है। किन्तु दूसरी और रिपोर्ट न करके वह कम्पनी के हित और नियम के विरोध में कार्य करने का अपना उत्तरदायित्व भी बढ़ाता है। फिर वह अपना निरोधात्मक प्रभाव खो बैठता है और कर्मचारी उसकी तथा कार्य निष्पादन की अवहेलना करने लगते हैं। ऐसी धर्मसंकट की स्थिति से निकलने का एक मात्र रास्ता यही है कि स्टाफ अधिकारी कर्मचारी की भूलों और त्रुटियों को पकड़कर अपने ठोस सुझाव और विशिष्ट सम्मतियों द्वारा, कार्यरत कर्मचारियों से ही उन्हें दूर करा देना चाहिए। इसके लिए उसे अपनी सहानुभूति एवं सक्रिय सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार, न तो वह कम्पनी का, और न ही अपने मित्र सहयोगी का अहित करेगा और अपना सम्मान और प्रभाव भी संगठन में बनाए रख सकेगा।
(2) संयुक्त या समानान्तर अधिकार प्रदान करना (Granting Concurrent Authority) –
स्टाफ अधिकारी की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए कभी-कभी उसे भी संयुक्त, समानान्तर या समधिकारी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इससे कोई भी कार्यवाही बिना उसकी सहमति के सम्भव नहीं होती। ऐसे संयुक्त अधिकार का प्रयोग गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। जब तक गुणवत्ता निरीक्षक कच्चे या अर्द्धनिर्मित माल की गुणवत्ता को स्वीकृति प्रदान नहीं कर देता, माल को आगे प्रेषित नहीं किया जा सकता। किसी प्रसंविदे पर उपाध्यक्ष के साथ कम्पनी के वकील के हस्ताक्षर, किसी कर्मचारी को रखने के पूर्व विभागाध्यक्ष के साथ सेविवर्गीय अबन्धक की स्वीकृति, किसी क्रय अधिकारी द्वारा पूँजीगत व्यय करने के पूर्व वित्ताधिकारी की स्वीकृति, संयुक्त या समानान्तर अधिकार के अन्य उदाहरण हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रेखाधिकारी की अबाध स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाकर, उसे बिना सोचे-विचारे कार्यवाही करने से रोकती है। फिर वरिष्ठ अधिकारी रेखा और स्टाफ दोनों ही अधिकारियों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। किन्तु इस व्यवस्था का प्रथम दोष यह है कि इसमें उत्तरदायित्व के खिसकाने का भय उत्पन्न हो जाता है। दूसरे, इसमें संयुक्त अधिकार के कारण विलम्ब और अवरोध का भय भी रहता है। इसलिए संयुक्त अधिकार केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जबकि स्टाफ की राय बहुत ही महत्वपूर्ण हो। संयुक्त अधिकार का चलन सरकारी विभागों में बहुत है। व्यावयसायिक संगठनों में इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है।
(3) क्रियात्मक अधिकार प्रदान करना (Granting Functional Authority) –
आदेश श्रृंखला में स्टाफ के प्रभाव को बढ़ाने का सबसे अधिक औपचारिक तरीका स्टाफ अधिकारी को क्रियात्मक अधिकार प्रदान कर देना है। क्रियात्मक अधिकार के प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि स्टाफ अधिकारी अपने नाम से रेखाधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे आदेश और निद्रेश दे सकता है और उसे फिर अपने सुझावों की वरिष्ठ रेखाधिकारियों के पास भेजने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके निर्देशों में फिर वही शक्ति हो जाती है जो कि एक आदेश श्रृंखला के वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में होती है। लेकिन उसे यह अधिकार केवल अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। किसी भी स्थिति में आदेश श्रृंखला के कर्मचारी और अधिकारी न तो उसके नियंत्रण में आ जाते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उसे बिना दाँत का अधिकारी (Authority without Teeth) कहा जाता है, क्योंकि वह कोई कार्यवाही अधीनस्थ के विरूद्ध सीधे नहीं कर सकता। इस व्यवस्था में स्टाफ के प्रभाव में वृद्धि के साथ-साथ समय की बचत भी होती है। यह अधिकार स्टाफ को तभी दिया जाता है जब उसे किसी क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, सेविवर्गीय प्रबन्धक को कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण और सुरक्षा के सम्बन्ध में, या चिकित्सा अधिकारी को शारीरिक परीक्षा के सम्बन्ध में, या वित्ताधिकारी को खर्च के सम्बन्धम क्रियात्मक अधिकार दिया जा सकता है और अपने आदेश से वे सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उस क्षेत्र में बाध्य कर सकते हैं।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


हेनरी फेयोल के सामान्य सिद्धान्त | general principles of henri fayol in Hindi


हेनरी फेयोल के सामान्य सिद्धान्त
(i) कार्य विभाजन का सिद्धान्त (Division of Work)- इस सिद्धान्त के अनुसार उद्देश्य प्राप्ति के लिए पहले समस्त आवश्यक क्रियाओं का सही अनुमान लगाया जाना चाहिए, फिर उनका उचित वर्गीकरण होना चाहिए। तत्पश्चात् तदानुसार विभागीकरण होना चाहिए और प्रतिष्ठान के कर्मचारियों में उनकी योग्यता और कुशलतानुसार कार्य का आवंटन किया जाना चाहिए।
(ii) अधिकार एवं दायित्व का सिद्धान्त (Authority and Responsibility)- अधिकार एवं दायित्व का चोली-दामन का साथ है। अतः उन्हें एक साथ रहना चाहिए तथा उनमें संतुलन होना चाहिए। अधिकार का अर्थ है आदेश देने की शक्ति तथा काम कराने का अधिकार और दायित्व का अर्थ है आदेशों के पालने का दायित्व तथा कार्य पूरा न होने पर अथवा आदेश की अवहेलना होने पर उसके लिए उत्तरदेयता। अतः प्रबन्धक को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके उत्तरदायित्वों एवं कार्यों के पूरा करने के लिए आवश्यक हों। साथ ही प्रत्रन्धकों पर उन सभी दायित्वों का भार होना चाहिए, जिनके लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की अधिकता उनके दुरोपयोग का कारण बनती है और उनकी कमी दायित्वों और कर्तव्यों के पूरा करने में बाधक सिद्ध होती है। अतः अधिकारों एवं दायित्वों में समता होनी चाहिए।
(iii) अनुशासन का सिद्धान्त (Discipline)- अनुशासन का आशय अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन, नियमों के प्रति आस्था तथा सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखने से है। एक संस्था में अनुशासन बनाये रखने की बहुत आवश्यकता है और एक अच्छा नेता ही अच्छा अनुशासन कायम कर सकता है। हेनरी फेयोल के ही शब्दों में “बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है।” अच्छा अनुशासन उच्च-कोटि के सुयोग्य अधीक्षकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों तथा समझौतों, विवेकपूर्ण दंड-विधान तथा न्यायोचित व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन में आत्म-नियंत्रण और बाह्य-नियंत्रण दोनों शामिल हैं। आज्ञाकारिता और सम्मान अनुशासन के दो आधार स्तम्भ हैं।
(iv) निर्देश की एकता का सिद्धान्त (Unity of Direction)- इस सिद्धान्त के अनुसार यदि उद्देश्य एक है तो प्रबन्धक को सभी क्रियाओं के लिए एक ही निर्देशों का पालन करना चाहिए। इससे संगठन में उद्देश्य की एकता, कार्य की एकरूपता तथा समन्वय की सुविधा का सृजन होगा।
(v) आदेश की एकता का सिद्धान्त (Unity of Command)- इस सिद्धान्त के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। उसको यह पता होना चाहिए कि किस अधिकारी से उसे आदेश मिलेंगे और किसे उसे अपने कार्य का निष्पादन दिखाना होगा। उत्तरदायित्व के खिसकाव तथा झगड़ों और भ्रान्तियों को रोकने के लिए दोहरी अधीनस्थता से हमेशा बचना चाहिए और आदेश की एकता का सिद्धान्त संगठन में अपनाया जाना चाहिए।
(vi) व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीनस्थ रखने का सिद्धान्त (Subordination of Individual Interest to General Interest)- संगठन का मुख्य लक्ष्य सामूहिक रूप से कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। इसलिए संगठन में रत कर्मचारियों, को संगठन का हित ही सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि वे अपने व्यक्तिगत हितों, कमजोरियों, आकांक्षाओं और स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, तो संगठन के सामान्य हितों की उपलब्धि संभव नहीं हो सकती। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार संगठन के सामान्य हित को, व्यक्तिगत हित से उत्कृष्ट समझने पर जोर दिया जाना चाहिए।
(vii) पारिश्रमिक का सिद्धान्त (Remuneration)- हेनरी फेयोल का मत था कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर एवं भुगतान की विधि उचित तथा संतोषप्रद रखी जाये। यदि मजदूरी पद्धति ठीक होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे और औद्योगिक सम्बन्धों में कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। फेयोल ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-वित्तीय प्रेरणायें देने पर भी बल दिया था।
(viii) केन्द्रीकरण का सिद्धान्त (Centralisation)- संस्था के प्रशासन में केन्द्रीकरण की नीति अपनाई जाये अथवा विकेन्द्रीकरण की इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति, आदि सभी बातों को समग्ररूप से देखते हुये करना चाहिए। संस्था में एक ऐसा केन्द्र बिन्दु होना चाहिए जहाँ से समस्त अधिकारों का प्रवाह हो और समस्त दायित्व का भार हो।
(ix) अधिकार की क्रमिक श्रृंखला का सिद्धान्त (Scaler Chain of Authority)- इस सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के संगठन में, प्रबन्धकों को ऊपर से नीचे की ओर वरिष्ठता (Seniority) तथा अधीनता के क्रम में परस्पर सम्बद्ध किया जाना चाहिए और सबसे वरिष्ठ अधिकारी (Chief Authority) के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण और आदेश के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के हर कर्मचारी को आ जाना चाहिए। इस प्रकार एक सुनिश्चित आदेश श्रृंखला का सृजन हो जायेगा। हर कर्मचारी संगठन में अपना सही स्थान समझ सकेगा और यह भी जान सकेगा कि उसको किससे निर्देश प्राप्त करने हैं और उसे किसे आदेश देने का अधिकार है। लेकिन आदेश श्रृंखला को अनावश्यक रूप से लम्बा नहीं होना चाहिए अन्यथा विलम्ब, संदेशवाहन में बाधाएँ और समन्वय की कठिनाईयाँ उत्पन्नह होने लगेंगी।
(x) व्यवस्था का सिद्धान्त (Order) – व्यवस्था का सिद्धान्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों की व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। फेयोल ने सामग्री तथा कर्मचारी व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित किया। सामग्री व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु के लिए एक नियत स्थान तथा प्रत्येक वस्तु उस निश्चित स्थान पर ही रहना चाहिए। कर्मचारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियत स्थान एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर ही होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने से सामग्री की क्षति एवं समय की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए प्रबन्धक को मानवीय एवं भौतिक साधनों की आवश्यकताओं का सही ज्ञान होना चाहिए एवं आवश्यकताओं और साधनों में निरन्तर संतुलन स्थापित करना चाहिए।
(xi) समता का सिद्धान्त (Equity)- प्रबन्ध का यह सिद्धान्त संगठन के समस्त कर्मचारियों एवं सदस्यों को समान व्यवहार और अवसर देने का सिद्धान्त है। इससे संगठन में सद्भाव, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा मिलता है और आपसी मतभेद, अधिकारियों के निरादर और कर्मचारियों के कुंठित होने की सम्भावना कम हो जाती है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


प्रबन्धन में जीवन दर्शन का महत्त्व, निर्माण एवं विकास
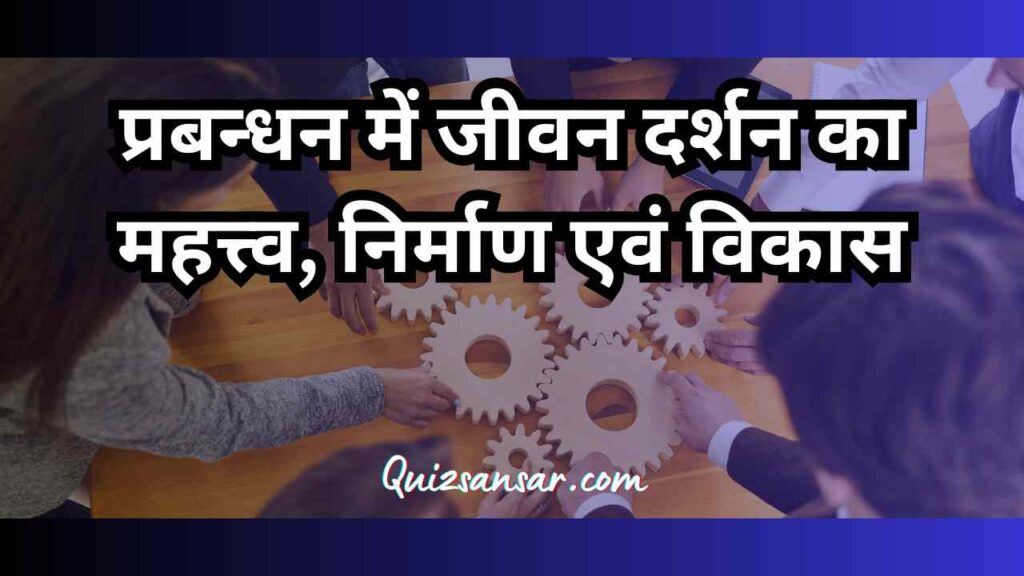
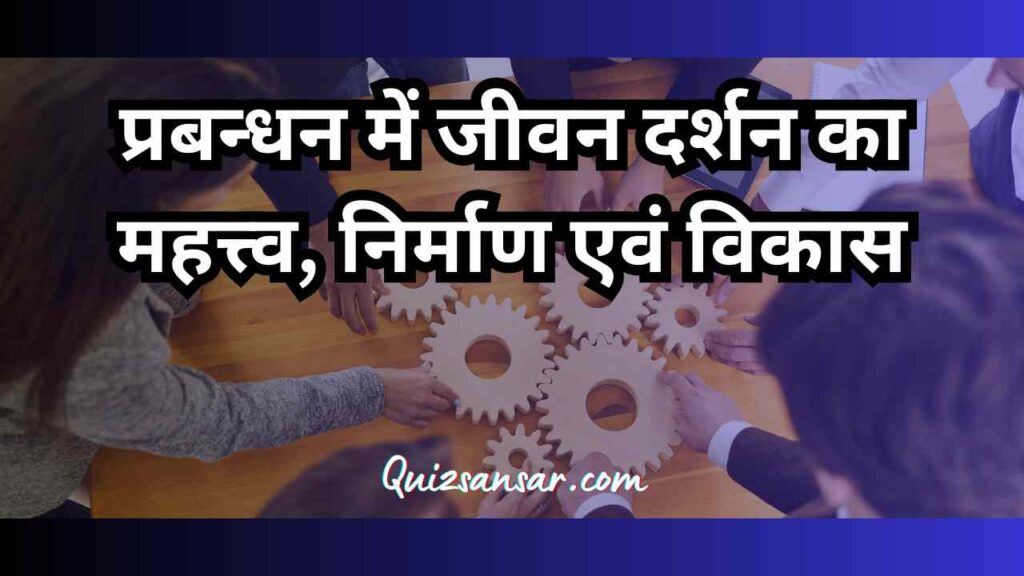
प्रबन्धन में जीवन दर्शन का महत्त्व
जीवन दर्शन का पारिवारिक जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। जीवन, विचार, भावनाओं एवं अनुभवों की सार्थकता का बोध जीवन-दर्शन के द्वारा ही होता है। परिवार के मानवीय सम्बन्धों की प्रकृति, परिवार की रूचियों, पारिवारिक वातावरण का निर्धारण, यहाँ तक कि जीवन में व्यवसाय का चयन जीवन-दर्शन से ही प्रभावित होता है। संक्षेप में जीवन-दर्शन का महत्त्व निम्नानुसार है-
- (अ) यह परिवार के समस्त सदस्यों के आचरण को निर्देशित करता है।
- (ब) परिवार के समस्त सदस्यों की पूर्णता एवं एकता के बोध का आधार जीवन-दर्शन ही होता है।
- (स) चयन तथा निर्णय की कसौटी के विकास में यह सहायक होता है।
- (द) गृह-निर्माण एवं पारिवारिक जीवन के लक्ष्यों की उत्पत्ति जीवन-दर्शन से ही होती है।
गृहस्थ जीवन मानव अनुभवों का वह भाग है जो घर में अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के साथ जीवन व्यतीत करने पर केन्द्रित होता है। इस अनुभव के अन्तर्गत सामान्य साधनों में साझेदारी, व्यक्ति-विशेष के व्यक्तित्व का विकास, मिलकर कार्य करने एवं अनुभव प्राप्त करने के द्वारा सन्तुष्टि प्राप्त करना, परिवार की सामाजिक क्रियाओं में योगदान देना तथा सक्रिय रूप से भाग लेना आदि सम्मिलित हैं। इन पारिवारिक अनुभवों के आधार पर ही व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में भाग लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है।
चूँकि परिवार के लक्ष्यों तथा उनके प्राप्त करने की विधियों का निर्धारण मुख्यतः पारिवारिक जीवन-दर्शन के द्वारा ही होता है, अतः जीवन-दर्शन की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना परमावश्यक है।
जीवन-दर्शन का निर्माण एवं विकास
जीवन दर्शन का निर्माण अनुभवों के आधार पर होता है। वे अनुभव जीवन की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन क्रियाओं के अन्तर्गत मनोरंजनात्मक, विद्यालयी, धार्मिक, व्यावसायिक आदि क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। वे समस्त क्रिया-कलाप एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं तथा जीवन-क्रम में एकीकृत हो जाते हैं। इन क्रिया-कलापों के परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों के ज्ञान-कौशल एवं अभिवृत्तियों में वृद्धि होती है। स्वस्थ जीवन के निर्माण के लिए निम्नलिखित क्रिया-कलापों की आवश्यकता होती है-
(1) धार्मिक क्रिया-कलाप- प्रायः प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म को मानता है। जिस धर्म में उसकी आस्था हो, उस धर्म से सम्बन्धित उत्सवों का आयोजन नितान्त आवश्यक है। धार्मिक सिद्धान्तों एवं उत्सवों के परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों की मान्यताओं का निर्धारण होता है।
(2) सांस्कृतिक क्रिया-कलाप- किसी समाज या जाति-विशेष का जीवन-दर्शन सांस्कृतिक स्वरूप का निर्धारण करता है तथा उस समाज या जाति-विशेष की सांस्कृतिक परम्पराएँ आगामी पीढ़ी के सदस्यों में अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास एवं उसकी अभिवृद्धि करने की भावना का संचार करती हैं। अतः परिवार का यह उत्तरदायित्व है कि वह स्वस्थ सांस्कृतिक रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं का मिलन करते हुए परिवार के सदस्यों को उनमें दीक्षित करें।
(3) विद्यालयीन क्रिया-कलाप- विद्यालय समाज व संस्कृति का सूक्ष्म स्वरूप ही होता है। बालक को घर में तो प्रारम्भिक शिक्षा मिलती ही है, परन्तु विद्यालय भी पाठ्य सहगामी – तथा पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों के माध्यम से बालकों के जीवन-दर्शन के निर्माण में अद्वितीय कार्य करता है। परिवार का उत्तरदायित्व है कि बालकों को ऐसे ही विद्यालय में शिक्षित करे जो स्वस्थ जीवन-दर्शन के निर्माण में सहायक हो।
(4) मनोरंजनात्मक क्रिया-कलाप- व्यक्ति के जीवन-दृष्टिकोण के निर्माण में मनोरंजनात्मक क्रिया-कलापों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में मनोरंजन की व्यवस्था व्यक्ति के समुचित विकास के लिए परमावश्यक है। परिवार सदस्यों के लिए ऐसी मनोरंजनात्मक क्रियाएँ आयोजित करे, जो उसके द्वारा निर्धारित जीवन-दर्शन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। घर में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ, चलचित्र आदि जीवन-दर्शन के निर्माण के अत्यधिक प्रभावशाली साधन हैं।
(5) सामाजिक कार्यों का आयोजन- मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक गुणों की शिक्षा समाज में रहकर प्राप्त करता है। समाज के व्यक्तियों के निकट सम्पर्क में आकर ही वह इन गुणों को ग्रहण कर पाता है। परिवार का उत्तरदायित्व है कि वह समाज के अन्य व्यक्तियों अथवा समुदायों से सम्पर्क साधने के अवसर प्रदान करे। विवाह आदि सम्बन्ध समान जीवन-दर्शन रखने वाले व्यक्तियों के साथ स्थापित किए जाएँ।
उपर्युक्त क्रिया-कलाप के फलस्वरूप व्यक्ति में विशिष्ट अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। जैसे-जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे ही अनुभव-जन्य अभिवृत्तियों जीवन क्रम को निर्देशित करने का कार्य करती हैं। फलतः जीवन-दर्शन का निर्माण होता है।
जब पति-पत्नी परिवार का निर्माण करते हैं, उस समय उनकी दो विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ होती है परन्तु बाद में वे दोनों मिलकर एक तीसरे ही प्रकार की नवीन अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। ये तीनों ही प्रकार की अभिवृत्तियाँ मिलकर पारिवारिक जीवन-दर्शन का प्रारम्भ करती हैं। इन्हीं के अनुसार नूतन परिवार के वातावरण की व्यवस्था की जाती है तथा घर का वातावरण अधिकांशतः उसके सदस्यों की अभिवृत्तियों तथा आदर्शों, पूर्वाग्रहों एवं संवेगात्मक भावनाओं का निर्धारण करते हैं। माता-पिता स्वयं अपने व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करके तथा विशिष्ट प्रकार के उत्तेजकों के माध्यम से बालकों की अभिवृत्तियों पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


प्रबन्ध सिद्धान्त की विशेषताएँ | Features of management theory in Hindi


प्रबन्ध सिद्धान्त की विशेषताएँ
प्रबन्ध के सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं-
(1) केवल सामान्यीकृत कथन (Only generalized statements) – प्रबन्धकीय सिद्धान्त अन्य सामाजिक विज्ञानों के सिद्धान्तों की भाँति केवल जीवन की वास्तविक घटनाओं के विश्लेषण और मानवीय-व्यवहार के बार-बार अवलोकन पर आधारित, कुछ व्यापक या सामान्यीकृत कथन होते हैं। चूँकि मानवीय व्यवहार सदैव परिवर्तनशील होता है और किसी पूर्वानुमान के परेय होता है, और उसका अध्ययन नियंत्रित दशाओं में जीवन की विषमताओं को हटाकर नहीं किया जा सकता, अतः उसके अवलोकन के आधार पर स्थापित सिद्धान्त केवल व्यापक रूप से ही सही हो सकते हैं। वे भौतिक सिद्धान्तों की भाँति दृढ़, सुनिश्चित एवं अपरिवर्तनीय नहीं होते, बल्कि लोचपूर्ण और सापेक्ष होते हैं।
हेनरी फेयोल ने प्रारम्भ में ही प्रबन्ध सिद्धान्तों को स्थिरता और सुनिश्चतता से अलग रखने का सुझाव दिया था और कहा था कि प्रबन्धकीय सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रबन्ध के क्षेत्र में कोई चीज दृढ़ या पूर्ण नहीं होती, यह प्रश्न तो केवल अनुपात का है। एक सी परिस्थितियों में उन्हीं सिद्धान्तों का उपयोग कदाचित ही दोबारा होता है। अतः बदलती हुई विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान उनके उपयोग के समय किया जाना चाहिए, क्योकि मनुष्य भी अन्य परिवर्तनशील घटकों की भाँति भिन्न-भिन्न होते हैं एवं बदलते रहते हैं। अतः प्रबन्धकों को इन सिद्धान्तों का चतुराई से लाभ उठाना चाहिए। उनका अन्धा अनुकरण नहीं करना चाहिए।
(2) परिवर्तनशील (Dynamic)- प्रबन्धकीय सिद्धान्त स्वभाव से स्थाई नहीं होते बल्कि अस्थिर एवं परिवर्तनशील होते हैं। वे वातावरण में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं अफसरशाही के अधिकतर सिद्धान्तों को आज प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रबन्धशास्त्र एक विकासशील सामाजिक विज्ञान है और नई शोध और अध्ययन के बाद नए-नए सिद्धान्तों की स्थापना हो रही है और पुराने बदले जा रहे हैं।
(3) परिस्थित्यात्मक (Situational) – प्रबन्ध सिद्धान्त निरपेक्ष होकर परिस्थितियों के सापेक्ष होते हैं। अतः हर परिस्थिति में उनको अन्धे होकर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। टैरी के शब्दों में, “प्रबन्धकीय सिद्धान्त चुने हुए प्रबन्ध समझदारी के कैप्सूल हैं जिनका उपयोग सावधानी तथा विवेक से किया जाना चाहिए।”
(4) सार्वभौम (Universal) – प्रबन्धकीय सिद्धान्तों को सभी मानवीय संगठनों में प्रयोग में लाया जा सकता है, चाहे संगठन व्यावसायिक हों या गैर व्यावसायिक, सरकारी हों या गैर सरकारी अथवा सामाजिक हों या सांस्कृतिक। उन्हें विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक वातावरण में तथा प्रबन्ध के हर स्तर पर अपनाया जा सकता है। प्रबन्ध सिद्धान्तों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरणीय भी होता है।
प्रबन्ध सिद्धान्तों की उपयोगिता – यद्यपि प्रबन्धकीय सिद्धान्त सामान्यरूप से ही सत्य होते हैं, तथापि वे अव्यवस्था में व्यवस्था की स्थापना करते हैं। वे प्रबन्धकों को वर्तमान स्थिति के समझने एवं भविष्य के पूर्वानुमान करने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा प्रबन्धकों के ज्ञान में वृद्धि, समझदारी में स्पष्टता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है। इनसे प्रबन्ध के क्षेत्र में शोध, नए सिद्धान्तों के सृजन एवं अन्य व्यक्तियों को प्रबन्ध का प्रशिक्षण देने में सहायता मिलती है। प्रबन्धकीय सिद्धान्तों से संगठन में मानवीय व्यवहारों के अध्ययन एवं विश्लेषण में बड़ी सहायता मिलती है। और अन्त में, वे संगठन की विषम समस्याओं के सुलझाने में प्रबन्धकों के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। यदि चतुराई और विवेक से उनका उपयोग किया जाए, तो प्रबन्धक निश्चय ही एक आदर्श संगठन की स्थापना कर सकते हैं।
यद्यपि कभी-कभी इन सिद्धान्तों की आलोचना उनके अवैज्ञानिक और केवल सैद्धान्तिक होने के आधार पर की जाती है, लेकिन जैसा कि अर्नेस्ट डेल ने लिखा है, “शायद ही कोई व्यक्ति इन मार्गदर्शकों की आवश्यकता पर प्रश्न करेगा, जो अनेकों सुयोग्य व्यक्तियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप बने हैं, और इसके स्थान पर संगठन को उन सहज बुद्धि एवं क्षणिक शक्तियों, और उन व्यक्तियों, जिनका सम्बन्ध केवल किसी विशेष परिस्थिति से हैं और जिनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ज्ञान निश्चितरूप से सीमित है, के अनुभव पर छोड़ देगा।”
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


गृह प्रबन्ध के उद्देश्य | Objectives of housekeeping in Hindi


गृह प्रबन्ध के उद्देश्य
गृह प्रबन्ध द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सीमित साधनों का ध्यान रखकर लक्ष्यों को प्राप्त करता है। गृह प्रबन्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी सदस्यों के एक साथ मिल-जुलकर कार्य करने पर बल दिया जाता है। गृह प्रबन्ध के अग्रांकित महत्त्व/उद्देश्य हैं-
(1) परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति (Wants of all Family Members is Satisfied) – गृह प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य है सभी सदस्यों को सन्तुष्ट करना। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य, सुविधात्मक आवश्यकताएँ उचित गृह प्रबन्ध द्वारा सन्तुष्ट की जाती है। यदि साधन अधिक होते हैं तो विलासात्मक आवश्यकतायें भी पूरा की जा सकती हैं; जैसे-गहने लेना, A.C. लगवाना इत्यादि।
परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी आयु, लिंग, कार्य एवं शारीरिक आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन मिलना चाहिए, तभी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रह सकेगा तथा उसमें कार्यक्षमता की वृद्धि हो सकेगी। रोगावस्था में आहार की स्थिति भिन्न होती है। छोटे बालकों के उचित शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। इसी तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त एवं मौसम के अनुकूल आरामदायक वस्त्र होने चाहिए ताकि अवकाश के क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति विश्राम एवं मनोरंजन कर सके। इसके लिए गृहिणी/प्रबन्धक को विभिन्न बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे-
- भोज्य तत्वों के गुण एवं विभिन्न भोज्य पदार्थों की विशेषताएँ।
- मौसम पर उपलब्ध भोज्य सामग्रियों को वर्ष भर तक संग्रहित रखने की जानकारी तथा भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का ज्ञान।
- वस्त्रोत्पादक रेशों की जानकारी तथा मौसम के अनुकूल उपयुक्त वस्त्रों की जानकारी होना।
- मकान हवादार है और उसमें पर्याप्त स्थान है या नहीं।
- घर की साफ सफाई, व्यवस्था एवं सजावट आदि।
(2) सीमित आय से अधिक से अधिक आवश्यकतायें पूरी करना (To Satisfy Maximum Wants with Limited Income) – परिवार की आय सीमित होती है। गृह प्रबन्ध का उद्देश्य है कि सीमित आय से ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जाये।
इसके लिए गृहिणी को बजट, आय-व्यय का सही सन्तुलन, हिसाब-किताब रखना चाहिए और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत करनी चाहिए तथा पैसों का विनियोग सही ढंग से करना चाहिए। गृह प्रबन्ध से गृह प्रबन्धक आय को नियोजित ढंग से प्रयोग में लाना सीखता है।
बजट बनाकर उसी के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए। आय में कमी होने पर व्यय में कटौती कर आय-व्यय को संतुलित करना चाहिए। बजट किस तरह से बनाना है, किन-किन सामग्रियों की खरीददारी की जानी है, वस्तुएँ कहाँ से खरीदनी हैं, परिवार की मासिक आय कितनी है? आदि महत्त्वपूर्ण बातों की जानकारी, गृहिणी को होनी चाहिए। पड़ोसियों की देखादेखी, छूट का लालच या विज्ञापनों के भ्रमजाल में फँसकर अनाप-शनाप खर्च करना तथा अनावश्यक वस्तुओं की खरीददारी नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने से व्यय आय से अधिक हो जाता है तथा परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाता है।
बजट बनाते समय व आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय गृहिणी को निम्न बिन्दुओं पर गौर करना चाहिए-
1. परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं एवं रूचि का ज्ञान होना चाहिए। वे आवश्यकताएँ जो अत्यधिक महत्त्व की है, उनकी पूर्ति पहले की जानी चाहिए।
2. आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही खरीददारी की जानी चाहिए। पड़ोसियों की देखा-देखा नहीं।
3. आय को केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च नहीं कर देना चाहिए बल्कि भविष्य के लिए भी बचाकर रखना चाहिए ताकि आकस्मिक आवश्यकताओं, जैसे-रोग, बीमारी, पार्टी, शादी-विवाह आदि के अवसरों पर आर्थिक तंगी नहीं रहे।
4. महँगी वस्तु ही हमेशा उत्तम गुण वाली होती है, ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। सस्ती वस्तुओं में भी महँगी वस्तु के समान गुण विद्यमान रहते हैं। उदाहरणार्थ-सस्ते फलों व सब्जियों में वै सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं जो कि महँगे फलों एवं सब्जियों में होते हैं।
5. समान सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए।
6. गृहिणी को बाजार भाव से परिचित होने के साथ ही कौन सी वस्तुएँ किस जगह पर सस्ती मिलती हैं, इसका भी ध्यान होना चाहिए।
7. डिब्बा बंद या सील बंद सामग्री ही खरीदनी चाहिए तथा इस पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
8. समान थोक विक्रेता से खरीदना अच्छा होता है। थोक मूल्य में चीजें सस्ती मिलती हैं। साथ ही बार-बार बाजार जाने से समय, शक्ति एवं धन व्यय होता है तथा मानसिक परेशानी होती है, इन सबसे भी छुटकारा मिलता है।
9. ऐसी सामग्री जो प्रतिदिन नहीं खरीदे जा सकते हैं, जैसे- फर्नीचर, जमीन, पंखे, कूलर, पलंग, टी.वी., कम्प्यूटर, रेडियो इन्हें खरीदते समय इनकी उपयोगिता, आकर्षण एवं टिकाऊपन पर ध्यान देना चाहिए।
(3) पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखना (Family Environment should be Clean)- गृह प्रबन्ध का उद्देश्य पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ व शान्तिमय बनाये रखना भी होता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों, पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना, अनुशासन बनाये रखना, गृह प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य है।
परिवार की सफलता, घर की सुख-समृद्धि, सम्पन्नता एवं विकास गृहिणी पर ही निर्भर करता है। वह घर की संचालिका एवं निर्देशिका होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि समान आर्थिक आय एवं साधन होते हुए भी दो परिवारों के रहन-सहन, नैतिक आचरण एवं जीवन-स्तर में विभिन्नता होती है। जिस घर की गृहिणी कुशल प्रबन्धक एवं बुद्धिमान होती है उस परिवार का रहन-सहन एवं जीवन स्तर फूहड़ गृहिणी वाले परिवार की अपेक्षा ऊँचा रहता है। अतः परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम, स्नेह, सौहार्द, अनुशासन एवं पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना भी गृह प्रबन्ध का उद्देश्य होता है।
(4) पारिवारिक स्तर को बनाये रखना (To Maintain Family Standard) – गृह प्रबन्ध का उद्देश्य है कि वह परिवार के रहन-सहह्न के निर्धारित स्तर को बनाये रखने और यदि सम्भव हो सके तो उस स्तर को उठाने का प्रयत्न करे। परिवार के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि स्तर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। गृह प्रबन्ध द्वारा परिवार उन्नति करता है। गृह प्रबन्ध द्वारा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाता है जिससे परिवार का स्तर ऊँचा उठता है।
(5) गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करना (To do Home Work Skillfully) – गृह प्रबन्ध का एक अहम उद्देश्य “गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक समय पर सम्पन्न करना भी है।” यहाँ कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने से तात्पर्य है, कार्य को इस ढंग से सम्पन्न किया जाय जिससे कि समय, शक्ति एवं श्रम की बचत हो। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए गृहिणी को योजना (Planning) बना लेनी चाहिए। योजना दिन भर, सप्ताह भर, माह भर तथा वर्ष भर की बनायी जा सकती है। कार्यों को महत्त्व, तीव्रता एवं आवश्यकता के मुताबिक प्राथमिकता देते हुए सम्पन्न करना चाहिए। हाँ! योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की राय लेना तथा उनकी मदद लेना आवश्यक है। योजना को कार्यरूप देने में परिवार के सदस्यों से कौन-कौन से कार्य में सहायता मिल सकेगी, इसका भी योजना में प्रावधान होना चाहिए। योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की रूचि, कार्यक्षमता, विश्राम आदि का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए योजना बनाना ही काफी नहीं है। बल्कि कार्य करने के तरीकों एवं विधियों का ज्ञान भी गृहिणी को होना चाहिए।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
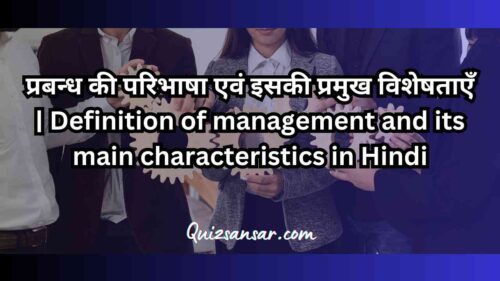
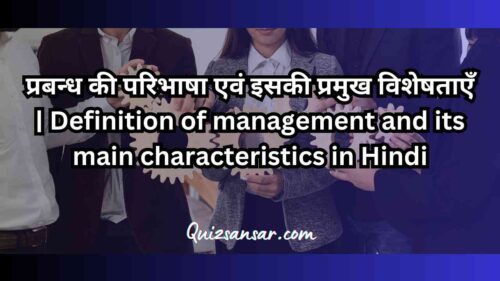
प्रबन्ध की परिभाषा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ | Definition of management and its main characteristics in Hindi


प्रबन्ध की अर्थ एंव परिभाषा
प्रबन्ध निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन के साधनों को समन्वित करने की प्रक्रिया है। “यह समूह में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा उनसे कार्य करवाने की प्रक्रिया है।” जार्ज आर. टेरी के शब्दों में, “प्रबन्ध नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियन्त्रण की विशिष्ट प्रक्रिया है।” डाल्टन ई. मैकफारलैंड के शब्दों में, “प्रबन्ध, विशिष्ट रूप से मार्गदर्शन, निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, निर्णयन, नियोजन तथा सृजन की प्रक्रिया है।” इस प्रकार प्रबन्ध मानवीय प्रयासों, कार्यों, तकनीक व अन्य संसाधनों को संयोजित करने एवं समन्वित करने की प्रक्रिया है ताकि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।
संस्था के विभिन्न संसाधनों को प्रबन्धकीय प्रक्रिया (नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण) के द्वारा समन्वित एवं रूपान्तरित करके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
प्रबन्ध कार्यों की एक श्रृंखला (A Series of Functions) है। हेनरी फेयोल लिखते हैं कि “प्रबन्ध कार्यों की एक प्रक्रिया है (Management is a process of Functions)” इसी प्रकार पीटर. एफ.ड्रकर ने कहा है कि, “प्रबन्ध एक अंग है तथा अंगों को उनके कार्यों के द्वारा ही वर्णित एवं परिभाषित किया जा सकता है।” कुछ प्रक्रियात्मक परिभाषाएँ निम्नांकित हैं-
हेनरी फेयोल के शब्दों में, “प्रबन्ध करने का आशय पूर्वानुमान करना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रित करना है।”
प्रो. आर. सी. डेविस के शब्दों में, “प्रबन्ध सर्वत्र कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं का नियोजन, संगठन एवं नियन्त्रण करने का कार्य है।”
ई.एफ.एल.बैच के अनुसार, “प्रबन्ध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी उपक्रम के निर्धारित उद्देश्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए इसकी क्रियाओं के प्रभावपूर्ण नियोजन एवं नियमन करने का उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है।”
जार्ज.आर. टैरी के अनुसार, “प्रबन्ध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण सम्मिलित हैं तथा जो व्यक्तियों एवं अन्य संसाधनों के प्रयोग से निश्चित लक्ष्यों के निर्धारण एवं पूर्ति के लिए निष्पादित की जाती है।”
डाल्टन ई. मैकफारलैण्ड के अनुसार, “प्रबन्ध एक प्रक्रिया है जिसके उत्तरदायी व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों को संयोजित करते हैं।”
इवेन्सविच एवं गिबसन के अनुसार, “संगठनात्मक लक्ष्यों की प्रभावपूर्ण प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, टेक्नालॉजी, कार्यों तथा अन्य संसाधनों को संयोजित एवं समन्वित करने की प्रक्रिया है।”
मेसकन एवं एलबर्ट के शब्दों में, “प्रबन्ध संगठनात्मक लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं में प्रबन्ध को एक विशिष्ट प्रक्रिया मानते हुए इसके तत्वों व कार्यों का विश्लेषण किया गया है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रबन्ध प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है।
प्रबन्ध की विशेषताएँ या लक्षण
1. एक प्रक्रिया अथवा कार्य (A Process of Function) – प्रबन्ध संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संयोजित करके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण व नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित हैं।
2. मानवीय प्रक्रिया (Human Process) – प्रबन्ध मानवीय व्यवहार एवं प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित है। मानव एवं उसका व्यवहार ही प्रबन्ध की मुख्य विषय-वस्तु है। पीटर एफ. ड्रकर का कथन है कि, “प्रबन्ध कार्य है, प्रबन्ध एक विधा है। किन्तु प्रबन्ध व्यक्ति भी है। प्रबन्ध की हर उपलब्धि प्रबन्धक की उपलब्धि है। हर सफलता प्रबन्धक की सफलता है। व्यक्ति प्रबन्ध करते हैं न कि “शक्तियाँ” अथवा “तथ्य” (People manage rather than forces or ‘facts’)। प्रबन्धकों की दृष्टि, समर्पण व सत्यनिष्ठा ही यह निर्धारित करती है कि वहाँ प्रबन्ध है या कुप्रबन्ध।
3. सामाजिक प्रक्रिया (Social Process) – प्रबन्ध को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के अन्तर सम्बन्धों को सम्मिलित किया जाता है। प्रबन्धक को सभी वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धों, हितों व कल्याण के लिए उत्तरदायी रहना होता है। प्रबन्ध लक्ष्यों की पूर्ति में व्यक्तियों के सहयोग एवं योगदान प्राप्त करने का उत्तरदायित्व है।
4. एकीकृत प्रक्रिया (Composite or Integrated Process) – प्रबन्ध अपने विशिष्ट कार्यों, जैसे-नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन सभी कार्यों को एक संयोजित एवं एकीकृत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। ये सभी कार्य पृथक-पृथक या एकांकी रूप से निष्पादित नहीं किये जाते हैं। ये सभी कार्य एक-दूसरे से सम्बन्धित एवं प्रभावित होते हैं।
5. सामूहिक प्रयास (Group Efforts) – प्रबन्ध सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था है। इसकी आवश्यकता व्यक्ति विशेष के प्रयासों के लिए नहीं होती है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति एक व्यक्ति की तुलना में सामूहिक रूप से कर पाना ज्यादा सुगम होता है। समूह के प्रयासों को समन्वित करने व प्रभावी बनाने के लिए प्रबन्धकीय निर्देशन एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
6. मानवीय संगठनों से सम्बन्धित (Related with Human Organisaion) – प्रबन्ध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। पशुओं, भौतिक संसाधनों, यंत्रों, भूमि-भवनों तथा अन्य निर्जीव वस्तुओं का प्रबन्ध नहीं होता। क्योंकि इन्हें निर्देश देना तथा उनका पालन करवाना सम्भव नहीं होता।
7. उद्देश्यपूर्ण (Purposeful) – प्रबन्ध संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय तथा नियंत्रण के महत्त्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, प्रबन्धकीय सफलता का मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देने व उन पर अधिकार रखने मात्र से प्रबन्धक नहीं बन जाता है, प्रबन्धक की वास्तविक पहचान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैसी (Massie) के शब्दों में, “प्रबन्धक वास्तव में क्रियाशील व्यक्ति (Managers are really people of action)”।
8. उत्प्रेरक तत्व (Catalytic Agent) – संगठन में प्रबन्ध की उपस्थिति “उत्प्रेरक तत्व” की भाँति होती है। प्रबन्धक के निर्देशन में व्यक्ति अपने प्रयासों को उत्पादक बनाते हैं। प्रबन्धक व्यक्तियों के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कार्य वितरित करते हैं तथा अभिप्रेरण के द्वारा व्यक्तियों के प्रयासों में गति लाते हैं। प्रबन्धक व्यक्तियों में उपलब्धियों के प्रति उत्साह, आकांक्षा व ऊर्जा का संचार करते हैं। जार्ज टैरी के शब्दों में “प्रबन्ध चीजों को घटित करता है (Management makes things happen)”
9. समन्वयकारी शक्ति (Integrating Force) – प्रबन्ध एक समन्वयकारी शक्ति है। वह व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने, विभिन्न वर्गों के हितों को समन्वित करने तथा संस्था के उद्देश्यों व उपलब्ध संसाधनों के मध्य एकीकरण करने की प्रक्रिया है प्रबन्धक अपने समस्त कार्यों-नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि में समन्वय के तत्व पर अधिक बल देता है। प्रबन्ध का आधारभूत स्वरूप समन्वयकारी ही है।
10. सर्वव्यापी प्रक्रिया (Universal Process) – प्रबन्ध सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इसके सिद्धान्त, कौशल व तकनीकें सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन में समान रूप से लागू होती हैं। व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक संगठनों के साथ-साथ प्रत्येक देश। एवं अर्थव्यवस्था मैं संस्थाओं की सफलता के लिए प्रबन्ध कार्य आवश्यक होता है। संगठन के विभिन्न स्तरों पर भी प्रबन्ध प्रक्रिया की समान रूप से आवश्यकता होती है।
11. पृथक अस्तित्व (Separate Entity) – आधुनिक व्यवसाय में प्रबन्ध का एक पृथक स्थान बन गया है। यह व्यवसाय के स्वामियों एवं कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों का ऐसा वर्ग हैं जिसके हाथों में प्रबन्ध व्यवस्था की, समस्त बागडोर होती है। प्रबन्ध निर्णय लेने, नेतृत्व प्रदान करने व कार्यों पर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों का एक विशिष्ट वर्ग है। प्रबन्ध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने एवं परिणामों के लिए दायी रहने वाले व्यक्तियों का एक गृषक वर्ग है। मैसी ने प्रबन्ध को “विशिष्टता प्राप्त वर्ग” (Distinguishable Group) कहा है। यह वर्ग ज्ञान, पद, स्थिति व अधिकारों में उच्च होता है। वर्तमान में प्रबन्धकों के इस विशिष्ट वर्ग को पेशेवर प्रबन्धकों के रूप में जाना जाता है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


प्रबन्ध सिद्धान्त की सार्वभौमिकता | universality of management theory in Hindi
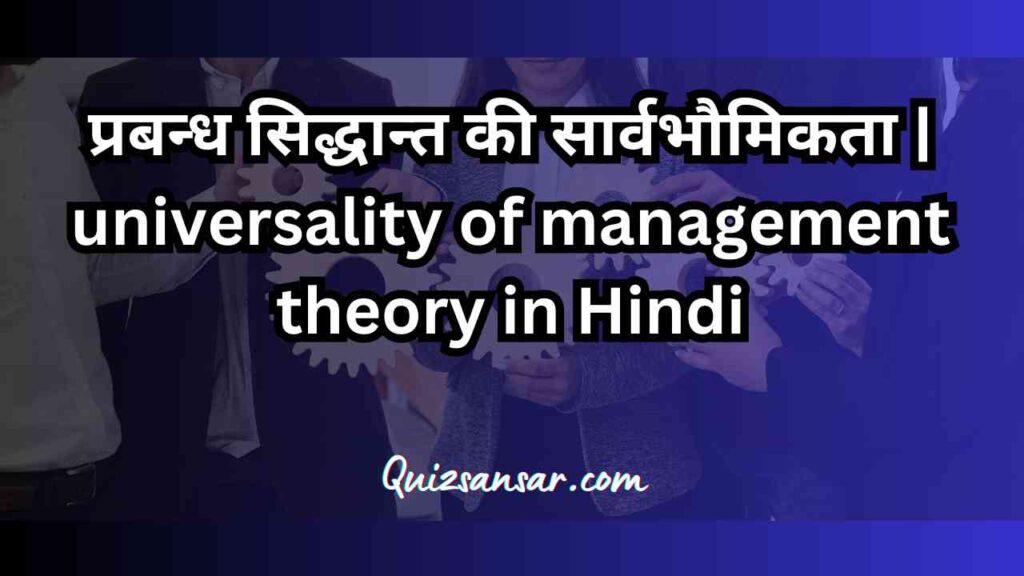
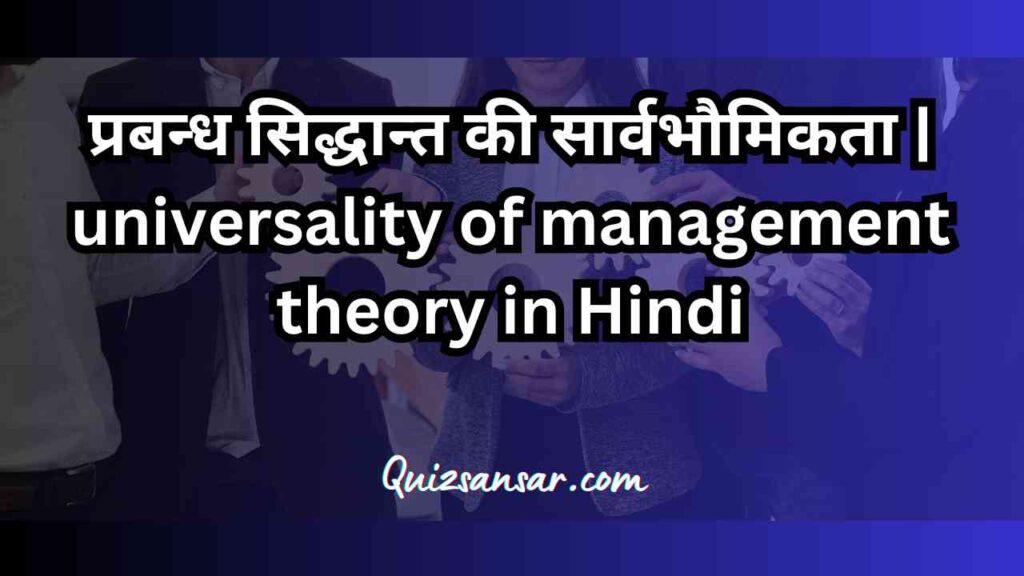
प्रबन्ध सिद्धान्तों की सार्वभौमिकता का वर्णन कीजिए।
सर्वप्रथम, हेनरी फेयोल ने प्रबन्ध प्रक्रिया के सार्वभौमिक होने पर जोर दिया। इसलिए, उन्हें प्रबन्धशास्त्र के इतिहास में सार्वभौमिक होने की संज्ञा दी गई है उन्होंने अपनी पुस्तक ‘जनरल एण्ड इन्ड्रसट्रियल मैनेजमेंट’ में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि प्रबन्ध के सिद्धान्त और कार्यों का व्यापक और सार्वभौमिक उपयोग किया जा सकता है। उनका सभी प्रकार के संगठनों (जैसे, औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सरकारी और सैनिक) में प्रयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों (जैसे उत्पादन, विपणन और वित्त) या प्रबन्ध के सभी स्तरों (जैसे, उच्च, मध्य या पर्यवेक्षण) पर किया जा सकता है। वे सभी देशों और सभी कालों में सत्य होते हैं। अर्विक, कूज एण्ड ओडेनिल, एल.ए. ऐलन, एल.आर. सैलेज, आलीवर सेल्डन, जे.डी.मूनी, सी.आई बर्नाड, सी.आर. फार लैण्ड और ए.एच. एलबर्स, आदि प्रबन्ध शास्त्रियों ने, हेनरी फेयोल की इस सोच से सहमति जताई है। कुंज एण्ड ओडेनिल के शब्दों में, “प्रबन्ध की आधारभूत विचारधारा और सिद्धान्तों का हर संगठन में उसके हर स्तर पर पर प्रयोग होता है। “एलबर्स के अनुसार, “यद्यपि संगठनों के लक्ष्यों में अन्तर होता है, तथापि उनकी प्रबन्ध प्रक्रिया एक ही रहती है। यह प्रक्रिया कारखानों, बैंकों, फुटकर विक्रय संस्थानों सैनिक संगठनों, चर्चा, विश्वविद्यालयों अस्पतालों, आदि में समान पाई जाती है।” और एल.ए.एप्ले लिखते हैं “वह व्यक्ति जो प्रबन्ध कर सकता है, किसी भी चीज का प्रबन्ध कर सकता है।”
प्रबन्ध की इस धारा के विचारकों का मानना है कि प्रबन्ध सिद्धान्तों का उपयोग अत्यन्त व्यापक रूप से किया जा सकता है। जो अनुभव और ज्ञान प्रबन्धक एक संगठन में अर्जित करता है, उसका प्रयोग वह अन्य संगठनों में भी कर सकता है। प्रबन्धकीय ज्ञान, कुशलताएँ और अनुभव हस्तांतरणीय हैं और उनका अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनका स्थानान्तरण एक विकसित देश से विकासशील देश को या एक औद्योगिक देश से कृषि प्रधान देश को किया जा सकता है और इसी तथ्य की वजह से प्रबन्धक के लिए प्रबन्धकीय योग्यताएँ, तकनीकी योग्यताएँ से, अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि ये सिद्धान्त केवल मार्गदर्शक हैं, जो लौचपूर्ण और विभिन्न परिस्थितियों में सामान्यरूप से सत्य होते हैं। इसलिए उनका उपयोग अत्यन्त चतुराई से सभी घटकों पर विचार करके किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, कुछ प्रबन्धशास्त्री प्रबन्ध की ‘सार्वभौमिकता’ की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। पीटर ड्रकर, आर्नेस्टडेल, मैकमिलन, आदि प्रबन्धशास्त्री इस विचारधारा को निम्न तर्कों के आधार पर अस्वीकार करते हैं। प्रथम प्रबन्धकीय सिद्धान्त बहुत सीमित व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकनों पर आधारित जीवन की घटनाओं के मात्र सामान्यीकृत कथन हैं, जो केवल व्यापक रूप से ही सत्य होते हैं। वैज्ञानिक कसौटी के बिना ऐसे कथनों को केवल लोककथा या लोकोक्ति से अधिक नहीं कहा जा सकता। इनमें से कुछ सिद्धान्त बहुत अस्पष्ट एवं भ्रान्तिपूर्ण हैं, तो कुछ इतने व्यापक और सामान्य कि उन्हें संगठन की विशेष समस्याओं में प्रयोग करना बहुत कठिन हैं। भ्रान्तियाँ तब और बढ़ जाती हैं जब दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त समक्ष आते हैं। उदाहरण के लिए, ‘विशिष्टीकरण का सिद्धान्त’ आदेश की एकता के सिद्धान्त के साथ असंगत है क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक अधिकारी सभी बातों का विशेषज्ञ हो। अतः ‘सार्वभौमिकता’ का दावा हास्यासपूर्ण लगता है। द्वितीय, प्रबन्ध संस्कृति से जुड़ा होता है। अतः प्रबन्ध सिद्धान्तों का प्रयोग किसी विशेष संस्कृति तक ही सीमित हो सकता है। फार्मर और रिचमैन के शब्दों में, “यदि कोई देश शक्तिशाली रूढ़िवादी, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा है, तो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक व्यवहार के प्रति विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में, आधुनिक प्रबन्धकीय विधियों को लागू करना बहुत कठिन कार्य होगा जो संसार की अधिक विवेकपूर्ण और तकनीकी परामर्श पर आधारित है। इसलिए किन्हीं ऐसे सामान्य सिद्धान्तों की खोज बेकार हैं जहाँ प्रबन्धकों को बहुत ही विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में काम करना होता है। तृतीय एक संगठन से दूसरे संगठनक के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न होते हैं और यही निर्धारित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबन्धकों की योग्यताएँ, क्षमताएँ और तकनीकें किस प्रकार की हों, अतः पीटर ड्रकर का मानना है कि प्रबन्ध की योग्यताएँ, क्षमताएँ और अनुभव जो प्रबन्धक ने एक संगठन में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित किये हैं, उनका उपयोग दूसरे संगठनों में, दूसरे उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित किये हैं, उनका उपयोग दूसरे संगठनों में, दूसरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। यह कितना हास्यास्पद है कि एक क्रिकेट टीम का सफल कप्तान एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अथवा एक कम्पनी के प्रबन्ध संचालक के रूप में उतना ही सफल होगा। एक संगठन के बदले हुए उद्देश्य, उनमें अन्तनिर्हित दर्शन और वातावरण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों, एवं व्यवहारों की अपेक्षा रखते हैं। जब एक संगठन का उद्देश्य अधिकतम लाभों को कमाना हो, और दूसरे का समाज की सेवा करना, तो किन्हीं समान सिद्धान्तों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति करना संगठनों के लिए असम्भव कार्य ही है। अतः प्रबन्ध सिद्धान्तों की सार्वभौमिकता की विचारधारा को ये प्रबन्धशास्त्री स्वीकार नहीं करते।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएँ | Characteristics of Mental Health in Hindi


मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएँ (Characteristics of Mental Health)
मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं को हम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के द्वारा समझ सकते है-
- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ
- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ
1) मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ (Characteristics of a Mentally Healthy Person) –
मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का ज्ञान मानसिक रूप से स्वस्थ या सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। ये विशेषताएँ निम्नवत हैं-
i) नियमित जीवन (Disciplined Life) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर एवं स्वाभाविक रूप से होते हैं। उनके रहन-सहन, खाने-पीने, सोने-जागने की निश्चित आदतें बन जाती हैं। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण ध्यान देते हैं। उनका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है।
ii) सामंजस्य (Adjustment) – मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों से शीघ्र ही समायोजित हो जाता है। वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को भली-भाँति समझकर उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करता है।
iii) संवेगात्मक परिपक्वता (Emotional Maturity) – ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा ईर्ष्या आदि संवेगों को नियंत्रण में रखने और उचित ढंग से प्रकट करने की योग्यता होती है।
iv) आत्मविश्वास (Self-Confidence) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास की भावना से परिपूर्ण होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर वे सभी कार्य करते हैं और सफल होते हैं।
v) आत्म-मूल्यांकन की क्षमता (Ability of Self-Evaluation) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपने गुण और दोषों का ज्ञान होता है। वह अपने किए गए उचित और अनुचित कार्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने में समर्थ होता है। वह अपने दोषों को सहजता से ही स्वीकार कर लेता है तथा स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न करता है।
vi) कार्य-क्षमता तथा कार्य में संतोष (Work Ability and Satisfaction in Work) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य में रुचि लेता है। इससे उसे आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उदाहरणार्थ- स्वस्थ विद्यार्थी जब पढ़ाई में रुचि लेता है, तब उसे आनन्द प्राप्त होता है और सफल होने पर उसे प्रोत्साहन मिलता है। इससे उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। स्वस्थ व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा रहता है, उसे उसमें रुचि होती है और उसे अपने कार्य से संतुष्टि भी होती है। इस प्रकार उसमें व्यवसाय सम्बन्धी कार्यकुशलता बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति में उपर्युक्त गुण होते हैं, वह मानसिक दृष्टि से स्वस्थ समझा जाता है।
vii) सन्तोषजनक सामाजिक समायोजन (Satisfactory Social Adjustment) – मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति समाज में अपने को भली-भाँति समायोजित कर लेता है। उसके सामाजिक सम्बन्ध बड़े सन्तुलित होते हैं। वह सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक भाग लेता है।
2) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ (Characteristics of a Mentally Unhealthy Person) –
खराब मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्नलिखित हैं-
- शंकालु, चिन्ता तथा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहना।
- संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना।
- शीघ्र परेशान हो जाना।
- अपराध की भावना से ग्रस्त रहना तथा अपने आपको कोसते रहना।
- आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति का अभाव होना।
- महत्वाकांक्षा का उचित स्तर स्थापित करने में असफल होना।
- मानसिक दबावों जैसे- निराशा, कुण्ठा, तनाव आदि से ग्रस्त रहना।
- निर्णय लेने की योग्यता का अभाव होना।
- सहनशीलता और धैर्य की कमी होना।
- जीवन तथा लोगों के विषय में गलत दृष्टिकोण बनाना।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
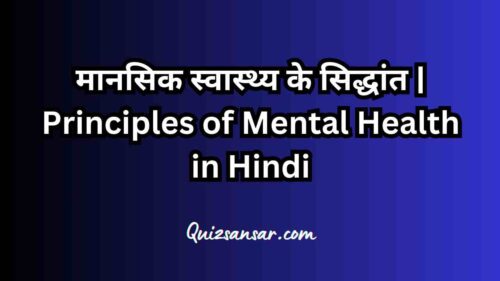
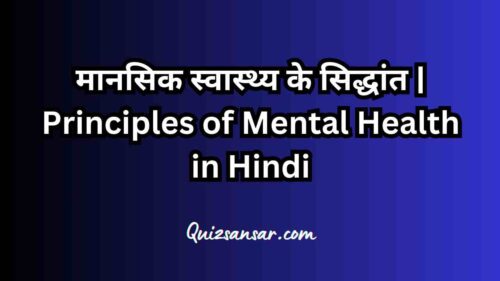
मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत | Principles of Mental Health in Hindi


मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत (Principles of Mental Health)
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं-
1) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक आंकलन एवं उपचार को प्राथमिकता के साथ कम से कम प्रतिबन्धात्मक तरीके से मूल्यांकन एवं उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।
2) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उन सेवाओं को सर्वोत्तम संभव चिकित्सीय परिणामों के बारे में लाने, वसूली और सामुदायिक जीवन में पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाना चाहिए।
3) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में सभी फैसले में शामिल होना चाहिए और इन फैसलों में शामिल होने या उनसे भाग लेने के लिए समर्थन किया जाना चाहिए और उनके विचारों और वरीयताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
4) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो जोखिम की एक डिग्री को शामिल करते हैं।
5) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकार, सम्मान और स्वायत्तता का सम्मान और प्रचार किया जाना चाहिए।
6) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य जरूरतों, जिनमें किसी भी शराब और अन्य नशीली दवाओं की समस्याएं शामिल हैं, को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए।
7) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों (चाहे वह संस्कृति, भाषा, संचार, आयु, विकलांगता, धर्म, लिंग, कामुकता या अन्य मामलों के रूप में) को पहचाना और जवाब दिया जाए।
8) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले एबोरिजिनल व्यक्तियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को पहचानने और जवाब देना चाहिए।
9) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले बच्चों और युवा व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता के रूप में पहचाना और प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसमें वयस्कों से सेवाओं को अलग से प्राप्त करना हो, जब भी यह संभव हो।
10) बच्चों, युवा व्यक्तियों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अन्य आश्रितों को उनकी जरूरतों, भलाई और सुरक्षा को पहचाना और संरक्षित होना चाहिए।
11) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए, जब भी यह संभव हो।
12) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं वाले व्यक्तियों के लिए देखभालकर्ता (बच्चों सहित) की भूमिका को मान्यता, सम्मान और समर्थित होना चाहिए।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
