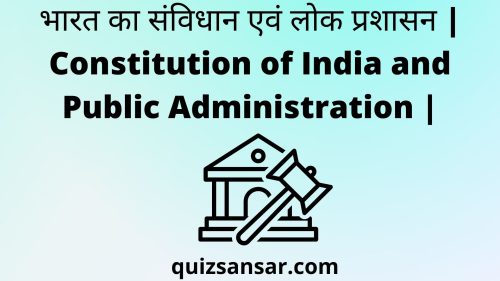
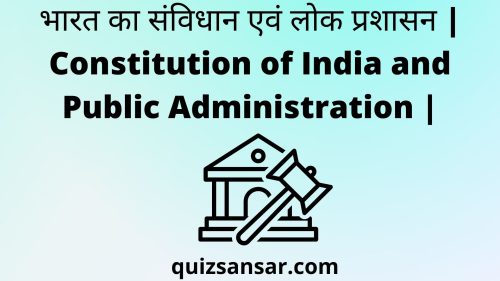
भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन | Constitution of India and Public Administration |
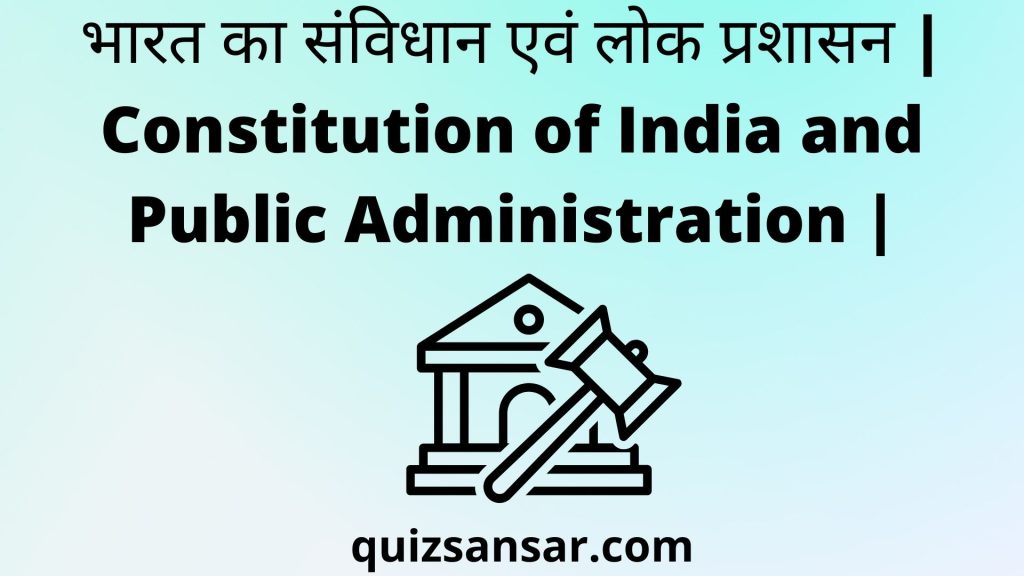
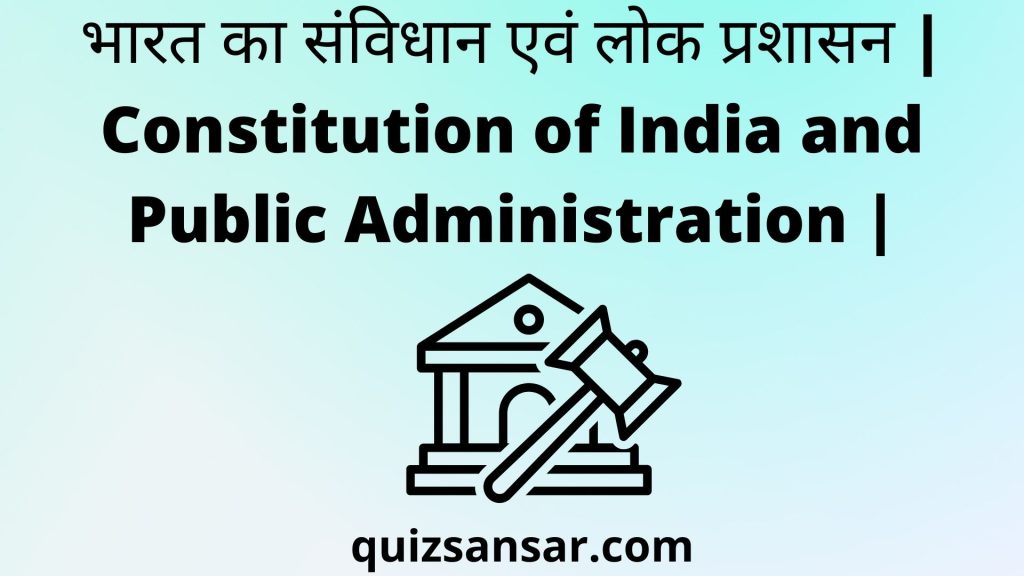
नमस्कार दोस्तों हमारी आज के post का शीर्षक है भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन | Constitution of India and Public Administration | उम्मीद करतें हैं की यह आपकों अवश्य पसंद आयेगी | धन्यवाद |
Table of Contents
भारतीय संविधान
- कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 ई. में किया गया।
- संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में प्रारम्भ किया गया। डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- 11 दिसम्बर, 1946 ई. को बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- 13 दिसम्बर, 1946 ई. को पं. जवाहरलाल नेहरू ने ‘उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियाँ बनाई गई। इसमें ‘प्रारूप समिति’ प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने की।
- प्रारूप समिति में डॉ. अम्बेडकर के अतिरिक्त एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान (1948 ई. में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी.टी. कृष्णामाचारी) और एन. माधवराव अन्य सदस्य थे। बी. एन. राब को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
- संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महोने और 18 दिन का समय सगा।
- संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। संविधान 26 नवम्बर, 1949 को तैयार हो गया था, किन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
- 1930 से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन ‘स्वाधीनता दिवस’ के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी, 1950 को प्रथम गणतन्त्र दिवस’ मनाया गया।
- संविधान सभा को अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई. को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
- मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के ‘जनक’ के रूप में जाना जाता है।
भारतीय संविधान के स्रोत
- ब्रिटिश संविधान संसदीय शासन प्रणाली, विधि-निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता।
- दक्षिण अफ्रीकी संविधान संविधान संशोधन प्रणाली।
- कनाडा का संविधान संघीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन |
- अमेरिकी संविधान प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतन्त्रता न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति उच्चतम तथा उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात |
- ऑस्ट्रेलियायी संविधान प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केन्द्र-राज्य सम्बन्ध |
- जर्मनी का बाइमर संविधान राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार |
- जापानी संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली |
- रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य |
- फ्रांसीसी संविधान गणतन्त्र |
- आयरलैण्ड का संविधान राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन |
- गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं।
स्मरणीय तथ्य
- संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज (तिरंगा) का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ‘जन-गण-मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।
- बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वन्दे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
- 26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चित्र के रूप में स्वीकार किया |
- भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च, 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक सम्वत पर जाधारित है।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ
- लिखित एवं लोक-निर्मित संविधान
- विभिन्न संविधानों से उद्धृत
- नम्य एवं अनम्य का मिश्रण
- विश्व का सर्वाधिक लम्बा व विस्तृत संविधान
- एकात्मक संघात्मक शासन का समन्वित रूप
- मौलिक अधिकारों को न्यायिक प्रकृति
- स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली
- लोकतान्त्रिक व्यवस्था
- एकल नागरिकता एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- 42 विधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तान में निरपेश समाजवादी पंथ निरपेक्ष , समाजवादी तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए।
- संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
- प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानन्द भारती बाद (1973) में इसे संविधान का अंग माना गया है।
राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त
- भारतीय संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 36-61 में राज्य के लिए नीति-निर्देशित वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये संकल्पना आयरलैण्ड संविधान से अभिप्रेरित (Motivated) है। जिन्हें आपरलैण्ड के सामाजिक सिद्धान्तों के समान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है।
- अनुच्छेद 36 मे नीति-निर्देशक तत्वों की परिभाषा एवं अनुच्छेद 37 में अन्तर्विष्ट तत्वों का लागू होना दर्शाया गया है।
- अनुच्छेद 38 के अनुसार, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना तथा भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना भारतीय राज्य का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 39 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे तथा इसके अन्तर्गत निम्न उल्लेख है –
- राज्य सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- राज्य का स्वामित्व एवं प्रबन्धन इस प्रकार करे जिससे कति का सर्वोत्तम साधन बन सके।
- राज्य को यह निर्देश करता है कि वह धन के समान वितरण का प्रावधान करे जिससे समाजवादी संकल्पना को बल मिल सके।
- अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि ये ग्राम पंचायत की स्थापना करें।
- अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत राज्य का दायित्व है कि वह कुछ दशाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन-सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे।
- अनुच्छेद 42 एवं 43 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य कामगारों को निर्वाह मजदूरी काम की मानवोचित दाएँ प्रसूति सहायता प्रदान करें। यह शिष्ट जीवनस्तर तथा अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए।
- अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि यह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता का निर्माण करे।
- अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह 6 या तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए।
- अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिया अन्य दर्बल वर्ग को शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि करना राज्य को कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत यह राज्य का दायिता है कि वह लोगों के जीवन-स्वर को ऊंचा उठाने हेतु उनके पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करे।
- अनुच्छेद 48 के अन्तर्गत राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गो-वध का प्रतिषेध करे।
- अनुच्छेद 45 (क) में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्यानो तथा वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 50 के अन्तर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को किया गया है।
- अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत राज्य का यह फर्त्तव्य होगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करे।
मूल अधिकार
- भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार सम्बन्धी प्रावधान है।
- भारतीय संविधान में नागरिकों को सात मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किये गए थे, लेकिन विधान संशोधन 1978 ई. द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 ‘क’ के अन्तर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
- अनुछेद 21 के अन्तर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है (अगस्त, 2017) |
- अनुच्छेद 21(A) राज्य 6-14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे म से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। (86ष संशोधन, 2002 ) ।
मौलिक कर्त्तव्य
- मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करते हैं, देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योगदान दें।
- भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं यह कल्पना पूर्व सोवियत संघ (रूस) से ली गई है।
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के तहत समाहित किया गया है। संविधान अनुच्छेद 61 (क) मौलिक कर्तव्यो का प्रावधान करता है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से तो नहीं कराए जा सकते, किन्तु संविधान के निर्वाचन में मूल्यवान दिशादर्शन के रूप से महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्त्तव्य
भारतीय संविधान के भाग (IV) (क) के अनुच्छेद 51 (क) के भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है –
- भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि ये भारतीय संविधान का पालन विधान के आदशों संस्थाओं, राष्ट्रीय राष्ट्रगान का सम्मान करें।
- भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे देश की सम्प्रभुता एकता अखण्डता की रक्षा करे तथा इसे रखें।
- भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रेरित करने वाले आदर्शों को उनका अनुपालन करें।
- भारतीय नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे।।
- भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि ये धर्म, भाषा, प्रदेश या जाति वर्ग से परे होकर, समरसता और भातृत्व की भावना का विकास करे। उन प्राओं का त्याग करें जो स्थियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
- भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य कवे भारतीय संस्कृति को समुद्र परम्परा की रक्षा करे, उसे बढ़ावा दे तथा उसको रक्षा करें।
- भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण (न नदी, अन्य जीव) की रक्षा करे, उनका बर्दन करे उनके प्रति दया भाव रखें |
- भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए मानववादी दृष्टिकोण रखे थानार्जन सुधारवादी भावनाओं का विकाश करें |
- भारतीय नागरिको का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे अहसात्मक विचार को आत्मसात कर हिंसा से दूर रहे।
- भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की प्रगति में गत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए निरन्तर प्रयत्न करें |
- भारतीय माता-पिता का संरक्षक का यह कर्तव्य है कि ये छ वर्ष से तक उम्र के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का प्रदान करें। (यह मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 61 (क) मे जोड़ा गया है।
संसदीय प्रणाली
- भारत का संविधान केन्द्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 24 और 28 केन्द्र में संसदीय और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों के व्यवस्था करता है।
- संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा कारकावेस्टमेस्टर भी कहा जाता है।
- भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से की गई है। इस तरह ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित है।
- अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्री लंका आदि देशों में अर्थपक्षीय वा राष्ट्रपति सरकार/ गैर संसदीय व्यवस्था प्रचलित है।
संसदीय सरकार की विशेषताएँ
भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है-
- नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका
- बहुमत प्राप्त दल का शासन
- सामूहिक उत्तरदायित्व
- राजनीतिक एकरूपता
- दोहरी मसदस्यता (विधायिका एवं कार्यपालिका)
- प्रधानमन्त्री का नेतृत्व
- निचले सदन का विघटन
- गोपनीयता आदि
संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश
भारतीय संविधान के भाग के अध्याय (अनुच्छेद 52-76 तक) के अधीन संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है
राष्ट्रपति
- भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है।
- भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र काही कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि प्रधानमन्त्री तथा उसके मन्त्रिपरिषद् में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों निहित है।
- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानपरिषदों के सदस्य शामिल नहीं किये जाते
- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है।
- राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित विवादों को छानबीन तथा निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है।
- महाभियोग प्रस्ताव समद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है।
- कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति संचालन सम्बन्धी शक्ति सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि।
- विधायी शक्तियाँ विधायी क्षेत्रका प्रशासन सदस्यों का मनो अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि।
- संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन्न संकट से निबटने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है, जिसका प्रयोग ह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल को सलाह से करता है, ये शक्तियां है
- युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति सम्बन्धित आपातकालीन व्यवस्था (अनुच्छेद 352)।
- राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था (अनुच्छेद 366)
- वित्तीय संकट (अनुच्छेद 300)।
स्मरणीय तथ्य
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो कार्यकाल तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे |
- नीलम संजीव रेड्डी निधि निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति के टी.वी. गिरिएकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय की चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी।
- वी.वी. गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।
- राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे।
- डॉ. जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे।
- श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
उपराष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपतिका पदेन सभापति होता है।
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्वको एकमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किन्तु यह स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़कता है या उसे राज्यसभा के तात्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से है। जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है |
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किन्तु राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है।
- राष्ट्रपति को अनुपस्थिति तथा अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है।
- जी.एस.पाठक, बी. डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्ला, कृष्णकान्त, भैरोसिंह शेखावत और हामिद अंसारी राष्ट्रपती पद पर पदोन्नतिन पाने वाले उपराष्ट्रपति रहे डॉ. कृष्णकान्त एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ।
मन्त्रिपरिषद् और प्रधानमन्त्री
- मन्त्रिपरिषद में एक प्रधानमन्त्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य मन्त्री होते हैं। 91वैधानिक संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र परिषद्को सदस् संख्या लोकसभा (केन्द्र के लिए) और विधानसभा (राज्यों के लिए) की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है।
- मन्त्रिपरिषद् में तीनों श्रेणिया, कैबिनेट मन्त्री, राज्यमंत्री और उपयो के मन्त्री सम्मिलित होते हैं, लेकिन मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नव निर्वाचित लोकसभा के बहुत दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है।
- प्रधानमन्त्री को वही वेतन तथा भने दिये जाते हैं, जो के सदस्यों को प्रदान किये जाते हैं।
- प्रधानमन्त्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति तथा मन्त्रिपरिषद् केबीच सम्बन्ध स्थापित करता है।
- प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् का निर्माण, विभिन्न मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी करता है।
भारत की संसद
- भारत की राष्ट्रपति राज्य लोकसभा में मिलकर बनी है।
- संसद के निम्न मदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं।
राज्यसभा
- संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है।
- राज्यमा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।
- राज्यसभाएका स्थायी सदन है। यह कभी भम नहीं होता बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक करते है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकर्षक है।
लोकसभा
- लोकसभा को अधिकतम सदस्य संख्या 552 [530 (राज्य में निर्वाचित) +20 (संघीय क्षेत्र से निर्वाचित) +2 (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल-भारतीय सदस्य)] हों सकती है |
- वर्तमान में 104 सेमविधान संशोधन, 2019 के लोकसभा मे समुदाय के प्रदत आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु प्रधानमन्त्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपतिद्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है |
राज्य सरकार
राज्यपाल
- राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किन्तु वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- वह मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- उसे राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका के निम्न सदन ‘विधानसभा’ को भंग करने की शक्ति है। यदि राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल रहा हो. तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
मुख्यमन्त्री
- मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतया विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमन्त्री विधानसभा का नेता होता है।
- वह मन्त्रिपरिषद् का निर्माण, विभिन्न मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में परिवर्तन करता है।
विधानपरिषद्
- राज्य के विधानमण्डल के उच्च सदन को विधानपरिषद कहा जाता है।
- वर्तमान समय में विधानपरिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है।
- विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है। विधानपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष पर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्यों का निर्वाचन होता है।
- संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के विधानपरिषद् में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, किन्तु साथ ही यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती।
- वधानपरिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है –
- 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं।
- 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते है।
- 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 से अध्यापन कार्य कर रहे हो।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनका साहित्य, विज्ञान, कता, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो।
विधानसभा
- विधानसभा राज्य के विधानमण्डलका निम्न सदन है। विधानसभा के का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य के मतदाताओं द्वारा होता है। राज्य की सभा के सदस्यों को अधिकतम 500 और है।
- गोवा (40), मिजोरम (40) और सिक्किम (32) इसके अपवाद है। (अनुच्छेद 371 )।
- विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों (SC) और में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। (अनुच्छेद-332)।
- साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसको पहली बैठक से पाँच वर्ष का होता है, किन्तु राज्यपाल द्वारा मुख्यमन्त्री के परामर्श पर इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
- केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार के उद्देश्य से 1983 में केन्द्र सरकार द्वारा न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया को अध्यक्षता आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग द्वारा केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सुधार हेतु कई संस्तुतियाँ दी गई थीं केन्द्र राज्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विवरण निम्न है-
- अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाता है। इसमें राज्यों के मन्त्रियो भी शामिल किया जाता है।
- संघ के राजस्व के स्रोत संघ के राजस्य स्रोतों का उल्लेख संघ सूची में किया गया है। संघ की आय के प्रमुख स्रोत है-निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क, कृषि आय के अलावा आप पर कर आदि।
- राज्यों राजस्व के स्रोत कृषि भूमि पर कर, भूमि एवं भवनों पर कर वाहनों पर कर पशुओं तथा नौकाओं पर कर बिक्री कर बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर आदि।
- केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध करों की वसूली एवं उसके बंटवारे द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं।
- कुछ कर संघ द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं, परन्तु उन्हें राज्यों पों को सौंप दिया जाता है। यथा उत्तराधिकार कर, समाचार पत्रों पर कर आदि।
- कुछ कर संघ द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं, परन्तु उनका संग्रहण एवं उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है। उदाहरणस्वरूप बिल, विनिमयों, प्रोमिसरी नोटो, हुण्डियो, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क आदि।
- कुछ कर सघ द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं, परन्तु उनका विभाजन केन्द्र एवं राज्यों बीच कर दिया जाता है। इन करों में प्रमुख है-आप कर, दवा तथा शृंगार सम्बन्धी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर लगाया गया उत्पादन शुल्क आदि।
- संघ की सम्पत्ति पर राज्यों द्वारा कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद द्वारा विधि के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान न कर दिया जाए। रेलवे अथवा भारत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के बिना राज्यों द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा
- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विकास योजनाओं को लागू करने, बाड़, कम्प एवं स्थिति से निपटने हेतुबजटघाटे को दूर करने के उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है,
क्षेत्रीय परिषद्
भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रको पाँच क्षेत्रों में बांटा गया है।
आपको हमारी यह post कैसी लगी नीची कमेन्ट करके अवश्य बताएं |
यह भी जाने
भारतीय संविधान क्या है ?
संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में प्रारम्भ किया गया। डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
11 दिसम्बर, 1946 ई. को बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
13 दिसम्बर, 1946 ई. को पं. जवाहरलाल नेहरू ने ‘उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियाँ बनाई गई। इसमें ‘प्रारूप समिति’ प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने की।
प्रारूप समिति में डॉ. अम्बेडकर के अतिरिक्त एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान (1948 ई. में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी.टी. कृष्णामाचारी) और एन. माधवराव अन्य सदस्य थे। बी. एन. राब को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महोने और 18 दिन का समय सगा।
संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। संविधान 26 नवम्बर, 1949 को तैयार हो गया था, किन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
1930 से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन ‘स्वाधीनता दिवस’ के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी, 1950 को प्रथम गणतन्त्र दिवस’ मनाया गया।
संविधान सभा को अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई. को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के ‘जनक’ के रूप में जाना जाता है।
भारतीय संविधान के स्त्रोत क्या है ?
दक्षिण अफ्रीकी संविधान संविधान संशोधन प्रणाली।
कनाडा का संविधान संघीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन |
अमेरिकी संविधान प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतन्त्रता न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति उच्चतम तथा उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात |
ऑस्ट्रेलियायी संविधान प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केन्द्र-राज्य सम्बन्ध |
जर्मनी का बाइमर संविधान राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार |
जापानी संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली |
रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य |
फ्रांसीसी संविधान गणतन्त्र |
आयरलैण्ड का संविधान राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन |
गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं।
भारतीय संविधान के स्मरणीय तथ्य कौन-कौन से हैं ?
रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ‘जन-गण-मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।
बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित ‘वन्दे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चित्र के रूप में स्वीकार किया |
भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च, 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक सम्वत पर जाधारित है।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?
विभिन्न संविधानों से उद्धृत
नम्य एवं अनम्य का मिश्रण
विश्व का सर्वाधिक लम्बा व विस्तृत संविधान
एकात्मक संघात्मक शासन का समन्वित रूप
मौलिक अधिकारों को न्यायिक प्रकृति
स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली
लोकतान्त्रिक व्यवस्था
एकल नागरिकता एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
42 विधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तान में निरपेश समाजवादी पंथ निरपेक्ष , समाजवादी तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए।
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानन्द भारती बाद (1973) में इसे संविधान का अंग माना गया है।
- Irrigation – Introduction, Importance, Definition & Objectives
- History and development of agriculture in ancient India – Agriculture in civilization era
- AGRO – CLIMATIC ZONES OF INDIA BY ICAR
- National and International research institute of India and their Full forms
- DEFINITION OF AGRICULTURE , MEANING AND ROLE OF AGRONOMY
- पर्यायवाची शब्द | Paryavachi Shabd |
- पं० प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय | हिन्दी निबंध | PT. PRATAP NARAYAN MISHRA KA JIVAN PARICHAY |
