

मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएँ | Characteristics of Mental Health in Hindi


मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएँ (Characteristics of Mental Health)
मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं को हम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के द्वारा समझ सकते है-
- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ
- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ
1) मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ (Characteristics of a Mentally Healthy Person) –
मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का ज्ञान मानसिक रूप से स्वस्थ या सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। ये विशेषताएँ निम्नवत हैं-
i) नियमित जीवन (Disciplined Life) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर एवं स्वाभाविक रूप से होते हैं। उनके रहन-सहन, खाने-पीने, सोने-जागने की निश्चित आदतें बन जाती हैं। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण ध्यान देते हैं। उनका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है।
ii) सामंजस्य (Adjustment) – मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों से शीघ्र ही समायोजित हो जाता है। वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को भली-भाँति समझकर उनसे उसी प्रकार का व्यवहार करता है।
iii) संवेगात्मक परिपक्वता (Emotional Maturity) – ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा ईर्ष्या आदि संवेगों को नियंत्रण में रखने और उचित ढंग से प्रकट करने की योग्यता होती है।
iv) आत्मविश्वास (Self-Confidence) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास की भावना से परिपूर्ण होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर वे सभी कार्य करते हैं और सफल होते हैं।
v) आत्म-मूल्यांकन की क्षमता (Ability of Self-Evaluation) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को अपने गुण और दोषों का ज्ञान होता है। वह अपने किए गए उचित और अनुचित कार्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने में समर्थ होता है। वह अपने दोषों को सहजता से ही स्वीकार कर लेता है तथा स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न करता है।
vi) कार्य-क्षमता तथा कार्य में संतोष (Work Ability and Satisfaction in Work) – मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य में रुचि लेता है। इससे उसे आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उदाहरणार्थ- स्वस्थ विद्यार्थी जब पढ़ाई में रुचि लेता है, तब उसे आनन्द प्राप्त होता है और सफल होने पर उसे प्रोत्साहन मिलता है। इससे उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। स्वस्थ व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा रहता है, उसे उसमें रुचि होती है और उसे अपने कार्य से संतुष्टि भी होती है। इस प्रकार उसमें व्यवसाय सम्बन्धी कार्यकुशलता बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति में उपर्युक्त गुण होते हैं, वह मानसिक दृष्टि से स्वस्थ समझा जाता है।
vii) सन्तोषजनक सामाजिक समायोजन (Satisfactory Social Adjustment) – मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति समाज में अपने को भली-भाँति समायोजित कर लेता है। उसके सामाजिक सम्बन्ध बड़े सन्तुलित होते हैं। वह सामाजिक कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक भाग लेता है।
2) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ (Characteristics of a Mentally Unhealthy Person) –
खराब मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्नलिखित हैं-
- शंकालु, चिन्ता तथा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहना।
- संवेगात्मक रूप से अस्थिर होना।
- शीघ्र परेशान हो जाना।
- अपराध की भावना से ग्रस्त रहना तथा अपने आपको कोसते रहना।
- आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति का अभाव होना।
- महत्वाकांक्षा का उचित स्तर स्थापित करने में असफल होना।
- मानसिक दबावों जैसे- निराशा, कुण्ठा, तनाव आदि से ग्रस्त रहना।
- निर्णय लेने की योग्यता का अभाव होना।
- सहनशीलता और धैर्य की कमी होना।
- जीवन तथा लोगों के विषय में गलत दृष्टिकोण बनाना।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
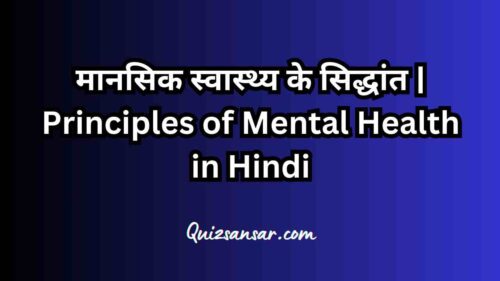
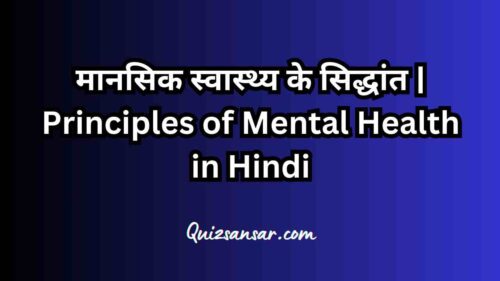
मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत | Principles of Mental Health in Hindi


मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत (Principles of Mental Health)
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं-
1) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक आंकलन एवं उपचार को प्राथमिकता के साथ कम से कम प्रतिबन्धात्मक तरीके से मूल्यांकन एवं उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।
2) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उन सेवाओं को सर्वोत्तम संभव चिकित्सीय परिणामों के बारे में लाने, वसूली और सामुदायिक जीवन में पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाना चाहिए।
3) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में सभी फैसले में शामिल होना चाहिए और इन फैसलों में शामिल होने या उनसे भाग लेने के लिए समर्थन किया जाना चाहिए और उनके विचारों और वरीयताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
4) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो जोखिम की एक डिग्री को शामिल करते हैं।
5) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकार, सम्मान और स्वायत्तता का सम्मान और प्रचार किया जाना चाहिए।
6) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य जरूरतों, जिनमें किसी भी शराब और अन्य नशीली दवाओं की समस्याएं शामिल हैं, को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए।
7) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों (चाहे वह संस्कृति, भाषा, संचार, आयु, विकलांगता, धर्म, लिंग, कामुकता या अन्य मामलों के रूप में) को पहचाना और जवाब दिया जाए।
8) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले एबोरिजिनल व्यक्तियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को पहचानने और जवाब देना चाहिए।
9) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले बच्चों और युवा व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता के रूप में पहचाना और प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसमें वयस्कों से सेवाओं को अलग से प्राप्त करना हो, जब भी यह संभव हो।
10) बच्चों, युवा व्यक्तियों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अन्य आश्रितों को उनकी जरूरतों, भलाई और सुरक्षा को पहचाना और संरक्षित होना चाहिए।
11) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन, उपचार और वसूली के बारे में निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए, जब भी यह संभव हो।
12) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं वाले व्यक्तियों के लिए देखभालकर्ता (बच्चों सहित) की भूमिका को मान्यता, सम्मान और समर्थित होना चाहिए।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक | Factors Affecting Mental Health in Hindi
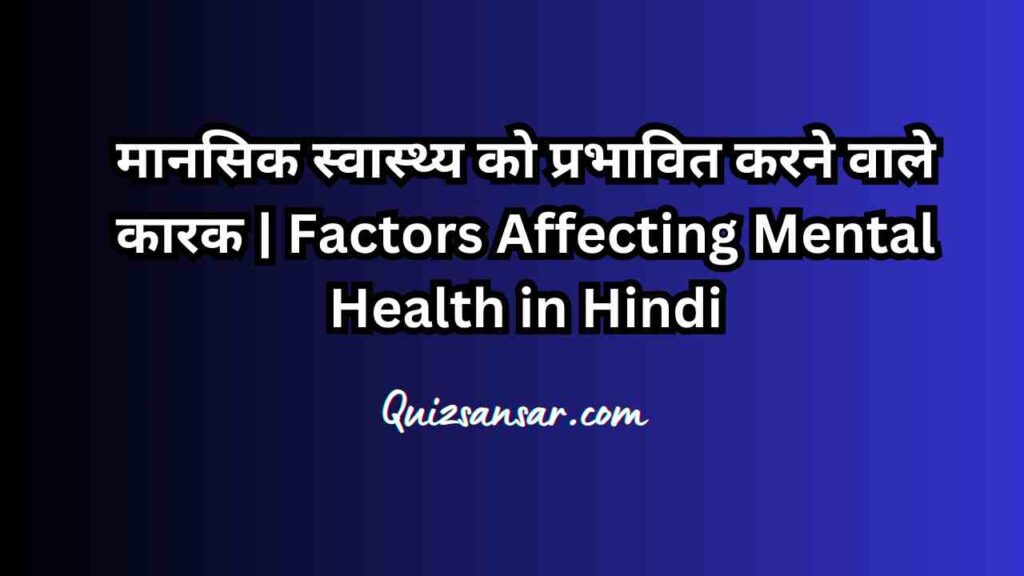
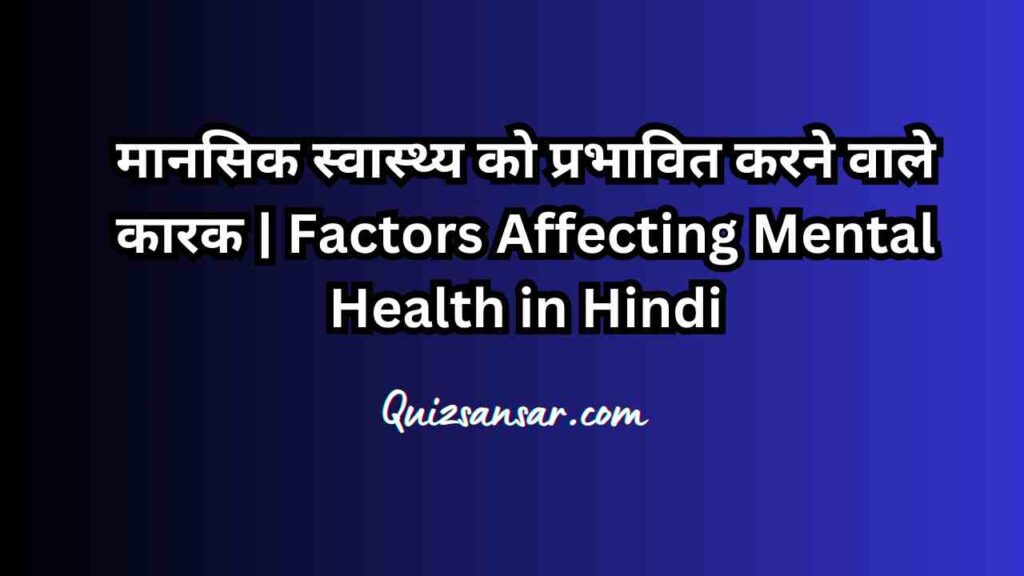
मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Mental Health)
जीवन में बहुत सारी घटनाएँ अनुकूल या प्रतिकूल रूप से व्यक्ति के मन को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है-
1) छात्रों / बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Mental Health of Students/Children) –
छात्रों/बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-
i) वंशानुक्रम (Heredity)- कई मानसिक रोग वंशानुगत होते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि किसी परिवार का कोई सदस्य मानसिक रोग से ग्रस्त होता हैं तो वह सदस्य उस परिवार के बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अतः दोषपूर्ण वंशानुक्रम के कारण ही बालक में मानसिक दुर्बलता की कमी के रोग पाए जाते हैं।
ii) शारीरिक स्वास्थ्य (Physical Health)- शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अंतरंग सम्बन्ध हैं। जो बालक शारीरिक रूप से कमजोर अथवा दोष का शिकार है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं होगा।
iii) समाज का प्रभाव (Impact of Society)- बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर समाज के संगठन एवं वातावरण का भी प्रभाव पड़ता हैं। वह समाज जो संगठित नहीं होता है, वहाँ पर बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता हैं।
iv) शारीरिक दोष या विकार का प्रभाव (Impact of Physical Disorder or Defect)-शारीरिक विकार बालक में दुर्घटना या बीमारी के कारण आ सकता हैं। शारीरिक दोष के कारण बालक में हीनता की भावना विकसित हो जाती हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं।
v) पारिवारिक कारक (Family Factor)- परिवार का बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता हैं। परिवार में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता हैं। जैसे- डांटना, मारना, लड़ाई, झगड़ा, प्रेम, स्नेह आदि इन सभी व्यवहार का असर बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हैं।
vi) शैक्षणिक कारक (Academic Factor)- समाज एवं परिवार की तरह स्कूल भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं। स्कूल में पक्षपातपूर्ण, वैयक्तिक मूल्यों की अवहेलना, मनोरंजन एवं पुस्तकालय के अभाव तथा सहगामी क्रियाओं का आयोजन न होने से बालक का विकास नहीं होता हैं जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक स्वास्थ्य दूषित हो जाता हैं।
vii) मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factor)- मानसिक स्वास्थ्य में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक भी आते हैं जो मानसिक विकार उत्पन्न करने में सहायक हैं, जिन्हें मानसिक संघर्ष, चिन्ता, थकान आदि कहा जाता हैं। इन सभी कारकों का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हैं।
2) शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Mental Health of Teachers) –
शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-
i) नौकरी की सुरक्षा का अभाव (Lack of Job Security) – आजकल सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की अवस्था बड़ी दयनीय हो गयी है। उनका व्यवसायिक भविष्य अन्धकारमय हो गया है। अध्यापकों की नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं होती है। सरकार के द्वारा नौकरी में कुछ सुरक्षा प्रदान की गयी है, लेकिन बहुत से प्रबन्धकों ने अभी तक इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया हैं।
ii) शैक्षिक उपकरणों का अभाव (Lack of Teaching Materials) – विद्यालय में शिक्षण सहायता के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री की व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है। शिक्षण सामग्री के अभाव में शिक्षक को अधिक बोलना व समझाना पड़ता है। इससे वह मानसिक रूप से अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।
iii) अपर्याप्त वेतन (Insufficient Wages) – अध्यापकों की मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख कारण है कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है, इसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं रहती। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
iv) अधिक कार्यभार (Excessive Workload) – विद्यालय में अध्यापकों को अधिक कार्यभार का वहन करना पड़ता है। उन्हें कक्षा में अनुशासन, अध्यापन हेतु पाठ तैयार करना, लिखित कार्य देना एवं उसको चेक करना, उपस्थिति रजिस्टर तैयार करना, परीक्षा पुस्तिकाओं की जाँच एवं रिपोर्ट-कार्ड बनाना इत्यादि कार्य करने पड़ते हैं। प्रायः अत्यधिक कार्यभार पड़ने से उसे सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। अतः अत्यधिक कार्य भार उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
v) पारिवारिक कठिनाइयाँ (Family Problems) – शिक्षक के ऊपर अपने परिवार के भरण-पोषण का भी भार रहता है उसको विद्यालय से पर्याप्त वेतन प्राप्त न होने के कारण वह अपने परिवार की आवश्यकताएँ पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। जिस कारण पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अतः वह उचित रूप से शिक्षण कार्य नही कर पाता है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय | Measures to Improve Mental Health in Hindi


मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय (Measures to Improve Mental Health)
आधुनिक समय में व्यक्ति शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक रोगों से अधिक ग्रसित है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के ज्ञान के साथ-साथ उसकी रोकथाम की भी उतनी ही आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं-
- छात्रों/बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय
- शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय
छात्रों/बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय (Measures to Improve Mental Health of Students/Children)
बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का उत्तरदायित्व परिवार, विद्यालय तथा समाज का हैं। ये कारक न केवल बालक की असमायोजन से रक्षा करते हैं। वरन् उसकी समायोजन क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं-
1) पारिवारिक कारक (Family Factors) – परिवार मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अग्रलिखित रूप से सहायक हो सकता है-
i) माता-पिता का व्यवहार (Parental Behaviour) – माता-पिता के उचित व्यवहार का असर सबसे ज्यादा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। वह परिवार जहाँ माँ अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है तथा पिता अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो उन परिवार के बालकों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अतः माता-पिता का व्यवहार बालक के मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग देता है।
ii) परिवार का वातावरण (Home Environment) – बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए परिवार तथा परिवार के सदस्यों को शान्तपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। यदि परिवार का वातावरण उत्तम होगा तो इसका बालक के मानसिक स्वास्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
iii) विकास के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना (Providing Essential Facilities for Development) – मानसिक रूप से स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना बालक में 6 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाती है। परिवार को बालक के मानसिक योग्यता एवं स्वास्थ्य के विकास के लिए पूर्ण अवसर, सुविधा और वातावरण प्रदान करना चाहिए।
2) विद्यालय के कारक (School Factors) – बालक के व्यक्तित्व का विकास परिवार से शुरू होते हुए विद्यालय तक चलता है, तथा विद्यालय में विभिन्न साधनों के द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न पन्न किया जाता है। अतः विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-
i) अच्छा वातावरण (Healthy Environment) – विद्यालय के वातावरण का बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय में सभी क्रियाएँ पूर्ण एवं उचित साधनों द्वारा होती हैं तो यह बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती हैं।
ii) अनुशासन (Discipline) – बालक में आत्मानुशासन की भावना जागृत करने का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। विद्यालय का अनुशासन जनतन्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होना चाहिए।
iii) सन्तुलित और उपयुक्त पाठ्यक्रम (Balanced and Appropriate Curriculum) – पाठ्यक्रम बालक की आयु, रुचि और आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का चयन करना उपयुक्त होगा जो बालक के विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देते हो।
iv) शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार (Affectionate Behaviour of Teachers)- शिक्षक को बालकों से नम्र, शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यदि शिक्षक बालक से स्नेहपूर्ण व्यवहार करेगा तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालेगा।
v) अच्छी नागरिकता की शिक्षा (Education of Good Citizenship) – बालकों को अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा विद्यालय से प्रारम्भ हो जाती है। बालकों में अच्छे गुणों के विकास के द्वारा उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता की जा सकती है।
शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय (Measures to Improve Mental Health of Teachers)
शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय निम्नलिखित हैं-
1) कार्यभार में कमी (Reduced Work Load) – यदि शिक्षकों के कार्य भार को कुछ कम कर दिया जाए तो वह कम समय में अधिक एवं अच्छा कार्य करेंगे जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठेगा।
2) उचित वेतन (Appropriate Wages) – अध्यापकों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों को नियमित रुप से उचित वेतन दिया जाए। जिससे उनकी पारिवारिक एवं आर्थिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके अतः उचित वेतन प्राप्ति से वह तनावमुक्त रहेंगे व अधिक रूचि से कार्य करेंगे।
3) नौकरी की सुरक्षा (Job Security) – अध्यापकों को उनकी सेवाएं सुरक्षित प्राप्त हों अर्थात् अल्पावधि की न हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें पेंशन देने की उचित व्यवस्था की जाए। ये सुविधायें उसको भविष्य चिंता से मुक्त रखेंगी।
4) विद्यालय का वातावरण (Healthy Atmosphere in School) – विद्यालय में किसी भी अध्यापक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी के साथ समान एवं उचित व्यवहार होना चाहिए। विद्यालय का अनुकूल वातावरण शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करता है।
5) प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग (Cooperation of Training Institutions) – अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर को ऊँचा उठाने में प्रशिक्षण संस्थाओं का विशेष महत्व है। ये प्रशिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की सहायता करती है।
6) आत्मविश्वास में वृद्धि (Boosting Self-Confidence) – अध्यापकों को स्वयं के आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहिए ताकि वह विषम परिस्थितियों में धैर्य रखे और उनका सामना स्वयं कर सके। गेट्स एवं अन्य के अनुसार, यदि शिक्षक स्वयं को भली भांति समझ ले और स्वयं को वैसा ही मान ले, जैसा वह है। यदि वह उत्साहपूर्वक अपने जीवन निर्देशन में सक्रिय भाग ले, यदि वह स्वयं को वैसा ही मापे जैसा कि वह अपने जीवन को सही निर्देशन देने हेतु पूर्ण उत्साहित है और सक्रियता से भाग लेता है, तो वह अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


INDIA vs AUS: इंडिया की हार को नहीं सह पाया बंगाल के राहुल


INDIA vs AUS: इंडिया की हार को नहीं सह पाया बंगाल के राहुल 23 साल की उम्र में हार के सदमें से कर ली आत्महत्या
भारत में क्रिकेट मैच बस एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक इमोशंस है। इसमें उतार-चढ़ाव कई बार इतने गहरे हो जाते हैं कि इंसान जिंदगी से हाथ खो बैठता है। इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में हार जाती है, 10 मैच जीतती है। 11वां मैच फाइनल होता है और एक हार के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। हर किसी की आँखें नम हैं। शुभमन गिल ने पोस्ट किया है कि 16 घंटे बीत गए हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि हम क्यों हारते हैं।
लेकिन पश्चिम बंगाल के बांकुरा के एक 23 साल के लड़के राहुल ने इंडिया की हार से हुआ दुख सहकर आत्महत्या कर ली। यह एक दुखद और परेशान करने वाली खबर है। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन इसे देखकर अनगिनत लोगों को बहुत दुःख हो रहा है। इंडिया में 1.4 अरब की जनसंख्या के बीच बहुत से लोग इस हार के बाद उदास हैं, खाने का स्वाद नहीं आ रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, हाइलाइट्स नहीं देख रहे, और क्रिकेट वीडियो की तकिलीफ महसूस कर रहे हैं। यह कहानी बहुत परेशान कर रही है।
सुमन गिल ने ट्वीट करते हुए क्या कहा ?
भारत को ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में मिली हार के बाद शुभमन गिल ने एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर अपनी भावनाएं लिखी हैं. शुभमन गिल ने एक इमोशनल कर देने वाला पोस्ट किया.
शुभमन गिल से लेकर तमाम लोगों ने इस असफलता की बात की है। शुभमन गिल ने ट्वीट किया, “16 घंटे हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी दर्द उतना ही है जितना पिछली रात हुआ था. “ इससे यह प्रतित होता है कि क्रिकेट ने लोगों को कैसे प्रभावित किया है और इस हार का आभास कराता है।
Been almost 16 hours but still hurts like it did last night. Sometimes giving your everything isn’t enough. We fell short of our ultimate goal but every step in this journey has been a testament to our team’s spirit and dedication. To our incredible fans, your unwavering support in our highs and lows means the world to us. This isn’t the end, it’s not over until we win. Jai Hind – Shubman Gill Tweet:
जब हमारा देश मैच हारता है, तो सभी दुःखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यह खबर जो है, वह और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। यह दिखाता है कि भारत में क्रिकेट कितनी अहमियत रखता है और लोग क्यों इतने भावनात्मक होते हैं। इससे उठता है सवाल कि लोग सब कुछ कैसे भूल जाते हैं?
हालांकि यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जीवन आगे बढ़ता है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। खोई हुई चीजों को भूलकर आगे बढ़ना ही जीवन है। यह एक खेल है, और हार-जीत होती रहती है। इसे एक खेल के रूप में ही देखना चाहिए, और उसका आत्महत्या से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण कामों में लगाना चाहिए और हार-जीत को सिर्फ एक हिस्सा मानना चाहिए, न कि जीवन का सब कुछ।
मुझे आशा है कि लोग इस सघन मुद्दे को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और आत्महत्या को रोकने के लिए सामाजिक उपायों की ओर बढ़ेंगे। खेलों को आत्महत्या से जोड़ना सही नहीं है और हमें इस पर सावधानी बनाए रखनी चाहिए।
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
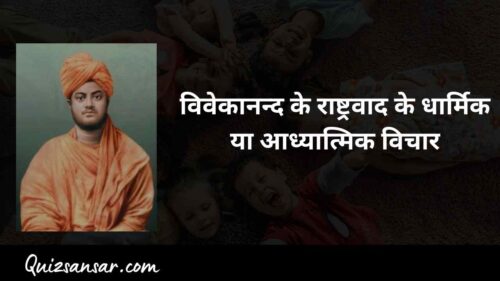
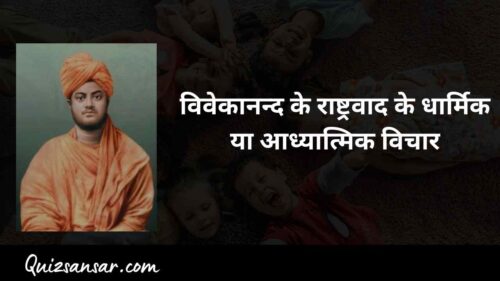
विवेकानन्द के राष्ट्रवाद के धार्मिक या आध्यात्मिक विचार


विवेकानन्द के राष्ट्रवाद के धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों की व्याख्या कीजिए ।
राजनीति में विवेकानन्द का कोई विश्वास न था और न ही उन्होंने किन्ही राजनीतिक कार्य-कलापों में कभी भाग लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि “मैं न राजनीतिक हूँ, न राजनीतिक आन्दोलनकारी। मैं केवल आत्म-तत्व की चिन्ता करता हूँ। जब वह ठीक रहेगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जायेंगे।” फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिन्तकों से कहीं आगे ले जाता है। विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धान्त नींव का निर्माण किया। वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदण्ड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का ही निषेध करने के समान है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा।
विवेकानन्द हीगल की तरह राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे। उनके मतानुसार भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को विजित करना होगा। उनका कहना था “एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है। उसे पचिश्म पर आध्यात्मिक विजय करनी है।”
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को विवेकानन्द इसी रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। चूँकि वे एक संन्यासी थे इसीलिए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे और यदि खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार में बन्द कर देती जिसका परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्हें सबसे अधिक प्रिय था उसमें विघ्न पड़ता। विवेकानन्द भारतीय राष्ट्रवाद के सन्देशवाहक थे। जब उन्होंने देशवासियों को कहा- “बंकिमचन्द्र को पढ़ो तथा उनके सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो” “जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो।”
(2) स्वन्त्रता सम्बन्धी धारणा- विवेकानन्द का स्वतन्त्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनका कहना था कि सम्पूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतन्त्रता को हो खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, “जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त – चिन्तन और कार्य में स्वतन्त्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है, उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा।” उन्हीं के शब्दों में, “शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उनकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हैं। जो सामाजिक नियम इस स्वतन्त्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतन्त्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है।”
विवेकानन्द ने स्वतन्त्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और यह इच्छा व्यक्त की कि समाज में सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिये। उन्हीं के शब्दों में, “प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धर्म का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाये और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुँचायें और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो।”
विवेकानन्द के मतानुसार स्वतन्त्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धान्त था, उपनिषद्कारों ने शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतन्त्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था। स्वामीजी ने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपने एक जोशीले देशभक्तिपूर्ण और उच्च भावनायें उत्पन्न करने वाले व्याख्यान में अपने देश को इस प्रकार सम्बोधित किया था, “हे भारत, क्या तू दूसरों की संस्थाओं की नकल पर निर्भर रहेगा और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए व्यग्र रहेगा और पद के अधिकार के लिये मूढ़ दासता, घृणित नृशंसता में फँसा रहेगा ? क्या तू इस प्रकार की निर्लज्ज कायरता से वह स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है, जिसके योग्य केवल वीर होते हैं? यह न भूल कि तेरा समाज महानता की भ्रान्ति में भूला हुआ है। अपने गिरे हुए गरीब, अज्ञ, भंगी, मेहतर को न भूल, वे तेरे रक्त-मांस हैं, वे तेरे भाई हैं। हे वीर, सहाय कर, गर्वित हो कि तू भारतीय है और बड़े वर्ग के साथ यह कह कि, मैं भारतीय हूँ और हरेक भारतीय मेरा भाई है, भारत की भूमि मेरे लिए सर्वोच्च स्वर्ग है भारत की भलाई मेरी भलाई है।”
(3) शक्ति और निर्भयता का सन्देश- विवेकानन्द ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का सन्देश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते और न अपने अधिकार की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। विवेकानन्द ने अप्रत्यक्ष रूप से यह सन्देश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं।
(4) व्यक्ति की गरिमा- विवेकानन्द के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिये। उन्हीं के शब्दों में, “आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहं का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे।”
(5) अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल- विवेकानन्द ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्व दिया। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार हों। मानवप्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने तथा अपने अधिकारों के लिये आग्रह करे, उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम शुभ की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग कर दे। इसलिये यद्यपि विवेकानन्द स्वयं भिक्षु और संन्यासी थे, किन्तु उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया।
(6) आदर्श राज्य की धारणा- विवेकानन्द के अनुसार, मानवीय समाज पर चार वर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (मजदूर) बारी-बारी से राज्य करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिये है। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है और इस काल में कला एवं सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुँच जाती है। उसके बाद वैश्य राज्य आता है। उनमें कुचलने और खून चूसने की मौन शक्ति अत्यन्त भीषण होती है। अन्त में आयेगा मजदूरों का राज्य । उसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी। सभ्यता का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा परन्तु असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति कम होते जायेंगे।
विवेकानन्द के अनुसार यदि ऐसा राज्य स्थापित करना सम्भव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार-भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके तो वह आदर्श राज्य होगा।
(7) अन्तर्राष्ट्रीयतावाद एवं विश्वबन्धुत्व- विवेकानन्द उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे। उनके अन्तर्राष्ट्रीयतावादी और विश्वबन्धुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया, “जहाँ अन्य सब प्रतिनिधि अपने-अपने धर्म में ईश्वर की चर्चा करते रहे वहाँ केवल विवेकानन्द ने ही सबके ईश्वर की बात की।” वे मानव-मानव के भेद को अस्वीकार करते थे, वे हिन्दू धर्म तथा भारत से असीस प्यार करते थे किन्तु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी। उन्होंने एक बार कहा था, “निस्सन्देह मुझे भारत से प्यार है पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि निर्मल होती जाती है। हमारे लिये भारत या इंग्लैण्ड या अमेरिका क्या है? हम तो उस ईश्वर के सेवक है जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सोचता है।”
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
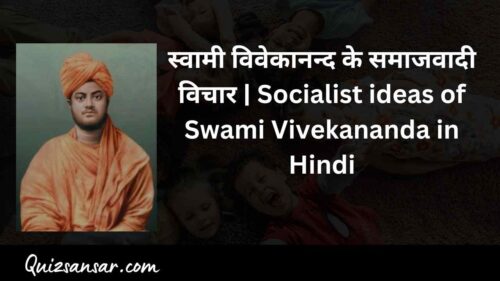
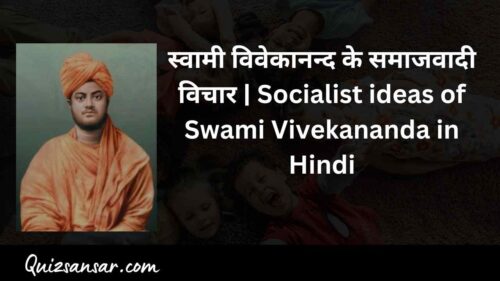
स्वामी विवेकानन्द के समाजवादी विचार | Socialist ideas of Swami Vivekananda in Hindi
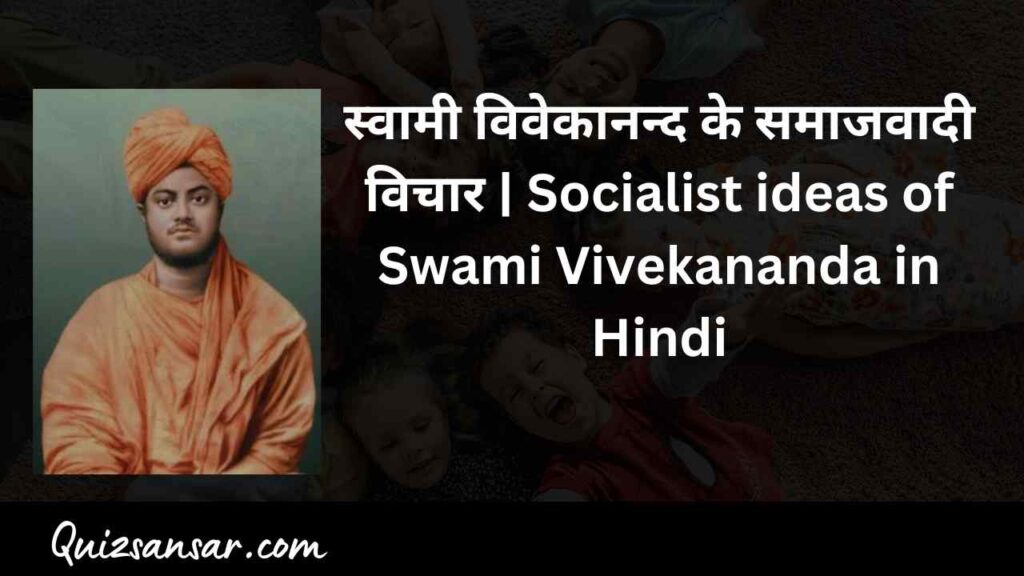
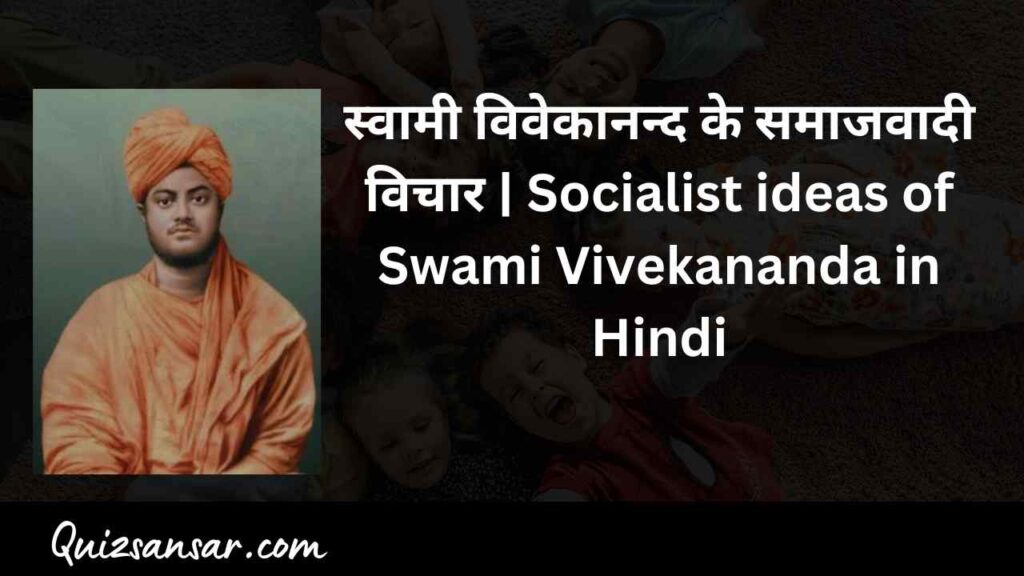
स्वामी विवेकानन्द के समाजवादी विचारों की विवेचना कीजिए।
विवेकानन्द सामाजिक सुधारों के प्रति सजग और इस सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट थे। उनके हृदय में एक आँधी थी, उनकी आत्मा में एक आग थी और वह भारत को जगाना तथा ऊपर उठाना चाहते थे। सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी लगन इसी तथ्य से स्पष्ट है कि उनका आग्रह था कि सामाजिक संघ कार्यों को अध्यात्म साधना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।
समाज का सावयवी रूप- स्पेन्सर के समान समाज के सम्बन्ध में विवेकानन्द की भावना सावयवी थी। उनके अनुसार अनेक व्यक्तियों का समूह समष्टि कहलाता है और अकेला व्यक्ति उसका एक भाग है। व्यक्ति की भांति समष्टि का भी अपना आंगिक जीवन है, उसका भी विकासशील मस्तिष्क और आत्मा है। सामाजिक प्रगति तभी सम्भव है जब उसके घटक कुछ बलिदान करें क्योंकि त्याग अथवा बलिदान किये बिना समष्टि के कल्याण की कामना करना व्यर्थ है। विवेकानन्द के अनुसार मनुष्य और समाज का अस्तित्व शुभ कार्य के लिये है, अतः शुभ कार्य करके ही व्यक्ति अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। व्यक्ति केवल अपने लिये नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है और इसी में उसकी मनुष्यता छिपी है। चूँकि समाज विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसके विकास के लिये व्यक्तियों द्वारा आत्म-त्याग अनिवार्य है। मानवीय सम्बन्धों का अन्तिम लक्ष्य और परिणाम सामूहिक कल्याण होना चाहिए, केवल व्यक्तिगत सुख नहीं।
विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके सामाजिक विषमताओं और बुराइयों के उन्मूलन के उपाय बताये। वे सामाजिक संगठन और सामाजिक मामलों में धर्म को सम्मिलित करने के विरुद्ध थे और इसी कारण वे जात-पात, सम्प्रदाय और छुआ-छूत तक सब तरह की विषमताओं के विरुद्ध थे। उनके मुख्य सामाजिक विचारों को अग्रलिखित शीर्षकों में वर्णित किया जा सकता है-
(1) रूढ़िवादिता और अस्पृश्यता – विवेकानन्द ने भारतीय समाज में व्याप्त अश्पृश्यता और रूढ़िवादिता की तीव्र आलोचना को रूढ़िवादिता को उन्होंने ‘रसोई धर्म’ और अस्पृश्यवाद कहकर उसकी भर्त्सना की। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा- “भारत में यह रोना धोना सच है कि हम बड़े गरीब है; परन्तु गरीबों के लिए कितनी दानशील संस्थायें हैं? भारत के करोड़ों गरीबों के दुःख और पीड़ा के लिए कितने लोग असल में रोते हैं? क्या हम मनुष्य हैं? हम उनकी जीविका और उन्नति के लिये क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं, उनकी संगति से दूर भागते हैं क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों ब्राह्मण- भारत की नीच और दलित जनता के लिये क्या कर रहे हैं? ‘मत छू’ – ‘मत छू’ एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथ हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं” “
(2) दलितों का उत्थान – स्वामी जी जाति प्रथा के विरोधी तथा गरीबों और दलितों के लिये उनमें असीम सहानुभूति थी। वे वास्तव में समाजवादी थे जो अमीर और गरीब के भेद को ठुकराकर पद दलितों को सीने से लगाने का सन्देह देते थे और अपने कर्ममय जीवन में, अपने मिशन में उन्होंने यह करके भी दिखाया। उनकी ललकार थी- “गरीब और अभावग्रस्त पीड़ित और पद दलित, सब आओ, हम सब रामकृष्ण की शरण में हैं।” इससे स्पष्ट होता है कि स्वामीजी व्यावहारिक और कार्य करने वाले थे न कि केवल उपदेशक इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा, “हम पूजा के इस ताम-झाम को यानी देव मूर्ति के सामने शंख फूँकना, घण्टा बजाना और आरती करना छोड़ दें। हम शास्त्रों का पठन-पाठन और व्यक्तिगत मोक्ष के लिये सब तरह की साधनाओं को छोड़ देंगे और गाँव-गाँव में जाकर गरीबों की सेवा करें। प्रत्येक को एक सामान्य धरातल पर ले जाना चाहिये। उच्चतर को निम्नस्तर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। एक ओर आदर्श है ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श है चाण्डाल और चाण्डाल को उठाकर उसे ब्राह्मण स्तर तक ले आना ही सम्पूर्ण कार्य है। उनका सन्देश है कि निम्नतर जातियों को संस्कृति दो।
(3) बाल-विवाह विरोधी- विवेकानन्द ने बाल-विवाह की भर्त्सना की और कहा, “जिस प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणिग्रहण होता है, उसके साथ मैं किसी प्रकार के सम्बन्ध रखने में असमर्थ हूँ…… बाल विवाह से असामयिक सन्तानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में सन्तान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं, उनकी दुर्बल और रोगी सन्तान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है आज घर-घर इतनी अधिक विधवायें पायी जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है, यदि बाल-विवाहों की संख्या घट जाये तो विधवाओं की संख्या भी स्वयमेव घट जायेगी।”
(4) जाति प्रथा के विरोधी- विवेकानन्द ने प्रचलित जातिवाद को देश और समाज के लिए हानिकारक मानते हुए कहा कि जाति-भेद केवल एक सामाजिक विधान है जिसकी उपयोगिता पूर्व में चाहे जो भी हो, अब तो वह भारतीय वायुमण्डल में दुर्गन्ध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। जाति भेद का नाश तभी सम्भव है जब लोग अपने खोये हुए सामाजिक व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करेंगे। जाति-प्रथा के विनाश के विषय में स्वामीजी की दृष्टि बहुत पैनी थी। उन्होंने भाँप लिया था कि आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा के युग में जाति-विचार अपने आप भ्रष्ट होता जा रहा है, उसके नाश के लिए किसी धर्म-विज्ञान की आवश्यकता नहीं।” वे जाति का अर्थ सकारात्मक रूप लेते हुए ‘विचित्रता की स्वछन्द गति’ मानते थे। उनके मतानुसार, “जाति का मूल अर्थ था- सैकड़ों वर्षों तक यही अर्थ प्रचलित रहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अपने विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता। चूँकि भारत ने जाति-सम्बन्धी इस भाव का परित्याग कर दिया, अत: वह अधःपतन की स्थिति में आ गया। उनके अनुसार आजकल का वर्ण विभाग अर्थात जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में रुकावट है। सचमुच, इसने सच्ची जाति अर्थात् विचित्रता की स्वच्छन्द गति को रोक दिया है।” जातिवाद भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था, उसे समूल नष्ट करना सम्भव नहीं था। अतः एक यथार्थवादी विचारक के रूप में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाये और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाये।
विवेकानन्द पुरोहित कर्मकाण्ड और परम्परावादी ब्राह्मण के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्त के विरोधी थे। उन्होंने पुरोहित धर्म की कटु शब्दों में निन्दा की, क्योंकि उससे सामाजिक अत्याचार को कायम रखने में सहायता मिलती थी और जनता की उपेक्षा होती थी। उन्होंने परम्परावादी ब्राह्मणों के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्त का खण्डन किया क्योंकि यह सिद्धान्त शूद्रों अर्थात् देश की बहुसंख्यक जनता को वैदिक ज्ञान के लाभ से वंचित करता है। उनके अनुसार “सभी मनुष्य समान हैं, और सभी को आध्यात्मिक अनुभूति तथा वैदिक ज्ञान का अधिकार है।”
(5) यूरोपीयकरण के विरोधी- विवेकानन्द ने सामाजिक जीवन में यूरोप का अनुकरण करने की कटु आलोचना की इस सम्बन्ध में उनके शब्दों के अतिरिक्त दूसरी अच्छी व्याख्या हो ही नहीं सकती। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा- “हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होना चाहिए। विदेशियों ने जो जीवन प्रणाली हमारे ऊपर थोप दी है उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, ऐसा करना असम्भव भी है। परमात्मा को धन्यवाद है कि यह असम्भव है, हमें तोड़-मरोड़ कर अन्य राष्ट्रों की आकृति का नहीं बनाया जा सकता। मैं अन्य जातियों की संस्थाओं की निन्दा नहीं करता, वे उनके लिये अच्छी हैं, किन्तु हमारे लिये अच्छी नहीं हैं। उनकी विद्यायें, उनकी संस्थायें तथा परम्परायें भिन्न है और उन सबके अनुरूप ही उनकी वर्तमान जीवन प्रणाली है। हमारी अपनी परम्परायें हैं और हजारों वर्षों के कर्म हमारे साथ हैं। इसलिये स्वभावतः हम अपनी ही प्रकृति का अनुकरण कर सकते हैं, अपनी ही लकीर पर चल सकते हैं, और हम वही करेंगे। हम पाश्चात्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए पश्चिम का अनुकरण करना निरर्थक है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
