

मानव अभिवृद्धि एवं विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार | Types of Changes in Human Growth and Development in Hindi


मानव अभिवृद्धि एवं विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार (Types of Changes in Human Growth and Development)
बालक के विकास में निरन्तर होने वाले परिवर्तन उसके शरीर तथा मन दोनों से सम्बन्धित होते हैं। हरलॉक (Hurlock) ने विकास में होने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है-
1) आकार में परिवर्तन (Change in Size)
यह परिवर्तन शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के विकास में दिखाई देता हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य भार, ऊंचाई, मोटाई, आदि में निरन्तर होने वाले परिवर्तन हैं। बालक के आन्तरिक भागों में भी परिवर्तन होता हैं। जैसे- हृदय, फेफड़ा, आंते आदि में वृद्धि होती है। यह सभी अंग शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमावश्यक हैं। आयु बढ़ने के साथ-साथ बालक का शब्द भण्डार एवं स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है।
2) अनुपात में परिवर्तन (Change in Proportion)
बालक का शारीरिक विकास सभी अंगों में एक समान रूप से नहीं होता है। नवजात शिशु के अन्य अंगों की अपेक्षा उसका सिर काफी बड़ा होता है परन्तु जैसे-जैसे शिशु का शारीरिक विकास होता हैं अर्थात् शिशु बढ़ता है वैसे-वैसे उसका सिर शरीर के अनुपात में तुलनात्मक रूप से कम बढ़ता है। इसी प्रकार बालक के मानसिक विकास में भी अन्तर दिखाई देता है । बाल्यावस्था की शुरुआत में बालकों की रुचि आत्म-केन्द्रित होती है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है उसके साथ-साथ उनकी रुचि का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है।
3) पुरानी आकृतियों का लोप (Disappearance of Old Images)
बालक में धीरे-धीरे उसकी बचपन की आकृतियों का लोप होना प्रारम्भ हो जाता है। बचपन में बालों तथा दांतों का लोप भी स्पष्टतम रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार बालक द्वारा बचपन में बोली जाने वाली भाषा जैसे- बलबलाना आदि का भी लोप हो जाता है। बचपन में बालक चलने की शुरुआत रेंगकर या घिसट कर करता है। धीरे-धीरे बचपन का रेंगना तथा घिसटना (creeping and crawling) भी समाप्त हो जाता हैं अर्थात् इसका लोप हो जाता हैं।
4) नई आकृतियों की प्राप्ति (Acquisition of New Images)
विकास की अवस्था में पुरानी आकृतियों में परिवर्तन के साथ ही नई आकृतियों का बनना प्रारम्भ हो जाता है। यह परिवर्तन बालक की शारीरिक तथा मानसिक दोनों अवस्थाओं में क्रमशः दिखाई देता है। यह परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया (learning process) तथा परिपक्वन (maturation) के परिणामस्वरूप होता है। आयु बढ़ने के साथ ही लैंगिक चेतना का भी विकास होता है। किशोरावस्था में बालकों एवं बालिकाओं में अनेकों शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त | Principles of Human Growth and Development in Hindi


मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त (Principles of Human Growth and Development)
विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। गैरिसन के अनुसार, “विकास अपने क्रम में कुछ नियमों का पालन करता है जिनको विकास के सिद्धान्तों के रूप में जाना जाता है।” बालक के विकास की पहचान तथा विभिन्न अवस्थाओं में उसकी विशेषताओं एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए विकास के सिद्धान्तों का अध्ययन आवश्यक है। विकास के कुछ सिद्धान्त निम्न प्रकार से हैं-
1) परस्पर संबंध का सिद्धान्त (Principle of Inter-relationship)-
इस सिद्धान्त के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में एक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बालक के जब किसी एक गुण में विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए तीव्र बौद्धिक विकास वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र तथा मंद बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी मन्द गति से होता है।
2) व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त (Principle of Individual Differences) –
इस सिद्धान्त के अनुसार, बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है परंतु विकास की गति में भिन्नताएं पायी जाती हैं अर्थात् उनकी वृद्धि एवं विकास वैयक्तिक भिन्नता लिए होता है। सभी बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास की अपनी एक स्वाभाविक गति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित अवधि में सभी बालकों में विकास भी समान गति से ही हो। बालक और बालिकाओं में भी विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। डगलस और हॉलैण्ड के अनुसार, “विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवनकाल में बनी रहती है।”
3) वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धान्त (Principle of Interaction of Environment and Heredity) –
मानव विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं प्रखर होती हैं। वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव तथा उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। वातावरण में वे समस्त बाह्य परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। स्किनर के अनुसार, “वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है।”
4) समान प्रतिमान का सिद्धान्त (Principle of Uniform Pattern) –
गैसेल और हरलॉक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के अनुसार एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है। उदाहरण के लिए- सभी बालकों का जन्म के बाद विकास सिर से पैरों की ओर होना। बालक का गत्यात्मक एवं भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। गैसेल ने बताया कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। हरलॉक के अनुसार, “प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं।”
5) सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धान्त (Principle of General to Specific Responses ) –
बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है। बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रारम्भ होती हैं। हरलॉक इस सिद्धान्त के समर्थक थे । जन्म के उपरांत प्रारम्भ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है लेकिन बड़े होने पर उसी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करना शुरू कर देता है। शारीरिक विकास की ही तरह संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी छोटा बच्चा केवल सामान्य संवेगात्मक उत्तेजना प्रदर्शित करता है। भय, प्रेम, क्रोध जैसे संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मानसिक विकास के होने के पश्चात् ही होती है।
6) विकास की दिशा का सिद्धान्त (Principle of Direction of Development) –
इस सिद्धान्त को केन्द्र से परिधि की ओर सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके अनुसार बालक के विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। व्यक्ति के सिर का विकास सर्वप्रथम होता है फिर यह पैरों की ओर बढ़ता है अर्थात् जो अंग सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास उतना ही बाद में होगा। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में। यही बात बालक के अंगों पर नियन्त्रण पर भी लागू होती है। बालक जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे-धीरे खिसककर चलता है और 1 वर्ष की आयु में वह खड़ा हो जाता है।
7) सतत् विकास का सिद्धान्त (Principle of Continuous Development) –
इस सिद्धान्त के अनुसार विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरन्तर चलता रहता है। बालक के जन्म के शुरुआती तीन-चार साल में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है, जो बाद में मंद होती जाती है। इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक स्किनर के अनुसार, “किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता। विकास एकाएक न होकर सतत् होता है।” उदाहरण के लिए दांतों का विकास भ्रूणावस्था में प्रारम्भ होता है, जो जन्म के 6 महीने बाद ही मसूढ़ों से बाहर निकलते हैं।
8) रेखीय न होकर पेंचदार विकास का सिद्धांत (Principle of Spiral Development) –
व्यक्ति में विकास एक रेखा के रूप में सीधा न होकर पेंचदार होता है। विकास एक सीधी रेखा में न होकर कई कड़ियों में विभक्त रहता है जो आगे-पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। विकास के कई पहलू होते हैं तथा उनके विकसित होने की गति और प्रक्रिया भी विशिष्ट होती है।
9) पूर्वानुमानता का सिद्धान्त (Principle of Predictability) –
व्यक्ति में विकास का क्रम समान रहता है लेकिन उसकी गति भिन्न होती है फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों पर परीक्षण करके उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की रुचि एवं व्यवहार का अनुभव कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ओवेन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकार्यों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है।
10) विकास-क्रम का सिद्धान्त (Principle of Development Sequence) –
व्यक्ति का विकास एक निरन्तर एवं क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास की सभी अवस्थाओं में संबंध पाया जाता है फिर भी उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग-अलग किया जा सकता है। बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था के लिए आधार प्रस्तुत करती है। विकास की इस प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था के अनुभवों का विशेष महत्व होता है, जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती ।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्तों का शैक्षिक महत्व | Educational Importance of the Principles of Growth and Development in Hindi
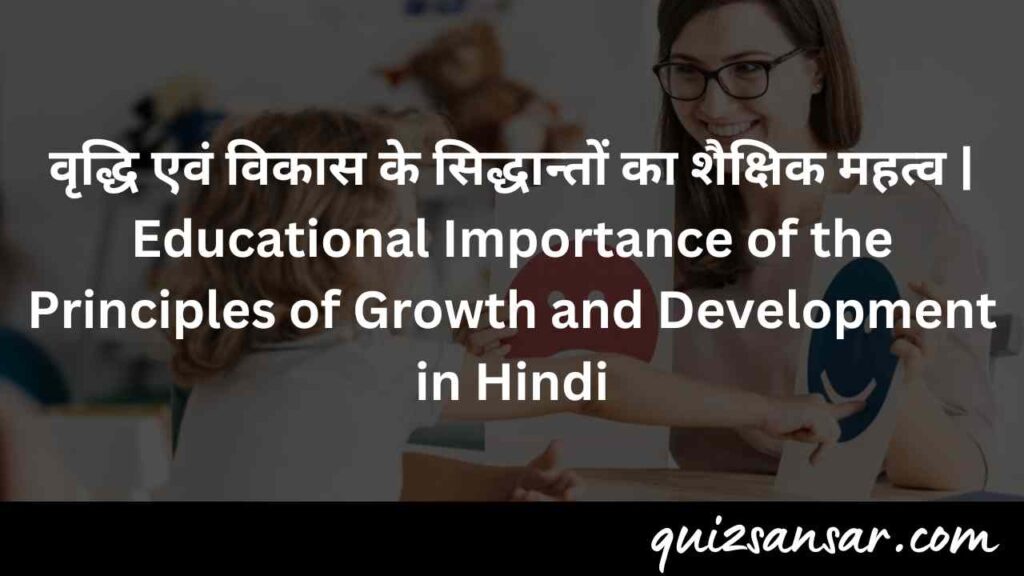
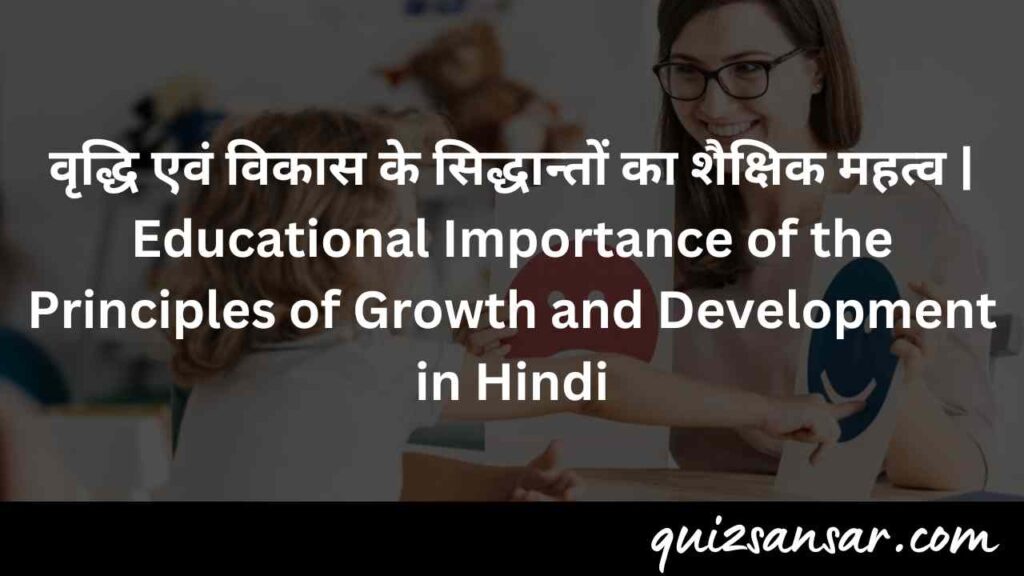
वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्तों का शैक्षिक महत्व (Educational Importance of the Principles of Growth and Development)
वृद्धि तथा विकास के सिद्धान्तों का शैक्षणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है जो निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-
1) वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त से हमें यह ज्ञात होता है कि वृद्धि तथा विकास की गति तथा मात्रा सभी बालकों में एक समान रूप से नहीं पायी जाती है। अतः सभी बालकों से एक जैसी वृद्धि तथा विकास की आशा नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत अन्तरों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।
2) बालकों में वृद्धि तथा विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने से हमें यह लाभ होता है कि भविष्य में जो बालक जैसा कर सकता है या जैसा बन सकता है, उसी को ध्यान में रखकर हम अपने प्रयास करते हैं। परिणामस्वरूप हम अपने आपको अनावश्यक परिश्रम और निराशाओं से मुक्त रख सकते हैं।
3) वृद्धि तथा विकास के विभिन्न पहलू जैसे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास. संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्धित होते हैं। इससे हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है। वृद्धि तथा विकास का प्रत्येक पहलू एक दूसरे से सम्बन्धित है। अतः यदि किसी एक पहलू पर ध्यान न दिया जाए तो विकास का प्रत्येक पहलू प्रभावित होगा ।
4) भविष्य में होने वाली वृद्धि तथा विकास को ध्यान में रखते हुए क्या-क्या विशेष परिवर्तन होंगे इस बात की जानकारी इन सिद्धान्तों के आधार पर हो सकती है। इससे न केवल माता-पिता तथा अध्यापकों को विशेष रूप से तैयार होने के लिए आधार मिलता है, अपितु वे होने वाले परिवर्तनों तथा समस्याओं के लिए अपने-आप को तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं।
5) बालक की वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण समान रूप से उत्तरदायी हैं। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमें बालकों को अधिक से अधिक कल्पना के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से वृद्धि तथा विकास सम्बन्धी सिद्धान्त बालक की वृद्धि तथा विकास को उचित दिशा में बनाए रखने के लिए हमें आधार प्रदान करते हैं।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानव अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक | Factors Affecting Human Growth and Development in Hindi


मानव अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Human Growth and Development)
विकास को विभिन्न कारक प्रभावित करते है जिनका वर्णन निम्नलिखित हैं-
- वंशानुक्रम (Heredity)
- जैविक कारक (Biological Factor)
- पर्यावरण ( Environment)
- शारीरिक कारक (Physical Factor)
- अन्य कारक (Other Factors)
वंशानुक्रम (Heredity)
विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक इस प्रकार हैं-
1) शारीरिक विकास पर प्रभाव- डिक मेयर के अनुसार, “वंशानुगत कारक जन्मगत विशेषताएँ होती है जो बालक के अन्दर जन्म से ही पायी जाती है। वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि गर्भाधान के समय स्त्री-पुरुष के जिस प्रकार के शरीर सम्बन्धी पित्रक (Genes) का संयोग होता है, बच्चे के शरीर के विविध अंगों का विकास उसके अनुसार होता है। पित्रैकों के माध्यम से ही शारीरिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित होते है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि गर्भस्थ बच्चे के विकास में अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine Glands) का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
2) मानसिक विकास पर प्रभाव- क्लिनबर्ग के अनुसार, “बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। वंशानुक्रम सम्बन्धी जितने भी प्रयोग किए गए है उनसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे भी बुद्धिमान होते है। कम बुद्धि वाले माता-पिता के बच्चे भी कम बुद्धि के होते है ।” अतः व्यक्ति के मानसिक विकास का आधार भी वंशानुक्रम होता है, परन्तु कभी-कभी इसके अपवाद भी होते है ऐसा इसलिए होता है। कि बालक माता-पिता के अलावा अपने पूर्वजों से भी गुण हस्तान्तरित करता है।
3) संवेगात्मक विकास पर प्रभाव- किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर निर्भर करती है इसलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। संवेदी माता-पिता की संतानें भी संवेदना के भाव से परिपूर्ण होती है।
4) सामाजिक विकास का प्रभाव- व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का निवास होता है। यही प्रवृत्ति व्यक्ति को समूह में रहने की प्रेरणा देती है। इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है वह उतनी ही तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में समायोजित हो जाता है। जिन परिवारों में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है उन परिवारों के बच्चे सामाजिक क्रिया कलापों में भागीदारी करते है और सामाजिक नियमों एवं परम्पराओं का निर्वहन करते है।
5) स्वभाव पर प्रभाव – व्यक्ति का स्वभाव मुख्यतया उसके सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। स्वभाव के विकास में सबसे अधिक भूमिका अन्तःस्रावी ग्रन्थियों की होती है।
6) चरित्र के विकास पर प्रभाव – व्यक्ति का चारित्रिक विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। इसका निष्कर्ष डगडेल ने चरित्रहीन ड्यूक के वंश के अध्ययन के आधार पर किया।
7) कॅटिल ने अपने अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि. मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है।
जैविक कारक (Biological Factor)
जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारकों से होता है जो आनुवांशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म के पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। मानव शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं के नियन्त्रण एवं समन्वय हेतु कुछ ग्रन्थियों साव करती हैं। ये ग्रन्थियाँ दो प्रकार की होती हैं-
1) बहि स्रावी ग्रन्थियाँ (Exocrine Glands) ये नलिका युक्त ग्रन्थियाँ होती हैं और अपने स्राव को नलिका (Duct) द्वारा शरीर के बाहर निकाल देती है।
2) अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine Glands)- ये नलिकाविहीन ग्रन्थियाँ होती हैं और अपना स्राव सीधे रक्त में डालती हैं। वस्तुतः कभी-कभी हम बहुत सक्रिय (active) तथा कभी-कभी निष्क्रिय (passive) हो जाते हैं व कभी-कभी उदास (depressed) हो जाते हैं इसका कारण यह है कि शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनका नियन्त्रण कुछ ग्रन्थियों द्वारा होता है। उन ग्रंथियों का वर्णन निम्नलिखित हैं-
i) पीयूष ग्रन्थि (Pituitary Gland) – इसका स्थान मस्तिष्क में होता है तथा अधिक हार्मोन्स (Hormones) स्रावित होने से व्यक्ति के शरीर की लम्बाई अधिक व कम होने से व्यक्ति बौना हो जाता है। इस ग्रन्थि के अग्रभाग से सोमेंटोट्रोकिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। इस हार्मोन्स के सहारे पीयूष ग्रन्थि अन्य ग्रन्थियों जैसे- एड्रीनल ग्रन्थि, गल ग्रन्थि (thyroid) आदि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है।
ii) अधिवृक्क ग्रन्थि (Adrenal Gland) – इस ग्रन्थि का स्थान वृक्क (kidney) के ऊपर होता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति का नियंत्रण होता है। भय, क्रोध, आदि संवेग में इस हार्मोन्स का अधिक महत्व है, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन्स (Emergency Hormones) भी कहा जाता है।
iii) गलग्रन्थि (Thyroid Gland) – गलग्रन्थि का व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके नष्ट हो जाने पर श्लेष्मकाय (Myxoedema) नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में शिथिलता आ जाती है। मस्तिष्क एवं पेशियों की क्रिया मन्द पड़ जाती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, स्मृति मन्द होने लगती है, ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाता, चिन्तन करना कठिन हो जाता है। जन्म से ही इस ग्रन्थि के न होने पर बालक की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। आजाम्बुक बालक (Cretins), बौने, कुरूप और मूढबुद्धि (Imbecile) बालक इसी ग्रन्थि के प्रभाव का परिणाम हैं।
इस ग्रन्थि के बहुत अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति में तनाव, अशान्ति, चिड़चिड़ापन, चिन्ता और अस्थिरता दिखाई पड़ती है वृद्धि के काल में गलग्रन्थि की क्रिया अधिक होने पर शारीरिक विकास, विशेषतया लम्बाई के विकास में अधिक तेजी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार संक्षेप में, गलग्रन्थि की क्रिया की अधिकता और कमी के साथ-साथ शरीर की क्रिया में अधिकता और कमी दिखाई पड़ती है। यद्यपि अन्य प्रभावों के कारण भी शरीर में यही परिवर्तन देखा जा सकता है।
iv) यौन ग्रंथि (Sex Gland) – इस ग्रंथि के विकास से स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों तथा पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास होता है।
पर्यावरण (Environment)
वातावरण व्यक्ति के आनुवांशिकता से प्राप्त गुणों के विकास में सहायक होता है। मनुष्य में वातावरण के अनुकूल गुणों का विकास होता है। इस प्रकार वातावरण मानव विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वातावरण जिन कारको या तत्वों द्वारा व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है वे निम्नवत् हैं-
1) मूलभूत आवश्यकताएँ (Basic Needs)- मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान (Food, Cloth and Shelter) हैं। ये सुविधाएँ व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएँ जितनी उत्तम होगी उसका विकास भी उतना ही उत्तम होगा।
2) पारिवारिक परिवेश ( Family Background) – व्यक्ति के विकास को उसका पारिवारिक वातावरण / परिवेश विशेष रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से सम्पन्न तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में पलने वाले बालकों का विकास अच्छा होता है। परिवार में उन्हें स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है।
3) रोग तथा दुर्घटना (Diseases and Injuries) – रोग, चोट या दुर्घटना के कारण बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। गम्भीर रोग में दी जाने वाली दवाओं के कुप्रभाव (Side effect) के कारण बालकों का विकास बाधित होता हैं।
4) विद्यालय (School) – विद्यालय का वातावरण तथा विद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जिन विद्यालयों में बालक के सर्वागीण विकास हेतु समस्त साधनों, सुविधाओं एवं अवसरों की समुचित व्यवस्था होती है उनमें अध्ययनरत छात्रों का विकास अच्छी प्रकार होता है। विद्यालयों में अध्यापकों का व्यवहार बालक के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श देते हैं उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विकास अच्छी प्रकार होता है।
5) समाज एवं संस्कृति (Society and Culture) – व्यक्ति का विकास समाज एवं संस्कृ ति द्वारा प्रभावित होता है। “मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है” (Human is a social animal) समाज के दुःख सुख उसके अपने दुःख सुख हैं। उपरोक्त कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का व्यवहार, कार्य एवं भाव समाज द्वारा प्रभावित होता. है। समाज के रीति रिवाजों, परम्पराओं, मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है।
शारीरिक कारक (Physical Factor)
यद्यपि आजकल व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले जैवकीय कारकों में अन्तः स्रावी ग्रन्थियों को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परन्तु जैवकीय कारकों के साथ शारीरिक रचना (physique) और शरीर रसायन (Physical chemistry) का वर्णन भी प्रासंगिक होता है। दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना से उसके स्वभाव का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य होता है। प्रायः मोटे व्यक्ति हँसी-मजाक पसन्द करने वाले, आरामपसन्द और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं और दुबले-पतले व्यक्ति संयमी, तेज और चिड़चिडे होते हैं।
शरीर रचना तथा स्वभाव के सम्बन्ध को समझने के लिए बहुत से प्रयोग किए गए हैं। परन्तु इस विषय में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सके हैं। वास्तव में शारीरिक रचना एवं व्यक्तित्व में निश्चित रूप से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अभी और प्रयोगों की आवश्यकता है। अभी तक हुए अधिकांश प्रयोग विद्यालय के विद्यार्थियों पर किए गए हैं। अतः उनके परिणामों से निश्चित निष्कर्ष निकालने के पहले प्रौढ़ एवं वयस्क व्यक्तियों पर भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी सह-सम्बन्ध (correlation) के आधार का प्रश्न रह जाता है। केवल सह-सम्बन्ध में शरीर रचना को विशेष प्रकार के स्वभाव का कारण नहीं माना जा सकता।
इस विषय में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति के व्यवहार में भी अन्तर पड़ता है। यह दैनिक अनुभव की बात है कि मोटे सुगठित शरीर वाले और दुबले-पतले व्यक्तियों के प्रति हमारे व्यवहार में उनके आकार-प्रकार के अनुसार भी अन्तर दिखाई पड़ता है। हमारे व्यवहार के इस अन्तर से भी उनके व्यक्तित्व में अन्तर आता है। अतः व्यक्तित्व के अन्तर को केवल शरीर के मोटे-पतले या बलिष्ठ- दुर्बल होने का कारण ही नहीं बल्कि दूसरों के उसके प्रति व्यवहार के कारण भी माना जाना चाहिए।
अन्य कारक (Other Factors)
बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक निम्नलिखित हैं-
1) बुद्धि (Intelligence) – बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है जबकि मन्द बुद्धि के बालकों का मानसिक विकास मन्द गति से होता है। मन्द बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाए किन्तु उनका सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास की गति अत्यन्त धीमी रहती है। कुशाग्र बुद्धि के बालक शीघ्र ही चलना एवं बोलना सीख लेते हैं वहीं मन्द बुद्धि बालक देर से चलना व बोलना सीख पाते हैं।
टर्मन ने अपने अध्ययन (जिसमें बालक के पहली बार बोलने और चलने का अध्ययन किया) के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि 13 वें मास में चलने वाले बालक प्रखर बुद्धि, 14 वें मास में चलने वाले सामान्य बुद्धि, 22 वें मास में चलने वाले मन्द बुद्धि और 23 वें मास में चलने वाले बालक मूढ़ होते हैं इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया में क्रमशः 11, 16, 34, 51 मास वाले बालक प्रखर बुद्धि, सामान्य, मन्द एवं मूढ़ बुद्धि वाले थे।
2) लिंग भेद ( Sex Difference)- लिंग भेद भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रभावशाली कारक हैं। इसका प्रभाव बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पड़ता है। अध्ययन में यह देखा गया कि जन्म के समय बालक का आकार, बालिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है परन्तु बाद में बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बालकों का मानसिक विकास, बालिकाओं की अपेक्षा देर से होता है। बालिकाओं में यौन-परिपक्वता भी बालकों की अपेक्षा जल्दी आती है।
3) पोषण (Nutrition) – बालक के विकास का एक अन्य प्रभावी कारक उचित पोषण है। पोषण का बालक के विकास पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है। उचित पोषण से बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास उचित ढंग से होता है। बालक के लिए सिर्फ भोजन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उस भोजन में उचित सन्तुलित पोषण का होना भी अनिवार्य है । सन्तुलित पोषण तत्वों को ग्रहण करने से बालक शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं और मानसिक रूप से भी उनका विकास उचित रूप से होता है।
4) शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश (Pure Water, Air and Light) – शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश भी बालक विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। जीवन के आरम्भिक दिनों में बालक को शुद्ध वायु तथा प्रकाश (धूप) की नितान्त आवश्यकता होती है। शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश के अभाव में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
5) प्रजाति (Race)- प्रजाति भी बालक के विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्लिनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति, नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि यूरोप की तुलना में भूमध्यसागरीय प्रदेशों के बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है।
6 ) आर्थिक स्थिति (Economic Conditions) – बालक विकास का अन्य प्रभावशाली कारक परिवार की आर्थिक स्थिति भी है। सम्पन्न परिवार के बालक मानसिक रूप से पूर्णतः सन्तुष्ट रहते हैं जिस कारण उनका समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इसके ठीक विपरीत आर्थिक रूप से कमजोर बालक स्वयं से असन्तुष्ट रहते हैं और उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति धीमी रहती है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानव अभिवृद्धि एवं विकास (HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT) : अर्थ एवं परिभाषाएँ


मानव अभिवृद्धि एवं विकास (HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT)
मानव अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्यय (Concept of Human Growth and Development)
प्रायः विकास को अभिवृद्धि के पर्याय के रूप में जाना जाता है लेकिन मनोविज्ञान इन दोनों शब्दों में विभेद करता है। अभिवृद्धि का अर्थ सीमित रूप में शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है अभिवृद्धि, विकास का ही एक चरण है। अभिवृद्धि में आकार तथा परिणाम दोनों में परिवर्तन होता है तथा इसका मापन सम्भव है परन्तु विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन हैं जिनका मापन अर्थात् नाप-तौल करना कठिन है।
विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यन्त चलती रहती है। मानव के जीवनकाल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि पहलू सम्मिलित हैं। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि विकास परिपक्वता के पश्चात् रुक जाता है परन्तु यह मत सत्य नहीं है क्योंकि विकास का क्रम आजीवन चलता रहता है। परिपक्वता की अवस्था के बाद उसकी गति धीमी अवश्य हो जाती है।
मानव अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Human Growth)
वृद्धि का अर्थ है ‘फैलना या बढ़ना’ । वृद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के Growth शब्द का हिन्दी रूपान्तर है जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना है। वृद्धि से अभिप्राय लम्बाई, भार, आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है।
इस प्रकार गर्भधारण से लेकर शैशवास्था बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार लम्बाई एवं भार में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है।
फ्रैंक के अनुसार, “अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे, लम्बाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य-प्राणी में होने वाले सम्पूर्ण परिवर्तनों से होता है।”
According to Frank, “Growth is regarded as multiplication of cells, as growth in height and weight while development refers to the changes in organism as a whole.”
मेरीडिथ के अनुसार, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में।”
According to Meredith, “Some writers reserve the use of ‘development of mean differentiation.”
जी.ए. हेडफील्ड ने अभिवृद्धि एवं विकास के अन्तर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है- अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है और विकास रूप एवं आकार दोनों में परिवर्तन का होना है ।
विकास (Development) एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें अभिवृद्धि का भाव हमेशा निहित होता है। अभिवृद्धि के अभाव में विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। अतः अभिवृद्धि एवं विकास दोनों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है।
अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर (Difference between Growth and Development)
अभिवृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर होता है-
| अंतर के आधार (Bases of Difference) | अभिवृद्धि (Growth) | विकास (Development) |
| अर्थ (Meaning) | अभिवृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से होता है। | विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ-साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। |
| परिवर्तन (Changes) | अभिवृद्धि में संरचनात्मक मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। | विकास में प्रकार्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। |
| परिपक्वता (Maturity) | अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। | विकास एक सतत् प्रक्रिया है। यह समाप्त न होकर आजीवन चलती रहती है। |
| प्रक्रिया (Process) | अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। | विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। |
| अवधारणा (Concept) | अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है। यह विकास का ही एक चरण है। | विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास में ही अभिवृद्धि निहित होती है। |
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


मानव विकास का अर्थ, परिभाषाएँ एवं विशेषताएँ | Meaning, Definitions and Characteristics of Human Development in Hindi


मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Human Development)
विकास शब्द अंग्रेजी भाषा के Development शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। विकास का अर्थ भी बढ़ना होता है। विकास में परिवर्तन मात्रात्मक नहीं होता है। यह बढ़ना शारीरिक रूप में न होकर मानसिक रूप में होता है।
इस प्रकार विकास का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक एकीकरण से है जिसके फलस्वरूप उसका व्यवहार विशिष्ट प्रकार का होता जाता है तथा वातावरण के साथ समायोजन में सहायक होता है। अतः विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को इंगित करता है।
विकास के अन्तर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएँ वृद्धि एवं क्षय होती है जो निरन्तर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यन्त चलती रहती है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र होती है जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यन्त मन्द होती है तथा जीवन के अन्तिम वर्षों में क्षय की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है जबकि वृद्धि प्रक्रिया की गति अत्यन्त मन्द हो जाती है।
इरा. जी. गोर्डन के अनुसार, “विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है।
हरलॉक ने मानव विकास को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उनके अनुसार, “विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं।
According to Hurlock, “Development is not limited to growing larger instead, it consist of progressive series of changes toward the goal of maturity. Development results in new characteristics and new abilities on the part of the individual.”
गेसेल के अनुसार, “विकास केवल एक प्रत्यय (विचार) ही नही है, इसे देखा, जाँचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है।”
According to Gesell, “Development is more than a concept. It can be observed, appraised and to some extent even ‘measured’ in the three major manifestations (a) anatomic, (b) physiologic and (c) behavioural. Behavioural signs, however, constitute a most comprehensive index of developmental status and developmental potentials.”
लाबाब के अनुसार, “विकास का अर्थ परिपक्वता से सम्बंधित परिवर्तनों से है जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं।”
सोरेन्सन के अनुसार, “विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। “
उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसका संबंध मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों से है। अपने भीतर व बाह्य वातावरण से समायोजन की कला ही विकास है।
मानव विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Human Development)
विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
1) विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है।
2) विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है ।
3) विकास एक परिपक्वता उन्मुख प्रक्रिया है ।
4) अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक व्यापक सम्प्रत्यय है, इसमें व्यक्ति के जीवनकाल में आये सभी परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है।
5) विकास एक सतत् एवं क्रमिक प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक अवस्था स्वयं की पूर्व अवस्था से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती है।
6) विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं।
7) विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर भिन्न होती है। बालक के जन्म के समय यह दर अपने उच्चतम स्तर पर होती है तथा प्रौढ़ावस्था में आकर मंद हो जाती है।
8) विकास को वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
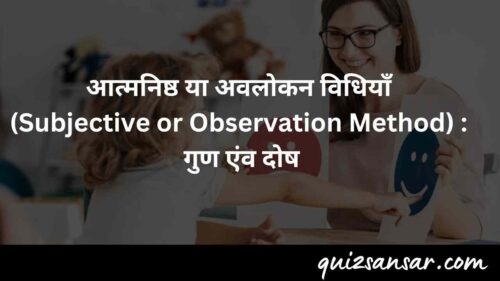
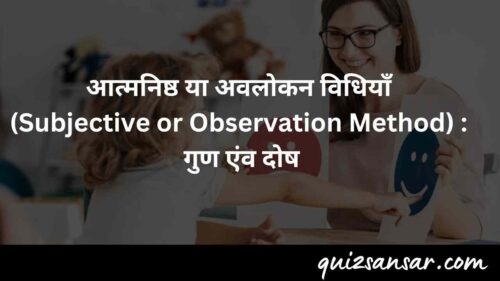
आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष


आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method)
इसके अन्तर्गत निम्न विधियाँ सम्मिलित हैं-
आत्मनिरीक्षण विधि (Introspective Method)
इस विधि को अन्तर्दर्शन, अन्तः निरीक्षण या अन्तर्मुखी अवलोकन विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि मनो विज्ञान की परम्परागत अर्थात् सबसे प्राचीन विधि है। इसका नाम इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक से सम्बद्ध है जिन्होंने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी थी, “मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण।”
According to Lock, “The notice which the mind takes of its own operations.” (Self Observation)
इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते है कि Introspection शब्द दो शब्दों ‘Intro’+ ‘Spection’, से मिलकर बना है जिसमें ‘Intro’ का अर्थ है भीतर या अन्दर तथा ‘Spection’ का अर्थ है- झाँकना ।
अतः शाब्दिक अर्थ में Introspection का अर्थ है “अपने अन्दर या भीतर झाँकना” । वुडवर्थ ने इसे ‘स्व अवलोकन’ (Self Observation) कहा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करता है।
स्टाउट के अनुसार, “अपने मस्तिष्क के क्रिया कलापों का क्रमबद्ध ढंग में अध्ययन करना ही अन्तर्दशन् है।”
According to Stout, “To Introspect is to attend to the working of one’s own mind in a systematic way.”
इसकी व्याख्या करते हुए बी. एन. झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं।
आत्मनिरीक्षण विधि के गुण या लाभ (Merits or Advantages of Introspection Method)
इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं-
1) सरल तथा कम व्यय वाली विधि (Simple and Economical Method) – सरलता इस विधि का एक मुख्य गुण है क्योंकि इस विधि के द्वारा बालकों की मनोदशा का आसानी से ज्ञान हो जाता है। इस विधि को हम कम व्यय वाली विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोगशाला, मूल्यवान उपकणों या किसी दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में किसी विशेष यन्त्र या सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण यह विधि खर्चीली नहीं है तथा दूसरी तरफ चूँकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह विधि बहुत सरल है।
2) मानसिक क्रियाएँ (Mental Processes) — इस विधि के द्वारा हम ऐसी मानसिक क्रियाओं को भी देख सकते हैं जिन्हें हम किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहते है। जैसे- लिंग अनुभव (Sex Experiences)|
3) प्रत्यक्ष अध्ययन (Direct Study) – यह विधि हमें बालकों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से कराती है जैसे स्वयं पुरस्कार प्राप्त होने पर या किसी अन्य बालक को पुरस्कार पाता देखकर उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों का ज्ञान बालकों से पूछकर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हमें उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में सहायता प्राप्त होती है।
4) रचनात्मक विधि (Creative Method) – इस विधि के द्वारा बालकों में किसी विषय के सम्बन्ध में सोचने-विचारने तथा समझने की शक्ति बढ़ती है अर्थात् उसे खास विषय पर ध्यान केन्द्रित करने का भी पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा बालकों को आत्म मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होता हैं क्योंकि स्वयं को पहचानने के लिए अन्तर्मुखी (introvert ) होना आवश्यक है।
5) विश्वसनीय परिणाम (Reliable Results) – इस विधि का प्रयोग कर हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मनोदशा का अध्ययन करता है तदुपरान्त उसे व्यक्त करता है और उसी के आधार पर कोई परिणाम निकाला जाता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन में अनुमान, पूर्वधारणा, अन्दाजा, आदि का प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।
6) अपूर्ण विधि (Incomplete Method) – आत्मनिरीक्षण विधि को एक अपूर्ण विधि भी कहा जा सकता है क्योंकि इस विधि का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान के अतिरिक्त किसी भी दूसरे विज्ञान में नहीं होता है। इस प्रकार यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान को एक अपूर्ण विज्ञान बनाती है।
7) कोई भी स्थान और समय (No Bar of Time and Place) – चूँकि इस विधि में व्यक्ति का मस्तिष्क ही उसकी प्रयोगशाला होता है। अतः इस विधि का उपयोग किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर किया जा सकता है।
8) व्यक्तित्व में सुधार ( Improvement in Personality) – यह विधि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार लाने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में कोई असाधारणता हो तो इस विधि द्वारा उसे दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं।
9) प्रयोगात्मक रिपोर्ट का भाग (Part of Experimental Report) – प्रयोगात्मक रिपोर्ट लिखते समय हम विषयी की अन्तर्मुखी रिपोर्ट भी सम्मिलित करते हैं अतः यह प्रयोगात्मक रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
10) शिक्षण में सुधार ( Improvement in Teaching) – अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को इस विधि की सहायता से नवीन ढंग के सुझावों द्वारा अधिक अच्छा बना सकता है।
इस प्रकार इस विधि में गुणों की महत्ता दर्शाते हुए डगलस व हॉलैण्ड के शब्दों में, “मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है।”
आत्म निरीक्षण विधि के अवगुण (दोष) या सीमाएँ (Demerits or Limitations of Introspection Method)
यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अतः इस विधि की अपनी सीमाएँ हैं उन्हीं को इसकी कमियाँ और दोष माना जाता है-
1) आत्मनिष्ठ (आत्मगत विधि) (Subjective Method) – यह विधि पूर्णतया व्यक्ति (विषयी) की योग्यता एवं स्व क्षमता पर आश्रित है इसमें व्यक्ति के स्व-अनुभव, विचार और निर्णय होते हैं अतः यह व्यक्तिनिष्ठ होती है, उससे प्राप्त निष्कर्षो पर पूर्णतया विश्वास भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसके आधार पर कोई सिद्धान्त या नियम बनाए जा सकते हैं। अतः आत्मगत होने के कारण यह विधि अवैज्ञानिक है।
2) अविश्वसनीयता (Unreliability ) – विश्वसनीयता को इसका एक गुण बताया गया है। जो कि युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपनी मनोदशा का अध्ययन करते समय यह सम्भव है कि व्यक्ति अपनी सत्य (सही) बातों को छिपा ले और झूठ (गलत) बातें बता दे। इस स्थिति में जो भी परिणाम निकाला जाएगा वह निश्चित ही गलत होगा।
3) मनोदशा की चंचलता (Versatility of Mental State) – मानसिक दशाएँ या प्रक्रियाएं इतनी चंचल होती हैं कि उनका ठीक-ठीक अध्ययन करना तथा अध्ययन के अनुसार उनको सही (उसी रूप में व्यक्त करना लगभग असम्भव कार्य है । अत्यंत छोटे बालकों के लिए तो यह अत्यंत मुश्किल कार्य है क्योंकि उनमें ध्यान को केन्द्रित करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वे अपनी चंचल मानसिक स्थिति का अध्ययन (निरीक्षण) यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकते। अतः यह विधि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए भले ही उपयुक्त हो किन्तु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यह विधि पूर्णतया अनुपयुक्त है।
4) ध्यान विभाजन (Distraction of Mind) – यह विधि व्यक्ति का ध्यान विभाजित करने में विश्वास रखती हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को प्रयोज्य और निरीक्षण दोनों का कार्य एक ही समय पर करना पड़ता है। अतः एक ओर तो वह अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण करता है तथा दूसरी तरफ वह उसी मानसिक स्थिति का शिकार बना रहता है। अतः उसका ध्यान दोनों तरफ विभाजित रहता है।
किंतु मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों तथा व्यक्ति के स्व-अनुभव के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ध्यान का विभाजन सम्भव ही नहीं है। अतएव कोई भी व्यक्ति एक ही समय में प्रयोज्य तथा निरीक्षक का कार्य नहीं कर सकता है और यदि करता है तो इस आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं हो सकता।
5) मनोदशा का विस्थापन (Displacement of Mental State)- इस विधि के द्वारा जैसे ही किसी मनोदशा का निरीक्षण प्रारम्भ होता है वह मनोदशा ही विस्थापित हो जाती है और तुरन्त दूसरी मनोदशा का निरीक्षण वास्तविक रूप में नहीं कर पाता है, अतः मनोदशा का विस्थापन इस विधि का प्रमुख अवगुण है।
जैसे- यदि कोई बच्चा क्रोध की अवस्था में है और उससे उस समय होने वाली अपनी मनोदशा का निरीक्षण करने के लिए कहा जाए तो यह जब तक वह निरीक्षण आरम्भ करता है तब तक क्रोध की स्थिति विस्थापित होकर चिन्तन या दूसरी मानसिक स्थिति में बदल जाएगी और यदि ऐसा नही भी होता है तो भी निश्चित रूप से निरीक्षण के समय क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। अतः किसी भी हालत में वास्तविक मनोदशा का यथार्थ निरीक्षण या अध्ययन सम्भव नहीं होगा।
6) भाषा का प्रभाव (Effect of Language) – इस विधि पर भाषा का गहरा असर पड़ता है क्योंकि जिन बालकों में भाषा विकसित ही नहीं है उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा सम्भव नहीं है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि गूँगे, बहरे तथा भाषा विकृत बालकों की मनोदशा का अध्ययन इस विधि से सम्भव नहीं है।
7) अवलोकन अनुदर्शन (Retrospection)— आत्मनिरीक्षण विधि में हम स्मरण शक्ति से काम लेते हैं, जब हम स्मरण से काम लेते हैं, तो यह अवलोकन अनुदर्शन बन जाता है क्योंकि हम अपने भीतर झाँकने के बजाय अपने भूतकाल में झाँक रहे होते हैं।
8) सार्वभौमिक प्रयोग नही (Universally not Applicable) – इस विधि द्वारा सार्वभौमिक प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इस विधि को शिशु बालकों, असाधारण लोगों, जंगलियों, अशिक्षितों तथा जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस विधि के दोषों का अध्ययन कर हम कह सकते हैं कि सम्भवतः इसके दोषों के कारण ही मनोवैज्ञानिकों में आत्मनिरीक्षण विधि का परित्याग कर दिया है। डगलस एवं हॉलैण्ड (Douglas and Holland) का मत है कि यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है।
निष्कर्ष (Conclusion)
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यूँ तो वर्तमान युग में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अनेकानेक वैज्ञानिक विधियाँ विकसित हो चुकी हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग आज भी बहुत लाभकारी होता है, मुख्यतः तब, जब अध्ययनकर्ता को अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की सत्यता की जाँच करनी हो और तब, जब अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की तुलना करनी होती है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
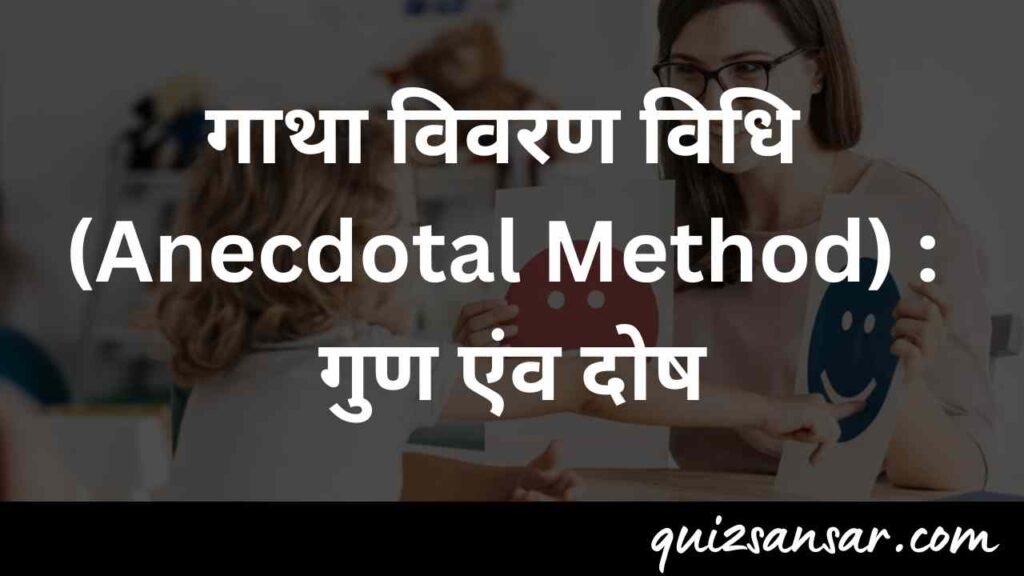
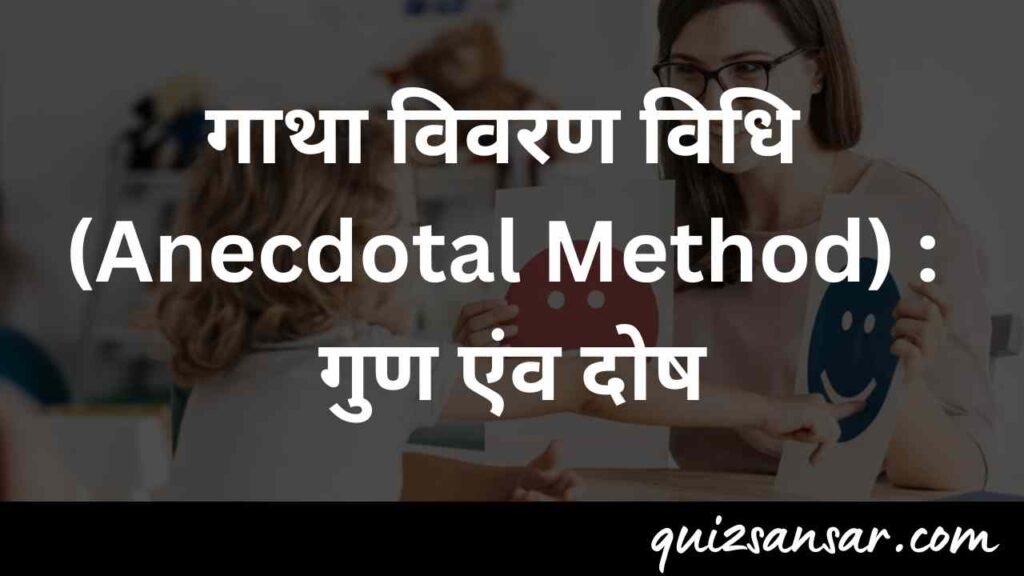
गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method)
गाथा विवरण पद्धति को उपाख्यान विधि भी कहते हैं। यह एक आत्म गतिविधि है। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण करके व्यक्ति एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है।
गाथा विवरण विधि के गुण (Merits of Anecdotal Method)
इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं-
1) इस विधि में विभिन्न घटनाओं एवं तथ्यों का संचय व्यक्ति स्वयं स्मरण करके करता है अतः ये तथ्य सत्यता पर आधारित होते हैं।
2) इस विधि में विभिन्न घटनाओं को संचित किया जाता है तदुपरान्त इस घटना की परस्पर तुलना की जाती है और आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या भी की जाती है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है।
गाथा विवरण विधि के दोष (Demerits of Anecdotal Method)
1) इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों को ठीक-ठीक स्मरण करके नहीं बता पाता तथा घटना से सम्बन्धित कई तथ्यों को वह भूल जाता है और कई तथ्यों को अपनी तरफ से जोड़ देता है। अतः यह विधि अविश्वसनीय है। स्किनर के अनुसार, गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
2) सभी घटनाएँ यथार्थ रूप में प्रकट नहीं हो पाती हैं अतः यह विधि वैज्ञानिक भी नहीं है।
3) अतः हम कह सकते हैं कि आत्मगत होने के कारण यह विधि विश्वसनीय नहीं है इसलिए इस विधि का उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जाना चाहिए।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com


निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
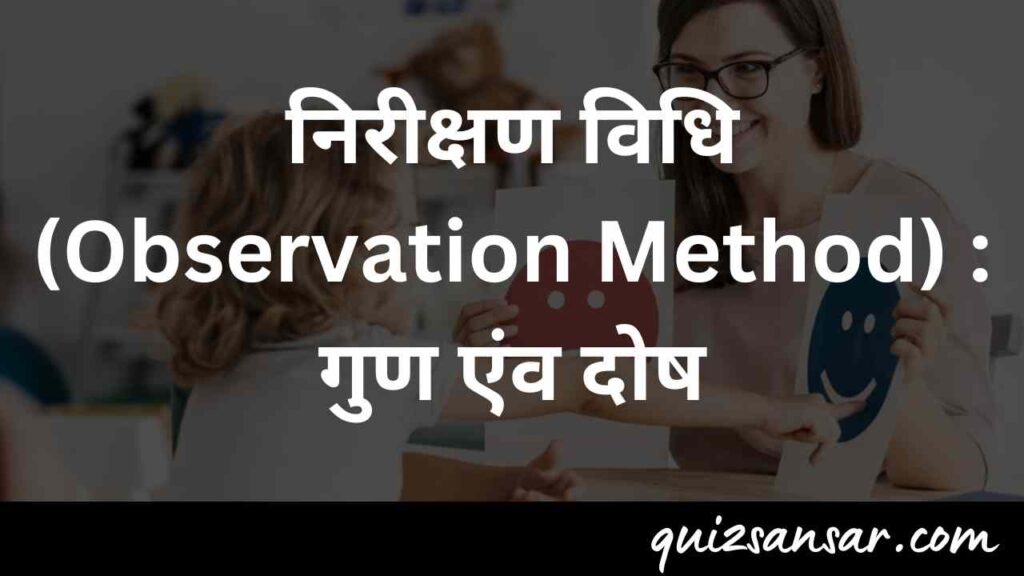
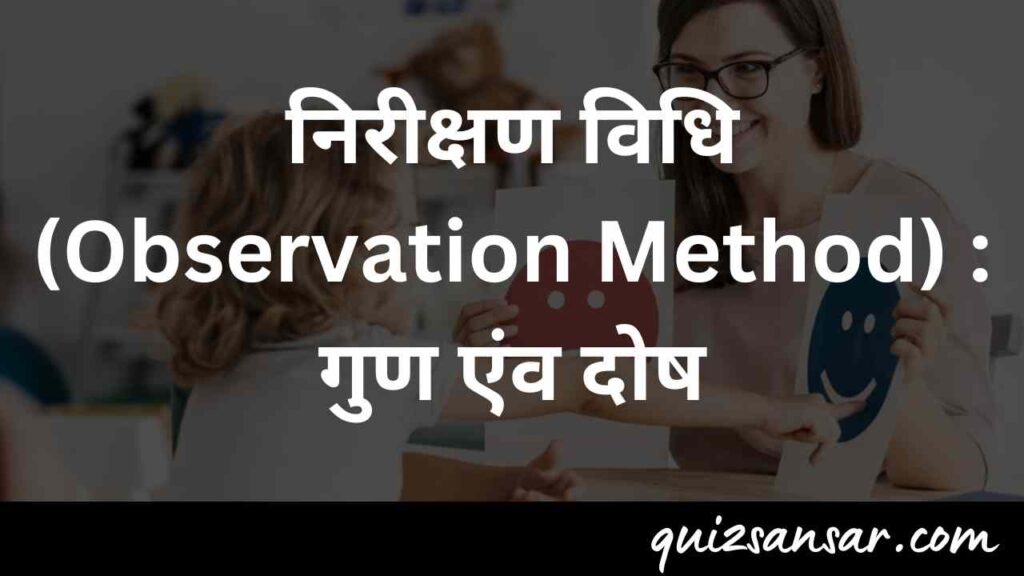
निरीक्षण विधि (Observation Method)
निरीक्षण विधि भी आत्मनिरीक्षण विधि जितनी ही पुरानी (प्राचीन) है। इस विधि को बहिर्मुखी अवलोकन, बहिर्दर्शन विधि, प्राकृतिक अवलोकन या अनियन्त्रित अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है।
इस अवलोकन के दो भाग होते हैं – नियन्त्रित अवलोकन (Controlled observation) तथा अनियन्त्रित अवलोकन (Uncontrolled observation) । नियन्त्रित अवस्थाओं में अवलोकन, नियन्त्रित अवलोकन कहलाता है। इसका दूसरा नाम प्रयोगात्मक अवलोकन भी है। अनियंत्रित अवलोकन, प्राकृतिक अवलोकन कहलाता है।
निरीक्षण, बहिर्दर्शन अथवा अवलोकन का शाब्दिक अर्थ है – किसी वस्तु या क्रिया को देखना मानव-व्यवहार के अध्ययन के सन्दर्भ में इसका अर्थ यह है कि मानव के बाह्य व्यवहार को देखना-समझना और उससे सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाना। कॉलसेनिक के अनुसार “यह निरीक्षण दो रूपों में किया जाता है- एक औपचारिक रूप में (Formal Form) और दूसरा अनौपचारिक रूप में (Informal Form)” |
1) औपचारिक निरीक्षण (Formal Form) – औपचारिक निरीक्षण, वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षणकर्ता. (निरीक्षण करने वाला) विषयी (Subject) के व्यवहार का निरीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में योजनाबद्ध तरीके से सम्पादित करता है। इस निरीक्षण में विषयी को यह ज्ञात रहता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। अतः इस स्थिति में विषयी अधिकतर कृत्रिम व्यवहार करते हैं।
2) अनौपचारिक निरीक्षण (Informal Form) – यह वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षणकर्ता, विषयी के व्यवहार का निरीक्षण बगैर किसी पूर्व निश्चित योजना के. अनियन्त्रित परिस्थियों में करता है। अतः इस निरीक्षण में व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। अतः विषयी स्वाभाविक व्यवहार करता है। अतः उसके द्वारा कृत्रिम (बनावटी) व्यवहार करने का कोई प्रश्न नही उठता है।
निरीक्षण विधि के गुण (Merits of Observation Method)
यदि इस विधि का प्रयोग हम सावधानीपूर्वक करते हैं तो यह एक अत्यन्त अच्छी विधि साबित होती है।
1) वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक (Objective and Scientific) – निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि से ज्यादा वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक है।
2) विश्वसनीय तथा प्रमाणिक (Reliable and Valid) – यह एक योजनाबद्ध विधि है, यह अन्तर्दर्शन विधि की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय है।
3) मितव्ययी (Economical) – निरीक्षण विधि अत्यंत संयमी विधि है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला के कीमती उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं होती है।
4) लचीली (Flexible) – यह विधि अत्यंत लचीली विधियों की श्रेणी में गिनी जाती है तथा इस विधि का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में तथ्यों को संग्रहित करने के लिए करते हैं।
5) विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार (Behaviour of Different Individuals) – यह विधि व्यक्ति विशेष तथा व्यक्ति समूह, दोनों के ही व्यवहारों का अध्ययन करने में सक्षम है। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति विशेष तथा व्यक्ति समूह के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे बच्चों, असाधारण मनुष्यों और जानवरों का व्यवहार देखने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
6) व्यक्ति तथा समूह का व्यवहार (Behaviour of Individual and Group) – इस विधि के द्वारा व्यक्ति तथा समूह के व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है।
7) प्रयोगात्मक विधि के लिए स्थान (Ground for Experimental Method) – यह विधि प्रयोगात्मक विधि के लिए आधार प्रस्तुत करती है। क्योंकि प्रयोग कठोर, नियन्त्रित या प्रयोगशाला की परिस्थितियों में बहिर्मुखी अवलोकन के अलावा और कुछ भी नहीं होता।
8) शिक्षा स्थितियों में लाभदायक (Useful in Educational Situations) – इस विधि की मदद से बच्चे के कमरे में पढ़ाई की निगरानी आसानी से की जा सकती है। समस्यात्मक बालकों, पिछड़े बालकों तथा प्रतिभाशाली बालकों का व्यवहार इस विधि के माध्यम से देखा जा सकता है तथा शिक्षा का परिणाम निकाला जा सकता है।
निरीक्षण विधि के दोष (Demerits of Observation Method)
इस विधि में अनेकोनेक गुण होने के बावजूद इस विधि की अपनी कुछ सीमाएँ या दोष भी हैं। जो निम्न हैं-
1) अप्रशिक्षित निरीक्षक (Untrained Observer)- इस विधि में सही अवलोकनार्थ हेतु प्रशिक्षित दर्शकों का मिलना कठिन है और अनट्रेंड दर्शक व्यर्थ तथा अनुचित तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। अतः इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं।
2) अन्तर्मुखी ( Introvert ) – यह विधि एक प्रकार से अन्तर्मुखी ही है। क्योंकि कभी-कभी दर्शक नर्म हो सकता है अर्थात् वह विषयी को रियायत दे देता है जबकि कभी-कभी वह कठोर हो जाता है और विषयी को किसी प्रकार की रियायत प्रदान नहीं कर सकता है।
3) बनावटीपन (Artificiality) – औपचारिक निरीक्षण में चूँकि विषयी को यह ज्ञात होता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है अतः वह सावधान (सजग) हो जाता है और कृत्रिम व्यवहार करने लग जाता है। उस समय यह विधि अर्थहीन हो जाती है। इसके अलावा कई बार व्यवहार में स्वतः ही बनावटीपन आ जाता है, जैसे- स्त्रियों के व्यवहार में अजनबी को देखकर स्वतः बनावटीपन आ जाता है।
4) व्यवहार घटित होने के लिए लम्बी प्रतीक्षा (Long Wait for Re-occurrence of Behaviour)— इस विधि में कई बार अमुक घटना के घटने के बाद उस घटना के पुनः घटने के लिए लम्बा इन्तजार करना पड़ता है, जैसे- यदि किसी बच्चे के क्रोध के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें उसके पुनः क्रोध में आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
5) व्यक्तिगत समस्याएँ (Personal Problems) – व्यक्ति की कुछ समस्याएँ तथा अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जैसे लिंग अनुभव ।
6) आन्तरिक व्यवहार (Internal Behaviour) – अवलोकन द्वारा किसी मनुष्य के आन्तरिक व्यवहार का पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के आन्तरिक व्यवहार को देखा नहीं जा सकता है।
7) अचेतन मन (Unconscious Mind) – किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन को हम निरीक्षण विधि द्वारा नहीं जान सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
यद्यपि प्राकृतिक अवलोकन की विधियों में बहुत सी कमियाँ हैं परन्तु आज भी इसका प्रयोग शिशु-मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में काफी होता है।
दूसरी तरफ निरीक्षण विधि काफी सीमा तक वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय भी है, बशर्ते कि इस विधि में निरीक्षण क्रमबद्ध रूप में सावधानीपूर्वक किया जाए, तथा प्राप्त तथ्यों को सावधानीपूर्वक लिखा जाए और आँकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें।
यदि निरीक्षणकर्ता विषयी के व्यवहार को विडियों द्वारा रिकॉर्ड करके उसका धैर्यपूर्वक निरीक्षण करे तो यह विधि और अधिक उपयोगी साबित होगी।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
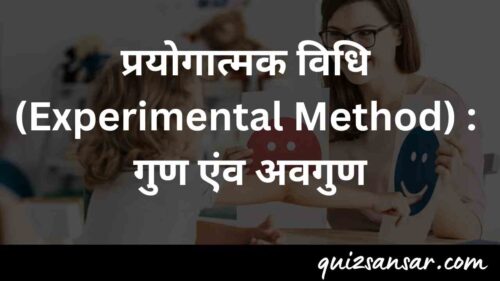
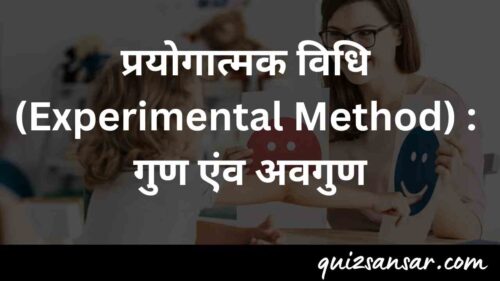
प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण


प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method)
प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) – प्रयोगात्मक विधि, मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगी और महत्पूर्ण विधि है विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन एक नियन्त्रित वातावरण में करना और उनका गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से विवेचन करना ही इस विधि की प्रमुख विशेषता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वुण्ट ने सन् 1879 में किया था।
एंजिल के अनुसार, “प्रयोग के अन्तर्गत् किसी विषय का निरीक्षण नियंत्रित अवस्थाओं में किया जाता है ताकि हम जान सकें कि किन कारकों का प्रभाव प्राप्त परिणाम पर पड़ रहा है।
According to Angell, “Experiment consists in making observation of phenomena under conditions of control, so that we may know just what factors are at work in producing the results observed.”
जहोदा के शब्दों में, ‘नियन्त्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है।
कैस्टिंयर के शब्दों में, प्रयोग के मूलाधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन का आश्रित चर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है।”
प्रयोगात्मक विधि के गुण (Merits of Experimental Method)
प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता को देखते हुए वुडवर्थ महोदय कहते हैं, प्रयोग ने मनोविज्ञान को पूर्ण बना दिया है।”
1) वैज्ञानिक विधि- यह विधि वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम वैध और विश्वसनीय होते हैं। इस विधि में कार्यों और कारणों का अध्ययन जितनी शुद्धता से किया जाता है उतना दूसरी किसी विधि में नहीं किया जाता है।
2) नियन्त्रित वातावरण- इस विधि द्वारा अध्यापक दक्षतापूर्वक अपने शिक्षार्थियों की मानसिक और भौतिक दशाओं का पता लगाता है और बच्चों को उचित तथा नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है।
3) पुनरावृत्ति – इस विधि का एक गुण है पुनरावृत्ति क्योंकि इस विधि में प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को और अधिक सत्य और विश्वसनीय बनाने हेतु प्रयोग को पुनः दोहराया भी जा सकता है।
4) प्रमाणीकरण – इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी दूसरी परिस्थिति में किए गये प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो की जाँच किसी अन्य परिस्थिति में आसानी से कर सकता है तथा इसमें दोनों के ही निष्कर्ष समान होते हैं। यही इस विधि की प्रामाणिकता है।
5) अन्तः निरीक्षण एवं बाह्य निरीक्षण का संकलन – इस विधि में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं अतः विषयी से अन्तःनिरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं अतः विषयी से अन्तर्निरीक्षण रिपोर्ट लेकर यह देखा जाता है कि यह रिपोर्ट प्रयोज्य के वस्तुनिष्ठ आँकड़ों के अनुरूप है या नहीं। इसी सन्दर्भ में टिचनर ने कहा है, “प्रयोग मात्र बाह्य निरीक्षण एवं अन्तः निरीक्षण को नियंत्रण में लाने की एक निपुण रीति है ।”
According to Titchener, “Experiments is simply an ingenious system for bringing introspection and observation under control”.
उपर्युक्त गुणों के कारण ही प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय होते हैं, फिर भी इसमें कई प्रकार की त्रुटियाँ भी रह जाती हैं।
प्रयोगात्मक विधि के अवगुण (Demerits of Experimental Method)
1) नियंत्रण की कठिनाई – वास्तविक रूप में विषयी की मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से नियन्त्रित नही किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर अनेक आन्तरिक एवं बाह्य दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इन बाह्य दशाओं को तो एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है किंतु आन्तरिक दशाओं को नियंत्रित करना अत्यन्त कठिन होता है।
2) सभी प्रयोग मनुष्यों पर सम्भव नही – इस विधि में सभी प्रकार के प्रयोग मनुष्यों पर सम्भव नहीं है। अतः इसी जगह पर इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इसके अलावा कई प्रकार की मानसिक क्रियाओं, जैसे अचेतन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन प्रयोगशाला में सम्भव भी नहीं है।
3) लम्बी एवं महँगी विधि- इस विधि में बहुत समय लगता है इस विधि को प्रयोग करने में व्यय भी बहुत अधिक होता है।
4) प्रयोगकर्ता के साथ सहयोग की कमी- कभी-कभी प्रयोज्य (विषयी) प्रयोगकर्ता के साथ पूरा-पूरा सहयोग नहीं करते है। इतने सारे दोष होने के बाद भी प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकारी जाती है। इस सम्बन्ध में स्किनर महोदय का कहना है, कि कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
