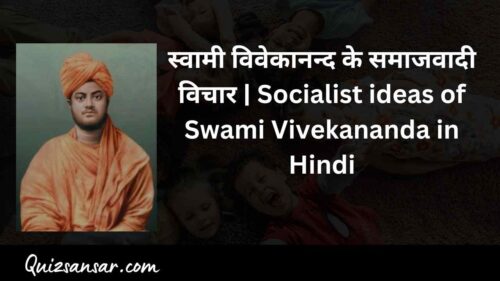
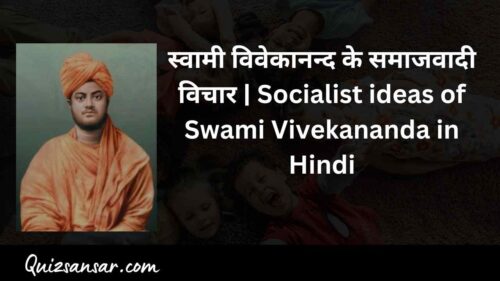
स्वामी विवेकानन्द के समाजवादी विचार | Socialist ideas of Swami Vivekananda in Hindi
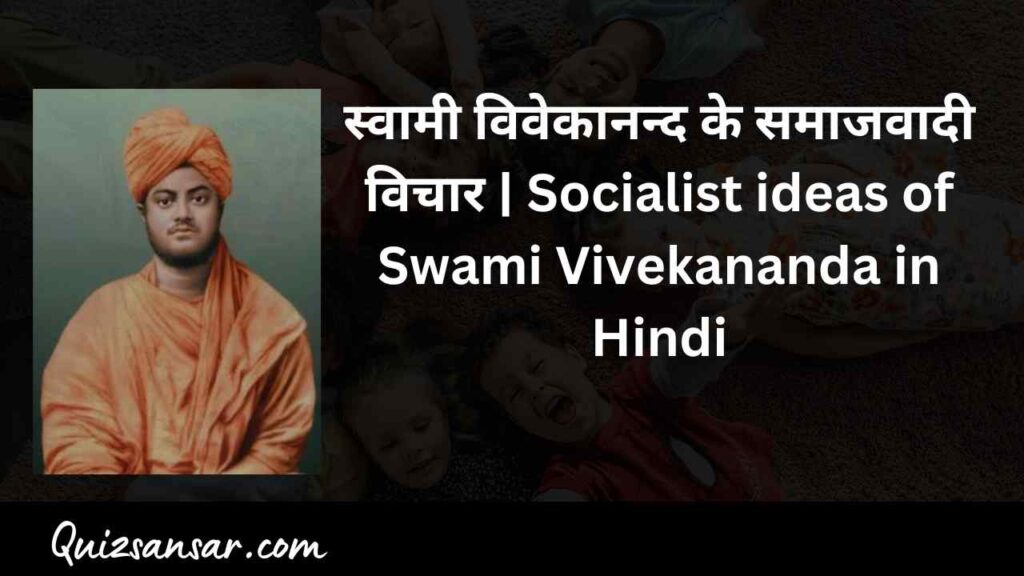
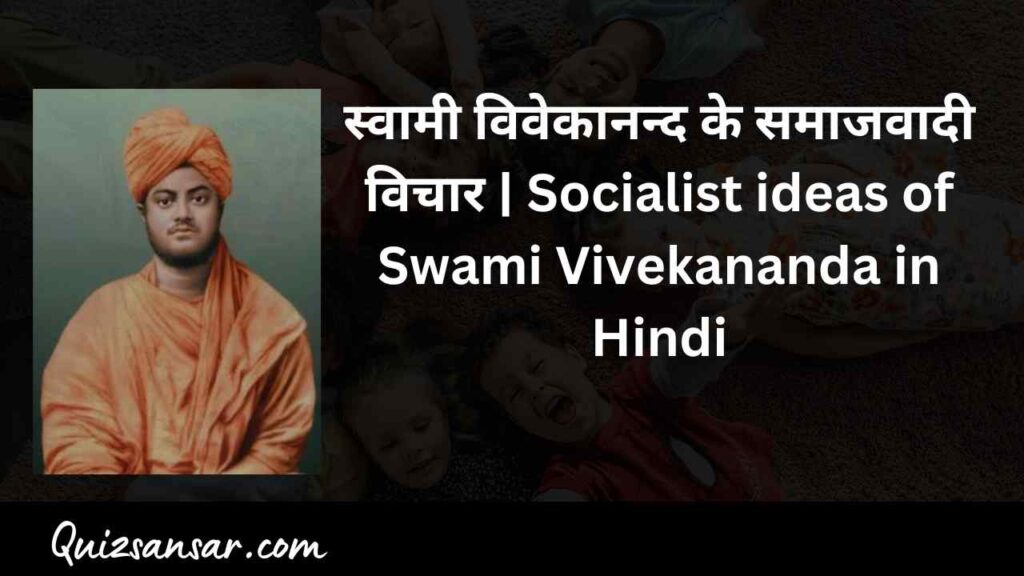
स्वामी विवेकानन्द के समाजवादी विचारों की विवेचना कीजिए।
विवेकानन्द सामाजिक सुधारों के प्रति सजग और इस सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट थे। उनके हृदय में एक आँधी थी, उनकी आत्मा में एक आग थी और वह भारत को जगाना तथा ऊपर उठाना चाहते थे। सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी लगन इसी तथ्य से स्पष्ट है कि उनका आग्रह था कि सामाजिक संघ कार्यों को अध्यात्म साधना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।
समाज का सावयवी रूप- स्पेन्सर के समान समाज के सम्बन्ध में विवेकानन्द की भावना सावयवी थी। उनके अनुसार अनेक व्यक्तियों का समूह समष्टि कहलाता है और अकेला व्यक्ति उसका एक भाग है। व्यक्ति की भांति समष्टि का भी अपना आंगिक जीवन है, उसका भी विकासशील मस्तिष्क और आत्मा है। सामाजिक प्रगति तभी सम्भव है जब उसके घटक कुछ बलिदान करें क्योंकि त्याग अथवा बलिदान किये बिना समष्टि के कल्याण की कामना करना व्यर्थ है। विवेकानन्द के अनुसार मनुष्य और समाज का अस्तित्व शुभ कार्य के लिये है, अतः शुभ कार्य करके ही व्यक्ति अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। व्यक्ति केवल अपने लिये नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है और इसी में उसकी मनुष्यता छिपी है। चूँकि समाज विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसके विकास के लिये व्यक्तियों द्वारा आत्म-त्याग अनिवार्य है। मानवीय सम्बन्धों का अन्तिम लक्ष्य और परिणाम सामूहिक कल्याण होना चाहिए, केवल व्यक्तिगत सुख नहीं।
विवेकानन्द ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके सामाजिक विषमताओं और बुराइयों के उन्मूलन के उपाय बताये। वे सामाजिक संगठन और सामाजिक मामलों में धर्म को सम्मिलित करने के विरुद्ध थे और इसी कारण वे जात-पात, सम्प्रदाय और छुआ-छूत तक सब तरह की विषमताओं के विरुद्ध थे। उनके मुख्य सामाजिक विचारों को अग्रलिखित शीर्षकों में वर्णित किया जा सकता है-
(1) रूढ़िवादिता और अस्पृश्यता – विवेकानन्द ने भारतीय समाज में व्याप्त अश्पृश्यता और रूढ़िवादिता की तीव्र आलोचना को रूढ़िवादिता को उन्होंने ‘रसोई धर्म’ और अस्पृश्यवाद कहकर उसकी भर्त्सना की। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा- “भारत में यह रोना धोना सच है कि हम बड़े गरीब है; परन्तु गरीबों के लिए कितनी दानशील संस्थायें हैं? भारत के करोड़ों गरीबों के दुःख और पीड़ा के लिए कितने लोग असल में रोते हैं? क्या हम मनुष्य हैं? हम उनकी जीविका और उन्नति के लिये क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं, उनकी संगति से दूर भागते हैं क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों ब्राह्मण- भारत की नीच और दलित जनता के लिये क्या कर रहे हैं? ‘मत छू’ – ‘मत छू’ एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथ हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं” “
(2) दलितों का उत्थान – स्वामी जी जाति प्रथा के विरोधी तथा गरीबों और दलितों के लिये उनमें असीम सहानुभूति थी। वे वास्तव में समाजवादी थे जो अमीर और गरीब के भेद को ठुकराकर पद दलितों को सीने से लगाने का सन्देह देते थे और अपने कर्ममय जीवन में, अपने मिशन में उन्होंने यह करके भी दिखाया। उनकी ललकार थी- “गरीब और अभावग्रस्त पीड़ित और पद दलित, सब आओ, हम सब रामकृष्ण की शरण में हैं।” इससे स्पष्ट होता है कि स्वामीजी व्यावहारिक और कार्य करने वाले थे न कि केवल उपदेशक इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा, “हम पूजा के इस ताम-झाम को यानी देव मूर्ति के सामने शंख फूँकना, घण्टा बजाना और आरती करना छोड़ दें। हम शास्त्रों का पठन-पाठन और व्यक्तिगत मोक्ष के लिये सब तरह की साधनाओं को छोड़ देंगे और गाँव-गाँव में जाकर गरीबों की सेवा करें। प्रत्येक को एक सामान्य धरातल पर ले जाना चाहिये। उच्चतर को निम्नस्तर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। एक ओर आदर्श है ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श है चाण्डाल और चाण्डाल को उठाकर उसे ब्राह्मण स्तर तक ले आना ही सम्पूर्ण कार्य है। उनका सन्देश है कि निम्नतर जातियों को संस्कृति दो।
(3) बाल-विवाह विरोधी- विवेकानन्द ने बाल-विवाह की भर्त्सना की और कहा, “जिस प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणिग्रहण होता है, उसके साथ मैं किसी प्रकार के सम्बन्ध रखने में असमर्थ हूँ…… बाल विवाह से असामयिक सन्तानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में सन्तान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं, उनकी दुर्बल और रोगी सन्तान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है आज घर-घर इतनी अधिक विधवायें पायी जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है, यदि बाल-विवाहों की संख्या घट जाये तो विधवाओं की संख्या भी स्वयमेव घट जायेगी।”
(4) जाति प्रथा के विरोधी- विवेकानन्द ने प्रचलित जातिवाद को देश और समाज के लिए हानिकारक मानते हुए कहा कि जाति-भेद केवल एक सामाजिक विधान है जिसकी उपयोगिता पूर्व में चाहे जो भी हो, अब तो वह भारतीय वायुमण्डल में दुर्गन्ध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। जाति भेद का नाश तभी सम्भव है जब लोग अपने खोये हुए सामाजिक व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करेंगे। जाति-प्रथा के विनाश के विषय में स्वामीजी की दृष्टि बहुत पैनी थी। उन्होंने भाँप लिया था कि आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा के युग में जाति-विचार अपने आप भ्रष्ट होता जा रहा है, उसके नाश के लिए किसी धर्म-विज्ञान की आवश्यकता नहीं।” वे जाति का अर्थ सकारात्मक रूप लेते हुए ‘विचित्रता की स्वछन्द गति’ मानते थे। उनके मतानुसार, “जाति का मूल अर्थ था- सैकड़ों वर्षों तक यही अर्थ प्रचलित रहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अपने विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता। चूँकि भारत ने जाति-सम्बन्धी इस भाव का परित्याग कर दिया, अत: वह अधःपतन की स्थिति में आ गया। उनके अनुसार आजकल का वर्ण विभाग अर्थात जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में रुकावट है। सचमुच, इसने सच्ची जाति अर्थात् विचित्रता की स्वच्छन्द गति को रोक दिया है।” जातिवाद भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था, उसे समूल नष्ट करना सम्भव नहीं था। अतः एक यथार्थवादी विचारक के रूप में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाये और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाये।
विवेकानन्द पुरोहित कर्मकाण्ड और परम्परावादी ब्राह्मण के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्त के विरोधी थे। उन्होंने पुरोहित धर्म की कटु शब्दों में निन्दा की, क्योंकि उससे सामाजिक अत्याचार को कायम रखने में सहायता मिलती थी और जनता की उपेक्षा होती थी। उन्होंने परम्परावादी ब्राह्मणों के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्त का खण्डन किया क्योंकि यह सिद्धान्त शूद्रों अर्थात् देश की बहुसंख्यक जनता को वैदिक ज्ञान के लाभ से वंचित करता है। उनके अनुसार “सभी मनुष्य समान हैं, और सभी को आध्यात्मिक अनुभूति तथा वैदिक ज्ञान का अधिकार है।”
(5) यूरोपीयकरण के विरोधी- विवेकानन्द ने सामाजिक जीवन में यूरोप का अनुकरण करने की कटु आलोचना की इस सम्बन्ध में उनके शब्दों के अतिरिक्त दूसरी अच्छी व्याख्या हो ही नहीं सकती। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा- “हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होना चाहिए। विदेशियों ने जो जीवन प्रणाली हमारे ऊपर थोप दी है उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, ऐसा करना असम्भव भी है। परमात्मा को धन्यवाद है कि यह असम्भव है, हमें तोड़-मरोड़ कर अन्य राष्ट्रों की आकृति का नहीं बनाया जा सकता। मैं अन्य जातियों की संस्थाओं की निन्दा नहीं करता, वे उनके लिये अच्छी हैं, किन्तु हमारे लिये अच्छी नहीं हैं। उनकी विद्यायें, उनकी संस्थायें तथा परम्परायें भिन्न है और उन सबके अनुरूप ही उनकी वर्तमान जीवन प्रणाली है। हमारी अपनी परम्परायें हैं और हजारों वर्षों के कर्म हमारे साथ हैं। इसलिये स्वभावतः हम अपनी ही प्रकृति का अनुकरण कर सकते हैं, अपनी ही लकीर पर चल सकते हैं, और हम वही करेंगे। हम पाश्चात्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए पश्चिम का अनुकरण करना निरर्थक है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
