

प्रबन्ध सिद्धान्त की सार्वभौमिकता | universality of management theory in Hindi
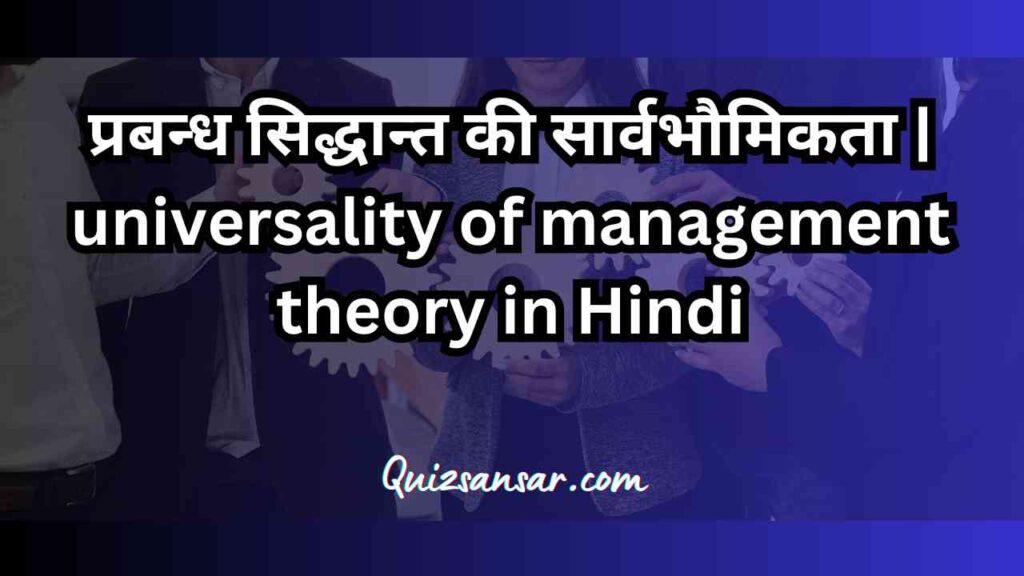
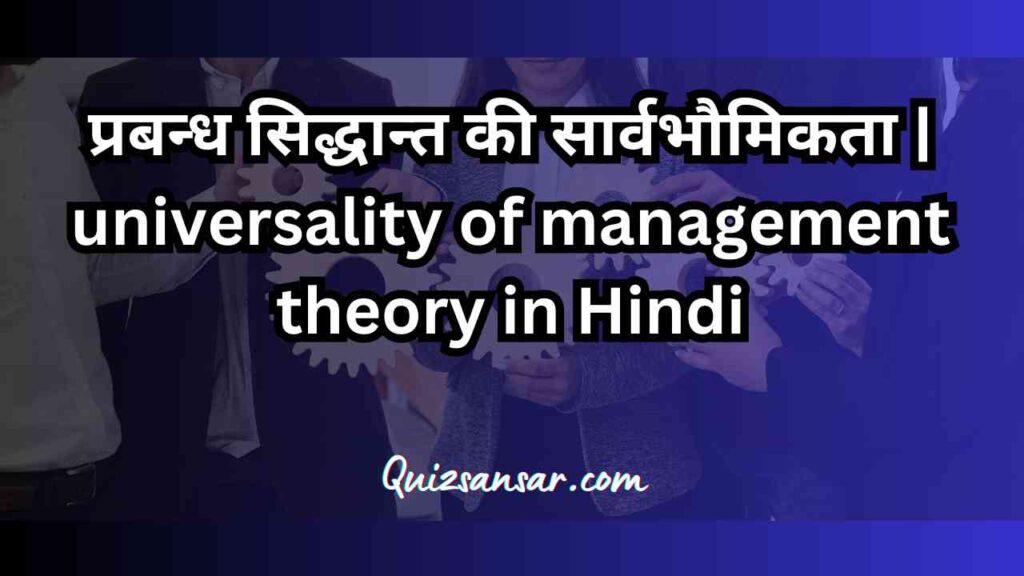
प्रबन्ध सिद्धान्तों की सार्वभौमिकता का वर्णन कीजिए।
सर्वप्रथम, हेनरी फेयोल ने प्रबन्ध प्रक्रिया के सार्वभौमिक होने पर जोर दिया। इसलिए, उन्हें प्रबन्धशास्त्र के इतिहास में सार्वभौमिक होने की संज्ञा दी गई है उन्होंने अपनी पुस्तक ‘जनरल एण्ड इन्ड्रसट्रियल मैनेजमेंट’ में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि प्रबन्ध के सिद्धान्त और कार्यों का व्यापक और सार्वभौमिक उपयोग किया जा सकता है। उनका सभी प्रकार के संगठनों (जैसे, औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सरकारी और सैनिक) में प्रयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों (जैसे उत्पादन, विपणन और वित्त) या प्रबन्ध के सभी स्तरों (जैसे, उच्च, मध्य या पर्यवेक्षण) पर किया जा सकता है। वे सभी देशों और सभी कालों में सत्य होते हैं। अर्विक, कूज एण्ड ओडेनिल, एल.ए. ऐलन, एल.आर. सैलेज, आलीवर सेल्डन, जे.डी.मूनी, सी.आई बर्नाड, सी.आर. फार लैण्ड और ए.एच. एलबर्स, आदि प्रबन्ध शास्त्रियों ने, हेनरी फेयोल की इस सोच से सहमति जताई है। कुंज एण्ड ओडेनिल के शब्दों में, “प्रबन्ध की आधारभूत विचारधारा और सिद्धान्तों का हर संगठन में उसके हर स्तर पर पर प्रयोग होता है। “एलबर्स के अनुसार, “यद्यपि संगठनों के लक्ष्यों में अन्तर होता है, तथापि उनकी प्रबन्ध प्रक्रिया एक ही रहती है। यह प्रक्रिया कारखानों, बैंकों, फुटकर विक्रय संस्थानों सैनिक संगठनों, चर्चा, विश्वविद्यालयों अस्पतालों, आदि में समान पाई जाती है।” और एल.ए.एप्ले लिखते हैं “वह व्यक्ति जो प्रबन्ध कर सकता है, किसी भी चीज का प्रबन्ध कर सकता है।”
प्रबन्ध की इस धारा के विचारकों का मानना है कि प्रबन्ध सिद्धान्तों का उपयोग अत्यन्त व्यापक रूप से किया जा सकता है। जो अनुभव और ज्ञान प्रबन्धक एक संगठन में अर्जित करता है, उसका प्रयोग वह अन्य संगठनों में भी कर सकता है। प्रबन्धकीय ज्ञान, कुशलताएँ और अनुभव हस्तांतरणीय हैं और उनका अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनका स्थानान्तरण एक विकसित देश से विकासशील देश को या एक औद्योगिक देश से कृषि प्रधान देश को किया जा सकता है और इसी तथ्य की वजह से प्रबन्धक के लिए प्रबन्धकीय योग्यताएँ, तकनीकी योग्यताएँ से, अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि ये सिद्धान्त केवल मार्गदर्शक हैं, जो लौचपूर्ण और विभिन्न परिस्थितियों में सामान्यरूप से सत्य होते हैं। इसलिए उनका उपयोग अत्यन्त चतुराई से सभी घटकों पर विचार करके किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, कुछ प्रबन्धशास्त्री प्रबन्ध की ‘सार्वभौमिकता’ की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। पीटर ड्रकर, आर्नेस्टडेल, मैकमिलन, आदि प्रबन्धशास्त्री इस विचारधारा को निम्न तर्कों के आधार पर अस्वीकार करते हैं। प्रथम प्रबन्धकीय सिद्धान्त बहुत सीमित व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकनों पर आधारित जीवन की घटनाओं के मात्र सामान्यीकृत कथन हैं, जो केवल व्यापक रूप से ही सत्य होते हैं। वैज्ञानिक कसौटी के बिना ऐसे कथनों को केवल लोककथा या लोकोक्ति से अधिक नहीं कहा जा सकता। इनमें से कुछ सिद्धान्त बहुत अस्पष्ट एवं भ्रान्तिपूर्ण हैं, तो कुछ इतने व्यापक और सामान्य कि उन्हें संगठन की विशेष समस्याओं में प्रयोग करना बहुत कठिन हैं। भ्रान्तियाँ तब और बढ़ जाती हैं जब दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त समक्ष आते हैं। उदाहरण के लिए, ‘विशिष्टीकरण का सिद्धान्त’ आदेश की एकता के सिद्धान्त के साथ असंगत है क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि एक अधिकारी सभी बातों का विशेषज्ञ हो। अतः ‘सार्वभौमिकता’ का दावा हास्यासपूर्ण लगता है। द्वितीय, प्रबन्ध संस्कृति से जुड़ा होता है। अतः प्रबन्ध सिद्धान्तों का प्रयोग किसी विशेष संस्कृति तक ही सीमित हो सकता है। फार्मर और रिचमैन के शब्दों में, “यदि कोई देश शक्तिशाली रूढ़िवादी, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा है, तो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक व्यवहार के प्रति विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में, आधुनिक प्रबन्धकीय विधियों को लागू करना बहुत कठिन कार्य होगा जो संसार की अधिक विवेकपूर्ण और तकनीकी परामर्श पर आधारित है। इसलिए किन्हीं ऐसे सामान्य सिद्धान्तों की खोज बेकार हैं जहाँ प्रबन्धकों को बहुत ही विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में काम करना होता है। तृतीय एक संगठन से दूसरे संगठनक के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न होते हैं और यही निर्धारित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबन्धकों की योग्यताएँ, क्षमताएँ और तकनीकें किस प्रकार की हों, अतः पीटर ड्रकर का मानना है कि प्रबन्ध की योग्यताएँ, क्षमताएँ और अनुभव जो प्रबन्धक ने एक संगठन में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित किये हैं, उनका उपयोग दूसरे संगठनों में, दूसरे उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित किये हैं, उनका उपयोग दूसरे संगठनों में, दूसरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। यह कितना हास्यास्पद है कि एक क्रिकेट टीम का सफल कप्तान एक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अथवा एक कम्पनी के प्रबन्ध संचालक के रूप में उतना ही सफल होगा। एक संगठन के बदले हुए उद्देश्य, उनमें अन्तनिर्हित दर्शन और वातावरण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों, एवं व्यवहारों की अपेक्षा रखते हैं। जब एक संगठन का उद्देश्य अधिकतम लाभों को कमाना हो, और दूसरे का समाज की सेवा करना, तो किन्हीं समान सिद्धान्तों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति करना संगठनों के लिए असम्भव कार्य ही है। अतः प्रबन्ध सिद्धान्तों की सार्वभौमिकता की विचारधारा को ये प्रबन्धशास्त्री स्वीकार नहीं करते।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
