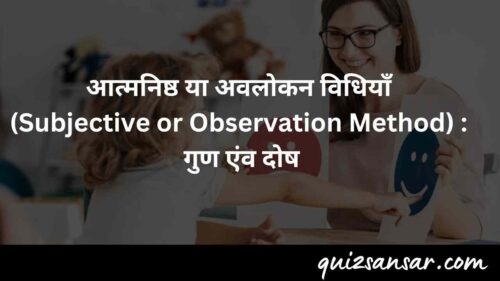
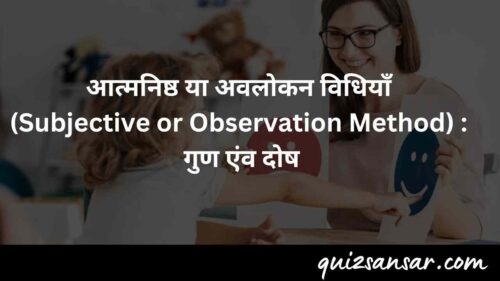
आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष


आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method)
इसके अन्तर्गत निम्न विधियाँ सम्मिलित हैं-
आत्मनिरीक्षण विधि (Introspective Method)
इस विधि को अन्तर्दर्शन, अन्तः निरीक्षण या अन्तर्मुखी अवलोकन विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि मनो विज्ञान की परम्परागत अर्थात् सबसे प्राचीन विधि है। इसका नाम इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक से सम्बद्ध है जिन्होंने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी थी, “मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण।”
According to Lock, “The notice which the mind takes of its own operations.” (Self Observation)
इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते है कि Introspection शब्द दो शब्दों ‘Intro’+ ‘Spection’, से मिलकर बना है जिसमें ‘Intro’ का अर्थ है भीतर या अन्दर तथा ‘Spection’ का अर्थ है- झाँकना ।
अतः शाब्दिक अर्थ में Introspection का अर्थ है “अपने अन्दर या भीतर झाँकना” । वुडवर्थ ने इसे ‘स्व अवलोकन’ (Self Observation) कहा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करता है।
स्टाउट के अनुसार, “अपने मस्तिष्क के क्रिया कलापों का क्रमबद्ध ढंग में अध्ययन करना ही अन्तर्दशन् है।”
According to Stout, “To Introspect is to attend to the working of one’s own mind in a systematic way.”
इसकी व्याख्या करते हुए बी. एन. झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं।
आत्मनिरीक्षण विधि के गुण या लाभ (Merits or Advantages of Introspection Method)
इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं-
1) सरल तथा कम व्यय वाली विधि (Simple and Economical Method) – सरलता इस विधि का एक मुख्य गुण है क्योंकि इस विधि के द्वारा बालकों की मनोदशा का आसानी से ज्ञान हो जाता है। इस विधि को हम कम व्यय वाली विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोगशाला, मूल्यवान उपकणों या किसी दूसरे सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में किसी विशेष यन्त्र या सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण यह विधि खर्चीली नहीं है तथा दूसरी तरफ चूँकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह विधि बहुत सरल है।
2) मानसिक क्रियाएँ (Mental Processes) — इस विधि के द्वारा हम ऐसी मानसिक क्रियाओं को भी देख सकते हैं जिन्हें हम किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहते है। जैसे- लिंग अनुभव (Sex Experiences)|
3) प्रत्यक्ष अध्ययन (Direct Study) – यह विधि हमें बालकों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से कराती है जैसे स्वयं पुरस्कार प्राप्त होने पर या किसी अन्य बालक को पुरस्कार पाता देखकर उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों का ज्ञान बालकों से पूछकर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हमें उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में सहायता प्राप्त होती है।
4) रचनात्मक विधि (Creative Method) – इस विधि के द्वारा बालकों में किसी विषय के सम्बन्ध में सोचने-विचारने तथा समझने की शक्ति बढ़ती है अर्थात् उसे खास विषय पर ध्यान केन्द्रित करने का भी पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा बालकों को आत्म मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होता हैं क्योंकि स्वयं को पहचानने के लिए अन्तर्मुखी (introvert ) होना आवश्यक है।
5) विश्वसनीय परिणाम (Reliable Results) – इस विधि का प्रयोग कर हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मनोदशा का अध्ययन करता है तदुपरान्त उसे व्यक्त करता है और उसी के आधार पर कोई परिणाम निकाला जाता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन में अनुमान, पूर्वधारणा, अन्दाजा, आदि का प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।
6) अपूर्ण विधि (Incomplete Method) – आत्मनिरीक्षण विधि को एक अपूर्ण विधि भी कहा जा सकता है क्योंकि इस विधि का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान के अतिरिक्त किसी भी दूसरे विज्ञान में नहीं होता है। इस प्रकार यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान को एक अपूर्ण विज्ञान बनाती है।
7) कोई भी स्थान और समय (No Bar of Time and Place) – चूँकि इस विधि में व्यक्ति का मस्तिष्क ही उसकी प्रयोगशाला होता है। अतः इस विधि का उपयोग किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर किया जा सकता है।
8) व्यक्तित्व में सुधार ( Improvement in Personality) – यह विधि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार लाने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति में कोई असाधारणता हो तो इस विधि द्वारा उसे दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं।
9) प्रयोगात्मक रिपोर्ट का भाग (Part of Experimental Report) – प्रयोगात्मक रिपोर्ट लिखते समय हम विषयी की अन्तर्मुखी रिपोर्ट भी सम्मिलित करते हैं अतः यह प्रयोगात्मक रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
10) शिक्षण में सुधार ( Improvement in Teaching) – अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को इस विधि की सहायता से नवीन ढंग के सुझावों द्वारा अधिक अच्छा बना सकता है।
इस प्रकार इस विधि में गुणों की महत्ता दर्शाते हुए डगलस व हॉलैण्ड के शब्दों में, “मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है।”
आत्म निरीक्षण विधि के अवगुण (दोष) या सीमाएँ (Demerits or Limitations of Introspection Method)
यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अतः इस विधि की अपनी सीमाएँ हैं उन्हीं को इसकी कमियाँ और दोष माना जाता है-
1) आत्मनिष्ठ (आत्मगत विधि) (Subjective Method) – यह विधि पूर्णतया व्यक्ति (विषयी) की योग्यता एवं स्व क्षमता पर आश्रित है इसमें व्यक्ति के स्व-अनुभव, विचार और निर्णय होते हैं अतः यह व्यक्तिनिष्ठ होती है, उससे प्राप्त निष्कर्षो पर पूर्णतया विश्वास भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसके आधार पर कोई सिद्धान्त या नियम बनाए जा सकते हैं। अतः आत्मगत होने के कारण यह विधि अवैज्ञानिक है।
2) अविश्वसनीयता (Unreliability ) – विश्वसनीयता को इसका एक गुण बताया गया है। जो कि युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपनी मनोदशा का अध्ययन करते समय यह सम्भव है कि व्यक्ति अपनी सत्य (सही) बातों को छिपा ले और झूठ (गलत) बातें बता दे। इस स्थिति में जो भी परिणाम निकाला जाएगा वह निश्चित ही गलत होगा।
3) मनोदशा की चंचलता (Versatility of Mental State) – मानसिक दशाएँ या प्रक्रियाएं इतनी चंचल होती हैं कि उनका ठीक-ठीक अध्ययन करना तथा अध्ययन के अनुसार उनको सही (उसी रूप में व्यक्त करना लगभग असम्भव कार्य है । अत्यंत छोटे बालकों के लिए तो यह अत्यंत मुश्किल कार्य है क्योंकि उनमें ध्यान को केन्द्रित करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वे अपनी चंचल मानसिक स्थिति का अध्ययन (निरीक्षण) यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकते। अतः यह विधि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए भले ही उपयुक्त हो किन्तु प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यह विधि पूर्णतया अनुपयुक्त है।
4) ध्यान विभाजन (Distraction of Mind) – यह विधि व्यक्ति का ध्यान विभाजित करने में विश्वास रखती हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को प्रयोज्य और निरीक्षण दोनों का कार्य एक ही समय पर करना पड़ता है। अतः एक ओर तो वह अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण करता है तथा दूसरी तरफ वह उसी मानसिक स्थिति का शिकार बना रहता है। अतः उसका ध्यान दोनों तरफ विभाजित रहता है।
किंतु मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों तथा व्यक्ति के स्व-अनुभव के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ध्यान का विभाजन सम्भव ही नहीं है। अतएव कोई भी व्यक्ति एक ही समय में प्रयोज्य तथा निरीक्षक का कार्य नहीं कर सकता है और यदि करता है तो इस आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं हो सकता।
5) मनोदशा का विस्थापन (Displacement of Mental State)- इस विधि के द्वारा जैसे ही किसी मनोदशा का निरीक्षण प्रारम्भ होता है वह मनोदशा ही विस्थापित हो जाती है और तुरन्त दूसरी मनोदशा का निरीक्षण वास्तविक रूप में नहीं कर पाता है, अतः मनोदशा का विस्थापन इस विधि का प्रमुख अवगुण है।
जैसे- यदि कोई बच्चा क्रोध की अवस्था में है और उससे उस समय होने वाली अपनी मनोदशा का निरीक्षण करने के लिए कहा जाए तो यह जब तक वह निरीक्षण आरम्भ करता है तब तक क्रोध की स्थिति विस्थापित होकर चिन्तन या दूसरी मानसिक स्थिति में बदल जाएगी और यदि ऐसा नही भी होता है तो भी निश्चित रूप से निरीक्षण के समय क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी। अतः किसी भी हालत में वास्तविक मनोदशा का यथार्थ निरीक्षण या अध्ययन सम्भव नहीं होगा।
6) भाषा का प्रभाव (Effect of Language) – इस विधि पर भाषा का गहरा असर पड़ता है क्योंकि जिन बालकों में भाषा विकसित ही नहीं है उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा सम्भव नहीं है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि गूँगे, बहरे तथा भाषा विकृत बालकों की मनोदशा का अध्ययन इस विधि से सम्भव नहीं है।
7) अवलोकन अनुदर्शन (Retrospection)— आत्मनिरीक्षण विधि में हम स्मरण शक्ति से काम लेते हैं, जब हम स्मरण से काम लेते हैं, तो यह अवलोकन अनुदर्शन बन जाता है क्योंकि हम अपने भीतर झाँकने के बजाय अपने भूतकाल में झाँक रहे होते हैं।
8) सार्वभौमिक प्रयोग नही (Universally not Applicable) – इस विधि द्वारा सार्वभौमिक प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इस विधि को शिशु बालकों, असाधारण लोगों, जंगलियों, अशिक्षितों तथा जानवरों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस विधि के दोषों का अध्ययन कर हम कह सकते हैं कि सम्भवतः इसके दोषों के कारण ही मनोवैज्ञानिकों में आत्मनिरीक्षण विधि का परित्याग कर दिया है। डगलस एवं हॉलैण्ड (Douglas and Holland) का मत है कि यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो दिया है।
निष्कर्ष (Conclusion)
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यूँ तो वर्तमान युग में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अनेकानेक वैज्ञानिक विधियाँ विकसित हो चुकी हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग आज भी बहुत लाभकारी होता है, मुख्यतः तब, जब अध्ययनकर्ता को अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की सत्यता की जाँच करनी हो और तब, जब अन्य विधियों से प्राप्त परिणामों की तुलना करनी होती है।
IMPORTANT LINK
- आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधियाँ (Subjective or Observation Method) : गुण एंव दोष
- गाथा विवरण विधि (Anecdotal Method) : गुण एंव दोष
- निरीक्षण विधि (Observation Method) : गुण एंव दोष
- प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) : गुण एंव अवगुण
- जीवन – इतिहास विधि (Case History / Study Method) : गुण एंव दोष
- उपचारात्मक विधि (Remedial Method) : गुण एंव दोष
- तुलनात्मक विधि – अर्थ, गुण एंव दोष | Comparative Method -Meaning, Merits and Demerits
- विकासात्मक विधि (Developmental Method) : गुण एंव दोष
- मनोविश्लेषण विधि (Psycho- Analytic Method) : गुण एंव दोष
Disclaimer: quizsansar.com does not own this book, PDF Materials Images, neither created nor scanned. The material and information contained on this website is for general information purposes only. If you have a complaint about something or find your content is being used incorrectly then kindly mail us: sansarquiz@gmail.com
