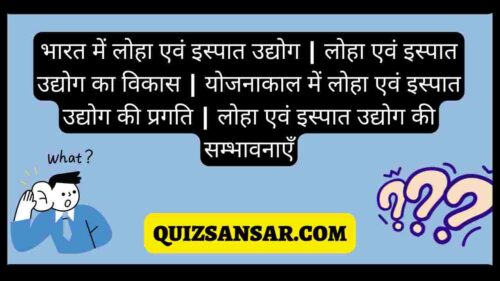
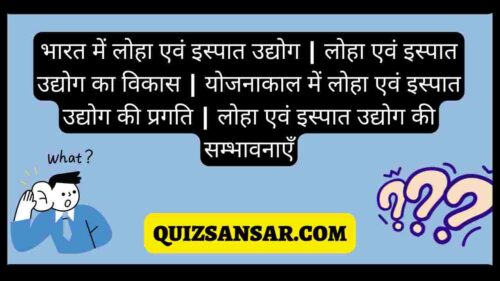
भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग | लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास | योजनाकाल में लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति | लोहा एवं इस्पात उद्योग की सम्भावनाएँ
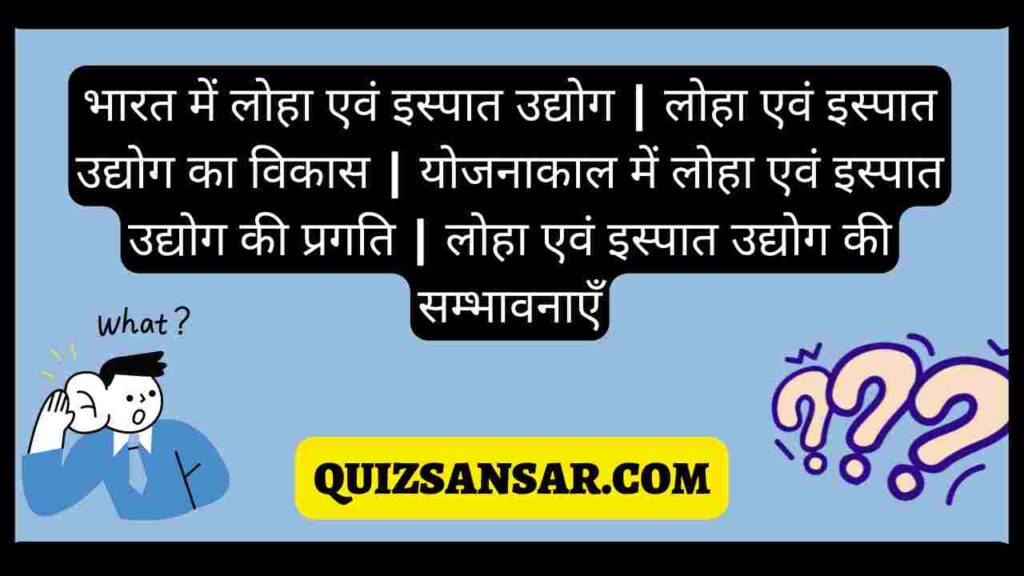
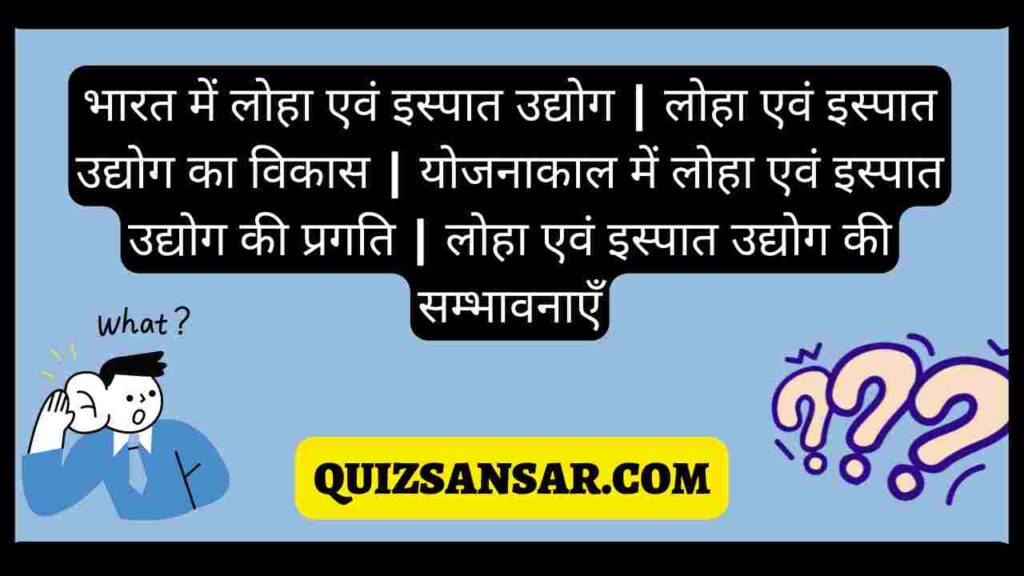
भारत के लोहा एवं इस्पात, उद्योग के विकास, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्भावनाओं की विवेचना कीजिए।
Table of Contents
भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग
लोहा एवं इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। दिल्ली में कुतुबमीनार के निकट लोहे की अशोक की लाट इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कोणार्क के सूर्य मन्दिर तथा पुरी के उद्यान मन्दिर की लोहे की छड़े भी इस उद्योग के प्राचीन गौरव का प्रतीक है। भारत में इस उद्योग के विकास के लिये प्रकृति बड़ी धनी है। यहाँ कोयला व लोहा पास-पास पाये जाते हैं। भारत में 2,100 करोड़ टन कच्चे लोहे के भण्डार होने का अनुमान है। यह विश्व के लोहे के भण्डार का 1/5 भाग है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट तथा मैंगनीज आदि, जो इस उद्योग के लिये कच्चे माल का काम देते हैं, भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।
लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास
आधुनिक रूप में इस उद्योग का प्रारम्भ 1830 में हुआ, परन्तु यह प्रयोग असफल रहा। 1874 में बंगाल में झरिया के निकट बाराकर स्टील वर्क्स की स्थापना की गयी । यहाँ केवल लोहा बन सकता था, इस्पात नहीं। 1875 में आसनसोल बंगाल आयरन कम्पनी तथा बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 1907 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO), 1918 में आसनसोल के पास हीरापुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) तथा 1023 में मैसूर के भद्रावती में मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स आदि कारखाने स्थापित किय गये। प्रथम महायुद्ध में लोहे की माँग एवं मूल्य बढ़ने के कारण इस उद्योग को उन्नति करने का अवसर मिला। इस अवधि के दौरान टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने बहुत उन्नति की, परन्तु 1921-22 के बाद विदेशी इस्पात का मूल्य गिरने से भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति रुक गयीं। 1924 में इस उद्योग को सरंक्षण मिला जो 31 मार्च, 1947 तक चलता रहा। इस प्रकार इस 23 वर्षों तक इस उद्योग को सरंक्षण मिलता रहा। 1936 में इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी तथा बंगाल आयरन कम्पनी का संविलयन करके 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1939 में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन क्रमशः 18 तथा 8 लाख टन था। द्वितीय महायुद्ध काल में इस्पात की माँग में वृद्धि होने से इसके मूल्य में भी वृद्धि हो गयी। उत्पादन के साथ-साथ इसकी किस्म में भी सुधार हुआ। 1950 में भारत में इस्पात का वार्षिक उत्पादन 10 लाख टन तथा कच्चे लोहे का उत्पादन 15 लाख टन था। द्वितीय महायुद्ध के बाद माँग कम होने से लोहा एवं इस्पात के मूल्य घटने लगे और उद्योग पुनः संकट में फँस गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में तीन कारखाने थे-टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO), इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) तथा मैसूर आयरन वर्क्स।
योजनाकाल में लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में निजी क्षेत्र का विकास किया गया जिसमें 49.4 करोड़ रूपये व्यय किये गये तथा इस योजना की समाप्ति से पूर्व मार्च, 1955 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन बड़े इस्पात कारखाने प्रारम्भ करने के लिए रुस, पश्चिमी जर्मनी एवं इंग्लैण्ड से समझौते किये।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। तथा राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (बंगाल) में तीन बड़े स्टील के कारखाने लगाये गये। इसके अतिरिक्त टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) की क्षमता का विस्तार किया गया। इस योजना के अन्त में लौह खनिज और तैयार इस्पात का उत्पादन क्रमशः 11 मि. टन और 2.39 मि. टन हो गया तथा इस्पात उद्योग की क्षमता लगभग 5 मि. टन हो गई, परन्तु तकनीकी कठिनाइयों के होने से इस क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका।
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में लोहा एवं इस्पात उद्योग के अनेक विकास कार्यक्रम बनाये गये जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में तीनों कारखानों की उत्पादन क्षमता को पर जोर दिया गया तथा बोकारों (बिहार) में अमेरिका की सहायता से एक स्टील का बड़ा दुगुना कारखाना लगाने का निश्चयस किया गया, परन्तु इस योजना में न तो बोकारों में इस्पात का कारखाना लगाया गया और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमत करने को लक्ष्य के अनुसार बढ़ाया जा सका। जनवरी, 1966 में बोकारों कारखाने के लिए रूस से समझौता किया गया।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में इस्पात की सिल्लियों तथा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 10.8 तथा 8.1 मि. टन रखा गया, परन्तु इन लक्ष्यों को प्राप्त नही किया जा सका क्योंकि इनका उत्पादन क्रमशः 6.61 तथा 4.89 मि. टन हुआ जिसके मुख्य कारण बोकारों कारखाने के निर्माण में देरी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में क्षणता विस्तार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित न किया जाना तथा मिलाई के विस्तार कार्यक्रम की प्रगति धीमी रहना है। इस उद्योग को विकसित करने के लिये एक सरकारी कम्पनी स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. (Sail) की स्थापना की गई तथा अन्य तीन नये कारखाने लगाने का निश्चय किया गया -(1) सलेम (तमिलनाडु), (2) विजयनगर (कर्नाटक), (3) विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)। 14 जुलाई, 1972 को सरकार ने कुप्रबन्ध के कारण इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में इस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिये 1,675 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान किया गया तथा इस योजना के अन्त तक तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 9.4 मि. टन रखा गया, बाद में जिसको संशोधित करके 8.8 मि. टन कर दिया गया, जबकि इस योजना के अन्त तक तैयार इस्पात का वास्तविक उत्पादन 6.6 मि. टन हो सका। इस योजना में भिलाई संयन्त्र की क्षमता में 4 मि. टन का विस्तार करने, बोकारों का निरन्तर विस्तार करने तथा विशाखापट्टनम व विजयनगर संयन्त्रों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की योजना बनायी गयी। 17 जुलाई, 1976 को सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था।
छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में इस उद्योग के विकास के लिये 3,613 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में लोहा एवं इस्पात के विकास के लिये अपनाई गई व्यूह रचना इस प्रकार थी- (i) उद्योग के विकास में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं का समाधान करना, (ii) बोकारों, दुर्गापुर और राउरकेला संयन्त्रों की आवश्यक संचालन क्रियाओं की पूर्ति के लिय सम्बन्धित शक्ति संयन्त्रों की व्यवस्था करना, (iii) धमन भट्टियों में कोयले के प्रयोग, स्टील निर्माण प्रक्रिया तथा उत्पादकता के सम्बन्ध में शोध एवं अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना (iv) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करना तथा (v) इस उद्योग की विस्तार योजनाओं के शीघ्रता से लागू करना। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. की स्थापना की गई जिसे विशाखापट्टनम इस्पात संयन्त्र स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया। इस योजना में तैयार इस्पात की माँग 12.9 मि. टन होने का अनुमान लगाया गया, जबकि इस योजना के अन्त तक तैयार इस्पात का वास्तविक उत्पादन केवल 7.8 मि. टन हो सका। माँग एवं पूर्ति के इस अन्तर को आयात के द्वारा पूरा किया जाना था। इस योजना में भिलाई और बोकारों कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य भी रखा गया। इस योजना में उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में इस्पात पिण्ड और तैयार इस्पात के उत्पादन करने के लक्ष्य क्रमशः 15.38 मि. टन और 12.64 मि. टन निर्धारित किये गये, जबकि इस योजना के अन्त तक इस्पात पिण्ड और तैयार इस्पात का वास्तविक उत्पादन क्रमशः 13.72 मि. टन और 13 मि. टन हो सका। इस योजना में इस उद्योग में कोई नई बड़ी परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई। इस योजना में बोकारों तथा भिलाई संयन्त्रों के विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने, विशाखापट्टनम संयन्त्र के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने और सभी संयन्त्रों में आधुनिकीकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया। इस योजना में बोकारों और भिलाई संयन्त्र की क्षमता का विस्तार किया गया तथा टिस्को के आधुनिकीकरण कार्यक्रम क द्वितीय चरण को पूरा किया गया।
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस्पात उद्योग के विकास कार्यक्रमों में विद्यमान इस्पात संयन्त्रों के आधुनिकीकरण तथा तकनीक के उच्चीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया गया है जिससे कि किस्म और मूल्य दोनों दृष्टियों से इस उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शक्ति मे बढावा जा सके। इस योजना के अन्त में उत्पादन के लक्ष्य तप्त धातु के लिए 20 मि. टन विक्रय योग्य कच्चा लोहा के लिए 2.16 मि. टन इस्पात पिण्ड के लिए 18.23 मि. टन और विक्रय योग्य इस्पात के लिए 15.94 मि. टन निर्धारित किए गए।
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) के अन्त में उत्पादन के लक्ष्य कच्चा लोहा के लिए 10.44 मि. टन इस्पात पिण्ड के लिए 24.35 मि. टन उत्पादन रहा।
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अन्त में उत्पादन लक्ष्य कच्चा लोहा के लिए 12.54 मि. टन इस्पात के लिए 45.18 मि. टन उत्पादन रहा।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्तर्गत लोहा का उत्पादन लक्ष्य 20.74 मि. टन तथा इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 64.87 मि. टन रहा।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत लोहा का उत्पादन लक्ष्य 32.35 मि. टन तथा इस्पात का उत्पादन 87.39 मि. टन रहा।
लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति
भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है-
|
संयन्त्र सार्वजनिक क्षेत्र : |
उत्पादन क्षमता |
| 1. राउरकेला संयन्त्र (Rourkela Plant) |
1.8000 |
| 2. भिलाई संयन्त्र (Bhilai Plant) | 4.0000 |
| 3. दुर्गापुर संयन्त्र (Durgapur Plant) | 1.6000 |
| 4. बोकारों स्टील प्लाण्ट (Bokaro Steel Plant) | 4.0000 |
| 5. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) | 1.0000 |
| 6. एलॉय स्टील प्लाण्ट (ASP) | 0.2600 |
| 7. विश्वेश्वरैय्या आयरन एण्ड स्टील लि. (VISL) | 0.0072 |
| 8. सेलम स्टील प्लाण्ट (SSP) | 0.0032 |
| 9. विशाखापट्टनम स्टील संयन्त्र (VSP) | 3.4000 |
| निजी क्षेत्र :
1. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) |
2.1600 |
भारत में उपर्युक्त लोहा एवं इस्पात के बड़े औद्योगिक उपक्रमों के अतिरिक्त 179 मिनी इस्पात कारखानें (Mini Steel Plant) हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 7.8 मिलियन टन है। यह उद्योग भारत का विशालतम एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें लगभग 10.000 करोड़ रूपये की पूँजी विनियोजित है और लगभग 2.4 लाख व्यक्तियों को इस उद्योग में रोजगार मिला हुआ है।
लोहा एवं इस्पात उद्योग की सम्भावनाएँ
इस उद्योग को निम्न प्रकार विकसित करना होगा-
( 1 ) एकीकृत इस्पात प्लाण्ट कार्यक्रम ( Integrated Steel Plant Programmes) – भारत के लोहा एवं इस्पात उद्योग को विकास के विभिन्न चरण पूरे करने के लिए एकीकृत स्टील प्लाण्ट कार्यक्रम प्रारम्भ करना होगा ताकि विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस कार्यक्रम में समुद्रतटीय इस्पात संयंत्रों को आयातित कोयले द्वारा संचालित करने का शीघ्र निर्णय लेकर उत्पादन कार्य प्रारम्भा कर देना चाहिए। इसके अलावा भिलाई विस्तार योजना, बोकारों संयंत्र की द्वितीय चरण योजना व विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र योजना को निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य बनाना चाहिए।
( 2 ) लघु इस्पात प्लान्ट कार्यक्रम (Mini Steel Plant Programme ) – भारत में लघु इस्पात प्लाण्ट कार्यक्रम भी अपनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत विद्युत भट्टियां विकसित की जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका व जापान आदि देशों में लोहा पिघलाने के लिए विद्युत भट्टियां प्रयोग की जाती हैं। इन विद्युत भट्टियों पर प्रति टन इस्पात तैयार करने में 60 डॉलर व्यय होते हैं जबकि भारत के एकीकृत संयंत्रों में 500 डॉलर प्रति टन व्यय होता है। इसलिए भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों के लिए विद्युत भट्टियां संचालित करना एक मितव्ययितापूर्ण कदम होगा।
