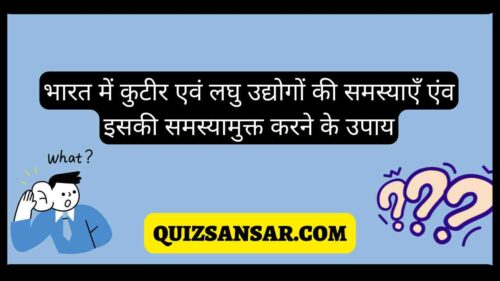
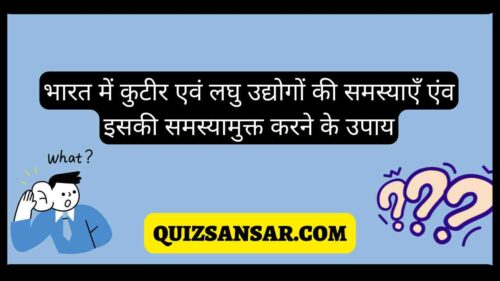
भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ एंव इसकी समस्यामुक्त करने के उपाय
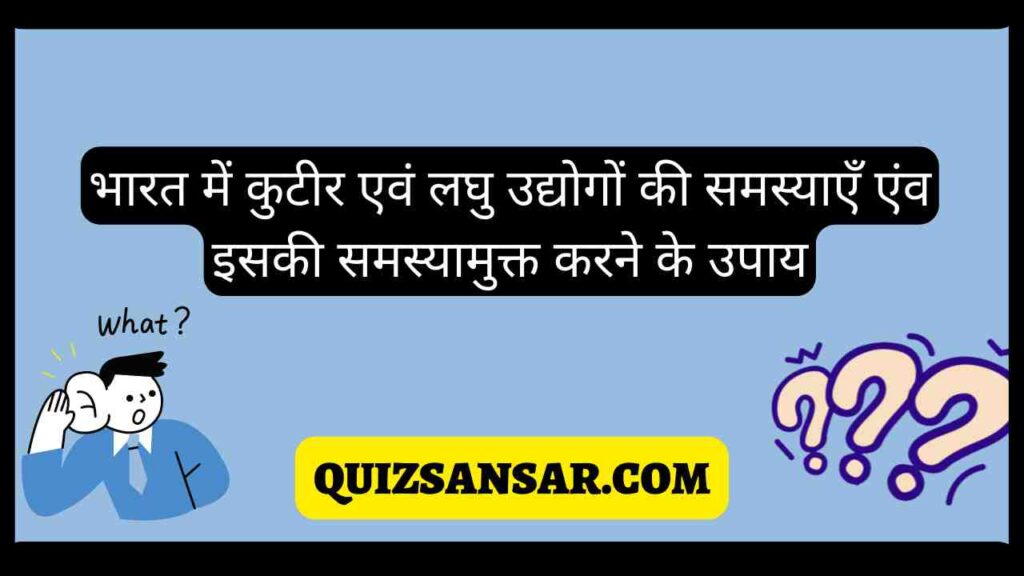
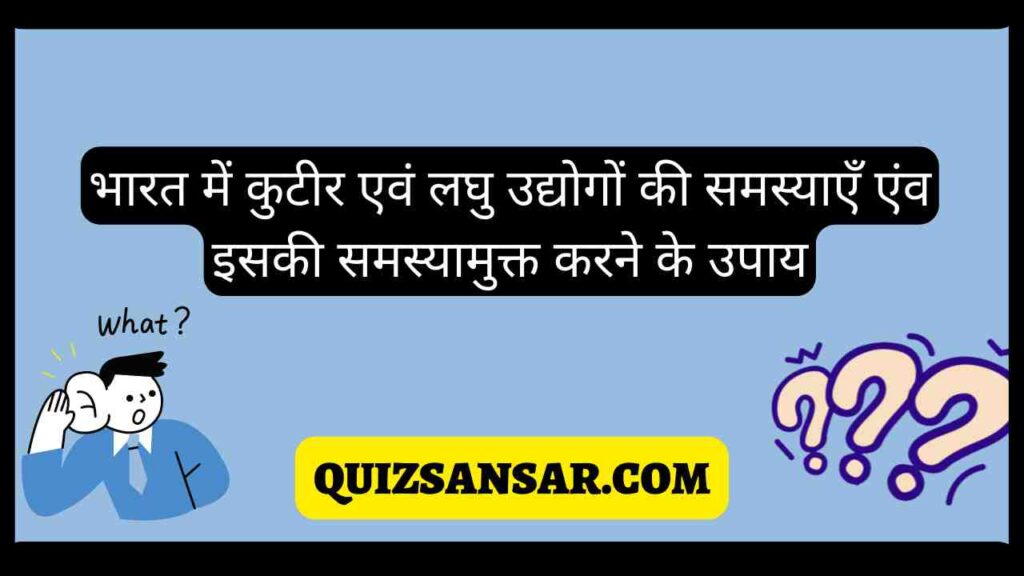
भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की क्या समस्याएँ हैं? कुटीर एवं लघु उद्योगों को समस्या मुक्त करने के उपाय बताइये।
भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याएँ
कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-
(1) कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw Material)- अधिकांश कुटीर उद्योग कच्चे माल हेतु स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन स्थानीय स्रोत दोहरा शोषण करते हैं, जैसे-कच्चे माल को ऊंचे दाम पर बेंचना व निर्मित माल कम कीमत पर खरीदना। लघु उद्योग जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन सामान्यतः बड़े उद्योग करते हैं, फलस्वरूप लघु उद्यमी कच्चे माल से वंचित रह जाते हैं, जबकि बड़े उद्यमी कच्चे माल को थोंक में खरीद लेते हैं।
( 2 ) वित्त की समस्या (Problem of Finance) – कुटीर एवं लघु उद्योगों की सर्वाधिक गम्भीर वित्तीय समस्या है, क्योंकि ऐसे उद्यमों को वित्त प्राप्त करने में विशेष कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, जो लघु उद्यमियों के लिए कठिन है। इसके अलावा वित्त प्राप्त करने में समय की बर्बादी होती है जिसे लघु उद्यमी निराश होकर बैंक, वित्त निगम व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि का सहारा छोड़कर स्थानीय महाजन अथवा साहूकर से ऋण प्राप्त कर लेता है।
( 3 ) बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धी की समस्या ( Problem of Competition from Large Industries) – भारत में बड़े उद्योग की तरह लघु उद्योग भी स्वतन्त्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन क्रियायें करते हैं। इससे दोनों प्रकार के उद्योगों में न केवल बाजारी-प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, बल्कि कच्चे माल, वित्त सुविधा प्राप्त करने में भी कलागाट प्रतिस्पर्धा होती है। इसी का परिणाम है कि लघु उद्योग बीमार उद्योग हो जाते हैं।
( 4 ) विपणन की समस्या (Problem of Marketing)- (अ) चूंकि ऐसे उद्यमियों की बाजार में कोई दुकाने कोई नहीं होती है, जहाँ उत्पादित माल सरलता से बेचा जा सके। फलतः फुटपाथ पर वस्तुएं रखकर विपणन करना पड़ता है।
(ब) ऐसे उत्पादकों को अपनील वस्तुएँ बिचौलिये के हाथों बेचनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें वस्तु की उचित कीमत नहीं मिल पाती है।
(स) ऐसे उत्पादकों की वस्तुएं प्रमापीकृत व वर्गीकृत नहीं होती है, अतः प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग मूल्य होता है।
(द) ऐसे उत्पादकों के उपभोक्ताओं की रुचि का ज्ञान नहीं होता है, अतः रुचि के विपरीत वस्तुएं उत्पादित होने पर उन्हें कम मूल्य पर वस्तुएं बेचनी पड़ती है।
(5) प्रमापीकरण की समस्या (Problem of Standardisation)- भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों का उत्पादन सदैव अप्रमापित रहता है, जिससे उन्नत किस्म समरूप व वर्गीकृत वस्तुओं का अभाव है। इससे उद्यम के श्रमिक, कारीगर व मालिक उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
( 6 ) अकुशल कारीगरों की समस्या (Problem in Inefficient Workers) – कुटीर एवं लघु उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि लघु उद्यमी न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को उद्योग में रखते हैं, इसका कुप्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। अतः असल मजदूरी न मिलने के कारण भी कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं होते हैं।
( 7 ) करभार की समस्या (Problem of Taxation)- सरकारी आदेशों में कुटीर एवं लघु उद्योगों कर मुक्त हैं। वास्तव में कुटीर उद्योग कर मुक्त है, परन्तु लघु उद्योग अनेकानेक करों से दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उत्पादन कर, रजिस्ट्रेशन फीस, आयकर, बिक्री कर व स्थानीय करों का भुगतान करना पड़ता है। अतः कुटीर एवं लघु उद्योगों का कर भार ऐसा है जिसे उपभोक्ताओं पर भी विवर्तित नहीं किया जा सकता है।
(8) कुशल प्रबन्ध व्यवस्था का अभाव (Lack of Efficient Administrative Strategy)- यदि कुटीर हैं, जिनमें लघु स्तरीय उत्पादन करने के लिए 75 लाख रु. तक की पूंजी विनियोजित करके 11 मजदूर से 50 मजदूर तक किराये पर रखकर कार्य सम्पन्न कराया जाता है।
कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्यामुक्त करने के उपाय
(1) वित्त की व्यवस्था (Arrangement of Finance)- कुटीर एवं लघु उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था हेतु विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ जैसे-व्यापारिक बैंक व राज्य वित्त निगम आदि स्थापित होने चाहिए। जो सरलता से ऐसे उद्योगों को ऋण प्रदान करें। इसी प्रकार कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए बैंक को ब्याज की दर भी कम होनी चाहिए, जिससे लघु उद्यमी भी तरलता अधिमान (Liquidity Preference) दे सके।
( 2 ) कच्चे माल की उपलब्धता (Availiability of Raw Materials) – कच्चा माल सुगमता से लघु उद्यमियों को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अतः कच्चे माल की आपूर्ति लघु उद्यमियों को सरलता से हो। इस हेतु सहकारी गठित होनी चाहिए, जो सामान्य वस्तुओं से सम्बन्धित इकाइयों के कच्चे माल को उपलब्ध करायें।
(3 ) तकनीकी सहायता (Technical Assistance)- तकनीकी सहायता से उद्यम की उत्पादन-कुशलता में वृद्धि एवं उत्पादन लागत कम होती है। नवीन वस्तुओं का उत्पादन भी तकनीकी सहायता पर निर्भर है। यह तकनीकी सहायता सरकार को लघु उपकरण, यंत्र, विद्युत चालित मशीनों के रूप में कम कीमत पर उपलब्ध करानी चाहिए।
( 4 ) बड़े एवं लघु उद्योगों की आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाए (Mutual Rivalry of Large and Small Industries should be Eliminated)- सरकार का दायित्व है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का बाजार सुरक्षित किया जाये, जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ नहीं विक्रय होनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि बड़े उद्योगों के पूरक या सहायक उद्योगों के रूप में इकाइयों को विकसित किया जाये, जिससे बड़े उद्योग प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसी इकाइयों पर निर्भर हो जायें।
(5) करो में छूट (Rebate in Taxes)- चूंकि लघु इकाइयों के उत्पादक कर भार को वस्तुओं की कीमत पर विवर्तित नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुटीर एवं लघु उद्योगों को शैशवावस्था में कर मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन लाभ में चलने वाली इकाइयों पर न्यूनतम कर भी लगाये जा सकते हैं।
( 6 ) विपणन सुविधाएँ (Marketing Facilities)- सरकार को विपणन व्यवस्था हेतु कुछ ऐसे बाजार निर्मित करने चाहिए जहाँ ऐसे उद्योगों का माल विक्रय हो। इसके अलावा सरकार केन्द्रीय विपणन संस्था की स्थापना करे, जो ऐसे उद्यमियों से प्रत्यक्ष रूप में माल खरीदे और निर्यात की व्यवस्था करें। यदि सम्भव हो तो ऐसे उद्योगों को सस्ते परिवहन की सुविधा भी समीचीन है।
( 7 ) उद्योगों में प्रमापीकरण व्यवस्था लागू हो (Standardisation System should be Imposed upon the Industries) – सरकार को उन्नत किस्म, वस्तु का आकार एवं गुणवत्ता की दृष्टि से प्रमापीकरण के अन्तर्गत नमूना या ट्रेडमार्क प्रयोग करना चाहिए, जिससे कुछ उद्योग परिष्कृत हो सकें । यह व्यवस्था प्रारम्भ में दस्तकारी वस्तुओं, खेलकूद के सामान व लघु इंजीनियरिंग से प्रारम्भ होनी चाहिए।
( 8 ) निःशुल्क लाइसेंस (Free Licensing)- कुटीर एवं लघु उद्योगों को निःशुल्क लाइसेंस देना आवश्यक है, क्योंकि लघु उद्यम स्थापित करते समय उद्यमियों को सर्वप्रथम लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया सरल नहीं है।
( 9 ) प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन- ऐसे उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए पृथक प्रदर्शनियाँ एवं मेलों का आयोजन किया जाए।
( 10 ) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं प्रशिक्षण (Establishment of Research Centers and Training)- इन उद्योगों का विकास करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित होने चाहिए, जो न्यूनतम लागत पर परिष्कृत एवं उच्च कोटि की वस्तुएँ उत्पादित कराने में उद्यमी का सहयोग करें। इसी प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था के अभाव में अकुशल श्रमिक ही उन्हें उपलब्ध हो पाते हैं। अतः सरकार को ‘ट्रेनिंग सेन्टर्स’ स्थापित करने चाहिए, जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करें।
