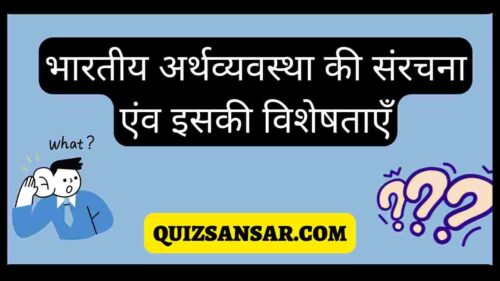
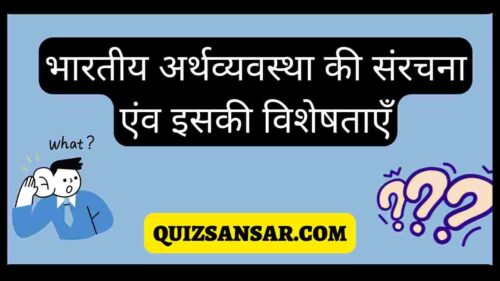
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एंव इसकी विशेषताएँ
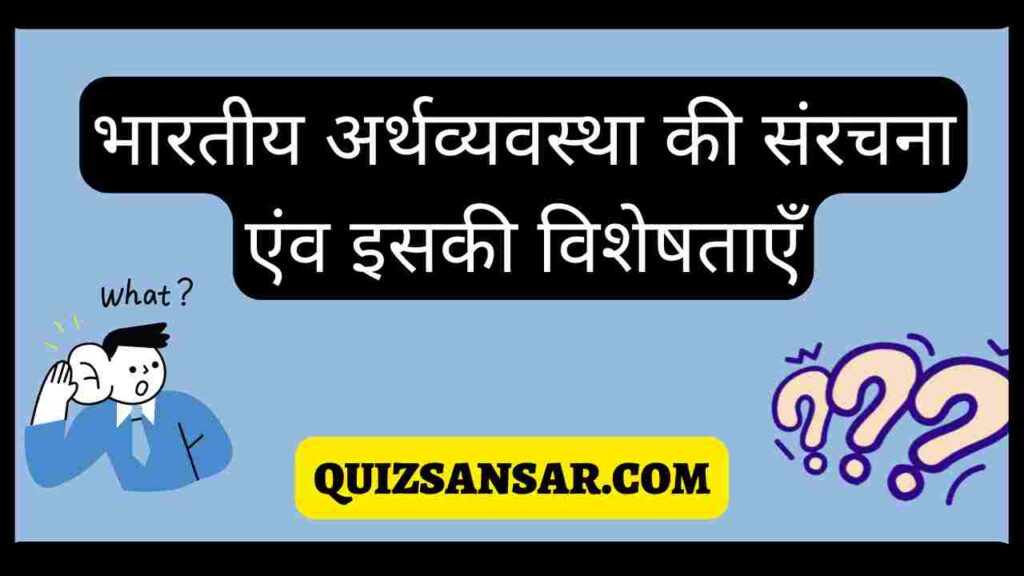
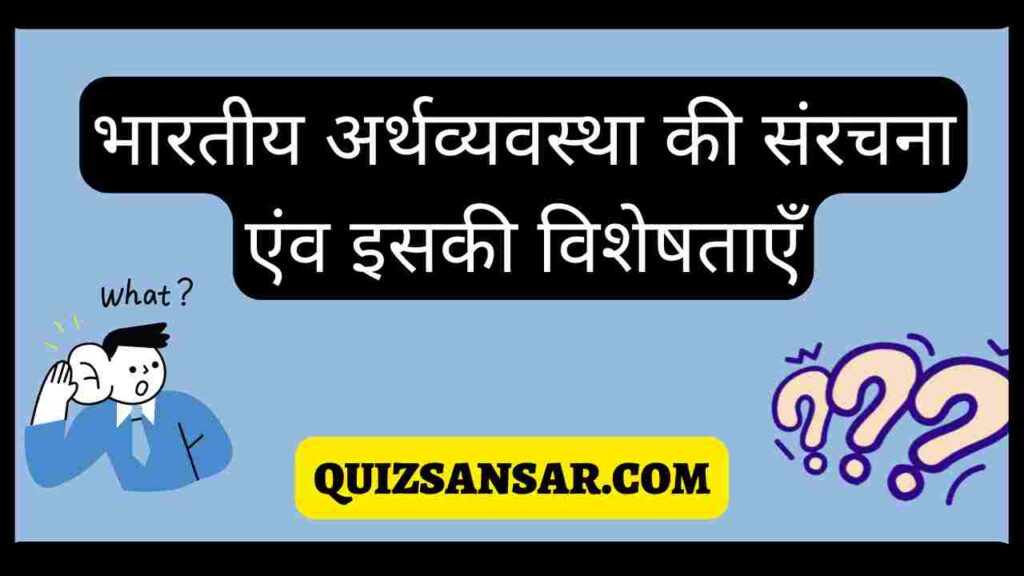
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की विवेचना कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है?
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना (Structure of Indian Economy)
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है-
- स्वामित्व के आधार पर
- व्यवसायों या क्रियाओं के आधार पर
- विकास के क्षेत्रों के अनुसार
1. स्वामित्व के आधार पर
भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है अतः इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है-
(i) सार्वजनिक क्षेत्र – मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और ये उद्यम सार्वजनिक उद्यम कहे जाते हैं। इस सार्वजनिक क्षेत्र में देश के महत्वपूर्ण बड़े उद्योग सम्मिलित होते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र का विकास- भारत की औद्योगिक नीति 1948 में अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण, अणुशक्ति निर्माण, रेलवे व डाक तार के विकास एवं स्थापना का पूरा दायित्व सरकार पर दिया गया। छः उद्योगों लोहा एवं इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, कोयला, खनिज, तेल, टेलीग्राम, टेलीफोन बेतार के उपकरणों का निर्माण इन सभी में विद्यमान इकाइयों को तो निजी क्षेत्र में रहने दिया, किन्तु नवीन इकाइयों की स्थापना राज्य के लिए सुरक्षित छोड़ दी गई। 18 उद्योगों के नियमन एवं नियंत्रण की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार 1956 की औद्योगिक नीति में 17 उद्योगों का विकास दायित्व सरकार पर रखा गया। 12 उद्योगों की स्थापना का अधिकार राज्य को दिया गया। शेष उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए। किन्तु औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सीमित कर दी गई और निजी क्षेत्र का बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। देश का वर्तमान औद्योगिक एवं आर्थिक ढाँचा काफी हद तक इन सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका का ही परिणाम है जिसे सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियाँ कहा जा सकता है। जैसे- पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्रों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में योगदान, निर्यात वृद्धि, लघु एवं सहायक, उद्योगों के विकास, आत्मनिर्भरता प्राप्ति में सहायक, आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगों का विकास।
(ii) निजी क्षेत्र – निजी क्षेत्र से अभिप्राय उन संस्थाओं से है जिनका स्वामित्व सरकार का नहीं है और जो जनता को वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करती हैं।
निजी क्षेत्र का विकास- भारत में 1948 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित थी। उस पर अनेक प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। इसी प्रकार 1956 की औद्योगिक नीति में भी, निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध थे। मोटे तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं को ही निजी क्षेत्र के लिए खोला था। यही नहीं, औद्योगिक विकास एवं नियमन, 1951 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र पर नियन्त्रण एवं नियमन की भी व्यवस्था थी। निजी क्षेत्र को नवीन कारखाने खोलने के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता था। इसी प्रकार अनेक वस्तुओं के उत्पादन के प्रारम्भ के लिए भी सरकार की अनुमति आवश्यक थी जिससे आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो जाए। इस प्रकार इन प्रतिबन्धों के कारण निजी क्षेत्र अपना विकास उचित प्रकार से न कर सका, किन्तु फिर भी इस क्षेत्र ने अच्छा विकास किया क्योंकि बाद में यह सोचा गया कि निजी क्षेत्र को प्रतिबन्धों से मुक्त कर उसे प्रोत्साहन दिया जाए। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्धों को ढीला करने का दौर आरम्भ हुआ और 1991 की नीति में निजी क्षेत्र को प्रायः नियन्त्रण से मुक्त कर दिया। इससे निजी क्षेत्र में रोजगार, पूँजी, कारखानों आदि में वृद्धि हुई।
क्रियाओं के आधार पर
(i) प्राथमिक क्षेत्र – अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कमी होती गई है। इसका प्रमुख कारण देश का विकासशील होना है।
(ii) द्वितीयक क्षेत्र – द्वितीयक क्षेत्र के दो प्रमुख भाग हैं-विनिर्माण और निर्माण 1950-51 में विनिर्माण का भाग GDP का 8.9 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार निर्माण का भाग 1950-51 में 4.1 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गया।
(iii) तृतीयक क्षेत्र – तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ शामिल की जाती हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ तृतीयक क्षेत्र का विकास भी बढ़ता गया ।
विकास के क्षेत्रों के आधार पर
(i) शहरी क्षेत्र – आर्थिक विकास की भिन्नता के कारण देश पर की अर्थव्यवस्था दो भागों में विभाजित हो गई है। एक तो शहरी अर्थव्यवस्था जो कि जटिल है तथा स्वावलम्बी नहीं है। यहाँ विनिमय का मुख्य साधन मुद्रा है। यहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ असीमित तथा विस्तृत होती हैं तथा उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होता है। शहरों का आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। यहाँ व्यापार, बैकिंग, शिक्षा तथा परिवहन आदि की सुविधाएँ विस्तृत होती हैं।
(ii) ग्रामीण क्षेत्र – ग्रामीण क्षेत्र में भारत की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएँ सीमित होती हैं, यहाँ उत्पादन छोटे पैमाने पर तथा परम्परागत, पुरानी विधियों से किया जाता है। यहाँ जीविका का मुख्य साधन कृषि है। यहाँ बैकिंग, व्यापार, परिवहन तथा शिक्षा आदि की सुविधाएँ भी कम पायी जाती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को अग्र भागों में बाँटा जा सकता है-
(i) परम्परागत विशेषताएं या अल्प-विकसित राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषताएँ (Traditional Characteristics)
अल्प-विकसित राष्ट्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
1. निर्बल आर्थिक संगठन – भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता निर्बल आर्थिक संगठन है। इसमें बचत सुविधाओं का कम होना, ग्रामों में जमींदारों और साहूकारों का कार्य करना, विनियोग क्षेत्र की पूरी जानकारी न होना तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए उचित दर पर और उचित मात्रा में वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की कम संख्या का होना सम्मिलित है।
2. पूँजी निर्माण की नीची दर – भारत एक गरीब राष्ट्र है, अतः पूँजी निर्माण एवं विनियोजन की गति भी बहुत धीमी है। पिछले कुछ वर्षों में नियोजन होने के कारण बचत व विनियोग दरों में कुछ वृद्धि हुई है।
3. आर्थिक विषमता – भारतीय अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति एवं आय के वितरण में काफी-विषमता है। NCAER सर्वेक्षण के अनुसार देश में उच्च स्तर के केवल 1 प्रतिशत व्यक्ति कुल आय का 14 प्रतिशत भाग प्राप्त कर लेते हैं जबकि नीचे स्तर के 50 प्रतिशत व्यक्तियों को कुल आय का केवल 7 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।
4. तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर – स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी भारत में तकनीकी शिक्षा अनुसंधान एवं विकास आदि की सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है जिसके कारण तकनीकी ज्ञान का स्तर निम्न है।
5. कृषि की प्रधानता – भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या का 65 से 70 प्रतिशत भाग कृषि व्यवसाय में संलग्न है, शेष आबादी उद्योग व सेवाओं में कार्यरत है, जबकि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान केवल 32.75 प्रतिशत है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 40 प्रतिशत निर्यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पदार्थों का होता है।
6. प्रति व्यक्ति निम्न आय – भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है। वर्ष 2016 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 630 डॉलर है। जबकि भारत की तुलना में अमेरिका, जापान व यू.के. की प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः 72, 65 व 53 गुना अधिक है।
7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था – स्वतन्त्रता के पश्चात् शहरों व शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है फिर भी देश की अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान है। वर्तमान में कुल जनसंख्या की 72.2 है प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 27.8 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है। इसके विपरीत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में ग्रामीण जनसंख्या क्रमश: 26%, 20% और 8% है।
8. जनसंख्या का अधिक भार-भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्वतन्त्रता के पश्चात् जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। स्वतन्त्रता के समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी जो 1994 की जनगणना के अनुसार बढ़कर लगभग 84.4 करोड हो गयी। 11 ई, 2000 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो गयी तथा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। भारत की जनसंख्या के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत के पास विश्व के कुल स्थान क्षेत्र का 2.42 प्रतिशत भाग है, जबकि सम्पूर्ण विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है।
9. व्यापक बेरोजगारी- बेरोजगारी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता बन गयी है। यह बेरोजगारी न केवल अशिक्षित बल्कि शिक्षित व्यक्तियों में भी है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2025 के अन्त तक 27 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होंगे और इसमें प्रतिवर्ष 60 लाख व्यक्तियों की और वृद्धि हो जायेगी। व्यापक बेरोजगारी के साथ-साथ यहाँ पर अर्द्ध-रोजगार भी पाया जाता है अर्थात् कुछ मसय के लिए लोगों को रोजागर मिलता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत एक अल्प विकसित राष्ट्र है।
(ii)अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां या विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषताएं (New Trends in Indian Economy)
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिससे कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं, नवीन उद्योग स्थापित हुए हैं, उत्पादन विधि में आधुनिक तकनीक का समावेश हुआ है, सामाजिक चिन्तन में परिवर्तन हुआ है जिसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई है और अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में निम्न नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं-
1. शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार – देश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सन् 1950-51 में प्रारइमरी मिडिल स्कूलों की संख्या 2.31 लाख थी जो सन् 2002-03 में बढ़कर 6.51 लाख हो गयी है। इस अवधि में विश्वविद्यालय एवं उसके समान संस्थाओं की संख्या भी 28 से बढ़कर 306 हो गयी है। देश में साक्षरता की दर 1941 में 16.61 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 67 प्रतिशत हो गयी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है।
2. आधारभूत संरचना का विस्तान देश में परिवहन, संचार एवं शक्ति इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। देश में 1947 में मात्र 1,400 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता थी, जो कि 2016 के अन्त तक बढ़कर एक लाख सत्तर हजार मेगावाट हो गयी। इस अवधि में रेलवे लाइनों की लम्बाई 53,596 किलोमीटर से बढ़कर 95,285 किलोमीटर तथा तसह वाली सड़कों की लम्बाई 1.57 लाख किलोमीटर से बढ़कर 50 लाख किलोमीटर हो गयी।
3. बचत और पूँजी निर्माण में वृद्धि भारत में बचत एवं पूँजी निर्माण की दर में निरन्तर प्रगति हुई। सन् 1950-51 में राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत भाग ही बचाया गया था तथा पूजी निर्माण दर 68 प्रतिशत थी जो 2015-16 में सकल बचत दर 45.5 प्रतिशत तथा सकल घरेलू पूँजी निर्माण दर 38.7 प्रतिशत रही।
4. राष्ट्रीय आय में वृद्धि – यह सत्य है कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय आज भी भारत में कम है किन्तु सत्य यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति, आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
5. उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि योजना – अवधि में कुछ अल्पकालीय उच्चावचनां को छोड़कर देश के उत्पादन में निरन्तर प्रगति हुई है। प्रथम योजना में विकास दर 3.6 थी जो आठवीं योजना में बढ़कर 6 प्रतिशत हो गयी एवं नवीं योजना में यह 7 प्रतिशत तथा 12वीं योजना में 8 प्रतिशत तक पहुँची है। इसी प्रकार कृषि उत्पादन में प्रगति दर प्रथम योजना में 4.1 थी जो आठवीं योजना में बढ़कर 5 प्रतिशत तथा नवीं योजना में 7 प्रतिशत एवं 12वीं योजना में 8 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 6. बैकिंग सुविधाओं का विकास-भारत में बैकिंग सुविधाओं में भी निरन्तर प्रगति हुई है। जून, 1969 में व्यापारिक बैंकों की 8,262 शाखाएँ थीं जो 2015 में बढ़कर 75000 हो गयी। जून, 1969 में 65,000 व्यक्तियों पर एक बैंक था जबकि 2015-16 में 12,000 व्यक्तियों पर एक बैंक है।
7. कृषि का आधुनिकीकरण – भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है। सिंचाई के साधनों का समुचित विकास हुआ | उन्नत बीज एवं खाद कृषकों को उपलब्ध करवाया गया है तथा भूमि है। सुधार कार्यक्रम को वृद्ध स्तर पर लागू किया गया है। कृषि वित्त एवं विपणन व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। इन सभी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हम खाद्यानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गये हैं।
